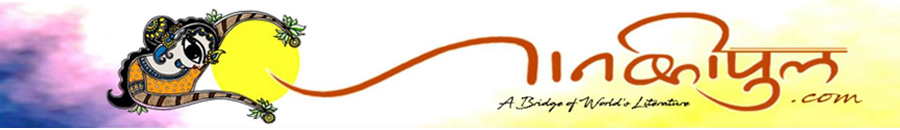रज़ा न्यास द्वारा आयोजित दो दिवसीय आयोजन ‘युवा’ की यह रपट लिखी है जानकी पुल की युवा संपादक अनुरंजनी ने-
==================
18 फरवरी को कृष्णा सोबती का जन्मशती पूरा हुआ। इस अवसर पर रज़ा न्यास द्वारा दिनांक 19-20 फरवरी को उन पर एकाग्र दो दिवसीय कार्यक्रम हुआ – ‘युवा-2025’, जिसमें विभिन्न विषयों पर कुल 9 सत्र हुए। यह ‘युवा’ का सातवाँ आयोजन था। जो इस आयोजन की रूपरेखा से परिचित हैं वे जानते हैं कि हर सत्र में युवा लेखकों के वक्तव्यों के बाद एक वरिष्ठ लेखक उन पर टिप्पणी करते हैं। ज़ाहिर है इस बार भी यह होना था।
कई मायनों में यह आयोजन सफ़ल रहा। एक तो यही कि किसी भी एक लेखक पर कई लोगों को बोलना-सुनना अपने आप में चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ऐसे में ऊब होने की बहुत संभावनाएँ होती हैं लेकिन इस बार यह उबाऊपन न्यूनतम महसूस हुआ। अधिकता रही तो रोचकता की ही, सुनने की ही, और यह तभी संभव हो सकता था जब वक्ता निर्धारित विषय पर पढ़ कर आए हों, तैयारी के साथ आए हों।
एक सत्र था ‘कृष्णा सोबती और हिन्दी आलोचना’। सामान्यतः इसका अर्थ यह लिया जा सकता है कि हिन्दी के आलोचना संसार ने कृष्णा सोबती के लेखन को कैसे, कितना, किस रूप में दर्ज़ किया है? लेकिन यह सत्र आश्चर्यजनक तरीके से रोचक हो उठा कि पाँच वक्ताओं में से चार ने इस पर बात की कि हिंदी आलोचना में कृष्णा सोबती कहाँ हैं? वे स्वयं आलोचना के क्षेत्र में क्या कर रही हैं? इस पर विचार करते हुए मुख्यतः उनके संस्मरणात्मक लेखन के आधार पर ही उनके आलोचक रूप को सामने लाने का प्रयास किया गया जो कि निश्चित ही, बेहद रोचक लगा।
रचना में जो लिखा जा रहा है वह पात्र की बात है या लेखक की, यह एक ऐसा जटिल सवाल है जिसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिलता। एक सत्र कृष्णा सोबती की भाषा पर भी था जिसमें यह जटिलता व उलझन ज्यों कि त्यों बनी रही कि कह कौन रहा है? क्योंकि एक ही रचनाकार अपनी रचना में जातिसूचक शब्द/गालियों का भी इस्तेमाल कर रही हैं और वही जाति व्यवस्था के खिलाफ भी लिख रही हैं।
इसी से मिलता-जुलता सवाल ‘लेखकीय दृष्टि और औपन्यासिक दृष्टि के अंतर्द्वंद्व’ से संबंधित भी है जिसकी चर्चा भी बखूबी हुई, जिसमें उनके यहाँ इस अंतर्द्वंद्व को ढूँढने और उसके कारण तलाशने के प्रयास नज़र आए।
उनके यहाँ स्त्री जिजीविषा कितने स्तरों पर उपस्थित हैं, यह भी एक सत्र में बातचीत का विषय था। अमूमन सोबती के रचना संसार में ‘स्त्री संघर्ष, स्त्री यौनिकता की उपस्थिति, इस तरह के ‘टर्म’ के सहारे बातचीत होती है जो कि ज़्यादा सरल लगते हैं। लेकिन ‘जिजीविषा के रूपक: स्वाधीन स्त्री की उपस्थिति’ इस एक विषय में संघर्ष के विभिन्न पहलुओं को समाहित करना, ज़्यादा चुनौतीपूर्ण लगा।
इस तरह के सवाल भी निरंतर केंद्र में रहे कि ‘वे अपने को स्त्रीवादी लेखक नहीं मानती थीं’, ‘आज उन्हें उस खाँचे में बांधकर माना जाना चाहिए कि नहीं’। इस बातचीत में तमाम असहमतियाँ भी थीं, किसी के लिए वे स्त्रीवादी लेखक हैं तो किसी ने उन्हें स्त्रीवादी मानने से मना कर दिया। कृष्णा सोबती किसी के लिए अभिजात्य वर्ग की लेखिका हैं तो किसी के लिए पुरखिन। और जैसे ही हम पुरखिन कहते हैं वैसे ही दिमाग़ में जो सबसे पहली छवि बनती है, वह आमलोगों के बीच की स्त्री की बनती है, न कि अभिजात्य स्त्री की!
बाक़ी सत्र भी महत्त्वपूर्ण तो लगे ही, जिसमें पर्यवेक्षक से कई सारे सुझाव भी मिले, मसलन – “लेखक को सिर्फ़ लेखक नहीं, बल्कि लेखक नागरिक होने की ज़रूरत है”, “लेखक को अति भावुकता से बचना चाहिए, इससे हमारे देश में जो हासिल है उसकी अस्वीकृति का भान होता है”, “लेखकों को आलोचना के क्षेत्र में नयापन करने की ज़रूरत है”, “इस पर सोचने की ज़रूरत कि क्या भारत को समझने के लिए विभाजन एक अनिवार्य बिन्दु है?”
इन सुझावों और कुछ सवालों के अतिरिक्त इस ओर भी ध्यान दिलाया गया कि आखिर ऐसा क्यों है कि “हिंदू जन्माष्टमी पर ऐसी कविताएँ चुन कर लगा सकता है जिसकी रचना मुस्लिम रचनाकारों ने की है, लेकिन क्या वे ऐसा कर सकते हैं? क्या उन्हें कोई ऐसी कविता/ रचना मिलेगी जिसका लेखक हिंदू हो और उसने मुसलमानों के त्योहारों/त्योहार पर कुछ रचनात्मक लिखा हो?” यह सवाल हम सभी को सोचना चाहिए, और यदि हम इससे व्यथित नहीं होते हैं तो हमारा देशप्रेम खोखला है।
इन सबके अलावा एक खास बात यह भी लगी कि एक रचनाकार के साथ और रचनाकारों को पढ़ने के अभ्यास से क्या होता है? यक़ीनन हम उनमें तुलना के ‘मोड’ में चले जाते हैं और कुछ समान, असमान बिंदुओं को एक-साथ रख कर उस पर विचार करते हैं। इस दो दिवसीय आयोजन में दो सत्र ऐसे भी थे, जिसने निर्धारित वक्ताओं को कृष्णा सोबती के साथ अन्य लेखकों को भी पढ़ने का मौका दिया। (‘कृष्णा – वैद – निर्मल: गल्प और यथार्थ’, कृष्णा सोबती इस्मत चुग़ताई महाश्वेता देवी)
इन सबके बाद समापन वक्तव्य में अशोक वाजपेयी जी के सुझावों पर सोचने, फिर यदि ठीक लगे तो अंगिकार करने की ज़रूरत है, जिनमें से कुछ हैं – “आत्मरति से बचना, आत्मालोचन करना, सवाल करना, लेखक नागरिक होना।”
अंत में अशोक वाजपेयी की एक और बात जो दर्ज़ होना ज़रूरी लगती है वह यह कि “इस युवा में स्त्रियों ने पुरुषों को पछाड़ दिया।” हालाँकि ऐसा नहीं है पुरुष वक्ताओं में प्रत्येक से उन्हें निराशा मिली, जिसका उल्लेख उन्होंने किया भी, उसी तरह यह भी ज़रूरी नहीं कि सभी स्त्री वक्ताओं से निराशा नहीं मिली होगी। दोनों ही स्थितियों में, हम सब को ही यह सीख ही मिलती है कि हम निरन्तर अभ्यास करते रहें, अपने अध्ययन का विस्तार करते रहें।
एक बात, जिसके बिना यह लिखा अधूरा लगेगा, वह यह कि सभी प्रतिभागियों के लिए कहना ज़रूरी लगता है कि उन्हें सभी सत्रों में, दोनों दिन अपनी उपस्थिति बनायी रखनी चाहिए थी।