हाल ही में प्रीति जायसवाल का पहला काव्य संग्रह ‘काँच की गेंद में सपने’ प्रकाशित हुआ है। इस किताब की समीक्षा की है प्रत्युष चन्द्र मिश्रा ने। यह समीक्षा इस किताब के बहाने स्त्री-लेखन पर भी बात करती है, आप भी पढ़ सकते हैं – अनुरंजनी
========================
काँच की गेंद में सपने:काँच की गेंद में बंद सपनों का विस्तृत आकाश
किताब आने की ख़ुशी घर में किसी नए सदस्य के आने की ख़ुशी की तरह होती है और यह किताब यदि कविता की हो तो बात ही क्या! पिछले दिनों प्रीति जायसवाल की किताब ‘काँच की गेंद में सपने’ अनन्य प्रकाशन से छप कर हिंदी के बृहत्तर पाठक समुदाय के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कर चुकी है। स्वागत, शुभकामना, बधाई की औपचारिकताओं से परे हटकर मेरी इच्छा थी कि पहले किताब पढ़ ली जाए. किताब में जीवन और समय-समाज की जो अनुगूंजें हैं उन्हें सुना जाए और फिर यदि आवश्यक हो तो उसपर बात की जाए। जैसा कि लेखिका ने अपने आत्मकथ्य में लिखा भी है कि ‘मेरा लिखना प्रयास है दुनिया सुन्दर बनाने का।’ कला का यही तो काम है- दुनिया सुन्दर बनाने की सदिच्छा से भरे रहना। कला यदि समय और समाज की विद्रूपताओं को रेखांकित करती है तो उसके मूल में भी यही बात छिपी रहती है। प्रीति की कविताओं से मेरा परिचय इस किताब को पढने के पूर्व से था। अपनी जिद और अपनी आकांक्षा में वह मनुष्य बने रहने की तमाम जद्दोजहद से गहरे जुड़ी रही हैं। वह स्त्री होने को कविता में अतिरिक्त छूट लेने की तरह नहीं बरतती हैं जैसा कि स्त्री लेखन का बहुलांश करता रहा है। स्त्री-अस्मिता की उनकी समझ निजी अनुभव से जुड़े होने के बावजूद व्यापक मानवीय चिंताओं से गहरे नाभिनालबद्ध है। जाहिर है प्रीति आत्ममुग्धता और आत्मप्रशंसा से बचते हुए अपने कवि-कर्म को जोखिम की हद तक ले आती हैं। इस संग्रह को पढ़ते हुए मुझे एक आतंरिक ख़ुशी इस कारण भी हुई कि इस संग्रह में स्त्री-जीवन के कई ऐसे पहलुओं का भी विस्तृत ब्यौरा है जिन्हें विमर्शों की दुनिया घरेलूपन कह कर दरकिनार कर देती है। घरेलू जीवन के कई अनछुए संदर्भो को अपनी कविताओं का विषय बनाती प्रीति वैचारिक और भावात्मक, दोनों दृष्टियों से सबल दिखती हैं। देखा जाए तो जब भी हिंदी की किसी स्त्री कवि की रचना सामने आती हैं तो पाठकों के ज़हन में स्त्री-कविता की एक सुदीर्घ परम्परा और उस परम्परा से छन कर आनेवाली मुक्ति की आकांक्षा भी कविता में अनायास चली आती है। यह अकारण नहीं कि थेरीगाथा, मीरां, अक्क महादेवी के साथ ही महादेवी वर्मा, सविता सिंह, अनामिका, गगन गिल, निलेश रघुवंशी, रूपम मिश्र, अनुपम सिंह तक की आवाज़ हमारे सामने अनायास गूँजने लगती हैं। यह सूची और विस्तृत हो सकती है पर इन पंक्तियों के लेखक के अध्ययन और ज्ञान की सीमा एक साथ सामने आ जाती है। कोई भी कला किसी नारे या वाद की मुहताज नहीं रहती परन्तु इसके मूल में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का मानवीय पहलू अनिवार्यतया समाहित रहता है। कला की हर आवाज़ अन्याय और शोषण का प्रतिकार है। आदिकवि वाल्मीकि से बढ़कर इस बात को भला और कौन बेहतर समझा सकता है कि ‘कविता जन्मना प्रतिपक्ष है’। प्रीति के इस पहले काव्य संग्रह को पढने के बाद यह सारे सवाल एक साथ कौंधने लगे। संग्रह की छप्पन कविताओं से गुजरते हुए एक युवा स्त्री की बेचैनी, दृढ़ता, नाराजगी और चीजों से उसके गहरे लगाव को महसूस किया जा सकता है। यह संग्रह ‘कुछ नहीं’ और ‘सब कुछ’ की पीड़ा को एक साथ हमारे सामने रख देता है।
प्रीति के यहाँ चीजों के बनने की शुरुआत ‘ढहने’ से होती है। प्रीति कहती हैं ‘बनने के लिए/ ढहना पड़ता है/बार-बार(व्यामोह)। रंग-अनुभव को लेकर प्रीति के यहाँ कई कविताएँ हैं। संग्रह की शीर्षक कविता ‘काँच की गेंद में सपने’ में निर्देशक कलाकार से वह सब कुछ करवा रहा है जो उसे अपने रंगमंच के लिए चाहिए। ’ध्यान’, ‘ओंकार’, ‘समाधि’ के माध्यम से निर्देशक कलाकार के भीतर अभिनय के रंग को सामने लाना चाहता है ताकि कलाकार जिन्दा किरदार अपने अन्दर भर सके.यहाँ कविता एकाएक रंग अनुभव को जीवनानुभव में तब्दील करती दिखती है। इसी तरह प्रीति की कविता ‘ओ निर्देशक’ में कवि निर्देशक से ‘नेपथ्य के एकांत संगीत में बहना कब सिखलाओगे?’ का विस्मित करता सा सवाल करती है। जीवन में नेपथ्य का एकांत संगीत कहाँ मिलता है सबको? या तो नेपथ्य या फिर भीड़ का संगीत! मगर जब ये दोनों आपके जीवन में हों तो इससे सुखकर और क्या होगा भला! इसी तरह ‘सुनो निर्देशक’ कविता में वे कहती हैं कि ‘धब्बेदार मन का/असुंदर टुकड़ा/ कैसे छुपाकर रख दूँ/कि शर्म,हया, संकोच,डर/के सिपहसालार/खड़े/चप्पे-चप्पे। प्रीति अक्सर कम शब्दों में अपनी बात कहती हैं। छोटे-छोटे वाक्यों के साथ अपनी स्मृति और अपने अनुभव का सहारा लेकर वे अपने बिम्ब खड़े करती हैं। प्रीति की एक कविता है ‘कलाकार’। जब वे कहती हैं- ‘पेट के पास/अद्भुत ताकत है!सब कुछ करवाने की/आदमी को सूअर,कुत्ता,केंचुआ,भालू,बन्दर/कुछ भी बना सकने की’ और इसी क्रम में आगे कहती हैं ‘कठपुतलियों की डोर/खुदा के हाथ नहीं/पेट के पास है’। पापी पेट का सवाल यहाँ मुखरता से बोलता है। इसी तरह की एक और कविता है ‘कागजात हो गये रद्दी’। इस कविता में प्रीति कहती हैं कि जैसे दराज में रद्दी कागज़, जंग खाई पेपर पिंस और छोटे-बड़े पत्थर रखे हैं इसी तरह मन में दबी पड़ी हैं तमाम बातें। यह कविता अपने गठन में मानव जीवन की अनेक विडम्बनाओं का दस्तावेज लगती है। इस संग्रह की एक और बेहतरीन कविता है ‘गुस्सा’, जहाँ परीक्षा कक्ष में चपरासी कक्ष-पर्यवेक्षक की कुर्सियों के नीचे पुरानी अनुक्रमांक स्लिपों को फेंक कर अपने गुस्से का इजहार करता है। संग्रह की एक कविता है ‘खेती’। इस कविता में प्रीति ने गाँधी को नुमाइश और संग्रहालयों की चीज बना देने पर जबरदस्त व्यंग्य किया है। सचमुच इस देश में गाँधी और उस दौर में अर्जित मूल्य अब सिर्फ प्रदर्शन की विषयवस्तु हो गये हैं। वे नारों में हैं, किताबों में हैं, संग्रहालयों में हैं, फैशन में हैं बस आचरण में नहीं हैं। और जिन्होंने ऐसा किया है वे इस शस्य-श्यामला-धरा को छुट्टे सांड की तरह चर रहे हैं। यही तथ्य उनकी कविता ‘गाँधी जी का विग’ में भी दिखाई पड़ता है।
प्रीति की नजर अपने आस-पास की चीजों पर गहराई से पड़ती है। वे सिर्फ इनपर चलताऊ टिप्पणियाँ भर नहीं करतीं बल्कि उस विडंबना को भी उजागर करते चलती हैं जिसके चलते इन चीजों का बोध हमारे भीतर धुंधला होता जाता है। हर कवि में यदि वह सच्चा है तो उसका परिवेश चाहे-अनचाहे उसकी रचनाओं में आ ही जाता है। प्रीती ठेठ बनारसी हैं। ज़ाहिर है उनकी कविताओं में बनारस का ‘लोक’ जम कर बोलता है। इस शहर के बारे में बात करते हुए वे कहती हैं कि ‘बनारस शहर नहीं तासीर है’, यह ‘गलियों का शहर है’, न केवल गलियों का वरन गालियों का भी। जाहिर है बनारस का नक्शा सिर्फ मंदिरों, घाटों, गंगा, लंका, बीएचयू, दालमंडी, कैंट, रामनगर से ही नहीं बनता बल्कि संगीत, कला, बोली-बानी और यहाँ के लोक के बीच पैबस्त ‘मधुर मनोहर अतीव सुंदर’ होने से बनता है। अपने किसी अनाम दोस्त को संबोधित करते हुए वे कहती हैं-बीत जाने के बाद सारा दिन/रात सपने में/तुम्हें छुवेगा बनारस/करेगा बात/सारी रात/सुबह होने तक/कहोगे उससे तुम/इक बात/दो बात /बात-दर-बात/बेपर्दे/वो सारी बात तहाकर/रख लेगा/अपने पास/तुम्हें पता न चलेगा/जाने कब/तुम्हारा राजदां/हमराह/बन जायेगा बनारस/जहाँ भी जाओगे/मेरे दोस्त! तुम्हारे साथ वही/जाएगा बनारस। इस कविता की ‘इंटेंसिटी’ को बनारस से किसी भी रूप में जुड़ा हर व्यक्ति महसूस कर सकता है।
संग्रह की एक कविता है-‘सीता की रसोई’। इस कविता में एक कामकाजी स्त्री के घर-बाहर की चकरघिन्नी में पिसते जाने और पुरुष उपेक्षा के दंश को मार्मिक अभिव्यक्ति मिली है। सच ही तो है स्त्रियाँ काम से लौटकर काम पर ही लौटती हैं। इस कविता की बुनावट में प्रीति अद्भुत कल्पनाशीलता का सहारा लेती हैं। सीता और राम के संदर्भों से जुड़कर इस कविता के बारे में कहा जा सकता है कि ‘सिर्फ घर से नहीं चल सकता काम/सिर्फ बाहर से नहीं चल सकता काम/सिर्फ काम से नहीं चल सकता काम’।
प्रीति के इस संग्रह में प्रेम कविताएँ भी हैं. ‘प्रेम में’ कविता में वे कहती हैं-‘उगा सूरज/आसमान के बीच माथे/कह रहा/चिड़ियों ने चहक कर/भरी हामी/हुंकार भर रही चीटियाँ/कतार में जाती/ताड़ के मस्तक पर बैठा कागा/सुना रहा बात चार/चटके हुए हींग की सुवास फैली/धनिया हो रही कुछ और धानी/दाल पर बिछकर/तो चलो मान लूँ/प्रेम में हूँ मैं/प्रेम में ही तो/सुन्दर हो सकता है/सब कुछ/सुन्दर सजीला/ प्रेम सिखाता है/सुन्दर दिखना/सुन्दर देख लेना’। यदि आप प्रेम में हैं तो जरुर कुछ सुन्दर आपको दिखेगा। न केवल लोग बल्कि यह दुनिया भी। स्त्री कवियों की कई प्रेम कविताओं से गुजरने के बाद इस कविता को पढ़कर एक अजीब सुकून मिला। यह स्त्री जो प्रेम में है, जो सब कुछ सुंदर देख रही है उसके आसमान में सूरज उग आया है। क्या यह नहीं है कि कोई भी अच्छी प्रेम कविता स्त्री-पुरुष की बाइनरी से बाहर निकलकर पूरी कायनात से जुड़ जाती है।
प्रीति के इस संग्रह में पेड़ों-फूलों को लेकर कई कविताएँ हैं। यहाँ ‘अमलतास है,मोगरे के फूल हैं तो नीम भी है। एक स्त्री के घरेलू साजोसामान की हर रंगत को प्रीति ने अपनी कविताओं में ढाला है. ‘हल्दी’, ’नमक’ ‘बूंदी का रायता’, ‘तिलौरी’, ‘चौलाई’, ‘छीमियाँ’, ‘चकरी’, ‘सिल’, ‘ढोका नमक’ सबको वे अपनी कविताओं का विषय बनाती हैं। कह सकते हैं कि प्रीति अपने काव्य-कर्म के लिए जिन विषयों को उठाती हैं उनसे वे पूरी तरह परिचित हैं। ये सारे विषय उनके आस-पास के हैं। देखा जाए तो अपनी कविता के लिए वे बड़े विषयों का चुनाव नहीं करती बल्कि अधिकांश कविताओं में जीवन के छोटे-छोटे दृश्यों से बड़ी कविता संभव करती हैं। यहाँ उनकी सिल कविता का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता है. ’पिस डाला/धानी हरी इच्छाओं को/समय-सिल पर/दरकेचकर/तुम्हारे जायके के लिए/डाल दिया/नमक-मिर्च/भकभकाता रहा न जाने कब तक/मेरा हाथ/ये अलग बात!’ बिना किसी अतिरेक के यह कविता स्त्री-जीवन के कटु यथार्थ को हमारे सामने उधेड़कर रख देती है। इसी तरह की इनकी एक और कविता है-‘आकाश से’। इस कविता में स्त्री-पुरुष का द्वंद्व खुलकर सामने आता है जहाँ नैरेटर कहती है-‘छूट गये तुम/तो क्या करूं मैं?/ताकत भर ताकत लगाई तुमने/मेरे पंख नोचने में/काश!इसे भरते तुम मेरी उड़ान में।’ प्रीति यहीं नहीं रुकतीं। अपनी कविता ‘वजूद’ में वे जैसे समूची स्त्री जाति की आवाज बन जाती हैं। ‘बहुत प्यार में अघाकर/जब कोई मुझे/बेटा कहता है/तमाचा लगता है/पूरे वजूद पर मेरे/मुझे पसंद है/मेरा स्त्री होना/मुझे प्यार करने के लिए/प्यार करना होगा/मेरे स्त्री होने से’। वे एक साथ संबंधों में ‘नरमी और गरमी’ दोनों को बचाने की बात करती हैं। बहुत खूबसूरती से वे इस बात को रेखांकित करती हैं कि ‘अपने सूरज को/ ऐसा मत बनाओ कि/सिर्फ तुम्हारी ही बालकनी में/आये धूप/अपने सूरज को बताओ/सूरज सबका है।’ कला की चौहद्दी ‘फॉर ऑल’ से ‘फोर एवर’ तक ही तो है। यह तो हम हैं जो हर वक्त सीमांकन करते रहते हैं। अपने तयशुदा फीते लिए हुए। संग्रह की कई कविताओं में निजी जीवन की परतें हैं। कवि अपने जीवन को देखते हुए समाज और दुनिया को भी देखते चलती हैं। स्मृतियों का गुच्छा खुलता है और फिर वे झोले में मूरई और भंटे के साथ एक ‘बाल पत्रिका’ की भी जगह तलाशती हैं। ’चीनी का बोरा’, ’टट्टी’ ‘इन्द्रधनुष’ के साथ ही संग्रह की एकमात्र लम्बी कविता ‘मेरी फुटबॉल कहाँ है मम्मी’ तक आते-आते प्रीति की छवि एक ऐसी कवि के रूप में सामने आती है जो एक साथ अपने स्त्री होने को गरिमा और सौन्दर्य से आप्लावित करते चलती हैं। हाँ, यहाँ यह भी उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ रहा है कि घरेलू जीवन के कई प्रसंगों को कविता में दर्ज करते हुए प्रीति उसे कलात्मक ऊँचाई तक नहीं ले जा पाती हैं। कई बार उनके निजी अनुभव सामाजिक यथार्थ की अनुकृति भर बन कर रह जाते हैं। कहीं-कहीं तो महज निजी जीवन के ब्यौरे भर तक! खासकर ‘ढोका नमक’, ‘चौलाई’ और ‘छीमियाँ’ शीर्षक कविताओं को पढ़ते हुए पाठक इस बात को महसूस कर सकता है। मगर यहाँ इस बात को भी दर्ज किया जाना चाहिए कि यह प्रीति का पहला ही संग्रह है और इस संग्रह में अपने कवि होने को उन्होंने मजबूती से स्थापित किया है।
कह सकते हैं संघर्ष के साथ सृजन और ज्ञान के साथ संवेदना के इलाके उनकी कविताओं की जद में हैं। अपनी एक कविता में जब निर्मला पुतुल कहती हैं कि ‘तो फिर जानते क्या हो तुम/रसोई और बिस्तर के गणित से परे/एक स्त्री के बारे में?’ तो वे स्त्री जीवन के उन तमाम कोनों- अंतरों के बारे में भी दरियाफ्त कर रही होती हैं जिन्हें पुरुष समाज देखना भी नहीं चाहता। धार्मिक-सामाजिक रुढियों का पालन करती मरती-खपती स्त्रियाँ हमारे समाज में अब भी बहुतायत में हैं। सविता सिंह की ‘मैं किसकी औरत हूँ?’ का कथ्य आज भी एक सवाल की तरह हमारे सामने गूंजता रहता है। प्रीति की कविताओं को पढ़ते हुए यह कहा जा सकता है कि उनमें न केवल काव्य-परंपरा की गहरी समझ है बल्कि उन परम्परा की जकड़नों से निकलने की एक सचेत कोशिश भी है। प्रीति का यह संग्रह हिंदी की स्त्री-कविता से थोड़ा दूर और थोड़ा पास इसी रूप में है. उम्मीद की जानी चाहिए कि ‘कांच की गेंद में सपने’ की शुरुआत कवयित्री के लिए आकाश को अपने सपनों की जद में लेने से हो जैसाकि कई कविताओं में लक्षित भी किया जा सकता है.
परिचय–
नाम– प्रत्यूष चन्द्र मिश्रा
शिक्षा– एम.ए.,बीएड., पी-एच.डी.
सम्प्रति– सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, आयुक्त कार्यालय,मगध प्रमंडल गया
समीक्ष्य पुस्तक– कांच की गेंद में सपने
कवयित्री– प्रीति जायसवाल
प्रकाशक– अनन्य प्रकाशन, नई दिल्ली
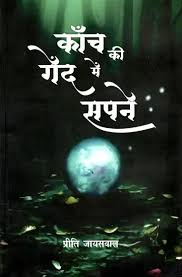
2 Comments
आपकी लिखी रचना ब्लॉग “पांच लिंकों का आनन्द” बुधवार 8 जनवरी 2025 को साझा की गयी है……. पाँच लिंकों का आनन्द पर आप भी आइएगा….धन्यवाद!
अथ स्वागतम शुभ स्वागतम।
सुन्दर समीक्षा