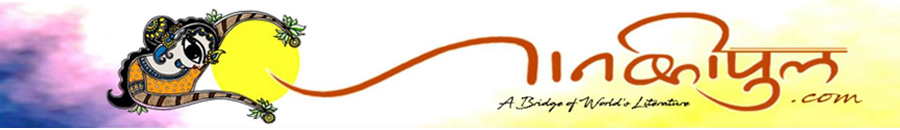संजय कृष्ण पेशे से पत्रकार हैं और चित्त से शोधार्थी। उन्होंने कई दुर्लभ किताबों की खोज की है और उनका प्रकाशन भी करवाया है। उनका यह लेख चरखे को लेकर गांधी-टैगोर बहस के बहाने कई बड़े मुद्दों को लेकर है-
=======================
सन् 1915 से लेकर 1947 तक के कालखंड को गांधीयुग के नाम से जाना जाता है। तीन दशकों का यह कालखंड भारतीय राजनीति का महत्वपूर्ण औैर स्वतंत्राता आंदोलन की दृष्टि से अत्यंत निर्णायक रहा है। इन्हीं तीन दशकों में गांधी से महात्मा तक के सफर का अपना देश साक्षी रहा है। बिहार के चंपारण लेकर देश की आजादी और बंटवारे का दुख, दर्द, दंश और इन्हीं अंतिम समयों में देश के कुछ हिस्सों में दंगे से लहूलुहान इंसानियत और टूटते भरोसे का भी यह समय रहा। इन्हीं कालखंडों में गांधी कभी थकते नजर आते हैं तो किसी को चूकते नजर आते हैं। किसी को लगता कि गांधी तो अब देश की राजनीति के लिए अप्रासंगिक हो चुके हैं। अब देश को उनकी जरूरत नहीं। उन्हें अब स्थायी तौर पर आश्रम में चले जाना चाहिए। भला, बिना बम के दर्शन के क्रूर अंग्रेज देश को यूं ही आजाद कर जाएंगे? इस तरह के कई मौजू सवाल उस दौर की फिजाओं में तैर रहे थे। अंग्रेजों को भी नहीं लगता था कि जिस लुटियन में वे एक नए शहर की नींव रख रहे हैं, उसे दो दशक बाद ही छोड़कर चले जाएंगे। यह भरोसा होता तो वे भला नए शहर की कल्पना ही क्यों करते?
इसी दौर में, यानी 1925 के आस-पास भारतीय राजनीति में गांधी के भी अप्रासंगिक होने का यह स्वर कुछ तेज सुनाई देने लगा था। लेकिन इन स्वरों और कोलाहलों से परे गांधी अपनी धुन में काम कर रहे थे। उन्हें इन कोलाहलों से जैसे कोई सरोकार न हो और वे अपने रचनात्मक कार्यों को लेकर उतने ही उत्साहित थे। देश की आजादी से इतर वे गांव की आजादी के पक्षपाती रहे। देह की भौतिक आजादी से अलग वे मन की आजादी के लिए फिक्रमंद दिखे। उनका मानना था कि मन की आजादी, देह की आजादी से जरूरी है। इसलिए, हम सिर्फ गांधी को एक राजनीतिक इकाई के तौर पर मूल्यांकन नहीं कर सकते। उनके लिए आजादी से कम महत्वपूर्ण नहीं था छुआछूत, स्वच्छता, जाति-भेद, चरखा। इस व्यापक अर्थ में हम देख सकते हैं कि वे केवल राजनीतिक व्यक्ति नहीं थे, जैसा कि हम देखते हैं कि उस समय के सभी नेताओं का दायरा सिर्फ राजनीति तक ही सीमित था। जो नेता इस दायरे को तोड़ पाए, वह भी गांधीजी के कारण ही संभव हुआ। इसलिए, इस व्यापक अर्थ और परिप्रेक्ष्य में देखें तो महात्मा का मकसद सिर्फ देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्ति भर नहीं था। वे गांव को सशक्त, स्वच्छ औेर संपन्न बनाने की दिशा में भी उतनी ही तन्मयता से लगे हुए थे। राजनीतिक सत्ता पाना उनके जीवन का लक्ष्य नहीं, व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन उनकी मंजिल थी। व्यक्ति, गांव, समाज को वे आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। इसके लिए उनके पास कुछ बुनियादी चीजें थीं, जिसके अमल के वे हिमायती थे। कुछ को लगता, गांधीजी यह क्या कर रहे हैं। यह काम तो आजादी के बाद भी हो सकता है, लेकिन उनके लिए आजादी से कम जरूरी ये चीजें कतई नहीं थीं। चरखा उनमें से एक था। चरखे से वे आजादी की बात करते थे। लोग सोचते, भला चरखा से आजादी का क्या संबंध? इस चरखे को लेकर कविगुरु रवींद्रनाथ टैगोर (1861-1941) की सोच कुछ दूसरी थी। जिस मानसिक धरातल पर गांधी (1869-1948) चरखे को लेकर सोच रखते थे, कविगुरु उसके सिर्फ भौतिक स्वरूप को ही समझ पा रहे थे। चरखे को लेकर कवि औेर महात्मा के बीच खूब वैचारिक बहसें हुईं, लेकिन दोनों के बीच आत्मीय संबंध की उष्मा कभी कम नहीं हुई। भारतीय राजनीति का भी यह एक विरल अध्याय है। गुरु और गांधी वैचारिक मतभेदों के बावजूद दोनों में आंतरिक रूप से कोई कटुता नहीं थी। दोनों वैश्विक व्यक्तित्व थे। दोनों की शिक्षा-दीक्षा यूरोप में हुई, लेकिन गांधी ने अपने ऊपर यूरोप की शिक्षा को कभी हावी होने नहीं दिया और राजनीति में वे पूरी सादगी और संत जैसा जीवन व्यतीत करते रहे। टैगोर भी शांति निकेतन के जरिए एक नई शिक्षा पद्धति औैर संस्कार की नींव रखी लेकिन दोनों में काफी वैचारिक मतभेद भी थे। कभी-कभी कटु भी हो जाते थे, लेकिन मित्रता अटूट ही रही। दोनों के मध्य जो सबसे तीखी बहस हुई, वह चरखे को लेकर थी। यह 1925 की बात है। दोनों के बीच चरखे को लेकर क्या चल रहा था, वह उनके लेखों और पत्रों से बजाहिर होता है।
बीआर नंदा ने गांधी की ‘एक जीवनी’ में उस चरखे को लेकर विस्तार से बात की है। बात ही नहीं की है, चरखे की जरूरत क्यों थी, इस देश में, उसका तर्क भी दिया है। नंदा लिखते हैं, ‘उन दिनों गांधीजी के बारे में प्राय: हर अंग्रेज यही कहता सुना जाता था कि गांधी थक गया है, खत्म हो गया है, और भारतीय नेता ऐसा मानने लगे थे कि साबरमती के संत ने राजनीति से संन्यास ले लिया है। उस समय भी राजनीति में- प्रांतीय और केंद्रीय कौंसिलों की कार्यवाहियों और समाचार पत्रों के सांप्रदायिक विवादों में अवश्य गांधीजी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजनैतिक स्वतंत्रता को वह देश के आर्थिक और सामाजिक पुनरुत्थान की अनुवर्ती मानते थे और उनका कहना था कि स्वयं जनता के अपने प्रयत्नों से ही यह पुनरुत्थान होगा। इस संबंध में उन्होंने लिखा था- ‘राजनैतिक आजादी का मतलब ही है जन चेतना में वृद्धि; और जनता की चेतना में वृद्धि तभी संभव है जब राष्ट्रीय जीवन के सभी क्षेत्रों में काम हो।‘ गांधीजी के लिए आजादी का मतलब सिर्फ चेतना में वृद्धि भी था। औैर इसके लिए जरूरी था स्वावलंबन। आत्मनिर्भरता। और चरखा ही वह माध्यम था, जिसके सहारे हर भारतीय आत्मनिर्भर बन सकता था। राजनैतिक आजादी और चेतना में वृद्धि को लेकर दोनों की सोच में अंतर था। गांधीजी की कई बातों पर टैगोर की घोर असहमति रही। सत्याग्रह को लेकर दोनों में मतभेद रहे। टैगोर सत्याग्रह को माध्यम बनाने के दृष्टिकोण से घृणा करते थे। उन्हें लगता था कि राजनयिक लोग गांधी के ‘सत्याग्रह’ को राजनीति के दांव-पेंच के रूप में इस्तेमाल कर रहे। सत्याग्रह के अलावा टैगोर को इस बात का भी दुख था कि गांधी शिक्षण संस्थाओं के बहिष्कार की बात कर रहे थे। कई और सवाल भी थे, जिन पर दोनों के बीच गहरे मतभेद रहे। यही बात चरखे को लेकर भी थी।
गांधीजी ने चरखा के बारे में टैगोर के दृष्टिकोण को अस्वीकार कर दिया था और खादी के बारे में अपने सिद्धांत का स्पष्टीकरण करते हुए लिखा- ‘विदेशी वस्त्रों के प्रति हमारे प्रेम के कारण ही चरखा अपने गरिमामय स्थान से बहिष्कृत हुआ है। इसीलिए विदेशी वस्त्रों को पहनना मैं पाप समझता हूं। मेरा मानना है कि मैं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र के बीच में कोई गहरा अंतर नहीं कर पाता।‘ इस गहरे अंतर न कर पाने की स्थिति में ही गांधीजी के लिए चरखा महत्वपूर्ण था। यह मन-तन की गुलामी से भी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता था। पर, इस चरखे को लेकर बहस की शुरुआत तब हुई जब रवींद्रनाथ टैगोर ने माडर्न रिव्यू, 1925 के सितंबर अंक में ‘चरखा यज्ञ’ लिखा था। हालांकि यह लेख पहले पहल बांग्ला की साहित्यिक पत्रिका ‘सबुज पत्र’ में ‘चरखा’ नाम से प्रकाशित हुआ, जिसका अंग्रेजी अनुवाद माडर्न रिव्यू में छपा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि निराला (1896-1961) ने उसी समय कवि के लेख की पृष्ठभूमि बताई है, हालांकि टैगोर ने भी अपने लेख के आरंभ में यह बात बताई है। निराला लिखते हैं, ‘चरखा’ शीर्षक कविवर रवींद्रनाथ का इक्कीस पृष्ठों का प्रबन्ध पहले-पहल बंगला के मासिक ‘सबुज पत्र’ में पढऩे को मिला था, उसके भादो के अंक में। बंद हो जाने के बाद इसी अंक से पत्र को पुनर्जन्म प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। इस लेख के लिखने का कारण और कुछ नहीं, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने कहीं छापे की स्याही द्वारा कविवर पर चरखे के प्रचार से उदासीन रहने के कारण अपवाद और लांछन लगाने की चेष्टा की थी, यह लेख आचार्य राय की उसी क्रिया की प्रतिक्रिया है- ठेठ भाषा में यह चपत का जवाब घूंसा है। टैगोर का यह प्रबंध लंबा है। उसी अंक में स्वराज्य के लिए संघर्ष लेख भी टैगोर का प्रकाशित हुआ, जिसमें चरखा व स्वराज्य को लेकर कवि ने कुछ और प्रश्न उठाए थे। गुरुदेव ने आयरलैंड का एक उदाहरण दिया। लिखा- ‘आयरलैंड के आर्थिक पुनरनिर्माण के सर होरेस प्लनकैट द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों को लागू करने के प्रयास में उन्हें जो निराशा, विफलता और बार-बार प्रारंभ करने की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, वे अब इतिहास का विषय हैं। चरखे के बहाने धर्म और जाति पर भी गुरुदेव ने अपने विचार प्रकट किए। गुरुदेव की कई चिंताएं थीं। गांधीजी को प्रत्युत्तर तो देना ही था ताकि चरखे को लेकर कोई भ्रम की स्थिति न रहे।
पर, कवि को जवाब देने में महात्मा ने कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। गांधीजी ने नवंबर में ‘यंग इंडिया’ में ‘कवि ओर चरखा’ शीर्षक से लेख लिखकर इसका जवाब दिया। जवाब में किसी प्रकार की कटुता नहीं थी। गांधीजी ने माना- ‘अत्यधिक प्रेम रखने के कारण मुझ पर की गई एक मीठी चोट है।‘ कवि के प्रश्नों का यह सिलसिलेवार जवाब नहीं था, बल्कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न कवि ने उठाए थे, उनका उत्तर उन्होंने दिया। गांधीजी कहते हैं- ‘यहां मेरा इरादा कवि की तमाम दलीलों का तफसीलवार खंडन करने का नहीं है। जहां हमारे मतभेद बुनियादी हैं, -और ऐसे मतभेदों को बताने की मैंने कोशिश की है -वहां कवि की दलील में ऐसी कोई बात नहीं है जिसको स्वीकार करते हुए भी मैं चरखे के विषय में अपनी स्थिति कायम न रख सकूं। चरखे के संबंध में उन्होंने जिन बातों का मजाक उड़ाया है, उनमें से बहुत-सी तो ऐसी हैं, जो मैंने कभी कही ही नहीं है। मैं चरखे में जिन गुणों के होने का दावा किया है, वे कवि के प्रहारों से उन गुणों की सच्चाई पर कोई आंच नहीं आई है।…सिर्फ एक बात से, मेरे दिल को चोट पहुंची है। कविगुरु ने फुरसत के समय इधर-उधर की बातचीतों में सुना और विश्वास कर लिया है कि मैं राममोहन राय को बहुत ‘मामूली आदमी’ समझता हूं। मैंने उस महान सुधारक को कभी ‘मामूली आदमी’ नहीं कहा, उन्हें मामूली मानने की बात तो दूर, जिस प्रकार कविगुरु की दृष्टि में वे बहुत बड़े आदमी हैं, उसी प्रकार मेरी दृष्टि में भी हैं।‘ नवंबर के बाद मार्च के अंक में गांधीजी ने ‘कविवर और चरखा’ शीर्षक से पुन: ‘यंग इंडिया’ में लिखा। यह लेख अपेक्षाकृत छोटा था।
कविगुरु को लगता था, भला चरखे से स्वराज का क्या संबंध? वह लिखते हैं- ‘बहुत से लोग हैं तो दृढ़तापूर्वक कहते हैं और कुछ लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि चरखा से स्वराज मिल सकता है, लेकिन मुझे अभी तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जिसकी इस प्रक्रिया के बारे में स्पष्ट धारणा हो। इसीलिए कोई विचार-विमर्श नहीं, बल्कि इस प्रश्न पर केवल झगड़ा है। यदि मैं कहूं कि बंदूकों और तोपों से लैस विदेशियों को अपने देसी तीर-कमानों से नहीं मार गिराया जा सकता, तो मैं मानता हूं कि ऐसे लोग अभी हैं तो मेरी बात का खंडन करेंगे और पूछेंगे क्यों नहीं?’
गांधीजी चरखा को इतना महत्व क्यों देते थे, आजादी से इसका क्या संबंध है, नंदा प्रकाश इस पर प्रकाश डालते हैं- ‘चरखे से गांधीजी के इतने अधिक लगाव को न जो अंग्रेज ठीक से समझ पाते थे और न शहरों में रहने वाले आधुनिक शिक्षा-प्राप्त भारतीय ही।‘ नंदा कहते हैं ‘गांधी के चरखा प्रेम को समझने के लिए भारतीय ग्रामीणों की भयंकर गरीबी का सही ज्ञान होना नितांत आवश्यक था। अंगरेजों की इस ओर न रुचि थी न इच्छा, और पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त भारतीय नागरिकों का गांवों के संबंध में घोर अज्ञान स्थिति को ठीक सेे समझने में बाधक था।‘ पर, गांधीजी के लिए चरखा ‘आधुनिक यंत्रवाद, औैद्योगिकरण और भौतिकवाद के विरोध का मूर्तरूप था। वे जानते थे कि गांव के सबसे गरीब लोगों को चरखा ही जोड़ सकता है। चरखा ही उन्हें आॢथक गुलामी से मुक्त कर सकता है।‘
पर, गुरुदेव को लगता था कि चरखा या सूत कातना अपनी ऊर्जा को निर्जीव करना है। वह लिखते हैं, ‘कुछ लोग कहेंगे सूत कातना भी सृजनात्मक क्रिया है। लेकिन ऐसी बात नहीं है- चरखा घुमाने से मनुष्य चरखे का ही अंग बन जाता है। अर्थात वही करता है, जो मशीन से भी किया जा सकता है। वह अपनी जीवंत ऊर्जा को पहिया घुमाने में निर्जीव कर देता है। मशीन के पास मन नहीं है इसीलिए एकाकी है वह। बाहर उसका कुछ नहीं है। इसी तरह सूत कातता मनुष्य अकेला है, उसके चरखे का सूत किसी और के साथ उसका योग नहीं कराता, उसके लिए यह जानना भी जरूरी नहीं उसका कोई पड़ोसी भी है रेशम के कीड़े की तरह अपने चारों ओर धागा बुनता है।। वह मशीन बन जाता है-एकाकी और संगी-साथी विहीन।‘
चरखा और सूत कातने को लेकर गुरुदेव की यही सोच थी। जिस तल पर गांधीजी चरखे को लेकर सोचते थे, गुरुदेव ठीक उसके उलट। गांधीजी यह नहीं चाहते थे कि लोग दिन रात चरखा ही चलाएं। और, चरखा चलाने वाला एकाकी कैसे हो सकता है। वैसे भी, बहुत से ऐसे काम हैं, जो एकाकी ही किए जाते हैं। कविता, कहानी, चित्रा बनाना आदि। एकाकी और शांत वातावरण सृजन के लिए अनुकूल होता है। गांधीजी का मानना था कि ‘चरखे का उद्देश्य हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के हितों में जो बुनियादी और जीवंत ऐक्य है, उसे मूर्त करना है। प्रकृति के भव्य और क्षण-क्षण बदलते हुए रूप के भीतर भी हेतु योजना और आकृति की एकता दिखाई देती है, जो उतनी ही स्पष्ट है जितना कि उसका वैविध्यममय बाह्य रूप। महात्मा ने पूरे तर्क के साथ कवि को जवाब दिया था, लेकिन कहीं कोई तल्खी नहीं थी। गांधीजी की तार्किकता में एक ग्रामीण सरलता भी दिखती है। इसे देखना हो तो दक्षिण अफ्रीका में उनके आंदोलन या भारत में चंपारण आंदोलन में देखा जा सकता है।
दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद एक साल देश भ्रमण ने उनकी आंखें खोल दी औेर फिर उस समय एक अलग ढंग से आंदोलन का स्वरूप और कार्यक्रम निर्धारित किए, जिन पर उन्हें बहुत भरोसा था। उन आंदोलनों का एक उपादान यह चरखा भी था। तब, वाकई कवि की तरह बहुत से लोग यही सोच रहे थे आखिर आजादी का इस चरखे से क्या संबंध? पर, गांधी गांव की गरीबी देखे थे। चंपारण आंदोलन में झुलसाती गर्मी पर नंगे पैर चलना, गांव-गांव घूमना और किसानों से बातचीत करना उन्हें बहुत कुछ सबक दे गया। वे समझ गए थे कि सिर्फ राजनीतिक आजादी से काम नहीं चलेगा, इसके साथ कई रचनात्मक काम भी करने होंगे। इसलिए, अपनी मृत्यु से एक दिन पहले जो वसीयत छोड़ी, जिस पर प्राय: चर्चा नहीं होती, उसमें उन्होंने एक बेहतर भारत की कल्पना की थी औैर उसके निर्माण के रास्ते भी बताए थे। उसी में एक था गांव। गांधीजी ने पूरी साफगोई से लिखा है-‘ मेरी दृढ़ मान्यता है कि अगर भारत को सच्ची आजादी प्राप्त करना है और भारत के जरिए संसार को भी, तो आगे या पीछे हमे यह समझना होगा कि लोगों को गांवों में रहना है, शहरों में नहीं। झोपडिय़ों में रहना है महलों में नहीं। करोड़ों लोग महलों या शहरों में कभी एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक नहीं रह सकते। उस परिस्थिति में उनके पास सिवा इसके कोई चारा नहीं होगा कि वे हिंसा और असत्य, दोनों का सहारा लें।‘ और इसे प्राप्त करने के तरीके भी बताए- ‘सत्य और अहिंसा को हम ग्रामीण जीवन की सादगी में ही प्राप्त कर सकते हैं।‘
गांधीजी गांव पर जोर देते रहे। उन्हें पता था कि भारत गांवों का देश है। भारत के सात लाख गांव बचेंगे तो ही देश बचेगा। इसे अंग्रेज भी बहुत अच्छी तरह समझते थे। इसलिए, वे गांव की अर्थव्यवस्था और उसकी स्वायत्तता पर हमला बोले। ग्रामीण कारीगरी, कुटीर उद्योग, सूत कताई को तहस-नहस किया। एआर देसाई ने लिखा है-‘आर्थिक रूप से गांव आत्मनिर्भर थे। स्थानीय श्रम एवं साधने प्रसूत स्थानीय उत्पादन का स्थानीय उपभोग होता था। गांव और बाहर की दुनिया के बीच विनियम संबंध लगभग शून्य थे। अक्सर सप्ताह में किसी एक दिन किसी बड़े गांव के बाजार में कई केंद्रों से आए तरह के सामान की बिक्री होती थी। उन दिनों जो थोड़ा सा व्यापार होता था, वह इसी रूप में संभव था।‘ प्राक ब्रिटिश भारत का यही ग्रामीण अर्थतंत्र था। धीरे-धीरे स्थितियां बदलने लगीं। औद्योगिकरण ने एक नई संस्कृति को जन्म दिया। गांव से पलायन शुरू हुआ। गांव के कुटीर उद्योग बंद होने लगे। किसान मजदूर बनने लगे। किसानी पर लगान का चाबुक चलने लगा। एक तरह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न होने लगी औैर शहरों में चाल और खोली बनने लगे। यह आजाद भारत में भी जारी है। आजादी के बाद गांधीजी गांव को संपन्न करना चाहते थे, लेकिन हमारा पूरा जोर 70 सालों में शहरीकरण का रहा। इस शहरीकरण औेर विकास की आंधी में गांव छूटते गए, जल, जंगल, जमीन के आधिपत्य का चरित्र बदलने लगा औैर इसका नतीजा अब देश की जनता भुगत रही है। विकास के नाम पर जंगलों की अंधाधुंध कटाई से लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है और तरह-तरह की बीमारियां पैदा हो रही हैं। जल के बाजारीकरण ने हमारा भूमिगत जल को भी प्रदूषित कर दिया है। नदियां पहले से ही कराह रही हैं। मनुष्य की आकांक्षाए आसमान छू रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों का तेजी से क्षरण हो रहा है। सौ साल में ये प्रकृति प्रदत्त खनिज संपदा भी खत्म हो जाएंगे, तब उस समय की दुनिया कैसी होगी, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं।
गांधीजी ने इसीलिए मशीनीकरण का विरोध किया था। इसका इस्तेमाल विवेक के साथ होना चाहिए, अंधों की तरह नहीं। हम इसी तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरी ओर जलवायु पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। जिसके कारण हम इस पृथ्वी के विनाश की पटकथा लिख रहे हैं, उसे जानते हुए भी उस ओर से आंख मूँदकर कृत्रिम बहसों में उलझ और दुनिया को उलझा रहे हैं। नीति निर्माताओं में सत्य से साक्षात्कार का साहस नहीं। इसलिए, वे तरह-तरह की बहसों को इजाद कर रहे हैं। जल पर संकट, जंगल पर संकट, जीव-जंतुओं पर संकट, नदियों पर संकट-और ये सब मिलकर मनुष्य को भी संकट में डाल दिए हैं। क्योंकि सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गांधीजी सौ साल पहले यह सब कह गए। चरखा की तरफदारी उन्होंने इसीलिए की थी कि हम धरती को बचा सकें। हम आज भी उनकी बातों को अनसुना किए हुए हैं। वे तो उसी समय कह गए थे-‘भारत की जरूरत यह नहीं है कि चंद लोगों के हाथों में बहुत सारी पूंजी इकट्ठी हो जाए। बल्कि पूंजी का ऐसा वितरण होना चाहिए कि वह इस 1900 मील लंबे और 1500 मील चौड़े विशाल देश को बनाने वाले साढ़े सात लाख गांवों कको आसानी से उपलब्ध हो सके।‘ हमारी आधुनिकता हमारी जमीन से पैदा नहीं हुई थी, नकल से हुई थी। हमने पश्चिम की नकल की और नकल में हमने उसकी अच्छाइयों को कम, बुराइयों को भी अपनाया। हम नदी की पूजा करते हैं औेर उसी में समस्त गंदगी उड़ेल देते हैं, वृक्ष की पूजा करते हैं, लेकिन उसे काटने में तनिक भी देर नहीं करते। आज हम गुरुदेव की राह पर चलकर एक बेहतर देश का निर्माण नहीं कर सकते। बेहतर भारत ही नहीं, दुनिया का निर्माण गांधी मार्ग पर चलकर कर सकते हैं। यह निर्माण उनके राजनीतिक नहीं, सामाजिक और रचनात्मक कामों के जरिए ही संभव है, जो वे अपने अंतित वसीयत में लिख गए हैं। उद्योग सबको काम नहीं दे सकता। संभव ही नहीं हैं। फिर विकल्प क्या है? विकल्प गांधीजी के पास है। मनुष्यत और मनुष्यता को दांव पर लगाकर विकास का जो ढांचा तैयार कर रहे हैं, वह आत्मघाती है। वह दिखाई भी देने लगा है। निराला ने भी तब चरखा को लेकर कवि और महात्मा के वैचारिक मतभेदों पर ‘चरखा’ नाम से लंबा प्रबंध लिखा था। उसे भी पढऩा चाहिए। गांधीजी जयंती का यह 150 वां साल है। इसलिए, हमें फिर से गांधी को पढऩा चाहिए। टैगोर के उस प्रबंध को भी और आज के समय को भी। तब हमें यह भी सोचने का अवकाश मिलेगा कि यदि हम गांधी के मार्ग पर चलते तो आज जितनी दुश्वारियां मनुष्य सभ्यता के सामने अपने वीभत्स रूप में प्रकट हुई हैं, वह हुई होती? यह भी सोचें कि भारत के तथाकथित आधुनिक मंदिर आज किस हाल में हैं? वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके? सिर्फ एक उदाहरण यहां देंगे। रांची में एचइसी का निर्माण हुआ। हैवी मशीन यहां बनते थे। पं नेहरू के सपनों की यह कंपनी है। तब 22 हजार आदमी काम करते थे। सात हजार एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई थी। 12 मुंडा गांवों को उजाड़ा गया था। कंपनी औेर पूरा रिहायशी साढ़े तीन हजार एकड़ में बना। बाकी तमाम फैक्ट्रियां लगी ही नहीं। आज एक-डेढ़ हजार आदमी काम कर रहे हैं। एचइसी अपनी बाकी जमीन बेच रही है। उसकी जमीन पर ही क्रिकेट स्टेडियम बना। विधानसभा और हाइकोर्ट बन रहे हैं। अब कल्पना कीजिए, उन परिवारों को जो आज से साठ साल पहले उजड़े। उनकी जमीन गई। रोजी-रोजगार किया। दरबदर हुए, लेकिन हासिल क्या हुआ? और, देश को भी हासिल क्या हुआ? अब तो सरकार अपनी हर कंपनी को निजी हाथों में सौंपने का उद्यम कर रही है। ऐसे देश में न जाने कितने आधुनिक मंदिर हें, उनका आज तक सर्वे नहीं हुआ कि वे जिन उद्देश्यों के लिए बने, वह कितना पूरा कर सके। तब, हमें पता चलेगा कि दूरदर्शी कौन था? तब हम आधुनिकता का अर्थ और अभिप्राय भी समझने की कोशिश करेंगे। यह भी कि यह हमारे भारतीय चित्त के अनुकूल था या नहीं?
गणेश मंत्री ने डॉ राम के वेता की पुस्तक ‘न्यू टेक्नोलॉजी-ए गांधियन कंसेप्ट’ का हवाला दिया है। वेता कहते हैं- ‘गांधी की मूल्य प्रणाली में जोर तंत्रा पर नहीं, मनुष्य पर रहा है। मनुष्य जिसका अपना नितांत निजी जीवन है और जो परिवार, ग्राम, समुदाय और राष्ट्र के सदस्य के रूप में एक समग्र तंत्र का सजीव अंग भी है। पुर्जा नहीं, सजीव अंग। यही कारण है कि गांधी के लिए जितना साध्य महत्वपूर्ण है, उतना ही साधन भी। साधन-साध्य के इस अभिन्न संबंध के कारण ही गांधी बोल्वेशिकों द्वारा की गई जोर-जबरदस्ती को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। वे सहज प्रेरणा से यह समझ गए थे कि गलत साधनों से सही साध्य तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि कालांतर में गलत साधनों के आधार पर निर्मित व्यवस्था ही सब कुछ बन जाती है और व्यक्ति गौण हो जाता है। इसलिए हम अपने युग को देखते हुए ममफोर्ड के इस कथन को याद रखें कि ‘अपने मानवीय आधार के नष्ट होने के बाद कोई भौतिक ढांचा अधिक समय तक खड़ा नहीं रह सकता। मेगामशीन और मशीन मिथक के आधार पर खड़े ढांचे की भी यही स्थिति है।‘ गांधीजी का चरखा यही संदेश तब दे रहा था। गांधीजी ने ‘कविवर औेर चरखा’ नाम से 11 मार्च, 1926 के अंक का एक अंश इसी ओर प्रकाश डालता है। वे लिखते हैं- ‘जीवन एक सजीव अखंड वस्तु है। अंतत: महत्व तो उस आंतरिक सत्ता का ही है जो हमें प्राणित करती है। यह सही नहीं है कि हमारे हाथों में बल की कमी है। सत्य तो यह है कि हमारा मन जाग्रत नहीं हुआ है…इसलिए हमारी सबसे बड़ी लड़ाई मानसिक शिथिलता के विरुद्ध ही है। गांव भी एक सजीव हस्ती है। आप इसके किसी भी विभाग की उपेक्षा नहीं कर सकते, एक विभाग की उपेक्षा करने से दूसरे विभाग को भी नुकसान पहुंचेगा। यह समझ लेना चाहिए कि हमारे देश की आत्मा एक और अखंड है। उसी तरह हमारे दुख और दुर्बलताएं भी एक दूसरे से गुथी हुई औेर इसलिए अखंड हैं।‘ फिर भी दोनों के बीच एक अद्भुत सामंजस्य और एक दूसरे की समझ के प्रति आदर और सम्मान सदैव बना रहा। टैगोर का गांधीजी को 27 दिसंबर, 1925 का पत्र देख सकते हैं। टैगोर ने लिखा है- ‘मैंने वह पत्र देख लिया है जो आपने शास्त्री महाशय को लिखा है। यह आपके उदात्त मनोभाव से परिपूर्ण है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि जिस प्रयोजन को आप सत्य समझते हैं, उसके लिए यदि आप मुझे कठोर आघात भी पहुंचाते हैं तो मैं उस आघात को सहन करूंगा और उससे आहत नहीं हूंगा। इससे हमारे व्यक्तिगत संबंधों पर आंच नहीं आएगी जो हमारे परस्पर के सम्मान पर आधारित है।‘
इस पत्र के प्रसंग के पीछे का संदर्भ यह है कि चरखे को लेकर गांधीजी ने ‘कवि औेर चरखा’ नाम से जो उत्तर दिया था, उसकी पहली पंक्ति में गांधीजी ने रवींद्रनाथ को ‘सर’ लिख दिया था ‘…कुछ समय पहले जब सर रवींद्रनाथ की चरखे की आलोचना प्रकाशित हुई थी…।‘ इस सर की उपाधि लिखे जाने पर कुछ लोगों ने माना कि गांधीजी ने ईर्ष्या के कारण ही ‘सर’ लिखा। जब गांधीजी को मालूम हुआ कि उनके ‘सर’ लिखने से कविवर को कष्ट हुआ तो उन्होंने शांतिनिकेतन के वरिष्ठ अध्यापक शास्त्री महाशय को अपनी स्थिति का स्पष्टीकरण देते हुए इस उम्मीद से पत्र लिखा कि यह संदेश टैगोरे तक पहुंचा दिया जाएगा।…गांधीजी ने लिखा कि ‘….कृपया आप कवि से यह आश्वासन प्राप्त करें कि कम से कम उन्होंने तो मुझेे गलत नहीं समझा है।‘
इस तरह, इस चरखे ने दोनों के बीच बहस का स्पेस तो क्रिएट किया, विवाद का नहीं। अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर ने लिखा है- गांधीजी गेहूं की खेत की तरह हैं तो टैगोर गुलाब बाग की तरह। मत-मतांतर के बावजूद दोनों एक दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता करते थे। दोनों के बीच 1915 से 1941 तक के पत्र-व्यवहारों में इस उपमा को देखा जा सकता है। हालांकि चरखे की विवाद की आंच उस समय कई पत्र-पत्रिकाओं तक पहुंची थी। कुछ का निराला ने अपने उसी चरखा वाले लेख में किया है। उसे भी देखना चाहिए। निराला ने लिखा है- ‘गांधी-रवींद्र-विवाद पर ‘भारती’ की सुयोग्य संपादिका श्रीमती सरला देवी चैधुरानी की कुछ टिप्पणियां मैंने उसी (अस्वस्थ) अवस्था में पढ़ी थी। एक शीर्षक है-‘कवि ओ कर्मीर लड़ाई’ और एक दूसरी है ‘गुरु-गंजना’। निराला ने एक तरह से इस लंबे लेख में सरला देवी को भी जवाब दिया था। निराला के उस लेख को भी पढऩा चाहिए, जो ‘प्रबंध प्रतिमा’ में संग्रहित है।
हमें देखना चाहिए, 94-95 साल बाद क्या आज इस तरह की बहस की गुंजाइश बची हुई है? नहीं, तो उसके पीछे क्या कारक हैं? क्या गांधीजी की आज भी जरूरत नहीं बनी हुई है? आज फिर से गांव-गणराज्य की बात हो रही है तो गांधी केंद्र में आएंगे ही। क्या गांवों को सशक्त और संपन्न किए बिना हम शहर को बेेहतर बना सकते हैं? देश की आॢथक संपन्नता का मार्ग तो गांव ही प्रशस्त करेगा, इसलिए गांव की बड़ी आबादी का सही नियोजन तो करना पड़ेगा। आजादी के बाद हम जिस मार्ग पर चले, 71 साल बाद उसका मूल्यांकन तो करना चाहिए। एकबारगी पीछे मुड़कर देख लें, फिर आगे बढ़ें। गांधीजी की 150वीं जयंती वर्ष में तो हम एक कदम ठहरकर सोच ही सकते हैं।
संदर्भ-
1-महात्मा और कवि-सव्यसाची भट्टाचार्य
2-प्रबंध प्रतिमा: निराला
3-मार्क्स, गांधी और समसायिक संदर्भ: गणेश मंत्री
4-गांधी की कहानी-लुई फिशर
5-महात्मा गांधी-एक जीवनी- बीआर नंदा
6-गांधी एंड टैगोर? ए क्रिटिकल एनालासिस-इनाम उल हक
7-महात्मा गांधी-भवानी दयाल संन्यासी
8-मेरे सपनों का भारत: गांधी
9-भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि एआर देसाई
======================