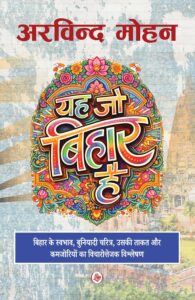हिन्दी कथा-साहित्य में जब भी शिल्प के नए प्रयोगों पर बात होती है तो उनमें एक नाम बहुत ही प्रमुखता से आता है, विनोद कुमार शुक्ल । उन्हीं का एक बहुचर्चित उपन्यास है ‘नौकर की कमीज़’ , इस उपन्यास का प्रथम प्रकाशन 1979 ई. में हुआ । प्रत्येक साहित्य का चार समय माना जा सकता है- रचना का समय, रचनाकार का समय, रचना में समय और पाठक का समय । आज इस उपन्यास के प्रकाशन के लगभग 45 वर्षों बाद जब कोई इसे पढ़ेगा या पढ़ेगी तो उसका विश्लेषण निश्चित ही इन 45 वर्षों में घटित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करेगा/करेगी । उसकी दृष्टि इन बीत चुके 45 वर्षों की परिस्थितियों के आलोक में बनेगी । यह दृष्टि युवा लेखक महेश कुमार के इस लेख में भी भरपूर मिलती है । उनके लेखों में शोधपरक दृष्टि खूब मिलती है । इस उपन्यास की समीक्षा करते हुए भी उन्होंने खूब शोध किया है जिसमें वे उन तमाम दस्तावेजों से भी रूबरू होते हैं जो तत्कालीन समय की आर्थिक स्थिति का बयां करते हैं । एक तरह से कहा जाए तो महेश आर्थिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते ‘नौकर की कमीज़’ का पुनर्पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। महेश काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शोधार्थी हैं । उनके कई लेख आलोचना, समालोचन, सबलोग, पक्षधर, कृति बहुमत, समकालीन जनमत, वागर्थ, फॉरवर्ड प्रेस, सुचेता, मेराकी इत्यादि में प्रकाशित हो चुके हैं । जानकीपुल पर भी वे पहले प्रकाशित होते रहे हैं, उसी क्रम में उनका यह लेख पढिए- अनुरंजनी
==============================
‘नौकर की कमीज’ का प्रथम प्रकाशन 1979 में हुआ था । उपन्यास के लेखक विनोद कुमार शुक्ल हैं । उपन्यास में एक संतू बाबू हैं, वे एक विभाग में क्लर्क हैं । एक डॉक्टर के मकान में अपनी पत्नी के साथ किराए पर रहते हैं । अपना काम ईमानदारी से करते हैं और विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के प्रति उनके मन में एक असंतोष है । लोग अपना काम न करके अपने साहब की चापलूसी करते हैं । विभाग के साहब को एक आदर्श नौकर की जरूरत है । साहब ने आदर्श नौकर के लिए एक कमीज बनवा ली है । उस कमीज के साँचे में फिट आने वाले नौकर की खोज है । संतू बाबू को वह कमीज फिट आ जाती है । जबतक कोई नौकर नहीं मिल जाता है तबतक संतू बाबू को वहाँ काम पर जाने के लिए कहा गया है । संतू बाबू इससे छुटकारा चाहते हैं । संतू बाबू अपने व्यवहार और व्यक्तित्व से धीरे-धीरे विभाग के अन्य पीड़ित कर्मचारियों का साथ पाने में सफल होते हैं और अंतत: ‘नौकर की कमीज’ का दहन कर दिया जाता है।
उपन्यास में नौकर की कमीज लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीछे छूट गए (जानबूझकर छोड़ दिए गए) और हर व्यवस्था में शोषित जन का रूपक है । इस बात को समझने के लिए तत्कालीन परिस्थितियों की पड़ताल करनी जरूरी है। उपन्यास 1979 में प्रकाशित हुआ, आपातकाल के ठीक बाद । उस समय की आर्थिक स्थिति के साथ-साथ दफ्तरों में नौकरशाही की स्थितियों पर एक नजर डालनी चाहिए।
अशोक भार्गव और गोपाल बालचंद्रन ने अपने लेख में बताया था कि “1974-75 में राष्ट्रीय आय का विकास दर 2.1 प्रतिशत था जो कि 1971-72 में भी था । कृषि के विकास दर में 3.1 प्रतिशत की गिरावट हुई, वहीं खाद्यान्न की उपलब्धता में 3.4 प्रतिशत कमी आयी । ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ के एक खबर का हवाला देते हुए बताते हैं कि 17 जून 1975 को पचास हजार चाय बागान मजदूरों को निकाल दिया गया । निजी सेक्टर में रोजगार की भारी गिरावट दर्ज हुई ।”[1] इसी लेख में आगे लिखा गया है कि 1976 आते-आते खाद्यान्न की उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। “1975 में अठारह मिलियन टन था जो 1976 में बाईस मिलियन टन हो गया । इसके बावजूद प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता मात्र 430 ग्राम था जो कि 1958 और 1966-67 के अकाल के समय से भी कम था। अकाल के दौरान भी प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उपलब्धता 431 ग्राम था।”[2] उपन्यास में प्रत्यक्ष रूप से तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था पर कुछ नहीं कहा गया है लेकिन संतू और अन्य निम्नवर्गीय पात्रों की घरेलू और व्यावसायिक स्थितियों का वर्णन उपर्युक्त तथ्यों को सही सिद्ध करते हैं । संतू बाबू के घर में कभी-कभी ही सब्जी बनती है । उनकी आय इतनी कम है कि वे एक ठीक-ठाक किराया का मकान भी नहीं ले सकते हैं । उनका किराया का मकान बारिश में चूता रहता है । गुप्ता के किराने के दुकान में इतना बकाया हो चुका है कि उसे लगता है कि गुप्ता हमेशा उसे घूर रहा है । दफ्तर में काम करने वाला एक ईमानदार क्लर्क के पास इतनी आमदनी भी नहीं है कि वह राशन नगद खरीद सके । इसी तरह महावीर नाम का एक खोमचे वाला है जो एक स्कूल के बाहर मूँगफली बेचता है । जब उसके पास पैसे कम होते हैं तब वह मूँगफली नहीं खरीद पाता है । ऐसे में वह खाली हाथ वहाँ खड़ा रहता है । कभी-कभी बाजार में ही मूँगफली नहीं मिल पाता । इससे दो बातें निकलती हैं कि बाजार में खपत होने लायक उत्पादन नहीं हो रहा था। मतलब नियमित रूप से ‘माँग और पूर्ति’ का पालन नहीं हो पा रहा था । दूसरी बात कि वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ गयी थी । लेखक ने संकेत में इन बातों को रखा है ।
एक तरफ बेरोजगारी बढ़ी, खाद्यान्न की कमी और आय में गिरावट हुई तो दूसरी तरफ सरकारी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों में भ्रष्टाचार बढ़ा और कार्य करने की संस्कृति में तेजी से गिरावट आयी । इस मुद्दे पर 1988 में ओ.पी. द्विवेदी और आर.बी.जैन ने एक लेख लिखा ‘ब्यूरोक्रेटिक मोरालिटी इन इंडिया’। इस लेख में उन्होंने 1978 में प्रकाशित शाह कमीशन को आधार बनाया जिसमें यह लिखा गया था कि, “नौकरशाहों ने कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर आपस में एक सहमति बना ली है । वे इसे नए तरह के अधिकार और मूल्य मानते हैं और इसे एक अवधारणात्मक स्तर पर स्वीकार कर लिया है।”[3] शाह कमीशन के प्रकाशन का समय वही है जो उपन्यास का है । इस बात को ध्यान में रखने से उपन्यास में मौजूद दफ्तर के साहब और नौकरशाही के चित्रण को समझने में मदद मिलती है । ओ. पी द्विवेदी शाह कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि “भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारी अपनी जाति, वर्ग, क्षेत्र और एथनिक पहचानों से बहुत गहरे रूप में जुड़े हुए हैं । अपने-अपने हित समूहों के लिए काम करने और उनके लिए अनैतिक रूप से जगह बनाने को वे अनैतिक नहीं मानते।”[4] इसी में वे आगे लिखते हैं कि “आजादी के बाद लोकतंत्र में राजनेताओं और उनके परिवारों की बढ़ती शक्तियाँ और अधिकारियों के लिए दंड के प्रावधान में लचीलापन उन्हें जिम्मेदारी और जवाबदेही के प्रति लापरवाह बनाती गयी । इस कारण से भी सरकारी दफ्तरों में नौकरशाही का दबदबा बनता गया ।”[5] विनोद कुमार शुक्ल इस उपन्यास में उपर्युक्त मुद्दे को बड़ी सहजता से प्रस्तुत करते हैं । वे लिखते हैं कि साहब को जबतक आदर्श नौकर नहीं मिल जाता है तबतक दफ्तर के लोग ही ‘नौकर’ बन जाने के लिए तैयार हैं । इसी प्रवृत्ति ने अधिकारियों को अतिरिक्त शक्ति दी है और वे इसका प्रयोग कर्मचारियों और जनता को दबाए रखने के लिए करते हैं । परिणाम यह होता है कि दफ्तर में लोकतांत्रिक संस्थाओं में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच साहचर्य की भावना की जगह वर्ग-विद्वेष की भावना हो जाती है । उदाहरण के लिए उपन्यास में नाटक मंचन का एक दृश्य संतू बाबू बनाने की सोचते हैं।
संवाद में गौराहा बाबू कहते हैं:- “वह दरख्वास्त मेरी छुट्टी की होनी चाहिए, कि परिस्थितियों के कारण, जिनसे मैं बच नहीं सकता, दो रोज की आकस्मिक छुट्टी देने की कृपा करें । नीचे मेरा दस्तखत जरूर होना चाहिए।”
देवांगन बाबू ने कहा:- “उन परिस्थितियों को स्पष्ट करना होगा।”
गौराहा बाबू ने बोले:- “एक खराब परिस्थिति में रहते-रहते उसकी आदत पड़ जाती है और वह खराब नहीं लगती । परंतु, खराब हालत हो जाए तब दफ्तर से छुट्टी लेनी पड़ती है।”
मैंने कहा:- “अत्यंत खराब परिस्थिति की भी आदत पड़ जाए इसलिए आपकी छुट्टी मंजूर नहीं होगी।”[6]
यह संवाद दफ्तरों में व्याप्त वर्ग-विभेद की स्थिति को दर्शाता है । सरकारी दफ्तरों में काम के घण्टे, छुट्टियों के नियम और अन्य कर्मचारी सुविधाओं की नियमावली तय है । इसके बावजूद अधिकारी कर्मचारियों पर धौंस दिखाते हैं । उनकी अभिव्यक्ति का दमन करते हैं और अतिरिक्त काम लेते हैं । उपन्यास में ऐसे कई प्रसंग हैं जहाँ कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच वर्ग-विभेद खुलकर सामने आते हैं । संतू बाबू जब रात को दफ्तर में घूमने के उद्देश्य से जाते हैं तब भी देखते हैं कि लोग काम कर रहे हैं । यह दृश्य अब हर संस्थाओं में देखा जा सकता है । फैक्टरियों में मजदूर अतिरिक्त काम कर रहे हैं । रेलवे में ड्राइवर और अन्य कर्मचारी न चाहते हुए भी ओवरटाइम कर रहे हैं । विश्वविद्यालयों में अब प्राध्यापकों को एक निश्चित समय सीमा से बाँधने की कोशिश हो रही है । नौकरियों में सेवा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की आलोचना पर सेवामुक्त करने का प्रावधान है । ये सब प्रावधान अधिकारियों को शोषक बनाता है । ऐसी परिस्थितियों में जो सबसे ज्यादा शोषित होता है या तो वह उसमें ढल जाता है और अपनी नियति मानकर बस यांत्रिक रूप से अपना काम करता है, या ईमानदारी से काम करते हुए धीरे-धीरे अपनी व्यवस्था बदलने का प्रयास करता है । उपन्यास के अंत में ‘नौकर की कमीज’ दहन में जितने लोग संतू बाबू के साथ शामिल होते हैं, पहले वे सब संतू को सिरफिरा समझते थे । देवांगन बाबू और गौराहा बाबू का साथ में आना दरअसल कर्मचारी वर्ग की एकता का प्रतीक है और अधिकारी वर्ग के तानाशाही के प्रति एक बगावत का स्वर है ।
विभिन्न वर्गों का चित्रण, उनका आपसी संबंध और समकालीन संदर्भ
इस उपन्यास में चार वर्ग समूह हैं । संतू बाबू निम्नमध्यवर्गीय समूह के प्रतिनिधि हैं । महंगू, उसका बेटा, माली, नौकर, खोमचे वाला महावीर और झुग्गियों के अन्य पात्र निम्नवर्ग के प्रतिनिधि हैं । डॉक्टर, डॉक्टर की पत्नी, साहब और साहब की पत्नी उच्च वर्ग के प्रतिनिधि हैं । संतू बाबू की पत्नी वैसी महिला वर्ग की प्रतिनिधि है जो अपने गृहस्थी और स्वाभिमान को बचाने के लिए निरंतर संघर्षरत है । संतू बाबू इन सभी वर्ग समूहों में आवाजाही करते हुए व्यवस्था और समाज में व्याप्त शोषण की पहचान करते चलते हैं और अपना एक विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं ।
संतू बाबू एक पढ़े-लिखे सजग युवा हैं । वे न नौकर की कमीज में फिट होना चाहते हैं और न ही व्यवस्था की कमीज में फिट होकर अपने अधिकारियों के हाथों शोषण करवाने के लिए खुद को समर्पित करते हैं । एक तरह का सनकीपन उनके स्वभाव में है । यह ‘सनकीपन’ दरअसल समाज के उस प्रवृत्ति को संबोधित है, जिसमें कि हर जागरूक नागरिक को संदेह की निगाह से देखा जाता है । यह सनक भरा अभिव्यक्ति उपन्यासकार का एक कलात्मक प्रयोग है जिसके जरिये वे व्यवस्था के शोषणकारी परतों को संप्रेषणीय तरीके से उघाड़ते हैं । उदाहरण के लिए, संतू बाबू जब महंगू पर विचार करते हैं तब वे कहते हैं कि, “महंगू कितना भी ईमानदार हो पर सौ रुपए के लिए उसकी नीयत डोल सकती थी। यानी निन्यानबे रुपए तक वह ईमानदार था। हैसियत के हिसाब से नियत डोलने की सीमा निर्धारित होती है।”[7]
यहाँ संतू बाबू की दृष्टि व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर केंद्रित है । यहाँ महंगू की जगह कोई उच्च वर्गीय व्यक्ति होता तब शायद सौ रुपये की जगह लाख या करोड़ रुपए होता। उनकी बेईमानी पर समाज चुप रहता बल्कि उनकी हैसियत को देखकर डरता और उनसे चिपके रहकर अपना काम निकलवाने की कोशिश करता । यानी व्यक्ति की वर्गीय स्थिति का सीधा संबंध उसके सामाजिक सम्मान के स्थिति को तय करता है । अकारण नहीं है कि साहब यह कहते हैं कि, “मैं अपनी कमीज नौकर को कभी देना नहीं चाहूँगा। मैं घर का बचा-खुचा खाना भी नौकरों को देने का हिमायती नहीं हूँ। जो स्वाद हमें मालूम है उनको कभी नहीं मालूम होना चाहिए। अगर यह हुआ तो इससे असंतोष फैलेगा। उनका खाना वैसा ही दो जैसा वे खाते हैं। अगर ये स्वाद के चक्कर में पड़ गए तो अपनी जान बचानी मुश्किल हो जाएगी।”[8] डॉक्टर का यह विचार एक शोषक का विचार है । उसे बेहद अच्छी तरह अपने वर्गहित का पता है । वो नहीं चाहता कि निम्नवर्ग किसी भी तरह से उन संसाधनों के बारे में जान पाए जो उसकी जिंदगी को बेहतर बनाता हो । अच्छा खाना, कपड़ा और जीवन की मूलभूत सुविधाओं से निम्नवर्ग जितना वंचित रहेगा उच्च वर्ग का मुनाफा और सुविधाओं में उतनी ही बढ़ोतरी होती रहेगी । डॉक्टर की यह सोच असमानता, संसाधनों पर अवैध कब्जा और श्रम के अनैतिक दोहन का पोषक है । महंगू और साहब के बीच वर्गीय विभेद बना रहे इसके लिए साहब के पास पर्याप्त तरीके मौजूद हैं । यह तरीका इतना क्रूर और कारगर है कि अंततः महंगू मर जाता है और उसका बेटा उसकी जगह लेता है । यह शोषण इतना विभत्स है कि महंगू के बेटे की अपनी पहचान तक समाप्त हो जाती है और उसे भी दफ्तर और साहब के घर में महंगू की बुलाया जाता है । मतलब एक मनुष्य की पहचान व्यक्तिवाचक से जातिवाचक में बदल जाती है । मनुष्य की गरिमा का यह क्रूरतम अवमूल्यन है । उच्च हैसियत वाले समूह को अपने वर्ग की स्पष्ट समझ है । निम्नवर्ग वाले को इतना उलझा कर रखा गया है कि वे अपने वर्गहित को समझ ही नहीं पाते हैं और प्रायः बँटे हुए रहते हैं ।
संतू बाबू को अपने वर्गहित ही सटीक पहचान है । इसी कारण वे डॉक्टर के यहाँ अपना ईलाज नहीं करवाना चाहते हैं । वे जानते हैं कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में अब सीधे-सीधे शोषण नहीं किया जा सकता है । अब शोषण के लिए ‘एहसान’ और ‘उपकार’ का प्रयोग किया जाता है । कुछ दवाईयों और सुई के बदले डॉक्टर की पत्नी संतू बाबू के पत्नी से तमाम घरेलू काम करवाती है । शहर में रहते हुए वहाँ के वर्गीय रुचियों और ‘क्लैश ऑफ इंटरेस्ट’ को ठीक से समझते हैं । उनका मानना है कि “आँखों से जो कुछ भी देखा जाता है उसका काम अनुभव से चलता है, उससे भी ज्यादा अंदाज से जिसमें गलतियाँ ही गलतियाँ होती हैं । अंदाज से नहीं होशियारी और चालाकी से भी दुनिया चलती है जिसमें गलतियों की संभावना कम होती है। इसमें खुद का नुकसान कम दूसरों का नुकसान अधिक होता है। हम लोगों की सारी तकलीफ उन लोगों की होशियारी और चालाकी के कारण थी जो बहुत मजे में थे और जिसे हमारा परिचय नहीं था।”[9] यहाँ ‘होशियारी’ और ‘चालाकी’ के प्रतिनिधि डॉक्टर और साहब जैसे लोग हैं । लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी तरह की नीतियाँ इनके हित को ध्यान में रखकर बनाई जाती है । व्यवस्था में जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं उसमें इनका नुकसान नहीं होता है । भारतीय लोकतंत्र इसका उदाहरण है । हर मंत्रालय और विभाग के बड़े-बड़े घोटालों से उच्च वर्ग का कोई खास नुकसान नहीं होता है । पूँजीपति वर्ग के कर्जे आसानी से माफ हो जाते हैं, किसान वर्ग आत्महत्या के लिए मज़बूर हो जाता है, ऑक्सिजन की कमी से, दवाई की कमी से, परीक्षा घोटालों से और तमाम व्यवस्थागत और नीतिगत असफलताओं से समाज का मजदूर और निम्नमध्यवर्गीय वर्ग प्रभावित होता है। यह उपन्यास इन अर्थों में कई जटिल परतों को खोलने में मदद करता है । सरकारों को और व्यवस्था को जब भी लगता है कि असंतोष फैल सकता है वह तात्कालिक राहत की न्यूनतम व्यवस्था करके विद्रोह की चिंगारी को बुझा देती है । अनाज की कमी होगी तो वह कुछ किलो का मुफ्त राशन की व्यवस्था कर देगी । पानी की कमी होगी तो कुछ टैंकर पानी देगी और कहीं विस्थापन का सवाल होगा तब कुछ लोगों को नौकरी और मकान देकर उसे उस समाज का दलाल बनाकर अपना काम निकाल लेगी । संतू बाबू व्यवस्था के ऐसे तमाम पैंतरों से परिचित हैं। इसलिए वे कहते हैं “संघर्ष का दायरा बहुत छोटा था। प्रहार दूर-दूर से और धीरे-धीरे होते थे। इसलिए चोट बहुत जोर की नहीं लगती थी। शोषण इतना मामूली तरीके से असर डालता था कि विद्रोह करने की किसी की इच्छा नहीं होती थी या विद्रोह बहुत मामूली किस्म का होता था।”[10] उपन्यास में यह दूर-दूर से होने वाले प्रहार हैं । डॉक्टर का यह कहना कि “छप्पर सूखने में तीन दिन का समय लगेगा । तीन दिन धूप लगने दो तब मजदूर बुलवाकर काम करवा दूँगा ।” इसी तरह पत्नी से कभी चावल चुनने को कह देना या साथ में बाजार चलने को कह देना । संतू बाबू जब डॉक्टर को बीमारी की हालत में जानबूझकर गाली देते हैं तब डॉक्टर द्वारा उसे अनसुना करना । यह सब तरीके विद्रोह को दबाने के लिए है । इसी तरह संगठित विद्रोह को दबाने के लिए दफ्तर में एक कर्मचारी को दूसरे कर्मचारी से अलग रखने की नीति अपनाई जाती है । गौराहा बाबू और देवांगन बाबू इसी नीति के कारण संतू बाबू से दूर रहते हैं । सरकारी दफ्तरों में विद्रोह को दबाने का सबसे उचित तरीका है वेतन में कटौती, सस्पेंड करना और तरह-तरह के नोटिस जारी करना । सरकारी दफ्तर मध्यवर्गीय आकांक्षाओं वाले लोगों की जगह है । उनके पास आय के निश्चित साधन यही हैं । इसलिए वेतन का ख्याल आते ही विद्रोह की भावना ढीली पड़ जाती है । संतू बाबू की नजर में “वेतन एक कठघरा था जिसे तोड़ना मेरे वश की बात नहीं थी।”[11] इसी वेतन से वो खर्च चलाते थे, परिवार चलाते थे और कभी-कभी सिनेमा भी चले जाते थे । जो सरकारी दफ्तरों में नहीं हैं, वे मजदूरी में अपने पेट भर भोजन की व्यवस्था में ही इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें विरोध और विद्रोह के बारे में सोचने तक का फुरसत नहीं है । संतू बाबू को इसका प्रत्यक्ष अनुभव है । वे नौकरी बाजार में लगने वाले रोजाना के भीड़ को देखते रहे हैं । बेरोजगारी के बढ़ते हालत को संतू बाबू ने ऐसे बयान किया है, “नौकर बाजार में भीड़ के बढ़ते जाने से मजूरी इतनी सस्ती हो गई थी कि एक बटकी पसिया पेज की रोजी में कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाता था। बहुत सारे मोची, बढ़ई खजरु मोची की तरह काम खोजने के बदले भीख माँगने लगे थे। पर अचानक भीख देने की सँस्कृति का लोप हो गया था।”[12] जिस देश और समाज में ऐसी आर्थिक परिस्थिति हो और उस वर्ग को अपने वर्गहित के बारे में ठीक से पता भी नहीं हो वहाँ विद्रोह की भावना विकसित नहीं हो सकती है । कमर तोड़ मेहनत करने के बावजूद उचित मजदूरी के अभाव में व्यक्ति भरपेट भोजन नहीं जुटा पा रहा है । इसका सीधा मतलब है कि मजदूर वर्ग के श्रम का अवमूल्यन करके उसके श्रम से उत्पादित अतिरिक्त उत्पादन से पूँजीपति वर्ग और उच्च वर्ग मुनाफा कमा रहा है । सरकार का हिस्सा भी इन मुनाफाखोरों के साथ है । इस पर भी ध्यान देना जरूरी है कि जब यह उपन्यास प्रकाशित हुआ उसके ठीक बाद नई आर्थिक नीति की बात होने लगी थी । कल्याणकारी राज्य और कल्याणकारी योजनाओं के नुकसान गिनाए जाने लगे थे और मुक्त व्यापार के लिए दवाब बनाया जाने लगा था जिसकी परिणति 1991 में एलपीजी मॉडल के रूप में आता है। उपन्यास में उसकी झलक दिखाई पड़ती है । जब संतू कहता है कि विज्ञान से गरीबों को कोई खास लाभ नहीं मिला या कि “हालत सुधारने के लिए अधिक से अधिक मेहनत करने के उपाय पर मुझे विश्वास नहीं था । कुदाली चलाने वाला मजदूर दिन-रात कुदाली चलाकर भी अपनी हालत सुधार नहीं सकता।”[13] संतू बाबू का यह विश्वास निर्रथक नहीं है । आज 2024 में स्थिति में खास बदलाव नहीं है । मजदूरों की आय इतनी नहीं है कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सके । भुखमरी में हर साल भारत का खराब प्रदर्शन और करोड़पति की सूची में भी कई भारतीयों का नाम होना यह बताता है कि यहाँ आर्थिक असमानता और संसाधनों का असमान वितरण बहुत ज्यादा है । ठीक ऐसी परिस्थिति में नारायण मूर्ति जैसे उद्योगपति कहते हैं कि कर्मचारियों को सप्ताह में सत्तर घण्टे काम करना चाहिए और मुफ्त में कुछ भी नहीं मिलना चाहिए । वे यह नहीं कहते कि कर्मचारियों का वेतन बढ़ना चाहिए और वंचितों को उनके जरूरत के हिसाब से न्यूनतम आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराना चाहिए । वे यह नहीं बताते कि सत्तर घण्टा काम करने से व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन में क्या बदलाव आएगा और उसकी अपनी उन्नति कितनी होगी? इस तरह के सोच पूँजीवादी राज्य को स्थापित करने में मदद करते हैं और कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को खत्म करते हैं । वे पूँजीपति वर्ग से यह नहीं पूछते कि उनको इतना अकूत संसाधन क्यों चाहिए? संतू बाबू उपन्यास में इस प्रश्न को अच्छी तरह चिन्हित करते हैं । वे साहब और उनकी पत्नी के संसाधनों पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि, “नौकर की उन्हें कमी नहीं थी, पर बिना कमी के भी जरूरत होती रहती थी। जैसे बाई साहब के पास पचास साड़ियाँ हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास पचपन साड़ियाँ नहीं हैं। नंबर से जरूर का हिसाब पूरा नहीं होता है। नंबर से जरूरत का हिसाब कम पड़ता है।”[14]
यही है संसाधनों पर अनैतिक कब्ज़ा जिसके खिलाफ जाने पर व्यवस्था और राज्य दोनों मजदूरों का दमन करती है । यह उपन्यास अपने सरल वाक्य विन्यासों से और बिना राजनीतिक कठोरता के आम जनता के सारे सवाल और उसका विश्लेषण पाठकों के सामने रखता है ।
इस उपन्यास में एक जरुरी पक्ष स्त्री-पुरुष या पति-पत्नी के आपसी संबंधों का है । घरेलू हिंसा का जिक्र है । संतू का दोस्त संपत अपनी माँ पर हाथ उठाता रहा है । मुख्य रूप से संतू और उनकी पत्नी, डॉक्टर और उनकी पत्नी तथा साहब और उनकी पत्नी हैं । तीनों घरों की स्त्रियों की आर्थिक स्थिति अलग-अलग है । यह उनके स्वभाव में भी झलकता है । संतू बाबू की पत्नी एक निम्नमध्यवर्गीय स्त्री है । उसके भीतर स्वाभिमान है । वह अपने स्वाभिमान से कहीं-कहीं समझौता करती है ताकि उसका गृहस्थ जीवन ठीक से चले । वह पति पर अपने दुखों का बोझ नहीं डालती है और यथासंभव मेहनत करती है । पति के साथ दोस्ताना संबंध है पर, कहीं न कहीं पति उसपर हावी है । इसके बावजूद संवाद की पर्याप्त गुंजाइश है और एक हद तक बराबरी का रिश्ता है । डॉक्टर की पत्नी का उसके पति के साथ बराबरी का रिश्ता का पता नहीं चलता । वह बस डॉक्टर की बहन का शोषण करती है, क्योंकि वह विधवा है और आर्थिक रूप से निर्भर । साहब की पत्नी भी अपने पति के लिए एक ‘शोपीस’ की तरह है । पैसा है और सुविधा है पर चेतना नहीं है । स्त्रियों का पक्ष संतू की पत्नी की तरफ से ही प्रमुखता से उभरता है। हालाँकि पत्नी का कोई नाम नहीं है । मतलब उसकी पहचान उसके पति से ही है । उसका अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व उभरकर उपन्यास में नहीं आता है । वह अपने होने को उपन्यास में दो जगह स्थापित करती है । जहाँ-जहाँ संतू उसकी निजता का अतिक्रमण करता है वहाँ उसकी पत्नी अपना पक्ष मजबूती से रखती है । पहला प्रसंग है जब संतू उसका संदूक खोलना चाहता है । वह मुखर विरोध करती है । संदूक में पैसे हैं । पत्नी कहती है कि ,”मैं रुपए तुम्हें खर्च करने नहीं दूँगी। ये मेरे रुपए हैं। संतू बाबू कहते हैं, “तुम तो कमाती नहीं हो, तुम्हारे रुपए कहाँ से हुए?”[15] यहाँ ध्यान देने की बात है कि यही पत्नी उनके साथ तमाम अभावों में साथ रहती है । इसलिए उनको अपनी पत्नी से बेहद प्रेम है । लेकिन जैसे ही बात अर्थ की आती है उनका पुरुषवाद सजग हो जाता है । वो यह नहीं देखते कि उनकी पत्नी जितना श्रम करती है उसका हिसाब लेने लगे तब वो भरपाई नहीं कर पाएँगे । वह डॉक्टर की पत्नी का काम करने के लिए विवश है क्योंकि उसका पति उस लायक नहीं है । संतू बाबू यह सब नहीं देख पाते । उनके पास पत्नी के अवैतनिक श्रम का कोई हिसाब नहीं है । यहाँ वे पितृसत्तात्मक व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं । दूसरा प्रसंग है जब संतू बाबू अपनी पत्नी को झिड़कते हैं कि तुममें हिम्मत नहीं है । पत्नी कहती है, “मुझमें बहुत हिम्मत थी, अब भी है। मुझे डर लगता है कि हिम्मत है दिखलाई तो तुम साथ छोड़ दोगे और मुझे दोष दोगे।”[16]
यह संवाद एक आत्मविश्वास से भरी हुई स्त्री का स्वर है। यह एक साथ विवाह संस्था के भीतर की घुटन और स्वतंत्रता की चाह की अभिव्यक्ति है । एक दोस्ताना रिश्ता होते हुए भी बराबरी का रिश्ता नहीं है । आखिर उसकी हिम्मत में ऐसी क्या बात है जिससे उसका पति छोड़ देगा और दोष देगा? संभवत: वह बाहर काम करने की स्वतंत्रता और आत्मनिर्णय का अवसर चाहती है । वह अपनी आर्थिक स्थिति सुधारना चाहती है । इससे यह पता चलता है कि पितृसत्ता बहुत गहरे धँसी हुई विचारधारा है जिससे स्त्री-पुरुष संबंधों में कहीं न कहीं गैर-बराबरी रह ही जाती है।
भाषा की सम्प्रेषणीयता, प्रयोगवादी शिल्प और कहने का अनूठापन
यह उपन्यास भाषा की सम्प्रेषणीयता के लिए जाना गया है । इस उपन्यास की भाषा में वाक्य विन्यास और शब्द सरल और छोटे होते हुए भी पाठक को नया-नया लगता है । यह नयापन यथार्थ को कल्पना की तरह कहने के ढंग के कारण आया है । जिस तरह शब्दों को क्रमबद्ध करके छोटे वाक्य बनाए गए हैं उसके भीतर से ही अर्थ खुलता जाता है । उदाहरण के लिए, उपन्यास का शुरुआती अनुच्छेद इस प्रकार है कि “ घर बाहर जाने के लिए उतना नहीं होता जितना की लौटने के लिए होता है। बाहर जाने के लिए दूसरे के घर होते हैं। दूसरे के घर यानी परिचित या जिससे काम हो। लौटने के लिए खुद का घर जरूरी होता है चाहे किराए का एक कमरा हो या कमरे में कई किराएदार हों।”[17] घर से बाहर जाना और लौट आना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन यहाँ उपन्यास में छोटे वाक्यों में इस बात को जिस क्रमबद्धता से कहा गया है उससे एक निम्नमध्यवर्गीय व्यक्ति का घर के प्रति आसक्ति और उसकी सामाजिक गतिशीलता (mobility) का एक अनुमान लगता है । इसी के बाद पंक्ति आती है कि ‘पत्नी घर से निकलती नहीं है इसलिए उसे घर लौटने की जरूरत नहीं पड़ती है।’ इससे स्त्री और पुरुष के गतिशीलता और सार्वजनिक जगहों पर उनकी उपस्थिति के दर का पता चलता है । यही वह भाषा को बरतने का नया तरीका है जिससे पाठकों को आकर्षित किया । यथार्थ कल्पना की तरह लगने लगता है।
विनोद कुमार शुक्ल कवि भी हैं । उपन्यास में भी कविता का मिजाज बार-बार भाषा में प्रकट होता है नए तरह के उपमाओं के साथ । एक जगह पति-पत्नी संवाद है । फर्श जल्दी सूख जाए इसके लिए संतू बाबू सारे दरवाजे और खिड़कियाँ खोल देते हैं । पत्नी कहती है, “दरवाजे-खिड़की क्यों खोल दिए, घर बिल्कुल नंगा हो गया।” संतू बाबू खिड़की बन्द करते हुए कहते हैं, “लो , घर को चड्डी पहना रहा हूँ। पिछवाड़े के दरवाजे को बंद करते हुए मैंने कहा “घर को पायजामा पहना रहा हूँ।”[18]
यहाँ घर का ‘नंगा’ होना, ‘चड्डी और पायजामा पहनाना’ कविता की भाषा और उपमा है। लेखक का यह प्रयोग उपन्यास को बाधित नहीं करता है बल्कि निम्नमध्यवर्गीय परिवार के जीवन के संकटों को उभारता है ।
उपन्यास में शिल्प के स्तर पर एक और अच्छा प्रयोग है । उपन्यासकार को जब भी निम्नवर्ग के बारे में लिखना होता है वह अपने मुख्य पात्र संतू बाबू को कस्बे के सैर पर निरुद्देश्य ले जाता है । उपन्यास में जब भी नौकर बाजार, झुग्गियों और खोमचे वाले का जिक्र आता है तब-तब संतू बाबू घर से बाहर निकलकर निरुद्देश्य घूम रहे होते हैं । यह विचार और शिल्प के स्तर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि, यदि समाज के वास्तविक स्थिति का ठीक-ठीक पता लगाना है तब आम जनता के जीवन को घूम-घूम कर देखना बेहद जरूरी है । उपन्यास में जहाँ-जहाँ वर्ग विभेद को विस्तार से बताया गया है वहाँ संतू बाबू इन्हीं समाजों के बीच घूम रहे होते हैं । चाहे वह मिट्टी तेल के लिए शहर से थोड़ा निकल आये हों और कालाबाजारी के बारे में लोगों को बता रहे हों या फिर नौकर बाजार जाकर बेरोजगारी और भुखमरी की स्थिति पर विचार कर रहे हों । इससे पता चलता है कि समाज के विश्लेषण के लिए यायावरी का होना जरूरी है । यही यायावरी संतू बाबू को यह बोध कराता है कि “खर्च पूरा न बैठने के कारण दया और उदारता कम हो जाती है। यह बात समझ में जल्दी आती थी। उदारता और दया का सीधा संबंध रुपए से है। सिर पर हाथ फिराना ना तो उदारता होती है ना दया, बस सर पर हाथ फिराना होता है।”[19] यह एक कमाने-खाने वाले व्यक्ति का बेहद व्यावहारिक पक्ष है । पूँजीपति त्योहारों और सार्वजनिक महत्त्व के कार्यक्रमों में खूब दान देते हैं, लंगर चलाते हैं और समाजसेवा का ढोंग करते हैं । वो ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनके पास रुपए हैं । वे इसके जरिए कई लोगों को अपना एहसानमंद बना सकते हैं । एक सामान्य नागरिक ऐसा नहीं कर सकता है । यानी उदारता का सीधा संबंध पूँजी से है । लेखक इस बात को चार छोटे वाक्यों में कह देता है ।
उपन्यासकार ने अपने कथानकों को स्पष्ट करने के लिए, विषय परिवर्तन के लिए और उनमें एक क्रमबद्धता बनाये रखने के लिए उपशीर्षकों का सहारा लिया है । इन उपशीर्षकों को एक साथ रख देने से एक कविता लगने लगती है । उपशीर्षक अपने आप में व्यक्ति की आर्थिक और सामाजिक जटिलताओं का सार लगता है । उदाहरण के लिए, “धूप कमरे में आती है। सूर्य नहीं आता। बारिश के दिन लगातार तीन दिनों की धूप की जरूरत थी। तीन दिन से ज्यादा की धूप नहीं चाहता था।”[20] इसका सीधा संबंध व्यक्ति के आर्थिक स्थिति से है। घर चू रहा है। सूखने के लिए धूप चाहिए ताकि मरम्मत हो सके । इस उपशीर्षक में व्यक्ति और आर्थिक सत्ता के संबंधों का सार है । इसी तरह एक उपशीर्षक है “गड्ढे के अंदर बहुत बड़ा मैदान है, लगता ही नहीं की गड्ढे के अंदर हैं। गड्ढे के अंदर में भी सबकी जगह निश्चित है।”[21] मतलब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो समाज में अबतक हाशिये पर हैं उन्हें हाशिये पर बनाये रखने की पूरी योजना है । जिनके पास पूँजी है जो राज्य और उसके संस्थाओं से मोलभाव कर सकते हैं वे ही इस लोकतंत्र में अपने अधिकार का उपभोग कर पाएँगे । इस तरह उपन्यास की भाषा में बिना राजनीतिक विचारधारा की अभिव्यक्ति के भी लेखक ने बता दिया है कि उसकी सहानुभूति किस वर्ग के साथ है।
इस उपन्यास में तत्कालीन राजनीति के अनुरूप कहीं भी जनक्रांति की गूँज नहीं है, कोई राजनीतिक पक्षधरता भी उभर कर नहीं आती है । लेखक को जो कहना है वह दैनिक जीवन के छोटे-छोटे विवरणों के माध्यम से ही कहता है । मतलब भाषा और कथ्य से ही लेखक की पक्षधरता सामने आती है । कथानक में जीवन की जटिल और कटु परिस्थितियों से जो क्षोभ और गुस्सा उभर कर आता है उससे यह उपन्यास भारतीय लोकतंत्र पर एक व्यंग्य के रूप में सामने आता है । पात्रों के सनकीपन और भाषा को प्रस्तुत करने के तरीके से नाटकीयता का बार-बार आभास होता है । यह नाटकीयता अखरती नहीं है । इसी नाटकीयता की वजह से पात्रों में जीवन के प्रति एक रागात्मकता है, खिलंदड़पना और खुलापन है जो उन्हें अपने जीवन को जीने लायक बनाता है।

====================
संदर्भ –
[1] Bhargav.Ashok, Balchandran. Gopal, economic change during indian emergency, Bulletin of concerned asian scholars, ISSN- 0007-4810, www.tandfonline.com /journal. Page:- 50, Access date:- 18.02.24
2 Ibid. Pp:-52
3 Dwivedi.O.P, Jain. R.B, Bureaucratic morality in india, International political science review (1988), vol.9,No:-3, pp-205-214, http:/JSTOR.org/, pp:- 206
4 Ibid. Pp:-214
5 Ibid, pp:-214
6 नौकर की कमीज, विनोद कुमार शुक्ल, राजकमल प्रकाशन, पहला संस्करण, 1994, सातवां, 2017, पृष्ठ:- 34
7 वही, पृष्ठ:-13
8 वही, पृष्ठ:-95
9 वही, पृष्ठ:-15
10 वही, पृष्ठ:-17
11वही, पृष्ठ:-17
12वही, पृष्ठ:-169
13 वही, पृष्ठ:-92
14 वही, पृष्ठ:-95
15वही, पृष्ठ:-88
16वही, पृष्ठ: 162
17वही, पृष्ठ: 10
18वही, पृष्ठ:-52
19वही, पृष्ठ:-77
20वही, पृष्ठ:-09
21वही, पृष्ठ:-09