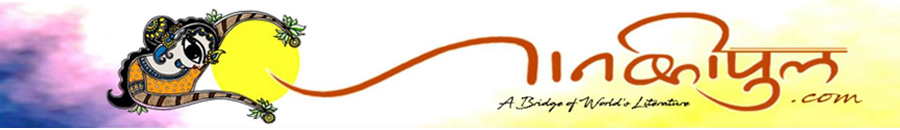हिंदी में अनूदित साहित्य का विस्तार हुआ है. बड़े पैमाने पर विश्व साहित्य हिंदी में लगतार उपलब्ध हो रहा है. लेकिन अनुवाद का स्तर, उसके लिए मिलने वाला मेहनताना जैसे मुद्दे लगातार विवाद के विषय रहे हैं. स्वतंत्र मिश्र की यह ‘स्टोरी‘ इन्हीं कुछ पहलुओं के विश्लेषण का प्रयास करती है. एक दिलचस्प स्टोरी- जानकी पुल.
========================================================================
‘प्रकाशक प्रति शब्द 10 या 15 पैसे देता है. इसके बाद आप उम्मीद करें कि बढ़िया अनुवाद हो जाए. क्या यह संभव है?’
विश्व क्लासिकल साहित्य श्रृंखला (राजकमल प्रकाशन) के संपादक सत्यम के ये शब्द उस बीमारी की एक वजह बताते हैं जिसकी जकड़ में हिंदी अनुवाद की दुनिया आजकल है. अनुवाद यानी वह कला जिसकी उंगली पकड़कर एक भाषा की अभिव्यक्तियां दूसरी भाषा के संसार में जाती हैं और अपने पाठकों का दायरा फैलाती हैं. लेकिन इस कला की सेहत आजकल ठीक नहीं. जानकारों के मुताबिक हिंदी में होने वाले अनुवाद का स्तर बहुत खराब है. इसके चलते दूसरी भाषा की अच्छी रचनाओं को हिंदी में पढ़ने का आनंद काफी हद तक जाता रहता है. जैसा कि पुस्तक समीक्षक पंकज चौधरी कहते हैं, ‘कई बार अंग्रेजी से हिंदी में आई कोई किताब पढ़कर लगता है कि इससे अच्छा तो अंग्रेजी में मूल किताब ही पढ़ ली जाती.’
कहानीकार प्रभात रंजन का अनुभव अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है. वे कहते हैं, ‘पेंगुइन जैसा बड़ा प्रकाशक डिमाई आकार के एक पन्ने (औसतन 300-350 शब्द) के लिए 80 रुपये मेहनताना देता है. राजकमल और वाणी प्रकाशन का रेट थोड़ा ठीक है. वे प्रति शब्द के लिए 40 पैसे देते हैं.’ पेंगुइन प्रकाशन में हिंदी संपादक की जिम्मेदारी संभाल चुके सत्यानंद निरुपम कहते हैं, ‘प्रकाशक प्रति शब्द के लिए 22 पैसे मेहनताना देते हैं जबकि गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) एक रुपये प्रति शब्द या इससे ज्यादा भी दे देते हैं. जबकि साहित्य की सामग्री का अनुवाद एनजीओ की सामग्री की तुलना में कहीं ज्यादा कठिन है.’
लेकिन अनुवाद की बदहाली का कारण सिर्फ कम मेहनताना नहीं. विशेषज्ञता की कमी भी इसके लिए जिम्मेदार है. सत्यम कहते हैं, ‘यूरोप में विशेषज्ञ अनुवादकों की लंबी परंपरा रही है. मसलन चेखव का अनुवाद करने वाले उनके साहित्य के शोधार्थी रहे हैं. उनपर लगातार लिखने या जानने वाले लोगों को ही यह जिम्मा मिलता रहा है. लेकिन भारत में आपको हजारों उदाहरण ऐसे मिल जाएंगे जिसमें अनुवादकों को अनुवाद के विषय की कोई जानकारी नहीं होती है. यही वजह है कि वे ‘हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत’ गाने में कोई संकोच नहीं करते.’
प्रकाशकों द्वारा अनुवादकों का नाम नहीं दिया जाना भी एक बड़ा कारण है. ‘गीतांजलि के हिंदी अनुवाद’ पुस्तक के लेखक देवेंद्र कुमार देवेश कहते हैं, ‘प्रकाशक अनुवादकों का नाम किताब में शामिल नहीं करना चाहते.’ इसका कारण बताते हुए वे कहते हैं, ‘दरअसल वे अनुवाद के काम को दोयम दर्जे का मानते हैं. खासतौर पर बांगला से हिंदी में अनूदित किताबों में नाम देने की परंपरा रही ही नहीं है. नाम दिए जाने से अनुवादकों की जिम्मेदारी तय होती है और जाहिर सी बात है कि वे काम को गंभीरता से लेते हैं.’ कमोबेश यही आलम अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में भी है. एक अनुवादक और लेखक नाम न छापने की शर्त पर बताते हैं कि अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के काम को शुरू करने वाला प्रभात प्रकाशन अपने अनुवादकों का नाम सामान्य तौर पर किताब में शामिल नहीं करता.
यही वजह है कि अनुवादक विमल मिश्र अनुवादकों की जिम्मेदारी तय करते हुए कहते हैं, ‘मूल रचनाकार अपनी रौ में लिखता जाता है, उसपर कोई बंदिश नहीं होती. लेकिन अनुवादक को रेलगाड़ी की तरह पटरी पर चलना पड़ता है.’ वे आगे जोड़ते हैं, ‘जैसे इंजन के ड्राइवर की जिम्मेदारी होती है मुसाफिरों को उनके गन्तव्य तक सुरक्षित पहुंचाने की, ठीक वैसी ही जिम्मेदारी अनुवादक की होती है मूल रचना के भाव को अनूदित रचना में समेकित करने की. अनुवादक को जवाब देना पड़ता है – प्रकाशक को, पाठकों को और मूल पुस्तक के रचनाकार को.’
हालांकि जब हम मुद्दे का दूसरा पहलू यानी प्रकाशकों को टटोलते हैं तो समस्या की एक और ही वजह सामने आती दिखती है. वाणी प्रकाशन के मालिक अरूण माहेश्वरी कहते हैं, ‘काम और पैसे देने वालों की कोई कमी नहीं है. हमने मंटो की कहानी उर्दू से हिंदी में कराई. अनुवादक महोदय ने चवन्नी नामक पात्र को चन्नी कर दिया. इसमें पैसे का मामला कहां है? हम मेहनताना तय करना अनुवादकों पर छोड़ देते हैं. हकीकत तो यह है कि अनुवाद की किताबें हमारे लिए मुनाफा देने वाली नहीं होती हैं.’ ऐसा क्यों, के जवाब में माहेश्वरी कहते हैं, ‘अनुवाद की किताब तैयार करने में अनुवादक, प्रूफ रीडर और संपादक को अलग-अलग पैसा देना होता है.’ अनुवादकों को मुंहमांगी कीमत देने के नाम पर माहेश्वरी महात्मा गांधी के पौत्र और प. बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी का नाम गिनाते हैं. गांधी ने वाणी प्रकाशन के लिए विक्रम सेठ की किताब ‘ए सुटेबल ब्यॉय’ का अनुवाद किया है.
लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसे उदाहरण इक्का-दुक्का हैं और ज्यादातर अनुवादक गोपाल कृष्ण गांधी की तरह अपना मेहनताना खुद तय करने जैसी स्थिति में नहीं होते. रही बात कम मुनाफे की तो अगर ऐसा होता तो इस समय बाजार में अनुवादित सामग्री की जो बाढ़ आई हुई है वह नहीं दिखती. अंग्रेजी के प्रकाशक पेंगुइन और हार्पर कॉलिन्स इस काम को बड़े पैमाने पर कर रहे हैं. सत्यम कहते हैं, ‘ज्यादातर मामलों में अनुवाद मशहूर किताबों का होता है. अंग्रेजी के बड़े लेखकों की किताब का हिंदी में अनुवाद कराया जाता है इसलिए लाइब्रेरी से खरीद बड़े पैमाने पर हो जाती है. इन किताबों के अनुवाद के कई संस्करण प्रकाशित होते हैं और इनसे प्रकाशक लंबे समय तक मुनाफा कमाते हैं.‘
वजहों पर भले ही एकराय न हों, इस पर सब सहमत हैं कि अनुवाद का स्तर गिरा है. अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद के मामले में ऐसे भी कई उदाहरण मिल जाते हैं, जहां दो शब्दों से लेकर तीन-तीन पैराग्राफ या कई पन्ने छोड़ दिए जाते हैं. अंग्रेजी के कई मुहावरे जिनका हिंदी में अनुवाद हो सकता है और जो पाठकों की दिलचस्पी बढ़ाने में मददगार हो सकते हैं, उन्हें अनुवादक हिंदी पाठकों के स्तर का हवाला देकर छोड़ देते हैं. इसे समझने के लिए यहां यथार्थवाद के प्रवर्तक और प्रसिद्ध फ्रांसीसी लेखक स्तांधाल के सबसे चर्चित उपन्यास ‘सुर्ख और स्याह’ से एक उदाहरण का सहारा लिया जा सकता है. ‘सच, बस सच, अपने पूरे तीखेपन के साथ’ – दांतों. उपन्यास में विभिन्न अध्यायों की शुरुआत में ऐसा ही कोई पद्यांश या सूक्ति कथन दिया गया है जिसके साथ किसी विख्यात हस्ती का नाम है. ये उपन्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. मगर हिंदी में पहली बार प्रकाशित अनुवाद से ये नदारद थीं.
अनुवाद में लापरवाही का यह सिलसिला अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद तक ही सीमित नहीं. बांगला के कई क्लासिक उपन्यासों के अनुवादित संस्करण दशकों से हिंदी पाठकों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे हैं. लेकिन इनमें भी बड़ी भूलें मौजूद हैं. 20 वें पुस्तक मेले में शरतचंद्र और रवीन्द्रनाथ ठाकुर के उपन्यासों के नये हिंदी अनुवाद का लोकार्पण किया गया. इन किताबों का नये सिरे से अनुवाद कराने की जरूरत पर राजकमल प्रकाशन के मालिक अशोक माहेश्वरी का कहना हैं, ‘ये किताबें अब रॉयल्टी से बाहर हो चुकी हैं. मगर इन किताबों के जो हिंदी संस्करण बाजार में बिक रहे हैं, वे आधे-अधूरे हैं. उनके अनुवाद बहुत खराब हैं. पन्ने के पन्ने गायब हैं. बांगला में कुछ कहा गया है और हिंदी अनुवाद में कुछ और.’ राजकमल से प्रकाशित ‘पथ का दावा’ के अनुवादक विमल मिश्र किताब की भूमिका में लिखते हैं, ‘शरत् बाबू के उपन्यास ‘पथेर दाबी’ का हिन्दी अनुवाद ‘पथ का दावा’ होगा न कि ‘पथ के दावेदार’. दरअसल इस उपन्यास के कथानक का मूल आधार है ‘पथ का दावा’ नाम की समिति है. हिन्दी के ‘दावेदार’ शब्द के लिए बंगला में ‘दाबिदार’ शब्द है.‘
खराब अनुवाद की एक बड़ी वजह अनुवादकों में नजरिये का अभाव होना भी है. मसलन किसी खास समाज में किसी शब्द का क्या मतलब है, इसे जाने-समझे बगैर अनुवाद कर देने से अर्थ का अनर्थ होना तय है. दिल्ली विश्वविद्यालय में एम.ए. अंग्रेजी का ही एक हिस्सा ’कंपरेटिव लिटरेचर’ में कथाशिल्पी मुंशी प्रेमचंद ‘गोदान’ का अंग्रेजी अनुवाद पढ़ाया जा रहा है. किताब का नाम गोदान की व्याख्या करते हुए अनुवादक ने ‘अ गिफ्ट ऑफ काउ’ लिखा है जबकि इसका सटीक अनुवाद ‘ऑफरिंग ऑफ अ काऊ’ होगा. अपने किसी प्रियजन के मरने के बाद ब्राह्मण आत्मा को मुक्त करने के नाम पर यजमान पर दान-दक्षिणा के लिए दबाव बनाता है. ब्राह्मण इसे यजमान की इच्छा पर नहीं छोड़ता है. ‘गोदान’ उपन्यास का पूरा कथानक ही वर्णवादी व्यवस्था की इस कुरीति के खिलाफ है. इस बारे में वरिष्ठ पत्रकार राजेश वर्मा कहते हैं, ‘अनुवाद हमेशा भाव का होता है. शब्द का अनुवाद करने की कोशिश करेंगे तो हमेशा गड़बड़ियां पैदा होंगी.‘
एक और अहम बात यह है कि तीन-चार दशक पहले तक कई नामी-गिरामी साहित्यकार व्यापक स्तर पर अनुवाद किया करते थे. उनका काम बाकी लोगों के लिए मिसाल होता था. अशोक माहेश्वरी अनुवादकों की फेहरिस्त सामने रखते हुए मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, निर्मल वर्मा और द्रोणवीर कोहली जैसे नामवर साहित्यकारों का भी नाम लेना नहीं भूलते.
तो फिर क्या वजह है कि आज नामचीन साहित्यकार अनुवाद की कला से दूर होने लगे हैं? इसके जवाब में अशोक माहेश्वरी कहते हैं, ‘आज साहित्यकारों के लिए अनुवाद करना रोजी-रोटी का विकल्प नहीं रह गया है. उनके सामने विश्वविद्यालय में पढ़ाने से लेकर फिल्म और टेलीविजन की दुनिया में पटकथा लेखन के दरवाजे खुल गए हैं.’
दरअसल अनुवाद या तरजुमा सिर्फ एक भाषा की सामग्री को दूसरी भाषा में बदल देने की कला भर नहीं है. अनुवाद के जरिए एक भाषा में कहीं गई बात, उसमें छुपे या प्रकट भावों को बहुत ही संजीदगी से दूसरी भाषा में अनूदित करना होता है. सत्यानन्द निरूपम कहते हैं, ‘अनुवाद के जरिये आप एक संस्कृति का भी अनुवाद कर रहे होते हैं. अगर यह काम ठीक से न हो तो ऐसे में निश्चित तौर पर एक भाषा से दूसरी भाषा की समृद्धि का मामला तो पिछड़ेगा ही, अनूदित किताबों के बाजार की संभावनाएं भी कमजोर होंगी.’
‘तहलका’ से साभार