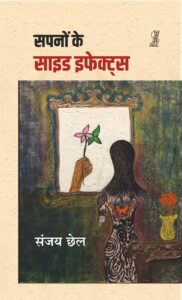आज अशोक वाजपेयी ने श्रेष्ठता और लोकप्रियता को लेकर ‘जनसत्ता’ में अपने स्तंभ ‘कभी-कभार’ में अच्छा लिखा है. बहसतलब- जानकी पुल.
===========================
लोकतंत्र और आधुनिक संसार दोनों में संख्या का बड़ा महत्त्व है। बाहुबल और धनबल आदि का इस्तेमाल लोकतंत्र में अंतत: संख्याबल पाने के लिए किया जाता है।
जिसके पाले में अधिक संख्या में वोट, वह विजयी: जो संसद या विधानसभा में अधिक संख्या जुटा ले वह सत्तारूढ़। लोकप्रियता के जितने मापदंड दृश्य पर हैं वे सभी संख्या को मूल आधार बनाते हैं। अखबार और टीवी चैनल की लोकप्रियता उसके पाठकों और दर्शकों की संख्या से आंकी जाती है और फिर यही लोकप्रियता उनके विज्ञापन बटोरने और धनार्जन करने का कारण बनती है।
ऐसे लेखक हैं जो अपनी वरीयता इस आधार पर मानते हैं कि उनके पाठकों की संख्या अधिक है। कई बार किसी पुस्तक की प्रतियां अधिक बिकने से उसे महत्त्वपूर्ण मान लेने की वृत्ति भी उभरती रहती है। संख्या पर आधारित लोकप्रियता अपने आप में एक सचाई है, पर उतना ही सच यह विडंबना भी है कि कम से कम हमारे साहित्य में लोकप्रियता और महत्त्व का संगम कम ही हो पाया है। मैथिली शरण गुप्त, प्रेमचंद, दिनकर, बच्चन आदि लोकप्रिय रहे हैं, पर वे बिरले हैं और अपवाद ही माने जा सकते हैं। हमारे बड़े लेखकों में से अधिकांश- निराला, प्रसाद, अज्ञेय, शमशेर, मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय, निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, कृष्ण बलदेव वैद आदि लोकप्रियता के संख्यावाची आयाम में अल्पसंख्यक ही हैं। इससे यह नतीजा निकालना शायद अधीरता होगी कि हिंदी में महत्त्व अधिकतर लोकप्रियता से परे ही रहा आया है। पर इस विडंबना को अलक्षित नहीं जाना चाहिए। शायद बांग्ला, मलयालम, कन्नड़ आदि में ऐसी विडंबना या तो नहीं है या उतनी तीखी नहीं जितनी हिंदी में। यह कहना शायद सही न हो कि इधर हिंदी में लोकप्रियता का आतंक तेजी से बढ़ रहा है। बाजार के विस्तार का एक लक्षण यह भी है। बल्कि एक तरह का बाजारूपन धीरे-धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। बाजार में संख्या एक अत्यंत वांछनीय तत्त्व है।
मेरे पास एक प्रकाशक ने, जिनकी ईमानदारी पर शक करने का कोई कारण नहीं है, मेरे एक कविता संग्रह और आलोचना की एक पुस्तक की साल भर बनी रॉयल्टी का एक चेक भेजा, जो सात सौ रुपए का है। बड़े लेखक और कथाकार निश्चय ही इतनी ही अवधि के लिए रॉयल्टी का बड़ा चेक पाते होंगे। यह क्लेश तो नहीं होता कि मेरी पुस्तकें इतनी कम क्यों बिकती हैं: जो लिखता हूं और जैसे लिखता हूं उसके पाठक अधिक होंगे, इसकी संभावना शायद अव्वल ही कम है। दूसरे, हमारे प्रकाशक पाठक जुटाने के लिए कोई निश्चित और थोड़ी आक्रामक नीति भी नहीं अपनाते। तीसरे, संख्या बढ़ाने के लालच या उत्साह में अपनी शैली, विधा और अनुभव को बदलना संभव नहीं है। अम्बर्तो इको ने कहीं कहा है: हम अपनी एक संभव दुनिया बनाते हैं और सामने रखते हैं। बोतल में संदेश रख कर समुद्र में बहाने की तर्ज पर। वह कितनों तक और कहां पहुंचती है इस पर हमारा बस नहीं। हम अपनी दुनिया और अपनी जमीन छोड़ नहीं सकते। लिखने की जिद है, समझे जाने की आकांक्षा और उम्मीद भी। पर अगर आपका भाग्य अल्पसंख्यक बन कर रह जाने का है तो वही सही। साहित्य हमेशा निराशा का कर्तव्य होता है, आज भी है और आगे भी रहेगा। अच्छा यह है कि यह निराशा आपको साहित्य से विरत नहीं करती और आप लिखना छोड़ कर कुछ अधिक उपयोगी और लोकप्रियता की संभावना वाला विकल्प नहीं अपनाते। निराश हैं, पर अपनी जमीन पर जमे हुए हैं, शायद थोड़ी बेशर्मी से, साथ ही साथ अपने को यह बराबर याद दिलाते हुए कि यह अल्पसंख्यकता जरूरी नहीं है कि महत्त्वपूर्ण होने की कोई गारंटी हो।