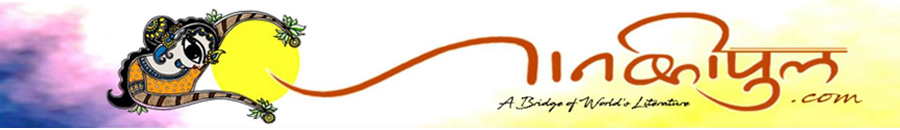समकालीन कविता क्या अपने समय-समाज का रूपक है? क्या समकालीन कवि आधुनिक हिंदी कविता की छायाओं से मुक्त हो चुका है? क्या देश की बदलती राजनीति को समकालीन कविता के माध्यम से समझा जा सकता है? अशोक कुमार पांडे का यह लेख कुछ ऐसे ही विचारोत्तेजक सवालों को उठाता है- जानकी पुल.
नब्बे का दशक स्वतन्त्र भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण विभाजक रेखा है. सोवियत संघ के विघटन के साथ जहाँ एक तरफ समाजवादी राज्य का स्वप्न खंडित हुआ वहीं दूसरी तरफ देश के भीतर नेहरूयुगीन अर्थव्यवस्था को तिलांजलि दे नई आर्थिक नीतियों के नाम से जो नीति लागू की गयी उसने भारत को विश्व साम्राज्यवाद से नाभिनालबद्ध कर दिया. ऐसा नहीं कि इसके पहले जो नीतियाँ लागू थीं वे किसी समतामूलक समाज की स्थापना के उद्देश्य से परिचालित थीं, लेकिन दो-ध्रुवीय विश्व अर्थव्यवस्था में सोवियत ब्लाक की उपस्थिति और देश में एक मजबूत समाजवादी आंदोलन की उपस्थिति ने राज्य पर थोड़ा नियंत्रण तो रखा ही था. हालाँकि भारतीय लोकतंत्र से मोहभंग तो साठ के दशक में ही शुरू हो गया था और सत्तर का दशक आते-आते नक्सलबारी के रूप में जो जनउभार सामने आया था उसका प्रतिबिम्बन साहित्य में भी साफ़ दिखाई दिया था. मुक्तिबोध अगर रक्तपायी वर्ग से बुद्धिजीवियों की नाभिनालबद्धता देख पा रहे थे तो सत्तर और अस्सी के दशक का कवि उसके खिलाफ पूरे दम-ख़म के साथ खड़ा था और सत्ता व्यवस्था को चुनौती दे रहा था. कुमार विकल, गोरख पांडे, आलोक धन्वा जैसे वामपंथी और नक्सल समर्थक कवि ही नहीं अपितु धूमिल जैसे गैर वामपंथी कवियों का स्वर भी व्यवस्था के प्रखर विरोध से भरा हुआ था. लेकिन इस विरोध की खासियत थी इसमें अन्तर्निहित एक प्रचंड आशावाद. दुनिया के शीघ्र बदल जाने का एक आत्मविश्वास और इसका हिस्सा होने की जिद. ज़ाहिर तौर पर यह उस दौर की राजनीतिक हकीक़त से उपजा था. नक्सलवादी आंदोलन की विफलता फिर आपातकाल और उसके बाद सम्पूर्ण क्रान्ति के नाम पर चले आंदोलन की विफलता, सोवियत संघ का बिखराव, एक ध्रुवीय विश्व के सरगना के रूप में विश्व साम्राज्यवाद के अनन्य नायक की तरह अमेरिका के उद्भव तथा भारतीय शासक वर्ग के उसके समक्ष सम्पूर्ण समर्पण ने नब्बे के दशक में जो सामाजिक-राजनैतिक-आर्थिक परिस्थितियाँ उपस्थित कीं उनके प्रभाव में उसका चेहरा और उसकी अंतर्वस्तु को अपने पिछले दौर से अलग होना ही था. यहाँ उस प्रचंड आशावाद का ताप मद्धम पड़ा, चिंताएँ और गहरे रूप में सामने आईं, एक निराशा और दुःख का प्रतिबद्ध कवियों की कविताओं में दिखाई दी तों तमाम लोगों के विश्वास सोवियत संघ के विघटित होने के साथ ही खंडित हुए और उन्होंने किसी आमूलचूल परिवर्तन की उम्मीद छोडकर अपनी दूसरी राह चुन ली. हम आगे उन नयी प्रवृतियों और कमजोर पड़ चुकी कुछ पुरानी प्रवृतियों के उद्भव और उनके स्रोतों पर भी विस्तार से बात करेंगे.
नब्बे के दशक के बिल्कुल आरंभिक दौर में इंडिया टुडे में प्रकाशित अस्सी के दशक के प्रमुख कवि कुमार अम्बुज की कविता ‘क्रूरता’ इस दौर की कविताओं की प्रवृति को स्पष्टतः रेखांकित करती है. अपनी पूर्ववर्ती कविता के तीव्र स्वर से अलग यह कविता समाज में वर्चस्व जमाती जा रही शक्तियों की मंशा का खुलासा करती है. अपने बेहद सब्लाइम ट्रीटमेंट के साथ यह कविता नव उदारवाद के मानवविरोधी चरित्र को रेशा-रेशा खोलती है.
तब आएगी क्रूरता
पहले ह्रदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी
फिर घटित होगी धर्मग्रंथो की व्याख्या में
फिर इतिहास में और
भविष्यवाणियों में
फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी
….वह संस्कृति की तरह आएगी,
उसका कोई विरोधी नहीं होगा
कोशिश सिर्फ यह होगी
किस तरह वह अधिक सभ्य
और अधिक ऐतिहासिक हो
…यही ज्यादा संभव है कि वह आए
और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना
पहले ह्रदय में आएगी और चेहरे पर न दिखेगी
फिर घटित होगी धर्मग्रंथो की व्याख्या में
फिर इतिहास में और
भविष्यवाणियों में
फिर वह जनता का आदर्श हो जाएगी
….वह संस्कृति की तरह आएगी,
उसका कोई विरोधी नहीं होगा
कोशिश सिर्फ यह होगी
किस तरह वह अधिक सभ्य
और अधिक ऐतिहासिक हो
…यही ज्यादा संभव है कि वह आए
और लंबे समय तक हमें पता ही न चले उसका आना
यहाँ नब्बे के दशक में पैर जमाते सांस्कृतिक साम्राज्यवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद दोनों की पदचाप साफ़ सुनाई देती है और साथ ही इसके प्रभावों को जिस तरह अम्बुज रेखांकित करते हैं वह कविता की उस ताक़त को बताता है जिससे वह भविष्य के खतरों को देख-समझ पाती है तथा समाज को उसके प्रति आगाह करती है. इस कविता में दिख रही निराशा को समझने के लिए हमें डा नामवर सिंह के भाषण की इन पंक्तियों को याद करना होगा – ‘जो लोग कलकत्ते में हैं और इस वामपंथी सरकार को देखकर समझते हैं कि हिन्दुस्तान में भी क्रान्ति या समाजवाद आया हुआ है तो मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ी सी निराशा बचाए रखो. वह समझ देगी, विवेक देगी और ताक़त देगी. घनघोर आशावाद तुम्हें धाराशायी करेगा. कवि है जो सतर्क रहता है. आत्म प्रवंचना है आशावाद, इसीलिए उस निराशावाद को बचाए रखो.’[i]नब्बे के दशक के बाद की कविता इसी ‘सतर्क निराशावाद’ की कविता है. यह अलग बात है कि कहीं-कहीं ‘सतर्कता’ सयानेपन में बदल जाती है तों कहीं-कहीं ‘निराशावाद’ अवसरवाद में.
लेकिन इस तथ्य के बावजूद इस दशक की कविता का कोई इकहरा चेहरा प्रस्तुत करना सरलीकरण होगा. वाम की तात्कालिक पराजय, पश्चिम में इतिहास के अंत की घोषणाओं के साथ उत्तरआधुनिकता के बढ़ते वर्चस्व, देश के तमाम हिस्सों में उग्र आन्दोलनों के प्रभाव, बाज़ार के लगातार पूँजी केंद्रित होते जाने के साथ एक ध्रुवीय विश्व के नेता अमेरिकी साम्राज्यवाद के साथ भारती शासक वर्ग के गठबंधन और देश में साम्प्रदायिक शक्तियों की ताक़त में लगातार बढोत्तरी के प्रभाव में हिन्दी साहित्य में भी अनेकानेक प्रवृतियाँ जन्मीं. यही कारण है कि इस युग के लिए कोई एक नाम दे पाना आलोचकों के लिए संभव नहीं हुआ. उस समय से लेकर इक्कीसवीं सदी के पहले दशक के बीच तक लिखी गयी कविताओं में अलग-अलग तरह की तमाम प्रवृतियाँ दिखती हैं. एक तरफ वाम अब भी विचार के रूप में संघर्ष तथा प्रतिरोध के आकांक्षी कवियों के लिए महत्वपूर्ण था तो दूसरी तरफ खुद को वाम कहने वाले तमाम कवि अस्मिताओं की पहचान पर जोर देने वाले विमर्शों की कविताएँ लिख रहे हैं. दलित और स्त्री विमर्श इस दौर में बेहद महत्वपूर्ण होकर उभरे हैं. साथ ही सोवियत संघ के टूटने के साथ बहुत सारे कवियों और आलोचकों ने वाम का लबादा उतार कर कला और एक खास तरह की लक्ष्यहीन परन्तु सुन्दर कविता का सहारा लिया. इसे ठीक-ठीक कलावाद कहना सही नहीं होगा. क्योंकि अपनी कला की गुणवत्ता के स्तर पर वह वहाँ भी नहीं पहुंचती लेकिन इसकी लाक्षणिकता इसके वाम विरोध में है. उद्देश्यहीन नास्टेल्जिया, दार्शनिक प्रलाप, दैहिक प्रेम, अराजनीतिक आदर्शवाद और दंत नख विहीन मानवतावाद से प्रेरित इन कविताओं को ‘वैश्विक स्तर’ का बताने वाले आलोचकों की भी कोई कमी नहीं. हम आगे इन प्रवृतियों और इनके उभरने के कारणों पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे.
इस दौर में स्त्री विमर्श और दलित विमर्श के उभार के साथ एक और परिघटना बेहद महत्वपूर्ण तरीके से सामने आई है. वाम कही जाने वाली धारा का साम्प्रदायिकता विमर्श तक सिमटते जाना. नब्बे के दशक में बाबरी मस्जिद विध्वंस और देश भर में लगातार गहराती जा रही साम्प्रदायिकता के बरक्स कविता में इसकी मुखालफत ज़रूरी भी थी और अपरिहार्य भी. और यह कहना होगा कि हमारे कवियों ने यह भूमिका निभाई भी पूरी ताक़त से. एकांत श्रीवास्तव की ‘दंगे के बाद’ हो, बोधिसत्व की ‘पागलदास’ या पवन करण की ‘मुसलमान लड़के’ या फिर गोधरा के बाद लिखी गयी निरंजन श्रोत्रिय की कविता ‘जुगलबंदी’, इस दौर के लगभग सभी कवियों ने साम्प्रदायिकता के विरोध में बेहद सशक्त कविताएँ लिखी हैं. लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि इस दौर में वाम होने का अर्थ लगातार साम्प्रदायिकता विरोधी होने तक संकुचित होता चला गया. इस साम्प्रदायिकता विरोध में भी प्रमुख स्वर गाँधीवादी सर्व धर्म समभाव का विगलित स्वर था. धर्म की संस्था के खिलाफ खड़े होने या फिर ‘रक्तपायी वर्ग से इसकी नाभिनालबद्धता’ को रेशा-रेशा साफ़ करने की जिद यहाँ उतनी नहीं दिखती और इसीलिए स्वर बहुत धीमा, उदास और किसी पराजित वक्तव्य सा लगता है. इनका मूल स्वर उदासी का है.
इतना कह कर वे चुप हो गए
मुझे सरजू पार कराया और बोले-
जितना जाना मैंने
पागलदास की उदासी का कारण
कह सुनाया
अब जाने सरजू कि उसके दक्षिण तरफ
बस कर भी क्यो उदास रहे पागलदास। (बोधिसत्व की कविता पागलदास से)
मुझे सरजू पार कराया और बोले-
जितना जाना मैंने
पागलदास की उदासी का कारण
कह सुनाया
अब जाने सरजू कि उसके दक्षिण तरफ
बस कर भी क्यो उदास रहे पागलदास। (बोधिसत्व की कविता पागलदास से)
इस उदासी के कारण भी उस समय की स्थितियों में खोजे जा सकते हैं. एक तरफ वामपंथ की राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पराजय और दूसरी तरफ देश के भीतर सत्ता और समाज पर साम्प्रदायिक तत्वों का बढ़ता जा रहा नियंत्रण…इन दोनों के साथ ही उदारीकरण के नाम पर हो रहे आर्थिक बदलावों ने समाज के भीतर एक गहरी निराशा और पस्ती का जो भाव भरा था उसकी यह परिणिति स्वाभाविक ही थी. आप देखिये कि उर्दू की जुझारू परम्परा से आये कैफी आजमी भी जब अयोध्या पर अपनी प्रसिद्द नज्म लिखते हैं तो वहाँ भी यह उदासी साफ़ झलकती है. मैं इस उदासी को निश्चित तौर पर सकारात्मक कहना चाहूँगा. बस दिक्कत यह है कि उन कविताओं के साथ लिखी दूसरी कविताओं में अपने समय, समाज और राजनीति की जो मुकम्मल समझ और बदलाव की जो दिशा दिखानी चाहिए थी वह बहुत अस्पष्ट और भावुक है. इसकी एक अभिव्यक्ति बाज़ार से बाहर होते जा रहे उन ग्रामीण प्रतीकों और वस्तुओं के कविता में प्रवेश के रूप में हुई जो वस्तुतः पिछडी हुई तकनीकों की उपज थे और आर्थिक विकास के साथ उनका बाज़ार से बाहर होते जाना स्वाभाविक तो था ही साथ में कई बार उन लोगों के लिए भी मुक्तिदाता था जो इसका उपयोग कर रहे थे. लेकिन शहरों में रह रहे हमारे मध्यवर्गीय कवियों की गाँवों से जुड़ी स्मृतियों में ये वस्तुएँ गहरे समाई हुई थीं तो कविता में इनका प्रवेश किसी पवित्र प्रतीक की तरह हुआ. कुदाल, पिंजन, चूल्हा, कुल्हाडी जैसे विषयों पर तमाम कविताएँ लिखीं गयीं. लेकिन इनका एक पक्ष इनसे जुड़े हुए कारीगरों की बदहाली पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करना भी था. नई आर्थिक नीतियों के बाद के अंधाधुंध मशीनीकरण से जो शिल्पकार बदहाल होते जा रहे थे उनकी नियति और उनके संघर्षों पर इनमें से कुछ कविताएँ गंभीर प्रश्न भी खडी करती हैं. लेकिन ज्यादातर कविताएँ उन स्मृतियों को सहेजने से आगे नहीं जातीं.
एक समय तांय-तांय बजते कानों में /सर्द संगीत भरते पिंजन अब देह पर/दशहरा पूजन का निशान लिए देह पर/ कोनों में पड़े ताकते हैं टुकर-टुकर/कड़ेरे अब उन्हें पूछते ही नहीं
(पवन करण की कविता ‘पिंजन’)
मेरे घर में अब भी एक पीढा/चुपचाप पड़ा है बारजे पर.
(जितेन्द्र श्रीवास्तव की कविता पीढा)
यह नास्टेल्जिया कविता में उस पुराने समय की वेदना को तो दर्ज करती है लेकिन इसके आगे किसी सार्थक बहस को जन्म नहीं देती. इसी के साथ गाँव से शहर में बसे इन कवियों की ग्रामीण परम्पराओं और उनकी सहज मानवीयता का चित्रण करने वाली कविताएँ भी हैं जो आधुनिक समाज की अमानवीयता का अपने ढंग से प्रतिकार करती हैं. ऐसे ही जब नीलेश रघुवंशी ‘हंडा’ कविता में लिखती हैं ‘वह हंडा/ एक युवती लाई अपने साथ दहेज में/ देखती रही होगी रास्ते भर/ उसमें घर का दरवाजा/बचपन उसमें अटाटूट भरा था/ भरे थे तारों में डूबे हुए दिन’ तो यह महज नास्टेल्जिया नहीं रह जाती अपितु एक औरत के जीवन की सबसे बड़ी विडम्बना को रेखांकित करते हुए ऎसी स्मृति में बदल जाती है जो भविष्य के लिए दरवाजे खोलती है.
इस दौर में कविता की नागरिकता विस्तृत होकर महिलाओं और दलितों तक पहुँचना शुरू करती है. इस दशक की महिला कवियों का स्वर न तो ‘नीर भरी बदली’ वाला है, न ही ‘बुंदेले हरबोलों वाला’. यहाँ स्त्री का जीवन अपने पूरे आदमकद रूप में उसके संघर्षों और प्रतिकार के साथ आया है. ‘चौका’ कविता में अनामिका जिस तरह से ‘मैं रोटी बेलती /जैसे पृथ्वी/ ज्वालामुखी बेलते हैं पहाड़/ भूचाल बेलते हैं घर/ सन्नाटे शब्द बेलते हैं, भाटे समुंदर’ लिखती हैं या ‘हे परम पिताओं /परम पुरुषों/ बख्शो अब हमें बख्शो (स्त्रियाँ) लिखती हैं या सविता सिंह जब लिखती हैं कि ‘डरी रहती है बिस्तर में भी अपने पुरुषों के संग/ बेवजह ख़लल नहीं ड़ालती उनकी नींद में/ रहती हैं सेवारत बरसाती प्रेम सहिष्णुता/ चाहिए उन्हें वैसे भी ज्यादा शांति / बहुत कम प्रतिरोध अपने घरों में/ फिर भी/ अपने एकांत के शब्दरहित लोक में/ एक प्रतिध्वनि – सी / मन के किसी बेचैन कोने से उठती जल की तरंग-सी /अपने चेहरे को देखा करती है /एक दूसरे के चेहरे में /बनाती रहस्यमय ढंग से/ एक दूसरे को अपने सच का दर्पण.’ तो यह मर्दों की दुनिया में आजादी के लिए व्यग्र और तत्पर महिलाओं की आवाज़ बन जाती है. लेकिन दिक्कत तब होती है जब इस नए विमर्श को एक हिट फार्मूले की तरह प्रयोग किये जाने से स्त्री केंद्रित कविताओं की एक बाढ सी आ जाती है जिसमें स्त्री प्रश्न पर किसी गंभीर समझदारी या किसी गहरी चिंता की जगह एक तरह की सतही भावुकता और कालान्तर में पूरे स्त्री-मुक्ति को देह-मुक्ति के आख्यान में बदलकर उसका गुड-गोबर कर दिया जाता है. यह कविता में धीरे-धीरे जगह जमा रहे और अपने सवालों को लेकर जूझ रहे स्त्री स्वर को न केवल धुंधला करता है, बल्कि कई बार स्त्री विमर्श की आड़ में स्त्री-मुक्ति के सवाल को ही सरलीकृत कर देता है.
इसी तरह कविता में दलित स्वर का भी प्रवेश पूरे दम-ख़म के साथ होता है. अपनी एक कविता में बद्रीनारायण जब यह कहते हैं कि ‘आकाश में मेरा एक नायक है/राहू/ गगन दक्षिणावर्त में जग-जग करता/ धीर मन्दराचल-सा/ सिंधा, तुरही बजा जयघोष करता/
चन्द्रमा द्वारा अपने विरुद्ध किए गए षड़यन्त्रों को/ मन में धरे/ मुंजवत पर्वत पर आक्रमण करता /एक ग्रहण के बीतने पर दूसरे ग्रहण के आने की करता तैयारी/
वक्षस्थल पर सुवर्णालंकार, जिसके कांचन के शिरस्त्राण/ ब्रज के खिलाफ़ एक अजस्र शिलाखण्ड/ भुजाओं में उठाए/ अनन्त देव-नक्षत्रों का अकेला आक्रमण झेलता/
अतल समुद्र की तरह गहरा/ और वन-वितान की तरह फैला हुआ/ तासा-डंका बजाता/ और कत्ता लहराता हुआ ……. ऋगवेद के किसी भी मण्डल के अगर किसी भी कवि ने/ उस पर लिखा होता एक भी छन्द तो मुझे/ अपनी कवि कुल परम्परा पर गर्व होता’ तो वह कविता की एक नयी परम्परा की तलाश और उसकी स्थापना का ही उद्घोष है. इसी क्रम में मुसाफिर बैठा लिखते हैं कि
चन्द्रमा द्वारा अपने विरुद्ध किए गए षड़यन्त्रों को/ मन में धरे/ मुंजवत पर्वत पर आक्रमण करता /एक ग्रहण के बीतने पर दूसरे ग्रहण के आने की करता तैयारी/
वक्षस्थल पर सुवर्णालंकार, जिसके कांचन के शिरस्त्राण/ ब्रज के खिलाफ़ एक अजस्र शिलाखण्ड/ भुजाओं में उठाए/ अनन्त देव-नक्षत्रों का अकेला आक्रमण झेलता/
अतल समुद्र की तरह गहरा/ और वन-वितान की तरह फैला हुआ/ तासा-डंका बजाता/ और कत्ता लहराता हुआ ……. ऋगवेद के किसी भी मण्डल के अगर किसी भी कवि ने/ उस पर लिखा होता एक भी छन्द तो मुझे/ अपनी कवि कुल परम्परा पर गर्व होता’ तो वह कविता की एक नयी परम्परा की तलाश और उसकी स्थापना का ही उद्घोष है. इसी क्रम में मुसाफिर बैठा लिखते हैं कि
‘मुझे क्या था मालूम
कि/ हरि पर तो कुछेक प्रभुजन का ही अधिकार है/
और इस देवी मंदिर को/
ऐसे ही प्रभुजनों ने
अपनी ख़ातिर सुरक्षित कर कब्ज़ा रखा था. (मैं उनके मंदिर गया था)
कि/ हरि पर तो कुछेक प्रभुजन का ही अधिकार है/
और इस देवी मंदिर को/
ऐसे ही प्रभुजनों ने
अपनी ख़ातिर सुरक्षित कर कब्ज़ा रखा था. (मैं उनके मंदिर गया था)
इसी समय में प्रेमचंद गाँधी जैसे प्रतिबद्ध कवि इस पूरी अवधारणा को मानवमुक्ति की बड़ी लड़ाई के साथ जोडकर देख रहे थे लेकिन साथ ही दलितों का जीवन संघर्ष और उनकी वंचना भी उनकी कविताओं में जगह बना रहे थे.
हम क्षत्रिय नहीं थे लेकिन
पीढ़ियों तक लड़ते रहे गाँव की ख़ातिर
उस गाँव की ख़ातिर
जहाँ हमारे लिए कुँए के पास जाना भी वर्जित था
मंदिर को भी हम फ़ासले से ही धोक पाते थे
वह भी दरवाज़ा बंद होने के बाद
पीढ़ियों तक लड़ते रहे गाँव की ख़ातिर
उस गाँव की ख़ातिर
जहाँ हमारे लिए कुँए के पास जाना भी वर्जित था
मंदिर को भी हम फ़ासले से ही धोक पाते थे
वह भी दरवाज़ा बंद होने के बाद
हमारा और गाँव के मवेशियों का एक ही जल-स्रोत था
गाँव के मवेशी भी हम नहीं छू सकते थे
उनके मरने से पहले
यूँ गाँव-भर के खेतों में
उम्र भर खटती रहीं हमारी पीढ़ियाँ
यूँ खटते-खटते ही आ गई आज़ादी
हमारे बुज़ुर्गों को आज तक पता नहीं आज़ादी का (हमारा गाँव)
नब्बे के दशक के बाद ये प्रवृतियाँ विस्तार भी लेती हैं और कविता की नागरिकता के विस्तृत होने के साथ-साथ कुछ और नई प्रवृतियाँ साफ़ दिखाई देने लगती हैं. सोवियत संघ के विघटन का ‘हैंग़ ओवर’ कमजोर पडता है, बाज़ार का मनुष्यविरोधी रूप साफ़ सामने आने लगता है, सामाजिक न्याय की विसंगतियाँ दिखती हैं और संपदा की लूट के साथ-साथ सरकारों का जो क्रूर और दमनकारी चेहरा दिखाई देता है वह कवियों को अपने तरीके से प्रभावित करता है. एक तरफ राजेन्द्र यादव जैसे तमाम लोग कविता को खारिज कर रहे हैं तों दूसरी तरफ विजय बहादुर सिंह जैसे तमाम लोग छंद की वापसी की बात कर रहे हैं. कविता के वजूद को लेकर ही एक नई बहस शुरू होती है. इसी दौर में इंटरनेट एक प्रमुख माध्यम के रूप में सामने आता है और पाठकों के खत्म होते जाने के भयावह शोर के बीच कवियों की एक पूरी नयी और ताज़ा खेप सामने दिखाई देती है. इस दौर में जिन कवियों ने अपनी पहचान बनाई और हिन्दी कविता को प्रभावित किया उनमें शिरीष कुमार मौर्य, गीत चतुर्वेदी, विशाल श्रीवास्तव, गिरिराज किराडू, कुमार अनुपम, आर चेतनक्रांति, अंशु मालवीय, नीलोत्पल, राकेश रंजन, संज्ञा सिंह,
View 154 Comments