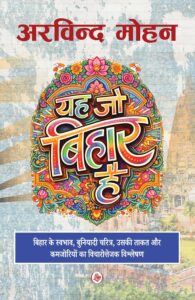‘वागर्थ’ पत्रिका के मई अंक में एक परिचर्चा प्रकाशित हुई है ‘समकालीन कथा साहित्य और बाजार’ विषय पर. इसमें मैंने भी सवालों के जवाब दिए थे. पत्रिका के सवालों के साथ अपने जवाब प्रस्तुत कर रहा हूँ. उनके लिए जिन्होंने न पढ़ा हो और जो पढना चाहते हों- प्रभात रंजन
====================
प्रश्न- कथा पुस्तकों की मांग अन्य विधाओं के बनिस्बत प्रकाशकों के यहाँ अधिक है, विशेष रूप से विवादास्पद या बोल्ड साहित्य की. इस दृष्टि से आज के कथा साहित्य का बाजार से भी कोई सम्बन्ध बनता है- घोषित या अघोषित रूप से.
उत्तर- सवाल के पहले हिस्से की यह बात तो सही है कथा पुस्तकों की मांग प्रकाशकों के यहाँ अधिक है. यह स्थिति कमोबेश हर भाषा की स्थिति है कि कविता से अधिक कथा साहित्य-उपन्यास की मांग अधिक है. अंग्रेजी में तो कहानी की पुस्तकें कम ही छपती हैं, वहां उपन्यास की मांग अधिक है. लेकिन यह कहना पूर्ण रूप से सही नहीं है कि विवादास्पद या बोल्ड साहित्य की ही मांग अधिक है. हालाँकि इस बात से इनकार भी नहीं किए जा सकता कि विवादास्पद या बोल्ड साहित्य लिखने की प्रवृत्ति बढ़ी है. विवादास्पद या बोल्ड लिखने से तात्कालिक तौर पर लोकप्रियता मिल जाती है. लेकिन साहित्य तो तात्कालिक लोकप्रियता के लिए नहीं लिखा जाता है, उसका यह उद्देश्य नहीं होना चाहिए. इसीलिए बोल्ड या विवादास्पद साहित्य को लेकर तात्कालिक रूप चर्चा हो जाती है लेकिन बहुत जल्दी इस तरह की कृतियाँ हमारे दिमाग से उतर भी जाती हैं.
जहाँ तक बाजार से साहित्य के रिश्ते की बात है तो यह थोडा जटिल मामला है. देखिये केवल बिकने के लिए साहित्य लिखने से लिखने वाले की आय में वृद्धि होती है, प्रकाशक की कमाई होती है मगर पाठक को इससे कोई फायदा नहीं होता. हम बसों में, ट्रेनों में ऐसे साहित्य को पढ़ते हैं और अक्सर उनको सँभालने की परवाह नहीं करते. जबकि साहित्य हमारे घर का हिस्सा होता है. हम अच्छे साहित्य को खरीदकर घर में रखते हैं, और उनको लेकर गर्व का अनुभव करते हैं.
लेकिन दूसरी तरफ यह भी है बाजार लेखक को आजाद करता है. मेरे लिए आदर्श स्थिति यह है कि लेखक को अपने लेखन के अलावा किसी तरह की नौकरी न करनी पड़े और उसका जीवन भी बेहतर ढंग से चल जाए. हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य बहुत बड़ी मात्रा में स्वतंत्र लेखकों द्वारा लिखा गया है. इसलिए मेरा मानना है कि अगर हिंदी पुस्तकों का बाजार बढेगा तो उससे लेखकों को आजादी मिलेगी, उनका सम्मान बढेगा. आज हिंदी ज्यादातर साहित्य पार्ट टाइम लेखकों द्वारा लिखा जा जा रहा है. इसके बेहतर भविष्य के लिए जरूरी है फुल टाइम लेखक सामने आयें.
प्रश्न-2 यदि हाँ, तो क्या आज कथाकार बाजार के दबाव में या ‘बिकाऊ’ होने के लिए जान-बूझकर कुछ बोल्ड या विवादास्पद लिखने की दिशा में मुड़ गया है?
उत्तर-2 कुछ हद तक यह बात सही है कि आज लेखक तात्कालिक लोकप्रियता के लिए ऐसा कुछ लिखना चाहता है जिससे उसे तात्कालिक प्रसिद्धि मिल जाए. मुझे कमलेश्वर जी की एक बात याद आती है. उन्होंने कहा था कि आज साहित्य के इतिहास में अमरता की चाह बढ़ी है रचना के इतिहास में कोई अमर नहीं होना चाहता. लेकिन मेरा यह निवेदन भी है कि बाजार का अर्थ केवल बिकना नहीं होता पाठकों से जुड़ना भी होता है. आज ऑनलाइन साइट्स के माध्यम से पाठक किताबें खरीद रहा है, वह ब्लॉग्स, वेबसाइट्स के माध्यम से हिंदी किताबों, लेखकों से जुड़ रहा है. यह बाजार का सकारात्मक पहलू है जो लेखकों-पाठकों के खोये हुए सूत्र को फिर से जोड़ने का काम कर रहा है.
प्रश्न-3 मसाला कथा-साहित्य का क्या सर्जनात्मकता से भी कोई सम्बन्ध बनता है या केवल कथा-वस्तु या कंटेंट के आधार पर ही यह साहित्य(?) चर्चा का अधिकारी हो गया है?
उत्तर-3 मसाला साहित्य आज से नहीं प्रेमचंद के जमाने से ही रहा है. इब्ने शफी उस जमाने में लिख रहे थे. वह एक दुनिया समानांतर है. उसे साहित्य तो कभी नहीं माना गया. नहीं माना जा सकता. लेकिन उसकी एक भूमिका रही है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता है. वह आरम्भ में पाठकों में पढने की रूचि पैदा करता है. मसाला साहित्य पढने वाले एक दिन गंभीर साहित्य की तरफ मुड़ते हैं. तुर्की भाषा का उदाहरण दिया जा सकता है. उस भाषा में जासूसी उपन्यासों का बड़ा बाजार है, बड़ा पाठक वर्ग रहा है. उसी पाठक वर्ग ने वहां ओरहान पामुक जैसे लेखक को भी बड़ा मुकाम दिया. जिनको बाद में नोबेल पुरस्कार भी मिला. मेरा मानना है कि लोकप्रिय साहित्य का होना भी जरूरी है उससे नए पाठक तैयार होते हैं. लेकिन इससे ज्यादा महत्व न उनका रहा है न दिया जाना चाहिए.
प्रश्न-4 ऐसे कुछ सर्जनात्मक और गैर-सर्जनात्मक कथाकारों के नाम?
उत्तर-4 हिंदी में कुछ ऐसे लेखक भी हुए जिन्होंने उच्च कोटि का साहित्य भी लिखा और जिनको आम पाठकों में अपार लोकप्रियता भी मिली. कुछ नाम लिए जा सकते हैं, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु, श्रीलाल शुक्ल, मनोहर श्याम जोशी, निर्मल वर्मा, उदयप्रकाश आदि. जो गैर-सर्जनात्मक लेखक हैं उनका नाम क्या लेना. पढने वाले इस अंतर को बखूबी समझ जाते हैं.
प्रश्न-5 क्या केवल बिकाऊ हो जाने से कोई चीज रचना और सर्जना के स्तर पर श्रेष्ठ मानी जानी चाहिए. यदि हाँ, तो लोकप्रिय लेखन और सर्जनात्मक लेखन का पार्थक्य कहाँ जायेगा और उसे कौन रेखांकित करेगा? इसे रेखांकित करने वाले आलोचक आज कहाँ हैं और वे कौन हैं? कुछ नाम?
उत्तर-5 केवल बिकाऊ होना श्रेष्ठता का पैमाना नहीं हो सकता है. आज अच्छे और बुरे का अंतर मिटता जा रहा है. यह दुःख की बात है. इसका एक कारण आलोचना की विधा का लगातार कमजोर होते जाना है. आलोचक आज हिंदी विभागों में प्रोमोशन के लिए लिख रहे हैं या पुरस्कारों के लिए. आलोचना विधा की यह गिरावट आज चिंता की बात है.
प्रश्न- 6 समकालीन परिदृश्य के तुमुल कोलाहल में ऐसे लेखकों के बीच नेटवर्किंग और मार्केटिंग के बहाने क्या अमरता की होड़ नहीं लगी है?
उत्तर-6 देखिये, प्रायोजित लेखन बहुत दिन टिक नहीं पाता. ऐसे कई लेखक हैं जो खूब पुरस्कार बटोर लेते हैं, बड़े-बड़े लेखकों की सम्मति प्राप्त कर लेते हैं. लेकिन ऐसा लेखन टिकाऊ होता है क्या? जब तक उनका प्रचार तंत्र रहता है तभी तब उनका हो-हल्ला भी रहता है. फिर सब भूल भाल जाते हैं. हाल के दिनों में ऐसे कई लेखकों-लेखिकाओं की कुछ दिन खूब चर्चा हुई. लेकिन जल्दी ही लोग भूल भी गए. नाम लेना सही नहीं होगा. सब जानते हैं.
प्रश्न-7 इन विकृतियों के बाहर कुछ सच्चे कथाकार और उनकी कृतियों के नाम अवश्य बताएँ ताकि नए पाठक कुहासे से बाहर आकर सच्ची सर्जनात्मक कृतियों को देख और पढ़ सकें.
उत्तर-7 ऐसी अनेक कृतियाँ हैं, जिनको पढने से हमेशा कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है, नई तरह की अनुभूति होती है. प्रेमचंद का उपन्यास ‘रंगभूमि’ है, वह आज के समय में अधिक प्रासंगिक लगता है, अज्ञेय का उपन्यास ‘शेखर: एक जीवनी’ है, फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास ‘मैला आँचल’, मोहन राकेश की कहानियां हैं, उनका नाटक ‘आषाढ़ का एक दिन’ है, धर्मवीर भारती का उपन्यास ‘सूरज का सातवाँ घोड़ा’ है, अमरकांत की कहानियां हैं, श्रीकांत वर्मा का कविता संग्रह ‘मगध’ है, धूमिल का कविता संग्रह ‘संसद से सड़क तक’ है, रघुवीर सहाय का कविता संग्रह ‘आत्महत्या के विरुद्ध’ है, मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास ‘कुरु कुरु स्वाहा’, ‘कसप’ हैं, मृदुला गर्ग का उपन्यास ‘कठगुलाब’ है, मैत्रेयी पुष्पा का उपन्यास ‘इदन्न मम’ है, अलका सरावगी का उपन्यास ‘कलिकथा वाया बाईपास’ है, उदय प्रकाश की कहानियां हैं. ये महज कुछ नाम हैं, हिंदी में अच्छी कृतियों की कमी नहीं है. मुझे मनोहर श्याम जोशी की बात याद आती है. वे कहा करते थे कि आरम्भ में ही लेखकों को 100 श्रेष्ठ कृतियों की सूची बना लेना चाहिए और उसे उनका ही बार-बार अध्ययन करना चाहिए. क्लासिक को हर बार पढना एक नए तरह के अनुभव से गुजरना होता है, हर बार हमें कुछ नया ज्ञान प्राप्त होता है.
================================