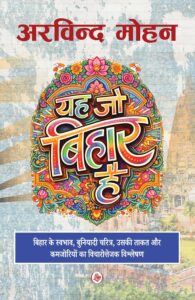मशहूर जर्मन कवि और लेखक राइनेर मारिया रिल्के, जो 1875 से 1926 तक हमारे बीच रहे। रिल्के की ज़िन्दगी एक बेचैन यायावर की तरह गुज़री। उन्होंने 30 कविता संग्रह, कहानियाँ, लेख, संस्मरण, समीक्षा और एक उपन्यास की रचना की। उनकी एक पुस्तक का हिंदी अनुवाद किया है राजी सेठ ने, जिसका नाम है ‘पत्र युवा कवि के नाम’। प्रस्तुत है पुस्तक का एक अंश : त्रिपुरारि कुमार शर्मा
प्रेम में होना अच्छा है, क्योंकि प्रेम दुर्गम है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को प्यार कर सके, यह संभवत: सबसे कठिन काम है, जो हम लोगों के जिम्मे है– एकदम आधारभूत काम– अंतिम प्रमाण और परिक्षा; बाकी सब कुछ तो वहाँ पहुंचने की तैयारी है। यही कारण है कि युवा लोग – जो हर क्रिया की शुरूआत में हैं – प्यार करने में सक्षम नहीं हैं। ये सीखने योग्य बातें हैं। अपने अकेले चिंतातुर, हडबड़ी भरे मन की सभी शक्तियों को एकाग्र करते हुए, अपने पुरे अंतर्तम से उन्हें प्यार करना सीखना चाहिए। सीखने का काल सदा लम्बा और अकेलेपन से घिरा होता है, इसलिए प्यार करने वालों को चिरकाल तक एक लम्बे गहरे और उत्कट किस्म के अकेलेपन में धकेल देता है।
प्यार का अर्थ घुल जाना, समर्पण कर देना या बन्ध जाना नहीं है (उस सम्मिलन का क्या अर्थ जिसमें दो व्यक्ति अस्पष्ट, अपरिष्कृत और असंबद्ध बने रहते हों,) बल्कि परिपक्व होने की ओर प्रस्थान है; अपने स्वत्व में कुछ होने का, एक संसार बन जाने का; दूसरे के निमित्त अपने भीतर एक पूरा संसार समेट लेने का। यह बहुत बड़ी बात है कि प्रेम अपने प्रस्फुटन के लिए एक उसी व्यक्ति पर अपना दावा रख रहा है, और बड़े विस्तारों के लिए एक उसी व्यक्ति को ही चुन और टेर रहा है। युवा लोगों को केवल इसी अर्थ में प्यार को ह्रदयंगम करना चाहिए। (to hearken and hammer day and night) घुल-मिल जाना, समर्पण करना या हर प्रकार की घनिष्ठता में प्रवृत होना, उनके लिए ठीक नहींजिन्हें अभी चिरकाल तक अपने) को बचाने और संचित करने की ज़रूरत है,) क्योंकि वहाँ तक पहुंच पाना एक पराकाष्ठा है जिसके लिए मनुष्यों के जीवन शायद ही कभी इतने विराट हो पायें।
पर यही तो है जो युवक लोग करना चाहते हैं। प्रेम की अनुभूति का एहसास होते ही (अपने स्वभाव की अधीरता के कारण) एक दूसरे पर झपट पड़ते हैं। अपने को छितरा लेते हैं, वैसे ही जैसा उनका वर्तमान जीवन है – गड्ड्मड्ड, अव्यवस्थित और दिशाहीन। इसकी क्या परिणति हो सकती है! खंडित चीज़ों के ढेर में से ज़िंदगी का क्या बनेगा, कहने को वह चाहे इसे भिन्नता कहें या आनंद या अपना भविष्य। दूसरे को पा लेने की चेष्टा में पहले तो वह अपने को ही गंवा बैठते हैं, फिर दूसरे को भी तथा अन्य कितने व्यक्तियों को जो आगमन के इच्छुक थे। कितने विस्तारों, कितनी संभावनाओं को वह नष्ट करते हैं। इस असफलता भरे संभ्रम में घिरे वह अपने निकट आती कितनी ही कोमल दृष्टिसंपन्न वस्तुओं को परे फेंक देते हैं। इस वस्तुस्थिति से क्या हाथ लग सकता है– क्षोभ, निराशा, हीनता या फिर रूढ़ि में पलायन। रपटीली जोखिम भरी सड़कों पर जैसे जगह-जगह जन शरणालय बना दिये जाते हैं, वैसे ही लोग रूढ़ि का सहारा लेने की कोशिश करते हैं। मनुष्य के जीवन अनुभव का कोई दूसरा क्षेत्र रूढ़ियों में इतना सीमित नहीं है जितना प्रेम। जीवन रक्षा के लिये तरह तरह के अविष्कार किये जाते हैं– नावें, तरण पंख इत्यादि। हर तरह का शरण्य खोजने में समाज अपने को मुख्यत: समर्थ पाता है, पर चुंकि प्रेमलिप्त जीवन को मुख्यत: अमोद-प्रमोद का साधन मान लेने की प्रवृत्ति है, इसलिए सस्ते, सुगम और सुरक्षित रास्ते चुन लिये जाते हैं, जैसे मनोरंजन के लिये और दूसरी चीज़ें।
असल में ज्यादातर युवक झूठा प्रेम करते हैं। (उदाहरणत: वह अपने स्वत्व का परित्याग करके आत्मसमर्पण कर देते हैं, सामान्य व्यक्ति हमेशा ऐसा ही करेगा) अपनी असफलता से फिर वह पीड़ित होते हैं और स्थिति को निहायत निजी तरह से संभालने और जीने योग्य बनाने की चेष्टा भी करते हैं। इस प्रक्रिया में ही वह समझ पाते हैं कि प्रेम की समस्याएं दूसरी महत चीज़ों की तरह, बाहरी तरीकों या ऐसे या वैसे समझौतों से सुलझाई नहीं जा सकती। वह एक इंसान से दूसरे इंसान के बीच बहती प्रश्नोन्मुखता है, जो कि एक बिलकुल नयी, विशिष्ट, पूरी तरह निजी और अंतरंग शैली की मांग करती है, पर ऐसा सम्भव नहीं हो पाता, क्योंकि उन दोनों का स्वत्व तो एक –दूसरे में गुम हो कर पहले ही अपनी परिसीमाएं खो चुका होता है। उनके पास कुछ भी अपना निजी नहीं रह जाता। तब, फिर वह नितांत अपने लिये कैसे कोई रास्ता ढूँढ सकते हैं। उनका एकांत तो पहले ही दफ्न हो चुका है।
वह लाचारियों से भरी पारस्परिकता में जीते हैं। सदाशयी मंसूबों के रहते अपने निकट आते परंपरागत समाधानों (जैसे विवाह) से बचने की कोशिश भी करते हैं पर पहले से कहीं ज्यादा पारंपरिक, अस्पष्ट और मारक विकल्पों का चुनाव कर बैठते हैं। तब तो वह पूरी तरह परंपरा से घिर जाते हैं। अपरिपक्व और अस्पष्ट घनिष्ठता में पगा हुआ हर कर्म सदा पारंपरिक होता है। तिस पर हर सम्बन्ध जो ऐसे संभ्रम में पोषित होता है, उसकी अपनी भी परंपराएं बन जाती हैं, चाहे वह कितना भी असाधारण क्यों न हो (सामान्य अर्थ में अनैतिक)। ऐसे में एक दूसरे से अलग हो जाना भी एक पारंपरिक समाधान ही कहा जायेगा– अनिजी, आकस्मिक, शक्तिहीन और असफल।
जो कोई भी गंभीरता से विचार करता है, जानता है कि मृत्यु का, प्रेम का, जो कि दुर्गम है, न तो कोई स्पष्टीकरण है न विकल्प! न किसी दिशा विशेष का कोई स्पष्ट निर्देश। इन दोनों स्थितियों में हम सदा अमुखर रूप से आच्छन्न रहते हैं। कोई सामान्य स्वीकृत नियम इस बारे में निर्धारित नहीं है, पर जिस प्रमाण में एक व्यक्ति की तरह हम जीवन की खोजबीन करते हैं, उसी प्रमाण में महत्तर चीज़ें हमारी आत्मीयता के घेरे में आती हैं। प्रेम जैसा दुर्गम कर्म हमसे जैसी अपेक्षाएं रखता है, वह जीवन से भी बृहत्तर किस्म की हैं। अनुभव के आरंभिक दिनों में हम इसकी समकक्षता में नहीं आ सकते। प्रेम को आसान हल्के–फुल्के खिलवाड़ के रूप में लेने – जिसके पीछे गंभीर से गंभीरतम व्यक्ति का भी असली रूप छिप सकता है – की अपेक्षा, यदि हम उसे ज्यादा सहिष्णुता और दीक्षा–भाव से लें, तो हमारे बाद आने वालों को वह उत्तानता और आलोक ज़रूर दिखेगा। बस, इतना ही काफी है।
किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सम्बन्ध की शुरुआत बेशक बिना किसी पूर्वाग्रह के स्वतंत्र रूप से होती है। सामने कोई बना–बनाया प्रतिरूप भी नहीं होता, फिर भी समय द्वारा किये गये परिवर्तनों में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी उस भीरू अनुभवहीनता में सहायक होती रहती हैं।
कोई भी किशोरी या स्त्री अपने आत्मप्रस्फुटन के काल में पुरुष के व्यवहार या दुर्व्यवहार का अनुकरण करती है, या उसके चुने हुए रुझानों या व्यवसायों की आवृत्ति करती है। संक्रमण काल की इस अनिश्चितता के बाद यह स्पष्ट होने लगता है कि इस प्रचुरता और विविधता को (हास्यास्पद सीमा तक) एक कृत्रिमता की तरह ओढ़े रहकर स्त्रियां अपनी असली आंतरिक प्रकृति का प्रक्षालन कर रही हैं और अपने को पुरुष जाति के कुप्रभावों से मुक्त कर रहीं थीं। स्त्रियों में जीवन दीर्घकालिक होता है, अधिक तत्पर, अधिक फलदायी, अधिक आश्वस्त, अधिक परिपक्व और गहराई में कहीं अधिक मानवीय; उस मनमौजी आरामपसंद पुरुष की अपेक्षा, जिस पर कभी भी, किसी भी रूप में अपनी सतह से नीचे खींचे जाने का भार नहीं पड़ता, दैहिक रूप तक में नहीं। वह दंभी, उतावला और अपनी प्राप्तियों को कमतर आंकने वाला होता है। तिरस्कार और यातनाओं के बीच, अपने गर्भ में संभाली गयी स्त्री की मानवीयता, उस समय पूरी तरह प्रकट होगी, जब वह अपनी बाहरी हैसियत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया में, मात्र स्त्री होने की मर्यादाओं से बाहर आ जायेगी। जो पुरुष इस प्रस्फुटन को नहीं जानते, वह चकित हो कर देखते रह जायेंगे।
किसी दिन (खास तो उत्तरी यूरोप के देशों में ऐसे आश्वस्त करने वाले लक्षण प्रकट हो रहे हैं) ऐसी लड़कियां या स्त्रियां होंगी, जिनके होने का अर्थ पुरुषपन के सम्मुख मात्र दूसरा ध्रुव उपस्थित करना ही नहीं होगा पर आत्मसंपन्न होना होगा। ऐसा कुछ जो शक्तियों या मर्यादाओं की बात को महत्व नहीं देता पर जीवन और यथार्थ के बीच स्त्री को एक मानवी की तरह अवस्थित करता है।
यह उत्तानता (पहले तो, पिछडे हुए पुरुष की इच्छा के विरूद्ध) प्रेम के अनुभव को बदलेगी, जो अब तक भूलों से भरा है। उसे आमूल साफ़ करेगी। इसके बाद जिस सम्बन्ध की पुनर्रचना होगी, वह एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के बीच होगा, न कि एक स्त्री एक पुरुष के बीच। यह विपुल मानवीय प्रेम (जो असीम हार्दिकता, कोमलता, सहिष्णुता और स्पष्टता से बंधने और मुक्त रखने की पारस्परिकता में अपने को परिपूर्ण करेगा) ही हमारा वांछित होगा, जिसकी तैयारी में हम आज इतनी यातनाएं सहते हुए भी संघर्षशील हैं। ऐसा प्रेम जिसमें दो एकांत सुरक्षित रहते हुए भी एक-दूसरे का अभिनंदन कर सकते हैं।