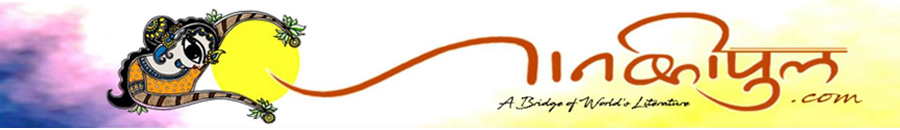कुछ लेखक ऐसे होते हैं जिनके पुरस्कृत होने से पुरस्कारों की विश्वसनीयता बनी रहती है. ऐसे ही लेखक उदय प्रकाश से दिनेश कुमार की बातचीत
आप हिन्दी के साहित्यिक सत्ता केन्द्रों के प्रति आक्रामक रहे हैं। साहित्यिक पुरस्कारों में इनकी अहम भूमिका होती है। बावजूद इसके आपको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसे कैसे परिभाषित करेगें?
उदय प्रकाश- मुझे भी आश्चर्य हुआ। कोई भी कलाकार या लेखक, जो व्यवस्था विरोधी लेखक के रूप में जाना जाता हो, ऐसे पुरस्कार की उम्मीद कर भी नहीं सकता। लेकिन दूसरे स्तर पर यह पुरस्कार मिलने के बाद मै थोड़ा सुरक्षित भी महसूस कर रहा हूं। मेरी दृष्टि में यह अघोषित आपातकाल का समय है। इस समय मेधा पाटकर, विनायक सेन जैसे मानवाधिकार के लिए बोलने और काम करने वालों को जो दूसरी तरह की ‘आइडेंटिटी” दी गई है उस लिहाज से मैं कुछ सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। मैं कृतज्ञ हूं उस जूरी का जिसने ‘मोहनदास” के लिए यह सम्मान दिया। यह और भी खुशी की बात है कि साहित्य अकादेमी इसका सभी भारतीय भाषाओं में अनुवाद कराने जा रही है।
आप ब्राह्मणवाद के विरोधी रहे हैं। अगर साहित्य में ब्राह्मणवाद ही सबसे बड़ी सच्चाई है तो निर्णायक मंडल को देखते हुए इस बार आपको यह पुरस्कार कतई नहीं मिल सकता था। आपका क्या मानना है?
उदय प्रकाश- मैं आज भी ब्राह्मणवाद संबंधी अपनी मान्यता पर अटल हूं। आलोचना के भीतर दूसरी प्रच्छन्न विचारधारा जो अब तक काम करती आ रही है वह जातिग्रस्त, साम्प्रदायिकताग्रस्त ब्राह्मणवादी विचारधारा ही है। यही विचारधारा पुरस्कारों नियुक्तियों आदि में काम करती रही है। किसी भी रूप में जातिवाद ब्राह्मणवाद ही है। मुझे पुरस्कार देकर उसने अपने आपको इस बार ‘ओवरस्टेप” किया है, सहिष्णुता दिखाई है। इसके लिए मैं उसके सामने नतमस्तक क्यों हो जाऊं? यह भी जरूरी नहीं कि हर ब्राह्मण ब्राह्मणवादी ही हो। मै निजी रूप में ब्राह्मणों का विरोधी नहीं हूं।
‘मोहनदास” कहानी जिस पर पुरस्कार मिला, बताती है कि दबे-कुचले व्यक्ति का अंतिम सहारा उसकी आइडेंटिटी है। पर सत्ता पर काबिज लोग उसकी वह आइडेंटिटी भी छीन लेते हैं। चार-पांच साल बाद इस कहानी को किस रूप में देखते हैं?
यह एकल संरचना वाली कहानी नहीं है। यह तीन-चार स्तरों पर चलती है। इसकी संरचना को लेकर सवाल उठाया गया कि बीच-बीच में नैरेटर हस्तक्षेप क्यों करता है? इससे कथा प्रवाह बाधित होता रहता है। मेरा कहना है कि अगर नैरेटर हस्तक्षेप कर आज का संदर्भ नहीं देता तो इसमें और प्रेमचंद की औपनिवेशिक दौर में लिखी कहानी में अंतर नहीं रह जाता। चार-पांच साल बाद आज मैं जब इसके बारे में सोचता हूं तो गहरी बेचैनी होती है। आज अस्मिता छीने जाने का संकट नहीं है बल्कि एक खतरनाक अस्मिता चिपका देने का गहरा संकट है। कहानी के मोहनदास से तो सिर्फ अस्मिता छीनी गई थी। बहुत संभव है आज के मोहनदास को माओवादी करार देकर मार ही दिया जाए। यह मूलत: सत्ताविमर्श की कहानी है।
आपके कई महत्वपूर्ण कहानी संकलन खासे चर्चित रहे हैं लेकिन कुछ का मानना है कि शुरुआती संकलन ‘तिरिछ” अधिक सशक्त है। बाद की रचनाओं में तात्कालिकता और प्रतिक्रिया की मात्रा बढ़ती गयी। क्या आप ऐसा मानते हैं?
उदय प्रकाश- इन ‘कुछ लोगों” की मैने कभी परवाह नहीं की। कभी इन्होंने ही ‘तिरिछ” को मान्यता नहीं दी थी। इन्होंने ‘और अंत में प्रार्थना” में मेरा संघी रुझान तो ‘वारेन हेस्टिंग्स का सांड” में पुनरुत्थानवादी दृष्टिकोण देख लिया। कुछ ने ‘पीली छतरी वाली लड़की” के खिलाफ बाकायदा अभियान चलाया। कुछ ने मेरी अकादमिक योग्यताएं दरकिनार कर मुझे प्रोफेसर के योग्य तक नहीं माना। मैं इन कुछ लोगों का क्या करूं? मैं तो पूरी ईमानदारी और शिद्दत से अपने समय पर लिखता हूं। मेरी सभी कहानियां अलग-अलग ढंग की हैं। मैं सभी समकालीन रचनाकारों से अपील करता हूं कि वे कुछ लोगों पर कभी ध्यान न दें। लेखक बस अपने समय के सरोकारों के प्रति प्रतिबद्ध रहे।
आपका विशाल पाठक वर्ग है और आपकी महत्ता आलोचकों से अधिक पाठकों की बदौलत है। पाठक के संकट से जूझ रहे लेखन के इस दौर में अपनी स्वीकार्यता के मूल में क्या कारण देखते हैं?
उदय प्रकाश- जब आप जनता के वास्तविक सरोकारों से जुड़कर रचना लिखेंगे तो व्यापक पठनीय स्वीकृति अवश्य मिलेगी। मेरी रचनाओं को हिन्दी के बाहर भी खूब स्वीकार्यता मिली है। उन्हें दूसरी भाषा के विद्वानों ने भी काफी पसंद किया है। दूसरी भारतीय भाषाओं में ‘पीली छतरी वाली लड़की” खूब चर्चित है। दरअसल हिन्दी में जिस राजनीतिक एजेडें के आधार पर कहानियां/उपन्यास लिखे जा रहे हैं, स्वयं उसका ही जनता द्वारा अनुमोदन नहीं है, भले रचनाओं को जनवादी नाम दे दिया जाए। वास्तव में यह जनवादी न होकर सांस्थानिक होती हैं।
आपकी कहानियां समय का महाआख्यान हैं। जिस निमित्त उपन्यास की जरूरत होती है वह काम आपकी लम्बी कहानियों से ही हो जाता है। क्या इसी कारण उपन्यास लेखन की ओर रुख नहीं किया?
उदय प्रकाश- इसका उत्तर में पहली बात तो यह कि उपन्यास लिखने के लिए अलग तरह की जीवन स्थितियों की दरकार होती है। उपन्यास के लिए अवकाश बहुत जरूरी है। अधिकांश महान उपन्यास अवकाश मे ही लिखे गए हैं। दुर्भाग्य से आर्थिक असुरक्षा के कारण मेरे जीवन में कभी ऐसा अवसर नहीं आ पाया कि मैं एक या दो साल टिककर लिख सकूं। दूसरे, कहानी को मैं कविता या उपन्यास से हीनतर कतई नहीं मानता। चेखव, ओ हेनरी, मंटो आदि ने कोई उपन्यास नहीं लिखा। स्वयं प्रेमचंद की उपन्यास से अधिक कहानियां चर्चित रहीं। आज भी सबसे अधिक पाठक वर्ग कहानी का ही है। कहानियों में तात्कालिकता और काव्यात्मकता एक साथ होती है और कविता उसका आंतरिक गुण है जो एक अच्छे उपन्यास के लिए भी आवश्यक होता है।
आप कविता से कहानी की ओर मुड़े और आपको जबर्दस्त सफलता भी मिली। आप आज भी कविताएं लिख रहें हैं लेकिन आपका कवि कहानीकार के नीचे दब सा गया लगता है। इसका क्या कारण मानते हैं?
उदय प्रकाश- मैं नहीं मानता कि मेरा कवि दब गया है। मैं अपने को मूलत: कवि ही मानता हूं। मुझे पहला पुरस्कार ‘भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार” कविता पर ही मिला। जिस ‘तिब्बत” कविता पर मुझे पुरस्कार मिला, उसे चीन और साम्यवाद के विरुद्ध माना गया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। तभी से एक खास तरह की गुटबंदी और राजनीति से प्रेरित होकर मेरी कविताओं को दरकिनार करने की कोशिश शुरू हुई। बावजूद इसके आज भी मेरे नए संकलन आ रहे हैं और पुराने के नए संस्करण प्रकाशित हो रहे हैं। मेरी कहानियां कविता का ही विस्तार हैं। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि इधर मुख्यधारा की जो कविता मानी गयी है, उसमें मुझे जानबूझकर ड्राप किया गया है।
हाल के वर्षों में कहानी सबसे आसान रचनात्मक विधा के रूप में सामने आयी है। एकाएक तीन दर्जन से भी अधिक कहानीकार सामने आ गए। इस प्रवृति का विश्लेशण कैसे करेंगें?
उदय प्रकाश- कहानी पर फोकस जरूर हो गया है लेकिन इस बीच कविताएं भी खूब लिखीं गईं हैं। कई नए कवि भी सामने आए हैं। इसी तरह इस बीच बहुत सारे उपन्यास भी सामने आए हैं। जो नए लोग आए हैं, उनमें कई में काफी संभावनाएं हैं। ये बदले समय को ध्यान में रखकर आज के जीवनानुभव की कहानियां लिख रहें हैं। लेकिन मूल बात यह है कि 90 के बाद पूंजी, श्रम और तकनीक का स्वरूप पूरी तरह बदल गया। यह आज भी सतत परिवर्तनशील है। इसलिए अब जो साहित्य लिखा जाना चाहिए, वह तात्कालिकता और सतही चीजों के आधार पर नहीं लिखा जाना चाहिए क्योंकि चीजें जिस तेजी से बदल रहीं हैं, उसमें इस तरह की रचनाएं बहुत जल्दी अप्रांसगिक हो जाएंगी। अच्छी रचना के लिए आज के समय के संकट और मुख्य अंतर्विरोध को समझना होगा, नहीं तो पुरानी शराब को नई बोतल में प्रस्तुत करने का कोई फायदा नहीं होगा।
आलोचना के संकट पर बहुत बातें हो रही हैं। हिन्दी आलोचना के वर्तमान परिदृश्य को कैसे देखते हैं?
आलोचना रचना और अकादमिकता से संपुष्ट होती है, जो आज नहीं हो रही है। कई सालों से हिन्दी आलोचना में कोई अकादमिक काम नहीं हुआ है। इतिहास लेखन, तुलनात्मक साहित्य अनुवाद आदि में कुछ भी नया नहीं हुआ है जिसे सार्थक कहा जा सके। वस्तुत: अपने समय की आलोचना द्वारा ही रचना चिह्नित होती है। यह काम लगभग बंद है। इस देश में 80-90 के बाद जो परिवर्तन आए हैं, वे मूलत: आर्थिक हैं। आप जब तक इस परिवर्तन को नहीं समझेगे तब तक प्रेमचंद के डंडे से ही नई रचनाओं को हांकते रहेंगे।
लेखन को लेकर क्या योजनाएं हैं?
उदय प्रकाश- बच्चों के लिए एक किताब लिख रहा हूं ‘चकमक”। इसके बाद लम्बी कहानी ‘गदरहा बाबा की तलवार” पूरा करूंगा। फिर ‘चीना बाबा” की योजना है। इसके अलावा विदेश यात्राएं और सेमिनार हैं।
राष्ट्रीय सहारा से साभार