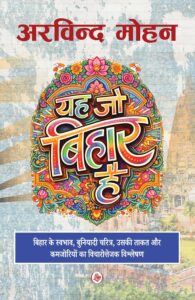कल हिंदी दिवस है. हिंदी के आह-वादी और वाह-वादी विमर्श से हटकर मैंने कुछ लिखा है. यह लेख मूल रूप से ‘प्रभात खबर’ के लिए लिखा था. अब आपके लिए- प्रभात रंजन
=========================================
हर साल हिंदी दिवस के आसपास हिंदी को लेकर दो तरह की चर्चाएँ होने लगती हैं- आह-वादी और वाह-वादी! वाह-वादी यह बताते हैं कि किस तरह दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक विश्वविद्यालयों में हिंदी की पढ़ाई होने लगी है, भाषा की भी साहित्य की भी, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में हिंदी के शब्द कितने बढते जा रहे हैं, इंटरनेट पर हिंदी का उपयोग इतना बढ़ता जा रहा है कि इस तरह की भविष्यवाणी की जा रही है कि इंटरनेट पर आने वाले समय में हिंदी सबसे बड़ी भाषा बनकर उभरने वाली है. आह-वादी यह याद दिलाते रहते हैं कि आजादी के ६५ सालों के बाद भी हिंदी को उसका उचित दर्जा दिलवाने के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया? इतनी बड़ी आबादी है हिंदीभाषियों की फिर भी हिंदी की किताबें नहीं बिकतीं. असल में हिंदी के बारे में विचार करते हुए इन दोनों ध्रुवान्तों से हटकर विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि हिंदी की वास्तविक तस्वीर भी उसी अध्ययन से सामने आया पाएगी. इसी से हमें इस सवाल का जवाब भी मिल सकता है कि हिंदी आखिर क्यों अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बना पाने में नाकाम रही है. साहित्य का सवाल गहरे रूप से भाषा से जुड़ा होता है. जब तक भाषा की धमक अंतरराष्ट्रीय स्तर होती है तो उसका साहित्य भी अंतरराष्ट्रीय होने लगता है.
मुझे लगता है कि इस सवाल से पहले कि हिंदी अंतरराष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान क्यों नहीं बना रहा है यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि स्वतंत्रता के ६५ सालों बाद देश में सबसे अधिक बोली-समझी जाने वाली भाषा हिंदी शर्म की भाषा क्यों बनी हुई है? क्यों वह आज भी आत्मसम्मान की भाषा नहीं बन पाई है? क्यों हिंदी का बड़े से बड़ा लेखक हिंदी समाज में ‘सेलिब्रिटी’ के रूप में नहीं देखा जाता? क्यों हिंदी की साहित्यिक किताबें खरीदने वाले को छोड़ भी दीजिए तो पढ़ने वाले को तरसती है? प्रेमचंद के अलावा हिंदी में ऐसे कितने लेखक हैं जिनको राष्ट्रीय स्तर पर बतौर लेखक जाना-पहचाना जाता है? हालांकि इस का अर्थ यह नहीं है कि हिंदी में स्तरीय साहित्य का अभाव है.
हम हिंदी साहित्य के अंतरराष्ट्रीयकरण की चर्चा कर रहे हैं जबकि इस समय हिंदी में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय लेखक अनुवाद के माध्यम से सामने आ रहे हैं. पिछले कुछ सालों में हिंदी में जितनी उल्लेखनीय साहित्यिक पुस्तकें आई हैं उससे अधिक मात्रा में उल्लेखनीय पुस्तकें अनुवाद के माध्यम से सामने आई हैं. इससे जुड़ा हुआ एक बड़ा सवाल यह है कि हिंदी के प्रकाशक हिंदी लेखकों को ‘ब्रांड’ के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करते, वे विदेशी भाषाओं के ब्रांड पर अधिक भरोसा करते हैं- चाहे वह गाब्रियल गार्सिया मार्केस हो या ओरहान पामुक. जब इन लेखकों की अंग्रेजी भाषा में प्रकाशन के बाद बड़े ब्रांड लेखक के रूप में प्रतिष्ठा हो जाती है तब इनके उपन्यासों के हिंदी अनुवाद प्रकाशित किए जाते हैं. जबकि हम यह भूल जाते हैं कि ये लेखक अपनी मातृभाषाओं के प्रतिष्ठित लेखक रहे हैं और अंग्रेजी अनुवाद ने इनको अंतरराष्ट्रीय बनाया. ओरहान पामुक तुर्की भाषा के सबसे महत्वपूर्ण लेखकों में हैं तो मार्केस स्पेनी भाषा के. जब तक हम अपनी भाषा में अपने लेखक को ब्रांड के रूप में प्रतिष्ठित नहीं करेंगे तब तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनको प्रतिष्ठित करने की बात बेमानी है.
हालांकि केवल यही कहकर इस सवाल से बचा नहीं जा सकता. कई सवाल और इससे जुड़े हुए हैं- क्या अनुवाद न हो पाना इसका कारण है या बाजार का न होना? इस सन्दर्भ में मुझे कुछ उदाहरण याद आते हैं- राही मासूम रजा के उपन्यास आधा गाँव या श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास रागदरबारी के अंग्रेजी अनुवादों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई चर्चा नहीं सुनाई दी, जबकि उनके अनुवाद एक प्रतिष्ठित अंग्रेज अनुवादिका ने किया था. वहीं दूसरी ओर अलका सरावगी के उपन्यास ‘कलिकथा वाया बाईपास’ का उदाहरण भी है, जिसे फ़्रांसिसी भाषा में वहां के सबसे बड़े प्रकाशक गैलिमार ने छापा, इटैलियन में उसका अनुवाद हुआ, अंग्रेजी अनुवाद छापा भले भारत के रूपा एंड संज से लेकिन उसकी अन्तराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री और चर्चा भी हुई. लेकिन उसकी इस उपलब्धि को हिंदी की उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जाता, नहीं बताया जाता. समाचारपत्रों को छोडिये कितनी साहित्यिक पत्रिकाओं में उसके इस पहलू के बारे में छपा. मेरा यह मानना है कि हम हिंदी वाले अपने लेखकों का सम्मान करना, उनको सेलेब्रेट करना नहीं चाहते. आज उदयप्रकाश निर्विदाद रूप से हिंदी के सबसे लोकप्रिय अंतरराष्ट्रीय लेखक हैं. उनकी किताबें अनेक यूरोपीय भाषाओं में न केवल प्रकाशित हुई हैं बल्कि समादृत भी हुई हैं. लेकिन हिंदी के लेखक उनको किस रूप में लेते हैं इसे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है. बहरहाल, इन कुछ उदाहरणों के आधार मैं यही कहना चाहता हूं कि हिंदी वाले अपने लेखकों को पढ़ने-सुनने को लेकर कुछ खास उत्साह नहीं दिखाते. हिंदी के समाचारपत्रों में अंग्रेजी के ‘बिकाऊ’ लेखकों के कॉलम तो नियमित छपते हैं लेकिन अपनी भाषा के मूर्धन्य लेखकों के विचार उनको किसी लायक नहीं लगते. टेलीविजन मीडिया तो खैर चलता ही ‘ब्रांड-सेलिब्रिटी’ के तर्क से है. जब तक हमारे लेखकों की राष्ट्रीय पहचान नहीं बनेगी अंतरराष्ट्रीय पहचान की बात करना बेमानी है.
कुछ तो मुझे लगता है कि हिंदी साहित्य में हिंदी समाज उस तरह से अभिव्यक्त नहीं होता जिसके कारण वह उस समाज की मौलिक कथा की तरह से पढ़ी जा सके. मार्केस, चिनुआ अचीबे या ओरहान पामुक सबसे पहले अपने समाज के विश्वसनीय लेखक हैं. वे अपने समाज को पश्चिम के तथाकथित आधुनिक नजरिये से नहीं देखते बल्कि अपने समाज के अंतर्विरोधों को अपनी दृष्टि से देखते हैं. क्या कारण है कि जो समाज राजनीतिक विद्रूपताओं का रूपक बन गया हो उस समाज को लेकर कोई ढंग का राजनीतिक उपन्यास तक नहीं लिखा गया, जिस हिंदी समाज ने देश में सबसे बड़े पैमाने पर विस्थापन देखा हो उस समाज के विस्थापन को लेकर हिंदी में कोई कृति याद नहीं पड़ती. जिस साहित्य में उसका अपना समाज नहीं झांकता हो उसकी कथा में भला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किसको दिलचस्पी होगी. इसके कारण बहुत गहरे हैं. एक कारण तो शायद यह है कि हिंदी में पूर्णकालिक लेखक बहुत कम हैं, क्योंकि साहित्य उनके गुजर-बसर के लिए कुछ भी नहीं दे पाता. अधिकतर लेखक दिनभर कहीं नौकरी करते हैं और रात में थकान के बोझ तले लिखते हैं. हिंदी का अधिकांश समकालीन साहित्य पार्टटाइम लेखक का उत्पाद है. पहले हमें इन बुनियादी सवालों से टकराना पड़ेगा कि हिंदी पुस्तकों का बाजार पारदर्शी क्यों नहीं है? क्यों प्रकाशकों का मुनाफा तो बढ़ता जाता है, लेखकों के हिस्से पुस्तकों के न बिक पाने की तोहमद आती है?
फ्लिपकार्ट.कॉम जैसे ऑनलाइन पुस्तक बिक्री केन्द्रों के आंकड़े बताते हैं कि हिंदी किताबों की बिक्री उत्साहवर्धक है. इस साल विश्व पुस्तक मेले के अवसर पर दिल्ली के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी समाचारपत्र ने लिखा था कि इस साल मेले में हिंदी किताबों की बिक्री अंग्रेजी पुस्तकों से अधिक हुई. पुस्तक बाजार में हिंदी कि गूँज सुनाई देने लगी है. यह गूँज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सुनाई दे इसके लिए बाजार विरोध की मानसिकता से भी निकलने की आवश्यकता है. यह नहीं भूलना चाहिए साहित्य प्रकाशकों-विक्रेताओं के लिए व्यवसाय है. जैसे-जैसे वह बढ़ता जाएगा दुनिया में उसकी धमक बढ़ती जायेगी. फिलहाल तो हिंदी के बाजार में विश्व-भाषाओं की किताबें मुनाफा कमाने के लिए अनूदित होकर आ रही हैं. प्रतीक्षा उस दिन की है जब हिंदी की साहित्यिक कृतियाँ विश्व-भाषाओं में अनूदित होकर मुनाफे में सेंध लगाएंगी. वह दिन हिंदी साहित्य के अंतरराष्ट्रीय होने का वास्तविक दिन होगा. वह विश्व हिंदी सम्मेलनों या प्रवासी हिंदी लेखन से नहीं होने वाला है.