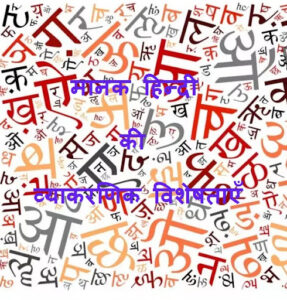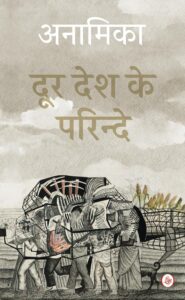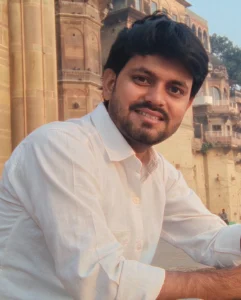लोक-गायक बालेश्वर के निधन को लेकर ज्ञानपीठ वाले सुशील सिद्धार्थ से चर्चा हो रही थी तो उन्होंने बताया कि दयानंद पांडे ने उनके ऊपर उपन्यास लिखा था ‘लोक कवि अब गाते नहीं’. बाद में जब युवा कवि-आलोचक-संपादक सत्यानन्द निरुपम से चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि यह उपन्यास उनके पास है. उन्होंने तुरंत वह उपन्यास भिजवा भी दिया. प्रस्तुत है उसी उपन्यास का एक अंश- जानकी पुल.
पहले तो वह सिर्फ नौटंकी देख-देख उसकी नक़ल पेश कर लोगों का मनोरंजन करते. फिर वह गाना भी गाने लगे. कंहरवा गाना सुनते. धोबिया नाच-चमरऊआ नाच भी वह देखते. इसका ज्यादा असर पड़ता उन पर. कंहरवा धुन का सबसे ज्यादा. वह इसकी भी नक़ल करते. नक़ल उतारते-उतारते वह लगभग पैरोडी पर आ गए. जैसे नौटंकी में नाटक की किसी कथावस्तु को गायकी के मार्फ़त आगे बढ़ाया जाता उसी तर्ज़ पर लोक कवि गांव की कोई समस्या उठाते और उस गाने में उसे फिट कर गाते. अब उनके हाथ में बजाने के लिए एक खजडी कहिये कि ढपली भी आ गई थी. जबकि पहले वह थाली या गगरा बजाते थे. पर अब खजडी. फिर तो धीरे-धीरे उनके गानों की हदें गांव की सरहद लांघकर जवार और जिले की समस्याएं छूने लगीं. इस फेर में कई बार वह फजीहत फेज से भी गुज़रे. कुछ सामंती–ज़मींदार टाइप के लोग भी जब उनके गानों में आने लगे और ज़ाहिर है इन गानों में लोक-कवि इन सामंतों के अत्याचार की ही गाथा गूंथते थे, जो उन्हें नागवार गुज़रता. सो लोक-कवि की पिटाई-कुटाई भी वह लोग किसी न किसी बहाने जब-तब करवा देते. लेकिन लोक-कवि की हिम्मत इन सबसे नहीं टूटती. उलटे उनका हौसला बढ़ता. नतीजतन जिला-जवार में अब लोक-कवि और उनकी कविताई चर्चा का विषय बनने लगी. इस चर्चा के साथ ही वह अब जवान भी होने लगे. शादी-ब्याह भी उनका हो गया. बाकी रोजी-रोजगार का कुछ जुगाड़ नहीं हुआ उनका. जाति से वह पिछड़ी जाति के भर थे. कोई ज्यादा ज़मीन-जायदाद थी नहीं. पढ़ाई-लिखाई आठवीं तक भी ठीक से नहीं हो पाई थी. तो वह करते भी तो क्या करते? कविताई से चर्चा और वाहवाही तो मिलती थी, कभी-कभी पिटाई, पिटाई बेइज्जती भी हो जाती, लेकिन रोज़गार फिर भी नहीं मिलता था. कुर्ता-पायजामा तक की मुश्किल हो जाती. कई बार फटहा पहनकर घूमना पड़ जाता. उसी समय एक स्थानीय कम्युनिस्ट नेता-विधायक फिर चुनाव में उतरे. इस चुनाव में उन्होंने लोक कवि की भी सेवाएं ली. उनको कुर्ता-पायजामा भी मिल गया. लोक कवि जवार की समस्याएं भी जानते थे और वहां की धडकन भी. उनके गाने वैसे भी वैसे भी पीड़ितों और सताए जा रहे लोगों के सत्य के ज्यादा करीब होते थे. सो कम्युनिस्ट पार्टी की जीप में उनके गाने ऐसे लहके कि बस पूछिए मत. यह वह ज़माना था जब चुनाव प्रचार में जीप और लाउडस्पीकर ही सबसे बड़ा प्रचार माध्यम था. कैसेट वगैरह तो तब देश ने देखा ही नहीं था. सो लोक कवि जीप में बैठकर गाते घूमते. मंच पर भी सभाओं में गाते.
कुछ उस कम्युनिस्ट नेता की अपनी ज़मीन तो कुछ लोक कवि के गानों का प्रभाव, नेताजी फिर चुनाव जीत गए. वह चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में चुनकर लखनऊ आ गए तो भी लोक कवि को भूले नहीं. साथ ही, लोक कवि को भी लखनऊ खींच लाए. अब लखनऊ लोक कवि के लिए नई ज़मीन थी. अपरिचित और अनजानी. चौतरफा संघर्ष उनकी राह देख रहा था. जीवन का संघर्ष, रोटी-दाल का संघर्ष, और इस खाने-पहनने, रहने के संघर्ष से भी ज्यादा बड़ा संघर्ष था उनके गाने का संघर्ष. अवध की सरज़मीं लखनऊ जहाँ अवधी का बोलबाला था, वहां लोक कवि की भोजपुरी भहरा जाती. तो भी उनका जूनून कायम रहता. वह लगे रहते और गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला छानते रहते. जहाँ चार लोग मिल जाते वहां ‘रइ-रइ- रइ- रइ’ गुहार कर कोई कंहरवा सुनाने लगते. बावजूद इस सबके उनका संघर्ष गाढ़ा होता जाता.
उन्हीं गाढ़े संघर्ष के दिनों में लोक कवि एक दिन आकाशवाणी पहुँच गए. बड़ी मुश्किल से घंटों ज़द्दोज़हद के बाद उन्हें परिसर में प्रवेश मिल पाया. जाते ही वहां पूछा गया, ‘क्या काम है?’ लोक कवि बेधड़क बोले, ‘हम भी रेडियो पर गाना गाऊंगा!’ उन्हें समझाया गया कि ‘ऐसे ही हर किसी को आकाशवाणी से गाना गाने नहीं दिया जाता.’ तो लोक कवि तपाक से पूछ बैठे, ‘तो फिर कैसे गाया जाता है?’ बताया गया कि इसके लिए आवाज़ का टेस्ट होता है तो लोक कवि ने पूछा, ‘इ टेस्ट का चीज़ होता है?’ बताया गया कि एक तरह का इम्तेहान होता है तो लोक कवि थोड़ा मद्धिम पड़े और भडके, ‘इ गाना गाने का किसान इम्तेहान?’
‘लेकिन देना तो पड़ेगा ही.’ आकाशवाणी के एक कर्मचारी ने उन्हें समझाते हुए कहा.
‘तो हम परीक्षा दूंगा गाने का. बोलिए कब देना है?’ लोक कवि बोले, हम परीक्षा पहले मिडिल स्कूल में दे चुका हूँ.’ वह बोलते रहे, ‘दर्ज़ा आठ तो नहीं पास कर पाए पर दर्ज़ा सात तो पास हूँ. बोलिए काम चलेगा?’ कर्मचारी ने बताया कि, दर्ज़ा सात, आठ का इम्तेहान नहीं, गाने का ही इम्तेहान होगा. जिसको ऑडिशन कहते हैं. इसके लिए फार्म भरना पड़ता है. फ़ार्म भरिये. फिर कोई तारीख तय कर इत्तिला कर दी जायेगी.’ लोक कवि मान गए थे. फार्म भरा, इंतज़ार किया और परीक्षा दी. पर परीक्षा में फेल हो गए.
लोक कवि बार-बार परीक्षा देते और आकाशवाणी वाले उन्हें फेल कर देते. रेडियो पर गाना गाने का उनका सपना टूटने लगा था कि तभी एक मोहल्ला टाइप कार्यक्रम में लोक कवि का गाना एक छुटभैये एनाउंसर को भा गया. वह उन्हें अपने साथ लेकर छिटपुट कार्यक्रमों में एक आइटम लोक कवि का भी रखने लगा. लोक कवि पूरी तन्मयता से गाते. धीरे-धीरे लोक कवि का नाम लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा. लेकिन उनका सपना तो रेडियो पर ‘रइ-रइ-रइ-रइ’ गाने का था. लेकिन जाने क्यों वह बार-बार फेल हो जाते. कि तभी एक शोमैन टाइप एनाउंसर से लोक कवि की भेंट हो गई. लोक कवि उसे क्लिक कर गए. फिर उस शोमैन एनाउंसर ने लोक कवि को गाने का सलीका सिखाया, लखनऊ की तहज़ीब और दंद-फंद समझाया. गरम रहने के बजाय व्यवहार में नरमी का गुण समझाया. न सिर्फ यह सब बल्कि कुछ सरकारी कार्यक्रमों में भी लोक कवि की हिस्सेदारी करवाई. अब और सफलता लोक कवि की राह देख रही थी. और संयोग यह कि कि कम्युनिस्ट विधायक के जुगाड़ से लोक कवि को चतुर्थ श्रेणी की सरकारी नौकरी मिल गई. एक विधायक निवास में ही उनकी पोस्टिंग भी हुई. जिसे लोक कवि ‘ड्यूटी मिली है’ बताते. अब नौकरी भी थी और गाना-बजाना भी. लखनऊ की तहजीब को वह और यह तहजीब उन्हें सोख रही थी.
जो भी हो भूजा, चना, सतुआ खाकर भूखे पेट सोने और मटमैला कपड़ा धोने के दिन लोक कवि की जिंदगी से जा चुके थे. यहाँ वहां जिस-तिस के यहाँ दरी, बेंच पर ठिठुरकर या सिकुडकर कर सोने के दिन भी लोक कवि के बीत गए. इनकी-उनकी दया, अपमान और जब-तब गाली सुनने के दिन भी हवा हुए. अब तो चहकती जवानी के बहकते दिन थे और लोक कवि थे.
इस बीच आकाशवाणी का ऑडिशन भी वह पास कर वहां भी अपनी डफली बजा कर ‘रइ-रइ-रइ-रइ’ गुहार कर दो गाना वे रिकॉर्ड करवा आये. उनकी जिंदगी से बेशऊरी और बेतरतीबी अब धीरे-धीरे उतर रही थी. वह अब गा भी रहे थे-
फगुनवा में रंग रसे-रस बरसे.’