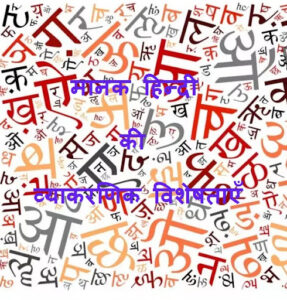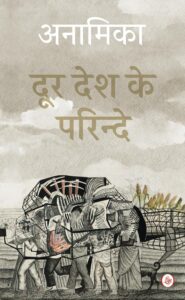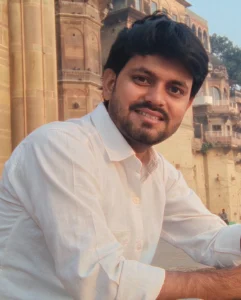ल्योसा को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिले ठीक से महीना भी नहीं हुआ था कि १९८७ में लिखा उनका उपन्यास ‘द स्टोरीटेलर’ हिंदी में छपकर आ भी गया- ‘किस्सागो’ के नाम से. वैसे तो यह ल्योसा का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास नहीं है लेकिन समकालीन भारतीय सन्दर्भ में इसके अनुवाद के प्रकाशन को प्रासंगिक कहा जा सकता है. जैसा कि अनुवादिका शम्पा शाह ने इसकी भूमिका में लिखा है, ‘आदिवासी जीवनदृष्टि तथा हमारी आज की आधुनिक सभ्यता के बरक्स उसकी इयत्ता को एक बड़े प्रश्न के रूप में करने वाला संभवतः अपनी तरह का अकेला उपन्यास है.’ आज हमारे देश के जनजातीय समाज और उनकी जीवन पद्धति तथा तथाकथित ‘विकास’ को लेकर जो बहस चल रही है उसके सन्दर्भ में इस उपन्यास की प्रासंगिकता को समझा जा सकता है.
कहानी अमेसान(आमेज़न) के जंगलों के आदिवासी समुदाय माचिग्वेंगा के सपनों-मान्यताओं-विश्वासों के सहारे चलती है. इस घुमंतू जनजाति को ‘आधुनिक’ बनाने के नाम पर एक स्थान पर बसाया जा रहा है, उनको आधुनिक शिक्षा, सभ्यता के पश्चिमी बानों से जोड़ने के प्रयास किये जा रहे हैं. लेकिन उस समाज के किस्सागो अपने किस्सों में उन परम्पराओं को बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं. उनकी पौराणिक-ऐतिहासिक स्मृतियों को संजोये रखने का प्रयास कर रहे हैं. अच्छे के देवता तासुरिंची और बुराई के देवता केंतीबाकोरी के किस्से जो पीढ़ियों से सुनाये जा रहे हैं, जिनमें उनके अतीत की स्मृतियाँ ही नहीं भविष्य के संकेत भी हैं. शताब्दियों से मिशनरी, फ़्रांसिसी, डोमिनिक निवासी जिनको सभ्य बनाने आते रहे, उनको अपने जैसा बनाने. आमेज़न का महत्त्व १९वीं-वीं शताब्दियों में और तब बढ़ गया जब विश्व बाज़ार का ध्यान इसकी ओर रबर की प्राकृतिक सम्पदा के कारण गया. बाद के दौर में नृतत्वशास्त्रियों, भाषाशास्त्रियों का ध्यान इसकी ओर सांस्कृतिक विविधता के कारण गया. कहते हैं आमेज़न के उन जंगली इलाकों में आज भी आधुनिक सभ्यता से दूर माचिग्वेंगा आदिवासी वास कर रहे हैं, अलबत्ता उनके किस्से-कहानियों के प्रति लोगों की रूचि कम होती जा रही है.
उपन्यास में एक पात्र है साउल सूरातास, जो कथावाचक के साथ आदिम सभ्यताओं के बारे में बातें करते हुए यह कहता है कि माचिग्वेंगा जैसे आदिम समाज को इस धरती पर अपने ढंग से रहने के अधिकार को मान लेना चाहिए तथा उनके ऊपर अपनी तथाकथित सभ्यता थोपने का प्रयास नहीं करना चाहिए. वह कहता है, ‘आखिर वे कहाँ जायेंगे? शताब्दियों से उन्हें अपनी ज़मीन सा खदेड़ा जा रहा है; हर बार वे अंदर, और अंदर धकेले जा रहे हैं. सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि इतनी विभीषिकाओं की मार के बावजूद वे अभी मिटे नहीं हैं. वे अब भी बचे हुए हैं, जिंदा.’ जवाब में कथावाचक कहता है, ‘क्या यह कि उन मुट्ठी भर आदिवासियों का जीवन पूर्ववत चलता रहे इसकी खातिर बाकी पूरे पेरू को आमेज़न क्षेत्र के विकास के प्रति उदासीन हो जाना चाहिए? क्या सोलह करोड़ पेरुवासियों को अपने देश के तीन चौथाई भू-भाग की प्राकृतिक सम्पदा का मोह त्याग देना चाहिए ताकि सत्तर-अस्सी हज़ार इन्डियन इत्मीनान से अपने धनुष-बाण चलाते रह सकें, खोपड़ी सिकोड़ सकें, नाग और अजगर की पूजा कर सकें?… यदि सोलह करोड़ पेरुवासियों के विकास और औद्योगिकीकरण की कीमत चुकाने के लिए उन कुछ हज़ार नंगे इंडियन लोगों को अपने बाल कटवाने पड़ें, गुदने मिटाने पड़ें, मेस्तिजो बनना पड़े, मानवशास्त्रियों को सबसे ज्यादा नापसंद शब्द- परसंस्कृत बनना होगा- तो ठीक है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है?’
उपन्यास में एक तरफ जनजातीय समाजों को लेकर इस तरह की बहस है तो दूसरी ओर माचिग्वेंगा समुदाय के किस्सागो द्वारा सुनाये गए किस्से हैं जो प्रकृति के साथ मनुष्य के आदिम संबंधों को बयान करते हैं. भूत-प्रेत, जादू-टोना, विश्वास-अविश्वास के किस्से जिसे आधुनिकता की तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता. ‘किस्सागो’ पूरी तरह से विमर्शात्मक उपन्यास है परंपरा और आधुनिकता का द्वंद्व अनवरत चलता रहता है. आज हमारे यहाँ भी आदिवासियों को लेकर यह बहस चल रही है कि क्या विकास के नाम पर उनकी परम्पराओं, उनके रहन-सहन के ढंग को नष्ट कर दिया जाना चाहिए? क्या प्रकृति से कटकर जीना ही आधुनिकता की पहचान है? हम उनकी परम्पराओं से तो कुछ नहीं सीखना चाहते हैं, उनको सिखाना अवश्य चाहते हैं. छत्तीसगढ़ के जंगलों में परम्परा और आधुनिकता का संघर्ष चल रहा है. जो इस उपन्यास की रौशनी में कुछ और साफ़ ढंग से दिखाई देता है. ‘किस्सागो’ में एक स्थान पर लिखा है, ‘हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आदिम समाजों को प्रगति या या आधुनिकीकरण की राह पर लाना क्रूरता है. इसका दो-टूक अर्थ है उन्हें जड़-मूल से मिटा देना.’
माचिग्वेंगा कथावाचकों की कथा का तात्पर्य भी इसी सन्दर्भ में समझ में आता है. उनकी वास्तविकताओं, उनकी परम्पराओं को नष्ट-भ्रष्ट किया जा रहा है, ऐसे में उन कथावाचकों की कथाओं में ही उनकी परम्पराएँ, उनके पूर्वजों का जीवन सुरक्षित दिखाई देता है. लेखक ने लिखा है, ‘एक कथावाचक की तरह बोलने का अर्थ होता है उस संस्कृति के मर्म में पैठकर जीना, उसे महसूस कर पाना, यानी उसके मर्म को भेदते हुए उसके इतिहास और पुरानों में पैठ पाना, उसके गोदने, छबियों, पूर्वजों की आकांक्षाओं और भय को मूर्त स्वरुप प्रदान करना.’
एक तरह से ‘किस्सागो’ में ल्योसा ने कुछ साभ्यतिक प्रश्न उठाये हैं. आधुनिक सभ्यता की हिंसा के स्वरुप को सामने रखने का प्रयास किया है. किस तरह आधुनिकता ने मनुष्यों को उनकी जड़ों से काट दिया है, विकास के नाम पर उनको असहिष्णु बना दिया है, स्मृतिहीन बना दिया है. इस स्मृतिहीन समाज में ‘किस्सागो’ की व्यंजना समझ में आती है. उपन्यास में एक स्थान पर यह सवाल उठाया गया है, ‘मैं पूछता हूँ कि कौन है जो अपनी जन्मजात नियति को त्यागकर सम्पन्नतर या पहले से अधिक श्रेष्ठ हुआ है? कोई नहीं. हमारे लिए श्रेयस्कर यही होगा कि हम वही रहें जो हम हैं. जो मनुष्य अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के कर्तव्यों का निर्वाह करने में जुटा रहेगा, वह एक दिन अपनी आत्मा ही गँवा बैठेगा.’
इन्हीं सन्दर्भों के कारण हिंदी में ‘स्टोरीटेलर’(स्पेनिश में आब्लादोर) के अनुवाद को समयोचित कहा जा सकता है. शम्पा शाह के अनुवाद में सहजता है लेकिन उपन्यास में माचिग्वेंगा समाज के बहुत से सन्दर्भ, पेड़-पौधों के नाम, पशु-पक्षियों, नदियों, पहाड़ों, देवताओं, दानवों के नाम आये हैं जिसे पाठकों को समझने में मुश्किल हो सकती है. ठीक उसी तरह जैसे हमें आदिवासियों की संस्कृति अपरिचित लगती है. वैसे संस्कृति और उसके विमर्श की बात और है उपन्यास उसके कारण अनेक स्थानों पर अपाठ्य हो गया है. बहरहाल, उचित समय पर राजकमल प्रकाशन ने इसका अनुवाद प्रकाशित किया है. इसका स्वागत किया जाना चाहिए और शम्पा शाह को धन्यवाद कि इस दुरूह उपन्यास को उन्होंने सहज बनाकर हिंदी के पाठकों के सामने प्रस्तुत करने का काम किया है.
उपन्यास राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है.