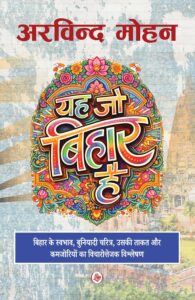‘युवा संवाद‘ पत्रिका का नया अंक जनकवियों की जन-शताब्दी पर केंद्रित है. इस अंक का संपादन अशोक कुमार पांडे जी ने किया है. इस अंक में कवि गोपाल सिंह नेपाली पर मेरा यह लेख प्रकाशित हुआ है- प्रभात रंजन.
११ अगस्त १९११ को बिहार में नेपाल की सीमा पर बसे शहर बेतिया में पैदा हुआ गोपाल बहादुर सिंह कवि गोपाल सिंह नेपाली के नाम से विख्यात हुए. यह उनकी जन्म-शताब्दी का साल है. बेतिया के कालीबाग दरबार के नेपाली महल में पैदा होने के कारण एक तो वहां के साहित्यिक-सांस्कृतिक माहौल में उनका लालन-पालन हुआ, दूसरे इसी कारण जब बाद में उन्होंने कविता लिखना शुरू किया तो नेपाली उपनाम को अपनाया. औपचारिक शिक्षा के मामले में वे मैट्रिक की परीक्षा भी नहीं दे पाए लेकिन बेतिया राज के समृद्ध पुस्तकालय में बैठ-बैठकर दुनिया भर का ज्ञान घोंट डाला. फिर बचपन से ही सैनिक पिता रेल बहादुर सिंह के साथ अफगानिस्तान, देहरादून, पेशावर की सैनिक छावनियों में रहने के कारण जीवन-जगत का अनुभव खूब प्राप्त किया. साहित्यकार नेपाली को आरंभिक प्रेरणा और संस्कार इन्हीं दो भिन्न प्रकार के परिवेश से मिले.
बेतिया राज उन दिनों साहित्य-संगीत का केंद्र था. ध्रुपद गायन का केंद्र था. इसके कारण वहां गुणीजनों की आमदरफ्त रहती था. काव्य-संध्याओं का आयोजन होता. इसलिए कम उम्र से ही कविताई शुरू कर दी. उन दिनों छायावाद का जोर था. आरंभ उसी तरह की कविताओं से किया. महज २२ साल की उम्र में उनका पहला कविता संग्रह ‘उमंग’ का प्रकाशन हुआ जिसमें ६२ कविताएँ थीं. दो साल बाद ही उनके सरस कविताओं का संकलन आया ‘पंछी’. उन आरंभिक कविताओं में प्रकृति के रहस्यों के प्रति जिज्ञासा का भाव था, समाज के बंधनों की जगह प्रकृति की उन्मुक्तता की चर्चा अधिक थी, जो इस तरह की कविताओं में दिखाई देती है- यह लघु सरिता का बहता जल/ कितना शीतल, कितना निर्मल/ हिमगिरि के हिम से निकल निकल/ यह निर्मल दूध सा हिम का जल/ कर–कर निनाद कल–कल छल–छल’ या ‘यह लघु सरिता का बहता जल/ कितना शीतल, कितना निर्मल.
लेकिन उन दिनों वे जिस माहौल में रह रहे थे वहां कवि-सम्मेलनों का आयोजन होता था. उसमें गीतकारों की धूम रहती थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका झुकाव गीतों की तरफ हुआ, कहते हैं उनके गीतों का उनके कंठ ने भी भरपूर साथ दिया. कवि के रूप में इससे एक तो मंचों पर लोकप्रियता मिलती थी और कुछ आय भी हो जाती थी. ‘रागिनी’ उनके इकतीस गीतों का पहला संकलन था जो १९३५ में आया, फिर उसके बाद ‘पंचमी’, ‘नवीन’, उनके गीतों के न सिर्फ संकलन आये उनके गीत आम जन में लोकप्रिय भी हुए. ‘तुम कहीं रह गये, हम कहीं रह गए, गुनगुनाती रही वेदना/
रात जाती रही, भोर आती रही, मुसकुराती रही कामना या ‘घोर अंधकार हो,
चल रही बयार हो,
आज द्वार–द्वार पर यह दिया बुझे नहीं
यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है जैसे गीतों से उनकी पहचान बनी.
रात जाती रही, भोर आती रही, मुसकुराती रही कामना या ‘घोर अंधकार हो,
चल रही बयार हो,
आज द्वार–द्वार पर यह दिया बुझे नहीं
यह निशीथ का दिया ला रहा विहान है जैसे गीतों से उनकी पहचान बनी.
छायावादी कवियों की तरह राष्ट्रवादी गीत भी उन्होंने लिखे और उन गीतों ने उस दौर में उनको राष्ट्रवादी कवि के रूप में स्थापित कर दिया. ‘निज राष्ट्र के शरीर के सिंगार के लिए
तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो,
तुम कल्पना करो’ या ‘तू चिंगारी बनकर उड़ री, जाग–जाग मैं ज्वाल बनूँ,
तू बन जा हहराती गँगा, मैं झेलम बेहाल बनूँ,
आज बसन्ती चोला तेरा, मैं भी सज लूँ लाल बनूँ,
तू भगिनी बन क्रान्ति कराली, मैं भाई विकराल बनूँ’ जैसे गीत उसी दौर के हैं. कहते हैं उनके इन्हीं गीतों से प्रभावित होकर एक फिल्मिस्तान स्टुडियो ने उनके फिल्मों में गीत लिखने के लिए अनुबंधित कर लिया. वहां चार साल गीत लिखने के बाद कहते हैं कि धार्मिक गीतों में उनका ऐसा जलवा जमा कि उन्होंने अगले लगभग दो दशक में करीब ४०० गीत अलग-अलग फिल्मों के लिए लिखे. उनके इस पहलू को लेकर अभी काम होना बाकी है.
तुम कल्पना करो, नवीन कल्पना करो,
तुम कल्पना करो’ या ‘तू चिंगारी बनकर उड़ री, जाग–जाग मैं ज्वाल बनूँ,
तू बन जा हहराती गँगा, मैं झेलम बेहाल बनूँ,
आज बसन्ती चोला तेरा, मैं भी सज लूँ लाल बनूँ,
तू भगिनी बन क्रान्ति कराली, मैं भाई विकराल बनूँ’ जैसे गीत उसी दौर के हैं. कहते हैं उनके इन्हीं गीतों से प्रभावित होकर एक फिल्मिस्तान स्टुडियो ने उनके फिल्मों में गीत लिखने के लिए अनुबंधित कर लिया. वहां चार साल गीत लिखने के बाद कहते हैं कि धार्मिक गीतों में उनका ऐसा जलवा जमा कि उन्होंने अगले लगभग दो दशक में करीब ४०० गीत अलग-अलग फिल्मों के लिए लिखे. उनके इस पहलू को लेकर अभी काम होना बाकी है.
बेतिया राज में शिक्षा-दीक्षा का अच्छा प्रचार-प्रसार होने के कारण हिंदी-अंग्रेजी की अनेक पत्र-पत्रिकाएं तो वहाँ आती ही थीं, दरबार का अपना प्रेस भी था जहाँ से किताबें भी छपा करतीं. इसके प्रभाव में उन्होंने कम उम्र से ही पत्रकारिता में भी हाथ आजमाए. १९३२ में उन्होंने ‘प्रभात’ और ‘मुरली’ नाम से क्रमशः हिंदी और अंग्रेजी में हस्तलिखित पत्रिकाएं निकालीं. बाद में कुछ दिनों के लिए सुधा से भी जुड़े जिससे उन दिनों महाप्राण निराला जी भी जुड़े हुए थे. उके बाद भी अनेक पत्र-पत्रिकाओं में संपादन कार्य से जुड़े. बाद में एक साल के लिए बेतिया राज के प्रेस के प्रबंधक रहे. लेकिन सबसे मुखर उनका गीतकार ही रहा. बाद में जब फिल्मों के लिए गीत लिखने लगे तो उस दौर में मंचों पर भी सक्रिय हुए. धीरे-धीरे उत्तर-छायावाद के कवियों की तरह उनके गीतों का स्वर भी रूमानी होने लगा, वे मंचों पर हित होने लगे. उसी दौर में शायद उनको ‘गीतों का राजकुमार’ कहा जाने लगा. एक बात है कि मंचों पर लोकप्रियता के बावजूद उनकी कविताओं में मंचीय लटके-झटके नहीं मिलते. बल्कि उनके गीतों का हमेशा जन से जुड़ाव बना रहा. उनकी भाषा की छ्यावादी तत्सम-प्रधानता दूर होती गई और वह अधिक जुबानी होती गई. उनके गीत जुबां पर चढ़ने लगे. ‘मेरा धन है स्वाधीन कलम’ या ‘तुम सा मैं लहरों में बहता मैं भी सत्ता गह लेता/ गर मैं भी ईमान बेचता, मैं भी महलों में रहता’ जैसे गीतों ने तो उनको लोकप्रियता के शिखर पर पहुंचा दिया. या फिर यह गीत-‘बदनाम रहे बटमार मगर, घर तो घर वालों ने लूटा/मेरी दुल्हन सी रातों को नौ लाख सितारों ने लूटा.’ इसमें कोई संदेह नहीं कि बच्चन, दिनकर, नरेन्द्र शर्मा जैसे कवियों के साथ मंच पर उनकी एक अलग ही छटा रहती थी.
बाद में उन्होंने हिमालय फिल्म्स और नेपाली पिक्चर्स नामक दो फिल्म कंपनियों की स्थापना की. बतौर निर्माता अपने बैनर से उन्होंने तीन फिल्मों का निर्माण भी किया. एक फिल्म थी ‘सनसनी’ जिसमें देवानंद-गीताबाली ने मुख्या भूमिकाएं निभाई थीं. एक और फिल्म ‘खुशबू’ में उस ज़माने के मशहूर अभिनेता मोतीलाल और अभिनेत्री श्यामा ने भूमिकाएं निभाईं. लेकिन संयोग से उनकी फ़िल्में चली नहीं. और वे भयानक आर्थिक संकट में घिर गए. लेकिन इससे उनका कवि रूप और प्रबल ही हुआ. उन्होंने इसके बावजूद किसी प्रकार का समझौता नहीं किया.
वैसे उनको असली प्रसिद्धि मिली १९६२ के चीन युद्ध के समय. उस समय उन्होंने कविता के माध्यम से जन-जागरण फैलाने का अभियान चलाया. घूम-घूम कर ‘शंकर की पूरी चीन ने सेना को उतरा/ चालीस करोड़ों को हिमालय ने पुकारा’ जैसे गीतों के माध्यम से उन्होंने चीन के खिलाफ माहौल बनाने का काम किया. और इसी अभियान के दौरान १९६३ में भागलपुर रेलवे स्टेशन पर उनका देहांत हो गया. महज ५२ साल की उम्र में. दुर्भाग्य की बात यह है कि इस राष्ट्रवादी कवि की कविताओं का उचित मूल्यांकन नहीं हुआ. वे सच्चे अर्थों में जनता के कवि थे इसीलिए आज तक वे जनता की स्मृतियों में बने हुए हैं. उनकी कविताएँ आज भी गुनगुनाई जाती हैं.