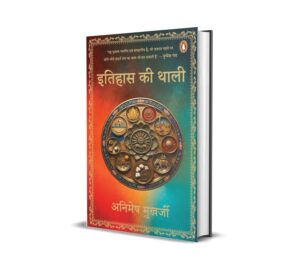मोहन राणा हिंदी के आप्रवासी कवि हैं, लेकिन उनकी कविताओं में भारत आकुलता की कोई व्यग्रता नहीं है. उनमें कोई अतीत्मोह भी नहीं है. बल्कि वे अपनी कविताओं के माध्यम से एक ऐसा सार्वभौम रचते हैं, जिसमें रिक्तता है, समकालीन मनुष्य का खालीपन है, वह बेचैनी है जो आज के समय की पहचान बन् चुकी है. मोहन राणा का नया कविता संग्रह प्रकाशित होने वाला है. उनके नए संग्रह से कुछ कविताएँ- जानकी पुल.
——————————————————————————————————————————-
दो पलों के बीच
खतरनाक होता है सबसे दो पलों के बीच अपलक
कभी पार कर लेगी सांस इन दो किनारों को
बिना पुल के किसी संकल्प सहारे
गोचर हो जाएगा भविष्य यहीं
बंद कर दूँगा उसकी खिड़की पर गुलेल मारना
आशा का जुआ उतार कर
मुक्त हो जाऊँगा अतीत की तानाशाही से
भयावह वर्तमान से,
फिलहाल मेरा झोला कंकड़ों से भरा है
नक्शानवीस
पंक्तियों के बीच अनुपस्थित हो
तुम एक खामोश पहचान
जैसे भटकते बादलों में अनुपस्थित बारिश,
तुम अनुपस्थित हो जीवन के हर रिक्त स्थान में
समय के अंतराल में
इन आतंकित गलियों में,
मैं देखता नहीं किसी खिड़की की ओर
रूकता नहीं किसी दरवाजे के सामने
देखता नहीं घड़ी को
सुनता नहीं किसी पुकार को,
बदलती हुई सीमाओँ के भूगोल में
मेरा भय ही मेरे साथ है
अपना एक देस
लोगों ने वहाँ बस याद किया भूलना ही
था ना अपना एक देस बुलाया नहीं फिर,
कोई ऐसा वादा भी नहीं कि इंतजार हो,
पहर ऐसा हवा भटकती
सांय सांय सिर फोड़ती खिड़की दरवाजों पर,
दराजों को खंगालता हूँ सबकुछ उनमें पर कुछ भी नहीं जैसे
चीज़ें इस कमरे में चीज़ें मैं भी एक चीज़ जैसे
मुझे खुद भी नहीं मालूम मेरी उम्मीद क्या निरंतर खोज के सिवा,
अपनी नब्ज पकड़े मैं देस खोजता हूँ नक्शों में
धूप की छाया से दिशा पता करते
पर मिलीं मुझे शंकाएँ हीं अब तक
सोफिया में पतझर
कब फिर वहीं लौटेगा धूमकेतू
तय समय किसी और जनम के साथ अंधेरे में प्रकाश पुंज,
भीगती दोपहर सोफिया में पतझर
एक चुपचाप शोर अपने आपसे बात करता,
समय नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें पहचान लूँ फिर से
जैसे देखा था पहली बार खुद को भूल कर
दरवेश सिफ़त
जो दरवेश सिफ़त उन्हें क्या कहते हैं. दुनियादारी के एकांत में.
यहाँ कुछ स्थिति ही ऐसी हमारे इस मकान में खिड़कियाँ बहुत
बाहर सब दिखता लगभग हर दिशा पर सवाल अक्सर होता कि कुछ दिखे मतलब का तो
कोई सरोकार सदृश्य के साये में,
शब्दों की दरारों में गिरती
काली चिड़िया की बेचैन अनुगूँज में सिवा पेड़ों
फीके आकाश पर घिसटते बादलों अलावा भी.
विडंबना गरमियों ना सरदियों के लिए रैनबसेरा अनूकल गनीमत
किसी अवदान की पुष्टि में शब्दकोष खोजना नहीं पड़ा एकांत जीने के लिए
उसके लिए काफी है एक खिड़की ही
गिरगिट
कितने नाम बदले चलन के अनुसार रंगत भी
बोलचाल के लिए बदले रूपक बदलने के लिए तेवर
और मुहावरे को नया हेयर कट
एक दो गालियाँ भी पर हर करवट बेचारगी के शब्दों से संपृक्त
सिक्का उछाल काम करती है यह ट्रिक हमेशा,
सोया हुआ हूँ बिल्ली के गले में कागज की घंटी बाँध सपनों में सलाहें देता
बदलाव की पुकार लगाता दिशाओं को गुमराह करता
लुढ़कता वसंत की ढलानों पर मैं गिरता हुआ पतझर ,
क्या मुझे याद रह पाएगा हर रंगत में हर संगत में
यह उधार का समय जो मेरी सांसों से जीता मेरा ही जीवन
रटते हुए भी अक्सर भूल जाता हूँ सच बोलना.
अगर
जंगल ना होते तो कैसे होती पहचान पेड़ की
दुख न होता तो खुशी को कैसे जानता
बनता कुछ और नहीं क्षण भर में ही अजन्मा नहीं
बस एक कमीज पतूलन सुबह शाम भोजन
कोई याद कभी करे एक नन्ही सी उम्मीद,
अगर चुनता मैं कुछ और
कह पाता कभी जो रह जाता हमेशा
बहरे प्रदेशों में अनसुना
खरगोश
हम अँधेरे में सुनते अपनी साँस
पर थोड़ी देर में वह बंद हो जाती सुनाई देना,
सुनते हैं अपनी धमनियों में रिसती पीड़ाएँ
पर थोड़ी देर में वे भी रुक जातीं रिसना
अँधेरा मिट्टी और हम एक हो जाते
1973
जाड़े की पहली लहर में सूख जाती आभासी उष्मा
हथेलियों को रगड़ते जमीन पे पड़ा पतझर टूटता थक चुके पैरों तले,
हरियाली धरती का नमक कुछ निकल पड़ता मुँह से खुद से कहते
अपने किसी कोने में सिमट जाता कोट को पसलियों में लपेट
ढीला होता जा रहा है हर साल यह उर्म के साथ,
मन में बज पड़ती आवाजों के ज्यूक बॉक्स से किसी प्रार्थना गीत की लहर,
वक्त था आया और गुजर गया
हम अपनी उधड़ी हुई आस्तीनों में अपने अलावा कुछ और नहीं पाते अंततः,
हर सुबह बायबिल को सुनते हुए
सुड़कती नाक पोंछते सर्द दिसंबर की सुबह
भरम अनेक
होती रहती खटर पटर कभी बर्तनों की
कभी सामान की कभी कमरों में अपनी नींद और सुबह के हमजीवों की,
जब लोगों से कहता हूँ, कट रही है
वे हँसी छुपाते हैरान गंभीर कहते हैं अरे नहीं
कैसी बात
बात जो मैं अब तक ठीक से ना कह पाया
अब भी
‘कबीरा कुँआ एक पानी भरे अनेक‘!
सबको नहीं मिलता पानी फिर भी, मिलता भरम अनेक
आलसी भी लगते मेहनती और झूठे भी सच्चे
कुदरत यह कबड्डी खेल खूब करती है, भरमाती मनुष्य को
और परिंदे तारों पर टँगे रहे आसमा भूल गया
बादलों की बहक में, रास्ता किसी समुंदर की तलाश में
खिड़की खोल भी दूँ फिर भी अँधेरा झिझकता है चौखट पर
कोने किनारों में सिमटता बाहर की रोशनी से विगत ही देख पाता हूँ
धूल पर झाड़न फेरता
देता हूँ जबरन हौसला गिर कर खुद को उठाते
निपट लूँगा जिंदगी के रोड़ों से, ये टोकते नहीं याद दिलाते हैं दोस्ती का अकेलापन.
देखा मुखौटा किसका चेहरा हर कोस कतार में अपना नाम बताते हुए
चौबीस घंटे चालू सुर्खियों के डिब्बे में मेरा दोस्त
संकट की पुड़िया को दर्दनिवारक विज्ञापित करता
अन्ना हम तुम्हारे साथ हैं मिर्च की पिचकारी आँखों में,
और थप्पड़ किसी नेता को, बुरे वक्त की निशानी कहते हैं बुजुर्ग चश्मे को ठीक करते
इन दांतों में अब दाने नहीं चबते हवा में मुक्के भांजते
प्रतिरोध की आँखों में मिर्च की पिचकारी मारता जॉन पाइक
जैसे छिड़कता हो गाफिल कोई नाशक दवा खरपतवार पर …
पालथी बैठे छात्रों के धीरज पर
दर्द से चीखना नहीं उन्हें तो उठकर राष्टगीत गाना चाहिए,
चीखते आँखों को बंद नहीं रख पाते वे खोल बंद नहीं कर पाते,
वही पिचकारी हाथ बन जाता एक कठपुतली हाथ थप्पड़ मारने के लिए,
भ्रष्ट गाल पर नहीं होता पर छाप कहीं और पड़ती है पाँचों ऊँगलियों की
किसी और चेहरे पर,
गुमनाम जिसे हर रात सोने के लिए नया फुटपाथ खोजना पड़ता है
एक दिन और दण्डवत नमस्कार इस धरती को
* कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे छात्रों पर लैफ्टिनैंट जॉन पाइक ने 18 नवं 2011 को मिर्च की पिचकारी से हमला किया.
पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन- सुन आवें हांसी।
घर में वस्तु न नहीं आवत, वन- वन फिरत उदसी। – कबीर
बबूल
जागते ही हर कर धर लेती मेरा भेस
दैनंदिन सांसारिकता आस पास मेरे अबाध
लग जाता मैं असली की पहचान में
अपना भी कोई भेस लगा कर
करीने से लगा रखा है मैंने अपनी उपलब्धियों को दीवारों पर
खोजा मैंने कई गुमशुदाओं को अपनी पहचान देकर
उनके खोने पर इश्तिहार चस्पाते हुए,
बबूल की शाखों से बाँध रखीं हैं उनकी यादें मैंने हवाई चप्पलों साथ
उसी न्यून हरियाली के कांटो में फंसा है मेरा मोजा भी,
भरा जा रहा हूँ उमसी हवा से कि बहुत हो गया अब कहते बहुत
कि बिना धरती के छोर पैदल गए होता जा रहा हूँ कोई पंखदार जंतु
जो उड़ नहीं सकता कहीं जा नहीं सकता सोया शीशाबंद आले में,
बदलती दिशाएँ रोशनी की
अपनी कील पर धूमती परिक्रमा अशेष
उपलब्धियों पर जमती धूल भी उपलब्धि कोई एक
मिली हुई चीज को खोने की कोशिश
लिखे शब्द को भूलने की आशा,
नकली को असली ना दिखा पाने का दुख
पहचान कर भी रोज़ उस अदृश्य ऐयार को.
जेन के लिए
पानी का रंग
यहाँ तो बारिश होती रही लगातार कई दिनों से
जैसे वह धो रही हो हमारे दाग़ों को जो छूटते ही नहीं
बस बदरंग होते जा रहे हैं कमीज़ पर
जिसे पहनते हुए कई मौसम गुज़र चुके
जिनकी स्मृतियाँ भी मिट चुकी हैं दीवारों से
कि ना यह गरमी का मौसम
ना पतझर का ना ही यह सर्दियों का कोई दिन
कभी मैं अपने को ही पहचान कर भूल जाता हूँ,
शायद कोई रंग ही ना बचे किसी सदी में इतनी बारिश के बाद
यह कमीज़ तब पानी के रंग की होगी !