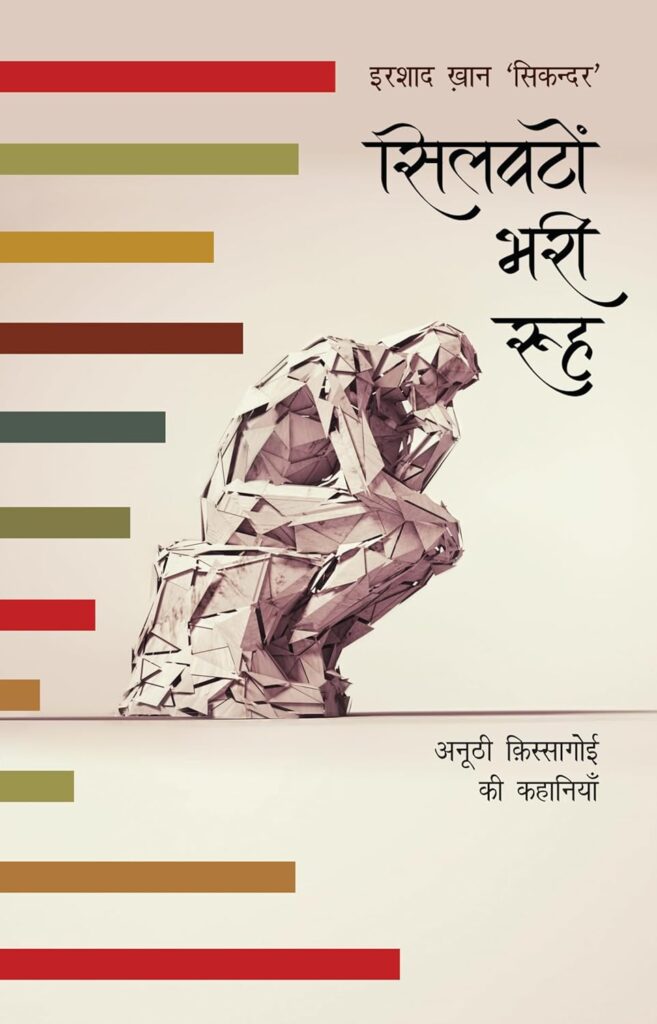युवा पत्रकार-कथाकार आशुतोष भारद्वाज छत्तीसगढ़ के जंगलों का सच लिख रहे हैं. हाल में ही अबूझमाड़ को लेकर इंडियन एक्सप्रेस में उनकी रपट काफी चर्चा में रही. यहां उनकी डायरी के कुछ अंश- जानकी पुल.
———————————————–
मार्च।
कोई कथित नक्सली जब गिरफ्तार होता है, जिसके खिलाफ किसी हिंसा में संलग्नता का सबूत नहीं होता तो पुलिस जुर्म-प्रमाण स्वरूप अक्सर उसके पास से ‘नक्सली साहित्य’ की जब्ती दिखाती है। इस ‘साहित्य की प्रतिनिधि रचनाओं’ का कभी खुलासा नहीं होता, लोहे का काला बंद बक्सा अदालत में पेश होता है उसके बाद थाने के मालखाने में। ऐसी ही एक गिरफ्तारी हाल ही यहां हुयी जिसमें ‘ढेर सारा नक्सल साहित्य’ बरामद हुआ। जुगाड़ से ‘प्रतिबंधित रचनायें’ दर्शनार्थ हुईं — ब्रेख्त की कवितायें, भगत सिंह, मार्क्स, एंगिल इत्यादि के पोस्टकार्ड। ‘क्या जुल्मतों के दौर में गीत गाये जायेंगे/हा, जुल्मतों के दौर के ही गीत गाये जायेंगे।‘
‘तुम्हारे पंजे देखकर डरते हैं बुरे आदमी/तुम्हारा सौष्ठव देखकर खुश होते हैं अच्छे आदमी/यही सुनना चाहूँगा अपनी कविता के बारे में।‘
ब्रेख्त की प्रसिद्ध कविताओं के कार्ड। एक खाकीधारी ने पूछा इसमें नक्सली साहित्य क्या है, उसके बास ने हड़का दिया। ऐसा नहीं बास की दुश्मनी है अभियुक्त से, वह पूरी शिद्दत से मानता है कि यह प्रतिबंधित चीजें हैं और अधिक मात्रा में किसी के घर से उनकी बरामदगी उसका माओवादी होना साबित करती हैं। उससे बहस कीजिये और वह पूरी निष्ठा से बतलायेगा कि वह समाज को भयमुक्त करने व सबको सुरक्षा देने के लिये ही इन कठिन इलाकों में अपना तबादला करा आया है। बात आगे बढ़ेगी तो दंड संहिता और अखीर में भारत का संविधान, जिसकी कई प्रतियां उसकी कुर्सी के पीछे बुक शेल्फ में चमकती हैं, आपके सामने बिछा देगा। हाँ, यह नहीं बतलायेगा एक ही किताब की इतनी प्रतियां क्यों रखे रहता है वह।
उसकी मूर्खता-मूढ़ता के किस्से आकाशवाणी से प्रसारित कीजिये, उसकी नादानी पर तरसिये या उसके विरोध में लिखिये। वह खुद को आपका एकमात्र रक्षक मानता है। कैसा भी प्रतिरोध, जब तक वह संविधान-सम्मत न हो यानी मानवाधिकार आयोग से आये नोटिस की शक्ल में न हो, उसकी संवैधानिक चमड़ी को खुरचता तक नहीं।
————————–
मार्च ही।
सत्ता जीवन को विरोधी ध्रुव में विभाजित हुआ मानती है। अगर आप पक्ष में नहीं तो सत्ता के अनिवार्य प्रतिपक्ष हैं। शत्रु हैं। संविधान की शपथ लिये कोई पुलिस अधिकारी, भले वह शपथ अपने क्रियान्वयन में कितनी बेईमान साबित हुई हो, चीजों को सिर्फ दो अर्थों में समझता है— संविधान-सम्मत या विरोधी। कविता भी उसके अनुसार संविधान की रक्षा के लिये होगी या तोड़ने के लिये। याद रखें वह कोई क्रूर, बर्बर स्टीरियोटाइप्ड खाकीधारी नहीं, ईमान और इंसानियत से लबरेज मनुष्य होगा।
इस विभाजन रेखा से परे की चीजें उसके लिये मायने नहीं रखती, दरअसल अस्तित्व में ही नहीं आती। संवैधानिक अनुच्छेदों से परे भी जीवन है, उसका जैविक-मानसिक विधान नहीं स्वीकारता। लेकिन यह उसका आनुवंशिक गुणसूत्र नहीं है। कालेज के दिनों तक जब वह गिटार बजाया करता था उसका इस किताब से फकत इतना परिचय था कि इसे भारत रत्न बाबासाहेब भीमराव डाक्टर अंबेडकर ने लिखा था और इसकी प्रतियां उत्तर भारत के खेतों, मौहल्लों में स्थापित नीली मूर्ति के दाहिने हाथ में टंगी थीं। संघ लोक सेवा आयोग का पवित्र इम्तिहान उत्तीर्ण कर यह ग्रंथ झटके में उस गिटारवादक का संचालक, अभिवावक हो गया। इतना त्वरित रूप-रूहांतरण मुश्किल है।
उसकी इस विधानांधता का आप लुत्फ भी ले सकते हैं कि बेचारे की बुकशेल्फ में दंडसंहिता और साक्ष्य अधिनियम के सिवाय कुछ नहीं, सुनाने के लिये महज मुठभेड़ों के किस्से जो अधिकांश फर्जी या मानवाधिकार आयोग का नोटिस झेल रहे हैं। वह गोदार्द और कुमार गंधर्व से अनजान है, एक निम्नतर प्राणी है।
लेकिन संवेदनशील, सर्वव्यापी दृष्टि होने के गुरूर में जीती कला क्यों इस वर्दीधारी पर अंतिम निर्णय सुनाये? कविता विद्रोही और बागी की अनिवार्य संगिनी रही है। उसने खुद को हमेशा सत्ता के आखिरी विपक्ष बतौर प्रस्तावित, प्रतिस्थापित किया, लेकिन इस अनिवार्यता ने क्या उसकी निगाह को निष्पक्ष रहने दिया? सत्ता का अनुषंगी होना अगर शब्द के लिये सबसे बड़ा कुफ्र है तो सत्ता से सर्वकालिक संदेह का संबंध भी सयानापन नहीं। और अगर संदेह को शब्द का धर्म मान धारण किया है तो शुरुआत खुद अपनी निगाह पर, मान्यता पर संदेह से करनी चाहिये।
तब शायद सत्ता के अनदेखे पहलू भी दिखलाई देंगे, स्थापनाओं को चुनौती देते हुये। मसलन कि रणभूमि में रिपोर्टिंग करते पत्रकारों की सबसे अधिक मदद पुलिस ही करती है, उन्हें खतरे से बचाती है। जंगल में कहीं इंटरनैट, फैक्स, तस्वीर स्कैन करने इत्यादि की सुविधा नहीं तो एसपी या कलक्टर का आफिस ही खबर भेजने का सहारा होता है। थाने के जनरेटर से कैमरा और लैपटाप की बैटरी चार्ज की जाती है।
पुलिसिये को मालूम होता है जो खबर रिपोर्टर उसके दफ्तर के कंप्यूटर पर टाइप कर रहा है, प्रशासन के ही विरोध में जायेगी कि वह जो कागज चोरी छुपे स्कैन कर रहा है दरअसल थाने की ही किसी फाइल से उड़ाये हुये हैं, तस्वीरें हड़बड़ी में भेज रहा है वो हवालात में बंद किसी चोटिल कैदी की चुपके से खींची गयी तस्वीरें हैं जो अखबार में छपते ही पमाड़ा हो जायेगा लेकिन थानेदार अनदेखा कर देता है। अगर सिपाही इशारा भी करे तो कहता है — ‘कर लेने दो, मीडियावाले हैं…काम कर रहे हैं अपना…भला ही होगा सबका।’
अचंभा लगेगा लेकिन दुर्गम जगहों में रिपोर्टिंग बगैर पुलिस -प्रशासन की खुफिया मदद के असंभव है। यह वो खुफिया लम्हे हैं जब खाकी अपने धर्मग्रंथ को ढील देती है, आपको अवसर देते हुये कि आप उस पर हमला कर सकें।
अगर सर्वमान्य क्रूर खाकी अपने संविधान में अपवाद और आपातकाल का स्थान बचाये हुये है तो क्या स्वघोषित संवेदनशील कला को सत्ता के प्रति अपनी निगाह और संबंध पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिये? जब कवि बस ड्राइवर में पिता तलाश लेता है, स्टीयरिंग के सामने लटकती चूड़ी में उसकी बिटिया का अक्स देख जाता है तो बंदूकधारी से छुआछूत क्यों? लहना सिंह भी तो सिपाही था।
दूसरे, सिपाही का दोष शायद फकत इतना कि वह किसी एक किताब पर अंतिम आस्था लिये जी रहा है। किसी ग्रंथ को आखिरी मान लेना, भले वह ईश्वरीय सत्ता प्रतिपादित करता हो या किसी विचार पुरुष की आदिपुस्तक, सृष्टि को विपरीत ध्रुवों में विभाजित कर देता है। अगर आपको किसी नियामक व्यवस्था में जीना है तो किसी किताब को होना ही होगा जिसके हर्फ उस समूचे ढांचे को वैधता-वैधानिकता देंगे। आप एडम स्मिथ को उद्धृत करें, गीता, मार्क्स या हिंद स्वराज को। व्यवस्था का सबसे छोटा कलपुर्जा भी खुद को सत्यापित आदिपुस्तक से ही करेगा। इसलिये या तो हर किस्म की व्यवस्था से बाहर निकलिये और अगर व्यवहारिक-सामाजिक कारक बतलायें कि ढांचा बेविकल्प है तो फिर इस ढांचे के प्रति अनिवार्य द्वंद्व का संबंध बेकार है। वह बिंदु खोजने ही होंगे जहां विलोम दिखलाई देते अवयव से भी संवाद हो सके।
आखिर कितने कवि होंगे जो आपको अपने घर में सम्मान से बिठायेंगे, मेज कुर्सी, कागज-पैन, कंप्यूटर-स्कैनर देंगे कि आप उसके विरोध में लिख सकें, उसे बेनकाब कर सकें?
पतझर। पत झर। अब न झर।
— कबकी आई तू?
— सुबह अंधेरे, तू ही तो बोला था महुये के नीचे मिलना…कहां था? सब लोग आ गये देख…खत्म हो जायेगा महुआ सारा।
— कोई नहीं, बहुत गिरा है आज। चल शुरु करते हैं।
पतझर के दिन हुआ करते थे। उनके जंगल में ढेर झरता था, पतझर। सुबह चार से दोपहर ग्यारह तक महुआ टपकता। सफेद छोटा फूल। धरती पर बिखर जाता। महुए का पेड़ खाली होता जाता। दोनो जल्दी उठ जाते। नीचे बिखरी सूखी लाल पत्तियों के बीच महुआ बीन टोकरी में भरते जाते। अजब था यह वृक्ष। पूरे साल का खुमार इस मौसम में उड़ेल देता। नशे के बीज वे धरती से बीनते। पूरे साल की हसरत अपनी झोंपड़ी के पीछे इकठ्ठा करते। महुए के जादुई लट्टू की नोक पे रात थिरकती। जंगल उनका काजल था, नदी गीला महावर जिसमें डूब वे अपनी देह का सुर्ख श्रंगार करते।
बीते पत्ते थे वो लेकिन। इस जनवरी वह एक थाने में मरा पाया गया। पुलिसिये बोले नक्सली था, फांसी लगा हवालात में आत्महत्या कर ली। कई मील दूर जंगल को चीर कर आया पूरा गांव उमड़ पड़ा। सड़क पर। पोस्टमार्टम के बाद लाष सरकारी एंबुलैंस में जगदलपुर से दंतेवाड़ा होती आ रही थी। एंबुलैंस ने जानबूझ कर लंबा रस्ता लिया था कि गांव वालों से बच जाये, चुपचाप उसका संस्कार हो जाये। सबको लेकिन खबर हो गयी थी, लठ्ठे डाल सड़क रोक दी गयी थी।
एंबुलैंस आयी थी। विराट चीत्कार, विकराल रुदन। गांव की औरतें गाड़ी के अंदर चढ़ीं थीं — कांच के नीचे सफेद में लिपटी एक देह। स्त्रियां कांच को मुठ्ठियों से पीटतीं थीं। कांच पर कांच टकराता था। चूड़ी चटक कर टूटती थीं, ताबूत का कांच मजबूत था। सरकारी था शायद इसलिये।
वह सड़क किनारे सिर झुकाये बैठी थी। चुप पोटली। बेहरकत। वह मुझे नहीं जानती थी। उसे नहीं मालूम था मैं दस घंटे दूर रायपुर से रात को चल वहां आया हॅूं, मेरे पास उसके पति की मैडीकल रिपोर्ट है कि उसे मृत्यु से पहले बेइंतहा पीटा गया था, उसके गुप्तांगों पर सूजन थी, समूचे बस्तर के किसी थाने में उसके खिलाफ कभी कोई मामला दर्ज नहीं हुआ था, कहीं उसका नाम नहीं था, फांसी लगाने के लिये उसके पास हवालात में कोई रस्सी नहीं थी, सिर्फ एक शॉल जिसे थोड़ा चीर उसने खुद को दरवाजे के महज तीन फुट उॅंचे कुंदे से टांग लिया कि उस शॉल की तस्वीर है मेरे पास और हवालात के दरवाजे की भी।
बेखबर वह चुप बैठी थी। ‘नक्सली’ पति के चिन्ह अपने भीतर सहेज। बाहों की जकड़ में फंसे घुटने बीच सिर झुकाये।
अगली सुबह मेरे अखबार ने पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर छापी थी खबर के साथ — पति की लाष की प्रतीक्षा करती गर्भवती स्त्री। दूसरे दिन मानवाधिकार आयोग का राज्य सरकार को नोटिस आ गया था।
यह लेकिन दो महीने पुरानी बातें हैं। पत्ते इस बरस फिर झरते हैं। महुआ फिर टपकता है। आज अठारह मार्च की सुबह वह अकेली टोकरी लेकर जाती है सफेद फूल बीनती है। वह अब भी वैसी ही है। चुप। चाप। पेट पर उभार थोड़ा अधिक हुआ है। शायद। दो सौ चालीस दिन की संतान भी अपनी उपस्थिति उसकी काया पर नहीं बतला पाती। भूख का गर्भषास्त्र यह। गर्भ का भूखशास्त्र।
महानगरीय स्त्री के इतने उभार पर शायद कहा जायेगा — थोड़ी मोटी हो गई हो, डाइटिंग करो। महानगरों की संताने सौवें दिन से पहले ही अपनी घोषणा कर देती हैं। दौर्बल्य बनाम सौष्ठव का द्वंद्वात्मक विधान जन्म से पहले निर्धारित हो जाता है। इस लम्हे को जी चुकी अपने परिवार की स्त्रियां याद आती हैं। घेरदार गाउन पहनती हैं। अचक कर चलती हैं। दिनभर कुछ टूंगती रहती हैं।
वह लेकिन अकेली महुआ बीनती है। खुद को खुद ही संभालती है। चुप। चाप। घनी पहाडि़यों के बीच। परसों उसे ढाई घंटे की लुढ़कती लड़खड़ाती बस में चल कलक्टर आफिस जाना है, बाबू की खिड़की पर लाइन में होना है पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लेने। कई मर्तबा पहले भी जा चुकी है लेकिन तारीख आगे बढ़ जाती है।
‘नक्सली’ पति का मृत्यु प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय लेने जाती स्त्री ने चलती बस में बच्ची को जन्म दिया।
क्या यह भी होना बाकी है?
कई साल बीतेंगे, बच्ची भी महुआ बीना करेगी। अपने पिता को पूछेगी। जब वह फ्राक पहनने लगेगी, एक दिन मां उसे उस थाने ले जायेगी जहां पिता ने शॉल गले से लपेट खुद को खत्म कर लिया था।‘
निर्मल ने कभी महुए की मुस्कुराहट लिखा था, महुए की मृत्यु उपयुक्त रहता।
उसका थोड़ा पढ़ा देवर मद्रास में अपना काम छोड़ यहां आ गया है। उसने मुझे इस इलाके में घूमते देखा तो झट पहचान गया — आप ही आये थे न जनवरी में।
अपने घर ले गया, बोला अब यहीं रहेगा, बड़े भाई की मृत्यु को मरने नहीं देगा। मन हुआ बतलाउॅं वह किस धंसकती जमीन पर अटका है। पिछले दो महीनों में वह पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक नहीं हासिल कर पाया है। यह संघर्ष महज आंतरिक है, आत्म-तुष्टि के सिवाय कुछ नहीं देता, न देगा। टिके रहने की संतुष्टि फकत, उसे भी अगर कुरेदो तो भीतर सिर्फ कोरी हवा दिखती है। ठंडी, सूखी हवा जिसके थपेड़ में सफेद फूल बिखरे चले जाते हैं।
उसे नही मालूम आत्मविष्वस्त पुरुषार्थ की जिस अरगनी पर उसने यह लाश टांग दी है वह कितनी कमजोर है। साल बीत जायें, पैरमापारा में रहते वह अधिकाधिक इतना कर पायेगा कि कलैक्टर, एसपी या स्थानीय पार्षद या विधायक को एकाध ज्ञापन दे आयेगा। उस ज्ञापन की फोटोस्टेट पावती पर सरकारी मोहर होगी जिसे वह अपनी फाइल में सहेज रखेगा, मुझ जैसे कभी यहां आयेंगे तो दिखलायेगा। पूरी कहानी षुरु से सुनायेगा। एक रात आखिर अरगनी टूटेगी, सूख चुकी लाश भरभराती गिरेगी।
यह लम्हा शब्द-पौरुष का गुमान भी ध्वस्त करता है, स्वीकारने को बाध्य करता है कि शब्द एक निर्वीय सत्ता है। स्वांतः सुखाय, स्वकेंद्रित। शब्द की पहुंच महज शब्द है, इसका प्रयोजन शब्द, निशाना शब्द, हासिल शब्द। वही जो संपादक दिल्ली से कहते हैं — हमेशा याद रखो, तुम महज एक रिपोर्टर हो। सिर्फ रिपोर्टर।
हथियार कहां शब्द बख्तरबंद भी नहीं है। शब्द दरअस्ल निश्शब्द है।