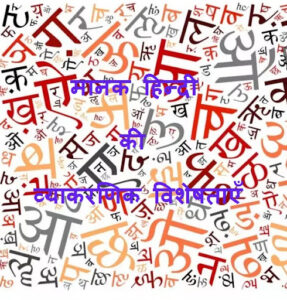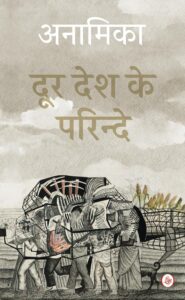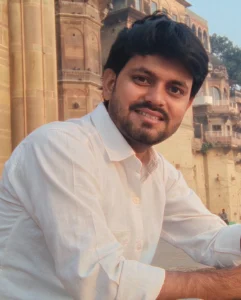दिल्ली में बलात्कार की नृशंस घटना के बाद जिस तरह से छात्र-युवा सड़कों पर उतरे हैं, उसके बाद इस आंदोलन की प्रकृति को लेकर बहस शुरु हो गई है. राकेश श्रीवास्तव के इस लेख को भी इसी सन्दर्भ में देखा जा सकता है- जानकी पुल.
===========================
…यह महज उच्च जातियों या ‘प्रभु वर्ग’से बने शहरी मध्यवर्ग की आकांक्षाओं और विश्व दृष्टि का प्रोजेक्शन हैं या इसका अर्थ इससे दूर तक जाता है…
बलात्कार की उस निर्मम ‘रेयरेस्ट ऑफ द रेयर’ घटना के विरूद्ध इंडिया गेट से लेकर रायसीना हिल पूरे राजपथ पर जबरदस्त प्रदर्शन। एक से अधिक चैनल उस प्रोटेस्ट के प्रति सहानुभूति दिखाते हुए भी उसे बार-बार राजपथ पर जुटी ‘भीड़’ का नाम दे रहे थे। क्या अन्ना आंदोलन में पहली बार बहुत प्रभावी रूप से सामने आई यह प्रवृत्ति जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वाकई एक भीड़ है, आंदोलन है या आंदोलन की पारंपरिक समाजशास्त्रीय परिभाषा का अतिक्रमण करते हुए भी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। यह महज सामान्यत: उच्च जातियों या ‘प्रभु वर्ग’ से बने शहरी मध्यवर्ग की आकांक्षाओं और वल्र्ड व्यूह का प्रोजेक्शन हैं या इनका अर्थ इससे दूर तक जाता है। क्या छात्र समुदायों के बीच कंयूनिस्टों या राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आदि ने जो पीछे काम कर रखा है और वह जो एक सांगठनिकता की पृष्ठभूमि है ऐसी भीड़ के प्रथम दौर का मोबलाइजेशन उससे होता है फिर पीछे पीछे मीडिया की शोर की बदौलत और लोग जुटने लगते हैं या ऐसे आंदोलन राजनीतिक संगठनों के लिए भी अचंभे की बात साबित हो रहे हैं। कई लोग तो इन्हें खुले तौर पर मीडिया प्रायोजित फैड तक कहते हैं। या फिर ‘युवा’ एक विशिष्ट और अंतिम रूप से प्रभावी समाजशास्त्रीय इकाई बनकर उभर रहे हैं।
बलात्कार की यह घटना नृशंस थी। ऐसी विदारक जिसकी कोई हद नहीं। सबकी रूह कांप उठी। पूरे देश और दिल्ली का व्यक्ति-व्यक्ति व्यथित था। यह घटना-विशेष तो सभी आम-आदमी के लिए एक मुद्दा है। इसलिए राजपथ पर जो भीड़ जुटी उससे सबने रिलेट किया होगा यह निश्चित है। पर इस प्रसंग में मेरे लिए जो कहना महत्वपूर्ण है वह यह कि यह भीड़ जो जुटी थी वह युवाओं की थी जिसमें लड़कियों का अनुपात पहले के ऐसे आंदोलनों की तुलना में अधिक था। बलात्कार की इस घटना ने युवाओं विशेषकर लड़कियों के असुरक्षा-बोध को हलक पर ला दिया है। विशेषकर वह असुरक्षा जो कम्यूट करने के दौरान ‘राउडी टाईप’ नाम से जानी जाने वाली दिल्ली और उसके आस-पास की एक डिस्टिंक्ट जनसंख्या के लोगों से हमेशा बनी रहती है। शिक्षित मध्यवर्ग के लोगों और इन ‘राउडी टाईप’ में हमेशा-ही एक सामाजिक-दूरी का संबंध रहा है। इस हमेशा से वलनिरेवल संबंध-व्यवस्था के भीतर इस बार एक चरम दुर्घटना घटी है।
हमारा प्रसंग यहां आंदोलन की प्रकृति है। यह सच है कि यह भीड़ अपनी प्रकृति में वही थी जो अन्ना आंदोलन के शुरूआती दौरों की भीड़ थी। अन्ना आंदोलन में भी केंद्रीय रूप से भीड़ शहरी शिक्षित मध्यवर्ग विशेषकर इस वर्ग के युवा लोगों की भीड़ थी। बाद में अन्ना आंदोलन में परिधि पर वह भीड़ जुटने लगी जिसे आमआदमी का वृहत्तर क्रौस-सेक्शन कह सकते थे। कल की भीड़ भी शहरी शिक्षित मध्यवर्ग युवाओं की भीड़ थी। कई दलित-चेतना के विद्वानों ने इसे मूलत: सवर्णवादी विश्व-दृष्टि वाले युवा कहा है, और कहा है कि यह वही भीड़ है जो आरक्षण-विरोध के नाम पर इकट्ठी होती आई है। अरूंधती रॉय ने भी इशारा कहा है कि यह भीड़ वह चेतना ली हुई भीड़ नहीं है जिसे हर प्रकार के बलात्कार की चिंता है। यानि इन्हें देश के हर जगहों पर हर जाति और वर्ग में होने वाले बलात्कारों की चिंता नहीं है बल्कि इनकी चिंता मात्र वैसे संभावित बलात्कार से है जिसका डर इन्हें भी समाया है।
मेरा मानना है कि यह तो सच है कि चाहे अन्ना आंदोलन हो या बलात्कार पर क्षोभ प्रकट करता यह आंदोलन, ये प्रधानत: श्हरी मध्यवर्ग के आंदोलन हैं। पर इनकी जो भावात्मक उर्जा है वह वर्गीय हितों का अतिक्रमण करती है और भविष्य के नाम कुछ महत्वपूर्ण संकेत-सूत्र छोड़ती है।
कल के आंदोलन के बारे में कुछ कंयूनिस्ट छात्र-संगठन यह इम्प्रेशन छोड़ रहे हैं जैसे यह आंदोलन उनका जुटाया हुआ है और उन्होंने जो मुद्दे आर्टिकुलेट किए हैं वही इस आंदोलन के मुद्दे हैं। यह सही प्रतीत होता है कि जेएनयू के छात्रों का मोमेन्टम खड़ा करने में योगदान था पर यह संदेहास्पद ही है कि पूरे के पूरे मोमेंटम पर उनकी नैतिक दावेदारी उचित है, और यह भी कि महिला-मुद्दों के बारे में जो वामपंथी छात्र संगठनों का वैचारिक स्टैंड है वही इस आंदोलन से पुश हो रहा है।
जब अन्ना आंदोलन की शुरूआत हुई थी तो उसे लोकप्रिय होने की संभावना देख उसे आरएसएस ने भी हवा दी थी, शायद इस आशा के साथ कि एंटी- इस्टैवलिशमेंट भावनाएं अंतत: तो हमारे ही झोली गिरेंगी और उस आंदोलन से पैदा वैधता अपने काम आएगी। अन्य राजनीतिक दलों ने भी इसमें अपने लाभ की संभावनाएं तलाशी थी। पर मूंगेरीलालों के हसीन सपने पूरे न हुए थे।
अन्ना आंदोलन के समय से अब तक युवाओं का और उनके पीछे-पीछे आम आदमी का यह हुजूम इतनी बार खड़ा हो गया कि उसकी बारंबारता में एक पैटर्न और एक भविष्य को पढ़ा जा सकता है। यह युवा अभी मात्र शहरी मध्यवर्गीय युवा तो है, पर इसकी क्रोड़ में वर्गीय हितों से ऊपर ‘युवा-मात्र’ होने की संभावना छिपी है जिसके साथ देश के सभी क्षेत्रों और वर्गों के युवा कालक्रम में अपनी उर्जा मिला डालेंगे, विशेषकर सिस्टम में सुधार से संबंधित मैक्रो स्तर के मुद्दों के संदर्भ में।
भारत के मध्यवर्ग की आलोचना पिछले दशकों में होती रही कि यह प्रभुवर्ग मानसिकता रखने वाला, संकीर्ण नजरिये वाला और दूरगामी सामाजिक-सक्रियता से कोसों दूर वर्ग है। पर तब से अब तक गंगा में अगर नहीं बहुत-ज्यादा तो भी अच्छा-खासा पानी बहा है। आज मध्यवर्ग अंतनिर्हित रूप से बहुविध हो चला है जिसमें गांवों से शहर आकर यहां सफल हुए और जम गए लोग, सभी जाति समूहों के लोग अच्छी खासी संख्या में शामिल हैं। बहुविध स्रोतों से बना मध्यवर्ग बाह्य रूप से शैक्षणिक- सांस्कृतिक धरातल पर समरूप भी हो चला है। यह कहना तो अभी दूर की कौड़ी है कि भारतीय-मध्यवर्ग के चरित्र में आमूल-चूल परिवर्तन आ गया है, पर यह जरूर है कि भारतीय नव-मध्यवर्ग का मुहावरा तो उलझ ही गया है। अन्ना आंदोलन या वर्तमान राजपथ आंदोलन को भारत के पारंपरिक मध्यवर्ग के संकीर्ण हितों का प्रोजेक्शन मात्र कहना मेरी नजर में ज्यादती है और इसका सही अर्थ तभी निकलेगा जब देश के अन्य पुराने और हालिया प्रवृत्तियों के साथ इसकी संगति बैठाई जाएगी। मेरे द्वारा कल के आंदोलन के नाम के साथ अन्ना आंदोलन का नाम लेने का यह अर्थ कदापि न समझा जाए कि मैं कल के आंदोलन का श्रेय किसी भी प्रकार अन्ना आंदोलन से उभरे नेताओं को देने का प्रयास कर रहा हूं। इस दोनों का नाम एक साथ लेने का अर्थ मात्र इतना है कि मैं सामाजिक मुदृों के लिए शहरी शिक्षित मध्यवर्ग के बार-बार जुटने के निहितार्थों की चर्चा कर रहा हूं।
आजादी के बाद के भारत में विचारधाराओं के इर्द-गिर्द बुने सांगठनिक आंदोलन जिनमें राजनीतिक दलों के आंदोलन और जल-जंगल-जमीन के जुझारू आंदोलन दोनों शामिल हैं की सुगठित धाराएं तो रही ही हैं, इनके अतिरिक्त एक नियमित प्रवृति और रही है जो है क्षणिक स्वत:-स्फूर्त जन-प्रस्फोटों की और स्थानीय स्तर पर किसी सामाजिक कार्यकर्ता या प्रशासक को नायक बनाकर छोटे समय के जन-उभारों की। क्रोधों का ऐसे सड़क पर उतरने या किसी स्थानीय जुझारू कार्यकर्ता को नायक बनाने के पीछे सिस्टम की असफलताओं से जनित कुंठाएं काम करती रही हैं। जहां हमारे चुने हुए प्रतिनिधि और सरकारी-तंत्र हमारी आकांक्षाओं को तुष्ट करने में असफल होते थे वहां जनता का गुस्सा समय समय पर सिस्टम—जनित किसी दुघर्टना पर निकलता रहता था। या जनता की परिकल्पना में उसकी तात्कालिक मनोविज्ञान को तुष्ट करता कोई मसीहा बैठ जाता था। यह सब देश के हर क्षेत्र में विशेषकर सत्तर के दशक से लगातार चल रहा है। इन लघु-अवधि जन-उभारों और नेताओं के पीछे मोटिवेशन सिस्टम में व्यापक सुधार की गहरी बैठी आकांक्षा होती थीं। यानि इन्हें संगठित अच्छे- बुरे सभी आंदोलनों के समानांतर एक स्वतंत्र धारा कह सकते हैं। जहां जल-जंगल-जमीन के विचारधारात्मक आंदोलन अपने केंद्र में किसी माइक्रो इस्यू को रखते हैं जिस बिंदु से वे बड़े परिवर्तन के तर्कों को क्रमश: बिल्ड-अप करते हैं, वहीं उक्त छोटी अवधि के जन-उभारों की कल्पनाशीलता में ऐसे प्रतीक होते थे जो सिस्टम में आमूल-चूल सुधार की आकांक्षा को प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्ष एड्रेस करने वाले होते थे। ऐसे कई उभारों के नेता अक्सर स्थानीय जल-जंगल-जमीन के नेता भी हुआ करते थे। स्वयं अन्ना हजारे ने ऐसे कई उभारों का नेतृत्व किया है।
देश भर में ऐसे तमाम छोटे छोटे जन-उभारों में ऊर्जाएं संग्रहित होती आ रही हैं। बड़ी युवा जनसंख्या, मीडिया और सोशल मीडिया के उभार ने फैले हुए जन-उभारों में फंसी उर्जाओं को समेकित कर दिया है। वही जो छिटपुट प्रवृति रही है अब बड़े रूप में दिख रही है। अन्ना आंदोलन से लेकर कल के प्रोटेस्ट तक को हम इसका ही पुराने जन-उभारों की परंपरा का नया अवतार कह सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इन उभारों को उनके जेनेसिस पर जाकर पकड़ें तो हम पाएंगे कि यदा-कदा तात्कालिक प्रतिक्रियाशीलताओं के प्रदर्शन के बावजूद ये प्रगतिशील और अंतर्निहित रूप से सिस्टम को ओवरऑल दुरूस्त करने की आकांक्षा वाले उभार या आंदोलन रहे हैं। इन्हें अंतर्निहित रूप से प्रभु-वर्गीय कहना गलत है। यह जल-जंगल-जमीन और दलित आकांक्षाओं के आंदोलनों से नहीं बने हैं पर उनका विरोधी भी नहीं है। यह सभी आंदोलन एक दुरूस्त सिस्टम के लिए युवा-वर्ग का मनोवैज्ञानिक स्तर पर ‘विश’ का प्रोजेक्शन है। और बात जब ‘विश’ करने की है तो हम ऐसा ‘विश’ कर सकते हैं कि कालक्रम में इस शहरी शिक्षित और प्रभु-वर्ग से दिखने वाले युवा के साथ अन्य युवा जुड़ते जाएंगे। हम यह विश कर सकते हैं कि ‘युवा’ ‘सिस्टम—मेंकिंग’ के मुदृों को आर्टिकुलेट करता और क्रमश: बड़े आंदोलन खड़े करता चला जाएगा।
ये आंदोलन मुख्य धारा मीडिया के जितने नहीं हैं उससे कहीं ज्यादा सोशल-मीडिया के हैं। ये आंदोलन मुख्य धारा मीडिया से जितने नहीं बने हैं उससे ज्यादा मीडिया इनके कंधे की सवारी करता है।
‘रंग दे बसंती’ में सभी नायक अलग-अलग सामाजिक-पृष्ठभूमियों के हैं, पर अपने भीतर जमी अपनी पृष्ठभूमियों को तोड़कर ‘नए युवा’ बनते हैं। क्यों न एक समाजशास्त्रीय यथार्थ-भूमि पर एक ‘विश’ को खड़ा करें। आखिर राजनीति वह क्षेत्र है जिसमें संभावना है असंभव को संभव बना डालने की।