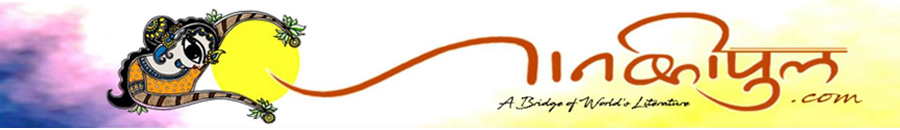प्रसिद्ध लेखिका अर्चना वर्मा का यह लेख राजेंद्र यादव की पुस्तक ‘स्वस्थ आदमी के बीमार विचार’ के सन्दर्भ में लिखा गया है- जानकी पुल.
========================
सुना है, राजेन्द्र जी से ही, कि महाभारत को मराठी में ‘यादवी’ कहते हैं और कुछ नंगई कुछ गुण्डई के अर्थ में ‘यादवी‘ मचा के रखना आम मुहावरे की तरह इस्तेमाल हुआ करता है। अपने हिन्दी के साहित्य जगत में भी ठीक ठीक महाभारत तो नहीं, लेकिन कुछ कुछ मेल खाते से रंग ढंग में, अपने देशकाल के अनुरूप बेहद टुच्चे से पैमाने पर, जब-तब यादवी मची रहती है। प्राय: उसके अगर कर्ता नहीं तो सूत्रधार हुआ करते हैं यादवनामी राजेन्द्र लेकिन इस बार की यादवी स्वयं उनके द्बार पर बाजे-गाजे समेत सम्पन्न ‘परिघटना’ रही और वे कर्ता या सूत्रधार की पदवी से वंचित पाये गये। उस हैसियत से कुछ साथी-सँगातियों समेत नमूदार हुए अजित अंजुम। राजेन्द्र जी के भृत्य-अभिभावक किशन की समझदारी से दरवाज़ा भीतर से बन्द कर लिया गया। आशंका जब चीख-पुकार और गाली गलौज की हदें पार कर मारधाड़ को पहुँचती नज़र आई तो किशन ने भी कुछ साथी-सँगाती जमा कर लिये। पास-पड़ोस ने भीड़ की तरह जमा होकर, शायद किसी संभावित तमाशे से वंचित रह जाने के लिये पछताते हुए, बीच-बचाव की यथोचित भूमिका निभाई। पड़ोसी उन्हें शान्त करने के जतन में अपने घर ले गये जिसका फल उन्हें भी थोड़ी बहुत उठा-पटक और तोड़ फोड़ के रूप में भुगतना पड़ा। जब अजित अंजुम के क्रोध का उबाल सारे किये धरे जतन के बावजूद संवरण को राजी न हुआ तो राजेन्द्र जी की बिटिया रचना यादव-खन्ना को उसी पास-पड़ोस के सौजन्य से सूचना दी गयी। वे गुड़गाँव से आईं। राजेन्द्र जी के घर मयूरविहार, दिल्ली तक आ उनके आ पहुँचने की घण्टा – सवा घण्टा भर की अवधि में यादवी जारी रही। अजित अंजुम से उनकी मुलाकात घर के बाहर ही हुई और पास-पड़ोस की बिचवई का सहारा लेते हुए उन्होंने किसी तरह मामले को रफा–दफ़ा करते हुए शान्ति की स्थापना और बात न बढ़ाने की याचना की। घर में घुसीं तो पाया कि राजेन्द्र जी आराम से खा-पीकर निश्चिन्त सो रहे हैं। उनसे यह प्रत्याशित भी है। रचना जी नाराज़ हुईं, बिगड़ीं और ‘परिघटना‘ के बारे में इधर उधर कोई बात न कहने करने की हिदायत उन्होंने यहाँ भी दी। उपरान्त-विचार में दोस्तों की बातचीत का एक यह विषय भी रहा कि कहाँ तो माँ बाप को बच्चों की करतूतों को ढाँपना, उनके लिये डाँटना बिगड़ना होता है, कहाँ यहाँ राजेन्द्र जी के करतब बिटिया को हलकान किये देते हैं। बिटिया की डाँट खाकर राजेन्द्र जी को शायद याद आया हो कि एक बार ‘मेरा हमदम मेरा दोस्त‘ या शायद ऐसी ही किसी और सिरीज़ में मन्नू जी की शिकायत-सूची के बारे मे उन्होंने लिखा था कि वे रचना को डाँटते क्यों नहीं और राजेन्द्र जी ने जवाब में कहा था कि बच्चों को डाँटने की एक दुकान खोल कर बैठ जाऊँ, कि यहाँ बच्चों को डाँटा जाता है, डँटाई के रेट दैनिक, हफ़्तावार: वगैरह के हिसाब से अलग अलग होते हैँ, तीन बच्चों के साथ एक माँ भी मुफ़्त डाँटी जाती है।
मित्रगण, हालाते हाजरा पर तफ़सरा स्टाइल में लिखित होने के बावजूद यह केवल स्टाइल ही है, हाल-हवाल की सारी सूचना दर-अस्ल सिर्फ़ सुनी- सुनाई है, वह भी सेकेण्ड, थर्ड और फ़ोर्थ हैण्ड। ‘मौके पर मौजूद’ जिस व्यक्ति के हवाले से यहाँ तक आई और आप तक पहुँचाई जा रही है, वह भी जाहिर और वाजिब कारणों से अनाम/गुमनाम बने रहना चाहता है। इसलिये किस्से में थोड़ी बहुत अतिरंजना होने की, मिर्च-मसाले में इजाफ़ा हुए होने की संभावना शत-प्रतिशत है। फिर इधर साहित्य उधर मीडिया। किस्से के किरदारों को देखते हुए यथार्थ के बयान में यथार्थ की अतिरंजना और सनसनी के अलावा यथार्थ में कल्पना के घालमेल की तो बनती है।
यहाँ ज़रा रुक कर परदे के पीछे की बिखरी पड़ी चीज़ों को एक करीना दे दिया जाय। यह बिखराव कालक्रम का भी है और तथ्यों के संयोजन का भी। किताब को आये हुए खासा अरसा हो चुका है। कम से कम आठ दस महीने। लगभग असाध्य बीमारी से लौटने के बाद की बिस्तरबन्द अवधि में आरोग्यलाभ के दौरान राजेन्द्र जी ने अपने अनर्गल-विचार-प्रवाह का इमला या श्रुत-लेख ज्योति कुमारी को लिखवाया।
अनर्गल-विचार-प्रवाह का मतलब यहाँ इस किताब का रूप-बन्ध भी है और सामग्री या विषय या अर्थ या वस्तु का स्वरूप भी। उस अवधि में जो भी लोग या घटनाएँ या चीज़ें या स्मृतियाँ उन्हें घेरती घुमड़ती रहीं, यहाँ उनको दर्ज किया गया है- कहीं केवल संक्षिप्त टिप्पणी भर में, तो कहीं किचित विस्तार के साथ। इन्हें लेखा-जोखा भी नहीं कहा जा सकता – न विगत ज़िन्दग़ी का, न किसी स्वयं-पर्याप्त अनुभव या अनुभव-खण्ड का।
लेखा-जोखा कहने में एक मूल्यांकन का सा बोध होता है। यहाँ सिर्फ़ ज़िन्दग़ी है। ज़िन्दग़ी में जो होता है, सो होता है। वह किसी मूल्यांकन का या अर्थसंगति का या तार्किक संयोजन का मोहताज नहीं होता। एक तरह से ज़िन्दग़ी का आदिम अनुभव, प्रथम प्रभाव, ‘जैसा देखा, भोगा, पाया’ का निपट निछद्दम का अंकन। इतना संक्षिप्त कि पाठक की तरफ़ से भी चीज़ों के जोड़-घटाव से कोई निष्कर्ष निकाल पाने या कोई आकार के उभार लेने की गुंजाइश नहीं। पाठक/आलोचक के लिये ऐसे परिप्रेक्ष्यविहीन दृश्य का कुल इस्तेमाल अधिक से अधिक राजेन्द्र यादव के संवेदन-कोष को समझने के लिये किया जा सकता है और निस्संदेह वे हमारे समय के महत्त्वपूर्ण लेखक हैं, अनेक शोध-निबन्धों और प्रबन्धों के लक्ष्य इसलिये वह भी अपने आप में एक सार्थक उद्देश्य माना जा सकता है, लेकिन इससे अधिक कुछ नहीं।
किताब में केन्द्रीय स्मृति पहले कभी किसी प्रेमिका के अन्तरंग सान्निध्य में बीते एकान्त की है, दीन-दुनिया, विमर्श, समाज, समता, संघर्ष, न्याय सबसे कटा हुआ निपट दैहिक एकान्त। केन्द्रीय कहने का कारण है इस स्मृति का अन्यों की अपेक्षा अधिक विस्तार। इस बार राजेन्द्र जी की बीमारी ज़रा संगीन किस्म की थी। कहने में शायद थोड़ा निर्मम लगे लेकिन मानो अन्त के आस-पास मँडराते आदमी का सिर्फ़ अपने अचेतन के अनर्गल प्रवाह को समर्पण, वह भी दीन-दुनिया की ओर से पूरी लापरवाही के साथ, दृश्य में बदल गया हो। उस वक्त बाकी सारा ताम-झाम झड़ जाता है, सिर्फ़ वही शेष रहता है जो मन की सबसे भीतरी तह में जड़ की तरह उगा और जमा रहता है। इस दृश्य में संवेदन की कोई खास गहराई, सम्बन्धों में से किसी के साथ भी कहीं कोई खास उलझाव दिखाई नहीं देता। शायद उम्र के इस मोड़ पर एक खास किस्म की दूरी या तटस्थता आ ही जाती हो। शायद जीवन के दिये हुए अनुभव ऐसे हों जिनका सामना सिर्फ़ निरावेग अनुपस्थिति के सहारे किया जा सकता हो। शायद स्वभाव या व्यक्तित्व ही भोगने वाले और देखने वाले व्यक्ति के दो स्तरों में बँटा हुआ हो जो कि लेखक के असली स्वभाव की मौलिक बनावट होती है और अपने मानसिक वितान के सिवाय कहीं लिप्त नहीं होने देती। इमला लिखवाने में अपने और अनुभव के बीच में किसी तीसरे की उपस्थिति ने शायद निजता के अहसास को खण्डित किये रखा हो अन्यथा लगता यही है कि जितने सब आस-पास हैं वे सभी उनके निकट हैं और निकट होने का अलग से कोई खास अर्थ या सम्बन्ध उनके लिये है नहीं।
अजित अंजुम और गीताश्री राजेन्द्र जी के प्रिय और निकट मित्रों में रहे हैं। अजित अंजुम ने ‘हंस’ के रिकॉर्डतोड़ मीडिया विशेषांक का अतिथि सम्पादन किया था। गीताश्री पिछले कई वर्षों से राजेन्द्र जी की वर्षगाँठ समारोह का आयोजन करती रही हैं जो दिल्ली के साहित्य-जगतमें मेल-मिलाप, मौज-मस्ती और खान-पान और अध्यात्म-विचार ( स्पिरिचुअलिज़्म – स्पिरिट के दूसरे अर्थ ‘सुरा‘ के साथ जोड़ कर) का एक मनभावन उत्सव हुआ करता है।
उल्लिखित किताब की अनेक टिप्पणियों में से कुछ गीताश्री, उनके लेखन, उनकी जीवन पद्धति के बारे में हैं। अजित अंजुम के विस्फोट की जाहिर वजह ये टिप्पणियाँ बताई गयी हैं।
गीताश्री हिन्दी की कुछ गिनी चुनी फ़ायर-ब्राण्ड स्त्रीवादी लेखिकाओं में से एक हैं और स्वयं अपने ब्राण्ड की विज्ञप्ति से हिचकती नहीं। एकाध गोष्ठी-सेमिनार में उनके इस ब्राण्ड का साक्षात्कार कर मैं भी मुग्ध हो चुकी हूँ। उनकी स्वच्छंदता, निर्भयता, भीतर की आग सब फ़ायर-ब्राण्ड के लक्षण हैं। इसलिये ऐसा लगता तो नहीं कि राजेन्द्र जी की टिप्पणियों को उनके लिये विशेष आपत्ति का विषय होना चाहिये। वे कोई नकारात्मक टिप्पणियाँ हैं भी नहीं। सिवाय उनके लेखन के विषय में इस एक टिप्पणी के कि वे अपने लेखन के शुरुआती दिनों में एकाध कहानी का किसी मित्र से पुनर्लेखन करवा चुकी हैँ। बेशक यह टिप्पणी राजेन्द्र जी के लिये अनुचित और अशोभनीय है लेकिन गीताश्री अपने कथासृजन को अनवरत रखकर इसका प्रत्याख्यान भी कर सकती हैं और स्वयं को प्रमाणित भी। गये ज़माने की बात है। रमेश बक्षी ने घोषणा की थी कि सुधा अरोड़ा की सारी कहानियाँ उन्होंने लिखीं हैं। सुधा का लेखन आज स्वयंप्रमाणित कर चुका है।
इसके आगे के ऊटपटांग अनुमान और निष्कर्ष शत-प्रतिशत मेरे हैं, इसलिये माने तो अप्रामाणिक, सन्दिग्ध और अवश्वसनीय भी हैं लेकिन इस आलेख की संगति में विचारार्थ पेश किये जा रहे हैं।
मेरे ख़याल से राजेन्द्र जी की जिस संगीन किस्म की बीमारी से उबर आने के बाद का नतीजा यह किताब है, उसी बीमारी से, उबर आने के पहले के भी कुछ नतीजे हैं।
ऐसा होता ही है। संगीन किस्म के रोग और संकट की गिरफ़्त में पड़े हुए निकट से भी निकट, प्रिय से भी प्रिय व्यक्ति के सिलसिले में उत्तराधिकार का प्रश्न रोग के संकट जितना ही संगीन बन जाता है। उसे निकटता पैमाना और प्रियता की परीक्षा की कसौटी बना लिया जाता है।
राजेन्द्र जी का उत्तराधिकार यानी ‘हंस‘ का भावी संपादन। उनकी विरासत की तरह ‘हंस‘ मौजूद था, एक संभावना और उसके साथ मौजूद था एक निर्मम सत्य कि राजेन्द्र जी के सही सलामत लौटने की उम्मीद नहीं थी। बिस्तरबन्द बेबस राजेन्द्र जी यहाँ घर में, फिर अस्पताल में कुछ योजनाएँ बना रहे थे जबकि वहाँ, हंस के दफ़्तर में उनके प्रिय और निकट जन भावी-संभावी उत्तराधिकारी कुछ और सपनों और हवाई किलों की उधेड़बुन में लगे थे। उत्तराधिकार के हस्तांतरण का समय मौजूद था।
शायद। ऐसा होता ही है। लेकिन जैसा कहा, यह जगत्गति और जीवन व्यवहार के आधार पर मेरे अपने ऊटपटांग निष्कर्ष और अनुमान हैं इसलिये इस बातचीत के सिलसिले में कोई नाम लेना मैं उचित नहीं समझती। ‘हंस‘ से अलग हुए मुझे चार बरस हो चुके और उसके साथ बाइस बरस जुड़े रहने के बावजूद आज वहाँ के भीतरी परिदृश्य से मैं पूरी तरह से अपरिचित हूँ। इतना भर तर्कसम्मत लगता है कि आज के ज़माने में निकटता और प्रियता अर्जित करने के प्रयास निरुद्देश्य नहीं होते। अर्जन के लिये अगर समय और श्रम खर्च किया गया हो तो मन में एक अधिकार और दावेदारी का भाव भी पैदा होता है। राजेन्द्र जी को धँस के रास्ता निकालने वाले इस किस्म के धाँसू लोग विशेष प्रिय भी होते हैं। उनके लिये वे मानवीय बुद्धि के सत्कारक और जिजीविषा की प्रतिमा होते हैं।
राजेन्द्र जी लौटे। भावी-संभावी का उनका निर्णय और हंस के प्रथम पृष्ठ पर घोषित संपादन सहयोगियों का नाम इन निकट और प्रियजन के लिये अप्रत्याशित था। यह देखते हुए तो और भी अधिक कि निकटता और प्रियता अर्जित करने के लिये इन लोगों ने ऐसा कुछ ठोस और व्यावहारिक किया भी नहीं था जिससे राजेन्द्र जी का यह निर्णय उन लोगों के निकट न्यायोचित ठहरता हो। निराशा तो हुई होगी।
निराशा का सबसे अधिक सहज कायाकल्प रोष और शत्रुता में होता है लेकिन ऐसे भी हालात हुआ करते हैं जब व्यावहारिकता के तकाजे से उसको टाले रखना ही उचित हुआ करता है। एक अजीब सी भीतरी खीचातानी की स्थिति होती है। कभी रोष और शत्रुता का उबाल काबू के बाहर होने लगता है, कभी उस पर ठण्डे छींटें डालने के लिये बर्फीला पानी ढोते ढोते बाल्टियाँ कम पड़ने लगती हैं। प्रेमचंद सहजवाला ने अंजना-विचारमंच की तरफ़ से आयोजित राजेन्द्र जी के सम्मान समारोह को सभागार में उपस्थिति प्रियजन और निकटजन की वक्ता-श्रोतामण्डली में से कुछ ने बाकायदा अपमान समारोह में बदल डाला जब वक्ताओं में से एक ने राजेन्द्र जी को बाकायदा वहाँ उपस्थित एक युवा-लेखक का वधिक घोषित किया और श्रोताओं में से दूसरी ने राजेन्द्र जी के पक्ष से कुछ कहने के इच्छुक एक दूसरे युवा को उसकी औकात और हैसियत बताने की ठान कर कहा कि उसने सभागार में कदम रखने की हिम्मत कैसे की। उन्होंने रमणिका गुप्ता की किताब के लोकार्पण समारोह में भी राजेन्द्र जी की मौजूदगी में उनको स्त्री का शत्रु घोषित करने वाला एक पर्चा भी पढ़ा। दो-तीन महीनों के अन्तराल में ये कार्यक्रम संपन्न होते चले जिनमें नवीनतम कड़ी की तरह अजित अंजुम के नवीनतम विस्फोट को गिना जा सकता है। लेकिन किताब की इन टिप्पणियों में अजित अंजुम के विस्फोट की तात्कालिक कुंजी खोजना तर्कसंगत नहीं लगता। किताब को आये हुए आठ दस महीने गुज़र चुके हैं। आपत्तिजनक उद्घाटनों को भी इतना अरसा गुज़र ही चुका है। किताब के आ चुकने के बाद वाली वर्षगाँठ का उत्सव भी गीताश्री ने पूरे समारोह के साथ मनाया था। यहाँ बात अलग रही कि अचानक बारिश ने मौसम को सुखद लेकिन वातावरण को असुविधाजनक कर दिया था। अधिक संगत बात यही लगती है कि शायद गुस्से की जाहिर वजह कुछ और है, असली वजह कुछ और। शायद यही कि रोष और शत्रुता के उबाल और व्यावहारिक औचित्य की जारी खींचातानी में कभी पहले की हार हो जाती है, कभी दूसरे की। और इतने दिन बीत चुकने के बाद भी एक दिन ऐसा बेबस आवेग कि विस्फोट बने, शायद ऐसी ही किसी मन:स्थिति का नतीजा हो। यानी परदे के पीछे कोई और अज्ञात और गोपन वजह मौजूद न हो तो।
राजेन्द्र जी के स्वभाव को थोड़ा बहुत जैसा भी मैने देखा है, उसके हिसाब से उनकी जगह अब भी वहीं मौजूद हैं, जहाँ वह पहले थी, यानी निकट मित्रों में। दिक्कत यह है कि निकटता की जो कसौटी मित्रों के मन में प्राय: हुआ करती है, उस पर राजेन्द्र जी की निकटता की भावना खरी नहीं उतरती। चीज़ों की नाप- जोख और मोल-भाव का राजेन्द्र जी का अपना तरीका है और उसकी वजह से अगर मैत्री व निकटता में कसर आए, जो कि आती ही है, तो वे प्राय: विस्मित पाए जाते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों। विस्मय में डूबते उतराते उन्हें शायद कभी सूझेगा भी नहीं यह उनकी अपनी करनी का नतीजा है। अपनी तरफ़ से तो उन्होंने बस उतना भर किया होगा जितना उनके हिसाब से बेलाग-लपेट, बिना किसी तरफ़दारी के, निर्मम-निष्पक्ष भाव से तर्कसम्मत और विवेकसंगत निर्णय का पोषक होगा। विवेकसंगति या तार्किक औचित्य का फैसला लक्ष्योन्मुख व्यवहार के अनुसार ही किया जा सकता है। फ़िलहाल राजेन्द्र जी के लिये हजार लक्ष्यों का एक लक्ष्य ‘हंस‘ है और राग हंस-कल्याण जीवन की एकमात्र धुन।
एक पलड़े पर अगर हंस के संपादन-सहयोग की लियाकत हो और दूसरे पर मैत्री और प्रियता का दावा और निकटता का अधिकार तो राजेन्द्र जी के हिसाब से लियाकत का फैसला दोस्ती के दावों से संचालित नहीं होना चाहिये (और वे लायक भी कोई दुश्मन तो नहीं), लेकिन उनके लिये दोस्ती के दावों को इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि फैसला उनके हक़ में नहीं।
लेकिन दोस्ती के दावेदार शायद ऐसा नहीं सोचते।
View 8 Comments