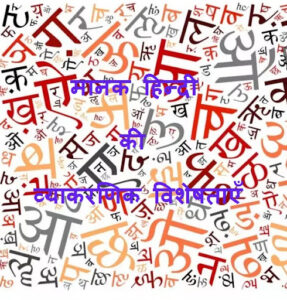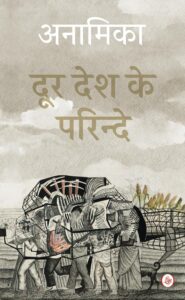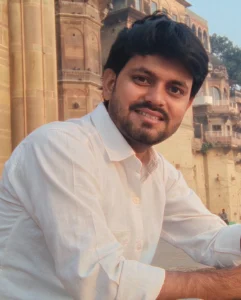मदन मोहन झा सर एक दिन घर के अन्दरवाले कमरे से एक पत्रिका निकाल कर लाए. देते हुए कहा था, इसे पढ़ना साहित्य के संस्कार आयेंगे. बात सन ८६ की है. उसी साल मैंने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी. उसी की कहानियों को पढते हुए मैंने कथाकार बनने के सपने देखे थे. देखते–देखते उस पत्रिका और मेरे सपने दोनों के २५ साल हो गए. उन दिनों सोचता था हंस के पन्नों पर मेरी भी कहानी छपेगी और तिरिछ या तिरियाचरित्तर की तरह मशहूर हो जायेगी या कार्लो हब्शी के संदूक की तरह या चिट्ठी की तरह. लेखक तो हंस में बिना छपे ही बन गया लेकिन शायद मशहूर नही हो पाया. हंस में छापना तब लेखक होने का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाने लगा था.
हंस का यह शायद सबसे बड़ा योगदान है कि जिस दौर में बड़े–बड़े प्रकाशन संस्थाओं से निकलने वाली धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान ढेर हो रही थी उस दौर में एक लेखक के व्यक्तिगत प्रयास से निकलने वाली इस पत्रिका ने साहित्य से लोगों को जोड़े रखने का काम किया. टेलीविजन के रंगीन तिलिस्म के सामने उसने मजबूती से साहित्य के जादू को बरकरार रखने का काम किया. जब पत्रिकाएं पढ़ने वाला परिवार टेलिविजन धारावाहिकों के जादू में खोने लगा था हंस ने साहित्य में लोगों का विश्वास बनाये रखने का काम किया. सबसे बड़ी बात है कि मनोरंजन प्रधान उस दौर में भी उसने साहित्यिक सरोकारों की लौ को बनाये रखा. पत्रिकाओं के नाम पर हिंदी में सन्नाटा छाता जा रहा था, बस एक हंस थी. न जाने कितने कथाकार हैं जिन्होंने हंस के पन्नों से गांव–समाजों तक अपनी व्याप्ति बनाई. हमारी पीढ़ी ने जिन कथाकारों कि ओर सर ऊँचा करके देखा और लिखने की प्रेरणा पाई संयोग से उन सबको हंस ने ही इतना ऊंचा बनाया.
केवल कहानियां या कविताएँ ही नहीं ९० के दशक में बिना किसी तरह की सनसनी या उत्तेजना फैलाये हंस ने हिंदी में नए विमर्शों की ज़मीन तैयार की. उत्तर–आधुनिकता की बहसों ने हिंदी के नए–नए आलोचक पैदा किये. उसी दौर में हंस ने स्त्री और दलित विमर्श की ज़मीन तैयार की और देखते ही देखते हिन्दी में एक नया वर्ग तैयार हुआ जिसने हिन्दी को ब्राह्मणवादी जकडबंदी से मुक्त करवाने का काम किया. हंस बाद में हिन्दी में दलितों और शोषितों की आवाज़ बन गया. हंस ने बने–बनाए सत्ता प्रतिष्ठानों का मुखौटा उतारना सिखाया. साहित्य का एक नया वर्ग तैयार किया. इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लगभग साहित्य विमुख होते जाते समाज में हंस ने पाठकों का एक नया तबका तैयार किया. ऐसा तबका जो हर बने–बनाए ढांचे को संदेह की नज़र से देखता था, सर्वस्वीकृत मान लिए गए पहलुओं को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता था. उस प्रश्नवाचक नज़र से जिससे विमर्शों की नई राह निकलती है.
सबसे बड़ी बात है कि बिना प्रेम या बेवफाई के विशेषांक निकाले, बिना किसी तरह की सनसनी फैलाये इस पत्रिका ने यह काम किया. साहित्य की गरिमा को बनाये रखने का काम किया. हंस को कभी अपनी व्याप्ति का ढिंढोरा नहीं पीटना पडा. हिंदी में सब जानते हैं कि उसकी व्याप्ति आज भी सबसे अधिक है. यह अलग बात है कि आज नए आन्दोलनों, नए विमर्शों की ज़मीन हंस के पन्नों से नही तैयार हो रही है, नयी रचनाशीलता का सर्वश्रेष्ठ हंस के पन्नों पर नही दिखाई दे रहा है. उसके पाठकों को लगने लगा है कि हंस कि दृष्टि लगातार संकुचित होती जा रही है. लेकिन फिर भी २५ साल के बाद भी हंस हमारे समाज में साहित्य का मानक बना हुआ है. आज भी लोग इस उम्मीद में हर महीने हंस खरीदते हैं और उसके पन्नों को इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि शायद इस बार कुछ नया दिख जाए, कुछ ऐसा जिसने हंस को हंस बनाया. यह कम बड़ी बात नहीं है. २५ सालों तक व्यक्तिगत प्रयास से निकलने वाली एक पत्रिका हिंदी में साहित्य–विमर्श का मानक बना रहे कोई हंसी–ठट्ठा नहीं है.
इन २५ वर्षों में मैं कहानीकार हो गया. कहानियों की एक किताब छाप गई. पिछले साल जब अपने शहर सीतामढ़ी गया तो अपने सर मदन मोहन झा से मिलने गया. उस सर से जिन्होंने साहित्यकार बनने का सपना आँखों में पैदा किया था. सर बूढ़े हो गए हैं. लेकिन हर महीने हंस खरीदना और पढ़ने की उनकी आदत वैसी ही है. उनको मैंने अपनी कहानियों की किताब दी. उन्होंने उलट–पुलटकर देखा. कहा, अच्छा भारतीय ज्ञानपीठ ने छपी है. अच्छी होगी. पढूंगा. फिर बातों–बातों में कहा, हंस में तुम्हारी कोई कहानी नहीं देखी. मैं उनका आशय समझ गया. उनके लिए आज भी हंस में छपना लेखक होने का प्रमाण है. जो हंस में नहीं छपा ज़रूर उसके लेखन में कुछ न कुछ कमी होगी. उनके जैसे ना जाने कितने होंगे दूर–दराज के गांव–देहातों तक में जो आज भी हंस के अलावा किसी हिंदी पत्रिका के बारे में ठीक से नहीं जानते. जानते भी हैं तो उनके ऊपर वैसा भरोसा नहीं करते जैसा हंस पर करते हैं.
हंस महज एक पत्रिका नहीं है, तमाम चीज़ों के बावजूद साहित्यिकता की परंपरा है. उस परंपरा के २५ साल हो गए.
हंस का यह शायद सबसे बड़ा योगदान है कि जिस दौर में बड़े–बड़े प्रकाशन संस्थाओं से निकलने वाली धर्मयुग, साप्ताहिक हिन्दुस्तान ढेर हो रही थी उस दौर में एक लेखक के व्यक्तिगत प्रयास से निकलने वाली इस पत्रिका ने साहित्य से लोगों को जोड़े रखने का काम किया. टेलीविजन के रंगीन तिलिस्म के सामने उसने मजबूती से साहित्य के जादू को बरकरार रखने का काम किया. जब पत्रिकाएं पढ़ने वाला परिवार टेलिविजन धारावाहिकों के जादू में खोने लगा था हंस ने साहित्य में लोगों का विश्वास बनाये रखने का काम किया. सबसे बड़ी बात है कि मनोरंजन प्रधान उस दौर में भी उसने साहित्यिक सरोकारों की लौ को बनाये रखा. पत्रिकाओं के नाम पर हिंदी में सन्नाटा छाता जा रहा था, बस एक हंस थी. न जाने कितने कथाकार हैं जिन्होंने हंस के पन्नों से गांव–समाजों तक अपनी व्याप्ति बनाई. हमारी पीढ़ी ने जिन कथाकारों कि ओर सर ऊँचा करके देखा और लिखने की प्रेरणा पाई संयोग से उन सबको हंस ने ही इतना ऊंचा बनाया.
केवल कहानियां या कविताएँ ही नहीं ९० के दशक में बिना किसी तरह की सनसनी या उत्तेजना फैलाये हंस ने हिंदी में नए विमर्शों की ज़मीन तैयार की. उत्तर–आधुनिकता की बहसों ने हिंदी के नए–नए आलोचक पैदा किये. उसी दौर में हंस ने स्त्री और दलित विमर्श की ज़मीन तैयार की और देखते ही देखते हिन्दी में एक नया वर्ग तैयार हुआ जिसने हिन्दी को ब्राह्मणवादी जकडबंदी से मुक्त करवाने का काम किया. हंस बाद में हिन्दी में दलितों और शोषितों की आवाज़ बन गया. हंस ने बने–बनाए सत्ता प्रतिष्ठानों का मुखौटा उतारना सिखाया. साहित्य का एक नया वर्ग तैयार किया. इस बात को समझने की ज़रूरत है कि लगभग साहित्य विमुख होते जाते समाज में हंस ने पाठकों का एक नया तबका तैयार किया. ऐसा तबका जो हर बने–बनाए ढांचे को संदेह की नज़र से देखता था, सर्वस्वीकृत मान लिए गए पहलुओं को प्रश्नवाचक दृष्टि से देखता था. उस प्रश्नवाचक नज़र से जिससे विमर्शों की नई राह निकलती है.
सबसे बड़ी बात है कि बिना प्रेम या बेवफाई के विशेषांक निकाले, बिना किसी तरह की सनसनी फैलाये इस पत्रिका ने यह काम किया. साहित्य की गरिमा को बनाये रखने का काम किया. हंस को कभी अपनी व्याप्ति का ढिंढोरा नहीं पीटना पडा. हिंदी में सब जानते हैं कि उसकी व्याप्ति आज भी सबसे अधिक है. यह अलग बात है कि आज नए आन्दोलनों, नए विमर्शों की ज़मीन हंस के पन्नों से नही तैयार हो रही है, नयी रचनाशीलता का सर्वश्रेष्ठ हंस के पन्नों पर नही दिखाई दे रहा है. उसके पाठकों को लगने लगा है कि हंस कि दृष्टि लगातार संकुचित होती जा रही है. लेकिन फिर भी २५ साल के बाद भी हंस हमारे समाज में साहित्य का मानक बना हुआ है. आज भी लोग इस उम्मीद में हर महीने हंस खरीदते हैं और उसके पन्नों को इस उम्मीद के साथ खोलते हैं कि शायद इस बार कुछ नया दिख जाए, कुछ ऐसा जिसने हंस को हंस बनाया. यह कम बड़ी बात नहीं है. २५ सालों तक व्यक्तिगत प्रयास से निकलने वाली एक पत्रिका हिंदी में साहित्य–विमर्श का मानक बना रहे कोई हंसी–ठट्ठा नहीं है.
इन २५ वर्षों में मैं कहानीकार हो गया. कहानियों की एक किताब छाप गई. पिछले साल जब अपने शहर सीतामढ़ी गया तो अपने सर मदन मोहन झा से मिलने गया. उस सर से जिन्होंने साहित्यकार बनने का सपना आँखों में पैदा किया था. सर बूढ़े हो गए हैं. लेकिन हर महीने हंस खरीदना और पढ़ने की उनकी आदत वैसी ही है. उनको मैंने अपनी कहानियों की किताब दी. उन्होंने उलट–पुलटकर देखा. कहा, अच्छा भारतीय ज्ञानपीठ ने छपी है. अच्छी होगी. पढूंगा. फिर बातों–बातों में कहा, हंस में तुम्हारी कोई कहानी नहीं देखी. मैं उनका आशय समझ गया. उनके लिए आज भी हंस में छपना लेखक होने का प्रमाण है. जो हंस में नहीं छपा ज़रूर उसके लेखन में कुछ न कुछ कमी होगी. उनके जैसे ना जाने कितने होंगे दूर–दराज के गांव–देहातों तक में जो आज भी हंस के अलावा किसी हिंदी पत्रिका के बारे में ठीक से नहीं जानते. जानते भी हैं तो उनके ऊपर वैसा भरोसा नहीं करते जैसा हंस पर करते हैं.
हंस महज एक पत्रिका नहीं है, तमाम चीज़ों के बावजूद साहित्यिकता की परंपरा है. उस परंपरा के २५ साल हो गए.