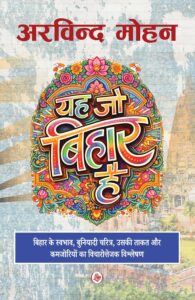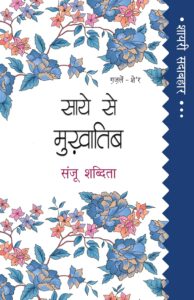पढ़ने में जरा देर हुई. कुछ तो इच्छा भी नहीं हो रही थी. लेकिन मित्रों के फोन से, फेसबुक से यह पता चल रहा था कि एक अति-वरिष्ठ लेखक ने एक वरिष्ठ लेखक(मैं उनकी तरह महुआ मांझी जी को युवा लेखिका नहीं लिख सकता) के बारे में कुछ ऐसा लिख मारा है कि उसने उसके अति-प्रसिद्ध उपन्यास का कुछ लेखन-संशोधन नुमा किया था, जिसकी कहानी दरअसल उसकी अपनी लिखी हुई ही नहीं थी. उन्होंने हवाला अपनी डायरी का दिया है, प्रामाणिक सबूत के तौर पर.
लेकिन इसमें नया क्या है यही सोचता रहा, पुराने प्लॉट में लिखी एक नई कहानी भर है. इस पूरे प्रसंग में कौन सही है कौन गलत है इस इसके ऊपर अपना कोई मत नहीं देते हुए मैं एक दूसरा सवाल पूछना चाहता हूं- मौलिकता की बात हिंदी में लेखिका के सन्दर्भ में ही क्यों उठाई जाती है? लेखिकाओं के पीछे एक पुरुष प्रेत खड़ा किए जाने की हिंदी में सुदीर्घ परंपरा रही है. सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता ‘झाँसी की रानी’ के असली रचयिता एक गुमनाम कवि को बताया जाता रहा. यह आजादी के पहले की बात है. हाल की बात करूँ तो नब्बे के दशक में जिन दो लेखिकाओं को साहित्य अकादेमी पुरस्कार मिले, उनके बारे में क्या कुछ लिखा गया इसको मैं यहां दोहराना नहीं चाहता. दोनों के पीछे पुरुष-प्रेत खड़े कर दिए गए. जबकि दोनों लेखिकाओं का एक बड़ा पाठक वर्ग है, दोनों ने निरंतर अच्छा लिखा है, लेकिन किस्से हैं कि चले जा रहे हैं. महुआ माझी के बारे में भी इस तरह के किस्से बहुत दिनों से सुने जा रहे थे, लिखा किसी ने पहली बार है. इसी तरह की कहानियां रस ले-ले कर झारखण्ड की एक कवयित्री के बारे में भी सुनाये जाते रहे हैं. बचपन से कहावत यह सुनी थी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री होती है, लेकिन हिंदी साहित्य में यह देखा है कि हर सफल लेखिका के पीछे एक पुरुष बिठा दिया जाता है. गोया महिलाओं को लिखना न आता हो, पुरुष न हों तो लेखिकाओं के लिए लिखना मुश्किल हो जाए.
मेरा सवाल यह है कि इस तरह के सवाल लेखकों के सन्दर्भ में क्यों नहीं उठाये जाते हैं? क्या पुरुषों की रचनाएँ कोई ठीक नहीं करता होगा, कोई उनका संपादन नहीं करता होगा. यह कोई नहीं लिखता कि कैसे देखते-देखते एक डॉक्टर को हिंदी के समकालीन प्रमुख लेखक साबित करने में एक ‘फैक्ट्री’ के लोग लगे हैं, जबकि उसकी सबसे बड़ी शिफत यह है कि वह एक बुजुर्ग लेखक का इलाज बढ़िया कर रहा है. लेकिन नहीं, पुरुषों के सन्दर्भ में इस तरह के सवाल उठाने से न तो सनसनी फैलेगी, न पढ़नेवाले चटखारे लेंगे, न सरगोशियाँ होंगी. यह दुर्भाग्य है कि हिंदी में अच्छी-अच्छी लेखिकाओं को भी आइटम नंबर की तरह देखा जाता है, उनका कोई सम्मान नहीं है. श्रवण कुमार गोस्वामी ने भी अपने लेख में संदर्भित लेखिका के ‘रूपसी’ होने की बात कही है. इस तरह के प्रसंग बताते हैं कि तमाम स्त्री विमर्श के बावजूद स्त्रियों के प्रति न नजरिया बदला न ही हिंदी में पुरुष वर्चस्व टूटा.
असल में, मुझे यह लगता है कि इसके मूल में कारण यह है कि हिंदी में संपादक नाम की संस्था का महत्व धीरे-धीरे कम होता गया है. अंग्रेजी में बड़े-बड़े लेखक भी संपादक के मुरीद होते हैं, जो उनकी रचनाओं को सन्दर्भों से जोड़कर एक ‘पर्सपेक्टिव’ दे देता है और साधारण रचनाओं को भी असाधारण बना देता है. हिंदी मौलिकता की इस कदर मारी हुई है कि कोई लेखक अपनी भाषा तक को दुरुस्त नहीं करने देता. जो संपादक को महत्व देता है उसके बारे में यह मान लिया जाता है कि जिसने संपादन किया है असली लेखक तो वही है. लिखने वाली अगर स्त्री है तो इस बात को कुछ और हवा मिल जाती है. दुर्भाग्य से तत्कालीन प्रसंग भी मुझे कुछ ऐसा ही लगता है.