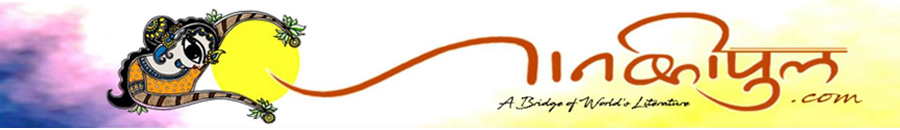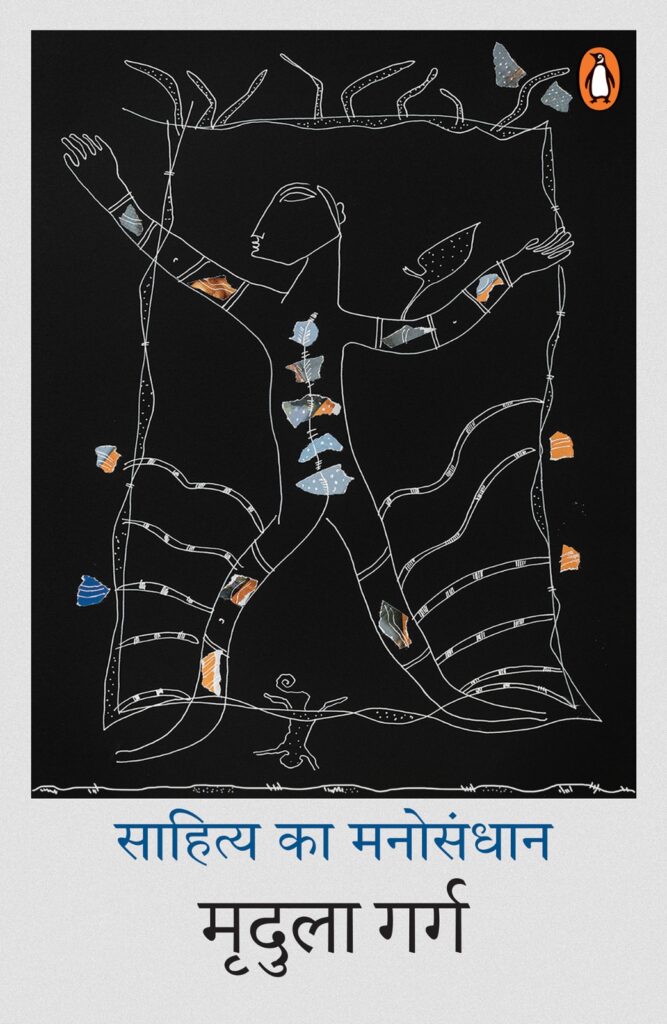प्रसिद्ध लेखिका मृदुला गर्ग के निबंधों का संग्रह हाल में ही पेंगुइन स्वदेश से प्रकाशित हुआ है- साहित्य का मनोसंधान। इस पुस्तक के शीर्षक निबंध का एक अंश पढ़िए, जो मनोविज्ञान और साहित्य को लेकर है- मॉडरेटर
=====================================
हर रचनात्मक लेखक कुछ हद तक मनोविश्लेषक का काम करता है; कम–से–कम उसका संबंध मनोवैज्ञानिक पड़ताल से होता है; भले व्यावहारिक रूप से प्रेक्टिस करने वाले मनोविश्लेषक, उसकी चेष्टाओं को अनाड़ी का दखल मानें। यानी जितना अपने पात्रों के आचार–व्यवहार को गढ़ने के लिए, साहित्यकार, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से उधार लेता है, उतना ही मनोविज्ञान, अपने सिद्धांत गढ़ने के लिए साहित्य से उधार लेते हैं। बल्कि साहित्यकार, विश्लेषण से कुछ आगे जाकर मनोसंधान करता है।
जो ऊपरी सतह पर स्पष्ट दिख रहा हो, उससे असंतुष्ट होने पर ही, वैकल्पिक संसार की रचना करने के ख़याल से कोई कलम उठाता है। दिखते यथार्थ के भीतर, जो परत–दर–परत द्वंद्वात्मक विडंबनाओं से लैस एक अन्य यथार्थ है, उसका अनुशीलन करना ही रचनाकर्म का सत्व है। यह अनुशीलन, व्यक्ति से भी ताल्लुक रखता है और सामान्य व असामान्य कहलाए जाने वाले व्यक्तियों से बने उस समूह से भी, जिसे हम समाज, सांस्कृतिक इकाई या राष्ट्र के नाम से जानते हैं।
एक मनोवैज्ञानिक की सबसे जटिल समस्या यह तय करना है कि मानव स्वभाव में क्या सामान्य है और क्या असामान्य । इतिहासजनित भ्रम या अहंकार के कारण सामाजिक व सांस्कृतिक रूढ़ि या व्यवस्था जिसे असामान्य घोषित करती है, दरअसल वह असाधारण वैचारिक सोच और अनुसंधान हो सकता हैं। मनोवैज्ञानिक शोध का एक काम, असाधारण और असामान्य के बीच के महीन अंतर को स्पष्ट करके मानव स्वभाव की जटिल संरचना को उद्घाटित करना रहा है। ठीक यही काम साहित्यकार भी करता है। कह सकते हैं, साहित्य का मूल स्वत्व, समाज व व्यवस्था के भ्रमों का निराकरण कर उसे चेताना है।
इसके विपरीत यह भी उतना ही सच है कि हर तथाकथित सामान्य व्यक्ति में कुछ–न–कुछ असामान्य तत्व विद्यमान रहते हैं। आप फ़्रायड के नियमों को मानें या नहीं, उसका यह महत्त्वपूर्ण योगदान स्वीकार करना होगा कि कोई व्यक्ति पूरी तरह से सामान्य नहीं होता। बल्कि कहें तो सामान्य शब्द ही व्यक्ति के संदर्भ में बेमानी है। एक तरफ़, हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है, इसलिए दोनों में से किसी एक को सामान्य नहीं माना जा सकता। दूसरी तरफ़, कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो धर्म, नस्ल, रंग, जाति, लिंग से परे हर व्यक्ति में यकसाँ होते हैं, जिन्हें शाश्वत मानवीय तत्व माना जा सकता है। इन्हीं शाश्वत तत्वों का अनुशीलन करके, रचना में उनका चित्रण व विश्लेषण, कालजयी और स्थानीयता को लाँघने वाले साहित्य का लक्षण है।
उदाहरण के लिए एक शाश्वत नैसर्गिक स्थापना यह है कि, सोच–विचारकर वैकल्पिक कर्म के बीच चुन पाने की शक्ति, केवल है मानव के पास है, पशु के पास नहीं। इसलिए वह अपने कर्म के लिए उत्तरदायी है। साथ ही सहज बोध या अंतःप्रज्ञा भी उसके व्यवहार को संचालित करते हैं। यानी वह वैचारिक चुनाव और सहज प्रतिक्रिया के बीच की द्वंद्वात्मक स्थिति में विचरता रहता है। दुविधा व द्वंद्व, उसके अस्तित्व या अस्मिता का स्थायी भाव है और उसका प्रयोजन, उनसे मुक्त होकर कर्म करना है। यह तत्व जितना साहित्य का विषय है, उतना ही मनोविज्ञान का।
स्वभाव या संस्कार? विरासत या पालन पोषण? मानव चरित्र को क्या अधिक प्रभावित करता है, यह प्रश्न मनोविज्ञान को हमेशा से चुनौती देते आए हैं। यही प्रश्न, साहित्यिक रचना में ख़ुद–ब–खुद प्रवेश पा लेते हैं। देखा जाए तो मनोविज्ञान की कई मान्य प्रवृत्तियाँ, पहले साहित्यिक रचना में मानवीय नियति के विद्रूप के रूप में अभिव्यक्त हुईं, बाद में उन्हें मनोविज्ञान में मान्यता मिली। फ़्रायड के मनोविज्ञान दर्शन के दो आधार स्तंभ, इलेक्ट्रा और इडीपस कांप्लेक्स, ग्रीक नाटकों में व्याख्यायित पात्रों के जीवन में घटित असामान्य घटनाओं से उपजी विडंबनाओं से उधार लिए गए थे ।
मैं, विश्व साहित्य के, जिसमें हिंदी साहित्य भी आता है, कुछ महत्त्वपूर्ण उपन्यासों के माध्यम से इन आधारभूत सिद्धांतों को स्पष्ट करना चाहती हूँ।
पहला है कामू का स्ट्रेंजर (अजनबी), जो उदासीनता के प्रतीक व्यक्ति के रूप में, मियरसौं की मनःस्थिति का अभूतपूर्व विश्लेषण करता है। अंत में न्यायाधीश के पूछने पर कि उसने एक अनजान व्यक्ति की हत्या क्यों की, उसका उत्तर, ‘सूरज के तेज़ ताप के कारण‘ भीतर तक हिला देने वाला सत्य वाचन है। कोई उसे गंभीरता से नहीं लेता। अदालत में बैठे तमाम दर्शक हँस पड़ते हैं। न्यायाधीश ही नहीं, उसका अपना वकील भी उसे एक अहमक़ाना जवाब मानता है। जो सच है, उसमें किसी की दिलचस्पी नहीं हैं, उसके अंतःकरण में झाँक कर देखने की न किसी को फ़ुर्सत है न रुचि। हत्या से ज़रा पहले वह कहता है, हर बार जब तेज़ रोशनी की धार; रेत के कणों, टूटे शीशे और विरंजित शंखों से टकरा कर चौंध फेंकती, मेरे जबड़े भिंच जाते। मैं शिद्दत से जो महसूस कर रहा था, वह माथे पर धमकते सूरज के ताप के मजीरे और दूर कहीं चाकू से निकलता प्रकाश का त्रिशूल था। उसका धधकता फल मेरी पलकों को बींध रहा था, जलती आँखों को भेद रहा था। तभी सबकुछ चक्राकार घूमने लगा। मेरा सर्वांग तन गया और हाथ बंदूक पर कस गया… अदालत में उसे यह सब कहने–सुनने का मौका नहीं दिया जाता। वहाँ बहस वकीलों के बीच होती है, उसकी हिस्सेदारी नगण्य है।
जब–जब मैंने यह उपन्यास पढ़ा, मियरसौं का बार–बार यह कहना कि फलां–फलाँ चीज़ उसकी नसों पर भारी पड़ रही थी, अत्यंत महत्त्वपूर्ण लगा । ‘सूरज का ताप, चमड़े और शवगाड़ी में जुते घोड़ों की लीद की मिलीजुली बू, लोबान और पॉलिश की गंध और बिनसोई कटी रात की थकान मुझे न ढंग से सोचने दे रही थी, न देखने।‘ माँ के अंतिम संस्कार के वक़्त कही गईं इन पंक्तियों से लेकर अपने मुक़दमे की अंतिम सुनवाई तक, वह बार–बार अनेक बाह्य स्थितियों के बारे में ऐसे वाक्य दोहराता है। शोर, धूप, तेज़ रोशनी, मौन, दिखावा। सबसे ज़्यादा, दिखावा! इस हद तक कि अपने और अभियोगी वकीलों के बयान सुनने में भी उसकी दिलचस्पी नहीं रह पाती।
अंततः उसे हत्या के लिए मौत की सज़ा मिलती है तो उसका मुख्य कारण यह रहता है कि, उसने अपनी माँ की मृत्यु पर अतिरिक्त दुख का दिखावा नहीं किया था। जिसकी वजह से उसे संवेदनहीन और निर्मम माना गया। चूँकि उसने स्वीकृत व्यवहार के खिलाफ़ सहज व्यवहार किया था, जैसे कॉफ़ी या सिगरेट पीना; माँ की आयु न जानने पर मनगढ़ंत उम्र न बतलाकर साफ़ कह देना कि उसे नहीं पता; मृत माँ का चेहरा न देखना, अगला दिन एक लड़की के साथ बिताना, मज़ाहिया फ़िल्म देखना, वगैरह। ग़लत यह नहीं माना गया कि वह माँ से प्यार नहीं करता था, जो वह करता था (बार बार माँ की कही बातें याद आना उसका परिचायक था) या उसकी मृत्यु से उसे गहरा आघात नहीं लगा था। बल्कि यह कि उसने रो–धो कर जतलाया नहीं था कि वह प्यार करता था और उसकी मृत्यु से उसे आघात लगा था। यानी समाज सज़ा देता है, दिखावा न करने की, स्वीकृत व सामान्य व्यवहार से फ़र्क़ व्यवहार करने की।
सवाल उठता है कि यह कौन तय करेगा कि सामान्य क्या है? सरकार? समाज? क़ानून? मनोविश्लेषक? या हमें मानना होगा कि असामान्य और सामान्य को अलग करने वाला फ़ासला, बहुत धूमिल और लचीला है। यह सवाल साहित्य को जितना आड़े लेता है उतना ही मनोविज्ञान के सिद्धांतों को।