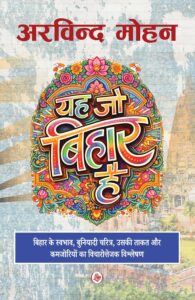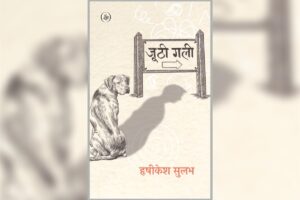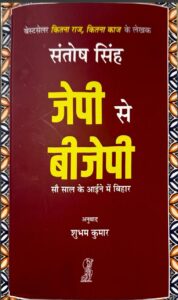हाल में वेस्टलैंड बुक्स से प्रसिद्ध अभिनेता अमोल पालेकर की संस्मरण-पुस्तक आई है- अमानत- एक स्मृतिकोष। मनोहर श्याम जोशी भारतीय मध्यवर्ग के दुचित्तेपन की बात करते थे यानी ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। ऐसे मध्यवर्गीय किरदारों को पर्दे पर अमोल पालेकर ने बखूबी निभाया है। उन्होंने निर्देशन भी किया, पेंटिंग भी की। कहने का मतलब यह है कि वे संपूर्ण कलाकार रहे हैं। आइये पढ़ते हैं उनके संस्मरण-पुस्तक की भूमिका- मॉडरेटर
=======================
सिगरेट के बिखरे
ठूंठों के बीच….
अपनी ज़िंदगी को समेटकर उस पर लिखना एक बेहद थकाऊ और अनचाहा प्रयास लगता है। ऐसा लगता जैसे मेरे हाथ में एक बड़ा सा थैला है जिसका आकार लगातार बड़ा होता जा रहा है और वह खमीर उठे आटे की तरह आकारहीन होकर फैल रहा है। ऊपर से भरी जा रही अनगिनत घटनाएं, लोग, भावनाओं का उफ़ान, विचारों–कल्पनाओं की निरंतर धारा, जाने–पहचाने और अनजान चेहरे, अच्छे–बुरे स्वाद, साफ़ और धुंधले दृश्य, दुख–वेदना, तरह–तरह की गंध और न जाने कितना कुछ और, जिसे भरने का कोई अंत ही नहीं है। इन सबकी अनगिनत बारीकियों को ठूँसना भी अपरिहार्य है, जैसे मेरे कंधे पर बैठे मेरे बिल्ले ‘रानटु’ का ‘लपलप‘ आवाज़ करते हुए मेरे कान के निचले हिस्से को चाटना, बेशुमार पानी पूरी खाने के बावजूद अगली पानी पूरी के स्वाद के बारे में मन में उभरने वाली उत्सुकता, नाटक का पर्दा उठते समय होने वाली ‘घर्रर्रर्र‘ की आवाज़ से हर बार मन में उठने वाली घबराहट, हर सुबह आईने में नज़र आने वाला मोदिग्लियानी (Amedeo Modigliani) की शैली में पिघलता हुआ ख़ुद का चेहरा… कितना और क्या–क्या भरूँ ?
और इन छोटे–छोटे, फ़िज़ूल विवरणों का क्या करूँ? पहली बार ताड़देव कचिन्स में सिलवाई शर्ट का शरीर से हुआ स्पर्श, दौड़ते–दौड़ते थक चुके मेरे पालतू कुत्ते, जूनियर के मुँह से लटकती लार को हाथ से पोंछते समय मन में उमड़ी ममता, टाटा द्वारा ख़रीदे गए मेरे पहले कैनवास को पैक करते समय महसूस हुई अंदरूनी कसक… ये कैसे महत्वपूर्ण नहीं हैं? यह सब वास्तव में फ़िज़ूल नहीं हैं, पर किताब की भौतिक सीमाओं में इन बिखरी बातों के लिए जगह शायद नहीं होगी। इतनी सारी जी हुई, भोगी हुई, महसूस की गई, संजोई गई, गढ़ी गई चीजें – मैं कैसे तय करूँ कि क्या चाहिए और क्या नहीं? क्या ये उन असंख्य जिए गए क्षणों के साथ नाइंसाफ़ी होगी जो यहाँ जगह नहीं बना पाए?
क्या इस प्रयास को यहीं छोड़ दूँ? जीवन जीते वक़्त भी ये उलझनें नहीं हुईं, तो अब क्यों सामना करूँ? जीना आसान था एक तरह से– शून्य गुरुत्वाकर्षण में पाँव आगे बढ़ाते हुए, फिर तैरते, गोते खाते, ख़ुद–ब–खुद दूर किनारों तक पहुँच गए; कभी हल्के से, तो कभी धड़ाम। पर तब भी कहाँ सब कुछ सहज और सरल लग रहा था? पहली पंक्ति में बैठने वाला हो या आख़री कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स, उसके लिए शो शुरू होने से पहले पर्दे के पीछे के अंधकार में हो रही हलचल देख पाने की ख़्वाहिश ही तो काफ़्काएस्क दुविधा (Kafkaesque conundrum) के समान है। मेरे हर निर्णय के साथ नई उलझनें आती थीं या फिर कभी बेपरवाही के कारण बिल्कुल भी नहीं आती थीं। नक़द साइनिंग अमाउंट बैग में भरकर लाए निर्माता को मना करते हुए कभी रोटी मिलने की चिंता नहीं की, न ही कभी ख़ुद के अभिनय से मोहित होकर एक ही तरह के रोल स्वीकार करता चला गया। प्रायोगिक नाटकों से हिन्दी फ़िल्मों की ओर जाते समय, दुबे (सत्यदेव दुबे) का साथ छूटने की संभावना की कभी परवाह नहीं की। मुझे शाल्मली के शब्द सुनाई देते हैं, ‘बाबा, क्या हालत बना रखी है तुमने ख़ुद की? छोड़ दो वो सिगरेट!’ उसकी आवाज़ में छिपी उस गहरी चिंता की चुभन को मैं कैसे व्यक्त करूँ? इन सारी छटाओं का क्या करूँ? इन सब भावनाओं में गुथे हुए अपने आपको बाहर निकालकर सामने रख देना और दूसरों के सामने परोस देना— बहुत ही कष्टदायक है।
शायद उन भूली–बिसरी या जान–बूझकर दफ़नाई गई घटनाओं को भी इस थैले में खींचा जा सकता है। मेरे भीतर गूँजती हुई आहों, सिसकियों और विलाप की प्रतिध्वनियाँ, बगोटा में खाए गए रानी मक्खी के कुरकुरे पेटों का मिट्टी जैसा स्वाद, शोर–शराबे वाली पार्टियों में थोपे गए बेकार कॉकटेल्स, सत्तर के ऑक्सीजन–स्तर पर थमी हुई सांस, चिरेबंदी से उठाया गया आख़री क़दम, नक्षत्रांचे देणे की मंच पर प्रस्तुति के दौरान भूली गई पंक्तियों के कारण दिल में उठी घबराहट, चार दिन की शूटिंग के बाद ठंडे बस्ते में डाल दी गई अश्वमेधेर घोड़ा, या पूरी तरह तैयार होकर भी प्रदर्शित न हुई पेपर बोट्स, निर्वाण, कल और अंकुश जैसी कई फ़िल्मों से भावनात्मक लगाव, चौदह साल तक संभालकर रखी कैरी की जर्जर फ़ाइल का जर्जर स्पर्श, जन्मांध व्यक्तियों की संवेदनाएं समझने के लिए आँखें कसकर बाँधकर की गई दिवाकर जी द्वारा लिखे गए आंधळे की रिहर्सल, संध्या के अस्पष्ट शब्द ‘हैंग इन देयर‘…
आख़िर क्यों अपने भीतर के इस तूफ़ान को शांत वर्तमान में खलबली मचाने दी जाए?
इतना सब कुछ थैले में हँसकर भरने के बाद भी, बिखरा हुआ अतीत चारों ओर फैला हुआ ही रह जाता है! इसे कैसे समेटा जाए? यह चालीस सालों में हर दिन फूँकी गई बहत्तर सिगरेटों के ठूंठों और लगातार उड़ाए गए धुएं को इकट्ठा करने जैसा प्रयास है। कहाँ–कहाँ फेंके होंगे वो सिगरेट के ठूंठे–आइफ़िल टॉवर के नीचे, प्राग की किसी पत्थरों वाली छोटी गली में, सिडनी के तास्मान सागर में, डेनमार्क की क्रूज़बोट के गंदे शौचालय में। और किस दिशा में ढूँढूँ वो धुआँ ? कितनों की छाती में घुस चुका होगा; कैसे ढूँढ़ सकता हूँ मैं उसे? क्या अलादीन का जिन्न भी वो फेंफड़े ढूँढ़ सकता जो चिता पर लेटे हों या उसके आगे चले गए हों? शायद यह काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) कर सकेगी– कुछ इलेक्ट्रोड्स को फेफड़ों से जोड़कर, कुछ को दिमाग़ से और बाक़ी सब कुछ विशालकाय क्लाउड डेटाबेस से जोड़कर। लेकिन उसे भी ‘कंप्यूटर विज़न‘ तो मुझे ही देना होगा। वरना मेरे डिजिटल अवशेषों का अर्थ मशीन कैसे समझेगी? तो क्या यह प्रक्रिया भी मेरी सीमाओं में फँस जाएगी! फिर वह मशीन मुझसे पूछेगी, ‘तुम कैसे दिखना चाहते हो? तुम्हारी स्टार्च की हुई शर्ट की तरह एकदम चकाचक, या स्नोमैन की तरह बेढंगा? या फिर कैनवास पर पुते रंगों की परतों जैसा?’ मशीन तो असंख्य विकल्प देगी पर अंतिम निर्णय तो मुझे ही लेना होगा।
‘हर कलाकार का अपना एक वर्ग चरित्र होता है,’ मेरे पसंदीदा समकालीन कवि नामदेव ढसाळ का यह वाक्य मुझे हमेशा सत्य (tautologous) लगता है। इस वास्तविकता को न वे टाल सकते थे, न ही मैं। अपने अस्तित्व की वह शाश्वत सीमा कोई टाल नहीं सकता; मेरा लेखन भी उससे बंधा रहेगा। तो क्या मैं अपने अस्तित्व और कार्यों की विस्तृत सामाजिक–सांस्कृतिक प्रतिध्वनियों को दरकिनार कर केवल अपने निजी प्रयासों को ही चुनूँ?
मेरे पास यादों का बेशक़ीमती ख़ज़ाना है जिसे मैंने साठ साल से अधिक समय में जुटाया है:
… दुबे को दिनेश ठाकुर के घर ले जाने के बाद उनकी अंतिम इच्छा पूरी करने का संतोष; ‘…अमोल और उत्पल अभी की सबसे लोकप्रिय रोमांटिक जोड़ी हैं‘ यह हेडलाइन पढ़ते वक़्त आँखों में उभरे आँसू; …मेरे बनाए एक चित्र के सामने प्रसिद्ध पेंटर गायतोंडे जी का ‘बहुत पसंद आया‘ कहकर दस–पंद्रह मिनट तक ठहरना; …सत्यजीत रे का मेरी फ़िल्म आक्रीत देखने के बाद मुझे घर पर बुलाकर बातें करना; ….वह स्वप्निल लम्हा जब संध्या ने मुझे ‘हाँ‘ कहा; … वह दिन जब राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, संजीव कुमार जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़कर मुझे पहला फ़िल्मफ़ेयर अवॉर्ड मिला; …वह अविस्मरणीय अलस्सुबह जब किशोरी–ताई ने मुझे रियाज़ सुनने के लिए बुलाया और राग ललित सुनाकर मंत्रमुग्ध कर दिया; …वह अनमोल क्षण जब मेरे साथ अपने घर में बैठे हुए हृषि दा ने मेरे साथ पाँच फ़िल्में करने की इच्छा जताई; राजश्री पिक्चर्स के राजबाबू बड़जात्या जी की पीठ पर दी हुई प्रशंसा से भरी थपकी; …कुसूर के पच्चीस हाउसफुल शोज़, जिसमें मैंने पचहत्तर साल की उम्र में लगातार अस्सी मिनटों तक रंगमंच पर एसीपी दंडवते का किरदार निभाया था!
इन सभी अत्यंत संतोषजनक पलों को यदि बाहर निकालता गया, तो गगनचुम्बी इमारत खड़ी हो जाएगी। पर फिर अपरिहार्य अनगिनत निर्णायक और दर्द से भरे क्षण यदि भरना चाहें, तो उनकी चुभती हुई नोकों से थैला फट जाएगा। शायद अच्छा ही होगा, यह तूफ़ान रुक जाएगा। और वही क्षण क़ैद करने लायक़ होगा—जब थैला फटेगा… भरे हुए सारे टुकड़े स्लो मोशन में बर्फ़ के फाहों की तरह हवा में तैरते हुए, धीरे–धीरे ज़मीन पर गिरेंगे। इनसे जो आकार बनेगा, वही मेरा आकार होगा—ब्लॉटिंग पेपर पर इधर–उधर फैलते अल्ट्रामरीन ब्लू के धब्बे की तरह, आकारहीन, फिर भी गीला। मौत के कुएं में चक्कर लगाने वाले और बाहर से उन चक्करों को देखने में मग्न व्यक्ति — दोनों का अनुभव और भावना एक जैसी कैसे हो सकती हैं? क्या कठिन परीक्षा से गुज़र रहे लोगों की गति दूर से देखने वालों की गति से मेल खा सकती है?
क्या रखना है, क्या नहीं की अपनी बात पर वापस आते हुए, क्या एआई टूल इस झमेले को सुलझाने में मेरी मदद कर सकता है? कंप्यूटर एक आदेश आसानी से मान सकता है: ‘सबसे पहले ज़मीन को छूने वाली मेरी यादों के सौ टुकड़ों को सामने रखो।‘ क्या इस तरह का एकाएक किया गया चयन वास्तविक सत्य साबित होगा! चलो किसी और को यह गुत्थी सुलझाने दो… शायद प्रकाशक; उन्हें निकालने दो उन सारी यादों को, जो उनकी अपेक्षित पृष्ठ संख्या में समा नहीं सकतीं। ‘बिन कही गईं’, ‘चीजें जो छूट गई‘ या ‘की गई ग़लतियाँ‘ अधिक बिकाऊ होंगी, शायद। वासनाकांड नाटक में समर्पण की तृप्ति का क्षण अधिक विस्तार से न कर पाना, कई कलाकारों को ‘वे साधारण हैं‘ बोलने का मौक़ा गंवाना, बी.आर. चोपड़ा जी के ख़िलाफ़ केस जीतने पर उन्हें अंगूठा न दिखा, माँ को माफ़ कर देने की बात उनसे कहनी रह गई, कई दोस्तों–गुरुओं– मार्गदर्शकों को अंतिम बार देखना रह गया… कौन जानता है किन अवशेषों की अधिक मांग होगी।
क्या मेरे पास इनमें से किसी के लिए भी जिस अनासक्ति की ज़रूरत है, वह है? क्या यह सब निस्वार्थ रूप से पूरा होगा? क्या मैं सच में ईमानदार रह सकूँगा? क्या मैं इस तरह की बायोप्सी के बाद भी निर्विकार रह सकूँगा–सिसिफ़स की तरह? यूरेनियम पर शोध करते समय मेरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की जिसके लिए उन्हें दूसरा नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन वही प्रयास उनकी मौत का कारण भी बना। उनकी मृत्यु अप्लास्टिक एनीमिया से हुई। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि उनकी नोटबुक, शोध–पत्र भी अगले पंद्रह सौ साल तक विकिरण छोड़ते रहेंगे।
ये सब मुझे अभी क्यों याद आ रहे हैं? This stream of consciousness… आकस्मिक, उतनी ही अनियंत्रित, बेतुके प्रस्फुटन… आठ दशकों की यह समग्रता यदि किसी को व्यर्थ लगे तो?
मेरे चाहने वालों की क्या अपेक्षा होगी मेरे इस प्रयास से? अभिनेता के किरदार के पीछे छिपे इंसान की तलाश सड़कों–स्टेशनों– इमारतों–घरों में करने वाला ‘एक अकेला शहर में! क्या यह इतना सरल और सीधा हो सकता है? फ़िल्म बनाने से पहले मैंने कभी यह नहीं सोचा कि उसका दर्शक वर्ग क्या होगा; विषय पसंद आया, फ़िल्म बनती गई, मेरी शैली में बनती गई और साथ में अपना दर्शक वर्ग भी लेकर आई। कुछ ऐसा ही इस मामले में भी होगा। गोल माल का हीरो मेरा एक छोटा सा हिस्सा है, पर मुझमें केवल वही नायक दिखाई दे, यह अपेक्षा ग़लत है। पर यह द्वंद्व तो हमेशा मेरे साथ जुड़ा है, इतने दशकों से! मैंने पहले ही इसे स्वीकार किया है, जिन्हें स्वीकार हो वे ही साथ चलेंगे, जैसे अब तक एक–दूसरे के साथ चलते आए हैं…
रेने मग्रीथ (Rene Magritte) के इस वाक्य से, जो मुझे प्रोत्साहित करता है, मैं यह समाप्त करता हूँ: ‘सिर्फ़ इसलिए कि दिन की रोशनी इस दुखी संसार को उजागर कर देगी, हमें उसका भय नहीं होना चाहिए।’ मैंने सबकुछ आपके समक्ष रख दिया है। मैं भार–मुक्त हो गया हूँ, सुंदर युवती को नदी के बीच से उठाकर दूसरी तरफ़ पहुँचाकर आगे बढ़ जाने वाले उस ज़ेन गुरु की तरह।
अपनी नई फ़िल्म को दर्शकों के सामने रखते समय, हम ‘Happy Viewing’ कहते हैं; उसी तरह इस पल मैं अपने पाठकों से ‘Happy Reading’ कहते हुए यह अमानत सौंप रहा हूँ।
अमोल पालेकर
पुणे