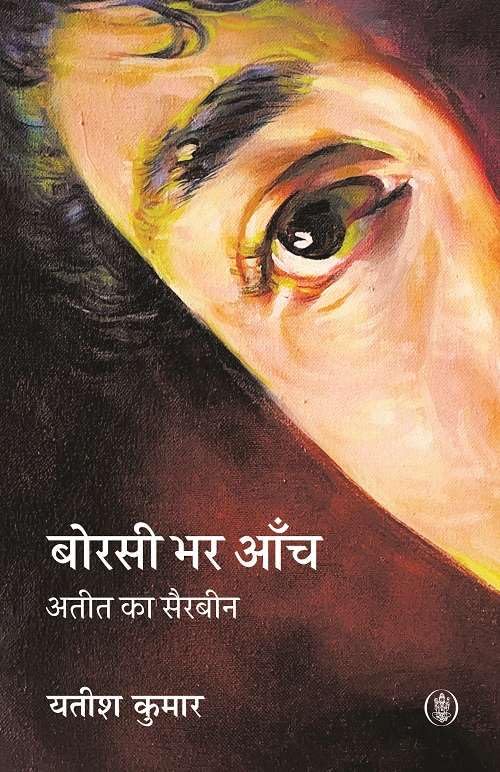आज सत्यजित रे का जन्मदिन है। इस मौके पर आज मुकेश चन्द्र पाण्डेय का लेख. मुकेश चंद्र पांडेय एक प्रोडक्शन हाउस के क्रिएटिव हेड हैं। बच्चों के लिए बनायी जाने वाली एनिमेशन सीरीज के एपिसोड्स लिखते हैं. इन दिनों आर के नारायण की कहानी “पेंटर ऑफ़ साइन्ज़” पर आधारित फिल्म पेंटर की स्क्रीनप्ले, संवाद लिख रहे हैं. मुंबई के शुरुआती दिनों के ख़ालीपन और डर ने उनके लिए सत्यजीत रे की फ़िल्मों का दरवाज़ा खोल दिया। इसी को याद करते हुए मुकेश ने यह लेख लिख भेजा है- संपादक
=========================
ये आज से करीब डेढ़ साल पहले की बात है मुंबई में आये आये अभी कुछ एक महीने ही गुज़रे होंगे पर इतने ही दिनों पर आने वाले कई सालों की साँसे अटक के रह गयी थीं.. स्वप्नों पर इस शहर की विषमताओं ने अपने घेरे बनाने शुरू किये। रातें यूँ ही मुन्तज़िर हो जागी रहतीं और दिनों पर अनिश्चिताओं के डोरे पड़ने शुरू हो चुके थे.. शहर दिल पर लिबास की तरह बदला था.. जैसे किसी ने मासूम सी खुली शर्ट पर अचानक ही बेतरतीब कई टालों का विकीर्ण मगर चमचमाता कोट आवरण कर दिया हो.. यहाँ हर तरफ की चकाचोंध के बीच कुछ तो बासीपन था कि हवा में एक नीरसता निरंतर बनी रहती और मैं इस एक लय व उकता देने वाले वक़्त को काटने के लिए अक्सर पृथ्वी थिएटर चला जाया करता। इस बेतरतीबी में कई कई घंटों वहां बिता देने के बाद भी मन भरा हुआ ही रहता। फिल्मों के प्रति लगाव सभी फंतासियों की गिरहें खोल कर यथार्थ के आभास पर आकर इस कदर टिक गया था मानों अरसे से निर्जलित पड़ी खुश्क चमड़ी पर वास्तविकता क्रूर हो अपने भेधक नाखूनों से निरंतर प्रहार कर रही हो और वक़्त की कई खरोंचे दिन ब दिन उम्र के हिसाब पर गाढ़ी होती जा रही हों.. जगह नयी थी और अभी काम मिलना बाकी था तो भरण की चिंता माथे पर लगातार बानी रहती और इस पर दिन और लम्बे और लम्बे हुआ करते। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि इस तरह के विकट समय को काटने का पुख़्ता इंतज़ाम न किया जाए तो ये आपको पूरा निगलने को आतुर होने लगता है और इसलिए ही खुद को बचाये रखने व चित्त को स्थिर रखने के लिए हम फ़िल्में देख लिया करते। ये वो दौर था कि जब सिर्फ फ़िल्में ही हमसफ़र की तरह साथ थी.. देश विदेश की कई भाषाओं पर बनी तमाम फ़िल्में एक के बाद एक लैपटॉप की स्क्रीन पर चलने लगी और वक़्त की लगाम कुछ देर को ही सही वास्तविकता की पकड़ से ढीली हो कथानक व वृतांत पर आकर रुकने लगी.. और फिर एक दिन हमारे हिस्से में एक ऐसी फिल्म आयी जिसने ना केवल उस वक़्त के तमाम संघर्षों के प्रति मेरे दृष्टिकोण को बदला बल्कि फिल्म निर्माण के बायस सभी पूर्वाभियासों को भी तोड़ दिया। ये उत्कृष्ट फिल्म थी सत्यजीत रे की पाथेर पांचाली.. दो घंटे व ६ मिनट तक चलने वाली ये फिल्म अपने आप में एक सम्पूर्ण यात्रा की तरह महसूस हुई.. इस फिल्म का औरा इतना गहरा था कि फिल्म ख़त्म होने के लम्बे अरसे तक भी ज़हन में कई सवालात लगातार घूमते रहे.. एक अजीब किस्म की टीस रह रह कर गला भिगाने लगी और एक पल में पूरी दुनिया ही बदल गयी.. और फिर खुद को लगातार कचोटने के बावजूद भी रहा न गया तो ट्रायोलॉजी की उत्तरगामी फ़िल्में अपराजितो व अपूरसंसार भी देख डाली। दुर्गा के मर्म से ले कर अप्पू की भटकन सब इतनी जिवंत लगने लगी जैसे वे किरदार न हो कर हमारा ही कोई अक्स हों.. जैसे रोज़ ना जाने कितनी ही दुर्गायें दारिद्र्य की जर्जर दीवारों पर जटिलताओं की खाख़ छानती अपनी कंपकपाती देह को सिमेटे हुए भाग्य की परखच्चे उड़ी छत के तले तिल तिल कर दुर्गत हुई जाती हों, ना जाने कितने ही अप्पू अपने ख्वाबों के बिछौने पर परिस्थिति की आंच में आधे हुए जा रहे हों.. ना जाने कितने घरों पर बादलों के तांडव बिजली गिरा रहे हों और कितने ही परिवार सिर्फ इसलिए विनाश के ग्रास बने हों क्योंकि वे यातनाओं की कतारों पर बिना किसी ख़ास प्रयास के अव्वल खड़े हों.. ये कोई फिल्म नहीं थी ये तो उस वक़्त के या कहें कि आज के भी, आधुनिक दौर की विकसित प्रदर्शनी का फड़फड़ाता हुआ सच था.. डार्क ट्रुथ। बहरहाल इसमें रंग तो दोनों ही हाल में नहीं थे परन्तु फिर भी फिल्मों के उस ब्लैक एंड वाइट एरा में भी सत्यजीत रे ने अपनी अनूठी कला क्षमता के माध्यम से इसमें जीवन के हर वो तमाम रंग उतार दिए जो कि किसी भी इंद्रधनुष का हिस्सा कतई नहीं थे.. ना जाने ऐसे कितने ही अज्ञात रंग उन्होंने आपने आसपास महसूस किये होंगे या महफूज़ रखे होंगे जिस लीक पर उन्होंने कभी फिल्म निर्माण के स्वप्नों को जिया होगा। विभूतिभूषण बंधोपाध्याय की पाथेर पांचाली से सत्यजित रे का जुड़ाव इतना गहरा रहा कि जब उन्होंने तमाम विषमताओं के बाद इसे परदे पर उतारा तो ना केवल एक सार्थक फिल्म साबित हुई बल्कि समाज के एक उपेक्षित हिस्से का प्रतिनिधित्व करती मुखर आवाज़ बन कर सधी रही.. और इसलिए ही वर्ष १९५५ मे प्रदर्शित फिल्म पाथेर पांचाली कोलकाता के सिनेमाघर मे लगभग १३ सप्ताह हाउसफुल रही। इस फिल्म को फ्रांस में प्रत्येक वर्ष होने वाली प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट ह्यूमन डाक्यूमेंट का विशेष पुरस्कार भी दिया गया। और बस यहीं से रे की फ़िल्मी उड़ान को आगाज़ मिला, इस फिल्म के प्रभाव का असर ये रहा कि अब एक के बाद एक रे की बाकी फिल्मों को देखना शुरू किया। जहाँ रबीन्द्रनाथ टैगोर की चोखेरबाली के माध्यम से वे जटिल रिश्तों की उधेड़बुन को बेहद शांत व सौहार्द कायम रख दर्शाते हुए दिखे तो वहीं उपन्यास सम्राट की शतरंज की बिसातों पर सधे कदमों से बाखूबी अपनी चालें रखते हुए आगे बढे.. शतरंज के खिलाडी उनकी पहली हिंदी भाषी फिल्म रही जो कि अपनी तमाम सफलता के बावजूद भी उनके दिल को सिर्फ इसलिए संतुष्ट नहीं कर पाई क्योंकि उनका मानना था कि फिल्म पर भाषाई बाधा के चलते फिल्म उम्मीद से हल्की रही वरना ये और भी बेहतर हो सकती थी.. कलाकार की कला वहीँ तक जीवंत रह सकती है जब तक वह खुद के प्रति संदेहात्मक रवैया ना इख़्तियार करता चले.. उनके इस समृद्ध फ़िल्मी सफ़र से तो कोई भी अछूता नहीं रहा .. खैर सत्यजीत रे ने न केवल फिल्मों, बल्कि रेखांकन के जरिये भी अपनी रचनात्मक ऊर्जा को बखूबी अभिव्यक्त किया। बच्चों की पत्रिकाओं और पुस्तकों के लिए बनाए गए रे के रेखाचित्रों को कला समीक्षकों ने खूब सराहा … बहुमुखी प्रतिभा के धनी सत्यजित रे कहानी लेखन से भी जुड़े रहे और विभिन्न मानवीय संवेदनाओं को निरंतर कलमबद्ध करते रहे.. वे ना केवल हम जैसे कंटेम्पररी फिल्म एस्पैरेंट्स के लिए एक चलता फिर फिल्म संस्थान हैं बल्कि पिछले दौर के कई दिग्गज फिल्म निर्मातों पर उनकी अमिट छाप देखने को मिलती है.. श्याम बेनेगल सत्यजित रे के बारे में अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि पाथेर पांचाली ना केवल उनका फ़िल्मी अध्ययन रही बल्कि फिल्मों के उनके सभी प्रयोगों पर एक असेसर की तरह हमेशा उन्हें सचेत करती रही..