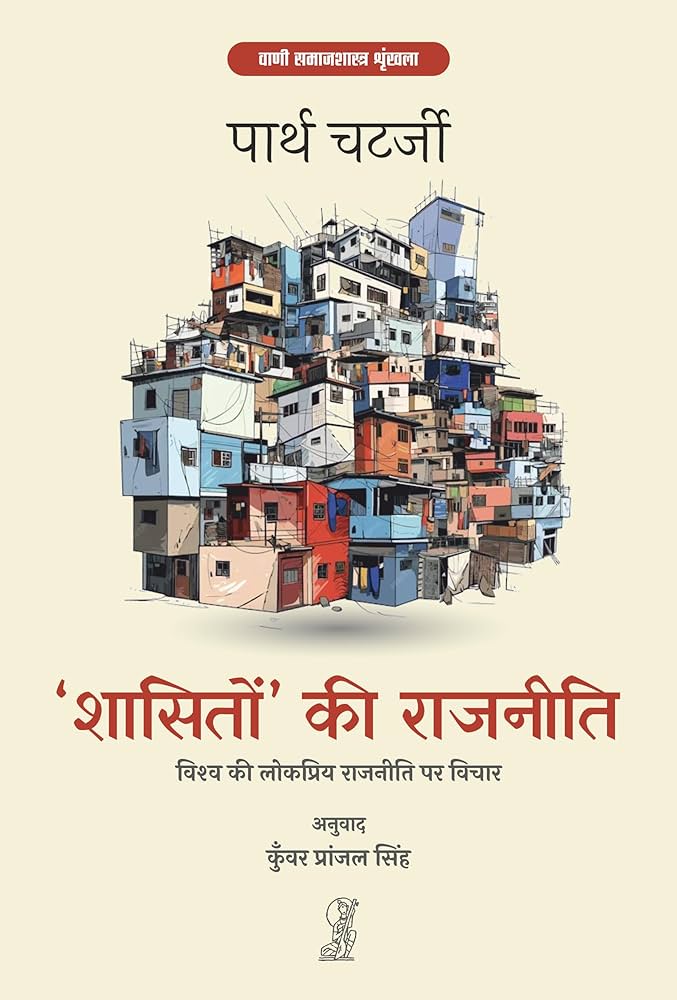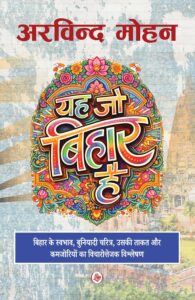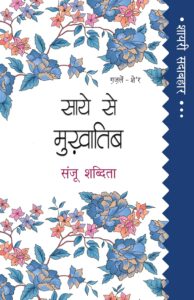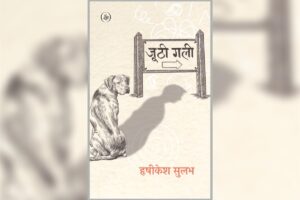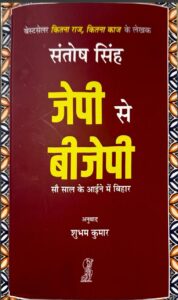इस साल हिन्दी में एक महत्वपूर्ण पुस्तक का अनुवाद आया। प्रसिद्ध राजनीतिक सिद्धांतकार पार्थ चटर्जी की किताब ‘The Politics Of Governed’ का अनुवाद ‘शासितों की राजनीति’ के नाम से। यह अपनी तरह की अनूठी किताब है जिसमें आम जन के नज़रिए से राजनीति को देखा गया है। पुस्तक का अनुवाद किया है दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में राजनीतिशास्त्र पढ़ाने वाले कुँवर प्रांजल सिंह ने। आइये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित इस किताब के अनुवादक की लिखी भूमिका पढ़ते हैं और जानते हैं कि इस किताब का हिन्दी में आने का क्या महत्व है- मॉडरेटर
=========================
अनुवादक की ओर से…
भारत की राजनीति, समाज और संस्कृति को एक पैनी निगाह से देखती हुई यह कृति समाज विज्ञान और सृजनात्मक साहित्य के बीच की दूरी को कम कर देती है। कदाचित इसलिए यह विद्यार्थियों और उस्तादों के बीच इतनी लोकप्रिय रही है। इस लोकप्रिय और कालजयी रचना का अनुवाद करना आसान काम नहीं था। फिर भी इस ज़ोखिम को मैंने इसलिए उठाया कि इस किताब का अध्ययन किये बिना हिंदी के समाज विज्ञान की बौद्धिक दुनिया लोकतंत्र के उस पक्ष को नहीं समझ सकती जिसे केवल ‘शासित’ कह कर संबोधित किया जाता रहा है, जिसका सीधा संबंध लोकप्रिय संप्रभुता से है। दरअसल पार्थ चटर्जी ने लोकप्रिय संप्रभुता के सैद्धांतिक आधार का खुलासा अपनी किताब के शीर्षक “शासितों की राजनीति” में ही कर दिया है और यह दावा किया है कि आधुनिक राज्य की वैधता स्पष्ट रूप से और दृढता से लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है। इस आधार पर पार्थ चटर्जी ने लोकतंत्र के उस सिद्धांत को चुनौती दी जहाँ यह सामान्य रूप से मान लिया गया था कि लोकतंत्र का मौलिक मूल्य “लोकप्रिय संप्रभुता” है। इसी आधार पर पार्थ चटर्जी ने लोकतंत्र को लोगों के शासन के स्थान पर “शासितों की राजनीति” के रूप में परिभाषित किया है।
इस किताब से मेरा पहला परिचय 2015 में प्रोफ़ेसर उज्ज्वल कुमार सिंह ने कराया था। तब मै दिल्ली विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग में एम. ए. का छात्र था। इस किताब की भाषा इतनी चुस्त और संश्लिष्ट थी कि मुझ जैसे हिंदी माध्यम के विधार्थी को दो बार पढ़ना पड़ता था। इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए मैंने हर उस दरवाज़े पर दस्तक दी जिसे मै पहचनता था कि वह मुझे इस किताब की सैद्धांतिकी को हिंदी में समझा सकता था। उस दरमियान किसी ने पास बैठाकर इस किताब की कुछ लाइनों को समझाया और किसी ने दरवाज़े से ही लौटा दिया। इस कड़ी में मै अलीशा ढींगरा को नहीं भूल सकता जिन्होंने उन दिनों अपने पीएचडी से समय निकलर मुझे इस किताब की सैद्धांतिक बनावट और पद्धति को समझने में मेरी मदद की। शायद यही वह समय था जब इस किताब से मेरा एक रिश्ता बन गया।
इस रिश्ते को निभाते हुए मैं अक्सर अपने मित्रों- अमरजीत, राजेन्द्र, नौशाद तथा विकास- के बीच इस किताब की चर्चा करने लगा। मित्रों के द्वारा यह कहा जाने लगा कि जब इस किताब पर इतना बोलते हो तो क्यों न इस किताब का हिंदी अनुवाद कर डालो! मित्रों की यह बात सुन कर मैं इसके अनुवाद पर विचार करने लगा। अपने इस मंसूबे को लेकर जब मैं अभय कुमार दुबे के पास पहुँचा तो अभय जी ने मेरे इस विचार को प्रोत्साहित करते हुए पार्थ चटर्जी से संपर्क करने को कहा और रास्ता भी दिखाया। और जब मैंने इस किताब के कुछ पन्नों का अनुवाद करके अभय जी को दिखाया, तब अभय जी ने बहुत साफ़ शब्दों में कहा, “इस बात को अपने दिमाग में बैठा लीजिये की अनुवाद मूल कृति का पुनरुत्पादन नहीं, पुनर्रचना है। अनुवाद एक समूचे पाठ को एक दूसरी भाषा में, दूसरी लिपि में, दूसरी वाक्य रचना में, दूसरी संस्कृति के जगत में रचना है”। अभय जी की इस सीख ने मेरे दिलोदिमाग में चल रहे कई मिथकों को तोड़ दिया जो अनुवाद से जुड़े थे। मसलन, अनुवाद कैसे शुरू किया जाये, कैसे होगा, अनुवाद की कैसी भाषा होगी? आज यह किताब जब हिंदी की शक्ल-सूरत ले रही है तो इसका पूरा श्रेय मैं प्रोफ़ेसर अभय कुमार दुबे को देना चाहूँगा। उन्होंने मुझ जैसे नाचीज़ पर भरोसा किया, इसके लिए मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। इसी के साथ मैं आकांक्षा सिंह और मेरे माता-पिता के प्रति आभर प्रकट करता हूँ जिन्होंने इस किताब के अनुवाद को न केवल पढ़ा बल्कि इसको पूरा करने के लिए प्रोत्साहित भी किया और समय समय पर फटकार भी लगायी। इस क्रम में, मैं अदिति जी को विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने मुझ पर अंतिम समय तक भरोसा बनाये रखा। पांडुलिपि को सुधारने और छपने योग्य बनाने में डॉ. रमाशंकर सिंह तथा वाणी प्रकाशन के सम्पादकीय मंडल ख़ास तौर से कुमार वीरेंद्र और भारद्वाज जी का आभारी हूँ।
अंत में, मैं यहाँ कुछ दबी आवाज़ में हिंदी के समाज विज्ञान के पाठकों से एक गुज़ारिश और शिकायत करना चाहूँगा। अख़बारी लेखन पढ़ते रहने के कारण बहुत से पाठक सीधे सरल और छोटे वाक्य पढ़ने का इस कदर अभ्यस्त हो चुके हैं कि लंबे और जटिल वाक्य समाने आते ही उनकी शिकायत होती है कि हिंदी सरल लिखी जानी चाहिए। यदि आप “सरल हिंदी” के भावात्मक अर्थ के तह में जाएँगे तो पाठक आप से किसी बाल-पत्रिका जैसी सरल हिंदी भाषा में समाज विज्ञान लिखने का ज्ञान दे रहा होता है। मेरा इरादा बाल-पत्रिकाओं की अवमानना करने का बिलकुल नहीं है बल्कि यह कहूँगा कि उसके लिए खास किस्म की संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है लेकिन जब आप समाज विज्ञान या ज्ञान के किसी अनुशासन की किताब पढ़ रहे हों तो ऐसी अपेक्षा हिंदी भाषा में ज्ञान निर्माण के लिए कोई बहुत ठीक बात नहीं होगी। विचित्र बात यह है कि अंग्रेजी पढ़ते समय पाठकगण यह शिकायत नहीं करते। उसके लिए वे शब्दकोश भी देखते हैं! सरलीकृत हिंदी की मांग करने वाला यह पाठक अनुवादक से भी किसी ‘पाठ’ के सरलीकरण की माँग करने लगता है। वह अपेक्षा करता है कि अनुवादक जटिल वैचारिक लेखन की भी छोटे-छोटे वाक्यों में तोड़ कर पेश करेगा। अनुवादक यह मांग पूरी करने के चक्कर में पाता है कि उसने वाक्य तो तोड़ दिये और काफी हद तक सरल भी कर दिये लेकिन मूल लेखन की बारीकियां और उसकी अंतनिर्हित एकात्मक अर्थवत्ता हाथ से निकल गयी।
आशा करता हूँ कि हिंदी के समाज विज्ञान से जुड़े विद्यार्थी, शोधार्थी और हिंदी के गंभीर पाठक पार्थ चटर्जी की इस कालजयी रचना से लाभान्वित होंगे। कहना न होगा कि अनुवाद की ख़ामियों की ज़िम्मेदारी केवल मेरी है।