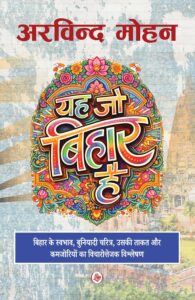हाल में ही हिंदी के वरिष्ठ कथाकार स्वयंप्रकाश को कथाक्रम सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई है. इस अवसर पर प्रस्तुत है इलेक्ट्रोनिक मीडिया, भारतीय समाज और हिंदी कहानी के पारस्परिक संबंधों पर उनके साथ माधव हाड़ा की बातचीत. बातचीत उपलब्ध करवाने के लिए हम कल्पनाशील संपादक, युवा आलोचक पल्लव के आभारी हैं- जानकी पुल.
कहानी अपनी प्रकृति से ही समाज निर्भर साहित्यानुशासन है। यह समाज के खाद-पानी से संभव होती है और इसी से जीवित रहती है। ‘इसमें लोग होते हैं, उनके संदर्भ और संबंध होते हैं, कुंठाएं, संघर्ष और स्वप्न होते हैं।’ कोई भी सामाजिक बदलाव इसलिए कहानी के आवयविक संगठन और इसकी अंतर्वस्तु को तत्काल प्रभावित करता है। यह नामालूम ढंग से सामाजिक परिवर्तन को आत्मसात कर अपने को तत्काल बदल लेती है। महायुद्धों के पूर्व की वैज्ञानिक उपलब्धियों से जैसे औद्योगिक क्रांति हुई वैसे ही युद्धांत्तर काल के तकनीकी विकास ने संचार क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। टीवी और इंटरनेट जैसे संचार माध्यमों के विकास और विस्तार ने वैयक्तिक और सामाजिक जीवन में बुनियादी रद्दोबदल कर दिया है। इससे मनुष्य के सोच और आचरण में आधारभूत बदलाव हुए हैं। भारत में संचार क्रांति का विस्तार विस्फोटक ढंग से हुआ। गत सदी के अंतिम दो दशकों में ही भारतीय समाज को एकाएक इससे रूबरू होना पड़ा। 1990 के दशक में शुरू हुई आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया से इसकी गति बहुत तेज हो गई। टेलीविजन की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ी। सरकार नियंत्रित दूरदर्शन और निजी केबल सैटेलाइट टेलीविजन की पहुंच और प्रभाव का दायरा भारतीय जनसंख्या के अधिकांश तक विस्तृत हो गया। इंटरनेट का प्रसार अभी शहरी और कस्बायी लोगों तक सीमित है, लेकिन आम भारतीय के लिए यह अब अजूबा नहीं रहा। इलेक्ट्रोनिक मीडिया के इस विस्फोटक प्रसार से भारतीय समाजार्थिक और सांस्कृतिक जीवन में व्यापक उथलपुथल पैदा की है। इसने भारतीय जनसाधारण के पारंपरिक जीवन मूल्यों, रुचियों और संस्कारों को बदलना शुरू कर दिया है। कहानी समाज निर्भर साहित्य रूप है इसलिए इस बदलाव से इसकी अंतर्वस्तु और आवयविक संगठन भी बदलना शुरू हो गए हैं, लेकिन पारंपरिक हिंदी साहित्यालोचना में इस बदलाव की पहचान और परख की कोई पहल दुर्भाग्य से अभी तक नहीं हुई है। यह इस ओर पीठ किए हुए है और इसको शक की निगाह से देखती है। इलेक्ट्रोनिक मीडिया सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारक बनकर उभरा है लेकिन हिंदी की ज्यादातर साहित्यकार बिरादरी का इसके प्रति नजरिया नफरत और हिकारत का है। धारणा कुछ भी हो, यह तय है कि गत दो दशकों के दौरान इलेक्ट्रोनिक मीडिया के विस्फोटक प्रसार ने भारतीय वैयक्तिक और सामाजिक जीवन को बदल दिया है और क्योंकि कहानी समाज निर्भर साहित्य रूप है इसलिए इस बदलाव से इसकी अंतर्वस्तु और आवयविक संगठन में भी ध्यानाकर्षक बदलाव हुए हैं।
विख्यान कहानीकार स्वयं प्रकाश का नजरिया इलेक्ट्रोनिक मीडिया के प्रति नफरत का नहीं है। वे इसे चुनौती की तरह लेते हैं और इससे पहले एक चिंतनशील नागरिक और बाद में कहानीकार के रूप में रूबरू होते हैं। उनकी कहानियों में इस मुठभेड़ से होने वाली अंतर्क्रिया के कई रूप मौजूद हैं। उनसे इस विषय पर हुई लंबी बातचीत यहां प्रस्तुत है।
माधव हाड़ा – बातचीत यहां से शुरू करते हैं कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया से भारतीय समाज किस तरह रूबरू हुआ? भारतीय समाज पर उसके प्रभावों को आप किस तरह देखते हैं?
स्वयं प्रकाश – सबसे पहले तो यह स्पष्ट करना जरूरी है कि जब हम इलेक्ट्रोनिक मीडिया की बात करते है तो हमें उसको साफ तौर पर दो भागों में बांटकर देखना चाहिए। एक है इलेक्ट्रोनिक मीडिया तकनीक के रूप में, तकनीकी विकास के रूप में, संचार के एक नये माध्यम के रूप में, एक नयी विधा के रूप में, और दूसरा यह कि उस तकनीकी विकास पर, संचार के माध्यम पर, संचार के नये रूप पर अधिकार किसका है और उसके प्रसार में हित किसके है। क्योंकि इन दो चीजों को अलग-अलग किए बिना उसकी पूरी शक्ल अपने सामने साफ नहीं होगी। बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं और ऊपरी तौर पर ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रोनिक मीडिया की वजह से हो रही हैं वह संभव है कि कुछ दूसरे कारणों से हो रही हों, जैसे साम्राज्यवाद के प्रसार से या जैसे वैश्वीकरण के कारण या जैसे राष्ट्र राज्यों की स्वायत्तता के हनन के कारण या जैसे उपग्रह संचार की तरक्की या इस पर सैन्य अधिकारों के कारण या सैन्य हितों के कारण। बहुत सारी चीजें स्पष्ट रूप से हमारे जीवन में हस्तक्षेप करती हुई दिखाई देती हैं, लेकिन उनका कारण मीडिया या उसकी तकनीक नहीं, बल्कि दूसरे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक कारण हैं। इन दोनों को अलग-अलग कर देखेंगे तो इलेक्ट्रोनिक मीडिया की करामातें हमें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगी।
माधव हाड़ा – ये जो दूसरी ताकते हैं वे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है इलेक्ट्रोनिक मीडिया को। एक माध्यम के रूप में जो उसकी भूमिका है उसे तो देखना ही पड़ेगा। उन ताकतों के बारे में भी विचार करेंगे लेकिन मुझे लगता है कि उन ताकतों के पास और भी माध्यम हो सकते थे, लेकिन वे इलेक्ट्रोनिक मीडिया को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही हैं, तो यह तो मानना ही पड़ेगा कि उसकी प्रभाव क्षमता या उसका मानवीय आचरण, मानवीय मूल्य व्यवस्था पर जो प्रभाव है, वह निर्णायक प्रभाव है और प्रभाव क्षमता को उन्होंने अच्छी तरह पहचान लिया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन ताकतों के साथ वह मानवीय मूल्य व्यवस्था को या मानवीय आचरण को किस तरह से प्रभावित कर रहा है?
स्वयं प्रकाश – एक कहानीकार और लेखक के रूप में नहीं, एक नागरिक के रूप में भी और एक चिंतनशील सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी सबसे पहले तो एक माध्यम के रूप में इलेक्ट्रोनिक मीडिया की शक्ति से मैं प्रभावित हूं और इसका स्वागत करता हूं। हर तकनीकी विकास ने इस प्रकार की चुनौतियां समाज के सामने रखी है कि उसमें कुछ बुनियादी तब्दीलियां, बदलाव आए हैं, बहुत सारी तब्दीलियां तो ऊपरी होती हैं, लेकिन कुछ बुनियादी तब्दीलियां भी हुई हैं। जब छापा चला, या जब किताब चली या जब सिनेमा आया या जब रेलगाड़ी चली तब भी इस प्रकार के डर, इस प्रकार के एप्रेहेन्शंस, इस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई थीं कि इससे लोगों का चरित्र बिगड़ जाएगा, आचरण बदल जाएगा। आचरण बदला तो सही लेकिन बिगड़ा कि नहीं, इसका फैसला उस समय ठीक तरीके से लोग नहीं कर पाए। समाज में उसका अनुमान लगाना कठिन होती है, जब भी इस प्रकार की कोई तब्दीली आती है तो इसी तरह से टेलीविजन के हमारे घरों में आने से, जाहिर है कि हम लोगों का सोच वगैरह सब कुछ बदल गया। ऊपरी तब्दीलियों के अलावा जो चीजें इनके भीतर से हुई है उसमें कुछ लोग यह भी मानते है कि तकनीक का भी अपना एक चरित्र होता है और जिसके भी अधिकार क्षेत्र में उसका संचालन हो, लेकिन उस तकनीक का वह चरित्र अपना प्रभाव छोड़ता है और मनुष्य के स्वभाव को परिवर्तित करता है। मसलन आज हम कल्पना करें कि हम एक समाजवादी देश में होते और वहां टीवी का प्रसार इसी तरह से अचानक हमारे गांव-गांव, देहात-देहात में हो गया होता तो क्यो वे परिवर्तन कुछ और तरह के होते? या मान लीजिए यह बिल्कुल एपॉलिटिकल हो जाए, इसके पीछे किसी वर्ग का कोई स्वार्थ या हित रहे ही ना और सिर्फ एक माध्यम के रूप में हमारे सामने यह नाचती गाती तस्वीरें दिखाए तो इस तरह से भी क्या वह हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकता है? यह होगा उसका चरित्र। एक तकनीक का जो अपना वर्ग चरित्र है या जो चरित्र है उसमें हमारे जीवन को बदलने की क्षमता का जो अनुमान है, उसका आकलन हम कर सकते हैं। बाद में हम इस पर भी विचार कर सकते हैं कि यदि यह जनपक्षीय होता तो इसका क्या प्रभाव पड़ता और कैसा प्रभाव पड़ता।
माधव हाड़ा – पूंजीवादी ताकतें इस मीडिया का इस्तेमाल कर रही हैं और विकल्प वाली दूसरी ताकतें भी कर रही हैं। लेकिन एक माध्यम के रूप में तो मीडिया की हैसियत है ही, बल्कि अब वह तकनीक से ज्यादा एक स्वायत्त सत्ता है। तो यह बताएं कि मनुष्य के आचरण पर, मनुष्य की समझ पर या उसके विवेक पर, यह किस तरह से प्रभाव डाल रहा है?
स्वयं प्रकाश – हॉ! हम यहां से शुरू करें कि जब सबसे पहले टेलीविजन चला था तो उस वक्त की एक प्रतिक्रिया और उसके करीब सत्तर साल बाद की एक प्रतिक्रिया देखें। हक्सले ने इसे इडियट बॉक्स या बुद्ध बक्सा कहा था और इसके पीछे उनका आशय यह था कि यह जो कुछ भी परोसता है उसे हम बुद्धु भाव से ग्रहण करते चलते हैं। इसमें इंटरकम्युनिकेबिलिटी नहीं है मैं उसमें कुछ नहीं देता। मैं सिर्फ उसको ग्रहण करता हूं। एक दर्शक के रूप में या एक प्रेक्षक के रूप में सिनेमा में और रंगमंच में भी मेरी प्रतिक्रिया होती है, जिसका कोई प्रभाव होता है लेकिन टेलीविजन के सामने तो मैं बिल्कुल निठल्ला, निकम्मा, निखट्टू बैठा रहता हूं और सिर्फ उसको ग्रहण करता रहता हूं इस लिहाज से इसको बुद्धु बक्सा कहा गया था। बाद में, बहुत बाद में मार्शल मेक्लुहान ने कहा था कि मीडियम इज मैसेज। अब इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि ऐसा क्या है जिसमें माध्यम ही संदेश बन जाता है। मैं इसको इस तरह से समझने की कोशिश करता हूं कि जो सबसे पहला काम टीवी करता है, कि हमारी मोबिलिटी को, हमारे चलने फिरने को, हमारे घुलने-मिलने को, हमारे घर से बाहर निकलने को, पास-पड़ोस में जाने को, खेलकूद को, पढ़ाई को और हमारे सामाजिक व्यवहार को सीमित और संकुचित करके हमें एक कुर्सी पर बैठा कमरे में कैद आदमी बना देता है। यहीं से इसका व्यक्तिवादी चरित्र आरंभ हो जाता है। लेकिन साथ में वो हमें सूचना संपन्न भी बनाता है। मैं बचपन से सोचा करता था कि नोबल पुरस्कार कहां और कैसे और किस तरह से मिला करता होगा। और मैंने अपने बचपन से लेकर जवानी तक भी इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी कि कभी वो दृश्य मुझे देखने को मिलेगा कि जहां नोबल पुरस्कार एक आदमी को दिया जा रहा हो और मैं उसे देख रहा हूं। यह बात आमतौर पर हर किसी घटना के लिए सही है, चाहे वह क्रिकेट का मैच हो या कहीं बरफ या तूफान या आंधी या ज्वालामुखी फटने की घटना हो। तो एक प्रकार से वह शिक्षित भी करता है और सूचना संपन्न होने में और शिक्षित होने में ज्यादा अंतर भी नहीं छोड़ता क्यों कि जब आप एक पुस्तक पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त आप चुन रहे होते हैं और चबा रहे होते हैं…… लेकिन जब आप टेलीविजन देख रहे होते है तब आप सिर्फ जीम रहे होते हैं। तो इसलिए सूचना और बोध का जो अंतर है वह थोड़ा-थोड़ा धूमिल होता चला जाता है और धीरे-धीरे आप बोध को भूलते चले जाते हैं। चीजों को अपने स्तर पर रिजोल्व करना बंद कर देते हैं और सिर्फ सूचनाओं के कीड़े बन जाते हैं। सूचना एक प्रकार की उत्तेजना देती है, लेकिन वह आपको निर्णय सक्षम नहीं बनाती क्योंकि वह आपके ज्ञान का हिस्सा नहीं बना है। इसलिए हम देखते हैं कि इसमें जो क्विज कंपीटिशंस आती हैं जिसको ज्ञान की प्रतियोगिता या सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं कहा जाता है। उनमें उछल-उछलकर एक सैकंड में दस-दस, बीस-बीस जवाब सही देने वाले बच्चे भी अपने जीवन में निर्णय लेने की बारी आती है तो अक्सर बहुत ही कमजोर और कृशकाय महसूस होते हैं अपने बुजुर्गों के सामने, जिनके पास संभव है इतनी सूचनाएं न हो, लेकिन जिनके पास बोध की पूंजी होती है। इस तरह से इसने एक तो आपकी मोबिलिटी को कम किया, आपके चलने-फिरने को कम किया, आपके मोहल्ले और पड़ोस में आपकी दिलचस्पी को कम किया, आपके शारीरिक व्यायाम और स्वास्थ्य को प्रभावित किया। साथ ही साथ इसने आपके मन से उस सामाजिकता बोध को भी निकाल दिया, जिससे आप एक सूचना को ज्ञान में तब्दील करते थे। ये इसके मोटे प्रभाव मनुष्य स्वभाव पर दिखाई देते हैं।
…… लेकिन अब इसके आगे चलिए, यह तो हुई वह तकनीक, जो यह हमें देती है। यह तकनीक का अपना चरित्र हुआ जो आपको इस स्तर पर प्रभावित करने के बाद दूसरा कदम यह उठाती है कि आपको व्यक्तिवादी सोच का गुलाम बनाती है। जब आप एक चैनल देख रहे होते हैं तब उस समय दूसरा कोई आदमी, दूसरा कोई चैनल देख ले, यह आपको बर्दास्त नहीं होता। एक परिवार में जितने सदस्य है उतने चैनल हों तो एक साथ, टीवी पर देखे नहीं जा सकते तब या तो आप आपस में लड़ेंगे या एक दूसरे के प्रति मन में द्वेष रखेंगे। एक सामान्य दृश्य है कि पुरुष समाचार देखना चाहते है, जबकि स्त्रियां घर-गृहस्थी की बातें देखना चाहती है, बच्चे कार्टून देखना चाहते हैं और जो बहुत सारे लोग हैं वे सिर्फ विज्ञापन देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार जब हम इसके टेक्नीक से इसकी वस्तु पर आएंगे तो इसके और आयाम खुलेंगे।
माधव हाड़ा – अब यह है कि जब वह मनुष्य की समझ, उसकी मूल्य व्यवस्था सबको बदलने की ताकत रखता है तो हमारे यहां जो उसका आगमन है वह इतना आकस्मिक है…. मतलब पश्चिम में उसका आगमन एक लंबी अवधि में या लंबी प्रक्रिया के तहत है तो वहां, मुझे लगता है कि संकट उतना नहीं है जितना हमारे यहां है। यह बताएं कि भारतीय समाज पर इसका तत्काल क्या प्रभाव दिखाई पड़ रहा है फिलहाल!
स्वयं प्रकाश – यह भी दोहरा प्रभाव है। इसे समझना आवश्यक है। हमारे यहां सरकार ने इस माध्यम को शुरू किया है और एक समय था जब हमारी प्रधानमंत्री गर्व के साथ यह घोषणा करती थीं कि प्रतिदिन एक दूरदर्शन केन्द्र खोला जा रहा है। जाहिर है, इसके पीछे राजनीतिक हित यह है कि कोई राजनेता इतनी बड़ी सभा नहीं कर सकता कि जिसके अंदर देश के अनेक महानगरों के सभी टेलीविजन रखने वाले नागरिक शामिल हो सकें। लेकिन, अगर आपको याद हो तो, उस समय में दूरदर्शन का उपयोग जनशिक्षा के लिए भी किया गया और अच्छा उपयोग किया गया। जैसे आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया जाए कि डीपीटी के तीन टीके वाला जो विज्ञापन है या साक्षरता के बारे में जिस प्रकार के संदेश इसमें प्रसारित किए गए या विकास के जो समाचार दिखाए गए या आयोडीन नमक या खेलों के बारे में जिस प्रकार की दिलचस्पियां पैदा हो गईं और इसकी छोटी-छोटी बारीकियों को लोग समझने लगे, तो इस प्रकार से एक जनरुचि वैज्ञानिक कार्यक्रमों की ओर सामाजिक कार्यक्रमों को भी बनाने का प्रयास सरकार ने अपने हितों के अतिरिक्त इस माध्यम का उपयोग करते हुए शुरू किया और यह सोचा जाने लगा कि जब पंचायतों में टेलीविजन लगेंगे या स्कूलों में टेलीविजन लगेंगे, इससे शिक्षा और ज्ञान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जा सकेगा और कुछ हद तक उस दिशा में हम बढ़ते हुए दिखाई भी दे रहे थे। लेकिन यहीं व्यवसाय ने हमला कर दिया और इसके बाद इसका चरित्र पूरी तरह से बदल गया।
माधव हाड़ा – लगभग इकॉनोमिक लिबरलाइजेशन वाली जो घटना है नरसिंह राव सरकार की, मुझे लगता है आप उससे…..
स्वयं प्रकाश – (बीच में काटकर) नहीं, नहीं। मैं नहीं सोचता ऐसा। मैं यह सोचता हूं कि आप याद करें जब कमलेश्वर दूरदर्शन के एडीशनल डायरेक्टर जनरल थे और वह इंदिरा गांधी का समय था। सुधारों से पहले का समय था और उन्होंने एक छोटी-सी बात पर इस्तीफा दे दिया था। एडीशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट छोटी-मोटी नहीं होती। और वह बात यह थी कि भारत में रंगीन टेलीविजन की इस वक्त आवश्यकता है कि नहीं है। जिस समय आपके यहां इलेक्ट्रोनिक मीडिया आया, एशियाड के समय में बहुत सारे टीवी बाहर से आए थे, उसी समय से विदेशी कंपनियां इस चक्कर में थीं कि आपको प्रभावित कर अपना माल भारत में खपाया जा सके और वे निरंतर सरकारी मशीनरी और सूचना प्रसारण विभाग के सचिवों को, अधिकारियों और मंत्रियों को इस दबाव में रखती थीं कि किसी न किसी तरह से इसका निजीकरण हो, व्यापारीकरण हो, व्यवसायीकरण हो और भ्रष्टीकरण हो। जो होकर रहा क्योंकि उसको रेजिस्ट करने की ताकत हमारे पास में नहीं थी…..
माधव हाड़ा – (बीच में) विज्ञापन से राजस्व की लड़ाई मुझे लगता है कि इकोनॉमिक लिरलाइजेशन की घोषणा के साथ शुरू होती है और उसके साथ ही दूरदर्शन के चरित्र में भी परिवर्तन आना शुरू होता है। उसके प्रोडक्शन पर,