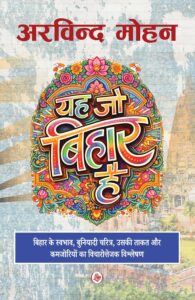युवा लेखक-आलोचक राकेश बिहारी ने हिंदी आलोचना की ‘आलोचना’ की है. आप उनसे सहमत हो सकते हैं असहमत हो सकते हैं, लेकिन बहस के कुछ बिंदु तो उन्होंने इस लेख में उठाये ही हैं- जानकी पुल.
================================================================
बहुत दिन नहीं बीते हैं जब एक पत्रिका में प्रकाशित एक कवर स्टोरी में कुछ वरिष्ठ लेखकों के हवाले से युवा रचनाशीलता की दशा-दिशा पर कुछ प्रश्न उठाये गये थे. उस पत्रिका के अगले ही अंक में एक चर्चित युवा लेखक ने अपने वरिष्ठ रचनाकरों द्वारा उठाये गये सवालों का उत्तर जिस अशालीन और लगभग अश्लील अंदाज़ में दिया उसके कारण कुछ लोग चाह कर भी उक्त युवा लेखक की कुछ तर्कसंगत बातों के पक्ष में भी नहीं खड़ा हो सके. इसी तरह पिछले दिनों अपनी पुस्तक की समीक्षा से विचलित होकर अपना पक्ष रखने के नाम पर कभी अशोभन तो कभी आत्ममुग्ध अंदाज़ में लेखकीय प्रतिरोध दर्ज़ कराने के भी कई मामले देखने में आये हैं. यहां इस बात का उल्लेख जरूरी है कि यह व्याधि आज किसी खास पीढ़ी तक सीमित नहीं है. दरअसल क्या युवा, क्या वरिष्ठ सबको इसने अपने चंगुल में ले रखा है. एक युवा लेखिका के उपन्यास की आलोचना के बहाने एक वरिष्ठ कथाकार-आलोचक के द्वारा अपनी निजी कुंठाओं के अश्लील वमन की एक घटना भी पिछले दिनों चर्चा के केंद्र में रही है.
आलोचना-प्रतिआलोचना के इन ताज़ा उदाहरणों से गुजरते हुये इस प्रश्न का उठना बहुत स्वाभाविक है कि क्या आज लेखकों में अपनी आलोचना सुनने का धैर्य नहीं रहा? प्रश्न जायज है, लेकिन तस्वीर का एक रूख और भी है, जो एक दूसरे प्रश्न को जन्म देता है कि क्या आज की आलोचना अपने संतुलन का विवेक खो रही है? ईमानदारी से कहा जाये तो इन दोनों ही प्रश्नों के उत्तरों से जो स्थिति निकलकर आती है वह खासी चिंताजनक है. असंतुलित आलोचना जो कि वस्तुनिष्ठता के अहाते का अतिक्रमण करते हुये पूर्वाग्रही और निजी आलोचना का पर्याय बन जाती है, के समानांतर लेखकों के बीच अपनी कृतियों की आलोचना को लेकर बढ़ती जा रही असहिष्णुता के परस्पर प्रतिवादी समय के बीच आज आलोचना के एक और लक्षण को भी बड़ी आसानी से रेखांकित किया जा सकता है. यह तीसरा लक्षण है – ठकुरसुहाती और चाटुकारिता का. छोटे-छोटे हित-अहित के संधान के चक्कर में आज लेखकों के भीतर इस प्रवृति का जिस तरह इजाफा हो रहा है वह भी कम चिंताजनक नहीं है.
कुछ महीने पुरानी एक घटना याद आ रही है. एक प्रतिष्ठित दैनिक में एक खास प्रकाशन से प्रकाशित पांच कहानी-संग्रहों पर एक सामूहिक समीक्षा-लेख प्रकाशित हुआ था. लगभग एक हज़ार शब्दों के उक्त आलेख को फेसबुक पर साझा करते हुये एक लेखक, जाहिर है जिनका संग्रह भी उक्त आलेख में उल्लिखित पांच किताबों में शामिल था, ने एक टिप्पणी लगाई कि आज के अलां अखबार में फलां आलोचक ने चिलां किताबों पर विस्तार से लिखा है. किसी पत्र-पत्रिका में एक साथ कई किताबों पर सामूहिक समीक्षा का प्रकाशन कोई नई बात नहीं है, लेकिन किसी लेखक का उस परिचयात्मक आलेख को विस्तार से लिखा हुआ बताना, वर्तमान समय में आलोचना शब्द के अर्थ संकुचन की तरफ इशारा करता है, जो हास्यास्पद से ज्यादा चिंताजनक है. दरअसल इस तरह की अतिउत्साही टिप्पणी के पीछे अपनी किताब की चर्चा के अतिरिक्त अखबार में अपनी तस्वीर देखने का सुख और लगे हाथ अपने प्रकाशक को खुश करने के भाव जैसे कई अन्य तरह के लोभ और दवाब काम करते हैं. आलोचना का प्रायोजित समीक्षाओं में सिमटते जाना तो हम देख ही रहे थे, यह घटना समीक्षाओं के विज्ञापन में तब्दील हो जाने का उदाहरण है. यहां इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि पिछले दिनों एक प्रकाशन गृह से प्रकाशित कुछ पुस्तकों के सेट की सामूहिक समीक्षायें भी पत्र-पत्रिकाओं में देखने को मिली हैं, जो निश्चित तौर पर उक्त प्रकाशक के लगन और मेहनत का परिणाम थीं. एक ऐसे समय में जब कुछ प्रकाशक लाख मिन्नतों-अनुरोधों के बावजूद समीक्षार्थ किताबें नहीं भेजना चाहते किसी प्रकाशक के इन प्रयासों की सराहना की जानी चाहिये. लेकिन यहां मैं एक दूसरी बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं. उक्त समीक्षाओं में एक से ज्यादा ऐसी समीक्षायें शामिल थीं जिनका अधिकांश किताबों के फ्लैप से उधार लिया गया था. यहां इस बात का एक बार फिर उल्लेख जरूरी है कि इन तथाकथित समीक्षाओं को भी कुछ लेखकों ने फेसबुक पर सहर्ष साझा किया. पुस्तकों का विज्ञापन एक अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिये. लेकिन जिस तरह ये समीक्षा वेशधारी विज्ञापन आलोचना और मूल्यांकन की किसी तरह बची-खुची जमीन का अतिक्रमण कर रहे हैं उसकी हानि अंतत: पुस्तकों और लेखकों को ही हो रही है. कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी समीक्षायें एक खास तरह की प्रकाशकीय चालाकी का हिस्सा होती हैं जिसमें बिना अतिरिक्त व्यय के पुस्तकों का विज्ञापन हो जाता है. लेकिन यह भी एक कटु यथार्थ है कि ऐसे विज्ञापनों से न किताबों के पाठक बढ़ते हैं न हीं उनका प्रिंट ऑर्डर. इस तरह के विज्ञापनी समीक्षाओं पर खुश होनेवाले लेखक काश इस बात को समझ पाते कि उनका अतिउत्साह आलोचना और मूल्यांकन के बचे-खुचे स्पेस को भी कम कर रहा है.
यह भी कम चिंताजनक नहीं है कि पिछले दिनों समीक्षा को संबंध साधने के औजार की तरह इस्तेमाल किये जाने की प्रवृत्ति भी लगातार बढ़ रही है. कुछ आलोचकों -समीक्षकों द्वारा समीक्षार्थ लाई गई (आई नहीं) किताबों की सूचना पहले लेखक को देना, पत्रिकाओं को समीक्षा भेजे जाने के पूर्व लेखक को फोन पर ही पूरी समीक्षा सुना देना, या कि प्रकाशन से पूर्व लेखकों को ईमेल से भेजकर समीक्षा का ‘अप्रूवल’ लेना आदि आलोचना की कुछ ऐसी उत्तर आधुनिक चारित्रिक विशेषतायें हैं जिसे मंच पर भले कोई न स्वीकारे, लेकिन नेपथ्य में इनकी बेलें लगातार विकसित हो रही हैं. समीक्षा कोई लिखना ही नहीं चाहता या कि समीक्षक समय पर लिख के नहीं देते जैसे तर्कों के साथ कुछ संपादकों द्वारा लेखकों से ही समीक्षा भिजवा देने का आग्रह भी इसी ‘संबंध-साधी’ प्रवृत्ति का एक अलग डाइमेंशन है. एक ही व्यक्ति का अलग-अलग नामों से समीक्षा लिखने के चलन को भी भी इन्हीं प्रवृत्तियों के विस्तार की तरह देखा जाना चाहिये. आश्चर्य यह कि यह सब इस बेशर्मी और ढिठाई से सम्पन्न हो रहा है कि एक ही समीक्षा दो अलग-अलग पत्रिकाओं में दो समीक्षकों के नाम से छप जा रही हैं और किसी को इसकी खबर तक नहीं, या कि कोई जानबूझकर ऐसी बातों का संज्ञान नहीं लेना चाहता. गोया आलोचना-समीक्षा की असली हैसियत का सबको अंदाज़ा हो.
हाल के दिनों में बेबाक और निर्भीक आलोचना के नाम पर भी कुछ देखने-सुनने को मिल रहा है. जिस तरह बेबाकी और दो टूकपन हमारी आलोचना से गये दिनों की बात होते जा रहे हैं, ऐसे में बेबाकी का स्वागत होना चाहिये. लेकिन यहां एक दूसरी बात गौरतलब है, वह यह कि कहीं बेबाकी ने हड़बड़ी, अशालीनता और अहमन्यता का हाथ तो नहीं थाम लिया है? इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाय उतना ज्यादा अच्छा है कि असावधान और अशालीन बेबाकी थोड़े समय के लिये सनसनी और चुटकुलेबाजी का मज़ा देने के बाद अन्तत: हास्यास्पद होकर रह जाती है. निर्भीक और बेबाक हस्तक्षेप की अनुगूंज दूर और देर तक सुनाई दे इसके लिये जरूरी है कि आलोचना महज एक प्रतिक्रियावादी उपक्रम भर होकर न रह जाये वर्ना प्रायोजन के समानांतर प्रतिप्रायोजन का खतरा बना रहता है.
आलोचना के अर्थ संकुचन को एक अलग फलक पर विस्तृत कर रहे उन महामहिमों की भी कम बड़ी भूमिका नहीं है जो अपनी मेधा, मेहनत और अनुभव की बदौलत अब आलोचक से विशुद्ध विमोचक की भूमिका में आ चुके हैं. आलोचक से विमोचक हो चुकी ये महान विभूतियां कब, कहां और किसे प्रेमचंद और मुक्तिबोध घोषित करती रहती हैं पता ही नहीं चलता. दृश्य तो तब देखने लायक होता है जब किसी सार्वजनिक सभा में उन्हीं का कोई वंशज उनकी इन स्थापनाओं पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर देता है और वे अपनी झेंप मिटाते हुये कभी समीक्षा और प्रोत्साहन गोष्ठी में फर्क बताने लगते हैं तो कभी लिखित और वाचिक परंपरा की बारीकी समझाने लगते हैं.
सवाल के घेरे में वे पत्रिकायें भी हैं, जिनके पन्नों पर समीक्षा का इंतज़ार करती-करती न जाने कितनी महत्वपूर्ण कृतियां धूल और दीमकों की भेंट चढ़ जाती हैं और वहीं दूसरी तरफ कुछ कृपापात्र लेखकों की औसत किताबें भी कई-कई समीक्षाओं से विभूषित होती हैं. किसी पत्रिका या संपादक विशेष के विवेक और निजी निर्णय का नाम देकर पत्रिकाओं की समीक्षा-नीति पर सवाल उठाने से आखिर हम कबतक बच सकते हैं?
आलोचना और समीक्षा के नाम पर लगातार बढ़ रहे अंधेरे के इस साम्राज्य के बीच कुछ उम्मीद की किरणें भी हैं जो तमाम पूर्वाग्रहों और प्रायोजित आयोजनों के विरुद्ध लेखकीय स्वन और संकल्प को खंगालते हुये अपने समय का प्रतिपक्ष रच रही हैं. आलोचना की साख पर बट्टा न लगे और उसकी प्रतिष्ठा फिर से बहाल हो इसके लिये इन आवाज़ों को चीन्हने-पहचानने की जरूरत है. जब तक ऐसा नहीं होता, आलोचना की बात करते हुये हमें राजेश रेड्डी के ये शेर हर बार याद आते रहेंगे –
“अबतक है राहबर पे तुम्हें इतना ऐतबार,
लगता है तुम न मानोगे रह में लुटे बगैर.
परवाज़ में कटेगी किसी की तमाम उम्र
छू लेगा आसमान को कोई उड़े बगैर.”
***
संपर्क : 09425823033
ईमेल: biharirakesh@rediffmail.com