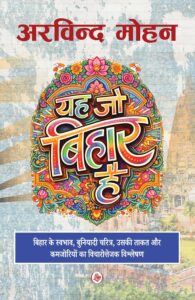वरिष्ठ कवि-आलोचक विष्णु खरे की कोई टिप्पणी बहुत दिनों बाद पढ़ने को मिली. यह लेख उन्होंने ‘फॉर अ चेंज’ किसी तरह के वाद-विवाद फैलाने की मंशा से नहीं लिखा है बल्कि आगामी चुनावों में लेखकों की सक्रिय भूमिका का आह्वान करते हुए लिखा है. खरे साहब की अपनी शैली है, अपने तर्क, हम सब तो बस पढ़ सकते हैं- जानकी पुल.
================================
आज “जैसे हैं,जहाँ हैं”, हिंदी लेखकों,बुद्धिजीवियों और पत्रकारों पर – जो एक ही बिरादरी हैं – ऐसी विडम्बनापूर्ण,विरोधाभासी ज़िम्मेदारी आन पड़ी है जो कभी-कभी उनकी कूवत,मंशा और नीयत तक से बाहर की लगती है.यूँ तो हिंदी साहित्य इस समय भारत का सर्वाधिक तथा संसार का एक अधिकतम प्रतिबद्ध साहित्य है.अपनी तमाम सर्जनात्मक,आस्थागत,नैतिक और बौद्धिक सीमाओं के बावजूद जितने सामाजिक और राजनीतिक सरोकार हिंदी में दिखाई देते हैं उतने अन्य विश्व-भाषाओँ में नहीं हैं. सामाजिक-राजनीतिक जागरूकता,भले ही उसमें लोकप्रिय छद्म वामपंथ का छौंक भी हो, आज हिंदी लेखक की अनिवार्य,मौलिक,स्व-चयनित अर्हता बन चुकी है,सर्जक वह अंततः किसी-भी श्रेणी का माना जाए.दुर्भाग्यवश,आज उसके और देश के सामने एक “क्लिअर एंड प्रेज़ेंट डेंजर” ( साफ़ और मौजूदा ख़तरा ) है लेकिन फ़िलहाल वह उससे आगाह नहीं लगता और न उसके ख़िलाफ़ किसी कार्रवाई की रणनीति बनाने की सोचता नज़र आ रहा है, जबकि वक़्त बहुत कम रह गया है – आम चुनाव चंद महीनों में ही होने वाले हैं.
ब्योरों में न जाते हुए “स्टेट ऑफ़ द नेशन” ( राष्ट्र-दशा ) का ख़ुलासा कुछ इस तरह किया जा सकता है कि इस समय हमें हमारे इतिहास की सर्वाधिक भ्रष्ट,असफल,दिग्भ्रमित,हास्यास्पद तथा अक्षम सरकार उपलब्ध है. 2014 में उसका सत्ता में लौट पाना लगभग असंभव है,पूर्णतः अवांछनीय तो वह है ही. लेकिन उसका जो विकल्प उपस्थित है उसके मुल्की और सूबाई रिपोर्ट-कार्ड और ट्रैक-रेकॉर्ड भी न सिर्फ़ डरावने हैं बल्कि अपनी फाशिस्ट आशंकाओं में देश और दुनिया के लिए एक अनिष्ट विपदा हैं.मुक्तिबोध की ‘दो पाटों के बीच’ फँसने की ‘ऐसी ट्रेजिडी है नीच’ पंक्तियाँ शायद ही कभी इतने भयावह ढंग से मौजूँ हुई हों. अखबार और टेलीविज़न भले ही असली-नक़ली मोदी-नीतीश-आडवाणी विवाद में ‘स्पिन’-रस ले रहे हों लेकिन वे राज्याभिषेक की थाली सजा चुके हैं.
देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से ऐसे प्रश्न उठते हैं जिनमें से सभी को एकदम नए तो नहीं कहा जा सकता लेकिन जिनके पुराने या आसान उत्तर भी किसी के पास नहीं हैं.क्या मतदात्री जनता इस बार (भी) सेकुलर-साम्प्रदायिक बाल की खाल निकालने से तंग आ चुकी है और मौजूदा निज़ाम को हर हाल में अगले बरस केंद्र से हटाने पर आमादा है ? क्या वाक़ई आम हिन्दू सांप्रदायिक वोट देता है, या मौक़ा देखकर सत्तारूढ़-विरोधी (एंटी-इन्कम्बेंट), या मिला-जुला ? क्या भारतीय मुस्लिम देश की सियासत में कोई अमली किरदार निभाना चाहता है – उसे उसके अपने-पराये निभाने दे रहे हैं ? यदि कोई प्रबुद्ध मतदाता हैं तो वे वर्तमान और आशंकित सत्ताधारी के अलावा किस पार्टी या मोर्चे को वोट दें ? वामपंथी दलों की कोई दिलचस्पी अखिल-भारतीय उपस्थिति या रसाई में नहीं दीखती, हिंदी-उर्दूभाषी निर्णायक इलाकों और अल्पसंख्यकों-दलितों में तो बिलकुल नहीं.सैकड़ों चुनाव-क्षेत्रों में उनके अपने या उनके द्वारा समर्थित उम्मीदवार होते ही नहीं.ऐसे में प्रगतिकामी,जागरूक वोट किसे पड़े ? क्या सोनिया-राहुल-मनमोहन को कोई सज़ा न दी जाए,उन्हें काबिज़ ही रहने दिया जाए?
प्रेमचंद के बाद के इन लगभग आठ दशकों में हमें उत्तरोत्तर निर्मम और युयुत्सु प्रेमचंदों की चार पीढ़ियाँ भी मिलनी चाहिए थीं, मिले हमें अधिकांशतः एक-से-एक निष्प्राण उपन्यासकार और कहानीकार. इसके बरक्स निराला और प्रगतिशील कविता से निसृत सामाजिक-राजनीतिक जागरूक जुझारूपन मुक्तिबोध, शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, रघुवीर सहाय, धूमिल से होता हुआ स्पष्टतः अधिकांश युवतम हिंदी कवि-कवयित्रियों तक पहुंचता है. लेकिन आज अनिवार्य है कि इनसे ही नहीं, संसार भर के प्रतिबद्ध स्वरों को सुना जाए और उनसे सीधी कार्रवाई सीखी जाए. 2014 के मद्दे-नज़र सभी प्रतिबद्ध या प्रबुद्ध आधुनिक हिंदी कवियों की बाकायदा अजेंडा-आधारित कई छोटी-छोटी स्थानीय और क्षेत्रीय बैठकें होनी चाहिए और अंत में अगले आम चुनाव से बहुत पहले से और चुनावी गतिविधियों के दौरान हर साहित्यिक विधा के लेखकों को अपनी भूमिकाएँ और कार्य-क्षेत्र तय करने चाहिए. हिंदी के सारे लेखक मिलकर एक साझा, नम्र किन्तु दृढ, निर्भीक और सुस्पष्ट घोषणा-सुझाव- एवं माँग-पत्र जारी करें जो सभी मतदाताओं के लिए भी उपयोगी हो और बिना किसी भेद-भाव हर पार्टी को भेजा जाए. अखबारों और टेलीविज़न से उसके प्रसार-प्रचार का अनुरोध किया जाए तथा इन्टरनैट का कल्पनाशील उपयोग किया जाए. नियमित पर्चे भी बाँटे जाएँ. वामपंथी लेखक संगठनों को अपनी बदहाली में भी इस दिशा में सक्रिय होना होगा.इस सब के लिए पैसा भी बेदाग़ स्रोतों से इकठ्ठा करना पड़ेगा.
कवि-लेखक टेलर मास्टर नहीं होते कि उन्हें नाप देकर मेड-टु-ऑर्डर चीज़ बनवा ली जाए, लेकिन विशेष स्थितियाँ विशेष रणनीतियों और रियायतों की माँग करती हैं.हिंदी कवियों को 2014 की तैयारियों के लिए पूर्ववर्ती बड़े कवियों की रचनाओं का इस्तेमाल तो करना ही होगा,मुक्तिबोध,नागार्जुन,शमशेर और रघुवीर सहाय की तर्ज़ पर सोची-समझी,’लेकर सीधा नारा’ मार्का राजनीतिक कविताएँ लिखने पर भी विचार करना पड़ेगा.”मेरा पैग़ाम सियासत है जहां तक पहुँचे”.कवियों को ऐसी कविताएँ येन केन प्रकारेण रचने,पढ़ने,छपाने,प्रसारित करवाने का कोई अवसर नहीं गँवाने दिया जा सकता.हिंदी में आज ऐसे अनेक वामपंथी या ग़ैर-वामपंथी किन्तु जनोन्मुख कवि-कवयित्रियाँ मौजूद हैं जो वर्षों से निर्भीक रचनाएँ ला रहे हैं. इस मुहिम में विनम्रतापूर्वक लोक-गायकों,गीतकारों तथा उर्दू और हिंदी के ग़ज़लकारों का सक्रिय सहयोग भी लेना होगा.इस कार्रवाई में दलित और अल्पसंख्यक लेखकों-बुद्धिजीवियों की सहभागिता अनिवार्य मानी जानी चाहिए. इस बात पर भी एक स्वस्थ जागरूकता रखनी होगी कि इन प्रयासों को कोई भी भीतरी-बाहरी तत्व कमज़ोर या दिग्भ्रमित करने में न जुटे हों.
मुंबई जैसे महानगर में,जहाँ मराठी के कतिपय श्रेष्ठतम प्रतिबद्ध साहित्यकार और पत्रकार सक्रिय हैं,हिंदी को अपना ‘आइसोलेशनिस्ट’ रुख तजना पड़ेगा. मेरा अनुभव रहा है कि मराठी लेखक-बुद्धिजीवी अपने हिंदी समानधर्माओं से मिलने के लिए अंग्रेजी का कहावती ‘एक्स्ट्रा माइल’ चलने और उन्हें अपने मंच भी देने को सहर्ष तैयार हैं.मुम्बई में लम्बे अर्से या स्थायी रूप से बसे हुए हिंदी लेखक मराठी भाषा,साहित्य और संस्कृति से दूर क्यों रहे चले आते हैं यह मेरी समझ से बाहर है.अधिकांश मराठीभाषी साहित्य-संगीत-कला-राजनीति को लेकर औसत हिन्दीभाषी की तुलना में अधिक जागरूक होते ही हैं,कारण जो भी हों.मैं समझता हूँ कि यदि मुम्बई-स्थित हिंदी लेखक 2014 के चुनावों को लेकर उपरोक्त कार्रवाई में मराठी साहित्यकारों-पत्रकारों-बुद्धिजीवियों का सहयोग चाहें तो अवश्य मिलेगा.लेकिन शोचनीय यह है कि मुम्बई के हिंदी लेखकों ने शायद अपने गुजराती समानधर्माओं से भी राब्ता क़ायम करने की बहुत कोशिश नहीं की है.संभव है मराठी-हिंदी-गुजराती के बीच कुछ वास्तविक-काल्पनिक गिले-शिक़वे भी हों – लेकिन वे ऐसे नहीं हो सकते कि आसानी से दूर न किए जा सकें.
सोवियत रूस के विघटन और यूरोपियन यूनियन बनने के बाद पुराने पूर्वी जर्मनी,चेक तथा स्लोवाकिया के विभाजित राष्ट्रों,हंगरी,बुल्गारिया,इटली,स्पेन,पुर्तगाल,यूनान,विभाजित युगोस्लाविया के नए राष्ट्रों आदि के ऐसे कई लेखकों से बातचीत के अवसर मिले हैं जो नई आज़ादी और यूरोपीय अस्मिता के हर्षातिरेक में राजनीतिक चिंतन,प्रतिबद्धता और सक्रियता को ग़ैर-ज़रूरी समझकर तज या भुला बैठे थे.अब वहाँ अधिकांशतः भ्रष्ट,प्रतिक्रियावादी,फाशिस्ट सरकारें हैं जो जाने-अनजाने नात्सी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहित कर रही हैं और जिन्होंने देश पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और रूसी नव-धनाढ्य माफिया का कब्जा होने दिया है.इन लेखकों-बुद्धिजीवियों की सामाजिक और राजनीतिक प्रतिवाद और प्रतिबद्धता की सलाहियत,भाषा और सक्रियता ही खो चुकी हैं..वे नव-पूँजीवाद का विरोध करने से डरते हैं और समाजवादी चिंतन से शरमाते-घबराते हैं.यह कहानी इतनी सहल और संक्षिप्त नहीं है – इसके दूरगामी दुष्परिणाम होने जा रहे हैं. अभी-अभी रहस्योद्घाटन हुआ है कि जिस वॉल-मार्ट का हम भारत में स्वागत करने जा रहे हैं उसने मेक्सिको में दाखिले के लिए करोड़ों डॉलरों की रिश्वत दी है.भारत की संसदीय प्रणाली सिर्फ साँपनाथ की जगह नागनाथ चुनने की आज़ादी देती है.लेकिन जब तक सच्ची जनवादी व्यवस्था का सपना साकार नहीं होता तब तक मुक्तिबोध की तर्ज़ पर “जो है उससे बेहतर चाहिए” की दिशा में हिंदी के कवियों-लेखकों को अपनी सर्जनात्मक तथा सृजनेतर सक्रियता किसी भी तरह बचाए-बनाए रखनी होगी.
यह टिप्पणी आज मुंबई नवभारत टाइम्स में छपी है