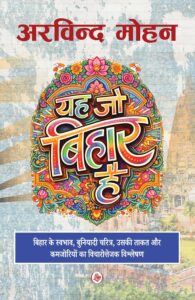शमशाद बेगम को श्रद्धांजलि देते हुए प्रसिद्ध लेखक-पत्रकार प्रियदर्शन का यह लेख उनकी गायकी के महत्व को रेखांकित करता है. प्रियदर्शन ने यह लेख ख़ास तौर पर जानकी पुल के लिए लिखा है, जानकी पुल उनके प्रति आभार व्यक्त करता है- जानकी पुल.
===================================
आम तौर पर हिंदी फिल्मों में महिला गायन की स्मृति इस हद तक लता मंगेशकर और आशा भोसले पर आश्रित रही है कि बाकी सारी आवाज़ें जैसे नेपथ्य में चली जाती हैं। हिंदी फिल्मों के सारे पुराने गाने या तो लता मंगेशकर के गाए मान लिए जाते हैं या फिर आशा भोसले के। सुमन कल्याणपुरे से लेकर हेमलता और वाणी जयराम तक की आवाज़ों को लोग लता मंगेशकर के खाते में डालते रहे। यही नहीं, जो आवाजें बड़ी आसानी से लता और आशा से अलग पहचानी जा सकती थीं, उन पर भी कई बार इन दोनों कलाकारों की कीर्ति का परदा पड़ा रहा। शमशाद बेगम और गीता दत्त जैसी निहायत अलग और निजी पहचान वाली आवाज़ों को भी इसका ख़मियाजा भुगतना पड़ा।
शायद इसी का नतीजा है कि ढेर सारे कर्णप्रिय और लोकप्रिय गीत गाने के बावजूद शमशाद बेगम का नाम बहुत सारे लोगों को अपरिचित या बहुत पुराना जान पडता है। 23 अप्रैल को उनके निधन के बाद जब लोगों ने ‘सीआइडी’ से लेकर ‘आरपार’और ‘क़िस्मत’ तक के खनकते-खिलखिलाते गीत सुने, तब उन्हें याद आया कि इस आवाज़ की खुशबू और खनक अपना अलग संसार रचती-बसाती है, उसे लता मंगेशकर और आशा भोसले की गायकी से काफी अलग खड़ा करती है।
कायदे से देखें तो शमशाद बेगम एक पुराने पुल का नाम है– नूरजहां और लता मंगेशकर के बीच की वह कड़ी, जहां खनक और माधुर्य के बीच, इठलाने और मनुहार के बीच, एक बारीक रेखा होती है। यह उदात्त धीर-गंभीर, उदासी के आंगन में टहलती हुई, विरह के गीत गाती हुई. चांद को पुकारती हुई, आत्मलीन नायिका की आवाज़ नहीं है, वह पूरे माहौल को ज़िंदा कर देने वाली एक ध़डकती-फडकती आवाज़ है- उस अल्हड़, ग्रामगंधी बाला की आवाज़, जो अपनी तुर्श-तिरछी कमनीयता में निमंत्रण भी देती थी और चुनौती भी। ‘बूझ मेरा क्या नाम रे’ या ‘गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हांक रे’ जैसे गीतों में शमशाद बेगम की आवाज़ में जैसे पूरा गांव बसा दिखाई पड़ता है, पूरी पगडंडी खुलती नज़र आती है।
गायकी के जानकार बताएंगे कि शमशाद बेगम की तरह खुले गले से गाने वाली गायिकाएं कम हुईं। कहते हैं, उन्होंने बहुत छुटपन से गाना शुरू कर दिया था और उन्हें माइक की ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन माइक के सामने आ जाने के बाद वे दूर से भी गाती थीं तो आवाज जैसे सप्तकों के पार जाकर सीधे अपने लक्ष्य तक पहुंचती थी।
कई मायनों में यह बराबरी और आज़ादी की मांग करती आवाज़ थी- ऐसी आवाज़ जो समर्पित नायिकाओं नहीं, विद्रोही प्रतिनायिकाओं को माकूल पड़ती है। वह नायक पर रीझी हुई, उसे मनाती हुई, उसमें डूबी हुई आवाज़ नहीं थी, उसके बिल्कुल बराबरी पर खड़ी, उससे मोहब्बत का इसरार करती, उसे छेड़ती आवाज़ थी। वह एक तरह से नायिका को भी अपने खोल से बाहर आने को मजबूर करती आवाज़ थी। फिल्म ‘मुगले आज़म’ की मशहूर कव्वाली ‘तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे’ में वह अनारकली के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा महत्त्वाकांक्षी और स्वतंत्र बहार की आवाज़ है जो सलीम को मोहब्बत की चुनौती देती है।
इस आवाज का सबसे शोख और अल्हड़ रंग खुलता है फिल्म ‘किस्मत’ के गीत ‘कजरा मोहब्बत वाला’ में, जिसमें आशा भोसले और शमशाद बेगम की जुगलबंदी जैसे दुनिया जीत लेती है।
यह सच है कि फिल्मी गायकी के उस सुनहरे दौर ने हमें ढेर सारी नायाब आवाज़ें दीं। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि उस गायकी के वसंतकाल में सबसे खिले हुए फूल का नाम शमशाद बेगम था। जिस गायकी की धूप बाद में लता और आशा की आवाज़ में अपनी पूरी चमचमाहट के साथ हर तरफ़ खिलती दिखी, उसका उषा काल शमशाद बेगम की आवाज़ में बसता है।
एक दौर ऐसा भी रहा कि शमशाद बेगम की आवाज़ जिसे छू देती थी वह सोना हो जाता था। कहते हैं, साहिर लुधियानवी और मजरूह सुल्तानपुरी के पहले कामयाब गीत शमशाद बेगम ने ही गाए। राज कपूर ने जब पहली फिल्म ‘आग’ बनाई तो शमशाद बेगम की आवाज़ का इस्तेमाल किया।
साठ के दशक के बाद शमशाद बेगम ने अचानक जैसे गाना छोड़ दिया। उनके बहुत क़रीबी लोगों को ही ये अंदाजा होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। यह बात कुछ इसलिए हैरान करती है कि उनका शुरू करना उनके छोड़ने से ज्यादा मुश्किल था। वे एक पाबंदियों वाले परिवार से आई थीं जहां पिता को भी बेटी का खुले में गाना नागवार गुज़रता था। तब उन्होंने सबको मना और समझा लिया, अपने लिए एक सरहद भी खींच ली कि सिर्फ गीत गाएंगी, सामने नहीं आएंगी। लेकिन जब वे अपने शोहरत के चरम पर थीं तभी अचानक जैसे वे मंच से उठकर नेपथ्य में चली गईं। अब यह बताने वाला कोई नहीं बचा है कि उनकी ज़िंदगी में कौऩ सा ऐसा साज़ सहसा टूट गया था कि उन्होंने यह फ़ैसला किया।
बहरहाल, उनके गीत कभी पुराने नहीं पड़े। उनकी आवाज़ में पुरानी मिट्टी की खुशबू, पुराने घरों का सोंधापन बोलता था। उनकी गायकी के हुलास में पनघटों की खिलखिलाहट और त्योहारों के रंग थे। इस छूटते हुए संसार की बहुत मार्मिक निशानियां उनके गीतों में मिलती हैं। लेकिन शमशाद बेगम की आवाज़ में इस स्मृतिजीविता से भी बड़ी एक चीज़ है- एक दुर्लभ शोखी जो खुलेपन का अपना ही भाष्य रचती है।
यह अनायास नहीं है कि जिस दौर में गीतों में दैहिकता का ताप बढ़ रहा है, मांसलता के सौंदर्य को बहुत सपाट और भोंडी प्रदर्शनप्रियता से विस्थापित किया जा रहा है, तब शमशाद बेगम के उन गीतों के रीमिक्स बन रहे हैं जिनकी दुर्लभ शोखी में तन से ज़्यादा मन विहंसता दिखता है। शमशाद बेगम का जाना और उनका गाना दोनों याद दिला रहे हैं कि हमारे संगीत में शोर और सतहीपन दोनों बढ़े हैं, पांव रोक लेने वाली और मन को बांध सकने वाली धुनें और आवाज़ें अब नहीं बची हैं।