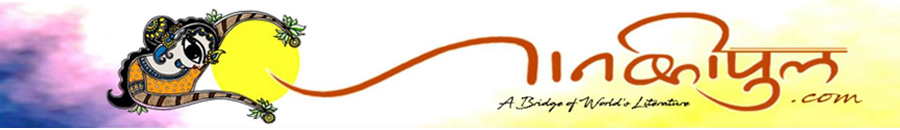इतिहासकार रविकांत सीएसडीएस में एसोसिएट फेलो हैं, ‘हिंदी पब्लिक स्फेयर’ का एक जाना-माना नाम जो एक-सी महारत से इतिहास, साहित्य, सिनेमा के विषयों पर लिखते-बोलते रहे हैं. उनका यह लेख प्रसिद्ध फिल्म-पत्रिका ‘माधुरी’ पर पर एकाग्र है, लेकिन उस पत्रिका के बहाने यह लेख सिनेमा के उस दौर को जिंदा कर देता है जब सिनेमा का कला की तरह समझा-बरता जाता था, महज बाज़ार के उत्पाद की तरह नहीं और सिनेमा की पत्रकारिता कुछ मूल्यों, कुछ मानकों के लिए की की जाती थी. ‘लोकमत समाचार’ के दीवाली विशेषांक, २०११ में जब यह लेख पढ़ा तो रविकांत जी से जानकी पुल की ओर से आग्रह किया और उन्होंने कृपापूर्वक यह लेख जानकी पुल के लिए दिया. जानकी पुल की ओर से उनका आभार. जानकी पुल के लिहाज़ से यह लेख थोड़ा लंबा है, लेकिन यादगार और संग्रहणीय. जो सिनेमा के रसिक हैं उनके लिए भी, शोधार्थियों के लिए तो है ही- जानकी पुल.
बहुतेरे लोगों को याद होगा कि टाइम्स ऑफ़ इंडिया समूह की फ़िल्म पत्रिका माधुरी हिन्दी में निकलने वाली अपने क़िस्म की अनूठी लोकप्रिय पत्रिका थी, जिसने इतना लंबा और स्वस्थ जीवन जिया। पिछली सदी के सातवें दशक के मध्य में अरविंद कुमार के संपादन में सुचित्रा नाम से बंबई से शुरू हुई इस पत्रिका के कई नामकरण हुए, वक़्त के साथ संपादक भी बदले, तेवर–कलेवर, रूप–रंग, साज–सज्जा, मियाद व सामग्री बदली तो लेखक–पाठक भी बदले, और जब नवें दशक में इसका छपना बंद हुआ तो एक पूरा युग बदल चुका था।[1]इसका मुकम्मल सफ़रनामा लिखने के लिए तो एक भरी–पूरी किताब की दरकार होगी, लिहाजा इस लेख में मैं सिर्फ़ अरविंद कुमार जी के संपादन में निकली माधुरी तक महदूद रहकर चंद मोटी–मोटी बातें ही कह पाऊँगा। यूँ भी उसके अपने इतिहास में यही दौर सबसे रचनात्मक और संपन्न साबित होता है।
माधुरी से तीसेक साल पहले से ही हिन्दी में कई फ़िल्मी पत्रिकाएँ निकल कर बंद हो चुकी थीं, कुछ की आधी–अधूरी फ़ाइलें अब भी पुस्तकालयों में मिल जाती हैं, जैसे, रंगभूमि, चित्रपट, मनोरंजनआदि। ये जानना भी दिलचस्प है कि हिन्दी की साहित्यिक मुख्यधारा की पत्रिकाओं – मसलन, सुधा, सरस्वती, चाँद, माधुरी – में भी जब–तब सिनेमा पर गंभीर बहस–मुबाहिसे, या, चूँकि चीज़ नई थी, बोलती फ़िल्मों के आने के बाद व्यापक स्तर पर लोकप्रिय हुआ ही चाहती थी, तो सिनेकला के विभिन्न आयामों से ता‘रुफ़ कराने वाले लेख भी छपा करते थे। फ़िल्म माध्यम की अपनी नैतिकता से लेकर इसमें महिलाओं और साहित्यकारों के काम करने के औचित्य, उसकी ज़रूरत, भाषा व विषय–वस्तु, नाटक/पारसी रंगकर्म/साहित्य से इसके संबंध से लेकर विश्व–सिनेमा से भारतीय सिनेमा की तुलना, सेंसरशिप, पौराणिकता, श्लीलता–अश्लीलता, सार्थकता/अनर्थकता/सोद्देश्यता आदि नानाविध विषयों पर जानकार लेखकों ने क़लम चलाई।[2]इनमें से कुछ शुद्ध साहित्यकार थे, पर ज़्यादातर फ़िल्मी दुनिया से किसी न किसी रूप से जुड़े लेखक ही थे। इन लेखों से हमें पता चलता है कि पहले भले हिंदू घरों की औरतों का फ़िल्मी नायिका बनना ठीक नहीं समझा जाता था, वैसे ही जैसे कि उनका नाटक करना या रेडियो पर गाना अपवादस्वरूप ही हो पाता था। पौराणिक–ऐतिहासिक भूमिकाएँ करने वाली मिस सुलोचना, मिस माधुरी आदि वस्तुत: ईसाई महिलाएँ थीं, जिन्होंने बड़े दर्शकवर्ग से तादात्म्य बिठाने के लिए अपने नाम बदल लिए थे। पारसी थिएटर का सूरज डूबने लगा था, ऐसी स्थिति में रेडियो या सिनेमा के लिए गानेवालियाँ ‘बाई‘ या ‘जान‘ के प्रत्यय लगाने वाली ही हुआ करती थीं। पुराने ग्रामोफोन रिकॉर्डों पर भी आपको वही नाम ज़्यादातर मिलेंगे। अगर आपने अमृतलाल नागर की बेहतरीन शोधपुस्तक ये कोठेवालियाँ[3]पढ़ी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। हिन्दी लेखकों ने ज़्यादा अनुभवी नारायण प्रसाद ‘बेताब‘ या राधेश्याम कथावाचक या फिर बलभद्र नारायण ‘पढ़ीस‘ की इल्तिजा पर ग़ौर न करते हुए[4]प्रेमचंद जैसे लेखकों के मुख़्तसर तजुर्बे पर ज़्यादा ध्यान दिया, जो कि हक़ीक़तन कड़वा था। उन्होंने आम तौर पर फ़िल्मी दुनिया को भ्रष्ट पूंजीपतियों की अनैतिक अय्याशी का अड्डा माना, माध्यम को संस्कार बिगाड़ने वाला ‘कुवासना गृह‘ समझा, उसे छापे की दुनिया में होने वाले घाटे की भरपाई करके वापस वहीं लौट आने के लिए थोड़े समय के लिए जाने वाली जगह समझा। पर पूरी तरह चैन भी नहीं कि उर्दू वालों ने एक पूरा इलाक़ा क़ब्ज़िया रखा है। हिन्दी और उर्दू के साहित्यिक जनपद के बुनियादी फ़िल्मी रवैये में अगर फ़र्क़ देखना चाहते हैं तो मंटो को पढ़ें, फिर उपेन्द्रनाथ अश्क और भगवतीचरण वर्मा के सिनेमाई संस्मरण, रेखाचित्र या उपन्यास पढ़ें।[5]भाषा के सवाल पर गांधी जी से भी दो–दो हाथ कर लेने वाले हिन्दी के पैरोकार, अपवादों को छोड़ दें तो, अपने सिनेमा–प्रेम के मामले में काफ़ी समय तक गांधीवादी ही रहे।
बेशक स्थिति धीरे–धीरे बदल रही थी, पर 1964 में जब माधुरी निकली तब तक इसके संस्थापक संपादक के अपने अल्फ़ाज़ में “सिनेमा देखना हमारे यहाँ क़ुफ़्र समझा जाता था।” उन्होंने इस क़ुफ़्र सांस्कृतिक कर्म को हिन्दी जनपद में पारिवारिक–समाजिक स्वीकृति दिलाने में अहम ऐतिहासिक भूमिका अदा की। माधुरी ने कई बड़े–छोटे पुल बनाए, जिसने सिनेमा जगत और जनता को तो आपस में जोड़ा ही, सिनेमा को साहित्य और राजनीतिक गलियारों से, विश्व–सिनेमा को भारतीय सिनेमा से, हिन्दी सिनेमा को अहिन्दी सिनेमा से, और सिनेमा जगत के अंदर के विभिन्न अवयवों को भी आपस में जोड़ा। पत्रिका की टीम छोटी–सी थी, और इतनी बड़ी तादाद में बन रही फ़िल्मों की समीक्षा, उनके बनने की कहानियों, फ़िल्म समाचारों, गीत–संगीत की स्थिति, इन सबको अपनी ज़द में समेट लेना सिर्फ़ माधुरी की अपनी टीम के ज़रिए संभव नहीं था। अपनी लगातार बढ़ती पाठक संख्या का रुझान भाँपते हुए, उसके सुझावों से बराबर इशारे लेते हुए माधुरी ने उनसे सक्रिय योगदान की अपेक्षा की और उसके पाठकों ने उसे निराश नहीं किया। प्रकाशन के तीसरे साल में प्रवेश करने पर छपा यह संपादकीय इस संवाद के बारे में बहुत कुछ कहता है:
हिन्दी में सिनेपत्रकारिता सभ्य, संभ्रांत और सुशिक्षित परिवारों द्वारा उपेक्षित रही है। सिनेमा को ही अभी तक हमारे परिवारों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है। फ़िल्में देखना बड़े–बूढ़े उच्छृंखलता की निशानी मानते हैं। कुछ फ़िल्मकारों ने अपनी फ़िल्मों के सस्तेपन से इस धारणा की पुष्टि की है। ऐसी हालत में फ़िल्म पत्रिका का परिवारों में स्वागत होना कठिन ही था।
सिनेमा आधुनिक युग का सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक मनोरंजन बन गया है। अत: इससे दूर भागकर समाज का कोई भला नहीं किया जा सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम इसमें गहरी रुचि लेकर इसे सुधारें, अपने विकासशील राष्ट्र के लायक़ बनाएँ। नवयुवक वर्ग में सिनेमा की एक नयी समझ उन्हें स्वस्थ मनोरंजन का स्वागत करने की स्थिति में ला सकती है। इसके लिए जिम्मेदार फ़िल्मी पत्र–पत्रिकाओं की आवश्यकता स्पष्ट है। मैं कोशिश कर रही हूँ फ़िल्मों के बारे में सही तरह की जानकारी देकर मैं यह काम कर सकूँ। परिवारों में मेरा जो स्वागत हुआ है उसको देख कर मैं आश्वस्त हूँ कि मैं सही रास्ते पर हूँ। आत्मनिवेदन: (11 फ़रवरी, 1966).
इस आत्मनिवेदन को हम पारंपरिक उच्च–भ्रू संदर्भ की आलोचना के साथ–साथ पत्रिका के घोषणा–पत्र और इसकी अपनी आकांक्षाओं के दस्तावेज़ के रूप में पढ़ सकते हैं। पत्रिका गुज़रे ज़माने के पूर्वग्रहों से जूझती हुई नयी पीढ़ी से मुख़ातिब है, सिनेमा जैसा है, उसे वैसा ही क़ुबूल करने के पक्ष में नहीं, उसे ‘विकासशील राष्ट्र के लायक़‘ बनाने में अपनी सचेत जिम्मेदारी मानते हुए पारिवारिक तौर पर लोकप्रिय होना चाहती है। कहना होगा कि पत्रिका ने घोर आत्मसंयम का परिचय देते हुए पारिवारिकता का धर्म बख़ूबी निभाया, लेकिन साथ ही ‘करणीय–अकरणीय‘ की पारिभाषिक हदों को भी आहिस्ता–आहिस्ता सरकाने की चतुर कोशिशें भी करती रही। भले ही इस मामले में यह अपने भगिनी प्रकाशन ‘फ़िल्मफ़ेयर‘-जैसी ‘उच्छृंखल‘ कम से कम समीक्षा–काल में तो नहीं ही बन पाई। बक़ौल अरविंद कुमार, जब पत्रिका की तैयारी चल रही थी, तो सुचित्राकी पहली प्रतियाँ सिनेजगत के कई बुज़ुर्गों को दिखाई गईं। उनमें से वी शांताराम की टिप्पणी थी कि इस पर फ़िल्मफ़ेयर का बहुत असर है। यह बात अरविंद जी को लग गई गई, और उन्हें ढाढ़स भी मिला। लिहाज़ा, माधुरी ने अपना अलग हिन्दीमय रास्ता अख़्तियार किया, और मालिकों ने भी इसे पर्याप्त आज़ादी दी। अनेक मनभावन सफ़ेद स्याह, और कुछ रंगीन चित्रों और लोकार्षक स्तंभों से सज्जित माधुरी जल्द ही संख्या में विस्तार पाते बड़े–छोटे शहरों के हिन्दी–भाषी मध्यवर्ग की अनिवार्य पत्रिका बन गई, जिसमें इसके शाफ़–शफ़्फ़ाफ़ और मेहनतपसंद संपादन – मसलन, प्रूफ़ की बहुत कम ग़लतियाँ होना – का भी हाथ रहा ही होगा। यहाँ ‘मध्यवर्ग की पत्रिका‘ का लेबल चस्पाँ करते हुए हमें उन चाय और नाई की दुकानों को नहीं भूलना चाहिए, जहाँ पत्रिका को व्यापकतर जन समुदाय द्वारा पढ़ा–देखा–पलटा–सुना जाता होगा। अभाव से प्रेरित ही सही, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामोफोन से लेकर सिनेमा–रेडियो–टीवी, पब्लिक फोन, और इंटरनेट(सायबर कैफ़े, ई–चौपाल) तक के आम अड्डों में सामूहिक श्रवण–वाचन–दर्शन–विचरण का तगड़ा रिवाज रहा है। संगीत रसास्वादन वॉकमैन और मोबाइल युग में आकर ही निजी होने लगा है। तो इस वृहत्तर पाठक–वर्ग तक फ़िल्म जैसे माध्यम को संप्रेषित करने के लिए माक़ूल शब्दावली जुटाने में मौजूदा शब्दों में नये अर्थ भरने से लेकर नये शब्दों की ईजाद तक की चुनौती संपादकों और लेखकों ने उठाई लेकिन अपरिचित को जाने–पहचाने शब्दों और साहित्यिक चाशनी में लपेट कर कुछ यूँ परोसा कि पाठकों ने कभी भाषायी बदहज़मी की शिकायत नहीं की। शब्दों से खेलने की इस शग़ल को गंभीरता से लेते हुए अरविंद जी ने अगर आगे चलकर शब्दकोश–निर्माण में अपना जीवन झोंक दिया तो किमाश्चर्यम, कि यह काम भी क्या ख़ूब किया![6]
सिने–जनमत सर्वेक्षण
बहरहाल, पूछने लायक़ बात है कि माधुरी के लिए सिनेमा के मायने क्या थे। ऊपर के इशारे में ही जवाब था – विशद–विस्तृत। पत्रिका ने न केवल दुनिया–भर में बन रहे महत्वपूर्ण चित्रों या चित्रनिर्माण की कलात्मक–व्यावसायिक प्रवृत्तियों पर अपनी नज़र रखी, बल्कि कैसे बनते थे/बन रहे हैं, इनका भी गाहे–बगाहे आकलन पेश किया, ताकि फ़िल्मी दुनिया में आने की ख़्वाहिश रखने वाले – लेखक, निर्देशक, अभिनेता, गायक – ज़रूरी हथियारों से लैस आएँ, या जो नहीं भी आएँ, वे जादुई रुपहले पर्दे के पीछे के रहस्य को थोड़ा बेहतर समझ पाएँ। इस लिहाज से ये ग़ौरतलब है कि माधुरी ने अपने पन्नों में सिर्फ़ अभिनेता–अभिनेताओं को जगह नहीं दी, बल्कि तकनीकी कलाकारों – छायाकारों, ध्वनि–मुद्रकों और ‘एक्स्ट्राज़‘ को भी, ठीक वैसे ही जैसे कि महमूद जैसे ‘हास्य‘-अभिनेताओं को आवरण पर डालकर, या फ़िल्म और टेलीविज़न इंस्टीट्यूट, पुणे से उत्तीर्ण नावागंतुकों की उपलब्धियों को समारोहपूर्वक छापकर अपनी जनवादप्रियता का पता दिया। उनकी कार्य–पद्धति समझाकर, उनकी मुश्किलों, मिहनत को रेखांकित करते हुए उनकी मानवीयता की स्थापना कर सिनेमा उद्योग के इर्द–गिर्द जो नैतिक ग्रहण ज़माने से लगा हुआ था, उसको काटने में मदद की।
इस सिलससिले में घुमंतू परिचर्चाओं की दो शृंखलाएँ मार्के की हैं: पहली, जब माधुरी ने मुंबई महानगरी से निकलकर अपना रुख़ राज्यों की राजधानियों और उनसे भी छोटे शहरों की ओर किया ये टटोलने के लिए कि वहाँ के बाशिंदे बन रही फ़िल्मों से कितने मुतमइन हैं, उन्हें उनमें और क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, आदि–आदि। जवाब में मध्यवर्गीय समाज के वाक्पटु नुमाइंदों ने अक्सरहाँ फ़िल्मों की यथास्थिति से असंतोष जताया, अश्लीलता और फ़ॉर्मूलेबाज़ी की भर्त्सना की, सिनेमा के साहित्योन्मुख होने की वकालत की। इन सर्वेक्षणों के आयोजन में ज़ाहिर है कि माधुरी का अपना सुधारवादी एजेंडा था, लेकिन इनसे हमें उस समय के फ़िल्म–प्रेमियों की अपेक्षाओं का भी पता मिलता है। हमारे पास उनकी आलोचनाओं को सिरे से ख़ारिज करने के लिए फ़िलहाल ज़रूरी सुबूत नहीं हैं, लेकिन ये सोचने का मन करता है कि इन पिटी–पिटाई, और एक हद तक अतिरेकी प्रतिक्रियाओं में उस ढोंगी, उपदेशात्मक सार्वजनिक मुखौटे की भी झलक मिलती है, जो अक्सरहाँ जनता के सामने आते ही लोग ओढ़ लिया करते हैं, भले ही सिनेमा द्वारा परोसे गए मनोरंजन का उन्होंने भरपूर रस लिया हो। मामला जो भी हो, माधुरी ने अपने पाठकों को भी यदा–कदा टोकना ज़रूरी समझा : मसलन, फ़िल्मों में अश्लीलता को लेकर हरीश तिवारी ने जनमत से बाक़ायदा जिरह की और उसे उचित ठहराया।
View 12 Comments