समकालीन हिन्दी कवियों में सपना भट्ट की कविताएँ बहुत पसंद की जाती हैं। उनकी गहरी संवेदनात्मक कविताओं में भाषा जैसे जीवंत हो उठती है। आज उनकी कुछ चुनी हुई कविताएँ जो इधर-उधर पत्रिकाओं से ली गई हैं- मॉडरेटर
=========================================
1
देजा वू
———–
किसी कौतुक के
संभावित पूर्व संकेत पर
स्मृति भ्रम का दृश्य गिरता है
सुधियाँ व्याकुल हो उठती हैं
मन स्थगन की चौखट पर बैठ जाता है
विगत किसी अर्थकोश में ढूंढे नहीं मिलता वह हेतु
जो ठीक ठीक बता सके
घटनाओं के पुनरावर्तन के विभ्रम का विज्ञान
आँख सब नया देखती है;
मन किन्तु नवेली संज्ञाओं को ध्वस्त करता हुआ
प्राचीन अनुस्मरण में प्रवेश करता है
जैसे यहीं इसी ऋतु में
चीड़ के इसी वृक्ष के नीचे
गले लग कर रोते रहे हों पहले भी
क्षीण ध्वनि की
इसी विवश आवृति की टेक पर
रुंधे कंठ से पुकारा हो पहले भी किसी को इसी तरह
जैसे इसी नभ के अछोर चँदोवे तले
हठीले मन को समझाया हो
कि तीव्र वेदना हो या कि अदम्य इच्छा,
कुछ भी समाप्त हो सकता है
उपसंहार के शिल्प में कभी भी
आत्मविस्मृत होकर
लौट भी आऊँ अपने ध्यानावस्थित घेरे में
मनोरोग की तरह, अर्थहीन कल्पनाएँ सर उठाती हैं
रात के तीसरे पहर
प्रणय के पर्याय विहँसते हैं
देह अंतरंग प्रतीकात्मकता में लजाती है
उसका स्पर्श देह में बार बार लौटता है
अब जबकि वह कहीं नहीं है
हिय के मन्द्र रागालाप में
एक उदास रुआँसी धुन बजती रहती है
विवेक छल करता है
भाषा भूल जाती हूँ….
========
2
आश्चर्य की वर्तनी में छुओ मुझे
देह से देह विलग हो
तो भी कामना जुड़ी रहे
ज्यों कोई सलोना सयुंक्ताक्षर
हर नवेली कोशिका को
फिर फिर नष्ट होने का अवकाश दो
प्रत्याशा के पूर्वाभ्यास में अभी
अभी इस निशा की निर्विकल्प द्युति में
कांपने दो श्वास का मालकौंस अनवरत
अभी हीरे से विषाक्त
और तीखे हथियार में बदलने दो अपनी चुप्पी
अभी याद को यातना में ढलने दो
अभी मैं नहीं जानती
प्रतीक्षा के अतिरिक्त कोई शास्त्र
अभी मैं अनुपस्थित हूँ
अपनी ही एन्द्रिक एषणाओं के खंडित स्वप्नफल में
अभी व्याकुलता की तटस्थ लाज गलने दो
आज की रैन
पश्चाताप के लिए भी
एक कातर तर्क हो;
छोड़ कर
जाने के लिए भी गढ़ो
पुनरुक्ति दोष सा एक लघु शिल्प आज की रैन
बस आज भर के लिए
कविता को इस ताप से मुक्त करो
मुझे अपने आदिम अंधेरे में उतरने दो ….
==================
3
कविता में मृदु सहवास हो
कि गद्य में कटु वैमत्य
अहर्निश कुछ नहीं रहता जीवन में
जैसे शेष नहीं रहती
कोई यंत्रणा देह के शोकागार में
कोई स्फुरण नाड़ी में देर तक नहीं टिकता
अनिष्ट घेरते तो हैं, भय अकुलाते तो हैं
किन्तु अधैर्य का क्लेश
अधिक दिवस हृदय में अतिथि नहीं रहता
सदा न रूप रहता है न लावण्य
सुमुखी कहते थे जो प्रियजन मुझे,
आज श्वेत केशों से भेद लेते हैं पराजय के वृतांत
पीड़ाओं की अनुक्रियाएँ,
कत्थई रक्त बहता है पाँच दिवस जिन दिनों
गात के सबसे अंधेरे प्रतीकों से झरता है नैराश्य
खिन्नता किन्तु छठे दिन शेष नहीं रहती
स्नानघर के दर्पण में
चिपकाई हुई मेरी बिंदियाँ भी
गिरती रहती हैं एक एक कर चीड़ के पिरूल की तरह;
सिंगार धूल में मिल रहता है
सबसे प्रेमिल स्पर्श भी नष्ट हो जाते हैं
वह सबसे कोमल संसर्ग
जो नाभि में क्षण भर को ठिठकता है
वह भी लोटे भर जल से बह जाता है उपत्यकाओं में
विवेक भी कहाँ सदा रहता है !
मनोरोग की तरह वह भी सांकेतिक भाषा मे सर उठाता है
तुम्हारे स्वरों के आभ्यंतरिक अंतर्वस्त्र पहने
आत्मीय मृतकों और पूर्वजों से
मोक्ष की दुर्बोध युक्तियाँ पूछती हूँ
किसी दिशा से कोई उत्तर नहीं आता
एक ठंडी उसाँस भरकर
निकट के एक शवदाह गृह में
अपनी सारी प्रेम कविताएँ छोड़ आती हूँ
इतने विपुल संसार में
प्यार का एक शब्द नहीं बचता
आत्मा के सीले अंधेरे में राख गिरती रहती है …
==============
4
यह जो स्मृतियों की
छाया से ढका निर्वात है पुरातन
आत्मा के इसी प्राचीन शून्यागार में
उसकी आवाज़ की उष्ण आवृत्तियाँ गूँजती थी
यही बोधि थी, यही प्रज्ञा
इन्ही अंतरंग आरोह अवरोहों के भरोसे थे संकेत
इसी भाषा पर ठिठकता था मेरे कानों का अबोध एकांत
इसी आवाज़ की तरंग पर चेतना भंग होती थी
मुझे कहां कुछ सूझता था ?
सिवाय इसके कि दुख हो या प्यार
उसकी ही आवाज़ में ढूंढता है कोई मुझे
इस अकुंठ वीतराग में भी
कोई पुकारता है मेरा नाम उसी की ध्वनि का सहारा ले
उसकी ही अर्वाचीन भंगिमाओं का चोला पहन
ध्यान के इस गह्वर में
मैं उसी की आवाज़ को टटोल कर आगे बढ़ रही हूँ भंते !
तुम्ही ने सिखाया था न
अनित्य है संसार, मिथ्या है जगत का मोह !
तब किस एषणा का धर्मबीज
मेरी क्लान्त छाती में खुबकर बंजर हो जाता है
मुक्ति की बात क्या कहूँ भंते !
मैं ठहरी विरह के बाण से बिंधी स्त्री
मौन समाधि में नेत्र मूँदे युगों तक बैठी ही रहूं तब भी
बैराग जगेगा ही नहीं, मोह छूटेगा ही नहीं
न ! मैं शील नहीं जानती
धम्म भी नहीं;
मैं तो बस यह जानती हूं कि
जिस देह के हर अणु को
प्रणय की प्रबल आदिम प्यास जलाती है
प्रेय को शिशु सा अंक में भर लेने की करुणा भी
उसी देहफूल से उपजती है
झर जाती है …..
==========
5
तीव्र ज्वर की नीम बेहोशी में रही
जितने दिन रही प्रेम में
शिराओं में
त्रिताल सा लयबद्ध बजता था
बस एक नाम अनथक
बहुत दिनों तक
एक ही स्वप्न से भरी रही आँखें
मन का मृग अपनी ही सुगंध के पीछे बौराता रहा
उस अचेतन में भी
नौकुचिया ताल के गहन जल में उगे
स्वर्ण पुष्प को छूने की लोर नहीं खींचती थी
वह तो तृष्णा थी जो मन और देह को छलती थी
जबकि अनन्त अभिनयों से
भरी रही देवताओं की पुतलियाँ
मन बहुत दिन भय के बहुलार्थों से मुक्त रहा
कितनी ऋतुएँ बीतीं
तुंगनाथ के हिम द्वार पर खड़े याचक सा
मेरा हृदय भूल गया समय और दिशाएँ
स्मृतियों के निर्जन द्वीप में
अकेला विहँसता रहा मन का शिशिर,
कितने दिन अपने ही निर्जन में भटकती रही
किंवदंतियों के अप्रचलित पुल से
यथार्थ तक पहुँचने का मानचित्र
अपनी नींद के भीतर जो रख कर भूल गयी थी
जितने दिन प्रेम में थी; पृथ्वी पर कहीं न थी
मुझे क्या पता
इतने दिवस क्या हुआ संसार में!
=======================
6
वे पत्नियाँ नहीं, प्रेमिकाएँ थीं
‘दर्प’ अभिमानिनी पत्नियों पर शोभता था
जबकि अदिष्ट प्रेयसियों पर ‘शोक’
उनके अंतर्बोध और तर्कणाओं की पराजय के वृतांत
प्रेमियों ने अपनी गृहस्थी के अलिखित प्रारूपों में
अँगूठा लगवाकर सहेज लिए थे
वे पार्श्व की सहनायिकाएँ थी
नेपथ्यों की अस्फुट ध्वनियाँ भर;
उनके होने न होने से
नाट्यलीलाओं में अधिक अंतर न आता था
भ्रम उनके मस्तक पर गौरव सा छपा था
मध्यरात्रि के लज्जित सम्भोग का अपयश
उनकी देह के पानी को कुम्हलाता था
प्रातः सूर्य का शुक्ल तेज
उनके दुर्भाग्य को प्रकाशित कर देता था
स्थानीयता की भी
अपनी एक निरुपाय यातना होती है
कोई उत्सव हो कि शोक
भय उनकी ही एषणा की पराजित उपकथाएँ कहता था
पूर्वजों की छाया
उनकी अछूत देह की सँवलाई धूप न छूती थी
यौवन की लाज ब्रह्मांड की ओट से भी न छिपती थी
पवित्रता केवल
सद्य सुहागनों के ललाट का वैभव था
प्रेयसियाँ नैतिकता
और न्याय के कटघरे की रहवासी थीं
यह निहोनी काली ऋतु
इस पृथ्वी पर यूँ ही न चली आई थी
किसी दिन विकल होकर एक भले आदमी ने
एक अभागी औरत से
उसका काँपता हाथ अपने हाथों में लेकर कहा था
कि “मैं तुम से प्यार करता हूँ”।
दसों दिशाएँ हँस पड़ीं
अवांछित होने की बेला जो द्वार पर थी
अंतरिक्ष ने इस खंडित मृषा को पहले ढका
क्षिति पर यह अपगति उसके बाद आई ….
============
7
एक अंतिम बार
_____
कौन नहीं जानता !
कि इस श्रावणी धारासार वर्षा का दोष
धरा को नहीं देह को लगा करता है
वर्षा थमती ही नहीं
वस्त्र सूखते ही नहीं
कि सहसा निरक्त तलुओं का दाघ उचक कर मस्तक छू लेता है
इतनी तरल होती हैं आँखें
कि इंद्रधनुष नहीं दीखता
एक लघु सूर्य आठोंयाम गात में दुबका रहता है
कामनाओं का ताप चढ़ता जाता है
एक मद्धम चोट
मेरुदंड में समताल पर बजती है
शिराओं में पुलकित रक्त लजाता है
एक मीठी धूजन से चित्त डोलता रहता है
स्वप्न में तुम्हारे गर्वीले वक्ष पर
अपनी तर्जनी से मध्य पसरा
यह अलंघ्य अंतराल दर्ज़ करती हूं
न! अब मुक्ति न चाहिए किसी युक्ति से
जिव्हा पर चाह का संकोच कितना रखूँ !
अब केशों में श्वेत गन्धराज नहीं
चटख टेसू के फूल खोंसे आना चाहती हूँ तुम्हारे पास
फिर चाहे जन्मचक्र की स्थिर ग्रह मुद्राओं में
झिलमिलाता रहे दुर्भाग्य का दर्पण
श्मशान में धू धू जलती रहे चिता
कांपता रहे मोक्ष का जल पुत्र की अंजुरियों में
पुनर्जन्म की सच्ची झूठी मान्यताओं के भरोसे
छोड़ भी दूँ तुम्हे छूने की निषिद्ध चाह एक बार
किन्तु अंतिम बार
तुम्हे देखने की इच्छा कैसे छोड़ दूँ प्यार मेरे !
कौन जाने ?
गंगा पार भी पहुंचे न पहुँचे विदग्ध देह धूम्र
तुम तक पहुँचे न पहुँचे यह मर्मान्तक विकल पुकार…
=============================
8
रात्रि आत्मा के
जिस सीले अंधेरे में प्रेम का क्लेश था
विदग्ध काया की उसी एकांतिक भूमि पर
ठंडी सुनहरी भोर उतर रही है
कैसी निस्सीम शांति है!
श्वास के हर धागे में
जिसके नाम का मनका बंधा है न
एक दिन वह माला भी टूट जानी है
हर रसद की एक मियाद हुआ करती है
जैसे अपने ही रुधिर से कम हो जाएं श्वेत रक्त कणिकाएँ
मन से प्रीत छीजती रहती है धीरे धीरे चुपचाप
कभी पुराने सितार से भी ज़ख़्मी हो जाती हैं उंगलियाँ
अंधेरे पर भी उजाले का दाग़ लगता है
सौंदर्य के आधिक्य से भी
कुम्हलाता है आँख का पानी,
बहुत दुख से ही आत्मा खोखली नहीं होती
बहुत प्यार भी उम्र खा जाता है
कोई करवट बदलूँ
साथी दुःख मेरी ओर ही मुँह करके सोते हैं
आँख खुलते ही मुस्कुरा कर कहते हैं
कि “जैसे सदा नहीं रहती कोई स्मृति, कोई इच्छा,
कोई स्पर्श या देह गंध इस पार्थिव जगत में
प्रेम का यह दुःख भी न रहेगा”
जब कुछ नहीं सूझता
तब प्रेम कांधे पर हाथ नहीं धरता
दिलासा नहीं देता
यह तो मृत्यु की सदाशयता है
जो एक दिन कान में आकर धीमे से कहती है
कि उठो!
उसकी स्मृतियों की पोटली बाँध लो
पृथ्वी पर रोने का यह तुम्हारा अंतिम दिवस है
आओ मेरे साथ चलो …
==========
9
घाट पर विवस्त्र
चंपा कनेर का दोना लिए
किसे मांगती हो वैखरी की प्राचीन विधाओं में ?
तुम्हारी ही
व्यथित प्रज्ञा के अतिरिक्त
और कौन सुनता है तुम्हारी प्रार्थनाओं के पुनर्पाठ!
अतिरेकी आस्तिकता की तरह
प्यार की निर्विकल्प आस्था का भी
कहीं कोई उपचार नहीं !
देखती तो हो,
कुम्भ में नित छूट रहे हैं
मित्र,भाई बांधव और प्रेमी
तब दक्षिण दिशा में
किसके नैवेद्य का आग्रह रखती हो छिपाकर
कि सहसा उजागर हो जाता है मृत्युबोध;
जीते रहने की शाश्वत कामना क्षीण होती जाती है!
इच्छाएं एक कल्प से
दूसरे कल्प की यात्रा करके
थकी हुई मक्खी की तरह
आत्मा के बहते हुए घाव पर बैठ जाती हैं
कथाओं उपकथाओं में
अपने प्रिय खाद्य के लिए बरजते हैं पुरखे;
बीड़ी सुपारी और कच्ची शराब की गन्ध
देर तक साथ रहती है
जानती हो न,
सुख बीत जाता है
सुख वाली स्मृतियों की हिंसा नहीं बीतती
देह भी सदा नहीं रहती,
अंतिम जीवाश्म के नष्ट होने से पहले
माटी में मिल रहते हैं
रक्त अस्थि मज्जा और प्राण
एक अश्रु भी भूमि पर गिरता है
तो आश्वस्ति उमगती है;
कि इस पृथ्वी पर
हमेशा भरोसा किया जा सकता है
ओक भर जल के लिए
हिय भर करुणा के लिए …
==============






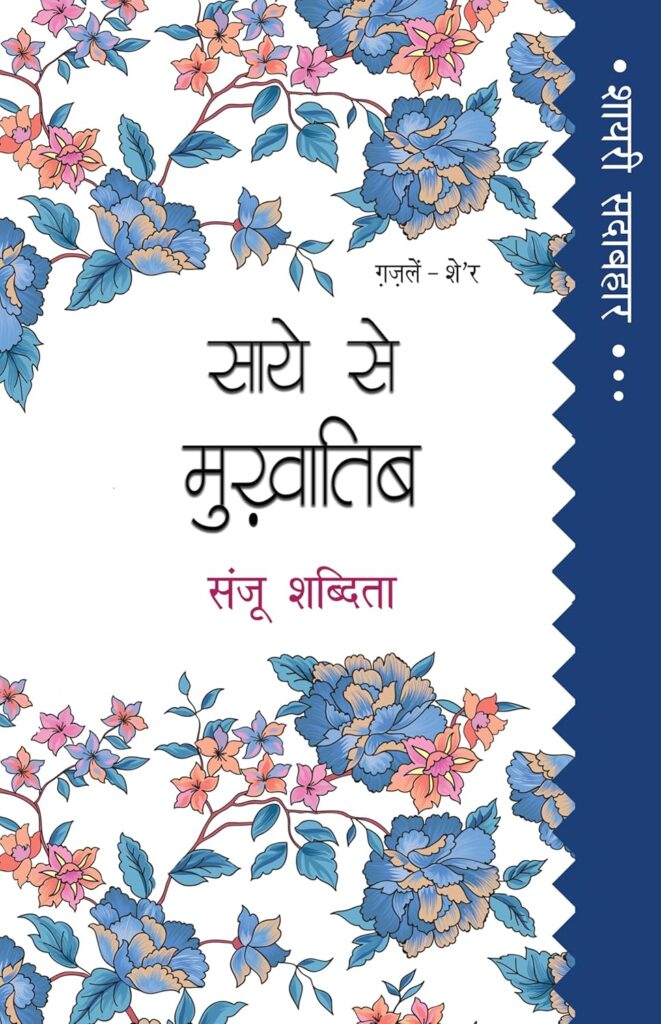
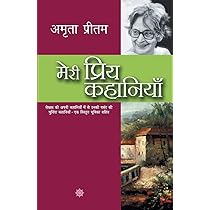

सुंदर चयन है। सभी मेरी प्रिय कविताएँ है, और सबकी पहले भी प्रशंसा कर चुका हूँ। जानकीपुल जैसे प्रतिष्ठित और गंभीर ब्लॉग पर इनको एक साथ देखना सुखद है। इन कविताओं पर अपनी टिप्पणियों के प्रति भी आश्वस्ति हुई। बधाई कवि! 🌻