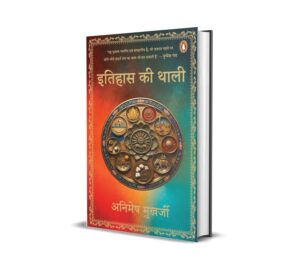मिथिलेश कुमार राय ग्रामीण जीवन को लेकर बहुत जीवंत लेखन करते हैं. उसकी राजनीति से अलग उसके जीवन को सहज रूप में देखने की कोशिश करते हैं. वे आजकल उपन्यास लिख रहे हैं ‘करिया कक्का की आत्मकथा’. उसी का एक अंश- मॉडरेटर
=======
‘काकी, कक्का हैं? जरा दरवाजे पर भेज दो.’
‘हैं कहाँ वे आँगन में.’
‘काहे, कहाँ गए इतने भोरे-भोर?’
‘का बताएं, बच्चू को कब से कह रहा था पम्प सेट के लिए. आज चार बजे जाकर लगाया खेत में. राजमा के पौधे पीले पड़ते जा रहे थे. उसी की सिंचाई में लगे हुए हैं.’
‘आज तो मौसम बहुते ख़राब है। इसी मौसम में उन्हें यह सब करना था.’
हाँ. आज दोपहर से पहले धूप क्या निकलेगी. लेकिन बच्चू को अगर आज ना कह देते तो अब पौधे मरणासन्न हो जाते. क्या करोगे. ऐसे ही चलती है. यह जिंदगी.’
‘हाँ. सो तो है. तुम कक्का को चाय पहुँचा दो. सर्दी बहुत है. उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी.’
‘हाँ. मैं भी खेत की तरफ ही निकल रही हूँ. लेकिन पहले इन बकरियों को कुछ चारा डाल दूँ. नहीं तो बेचारी मिमियाती रहेंगी.’
‘क्या खिलाओगी बकरियों को?’
‘पीछे से जलेबी का एक डंठल तोड़ लाती हूँ. उसी के पत्ते में लटकी रहेंगी.’
‘ओ.’
‘तुम सुनाओ. कैसे आये?’
‘आज इतवार है काकी. सोचा था कि इतनी सर्दी है तो कक्का बड़ा सा घूरा लगा के बैठे होंगे. मैं भी बैठ जाऊंगा. गप्पें करेंगे. तुम अदरक वाली चाय जरूर पिलाओगी.’
‘चाय पीना है तो क्षणिक बैठो. अभी बना देती हूँ.’
‘नहीं काकी. रहने दो. तू ना, बकरी को चारा डालकर कक्का को चाय पहुंचा दो. मैं फिर आ जाऊंगा. शाम को.’
‘जरूर आना. दोपहर तक सिंचाई का काम भी ख़त्म हो जायेगा. फिर तो कक्का घूरे के पास ही जमे रहेंगे.’
जरूर आऊंगा काकी.
—
बारह बजे के लगभग सूरज देव ने सबको दर्शन दिया था. लेकिन दो बजते न बजते पछिया ने जोर लगा दी तो फिर वे कुहासे की ओट में पता नहीं कहाँ छिप गए. अभी चार भी नहीं बजे थे और ऐसा लग रहा था कि रात होने वाली है. सर्दी के दिनों में जब भी इस तरह का खराब मौसम होता है, लोग अपने-अपने घरों में ही दुबके रहते हैं. लेकिन कक्का अब तक नहीं लौटे थे. खेत से. दरवाजे पर घूरा सुलग रहा था. सूखे गोबर, गोबर से बने उपले और बाँस की जड़ से जोड़ा गया यह घूरा आज पहले से ज्यादा मजबूत लग रहा था. नहीं तो काकी घूरे में उपले कहाँ देतीं हैं. कहती हैं कि उपले तो भोजन बनाने के लिए होता है. घूरे के लिए कक्का पहले ही सूखे गोबर और कटे बाँस की जगह से उसकी जड़ उखाड़ कर ढेर लगा देते हैं. सर्दी खत्म हो जाती है लेकिन घूरे की सामग्री खत्म नहीं होती.
काकी बकरियों को घर के अंदर ले जा रही थीं. फिर उन्होंने गाय की पीठ पर जूट से बने बोरे को सी कर बनाया गया झूल रख दिया.
‘कक्का अभी तक नहीं लौटे हैं?’
‘लौटने ही वाले हैं.’
‘बड़ी देर हो गई?’
‘अरे, आफत आती है तो दो चार आ जाती है.’
‘क्यों, क्या हुआ?’
‘मौसम को नहीं देख रहे!’
‘हाँ. सो तो है. बहुत बिगड़ा हुआ है.’
‘ऊपर से आधे खेत की सिंचाई भी नहीं हुई कि मशीन का डीजल खत्म हो गया.’
‘लेकिन डीजल तो किरतु के यहाँ मिलता है न?’
‘आज नहीं था. खत्म था. मशीन खेत से चला जाता तो फिर खींच के लाने में कितनी परेशानी होती है.’
‘तब?’
‘तब क्या. कक्का तुम्हारे छतरपुर गए. डीजल लाए. अब जाकर काम खत्म हुआ है. लो, आ गए.’
‘चाय बना दो.’
कक्का ट्यूबेल के पास चले गए.
‘अरे कक्का, पहले हाथ-पांव सेंक लो.’
‘आता हूं. आता हूँ. घूरे के पास ही आता हूँ. पहले देह पर एक बाल्टी पानी उढेल लूं.’
‘मैं कहती हूँ कि इस बखत स्नान करने का क्या तुक है. सिर्फ देह-हाथ पोंछ लो.’
‘हाँ कक्का, समय नहीं देख रहे.’
‘कुछ नहीं होगा.’
कक्का ने देह पर पानी उढेल ही लिया-हर-हर गंगे… हर-हर गंगे!
‘कभी किसी की सुने तब न!’
‘तू चाय बनाकर घूरे के पास लेती आ. शाम को भुनभुना मत. लक्ष्मी बुरा मान जाती है.’
‘काकी घूरे के पास पीढ़ा रख गई. कक्का जब लौटे, घूरा पूरा सुलग चुका था. इससे पहले उससे कुछ-कुछ धुआं निकल रहा था. जिस गोबर से धुआं निकल रहा था, अब वह सूख गया था और लुहार की भट्ठी की तरह अंगार की शक्ल में आ गया था.’
‘ठीक हो?’
‘हाँ कक्का.’
‘और बाल-बच्चा?’
‘सब ठीक है.’
‘सर्दी बढ़ गई है. सबको ध्यान से रहना पड़ेगा. नहीं तो यह दबोच लेती है.’
‘जैसे आप रहते हैं कक्का!’ मुझे हँसी आ गई.
‘अरे, यह जो देह है न, इसका सब पचाया हुआ है. अब के लोगों की बात दूसरी है. फिर हमारा क्या है. हम तो पके आम ठहरे. जब टपक जाएं. जिस विधि से टपक जाएं.’
काकी दो गिलास में चाय लेती आई. काकी के हाथ का चाय पीकर मजा आ जाता है. पता नहीं किस मात्रा में क्या मिलाती है कि स्वाद इतना दिव्य हो जाता है. फिर आज कल तो अदरक भी मिलाती है. आह! अदरक सर्दी के मौसम को कितना स्वादिष्ट बना देता है.
‘तू भी अपनी चाय यहीं ले आ.’
‘और चूल्हा-चौका कौन करेगा?’
‘अरे, सब हो जाएगा. हड़बड़-हड़बड़ में चूल्हा पर कुछ पकाएगी तो स्वाद बिगड़ जाएगा. ले आ. अपनी चाय यहीं ले आ. देख तो, घूरे की आग कितना सुख दे रही है. आह!’
‘काकी अपना गिलास ले आई.’
‘कहो तो, सर्दी के मौसम में हाथ में चाय का गिलास हो और आदमी घूरे के पास बैठा हो तो उसे कितना सुख मिलता है!’
‘हाँ कक्का, आप सच कहते हैं. कितना अच्छा लग रहा है.’
‘हाँ. घूरे की आँच जब देह में सर्दी के स्थान पर गर्मी रोपने लगती है न, मन आनंद से भर उठता है. इस पर तुम क्या कहती हो लक्ष्मी?’
‘जेठ की गर्मी में कभी चूल्हे के पास घंटा-दो घंटा बैठो तो सही बात पता चले.’
‘यह भी तुमने खूब कही.’
‘अच्छा बता. खाने में क्या बनाओगी?’
‘तुम कहो, क्या बना दूँ?’
‘ज्यादा ताम-झाम मत करना. रोटी बना लो और लहसून की चटनी. दूध तो है ही.’
‘ठीक है.’ काकी जूठे गिलास समेट कर निकल गईं.
‘लहसून की चटनी का स्वाद भी बड़ा दिव्य होता है कक्का.’
‘हाँ नहीं तो क्या. जाड़े का यह मौसम और लहसून की चटनी. आह! हमारे पूर्वजों ने कितने दिव्य स्वाद का उपहार दिए हैं हमें!’
‘काकी तो और जबरदस्त बनाती होंगी?’
‘हां। यह तो है. तेरी काकी के हाथों में कोई जादू है जैसे. बड़ी तन्मय हो कर खाना बनाती हैं. फिर लहसून की चटनी बनाना भी कोई बच्चों का खेल नहीं है.’
‘हाँ कक्का.’
‘लहसून और हरी मिर्च को आग में ठीक से भूनो. गर लहसून थोड़ा सा भी कच्चा रह गया तो वो स्वाद नहीं आ पाएगा. फिर उसमें सरसों का कच्चा तेल डालो. नमक और आम का अचार सही मात्रा में मिलाओ. फिर देखो स्वाद.’
‘बंद करो कक्का.’
‘काहे, मुँह में पानी आ गया!’
गाय चुप लेटी पगुरा रही थीं. कक्का के ठहाके से वह चौंक उठीं. मेरी भी खिलखिलाहट निकल गई. हम देर तक हँसते रहे.