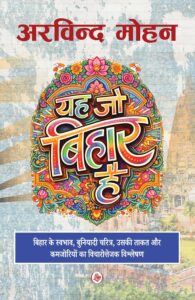फ़िल्म लापता लेडीज़ पर यह टिप्पणी लिखी है युवा लेखिका विमलेश शर्मा ने। आप भी पढ़ सकते हैं-
======================
भारतीय कथा-साहित्य में रवीन्द्रनाथ टैगोर से लेकर सत्यजीत रॉय तक के कथानकों-फिल्मांकन में नायिकाओं की अदला-बदली का उल्लेख है; परन्तु किरण रॉव लापता लेडिज में दुलहिनों की अदला-बदली का जो तार्किक-मार्मिक चित्रांकन करती हैं वह बेहद ख़ास है और यूँ किरण रॉव की सेल्यूलॉइड पर सादा-वापसी एक बार फिर दिल जीत लेती है। स्त्री मुद्दों पर बात बहुतेरे तरीकों और प्रसंगों से की जाती रही है परन्तु आमिर खान प्रोडक्शन और किरण राव के निर्देशन में ‘लापता लेडिज’ उसी ‘बात पुरानी को फिर-फिर नई’, के रंग में बख़ूबी प्रदर्शित करती है। स्त्री को सामान समझे जाने की जो पितृसत्ता की रणनीति है उसके तहत वह उसकी पहचान उसी से छिपा देती है, वो भी कुछ इस तरह की उसे यह बंदिश अजनबी-अटपटी ना लगकर भली-भली सी लगती है। पटकथा में फूल के संवाद इसी रणनीति की सच्चाई को ज़ाहिर करते हैं। यों कहानी भारत के किसी प्रदेश जिसे कहानी में निर्मल प्रदेश नाम दिया है की, वर्ष 2001 की है, परन्तु फिल्म देखने के बात गाँव से स्कूल-कॉलेज पढ़ने आती पर कोर्स पूरा न कर बीच में ही कहीं छूट जाती लड़कियाँ, बरबस याद आ जाती है और फिर लगता है कि इन 13 वर्षों में भी अर्थात् 2024 में भी समाज और हमारा भारत आख़िर कहाँ बदला है, या कि हम ही आख़िर कहाँ और कितना ख़ुद को बदल पाए हैं।
कहानी के प्रारम्भिक दृश्यों में ही फूल कुमारी की बोलती आँखें हैं जो यह जानने का प्रयास कर रही हैं कि आख़िर ख़ुशी के इन पलों में सब आँसू क्यों बहा रहे हैं, काहे माँ इतना रो रही है। उस विदाई में ही उसके पल्लू से पति की शुभेच्छाओं और मंगल हेतु खोइचा बाँध दिया जाता है, उसकी बोलती आँखों पर दाम्पत्य का मोटा परदा डाल दिया जाता है जैसे यह जताया जा रहा हो कि अब तुम्हें वही देखना है जो तुम्हारा जीवनसाथी तुम्हें दिखाए, उसी राह चलना है जिस पर वो तुम्हें लेकर चले और एक बार जो घूँघट ले लिया तो आगे नहीं नीचे देखकर चलना । अनगिन सीखों के साथ फूल सी दुलहिन मैंहदी के हाथ लेकर सैंया जी के साथ चल पड़ती है। वह अपने अबोध में यह मानकर इस सफर की शुरूआत करती है मानो उसका सातों जनम का टिकट इस साथ के साथ कट गया हो। ट्रेन की वह बोगी जिसमें तीन शादीशुदा जोड़े हैं के परिवार जन दहेज,सूट,जेवर और कपड़ों की तुलना इस तरह गौरवबोध के साथ करते हैं मानो यह रस्म करके उनका लाडला कोई लॉटरी जीत कर आया हो और इससे भी अधिक जैसे कि इन सब पर लड़के वालों का सनातन मालिकाना हक़ रहा हो। और जो तनिक भी कम-बेसी मिले या दहेज में कुछ ना ले-दे तो बड़ी आसानी से यह लोकापवाद भी फैलाने में यही समाज पीछे नहीं छूटता कि, “लड़के में ही कहीं कोन्हू खोट है।” समाज को प्रतिबिम्बित करती इसी बोगी में अख़बार में बोल्ड हर्फ़ो में छपी यह ख़बर भी है- ‘लुटेरी दुल्हन का शिकार बने फौजी-व्यापारी’, यह शीर्षक समाज की स्त्री-विषयक मानसिकता की कलई खोल कर रखता है जो यह बताती है कि, समाज आगन्तुक की कोमलता को प्रश्निल या शक़ की निगाहों से देखने का अभ्यस्त है। इसी बीच कहानी में क़ैद एक ज़िंदगी भुलावे में ही सही पर आज़ाद…कुछ आज़ाद हो जाती है। वह ज़िंदगी जो एक विवाह कर चुके प्रदीप के साथ ज़बरन ब्याह दी जाती है। प्रदीप जिस पर यह शक है कि उसकी पहली पत्नी को जला कर मारा गया है और अन्य तमाम दोषों से भी सम्पन्न है, दिशाहीन युवावर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। प्रदीप की ब्याहता जया को यह इल्म है कि वह दीपक कुमार की ब्याहता नहीं है परन्तु एक गफ़लत में वह दीपक के साथ चल देती है, क्योंकि ब्याह के बाद सिर्फ जूते देखने का रिवाज़ है राह या चेहरा देखने-दिखाने का नहीं, और जूता और पति तो दोनों नए हैं।
कहानी आद्युपान्त पर्दा-प्रथा पर तंज और व्यंग्य कसती नज़र आती है और यह व्यंग्य हर धर्म और वर्ग पर कसा हुआ दिखाई पड़ता है। अदला-बदली हुई जया भी पुष्पा ट्रेवल्स की बस से उतरने के बाद पुष्पा हो जाती है। जया के पुष्पा होने का सफ़र स्त्री-चेतना का डगमग सफ़र भी दिखाई देता है। पर इस चेतना में वे सीखें भी शामिल है जो जन्म से पाक और अन्य ललित कलाओं के साथ सिखाई जाती है कि ब्याह के बाद पति ही सर्वस्व होता है औऱ जो प्यार करता है वह मारने का हक़ भी रखता है। अदला-बदली हुई दोनों दुलहिनें फूल कुमारी और जया समाज से बहुत कुछ सीखती और सिखाती चलती हैं। यह अदला-बदली वैसी ही है जैसे किसी ने ग़लती से किसी दूसरे का सामान,जूता,साइकिल उठा लिया हो। आज भी लड़कियों की परवरिश पराए घर के सामान के रूप में की जा रही है, उस परवरिश में वह अपने नैहर और ससुराल का नाम तक जाने का इल्म नहीं अर्जित कर पाती है। वह परवरिश उसमें यह सोच नहीं विकसित कर पाती कि समाज उसे लड़कों के समान बराबरी का दर्ज़ा और अवसर आख़िर क्यों नहीं प्रदान करता है। पितृव्यवस्था ने स्त्रियों को इस क़दर क़ैद में रखा है कि अब उन्हें यह भी याद नहीं उन्हें किस चीज़ का शौक है और क्या उसकी पसंद-नापसंद। वह पिंजरे के बाहर और पिंजरे के भीतर, हर जगह समाज की थोपी हुई जड़ मान्यताओं में क़ैद है। पति का नाम न लेना, तम्बू सा घूँघट लादे रहकर पति का जूता देखने भर की इज़ाज़त जैसे कई प्रसंग सामाजिक जड़ता के प्रतीक भर है, जिनकी तह में जाने कितनी मान्यताएँ हैं जो औरतों के होंठों पर चुप की तरह धरी रहती हैं।
यों इस फिल्म में सामाजिक सरोकारों को आवाज़ दी गई है परन्तु उसके समानान्तर ही विरह की कसक और मिलन का भरोसा पूरी कोमलता के साथ मौज़ूद है। यह तरुणाई फिल्म के नायक-नायिकाओं की ही तरह है, कुछ कच्ची-कुछ पक्की। कहानी में व्यवस्था पर तंज है, भ्रष्ट क़ानून व्यवस्था का अंकन है और इन सबके बीच सारी मानसिक थकान को उतारती मंजू टी स्टॉल की मंजू है। मंजू उस स्त्री वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसने आर्थिक आज़ादी प्राप्त कर ली है। जो बेचारी नहीं है सबला है। जो यह जानती है कि औरत अनाज उगा भी सकती है और पका भी सकती है। बच्चा पैदा भी कर सकती है तो पाल भी सकती है। कथानक में यूँ कई झोल देखे जा सकते हैं, कई दृश्यों में अभिनय कुछ कम प्रभावी भी दिखाई पड़ा है परन्तु जिस सादगी के साथ जिस उद्देश्य को लेकर यह फिल्म बनाई गई है उसमें काफ़ी हद तक यह सफल प्रतीत होती है। पितृसत्ता जिसका दंश सदियों से स्त्री झेल रही है और जाने कितनी सदियों तक ओर झेलेंगी, का कहानी में बहुपरतीय अंकन है। स्त्री जब पितृसत्ता की पैरवी करने लगती है तो स्त्री के लिए सहज जीवन की राह और मुश्किल हो जाती है कहानी में यह इस संवाद के माध्यम से दिखाया गया है कि, “घर की औरतें सहेली नहीं बन पाती,सास-ननद-जेठानी सब बन जाती हैं।”
कहानी का सरल-तरल संगीत मन को बाँधता है तो फूल और जया का अभिनय और गफ़लत ग्राम्य स्त्री जीवन की सजीव झाँकी खींचता जान पड़ता है। दारोगा के किरदार में रवि किशन ने अपने अभिनय का लोहा फिर मनवाया है। कहानी और फिल्मांकन में सहजता इतनी ज्यादा है कि यह आज के जमाने से कदमताल करती नहीं जान पड़ती और अस्वाभाविक बन जाती है, पर दूसरी तरफ यह तथ्य भी उतना ही प्रामाणिक है कि भूगोल के गह्वरों में आज भी यह सादगी, भोलापन, पितृसत्ता की कुटिल कुचालें और स्त्री को वस्तु समझने की सोच, उसे बेचारी समझे जाने की मानसिकता पूरी तीव्रता के साथ मौज़ूद है। कहानी में ज़गहों के नाम से लेकर, हर संवाद में व्यंग्य को पूरी सहेजन के साथ परोसा गया है और ये तत्त्व ही फिल्म को मनोरंजन से परिपूर्ण भी बना देते हैं। लापता लेडिज उन लापता स्त्रियों की अस्मिता को खोजने का प्रयास है जो अनुभवी पितृसत्ता की बेड़ियों में भूला दी गईं हैं या कि स्वयं को भूला बैठी है। कुल जमा लापता
 कल्पना के रंगों से कम परन्तु यथार्थ के सादा रंगों से रंगी एक प्रभावी फिल्म है।
कल्पना के रंगों से कम परन्तु यथार्थ के सादा रंगों से रंगी एक प्रभावी फिल्म है।
डॉ.विमलेश शर्मा
आलोचक एवं कवयित्री
अजमेर,राजस्थान
9414777259