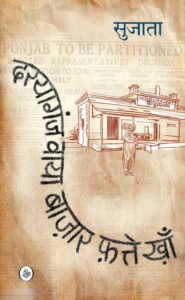पिछले दिनों प्रसिद्ध निबंधकार कुबेरनाथ राय के कुछ निबंधों पर प्रचण्ड प्रवीर ने जानकी पुल पर एक लेख लिखा था। उस लेख को पढ़कर प्रोफ़ेसर मनोज राय ने यह लेख लिखा है। मनोज राय महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिन्दी में पढ़ाते हैं और कुबेरनाथ राय के गहरे अध्येता हैं। आप उनका यह विद्वत्तापूर्ण लेख पढ़िए- मॉडरेटर
============================
पिछले दिनों दिल्ली के एक उद्भट शोधार्थी ने एक लिंक भेजकर प्रचण्ड प्रवीर के आलेख ‘विस्मृत नायक : कुबेरनाथ राय’ को पढ़ने का आग्रह किया। कुबेरनाथ राय ( लेख में आगे कुबेरनाथ राय को ‘कुनारा’ नाम से संबोधित किया गया है।) के लेखन से परिचय और रुचि होने के कारण लेख पढ़ गया। लेख अच्छा और तथ्यपरक लगा । लेख पढ़ते समय स्नायुमंडल में अनेक बातें उमड़ने-घुमड़ने लगीं । प्राय: होता यह है कि यदि लेख अच्छा है तो आनंद-पूर्वक पढ़ता हूँ और आगे बढ़ जाता हूँ। लेकिन इस लेख को पढ़ने के बाद ‘मन की बात’ करने/लिखने की इच्छा हुई और कलम/लैपटॉप लेकर बैठ गया।
‘विस्मृत नायक: कुबेरनाथ राय’ के लेखक का नाम प्रचण्ड प्रवीर है। दो शब्दों के इस नाम में दो उपसर्ग ‘प्र’ हैं। यह एक संयोग है कि ‘कुनारा’ को इस तरह के अनेक उपसर्गों से गहरा लगाव है और वे इनका खूब प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए–प्रशांत, प्रमूल्य, प्रलुब्धक, प्रगल्भ, महाजागरण, महासमन्वय, महाविद्या, महानिशा आदि।
लेख के आरंभ में ही लेखक के एक ‘प्रचण्ड वाक्य’ से भेंट हो गई – ‘कुछ ऐसी ही चालाकियाँ और मूर्खताओं का शिकार रही हैं कुबेरनाथ की रचनाएँ।’ है तो कटु कथन, पर बात तो सही है। विडम्बना देखिये कि अत्यंत पढ़ाकू और सावधान लेखक अनजाने ही सही गाफिल संपादक की मूर्खता का शिकार हो जाता है । हुआ यह कि कुछ लोगों से ‘कुनारा’ की प्रशंसा सुनकर उनके दो संग्रह ‘प्रिया नीलकण्ठी’ और ‘रस आखेटक’(फर्जी वाला) वह पढ़ भी लेता है। ध्यान देने की बात है इस ‘रस आखेटक’ में संग्रह ‘प्रिया नीलकण्ठी’ संग्रह का एक निबंध ‘हेमंत की संध्या’ सम्मिलित है। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। दरअसल ‘प्रचण्ड’ संज्ञा का यह एक विशेष गुण धर्म है जिसके वे इसके शिकार हो गए। ‘कुनारा’ की प्रारम्भिक तीन कृतियाँ भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई थीं- ‘प्रिया नीलकण्ठी’,‘रस आखेटक’ और ‘गंधमादन’ । दुर्भाग्य से फर्जी तरीके से प्रकाशित होने/छपने की बीमारी से ग्रस्त किसी गाफिल संपादक ने ‘रस आखेटक’ नाम से उनके दूसरे संग्रहों से निबंध उठाकर प्रकाशित करा दिया है और आजकल अमेजन पर वही उपलब्ध है। असल संग्रह नदारद। ग्रेशम का नियम ‘बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है’ यहाँ भी काम कर रहा है। अब जब 19 निबंधों का संग्रह भारतीय ज्ञानपीठ से ‘रस आखेटक’ के नाम से प्रकाशित है तो उसमें से चार निबंध लेकर फर्जी संग्रह प्रकाशित करना न केवल अनैतिक है अपितु एक किस्म का संपादकीय अपराध भी है। चयन और संकलन प्रकाशित करना उचित है पर शीर्षक का दुहराव कत्तई अनुचित है। लेखक प्रवीर द्वारा बड़ा सुंदर सवाल उठाया गया है- ‘इन सारे मंतव्य के बावजूद इन्हें पुस्तक के सम्पादन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी यह मेरे समझ से परे है।’ आजकल के गोमुखी व्याघ्र चयनकर्ताओं और संपादकों को समझना आसान नहीं है। तथ्य यह है कि जिन उद्धरणों के ब्याज से प्रचण्ड ने यह सवाल उछाला है, वे सभी कथन अंग्रेजी के अध्यापक रहे पी.एन.सिंह की किताब ‘कुबेरनाथ राय की साहित्यिक-सांस्कृतिक दृष्टि’ और गाफिल संपादक की उनसे बातचीत के आधार पर लिखे गए हैं।
पी.एन.सिंह ‘कुनारा’ के समकालीन रहे हैं। यह संयोग है कि कुनारा और पी.एन.सिंह दोनों ही अंग्रेजी के प्राध्यापक थे। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का होना स्वाभाविक है। बड़े-बड़े गुरु घंटाल जब द्रोणाचार्यों के सहारे शाखा-मृग बने हुए थे तब किशोर ‘कुनारा’ (कक्षा 8 /9 में पढ़ते समय) के लेख माधुरी और विशाल भारत में छप चुके थे। जब वे अपने गाँव-घर से दूर नलबारी में रहकर साहित्य-साधना में लगे थे, तब उनके समकालीन अपनी-अपनी राजनीति में लगे थे । पी.एन.सिंह भी इनमें से एक हैं । मनुष्य रूप में वे भले और एक सीमा तक ‘लिबरल’ भी थे। पर कुछ बात है कि … । पी.एन.सिंह ने ‘कुनारा’ पर एक भारी अहसान करते हुए (या अपनी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा के कारण) ‘कुबेरनाथ राय की साहित्यिक-सांस्कृतिक दृष्टि’ शीर्षक से एक पुस्तक लिखी । इस पुस्तक में ‘कुनारा’ पर देशी-विदेशी औजारों से खूब वार किए गए हैं। लेकिन ‘कुनारा’ की ऊंचाई इतनी है कि पी.एन.सिंह को थक हारकर कहना पड़ता है-‘उनका लेखन बहु-आयामी,अंतर्दृष्टि सम्पन्न एवं आकर्षक है,और ये ही उनके लेखक-व्यक्तित्व के आधार है।’ (पी.एन.सिंह : कुबेरनाथ राय की साहित्यिक-सांस्कृतिक दृष्टि, पृ 58) इसी पुस्तक के अंत में पी.एन.सिंह का एक आलेख भी संकलित है जो संभवत: ‘कुनारा’ की मृत्यु के बाद लिखा गया था। इसमें वे स्वीकार करते हैं कि ‘मेरी उनसे बमुश्किल पाँच-छह मुलाकातें हुई होंगी।’ (पी.एन.सिंह : कुबेरनाथ राय की साहित्यिक-सांस्कृतिक दृष्टि, पृ 93) और ढाई दशक बाद वीणा में प्रकाशित एक लेख में वे लिखते हैं-“वे मेरे निवास पर अक्सर प्रातः पाँच बजे आ जाया करते थे और तरह-तरह की बात अपने महाविद्यालय के बारे में कहते रहते। ….. यही बातचीत करते सात बज जाते। मैं उनको एक कप चाय और पिलाता और फिर नीचे उतरकर उन्हें प्रणाम कहते हुए सी-ऑफ करता।” (वीणा,वर्ष 94, अंक 6, जून 2021) एक शांत और समर्पित लेखक जो इस धरा पर नहीं था, उसके बारे में ऐसी टिप्पणी मर्माहत करने वाली है। ऐसी टिप्पणी इसलिए भी आती हैं कि उस शानदार और कालजयी लेखक के साथ कोई खड़ा होने वाला नहीं था। जिस फर्जी संग्रह ‘रस आखेटक’ को प्रचंड ने पढ़ा है उसका ‘अबसर्ड संपादकीय’ जो कई मायनों में अभूतपूर्व है, का अंतिम दो पैरा देखने लायक है- “मैं पी.एन. सिंह की पुस्तक के बारे में क्या कहूँ। कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कुछ भी निर्णायक रूप से कहना उचित नहीं लगता। डॉ. पी. एन. सिंह को कुबेरनाथ राय के बारे में जल्दबाजी में कुछ कहना आत्मश्लाघा होगी। लेकिन कुल मिलाकर, इतना निश्चित है कि कुबेरनाथ राय एक ऐसे निबंधकार हैं, जिन्हें ठीक से पढ़ना और लिखना चुनौतीपूर्ण है।” गाफिल मियां गुरु पी.एन. सिंह के कथन ‘… लेकिन व्यावहारिक स्तर पर भाजपाई । कुछ एक सहकर्मी मित्रों ने ऐसा मुझे बताया है’,(सिंह :पृ. 79) का पैराफ़्रेजिंग तो किए ही साहित्य के भरत मुनि बनते हुए यह भी घोषित कर दिये कि ‘कुबेरनाथ राय की कोई स्वतंत्र साहित्यिक दृष्टि नहीं है।’ यह देखना पाठक गण इस बात का लक्ष्य कर सकते हैं कि गाफिल चेला-संपादक और गुरु पी.एन. सिंह न केवल एक ही भाषा का प्रयोग करते हैं, अपितु सनातन की चिंता को वे अल्पसंख्यक और उर्दू विरोध तथा हिन्दू राष्ट्रवाद के समर्थक के रूप में देखते हैं। इसे मानसिक दिवालियापन के अलावा और क्या कहा जा सकता है? पाठक स्वयं विचार करें। ।
प्रचण्ड ने अपने नाम के साथ न्याय करते हुए गाफिल संपादक की बढ़िया से खबर लेते हुए यह जानने को उत्सुक है कि ‘इन्हें पुस्तक के सम्पादन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी यह मेरे समझ से परे है।’ लेखक की यह चिंता भी जायज है कि ‘जब आप महानुभाव को सन्दर्भ समझ ही नहीं आते तो आप सम्पादन का भार क्यों उठाते हैं।’ प्रवीर की प्रचण्ड राय और भी मानीखेज हो जाती है जब वह यह कहते हैं कि ‘रस आखेटक’ व ‘प्रिया नीलकण्ठी’ का सम्पादन और विश्लेषण कूढ़मगजों को अवश्य छोड़ देना चाहिए क्योंकि श्रम करना उनके बस का रोग नहीं है।’ गाफिल संपादक अपने संपादकीय में लिखता है-‘अभी तक मैंने उन पर तीन पुस्तकें देखी और पढ़ी हैं। … इसमें इसको सबसे अच्छा कहा जाए।’ गाफिल मियां को पता ही नहीं है कि 1979 में ही कुरुक्षेत्र वि. वि. के हिंदी विभाग से ‘कुबेरनाथ राय के निबंधों में लालित्य तत्त्व’ विषय पर एम. फिल. की उपाधि मिल चुकी थी। इसके बाद भी अनेक लोगों ने उन पर शोध किया था। मजेदार बात है कि कुनारा पर शोध करने वाले प्राय: दूसरे प्रदेशों के लोग थे, जिनसे न तो उनका कोई पूर्व परिचय था न ही बाद में कभी भेंट हुई । दरअसल आजकल बिना हर्र-फिटकरी के चोखा तैयार होने वाले संपादकों/प्रकाशकों का ज़ोर बढ़ता जा रहा है और वे ऐसे क्लासिक लेखकों की रचनाओं को छापने की जुगत में लगे रहते हैं । कुबेरनाथ राय भी ऐसे ही एक लेखक हैं। ‘सहज कृतज्ञ’ गाफिल संपादक की अन्य संपादकीय कृतियों में सम्मिलित संपादकीय वक्तव्यों को ठीक से पढ़ने वाला हर पाठक उसकी ‘चालाकी और नालायकी’ को समझ सकता है। संपादकीय अविवेक का उदाहरण हाल में प्रकाशित ‘कुबेरनाथ राय रचनावली’ में भी देखा जा सकता है जिसके प्रथम पृष्ठ से ही प्रचंड प्रवीर के अनेक कथनों की पुष्टि होती दिखती है। ‘कुनारा’ प्राय: अपनी किताबों में ‘अंत में’ या ‘अपनी बात’ शीर्षक के अंतर्गत पुस्तक के बारे में कुछ कहते/बताते हैं। इस रचनावली में तो गाफिल-द्वय संपादकों ने एक दूसरे संकलनकर्ता के संपादकीय ‘उनकी बात’ को ‘उनका’ ही समझकर उसे सद्य: प्रकाशित कर अभूतपूर्व कार्य किया है। इस पर फिर कभी चर्चा होगी । फ़िलहाल तो इतना ही कहना है कि ‘कुनारा’ के निबंधों का आनंद लेने के लिए उसे मूल में ही पढ़ना ही चाहिए न कि किसी संपादकीय सहारे से।
प्रचण्ड प्रवीर ने ‘कुनारा’ पर टीका-टिप्पणी करने की कुछ पूर्व शर्तें बताई हैं जिससे मेरी शत-प्रतिशत सहमति है। ‘कुनारा’ जैसे निबन्धकार की आलोचना तो और भी कठिन है जिसकी जड़ें पाताल तक फैली हों। पर मन है कि मानता नहीं और कुछ ‘जम्बुक’ पंड श्रम कर बैठते हैं । प्रवीर ने फकीर और गांधी के हिंसा-अहिंसा तथा प्रेमिका के ब्याज से बड़ी सुंदर बात कही है। इसका असल आनंद उठाने के लिए पाठकों को त्रेता के वृहत्साम में ‘कुनारा’ द्वारा लिखित संवाद ‘सिंह-शूकर’ को पढ़ना चाहिए। इस अद्भुत संवाद को समझते हुए आगे बढ़ना ठीक रहेगा। किसी समय एक जंगल में एक सिंह अपनी पद्मपलाश लोचना सिंहनी के प्रेम पाश में बद्ध होकर रात-दिन उसी के साथ विचरण करता था। जैसा कि जंगल में होता है छीना-झपटी में माहिर कमीने हुंडार (भेड़िए) भी सिंह-झुंड के आस-पास ही विचरण करते रहते हैं। जंगल की एक गज़ब खासियत है यह है कि शाश्वत दुश्मन भी अगल-बगल रह लेते हैं। बहरहाल सिंह इस बात को कई दिन से ताड़ रहा था कि हुंडार उस युगल-प्रेमी को दूर-दूर से देखा करता है। यह एक अद्भुत तथ्य है कि प्राय: सिंह ‘हुंड़ार-भेड़िए-कुत्ते’ का मांस नहीं खाते। इसलिए उसकी तरफ वे ध्यान नहीं देते। पर कभी-2 परिस्थितिवश ध्यान देना ही पड़ता है और एक दिन वह घटित हो ही गया। सिंह अकेले ही कहीं विचरण कर रहा था। सिंह के स्नायुमंडल में अचानक कपिशा प्रिया का ध्यान और उस पर से जार भाव उमड़ता है। सिंह काम के वशीभूत हो तीव्र वेग से लौटा। उसे दूर से ही दिखाई दिया कि कमीना हुंड़ार उसकी सोती प्रिया को सूंघ रहा है। पंजे से लेकर माथे तक बिजली दौड़ गयी। काल का पंजा उठा उसके एक ही प्रहार से उस कमीने हुंडार की गर्दन टूट गयी। दूसरे प्रहार की जरूरत नहीं पड़ी। कहना न होगा कि प्रवीर ने भी अपने लेख में प्रचण्ड वार किया है जिसके कारण तथाकथित गाफिल संपादक का तिलमिलाना स्वाभाविक है। हालांकि वे भले मन से कहते जरूर हैं कि ‘मैं केवल उनकी अल्पज्ञता, हठधर्मिता, हिंसा और अशुचिता को रेखांकित करना चाहता हूँ।’ ‘प्र’ उपसर्ग का इतना प्रभाव तो पड़ना ही चाहिए।
प्रचण्ड प्रवीर का अध्ययन अत्यंत समृद्ध है। कला-विज्ञान-दर्शन की समझ भी काबिलेतारीफ है। ‘कुनारा’ के स्नातक में विषय थे-अंग्रेजी साहित्य,गणित और दर्शन तथा उन्होने ‘श्री प्रियरंजन सेन, डॉ० सुबोध सेन गुप्ता एवं प्रोफेसर तारक सेन जैसे ‘टैगोरिस्टों’ के चरणों में बैठकर विद्या-लाभ लिया था ।’ (सरस्वती, जुलाई 1962) फलस्वरूप समय के साथ उनकी दृष्टि अत्यंत साफ और निर्मल होती गई है और ‘वे लोक से मानव जीवन का महत्तम उठा लेने’ की कला में निष्णात हो गए हैं और उसका सुखद परिणाम यह हुआ कि हमारे जैसे पाठकों को घर बैठे ही एक से बढ़कर एक कोहिनूर-निबंध पढ़ने को मिल जाता है ।
प्रचण्ड प्रवीर विज्ञान और गणित के सिद्धांत और लिबनिज, इन्टिग्रल-डिफरेंशियल कैलकुलस जैसे उदाहरणों के ब्याज से निबन्धकार द्वारा कुछ निचोड़ निकालने पर अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी हमारे सामने रखते हैं और ‘कुनारा’ की कुछ अवधारणाओं, जिसके अटपटे लगने के बावजूद सिरे और शीघ्रता से अस्वीकृत नहीं करने का आग्रह करते हैं। ‘कुनारा’ ने प्रकृति में नर की श्रेष्ठता को अवश्य रेखांकित किया है, पर उस व्यंजना का यदि हम ठीक से अभिग्रहण करें और गीता के श्लोक ‘ध्यायतो विषयान्पुंस:, सङ्गस्तेषूपजायते। सङ्गात्सञ्जायते कामः, कामात्क्रोधोऽभिजायते॥,’ से मिलाकर एक साथ देखेंगे तो अर्थ कुछ-कुछ स्पष्ट हो जाता है। बहरहाल जीवन का यह क्षेत्र बड़ा जटिल है और इस पर आत्यन्तिक निर्णय देना या थोपना उचित नहीं है। ‘कुनारा’ भी प्राय: इस बात की ताईद करते हैं।
प्रचण्ड का यह कथन कि ‘हमारे यहाँ उच्छिष्ट पढ़ने का रिवाज है,’ बावन तोले पाव रत्ती सही है। शास्त्र को मूल में ही पढ़ने की उनकी हिदायत भी सर्वथा उचित है। यह एक तथ्य है कि आज की इस सूचना विस्फोट युग में धैर्य पूर्वक मूल ग्रन्थों को पढ़ने का समय निकालना आसान नहीं है। तो उपाय क्या है? लेखक सुझाव देता है कि ऐसे में अंग्रेजी के प्रोफेसर कुबेरनाथ राय (और लोगों का भी नाम जोड़ा जा सकता है) के निबन्धों से ही काम चलाना ठीक रहेगा। यह सुझाव मानीखेज है। ‘कुनारा’ ने अपने निबंधों में रामायण और महाभारत सहित अनेक पौराणिक ग्रंथों पर अपनी कलम चलायी है । ‘कुनारा’ का मानना है कि किसी भी ‘राष्ट्र की कस्तूरी उसके साहित्य में होती है। यह कस्तूरी दुर्गन्धमयी न हो’ इसके लिए साहित्य को सरल-स्वच्छ-उच्चगामी होना होगा जिसके लिए विषय का उच्चाशय होना जरूरी है। क्रिया-योग की साधना के फलस्वरूप वे इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत हमारी ‘परमा स्मृति’ का हृदय रचते हैं। मर्कट वाम-विचारकों को यह जाँचता-पचता नहीं और वे उनपर दो तरफा आक्रमण करते हैं कभी ‘उपेक्षा’ से तो कभी ‘अतीत का कैदी’ कहकर। ‘कुनारा’ इन सबसे बेपरवाह हो तथ्य और रस दोनों के साथ न्याय करते हुए ‘पाठकों के मानसिक ऋद्धि और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार’ के अपने उद्देश्य से कभी विरत नहीं होते हैं। इस रचना-प्रक्रिया में कई जगह वे कल्पना का भी सहारा लेते हैं पर वहाँ भी वे व्यावहारिक धरातल को नहीं छोड़ते हैं। यह ठीक बात है कि समय के साथ अनेक अनुसंधान होंगे और नए तथ्य भी सामने आएंगे। हो सकता है कि तब कुछ निष्कर्ष धूमिल भी हो जाएँ। ‘कुनारा’ लिखते भी हैं-“अतः मेरा प्रस्ताव है कि इन निबन्धों पर कोई विचार करने चले तो ‘रस’ की कसौटी पर ही विचार करे, शास्त्र की कसौटी पर नहीं। इसके ‘रस’ के लिए ही मेरी सिसृक्षा यश या अपयश की भागी है। इसके ‘शास्त्र’ वाले अंश को तो मैंने ‘भारत का भूगोल’ (कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक) से लेकर हटन, चटर्जी, गुहा, प्रजुलुस्की आदि तक-वाङ्मय के अनेक घाटों से उपलब्ध किया है ।” (निषाद बांसुरी,पृ 243) स्पष्ट है कि शास्त्र वाले अंश के लिए वे तत्कालीन उपलब्ध साहित्य का सहारा लेते हैं और एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं। पर वे नए शोध का स्वागत भी करते हैं । उनका तो मानना है कि ‘शिशु कक्षा की पहाड़े की पुस्तक से लेकर आणविक भौतिक नवीनतम शाखा ‘प्लाज्मा फिजिक्स’ तक, सर्वत्र ललित निबन्ध के बीज उपलब्ध हो सकते हैं।’ (वही) यह सच है कि समय के साथ नवीन खोजों के आधार पर ‘नए प्रमाणों के आने से उनकी स्थापनाएं तथ्यात्मक रूप से पुरानी या कहें तो अशुद्ध भी’ हो सकती हैं। लेकिन उनकी असल चिंता से कौन इंकार करेगा? उनकी असली चिंता है आसेतु हिमाचल की। इसलिए वे कहते हैं कि ‘भारतीय ‘ब्रह्मा’ चतुरानन हैं, जिनके चार मुख हैं : आर्य-द्रविड़-किरात-निषाद’ । कौन नहीं जानता कि साठ-सत्तर के दशक में देश किन परिस्थितियों से जूझ रहा था। ‘कुनारा’ एक संवेदनशील और सजग लेखक हैं। वे उस काल खंड में ‘प्रत्येक स्वर का शुभाशुभ पढ़ने की चेष्टा’ करते हैं और लिखते हैं-“बंगाल से जम्बुक-स्वर उठता है: ‘भारत तो कोई एक राष्ट्र नहीं । यह तो बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र आदि अनेक राष्ट्रों के समूह का नाम है। हाँ, नौकरी और शरणार्थी के प्रश्न पर भारत ‘एक राष्ट्र’ अवश्य माना जाना चाहिए। फिर असम से जम्बुक-स्वर उठता है, ‘‘भारतमाता तुम मेरी मातामही हो सकती हो, पर मातृका नहीं ! माँ है ‘असमा!’ साथ ही एक ‘प्रगतिवादी’ स्वर उठता है: ‘ मैं मुसलमान, हम और तुम असमिया! परन्तु ये गुजराती-बिहारी-मारवाड़ी विदेशी!’ तमिलनाडु से स्वर उठता है, ‘हम हैं महान, आर्य हैं नीच! इस देश का पट्टा हमारे गौरांग प्रभु अगले 500 वर्षों के लिए हमारे नाम लिख गये! अतः आर्य=संस्कृति=उत्तर=भारत=हिन्दी=महात्मा गाँधी=रामायण हमारे दुश्मन नम्बर एक हैं !’” (रस आखेटक , पृ 132-133) इसलिए ‘कुनारा’ को पढ़ते समय चतुर्दिक सतर्क रहना होगा।
‘कुनारा’ अद्भुत प्रतिभा के धनी है। भारतीय परंपरा को गहराई से समझने और उसकी अभिव्यक्ति की उनकी अपनी शैली है। लेखन की शुरुआत तो वे ‘साहित्य में मेरा वादा’ से करते हैं और तीसोत्तरी तक आते-2 अपनी निजी ‘आत्मिक मूलाधार’ (Spiritual Base) को पहचान जाते हैं और फिर उस मूल प्रकृति से कभी विचलित नहीं हुए। फलस्वरूप वे राम और रामकथा के उत्स की ओर बढ़ते चले जाते हैं और निकाल लाते हैं ‘त्रेता का वृहत्साम’ जैसी अप्रतिम निबंध-मणि। इस संग्रह का ‘एकमात्र उद्देश्य है रामत्व के उस सौंदर्य का उद्घाटन जो तप, संकल्प, पुरुषार्थ, त्याग, ज्ञान और तेज से जुड़ा है। पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर राम के इस तेजस्वी शील और सौंदर्य का उद्घाटन करने की चेष्टा है। (‘त्रेता का वृहत्साम’, पृ vii ) मनुष्य भी अद्भुत जीव है। इसकी जिजीविषा भी अव्याहत है। यह निरंतर अतिक्रमण करता हुए ऊर्ध्वाधर होता चलता है। हालांकि इस क्षेत्र में सबका प्रवेश वर्जित है। पर कुनारा तो कुनारा है। पूर्वजों की विद्या को पहचानने और उसे पाठकों को परोसने के लिए इस क्षेत्र में भी बेधड़क प्रवेश कर जाते हैं। इस गुह्य विद्या के महाकांतार में प्रवेश को कुछ बाल-खिल्य तथा ‘मर्कट’ वामपन्थी उन्हें ‘हिन्दू राष्ट्रवादी’ कहते हैं। दरअसल इनका असली दर्द तो कुछ और ही है। आजादी के शुरूआती दशकों के साहित्येतिहास के आकाश पर संस्कृति तथा इतिहास-संशोधन के सरकारी विधाता-व्याख्याता और मनसबदार तथा नव्य-पुरातन वामपंथियों के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा सरपट दौड़ रहा था । अचानक ‘कुनारा’ अवतरित होते हैं घोड़े की लगाम को पकड़ लेते हैं और लिखते हैं-“19वीं शती का यह ‘संपूर्ण पुनर्जागरण’ मूलत: हिंदू महाजागरण था। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।” (सरस्वती, मार्च 1964) उनका यह कथन किसी भावावेश में नहीं अपितु सवा सौ वर्ष (1825-1950) में घटित हुए उन भाव-परिवर्तनों की गहन-विवेचना के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जिन्होंने अभिनव हिंदू धर्म के नए आयामों की सृष्टि की है। अपने दो आलेखों ‘मानववादी आंदोलन और सनातन का पुनर्गठन’ में उक्त अवधि के महत्वपूर्ण सामाजिक-धार्मिक आंदोलनों और उनके नायकों के अवदान के साथ-साथ राष्ट्रीय अस्मिता के चारों स्तम्भ-‘राष्ट्रीय दर्शन-राष्ट्रीय धर्म-राष्ट्रीय सौंदर्य दृष्टि तथा राष्ट्रीय साहित्यिक उत्तरदायित्व’ जो क्रमशः ‘कर्मनिष्ठ वेदांत-भक्ति-रस सिद्धांत और लोकसंग्रह’ हैं, का नीर-क्षीर विवेचन किया है जो उस कालखंड की सम्पूर्ण सांस्कृतिक-राजनीतिक कसमसाहट के साथ-साथ करवट बदल रही भारतीय महाजाति के अनहद नाद को समझने की दृष्टि देती है। ‘सांस्कृतिक-स्वातन्त्र्य’ और ‘बुद्धि-स्वातन्त्र्य’ के नाम पर जब उस कालखंड में ‘लोलिता’ का चंग बनाकर उड़ाया जा रहा था और ‘रामकथा/मानस’ को ही प्रश्नांकित कर रहे थे, तब उस संक्रमण काल में श्री राय को त्रेताकालीन मृदंग-ध्वनि सुनाई देती है । वे लिखते हैं -“मेरे मन के भीतर स्थित प्रजापति बार-बार मुझे आदेश दे रहे हैं कि त्रेतायुग के इस इतिहास खंड को मनुष्य जाति की चेतना का शाश्वत अंग बना डालूँ ।” (महाकवि की तर्जनी, पृ 58) जब ‘हिन्दू’ शब्द के उच्चारण से साहित्यकार बच रहे थे, कुनारा सगर्व उद्घोष करते हैं-“आधुनिक दृष्टिवाले काष्ठ योगी चाहे जो कहें, पर मैं तो हिन्दू हूँ और उसमें भी सिक्ख-बौद्ध-जैन नहीं, बल्कि सनातनी और मूर्तिपूजक है, और इस आसेतु हिमाचल, वसुन्धरा को मैं कभी मामूली मिट्टी नहीं मान सकता। यह तो साक्षात् देव-विग्रह है । इसे परमाप्रकृति का बृहत्तर देव-विग्रह मानकर ही मैंने आजीवन इसका स्तवगान लिखते रहने का संकल्प ले लिया है। (निषाद बांसुरी, पृ 85) वे इस नव्य हिंदू-दृष्टि को जो ‘विवेकानंद, तिलक और गांधी द्वारा परिष्कृत हिंदू राष्ट्रीयता’ है, को ‘हिंदुस्तान की प्रतिभा की उपज मानते हैं जिसका हिंदुस्तान की जिजीविषा से जैविक संबंध है तथा जिसके बल पर हम आसेतु हिमाचल बंधे हैं।”(प्रिया नीलकंठी,पृ94 )
‘कुनारा’ की दृष्टि में ‘भारतीय संस्कृति के तीन आधार हैं : वैदिक, तान्त्रिक और लोकायत’। अब जब मन हिंदूमय हो और आजीवन इसका स्तवगान लिखते रहने का संकल्प भी हो तो स्वाभाविक है कि वे इन तीनों के रसायन से ही वे अपने शोध-निबंध तैयार करेंगे। इसलिए उनके कुछ निबंधों में औपनिषदिक और वैदिक कालीन शब्दों के साथ-2 योग और तंत्र साधना के शब्द खूब मिलते हैं। ज्योतिष विद्या और खगोल शास्त्र में उनकी गहरी रुचि है। प्रचंड प्रवीर की दृष्टि इधर भी गई है और उन्होने अपने तईं ‘त्रिजटा-स्वप्न’ निबंध के ब्याज से इसकी ओर संकेत करते हुए उसके रामायण के मध्य में होने के कारणों को समझने का आह्वान भी किया है। दरअसल इस पूरे प्रसंग को ठीक से समझने के लिए सावित्री के चारो रूपों को लेकर लिखे तीन और निबंध-‘सीता सावित्री, उषा और अहिल्या तथा अनुसूय्या प्रसंग का अवगाहन करना होगा। मेरी अपनी समझ है कि महानिशा के इस महाविद्या की झलक पाने के लिए ‘कुनारा’ के रामकथा पर आधारित तीन निबंध संग्रह – ‘महाकवि की तर्जनी, त्रेता का वृहत्साम और रामायण महातीर्थम’ में डुबकी लगानी होगी। गो कि यह गारंटी नहीं है कि हाथ कुछ आ ही जाय। क्योंकि यह रास्ता ही असामान्य है। अत: मेरी तो यही सलाह होगी कि ‘रस’ से ही संतोष किया जाय। हाँ कोई माई का लाल चाहे तो बजरंग बली का नाम लेकर इस गूढ़ विद्या के क्षेत्र में विचरण करने का साहस कर सकता है। पर अपनी तो सीमा बस ‘शब्द-रस’ तक ही है। कुनारा ‘रस और बोध’ के आग्रही हैं। वे लिखते हैं –“मैंने सर्वत्र अपने लेखन में ‘रस’ और ‘बोध’ का समान भाव से वितरण किया है और ‘बोध’ की दुहाई देकर रस का पलड़ा हीन करने को मैं कहीं भी तैयार नहीं, ‘विषाद योग’ जैसे बोध-प्रधान संकलन में भी नहीं। मैंने ‘बोध’ और ‘रस’ के बीच अंश-भेद देखा है तत्त्व-भेद नहीं । ”(विषाद योग’,पृ 245 ) कुनारा द्वारा प्रयुक्त ‘उषा और ऊषा’ शब्दों की तरफ भी हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कुनारा ने दोनों का प्रयोग किया है। मेरे हिसाब से दोनों के बीच गहरा अर्थ भेद नहीं है।
कुनारा के निबंध हास्य,सौन्दर्य और व्यंग्य की खान हैं । उनके व्यंग्य प्रायः हर निबन्ध में अपनी छटा बिखेरते हैं । बस जरूरत है सावधानी से पढ़ने और समझने की- ‘‘व्याकरण भाषा का पुलिस मैन है। जब कोई शब्द वाक्य के भीतर कुमार्गगामी होता है तो उसकी आवारागर्दी को ठीक करने के लिए व्याकरण उसपर लाठीचार्ज करता है,अश्रु गैस छोड़ता है और गिरफ्तार करता है, जिससे वाक्य-संहिता का ठीक-ठीक पालन होता रहे। तब भी कुछ कालिदास और शेक्सपीयरों की शह पाकर कुछ शब्द नक्सलपन्थी रास्ता अख्तियार कर ही लेते हैं और बाद में अपनी क्रांति की संवैधानिक स्वीकृति भी पा जाते हैं । तब बेचारा व्याकरण अपना सा मुँह लेकर रह जाता है।’’(गंधमादन,पृ 9) यह निबंध उन्नीस सौ साठ के दशक के अंतिम वर्षों में लिखा गया है। इस कथन में उस समय की भारतीय राजनीति में प्रवेश के इच्छुक घंट-घड़ियाल लिए एक विचारधारा की ओर संकेत किया गया है जिसके खात्मे के लिये आज भी सरकार प्रयास रत है। राग की खेती में विश्वास करने वाले कुनारा व्यंग्य करते समय कभी-कभी गाँडीव भी उठा लेते हैं- ‘‘कहाँ सारे रसों के रस माधव की प्रिया और कहाँ व्याकरण का नमक-सत्तू । कहाँ शब्दों का नवरसों के मार्ग पर अभिसार और कहाँ प्रत्यय और विभक्तियों की तड़ातड़ बजती लाठियाँ और संधि-समास का अश्रु गैस।’’ (गंधमादन,पृ 11) गाँव की राजनीति पर किया गया उनका व्यंग्य अद्भुत है-‘‘धूल में रस्सी बटना कोई उनसे सीखे। सारे गाँव को वे तुर्कनाच नचा रहे हैं। … उनकी कृपा से अभागे ग्राम के शीश पर मामले-मुकदमे के मेघ, दफा एक सौ सात के इन्द्र धनुष और फौजदारी के विद्युत गर्जन से सदा पावस ऋतु छाई रहती है।’’(रस आखेटक,पृ14 ) कुनारा के निबंध अपने परिवेश के इतिहास-भूगोल के परिचय के साथ-साथ गंभीर अध्ययन की भी मांग करते हैं। “हिंदी में दो-चार के अंदर ‘फिराक’-परस्ती की जो धुन जगी है वह इसी पुरानी आदत के कारण है।” (सरस्वती, मार्च 1966) प्रचण्ड प्रवीर ने ‘विस्मृत’ शब्द का प्रयोग राह चलते नहीं किया गया है। दरअसल यह उनके प्रेम को दर्शाता है। कुनारा के लेखन से लोग न केवल परिचित थे अपितु भयग्रस्त भी थे। कुनारा द्वारा पंत के ‘लोकायतन’ (1964 में प्रकाशित और सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से 1965 में सम्मानित) की गई समीक्षा “’लोकायतन’ की सारी दार्शनिक पृष्ठभूमि में पराक्रमहीनता का घोर सौंदर्यवादी ‘कुरान शरीफ’ मिलता है जिसे पंतजी अनावश्यक ढंग से बार-बार फेटते हैं,”(सरस्वती, मार्च 1965) ने पंत को मैदान में उतरने मजबूर कर दिया और पंत ने अपने बचाव में सरस्वती के जून 1965 के अंक में ‘लोकायतन का उद्देश्य और दृष्टिकोण’ शीर्षक से एक बड़ा लेख लिखा । लेकिन कुनारा पीछे कैसे हटते ! उन्होने पंत के लेख का जबाव सरस्वती -अगस्त,1965 में ‘फिर लोकायतन पर’ शीर्षक से दिया और उपलढ़ आंकड़े बताते हैं कि पंत जी ने चुप बैठना ही श्रेयस्कर समझा। कल्पना की जा सकती है कि यह वह समय है जब पद्म श्री के सहारे पंत अपने शीर्ष पर थे और कुनारा बस लेखन में प्रवेश ही किए थे। यह एक कठोर सच्चाई है जिसकी तरफ प्रचण्ड के लेख में संकेत भी किया गया है कि साहित्य के इन ‘अश्वथामाओं’ ने उन्हें उसकी मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश भी की और कुछ हद तक सफल भी रहे। कुनारा इस बात को समझते थे। पर साहित्यकार से तो उनकी अपेक्षा कुछ और ही थी- “साहित्यकार’ न केवल ‘सत्य के प्रति ईमानदार रहे और सत्य के लिए ही एक सांस्कारिक, मानसिक वातावरण तैयार करे’ अपितु “यदि आत्मा द्वारा उपलब्ध सत्य ‘बहुमत’ के खिलाफ जाता है, तो साहित्यकार का धर्म है बहुमत के विरुद्ध खड़ा होना,अकेले खड़ा हो जाना,समूची ऐतिहासिक शक्तियों के विरुद्ध अकेली उठी हुई तर्जनी का रोष व्यक्त कर देना।”
अंत में एक बात की ओर इशारा कर अपनी बात को खत्म करूंगा । साहित्य की दुनिया में भाषा को लेकर खूब बहस हुई है और हो भी रही है। अनेक रचनाओं की भाषा को लेकर विवाद भी खूब हुए है। इन सबके बीच कुनारा भी अपनी भाषा को लेकर परेशान है। वे कहते हैं –“मैं गाँव-गाँव, नदी-नदी, वन-वन घूम रहा हूँ । मुझे दरकार है भाषा की। मुझे धातु जैसी ठन-ठन गोपाल टकसाली भाषा नहीं चाहिए। मुझे चाहिए नदी जैसी निर्मल झिरमिर भाषा, मुझे चाहिए हवा जैसी अरूप भाषा। मुझे चाहिए उड़ते डैनों जैसी साहसी भाषा, मुझे चाहिए काक-चक्षु जैसी सजग भाषा, मुझे चाहिए गोली खाकर चट्टान पर गिरे गुर्राते हुए शेर जैसी भाषा, मुझे चाहिए भागते हुए चकित भीत मृग जैसी ताल-प्रमाण झंप लेती हुई भाषा, मुझे चाहिए वृषभ के हुंकार जैसी गर्वोन्नत भाषा, मुझे चाहिए भैंसे की हँकड़ती डकार जैसी भाषा, मुझे चाहिए शरदकालीन ज्योत्सना में जंबुकों के मंत्र पाठ जैसी बिफरती हुई भाषा, मुझे चाहिए सूर के भ्रमरगीत, गोसाई जी के अयोध्याकाण्ड, और कबीर की ‘साखी’ जैसी भाषा, मुझे चाहिए गंगा-जमुना-सरस्वती जैसी त्रिगुणात्मक भाषा, मुझे चाहिए कंठलग्न यज्ञोपवीत की प्रतीक हविर्भुजा सावित्री जैसी भाषा।” अब जब ऐसी भाषा से जो साहित्य-फल निर्मित होगा वह तो अमृत फल होने के साथ-2 दीर्घायु भी होगा। इसलिए मेरा मानना है कि कुबेरनाथ राय भारतीय साहित्य के अमर नायक हैं।
प्रचण्ड प्रवीर के हाँ में हाँ मिलाते हुए मैं भी कहूँगा कि ‘हिन्दी साहित्य के वैभव, विशालता और प्रगल्भता के प्रतिमान’ इन निबंधों को अवश्य पढ़ा जाना चाहिए । मेरा दावा है कि जिस तरह महाभारत की लड़ाई में युधिष्ठिर का रथ धरती से सदैव चार अंगुल ऊपर-ऊपर चलता था ठीक उसी तरह पाठक भी भीतर-2 न केवल ऊर्ध्वाधर होगा अपितु उसके मानसिक और बौद्धिक क्षितिज का विस्तार होगा। अमृत काल में इससे सुंदर अमृत फल की और क्या ही कल्पना की जा सकती है।