युवा लेखिका कविता का समकालीन हिंदी कथाकारों में अपना खास मुकाम है. उनके आत्मकथ्य के माध्यम से उनके कथा-संसार की रोचक यात्रा पर निकलते हैं- जानकी पुल.
================================================
बात अपनी एक कहानी की कुछ पंक्तियों से ही शुरु करती हूं –
” कुछ अपना बिल्कुल अपना रचने का अहसास औरतों के मन में रचता है एक घर. घर एक सपना है औरतों की नींद में बचपन से सुगबुगाता, डग भरता, ढहता, टूट जाता…”(आशिया-ना)
अपनी ज़िंदगी में जिन्हें सबसे करीब से देखा जाना वे मेरे परिवार और आसपास की स्त्रियां थीं; शायद खुद को भी जानूं-समझूं उससे भी पहले से. उनके छोटे-छोटे सुख उनके बड़े-बड़े दुःख, उनकी पीड़ा, उनकी चाहना, उनके सपने और उनके सपनों का कुचला जाना भी.
पुरुष तो जो होते थे, शाम-सुबह घर में आये, दिखे फिर गायब. और जबतक घर में उपस्थित हैं घर भर के आकर्षण और ध्यान के केन्द्रविंदु बने हैं… उन्हें किसी चीज़ की जरूरत तो नहीं… उनके मन लायक खाना तो बना… उनके आसपास शोर गुल न करने की हिदायतें… आदि-आदि. उन्हें करीब से जानने-समझने का मौका ही कहां था.
…पर आसपास स्त्रियां थीं और भरपपूर थीं. खुद अपने ही घर में एक विधवा मां, चार बड़ी बहनें और आसपास भी इसी तादाद में इसी तरह के परिवार. स्त्रियां थीं तो कहानियां भी थीं; न सिर्फ उनके द्वारा कही जाने वाली बल्कि खुद उनकी कहानियां भी.
मेरी शुरुआती लगभग सभी कहानियां मैं शैली में लिखी गई हैं. जाहिर है इन कहानियों में मैं हूं, और मेरा जीवन भी… और वे कहानियां नहीं हुई होती अगर मैं स्त्री नहीं होती.
लिखना मेरे लिये एक यातना है, अपने पाने की बेचैनी, उसे पकड़ पाने की विकलता. ‘मैं’ आकर घेर लेता है मेरी बृहत्तता. ‘मैं’ मुझे सीमाओं में बांध देता है. ‘मैं’ के बिना मैं अवरोध रहित होती पर ‘मैं’ मेरे लिये एक चुनौती है. अपने को उघाड़ना, अपनी परतें खोलना ज्यादा दुःसाध्य है. ‘मैं’ मेरे लेखन पर इल्जाम भी बना रहा. पर मैने इस मैं को बार-बार खुरचा, परखा, रचा और पुनर्सृजित किया है. हां, इस क्रम में कई बार दूसरों के अनुभवों को भी मैं पहले ‘मैं’ की कसौटी पर परखती हूं; एक लेखक के रूप में, उससे भी ज्यादा एक स्त्री के रूप में.
कवितायें छोड़कर जब कहानियां लिखनी शुरु की निजी तौर पर बहुत उथल-पुथल का समय था. अपना शहर, अपना घर, अपने लोग सब छोड़कर आ चुकी थी; अपना परिवार भी… ज़िंदगी अपने दम पर चुनने का कोई जुनून था. पीछे छूटी लड़कियों और औरतों में से एक होना या बनना नहीं चाहती थी मैं. पर यह इतना असान भी तो नहीं था. आर्थिक समजिक और पारिवारिक कारणों के मद्देनजर बाहर निकलने, पढ़ने जाने की बात हर सिरे से मुश्किल थी. पर कुछ आसन सा करने का शौक भी तो नहीं था. एक परीक्षा देने दिल्ली आई फिर लौटी ही नहीं. राकेश वहां पहले से थे. हमने साथ-साथ रहना शुरु किया; पर वैसा भी कोई साथ नहीं. हम कई लोग मिल कर एक फ्लैट शेयर करते थे, जिसमें लड़की सिर्फ मैं. आरंभिक चिंता पहचान बनाने से ज्यादा कुछ पैसे कमा कर लान की थी. कला, साहित्य, स्त्री और समसामयिक मुद्दों पर लिखे अखबारी लेखों ने रहने-खाने लायक पैसे दिये और धीरे-धीरे एक पहचान भी. आर्थिक दिक्कतें धीरे-धीरे ठीक हो रही थीं पर मेरी दुश्चिंतायें दूसरी थीं. लगातार दवाब बनाता परिवार, अपने भीतर के आदिम और थोपे हुये संस्कारगत भय और कुछ हदतक सामाजिक मजबूरियां भी. मै लड़ रही थी लागातार अपने आप से, अपने पूर्वानुभवों से, अपने आसपास से और उन से भी जो मेरे सबसे ज्यादा अपने थे. लगभग साढ़े तीन-चार साल का वह समय बहुत कठिन था; पर अपने लिये खुद चुनने और कुछ कर पाने का अहसास भी मेरे भीतर कुलांचे मार रहा था. मेरी इन्हीं भावनाओं ने मेरी आरंभिक कहानियों का बाना लिया. ‘भय’, ‘मेरी नाप के कपड़े’ और ‘आ-शियाना’ मेरे और मेरे भीतर बैठी स्त्री के मानसिक, पारिवरिक और सामाजिक संघर्षों के ही तीन आयाम हैं.
मैंने इन कहानियों में बतौर स्त्री ‘लिव इन रिलेशन’ के आधुनिक जीवन पद्धति और परंपरागत विवाह संस्था के द्वन्द्वों को अपने अनुभवों के आधार पर पकड़ने की कोशिश की है. मेरा मानना है कि एक स्त्री के लिये ‘लिव इन रिलेशन’ महज एडवेंचर नहीं होता बल्कि इस जीवन शैली के तहत वह एक ऐसा प्रयोग कर रही होती है जिसमें स्त्री और पुरुष किसी परंपरा के तहत मजबूरी में नहीं बल्कि आपसी समझ और सूझबूझ के आधार पर एक दूसरे के साथ रह सकें. और यह अनायास नहीं होता. व्यक्तिगत , पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर तरह-तरह के भय और अन्तर्द्वन्द्व उसके साथ चलते हैं. आन्तरिक और बाह्य जगत के इस डर और असुरक्षाबोध की कुछ स्वाभाविक और स्त्रीजन्य छवियां आप भी देखिये –
“सीढ़ियां चढ़ने के क्रम में पता नहीं कैसे यह भय मेरे पीछे आ लगा. दिन भर का सारा सोचा-समझा पानी में. पर इसमें मेरा क्या दोष है. एक तो दरवाजा इतनी देर पर खुला, उस पर सामने इतना अजीब दृश्य. मैं कोई काठ-पत्थर की बनी हुई हूं…” (भय)
“मैं बिना कुछ बोले ऑटो में बैठ चुकी हूं पर जाने क्यों लगता है जैसे रवि को अंतिम बार देख रही हूं… मैं चाहती हूं यह याद करूं कि रवि मुझ पर अपनी इच्छाएं थोपता है, मुझसे लड़ता है, मुझपर गुस्साता है… पर ऐसा कुछ भी याद नहीं आता… रवि का उदास चेहरा बार-बार मेरे आगे आता है… कोई जरूरत हो, मुश्किल हो तो मुझे तुरन्त फोन करना…” (मेरी नाप के कपड़े)
“दो वर्ष तेरह मकान. तमाम जिल्लतें … क्या यही है उसकी तलाश की मंजिल. कहीं वह पीछे की ओर तो नहीं लौट रही… बढ़ते-बढ़ते पीछे लौट आना, यह कौन सी मंजिल है उसकी यात्रा की. क्या आगे बढ़ना ही गंतव्य का रास्ता है? पहले हम समझें कि हमे चाहिये क्या… कोई दूसरा क्यों नियत करे हमारी जय-पराजय, हमें सीखना तो अपने अनुभवों से ही होगा.” (आशिया-ना)
मेरी छोटी-छोटी लड़ाईयां, छोटी-छोटी जीत, छोटी-छोटी हार सबको मेरी कहानियों ने दर्ज किया और अपनी इन छोटी-छोटी उपलब्धियों और उसके अंकन ने अपने कुछ अलग कुछ विशिष्ट होने की अनुभूति तो जगाई ही, अपने ऊपर विश्वास करना भी सिखाया; अपने लेखन पर भी –
“ख्वाहिशों और ज़िंदगी के बीच बड़े गहरे फासले थे. उसके हिस्से तो बस दो-चार बूंदें थीं – खारी, छिछली, नमकीन. इतने से उसकी चाहत कम होती भी तो कैसे” (यह डर क्यों लगता है)
अब सोचती हूं तो हैरत होती है कि इस सारी कालावधि में राकेश (राकेश बिहारी, अब मेरे पति) भी तो मेरे साथ ही थे. कमोबेश उन्हीं स्थितियों-परिस्थितियों से गुजरते हुये और कहानियां भले ही प्रकशित न होने को भेजी जा रही हों पर सृजन के स्तर पर तो हम सहयात्री ही थे. ‘और अन्ना सो रही थी’, ‘बाकी बातें फिर कभी’ और ‘फांस’ जैसी उनकी कहानियां भी उसी कालावधि में तो लिखी गई हैं. पर इन कहानियो का फलक मेरी कहानियों से बिल्कुल भिन्न हैं. जहां मेरी कहानियों का संबंध मुझसे और मेरे अन्त्तर्जगत से है, राकेश अपनी कहानियों में कम हैं या कि गौण पात्र के रूप में. उनकी कहानियों का नाता बाह्य जगत और उसकी घटनाओं से है. शायद यह स्त्री और पुरुष की सोच का फर्क हो याकि फिर मेरे और उनके लिये कहानियों के विषय चुनने का, पर यह तो तय है कि जो बातें मेरे लिये महत्वपूर्ण थीं उनके लिये गौण. छोटे-छोटे सुख-दुःख उन्हें या तो व्यापते ही नहीं थे या कि उन स्थितियों से स्त्रियों को ही गुजरना होता है ज्यादातर. कोई चाहे तो उनके सरोकारों को बड़ा और मेरी दुनिया को छोटी कह सकता है. आखिरकार हमारा सामाजिक ढांचा भी तो पुरुषों को विशिष्ट और अलग होने की छूट देता ही है.
धीरे-धीरे मेरी कहानियां विकसित हो रही थीं. खुद से निकल कर यह कथायात्रा अब मां तक पहुंच गई थी. विधवा मां का दुःख, अकेलापन… मैं सोचकर सिहर उठती, जिस उम्र में मैं अपनी ज़िंदगी चुनने का निर्णय लेती या उसे लेने की भूमिका तय करती हूं तेरह की उम्र में ब्याही मां तबतक नौ बच्चों (सात जीवित और दो मृत) को जन्म देकर एक विधवा के बाने में आ चुकी होती हैं. यह त्रासदी कोई छोटी त्रासदी नहीं थी. मां के दुःख से मन भीतर तक द्रवित होता पर कुछ भी कर पाने या कि बदल पाने में मैं अपनी कहानी ‘नीमिया तले डोला रख दे मुसाफिर’ की प्रीति की तरह ही असमर्थ थी. मां का एकांत था कि कमता नहीं था और मुझे बस मूक दर्शक की तरह उसे देखते रहना था – ” मैं चौके तक पहुंची ही थी कि जैसे किसी की उपस्थिति के भान से सहमकर चक्की की घर्र-घर्र बन्द हो चली थी, साथ में मां का पिघलता-गलता स्वर भी – अम्मा कहे बेटी निस दिन अईयो, बाबा कहे छह मास रे… भैया कहे बेटी जग ही परोजन, भाभी कहे क्या है काम रे… मां की दृष्टि में मुझे देख कर एक राहत भाव तैरा था. तू है. मैं तो सोच रही थी कि किशोर लौट आया. इसी से भय लगा. मैने मां के कंधे पर अपनी संवेदना भरी हथेलियां रखी थी कि वह फूट-फूट कर रो पड़ी. पूरी ज़िंदगी में उन्हें पहली बार इस तरह रोते पाया था.” (नीमिया तले दोला रख दे मुसाफिर)
मां का अकेलापन, भरे-पूरे परिवार के होते हुये भी उसका अकेली और निहत्थी होती जाना जैसे कोंचते रहते मुझे, लगातार. एक जिरह निरंतर चलती रहती मेरे भीतर – ” मां ही क्यो थमी रहे आजीवन उसी मोड़ पर जिसकी चाह उसे नहीं थी… जब धरती, आकाश, ग्रह-नक्षत्र सब घूमते रहते हैं अपनी धुरी पर, नदियां बदल देती हैं अपना रास्ता फिर मां से अथाह धीरज की अपेक्षा क्यों? मां पर्वत नहीं थी. और पर्वत भे तो टूटता-छीजता है समय के साथ-साथ.” हम भूल चुके हों पर आदिम सुख-दुःख उन्हें भी व्यापते थे. इस निरंतर चलती बहस ने ‘नीमिया…’ के लगभग सात वर्षो बाद ‘उलटबांसी’ की रचना करवाई. ‘नीमिया…’ की मां-बेटी को जैसे इस कहानी में विस्तार मिल गया था. लेकिन यह सिर्फ कथ्य की ही नहीं मेरे कथाकार की भी विकासयात्रा थी और मेरे भीतर बैठी स्त्री की भी. ‘उलटबांसी की प्रौढ़ा मां अपने अकेलेपन से ऊबकर-टूटकर विवाह का निर्णय लेती है और पूरे परिवार के विरोध के बावजूद उस निर्णय में उसकी बेटी और पोती उसके साथ खड़ी होती हैं. बेटी तो अपने परिवार के टूटने की आशंका के बाद भी. ” निशा ने उनके कंधे पर सिर रख दिया है, मैने उनकी कलाईयां अपने हाथों में ले ली है. अब हम तीन पीढ़ी की औरतें नहीं. दादी, बुआ और पोती तो बिल्कुल भी नहीं. बस तीन स्त्रियां हैं, तीन बहनें या फिर तीन सहेलियां. समय ने अपने चारों तरफ से अपनी चौहद्दी हटा ली है. वह मूक सा खड़ा कोने से ताक रहा है, हम तीनों को. हमारी चुप्पी बतिया रही हैं आपस में बहुत सारी बातें… निशा कब बड़ी हो गई हमें पता ही नहीं चला… औरत कब बड़ी हो जाती है कौन जान पाता है.” (उलटबांसी)
इस कहानी को लिखकर मैं अपने वर्षों पुराने उस द्वन्द्व से जैसे निवृत्त हो चुकी थी, अपने ऊहापोह से भी. पर मूल चुनौती तो सामने अब आनी थी. जो यात्रा मैंने सात वर्षों में पूरी की थी, वह दूसरों की तो बिल्कुल भी नहीं थी. अमतौर पर पुरुषों के समझ से तो बिल्कुल परे की. पहली दृष्टि में तो राजेन्द्र जी ने ही इसे बकवास करार दिया… बूढ़ी मां अचानक शादी कैसे कर सकती है, कौन मिल जायेगा उसे?.. वह बूढ़ी नहीं है, प्रौढ़ा है. और गर पुरुषों को मिल सकती है कोई, किसी भी उम्र में तो फिर औरत को क्यों नहीं?.. होने को तो कुछ भी हो सकता है, तू मेरी मां हो सकती है, यह (राकेश) तेरा पिता हो सकता है… लिख डाल एक और कहानी… बातें खिंचती-खिंचती लम्बी खिंच गई थी और जो भी उस दिन हंस के दफ्तर में आता उस बहती गंगा में हाथ धो डालता. गौरीनाथ जी को तो उज्र था ही, ओमा जी (ओमा शर्मा) भी उस दिन वहां आये थे और बिना कहानी पढ़े बस विषय के आधार पर ही उसे खारिज कर गये. मेरे भीतर उस दिन बहुत कुछ टूट-बिखर रहा था… क्या मुझे कहानी लिखना छोड़ देना चाहिये..? राकेश के यह कहने पर कि ‘सब की पसन्द एक सी नहीं होती तुम इसे किसी और से भी पढ़वा कर देखो’, मैने वह कहानी अरुण प्रकाश जी को पढ़ाई थी. कहानी उन्हें पसंद आई थी. उन्होंने मेरा मनोबल भी बढ़ाया. सोचा था कहानी उन्हीं को दूंगी लेकिन टाईप होने के बाद राजेन्द्र जी ने कहानी दुबारा पढ़ने को मांगी. उन्हें पुनः कहानी दे कर मैं अभी घर तक लौटी भी नहीं थी कि उनका फोन आ गया था ‘मुझे कहानी पसंद है, मैं रख रहा हूं किसी कौर को मत देना. पर एक आपत्ति अब भी है मेरी…कहानी से एक पात्र सिरे से नदारद है… वह कौन है.. कहां मिला, कैसे मिला कुछ भी नहीं… मुझे उसकी जरूरत नहीं लगती.. कहानी मां और बेटी के बदलते संबंधों की है… मैंने तर्क दिया था, अपूर्वा के भीतर की स्त्री अपनी मां के निर्णय में उसके साथ है. लेकिन उसके भीतर की बेटी अपने पिता की जगह पर कैसे किसी और को देख कर सहज रह सकती है. इसलिये बेहतर है वह अपनी मां के नये पति के बारे में ज्यादा दिलचस्पी न दिखाये. राजेन्द्र जी भी अंततः मान गये थे. आज उन्हें यह मेरी कहानियों में शायद सबसे ज्यादा पसन्द है. राजेन्द्र जी अपने भीतर के पुरुष से लगातार संघर्ष करते हैं. उनकी यही खासियत उन्हें औरों से अलग करती है.
खैर, धीरे-धीरे मुझे यह महसूस हुआ कि इसमें किसी का दोष नहीं था; यह अचानक ग्राह्य हो जानेवाली बात भी नहीं थी, खास कर पुरुषों के लिये. मां शब्द ही हमारे यहां इतनी गरिमा त्याग और धैर्य का पर्याय है या कि बना दिया गया है कि उसके मामले में कोई छूट उसकी तथाकथित छवि से खिलवाड़ लगता है. ये बातें सिर्फ इसलिये कि इस कहानी को स्त्रियां जितनी जल्दी स्वीकार कर पाती हैं, पुरुष इतनी आसानी से नहीं कर पाते. आज इस कहानी को खुले मन से स्वीकार करने वाले कई मित्रों को भी मैंने तब ऊहापोह की स्थिति में देखा था. इसलिये यह कहानी कोई औरत ही लिख सकती थी. अन्यथा पुरुष के लिखने पर यह ‘तलाश’ (कमलेश्वर) हो जाती जहां मां बेटी की नजर मे ंएक खल चरित्र बन कर ही उभरती है और सहानूभूति योग्य नहीं हो पाती.
धीरे-धीरे मेरी दृष्टि अब ‘मैं’, ‘मां’, ‘परिवार’, ‘पास-पड़ोस’ से इतर स्त्री जगत के उन सारे संघर्षों को भी देखने लगी थी जिनके रास्ते और जिनकी दुविधायें दूसरी या नये तरह की हैं. इन स्त्रियों के मन तक पहुंचना तब और ज्यादा जरूरी लगने लगता है जब मैं अपने पुरुष कथाकार मित्रों की कहानियों में इन स्त्रियों को सिर्फ महत्वाकांक्षी, मौकापरस्त और मतलबी चेहरों की तरह पाती हूं. ऐसे में मंजिल की तलाश में जीवन के साथ रस्साकशी करती स्त्रियों की कहानियां लिखना खुद को उनके साथ एकाकार करना भी लगता है. ऐसा करते हुये मैं अपने ‘मैं’ को ही खुरचती-परखती और पुनर्सृजित करती हूं; एक स्त्री के रूप में, आधी आबादी की एक प्रतिनिधि के रूप में.
भले ही वह एक अखबारी खबर रही हो पर वह और उस जैसी आंखों के आगे से गुजरनेवाली कई अन्य खबरों की दहला देने वाली स्मृतियां ‘देहदंश’ के लेखन का कारण बनी. मैं प्रश्नों से बिंधी हुई थी. आखिर क्यों एक इंसान पल भर में किसी बनैले पशु में तब्दील हो जाता है? वे कौन से कारण हैं जो पिता जैसी पूज्य छवि को भी किसी दरिंदे में परिवर्तित कर देते हैं?. कैसी होती होगी उस बेटी की ज़िंदगी, उस ज़िंदगी की त्रासदी? ‘देहदंश’ में मेरे ‘मैं’ ने पिता द्वारा बलात्कृत एक ऐसी ही लड़की का जामा ले लिया था. वह कोई तूफानी रात थी जब रात के बारह बजे से सुबह चार बजे तक कलम रुकी नहीं थी पल भर को; सुबह शरीर ऐसा टूटा हुआ जैसे कि वह सबकुछ मेरे ही साथ घटा हुआ हो. ‘देहदंश’ कई लोगों को बहुत पसंद आई, कईयों को ‘भयानक’ भी लगी. कथाकार संजीव तब इस कहानी की निंदा करते न थकते थे. एक पाठक ने तो पत्र लिख कर यहां तक कह डाला कि ‘आपके घर में होता होगा यह सब, पर हमारे घर की बेटियों को अपने घर में सुरक्षित रहने दें’. पर सच कहूं तो यह कहानी अपनी कहानियों में मेरी एक पसंदीदा कहानी है; मेरे अपने ‘मैं’ की विकासयात्रा और उसके परकाया प्रवेशी विस्तार की भी.
हंस के जिस अंक में यह कहानी छपी थी उसमें एक और कहानी थी जिसके केंद्र में पिता द्वारा बलात्कृत बेटी थी. कहानी थी अजय नावरिया की ‘ढाई आखर’. मैंने यानी एक स्त्री ने जब इस कहानी को लिखा कहानी बलात्कार की उस घ्टना से आगे निकल कर ज़िंदगी की रौ में बह निकलने के निर्णय तक पहुंची; पिछला सबकुछ भूल कर एक पूर्ण ज़िंदगी जीने और चुनने की चाहत और सपने के रूप में. लेकिन अजय की ‘ढाई आखर’ की समीरा की ज़िंदगी वहीं, उसी विंदु पर बंद घड़ी की सूई की तरह अटकी रह जाती है. एक स्त्री होना कैसे हमारी कहानियों को प्रभावित करता है उसे इन दोनों कहानियों के अंतर से भी समझा जा सकता है.
हर काल में स्त्री और पुरुषों के लेखन और लेखन शैली में अंतर रहा है. हिन्दी कथा इतिहास के प्रारंभिक दौर में जब पुरुष लेखक स्त्री के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुये ‘विधवा
9 thoughts on “वे कहानियां नहीं हुई होती अगर मैं स्त्री नहीं होती”
Leave a Reply
1 mins








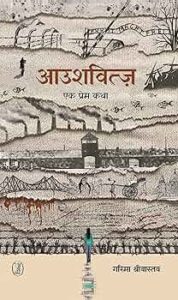

काफी खूबसूरत बयान है। कविता के लेखन में एक अन्दरूनी सन्नाटा है। कविता की खूबी यही है कि उसकी रचना का चेहरा निहायत व्यकितगत है,उस में झांकिए तो अपनी और वक्त का चेहरा झांकने लगता है।
वे कहानियां नहीं हुई होती अगर मैं स्त्री नहीं होती …
मैं अपनी ही कहूं तो आपकी कहानियां पढ़कर जो छवि आपकी मेरे मन में बंधी थी…वही तो सब कुछ
आपने यहाँ लिखा है …हां ! कुछ पर्सनल आपकी जद्दोजहद का पता अभी-अभी चला …दिल्ली के वो
सात साल।
बहुत चाव और निष्ठा से पढ़ी है आपकी कहानियां कविता जी…
और सिर्फ बहार से मॉडर्न दिखती शहरी लड़कियों के अंतरंग को भी तुम्हारे द्वारा बखूबी जाना-पहचाना…स्त्री-पुरुष के
आधुनिक संबंधों की घुटन इन कहानियों के ज़रिये महसूस की …उन संबंधों की सार्थकता और निरर्थकता भी
आपकी कहानियों ने उनकी अपनी ही आंतरिक प्रक्रिया द्वारा दर्शाई …एक स्त्री का दृष्टिकोण और उसके संबंधों की
सार्थकता का हासिल क्या हो, और उसकी (स्त्री की) पुरुष द्वारा सिर्फ जातीय उपयोगिता का सहज मंथन आपकी
कहानियों में मिला …स्त्री की चाहत, रिश्तों की सच्चाई व करूणा यहां इन कहानियों में नियुक्त रही …
कहानियां आपकी व्यर्थ नहीं…जो पढ़ेगा उसी के काम भी आएगी। स्त्री को तो कुछ ज्यादा ही पर पुरुष को भी एक
संवेदनशील दोस्त-प्रेमी होने का एहसास कराए और स्त्री के जीवन, सुख-दुःख और विकास का सहभागी भी बनाए …
आधुनिक नागरिक परिवेश में स्थित जागरूक व सच से प्रतिबद्ध, और अपनी अभिव्यक्ति के लिए भी बद्ध स्त्री की
मनःस्थिति का निरूपण करने में आप अन्य आधुनिक लेखिकाओं में कहीं पहली-पहली सी महिला लेखिका भी लगो …
आप बनी रहे और आपके अनुभवों की आधुनिक अभिव्यक्ति भी होती रहे …आपकी उन सारी पहली कहानियों के
दर्ज होने के अलावा भी 'खजुराहो … ' कहानी आपको फिर से स्थापित करती है …और आप अपनी आने वाली
कई नई कहानियों के ज़रिये अपने आपको स्थापित करती रहे यही दुआ …एक फ़ोर्स है आपके लेखन में …और
एक सहज शिल्प भी …आपका लिखा असहज कभी नहीं होता …क्योंकि इतना तादात्म्य आप कर पाती हो अपने
पात्रों से या कहूं अपने आपसे…परिवेश और शिल्प के तानेबाने सहज ही बंधे होते हैं कहानियों में और पंक्ति-दर-पंक्ति
आपका लिखा पठनीय हो उठता है …
आधुनिक लेखन और स्त्री-पुरुष के अंतरंग सत्यों या असत्यों की बयार सदा बहती रहे आपके लेखन में …और
आज की हमारी विषम आर्थिक, शारीरिक, मानसिक और सामाजिक इत्यादि जीवन परिस्थितियों में एक 'जीने लायक
जीवन सूत्र भी उजागर होता रहे आपकी कहानियों में…जो अब तक होता रहा है …आगे भी होता रहे ..
This comment has been removed by the author.
बहुत सुंदर , बेबाक और पारदर्शी प्रस्तुति ..
.स्त्री का लेखन ही अपने आप में संघर्ष है ..
अल्पना मिश्र का वागर्थ सम्मान के समय दिया वक्तव्य याद आ रहा है ठीक इसी वक़्त. आज लिख रही हर औरत इस तरह के संघर्षों से निकल के ही आ रही है…यही उसे और-और मज़बूत बना रहा है.
लिखना मेरे लिये एक यातना है, अपने पाने की बेचैनी, उसे पकड़ पाने की विकलता. ‘मैं’ आकर घेर लेता है मेरी बृहत्तता. ‘मैं’ मुझे सीमाओं में बांध देता है. ‘मैं’ के बिना मैं अवरोध रहित होती पर ‘मैं’ मेरे लिये एक चुनौती है. अपने को उघाड़ना, अपनी परतें खोलना ज्यादा दुःसाध्य है. ‘मैं’ मेरे लेखन पर इल्जाम भी बना रहा. पर मैने इस मैं को बार-बार खुरचा, परखा, रचा और पुनर्सृजित किया है. हां, इस क्रम में कई बार दूसरों के अनुभवों को भी मैं पहले ‘मैं’ की कसौटी पर परखती हूं; एक लेखक के रूप में, उससे भी ज्यादा एक स्त्री के रूप में. कवितायें छोड़कर जब कहानियां लिखनी शुरु की निजी तौर पर बहुत उथल-पुथल का समय था.अपना शहर, अपना घर,अपने लोग सब छोड़कर आ चुकी थी; अपना परिवार भी… ज़िंदगी अपने दम पर चुनने का कोई जुनून था. पीछे छूटी लड़कियों और औरतों में से एक होना या बनना नहीं चाहती थी मैं. पर यह इतना असान भी तो नहीं था. आर्थिक समजिक और पारिवारिक कारणों के मद्देनजर बाहर निकलने, पढ़ने जाने की बात हर सिरे से मुश्किल थी. पर कुछ आसन सा करने का शौक भी तो नहीं था….
सच आज भी घर परिवार के बीच से निकलकर एक स्त्री के लिए लिखना एक दुसाध्य काम है …आपने संघर्ष के बीच अपना एक मुकाम कायम किया है यह देखकर बहुत ख़ुशी हुयी..
सुन्दर प्रस्तुति के लिए धन्यवाद ..नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाओं सहित सादर…
सबसे पहले कविता जी को बधाई कि उन्होने जिस बेबाकी से अपनी बात रखी है वह वाकई सराहनीय है। उनकी साहित्यिक यात्रा दिल को छू लेती है। उनके प्रमाणिक अनुभव स्त्री जीवन के कई पक्षों को खोलते है।
महिला लेखन के संदर्भ में मुझे महिला लेखन में सामाजिक सरोकारों का अभाव देख बेहद निराशा होती है। महिला लेखन पूरा देह विमर्श के आस-पास ही सिमट गया है। सारी संवेदनाएं अपने सुख दुख को लेकर ही व्यक्त हो रही है। महिला लेखन का दायरा तेजी से सिमटता जा रहा है। पता नही मैं सही हूँ या गलत मुझे स्त्रियों द्वारा लिखी और स्त्रियों को लेकर और लोगों द्वारा लिखी जा रही अंधिकांश कहानियों में स्त्री को "सेक्स सिंबल बनने और बनाने" का पूरा षडयंत्र नजर आ रहा है। इन कहानियों में आम व साधारण मेहनती संघर्षशील स्त्री लगातार गायब होती जा रही है। इन स्त्रियों की जगह अब संबधों में अराजक व बेईमान, यौन कुंठित, स्त्रियों हिरोईन की तरह पेश की जा रही है और यह सब "स्त्री मुक्ति" और "स्त्री स्वतंत्रता" के नाम पर पेश किया जा रहा है।
कोई भी स्वतंत्रता या मुक्ति बिना सरोकार या मानवीय मूल्यों के बिना नही होती। और हम सब की स्वतंत्रता और मुक्ति एक दूसरे के सरोकारो और संवेदनाओं को साथ जुडी है। इन संवेदनाओं का दायरा मनुष्य से लेकर समाज तक जुडा हुआ है।
एक लेखक भी वक़्त के साथ "ग्रो " होता है .शायद कुछ वक़्त के बाद उसमे भी किसी फिल्मकार की तरह कुछ नया "रचने " का साहस होता है अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आकर .शायद आते वक़्त में कागज में "जेंडर "से स्वतन्त्र हो ने की प्रक्रिया भी . इससे उसका पिछला रचा महत्वहीन नहीं होता न गैर सरोकारी पर उसकी रेंज बढती है शायद तजुर्बे हमें ओर अधिक मनुष्य बनाते है
calm jazz