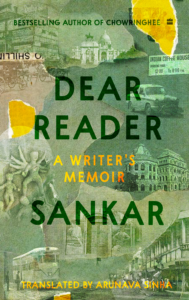पिछले महीने अभिनेत्री कामिनी कौशल का निधन हो गया। उन्होंने अभिनय के विभिन्न आयामोँ को छुआ। नई पीढी उन्हें चरित्र अभिनेत्री के रूप मेँ जानती है। चालीस के दशक मेँ अशोक कुमार और दिलीप कुमार के साथ उनकी कई फिल्मोँ बड़ी हिट रहीं। उनके अवदान को उन पर फिल्मायें गीतों के बहाने याद करता हुआ प्रचण्ड प्रवीर का आलेख जानकीपुल के पाठकों के लिये – मॉडरेटर
=========================
जाना ना दिल से दूर आँखोँ से दूर जाके – कामिनी कौशल और हिन्दी सिनेमा का स्वर्ण-युग
बीसवीँ सदी के भारतीय मौलिक चिन्तक यशदेव शल्य की विचार-व्यवस्था का प्रारम्भ इस सूत्र से समझा जाता है — हम जगद्भाव को प्राप्त चैतन्य हैं, किन्तु यह भाव चेतना के लिये अनिवार्य नहीँ है।
सरल शब्दोँ मेँ हर व्यक्ति को यह दुनिया मिलती है। इसमेँ सुन्दरता और कुरूपता, प्रिय और अप्रिय, हितकारी और अनिष्टकारी के निर्णय से बहुत पहले परिवार, भाषा, परम्परा, सम्बन्ध, मूल्य, ऐतिहासिक अवस्था, भौगोलिक परिस्थिति आदि स्वाभाविक रूप से अनिवार्यतः मिलते हैँ। हर मनुष्य की चेष्टा होती है कि मिली हुयी इस दुनिया मेँ अपने मुताबिक दुनिया बनाये, जहाँ उसका राग, उसकी कला, उसका अभीष्ट अपेक्षित नवीन रूप मेँ साकार हो सके।
प्रदत्त जगत् के स्वरूप की सामग्री मेँ अब फिल्मोँ का महती प्रभाव है। लेकिन यह भी विविध रूप मेँ प्रकट होता है। उदाहरण के लिये अशोक कुमार से पहला परिचय बचपन मेँ टीवी सीरियल ‘हमलोग’ मेँ आने एक थके-हारे बूढ़े के रूप मेँ हुआ। यह यकीन करना कठिन लगता था कि अशोक कुमार कभी फिल्मोँ मेँ नायक भी रहे होँगे। उसी तरह कामिनी कौशल (२४ फरवरी १९२७ – १४ नवम्बर २०२५) से परिचय भी विचित्र रूप से हुआ, प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री की तरह नहीँ। नवेँ दशक मेँ दूरदर्शन पर ‘चाँद-सितारे’ नाम का धारावाहिक आया करता था जिसमेँ वे कठपुतलियोँ और गुड़ियोँ के साथ आती थीँ। कामिनी कौशल की कहानियाँ बच्चोँ की पत्रिका ‘पराग’ मेँ आया करती थीँ। बड़ोँ ने परिचय कराया था कि कामिनी कौशल किसी जमाने मेँ फिल्म तारिका थीँ। यह भी विश्वास करना भी बहुत ही कठिन था ठीक उसी तरह दूरदर्शन मेँ अन्य धारावाहिक (दादा दादी की कहानियाँ) मेँ आने वाले भारत भूषण के फिल्मोँ के नायक होने की सम्भावना। शायद नायक का प्रारूप अमिताभ बच्चन की तरह बड़े बाल रखने वाला और मार-धाड़ करने वाला और नायिका का प्रतिदर्श श्रीदेवी की तरह चुलबुली छवि ही होगी।
कामिनी कौशल से फिर भेँट मनोज कुमार की फिल्म ‘शहीद’ (१९६५) मेँ भगत सिंह की माँ के रूप मेँ हुआ। जब दूरदर्शन पर ‘शहीद’ फिल्म दिखा गयी थी, उस समय भगत सिंह की माता जीवित थीँ। हमारे छोटे से शहर मेँ ‘भगत सिंह चौराहा’, भगत सिंह की माँ के दौरे के बाद बनाया गया था। हमारे लिये भगत सिंह ही नहीँ, बल्कि उनकी माँ भी आदर्श थीँ।
पर इन सबके बावजूद कामिनी कौशल की मानसिक चित्रण एक कमनीय आकर्षक अभिनेत्री के रूप मेँ करना कठिन था। जिस तरह सुरैय्या, नर्गिस, मधुबाला, सुचित्रा सेन, वैजयन्तीमाला, साधना, सन्ध्या, कल्पना कार्तिक आदि अभिनेत्रियोँ ने फिल्मोँ मेँ मुख्य चरित्र के अलावा किसी भूमिका को निभाने से मना कर दिया, उक्त कारण से उनकी छवि मोहक रूपसियाँ जैसी रह गयीँ।
फिर भी नयी पीढी के लिये यह विचारणीय रह जाता है कि सिनेमा के स्वर्ण काल (चालीस और पचास का दशक) मेँ किस तरह कामिनी कौशल प्रभावशाली नायिका थीँ। कान्स फिल्म समारोह मेँ सम्मानित ‘नीचा नगर’ (१९४६) के अलावा, उनकी फिल्मेँ ‘आग’ (१९४८), ‘जिद्दी’ (१९४८), ‘नदिया के पार’ (१९४८), ‘शहीद’ (१९४८), ‘शबनम’ (१९४९), ‘आरजू’ (१९५०), ‘बिराज बहू’ (१९५४) और ‘गोदान’ (१९६३) उनकी अभिनय क्षमता और विविधता के लिये देखी जानी चाहिये।
स्वर्ण-युग कहने का तात्पर्य यह है कि फिल्म निर्माण की विधा के सभी अङ्ग मेँ विशारदोँ की गरिमामयी उपस्थिति। स्वर्ण-युग केवल प्रतिष्ठित अदाकारोँ या निर्देशकोँ से ही नहीँ जाना जाता, बल्कि उस समय की फिल्मोँ के अविस्मरणीय सङ्गीत पक्ष, गीतोँ के बोल, पटकथा, संवाद, छायाङ्कन, सम्पादन, प्रेक्षकोँ मेँ कला की स्वीकृति और आदर से जाना जाता है। उदाहरण के लिये यदि पूछ लिया जाय कि समकाल मेँ प्रतिष्ठित पाँच सङ्गीतकार, पाँच गीतकार, पाँच गायक-गायिका, छायाकार के नाम कौन-से हैँ और उनकी उपलब्धि क्या है? इसका सहज उत्तर नहीँ मिलेगा। हमारे वर्तमान के प्रतिष्ठित अभिनेता और अभिनेत्री वैसा आदर नहीँ पाते। वैजयन्तीमाला ने किसी साक्षात्कार मेँ गुजरे जमाने के बारे मेँ याद करते हुए कहा था कि उस समय अभिनेत्रियोँ को राजकुमारी और देवी सरीखा सम्मान और प्रेम मिलता था, जिसकी वर्तमान मेँ कल्पना भी नहीँ की जा सकती। इस बात से अस्वीकार नहीँ किया जा सकता है कि फिल्मोँ के प्रतिनिधि अदाकार की निर्मिति के पीछे कई योग्य कलाकारोँ का हाथ होता था। इस उत्कृष्टता ने सब कुछ सोना-सा दमकता बना दिया था।
पहली व्यावहारिक समस्या है कि अच्छी और हितकारी कलाकृति की तरफ इंगित करने पर भी कोई-कोई ही प्रेरित हो कर उसे देखना चाहेँगे। दूसरी समस्या यह है कि किसी कलाकार/कथाकार/उपन्यासकार को उसके समय के अनुसार समझना। वह समय जो बीत चुका होता है, अपने साथ बहुत-से अनुत्तरित प्रश्न समेटे दूर चला जाता है। हम अनुमान लगाते रह जाते हैँ और कभी-कभी विह्वल हो कर उसे ढूँढने निकलते हैँ, इतिहास के पन्नोँ मेँ, पुरानी कृतियोँ मेँ, लेकिन गया दौर कभी वापस नहीँ आता। फिर भी कोशिश कर सकते हैँ कुछ गीतोँ को याद कर के, जो खोये हुए का दामन पकड़ने का प्रयास करते हैँ।
मेरा सुन्दर सपना बीत गया…
कामिनी कौशल से अगला परिचय यूट्यूब पर गीतोँ और फिल्मोँ की सुलभता के कारण मधुर रूप से हुआ। इस परिचय का सूत्र जुड़ा है गीता दत्त से परिचित होने का। गीता दत्त से परिचय होने का कारण पिताजी के लाये हुए ऑडियो कैसेट्स मेँ उनकी प्रमुख गीतोँ के संकलन से हुआ था। मेरा सुन्दर सपना बीत गया, मैँ प्रेम मेँ सबकुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया – पहली बार सुनने मेँ बड़ा अटपटा-सा लगा। फिल्म ‘दो भाई’ (१९४७) के इस मधुर गीत से सचिन देव बर्मन, राजा मेहदी अली खान, गीता दत्त ऐसा साथ जुड़ा, जो संगी-साथी जैसे बन गये। जिज्ञासा थी कि यह गीत कैसे फिल्माया गया होगा। इस गाने मेँ ‘कामिनी कौशल’ विरहनी नायिका की भूमिका मेँ हैँ। यह फिल्म पारिवारिक स्थितियोँ के कारण हुये उनके बहुचर्चित विवाह से पहले की है।
किसी भारतीय नेता ने स्वतंत्रता के ठीक बाद, बँटवारे के घमासान के समय कामिनी कौशल को देखने के लिये रेलवे स्टेशन पर भाव-विह्वल भीड़ पर गहरी खिन्नता व्यक्त की थी। कामिनी कौशल सहगल युग के अवसान के ठीक बाद उदित होती हैँ। देखा जाय तो हिन्दी फिल्म की चर्चा मेँ से भारतीय मूक फिल्मेँ, सोहराब मोदी, मोतीलाल, कुन्दन लाल सहगल आदि को अलग के देखने मेँ ही हमने बुद्धिमानी मानी है। लेकिन इससे कई कलाकारोँ के अवदान को ठीक से नहीँ समझा जा सकता।
जिन्दा हूँ इस तरह कि ग़म+ए+जिन्दगी नहीँ …
अशोक कुमार की पहली ‘जीवन नैय्या’ (१९३६) के निर्देशक जर्मनी के थे। इस फिल्म मेँ जर्मन मूक फिल्मोँ का हैंगओवर स्पष्ट दिखता है। यहाँ तक के फिल्म के संवाद भी जर्मन फिल्मोँ की शैली मेँ एकहरे और एक सुर मेँ लगे हुए हैँ। उनमेँ मूकफिल्मोँ की पहचान ली जाने वाली नाट्यधर्मिता स्पष्ट है। अशोक कुमार को इस बात का श्रेय दिया जाता है कि उन्होँने हिन्दी फिल्मोँ मेँ स्वाभाविकता का समावेश किया। विश्व के अन्य महान फिल्म निर्देशकोँ की तरह ह्वी॰ शान्ताराम भी मूक फिल्मोँ से बोलती फिल्मोँ पर नहीँ आना चाहते थे, किन्तु आना पड़ा।
चालीस के दशक की फिल्मोँ मेँ अभिनय की सहजता का पदार्पण धीरे-धीरे हुआ। उदाहरण के लिये सहगल की देवदास (१९३६) आदि मेँ नायिका के संवाद बेजान तथा अरुचिकर हैँ, जिसका आज मजाक उड़ाया जाता है। कामिनी कौशल की शुरुआती फिल्मेँ अभिनय की सहजता लिये हुए है, पर उनमेँ आज का यथार्थवाद न हो कर नाट्यधर्मिता विद्यमान अवश्य है। यह नाट्यधर्मिता अनिवार्यतया प्रस्तुत नहीँ है। यह उनकी फिल्म आग (१९४८) मेँ देखी जा सकती है। कहीँ का दीपक, कहीँ की बाती,आज बने हैं जीवन साथी, देख हँसा है चाँद, मुसाफिर, देख चाँद की ओर — इस छोटे से गाने की क्लिप मेँ कामिनी कौशल का गम्भीर रूप देखा जा सकता है।
कामिनी कौशल को नायिका के रूप मेँ फिल्माया हुआ एक अन्य गीत ‘आग’ (१९४८) का ही है। बहजाद लखनवी की गजल — जिन्दा हूँ इस तरह कि गम+ए+जिन्दगी नहीँ, जलता हुआ दिया हूँ मगर रौशनी नहीँ — पर राम गांगुली के संगीत से सजे गीत मेँ बिना मूँछोँ के राज कपूर के गाते हुए विरह गान की पृष्ठभूमि मेँ नवोढ़ा बनी कामिनी कौशल को एक खिड़की के चौखटे पर तड़पता हुआ फिल्माया गया है।
चन्दा रे जा रे जा रे …
फिल्म पड़ोसन (१९६८) का प्रसिद्ध गीत ‘एक चतुर नार’ सबने सुना होगा। उस गाने मेँ एक पङ्क्ति आती है —काला रे, काला रे जा रे, जा रे, खारे नाले मेँ जाके तू मुँह धोके आ, काला रे गा रे गा रे… — यह पङ्क्ति देव आनन्द की शुरुआती हिट फिल्म ‘जिद्दी’ (१९४८) के प्रसिद्ध गीत – चन्दा रे, जा रे जा रे – पर आधारित है। लता मङ्गेशकर इस गीत से पहले साधारण चरित्रोँ के लिये गाया करती थी। इस गीत से लता ने फिल्म की नायिकाओँ के लिये मुख्य आवाज बन गयी। दिग्गज संगीतकार ‘खेमचन्द प्रकाश’ के संगीत से सजी इस फिल्म मेँ किशोर कुमार ने छोटा-सा रोल भी किया और अपना पहला गाना – मरने की दुआयेँ क्यूँ माँगूँ – भी गाया था। खेमचन्द प्रकाश की अगली फिल्म ‘महल’ (१९४९) ने लता मङ्गेशकर को पूरे भारत मेँ प्रसिद्ध कर दिया।
इस गीत के फिल्मांकन मेँ यह नोट किया जा सकता है कि नायिका की गतिविधियाँ एक छोटे स्थान तक सीमित हैँ। मूक फिल्मोँ और उसके दो दशक बाद तक के सिनेमा मेँ सिनेमा ‘नाट्य’ की परम्परा का अनुकरण करता नजर आता है, जहाँ सेट के छोटे होने की विवशता है। जिस तरह मूक फिल्मोँ मेँ आँगिक अभिनय और सात्त्विक अभिनय प्रधानता लेता है, वही परिपाटी चालीस के दशक तक चलती रही। वाचिक अभिनय को अत्यन्त महत्त्व देने का श्रेय हिन्दी फिल्म सिनेमा मेँ अशोक कुमार और दिलीप कुमार को जाता है। उसके साथ ही मंच सज्जा का विस्तार कैमरे के बदलते अंग तथा आउटडोर शूटिंग से होती गयी। इन दिनोँ एनिमेशन और एआइ से मञ्च सज्जा (तकनीकी शब्दावली मेँ ‘रङ्ग’) को ही मुख्यतः निखारा जा रहा है।
सिनेमा को मैँ ‘नाट्य’ ही समझता हूँ। दार्शनिक और तकनीकी विस्तार के लिये मेरी पुस्तक ‘अभिनव सिनेमा’ (२०१६) या उसका अँगरेजी अनुवाद ‘सिनेमा थ्रू रसा’(२०२१) देखी जा सकती है।
बदनाम ना हो जाय मोहब्बत का फसाना, ओ दर्द भरे आँसुओँ आँखोँ मेँ ना आना
गुलाम हैदर के संगीत, राजा मेहदी अली खान और कमर जलालाबादी के गीतोँ से सजी फिल्म ‘शहीद’ (१९४८) मेँ सुरेन्दर कौर का गाया गीत – बदनाम ना हो जाय मोहब्बत का फसाना – मेँ कामिनी कौशल धीर-प्रशान्त नायिका का चरित्र निभाती हैँ। फिल्म के अन्त मेँ – वतन की राह मेँ वतन के नौजवाँ शहीद होँ –गाने के अन्तिम संस्करण मेँ कामिनी कौशल के चरित्र की नाटकीय इच्छामृत्यु (हृदयाघात?) उनकी गम्भीरता निर्वाह कर लेती है।
दिलीप कुमार के साथ उनकी प्रसिद्ध रोमाण्टिक फिल्मोँ मेँ ‘शहीद’ (१९४८), ‘नदिया के पार’ (१९४८), ‘शबनम’ (१९४९) और ‘आरजू’ (१९५०) प्रमुख हैँ। ‘नदिया के पार’ मेँ मछुआरे की ग्रामीण कन्या के चरित्र मेँ वह सच मेँ भोली-भाली और कामिनी हैँ। सी॰ रामचन्द्र के संगीत वाले गीतोँ मेँ – मोरे राजा हो, ले चल नदिया के पार – को दिलीप कुमार और कामिनी कौशल के यौवन के लिये देखना-सुनना चाहिये। इस गीत मेँ चञ्चलता और अठखेलियाँ देखने लायक है।
कामिनी कौशल की इस दौर की फिल्मोँ मेँ मोहम्मद रफी, लता मङ्गेशकर, गीता दत्त और किशोर कुमार का पदार्पण होता है, जिनका प्रभाव हिन्दी फिल्म सङ्गीत के इतिहास मेँ लम्बे समय तक बना रहा। फिल्म ‘आरजू’ (१९५०) मेँ अनिल बिश्वास का अविस्मरणीय संगीत उनके करियर की महत्त्वपूर्ण उपलब्धि मेँ गिनी जाती है। कहाँ तक हम उठाये गम, जिये अब या कि मर जायेँ और जाना ना दिल से दूर आँखोँ से दूर जाके – लता मङ्गेशकर के गाये महत्त्वपूर्ण गीतोँ मेँ याद किये जाते हैँ।
हिन्दी सिनेमा के स्वर्ण-युग मेँ साहित्य
कामिनी कौशल के अभिनय कौशल की चर्चा करने के लिये दो फिल्मोँ का उद्धरण आवश्यक है। इसके लिये हम उनकी ‘बिराज बहू’ (१९५४) और ‘गोदान’ (१९६३) पर पुनर्विचार कर सकते हैँ, जोकि महत्त्वपूर्ण और लोक-प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियोँ पर बनी हैँ।
बिराज बहू
कामिनी कौशल को शरत चन्द्र चट्टोपाध्याय के दूसरे उपन्यास ‘बिराज बाउ’ (१९१४) पर आधारित ‘बिराज बहू’ (१९५४) के लिये बहुत सम्मान मिला। आज के समय मेँ बिमल रॉय द्वारा निर्देशित ‘बिराज बहू’ का पुनर्मूल्यांकन होने कदाचित ही प्रशंसा मिलेगी। कामिनी कौशल ने फिल्म बनने से पहले उपन्यास को दो ही बार पढ़ा था। बिमल रॉय ने कामिनी कौशल को उपन्यास को बीस बार पढ़ने की सलाह दी। इसका परिणाम यह हुआ कि फिल्म मेँ रीटेक या रिहर्सल बहुत कम ही हुए।
सत्यजित रॉय बिमल रॉय की ‘दो बीघा जमीन’ (१९५३) और बन्दिनी (१९६३) के प्रशंसक थे, शायद वे बिमल रॉय की अन्य कृतियोँ के प्रति सम्भवतः उतने उदार नहीँ थे। (‘सम्भवतः’ शब्द कहने का आधार मेरी स्मृति मेँ सत्यजित राय का कोई पुराना इंटरव्यू है, लेकिन अब वह नहीँ मिल पा रहा है अतः मैँ केवल अपनी स्मृति के संस्कार को प्रमाणतया उद्धृत नहीँ कर सकता। इस वक्तव्य को संदेहास्पद माना जा सकता है।) देवदास के उपन्यास पर आधारित बनी प्रारम्भिक फिल्मोँ लेकर सत्यजित रॉय बड़े अनुदार थे। सत्यजित रॉय ने रवीन्द्रनाथ ठाकुर, बिभूतिबिभूषण बंदोपाध्याय, शंकर, सुनील गंगोपाध्याय, प्रेमचन्द जैसे साहित्यकारोँ की कृतियोँ पर महत्त्वपूर्ण फिल्मेँ बनायी पर शरत् चन्द्र साहित्य ने उन्हेँ कभी आकर्षित न किया।
सम्पूर्ण शरत चन्द्र के साहित्य की आलोचना अभीष्ट नहीँ है किन्तु शरत साहित्य की कुछ महत्त्वपूर्ण वृत्तियाँ पहचानी जा सकती हैँ। जिस तरह प्रेमचन्द ने धनवान को बहुधा खलनायक बनाया और ईसाइयत के चर्च द्वारा प्रायोजित सेवा के अनुकरण मेँ सेवाधर्म को महाधर्म बना कर प्रस्तुत किया, उसी तरह शरत चन्द्र चटर्जी ने आवारा, शराबी और चरित्रहीन कहे जाने वाले चरित्रोँ को नैतिक निष्ठा से ओत-प्रोत दिखा कर उनका महिमामण्डन किया।
इस उपक्रम को साहित्यिक तकनीक समझना चाहिये। इससे अधिक उनका मूल्य नहीँ। ऐसा इसलिये कि साहित्य मेँ मूल्य-बोध अन्तिम कसौटी है। उससे पहले आकर्षण, पठनीयता, नवीनता, साधारणीकरण जैसे तत्त्व उसकी काया रचते हैँ। बिना काया की आत्मा भूत ही कही जाती है, जीव नहीँ।
‘बिराज बहू’ फिल्म मेँ बिराज बहू के चरित्र का महिमामण्डन करने के लिये बिमल रॉय ने मूल कहानी मेँ कुछ हेर-फेर किया, जो शायद अब किसी के संज्ञान मेँ नहीँ होगा। शरत चन्द्र को बिसराया जा चुका है और बिमल रॉय को सिने-इतिहास मेँ निपटा दिया गया है। किन्तु कामिनी कौशल के अवदान के पुनर्मूल्यांकन के बहाने हम एक बार फिर ‘सिनेमा मेँ साहित्य के रूपायन’ पर पहुँचते हैँ।
शरत चन्द्र के शुरुआती दौर का उपन्यास ‘बिराज बहू’ उनके अन्य उपन्यासोँ की तरह ही है, जिसमेँ पारिवारिक सम्बन्धोँ मेँ अनिवार्यतः उपस्थित ‘मोह’ का महिमामण्डन किया गया है। निश्चित तौर पर मोह ‘आनन्ददायक’ होता है, किन्तु हर आनन्द मोह का ही परिणाम नहीँ है। ‘तमो गुण’ का मौलिक स्वरूप दुःखपरक न हो कर ‘मोहात्मक’ होता है। आलस्य, निराशा तथा भ्रम आदि तमस गुण ही हैँ, जिससे मनुष्य मोहित हो उठता है। वहीँ यह भी कटु सत्य है कि संसार ‘मोह’, ‘भय’ तथा ‘सम्बन्ध’ से चलता है।
शरत चन्द्र के कथानक का मूल कथ्य सदैव सात्त्विक वृत्ति और तामसिक वृत्ति सम्मिश्रण रहा है। जिस तरह चार्ली चैप्लिन कभी हँसी को करुणा से अलग नहीँ करना चाहते थे, उसी तरह शरत चन्द्र ‘रजस’ के द्वेषी थे और ‘तमस’ के प्रति सहानुभूति रखने वाले थे। ऐसा उनके उपन्यास ‘बड़ी दीदी’(१९०७), ‘देवदास’ (१९१७), ‘चरित्रहीन’ (१९१७), ‘श्रीकान्त’ (१९१७-१९३३), ‘गृहदाह’ (१९२०) आदि मेँ प्रचुरता से मिलता है। शरत चन्द्र बहुधा आत्मघात को बलिदान, अश्रुमिश्रित अनावश्यक मोह को निर्मल प्रेम, छोटे-मोटे अहं के अव्यावहारिक मुद्दे को स्वाभिमान का नैतिक प्रश्न बनाने से नहीँ चूकते। शरत चन्द्र के चरित्र और कथ्य, फ्रेडरिक नीत्शे के शब्दोँ मेँ ‘दास नैतिकता’ के पैरोकार हैँ जो कि पतन का स्वाभाविक सूचक है। शक्तिशाली कभी न्याय की चीख-पुकार नहीँ करता, केवल दुर्बल करता है। नीत्शे के शब्दोँ मेँ ईसाइयत मेँ ‘दास नैतिकता की पैरोकारी’ उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है, जिसे ब्रह्म समाज ने खूब अपनाया। नीत्शे के लिये समाजवाद और मार्क्सवाद भी कुछ और नहीँ ईसाइयत की ‘दास नैतिकता’ की वकालत है। आमतौर पर यह ध्यान किसी का नहीँ जाता है कि यह महाभारत और पौराणिक विचारोँ के सर्वथा विरुद्ध है। और जिन्हेँ यह दृश्यमान होता है वे भारतीय विचारोँ को गालियाँ देते हैँ पर समझने का प्रयास नहीँ करते।
सम्भवतया उन्नीसवीँ सदी के उत्तरार्द्ध तथा बीसवीँ सदी के प्रारम्भ के समय के दुर्बल समाज मेँ नैतिक सुदृढता ही लेखकोँ और विचारकोँ को किसी तरह का सम्बल प्रदान करती होगी। पर ऐसा उत्कर्ष चरित्रहीनोँ मेँ ढूँढना आधारहीन आशावाद के अतिरिक्त क्या है? शरत चन्द्र के बहुत से प्रशंसक इस टिप्पणी से आहत हो सकते हैँ। कथ्य की पुष्टि के लिये ‘बिराज बहू’ पर ध्यान देना चाहिये।
कहानी का सार-संक्षेप यह है कि एक छोटा-मोटा भूस्वामी ‘नीलाम्बर चक्रबर्ती’ (फिल्म मेँ आभि भट्टाचार्य द्वारा अभिनीत) अपनी पत्नी ‘बिराज चक्रबर्ती’ (कामिनी कौशल द्वारा अभिनीत) के साथ बङ्गाल के किसी गाँव मेँ रहता है। साथ मेँ छोटे भाई और उसकी पत्नी भी हैँ। बहन के ब्याह के खर्च के विवाद को लेकर छोटा भाई बँटवारा करके अलग हो जाता है। वहीँ गाँव के नदी के पास एक अय्याश जमीन्दार (प्राण द्वारा अभिनीत) छुट्टियाँ मनाने आता है, जो कि अत्यंत रूपवती बिराज बहू पर बुरी नजर रखता है। शादी निपटाने के बाद कर्ज मेँ पड़े नीलाम्बर की आर्थिक दुर्दशा हो जाती है। मामूली सी बात पर नीलाम्बर और बिराज बहू मेँ कहासुनी हो जाती है। गुस्से मेँ नीलाम्बर बिराज बहू को बर्तन से मार बैठता है और कहता है कि वह उसके हाथ का पानी तक न पियेगा। बिराज बहू इसी बार पर रुष्ट हो कर नदी मेँ डूब कर आत्महत्या करने चली जाती है। शेष कथा मेँ डूबने से बची रूपहीन और निस्तेज बिराज बहू किसी तरह अपने घर यह मनोकामना लिये वापस आती है कि वह अपने स्वामी के चरणोँ मेँ जान देकर पतिव्रता स्त्री का धर्म निभा सके। कहानी का अन्त देवदास, बड़ी दीदी, चरित्रहीन आदि की तरह दुःखान्त है।
बिमल रॉय की पूरी फिल्म, उपन्यास की मूल कथा और संवादोँ का हूबहू अनुकरण करती है केवल बिराज बहू के आत्महत्या के प्रयत्न के प्रसङ्ग को छोड़ कर। मूल कथा से वह प्रसङ्ग उद्धृत किया जा रहा है: —
विराज का मरना ही उचित था, मगर वह मरी नहीँ। बहुत दिनोँ से वह दुःख-दैन्य से पीड़ित थी। अनाहार ओर अपमान की चोट से उसका दुर्बल मस्तिष्क विकृत हो गया था। उसी रात को मरने से ठीक पहले क्षण मेँ सम्पूर्ण रूप से उसने दूसरी राह पर पैर बढ़ा दिया। मौत को छाती पर रखकर जब वह अपने हाथ-पैर आँचल से बाँध रही थी कि ठीक उसी समय कहीँ बिजली गिरी और उस भयानक शब्द से चौँककर उसने सिर उठाया। बिजली के तेज प्रकाश मेँ उस पार का नहाने का वह घाट ओर मछली मारने के लिये बनाया गया लकड़ी का मचान उसकी नजर मेँ पड़ गया। लगा जैसे उसकी प्रतीक्षा मेँ आँखेँ खोले चुपचाप वे उसकी ओर देख रहे थे। नजर मिलते ही संकेत से उसे बुला लिया। सहसा भयानक स्वर मेँ विराज कह उठी – “वे साधु पुरुष तो मेरे हाथ का पानी तक न पिएँगे, मगर, यह पापी तो पियेगा! अच्छी बात है।“
लोहार की धौँकनी मेँ जलते हुए कोयले की तरह विराज के प्रज्वलित मस्तिष्क के सामने उसका अतुलनीय-अमूल्य हृदय भी जल-भुन कर राख हो गया। पति, धर्म और मृत्यु को भूलकर प्राणपण से वह उस पार के घाट की ओर देखने लगी। आकाश की छाती को चीरती हुई अन्धकार मेँ एक बार बिजली कड़कड़ाकर कौँध गई। विराज की फैली हुई नजर सिकुड़कर अपनी और चली आई। सिर बढ़ा कर एक बार उसने पानी की ओर देखा, गरदन घुमाकर एक बार घर की ओर देखा, इसके बाद बन्धन खोलकर पलक मारते ही वह अन्धेरे जङ्गल मेँ गायब हो गई। उसके कदमोँ की आवाज से खस-खस, सर-सर करके कितने ही जीव-जन्तु उसका रास्ता छोड़ कर हट गये, मगर उसने उधर ध्यान ही नहीँ दिया – वह सुन्दरी के पास जा रही थी। पंचानन ठाकुरतल्ले मेँ वह रहती थी। पूजा चढ़ाने जाकर विराज कई बार उसका घर देख आई थी। इस गाँव की बहू होने पर भी बचपन मेँ इस गाँव का करीब-करीब सब रास्ता वह जान गई थी। थोड़ी ही देर मेँ सुन्दरी की बन्द खिड़की के पास वह पहुँच गई।
इसके करीब दो घण्टे बाद ही कङ्गाली मल्लाह ने अपनी नाव उस पार के लिये छोड़ दी। कितनी बार रात को पैसे के लालच मेँ उसने सुन्दरी को उस पार पहुँचाया है, और आज भी ले जा रहा है। मगर, आज एक के बदले दो औरतेँ चुपचाप बैटी हैँ, अन्धेरे मेँ उसने विराज का मुँह नहीँ देखा, देखता तो भी पहिचान नहीँ पाता। अपने घाट के पास आकर दूर से ही अँधेरे मेँ किनारे पर एक धुँधले दीर्घ शरीर को सीधा खड़ा देखकर विराज ने आँखेँ बन्द कर लीँ।
— १४, बिराज बहू
मूल कथा की तुलना मेँ फिल्म मेँ बिराज बहू की पूर्व नौकरानी सुन्दरी (मनोरमा द्वारा अभिनीत), जिसे बिराज बहू ने जमीन्दार के प्रस्ताव देने के कारण घर से निकाल दिया था, अपने अपमान का बदला लेने के लिये बेहोश बिराज बहू को जमीन्दार के बजरे (बड़ी नौका) पर छोड़ आती है। होश मेँ आने पर बलात्कार से बचने के लिये बिराज बहू नदी मेँ कूद जाती है। वहीँ उपन्यास मेँ बजरे पर स्वेच्छा से गयी बिराज बहू को स्वयं ही अपनी भूल समझ आती और वह नदी मेँ कूद जाती है। बिराज बहू का नैतिक स्खलन उसके अपराध बोध, स्वयं की मृत्युकामना और मृत्युवरण का मूल कारण है, जो कि फिल्म मेँ नदारद है।
मैँ समझता हूँ कई बार मूल कहानी मेँ परिवर्तन दरअसल कथाकार की मंशा को विकृत कर डालता है जैसे कि गिरीश कर्नाड ने ‘मृच्छकटिकम्’ का अन्त, मूल नाटक पर आधारित फिल्म ‘उत्सव’ मेँ चारुदत्त और वसन्तसेना के विवाह के बजाय विरह से कर दिया। यहाँ ध्यान देना चाहिये कि जब भवभूति ‘उत्तररामचरित’ मेँ वाल्मीकि रामायण के ‘उत्तरकाण्ड’ का कथानक बदलते हैँ, तो वे केवल कथा का अन्त ही नहीँ, अपितु कथा भी अपने अनुसार बदल ही देते हैँ जिसमेँ राम अत्यन्त भावुक और शीघ्र मूर्छित होने वाले हैँ।
प्रश्न उठता है कि बिमल रॉय ने कहानी मेँ यह परिवर्तन क्योँ किया? इसी तरह उन्होँने देवदास के कायर स्वरूप को महिमामण्डित करने मेँ भी कोई कसर नहीँ छोड़ी। इन्हीँ कारणोँ से क्षुब्ध हुआ जा सकता है कि कमसे कम शरत् चन्द्र तो यह जानते थे कि देवदास अविवेकी है और उपन्यास के अन्त मेँ पाठकोँ से यह निवेदन भी करते हैँ कि यदि आस-पास कोई देवदास जैसा चरित्र मिले तो उसे समझाइये। बिराज बहू की कथा कुछ अंशोँ मेँ अविश्वसनीय है कि नैतिक रूप से उच्च नायिका आवेश मेँ, या पति को सबक सिखाने के लिये अन्य पुरुष से समागम के लिये उद्धत हो जाती है, क्योँकि ऐसा कोई चारित्रिक सूत्र पूरी कथा मेँ मिलता नहीँ है। सम्भवतः बिमल रॉय शरत चन्द्र का उक्त दोष दूर करने मेँ अनुरक्त थे या फिर वह समाज के अनुकूल कथा को ग्राह्य बना रहे थे।
कामिनी कौशल ने इस फिल्म मेँ अपनी अभिनय क्षमता का विस्तार प्रदर्शित किया है। वह ममतामयी भाभी, निष्ठावान् पत्नी और हिन्दू पतिव्रता के बहुत सारे आयामोँ को अपने भाव-प्रणव अभिनय से समेट लेती हैँ। कहा जाता है कि मधुबाला यह भूमिका निभाना चाहती थीँ, किन्तु बिमल रॉय को यह डर था कि वह मधुबाला की फीस नहीँ दे पायेँगे।
गोदान और अन्य चरित्र भूमिकाएँ
प्रेमचन्द के अन्तिम उपन्यास ‘गोदान’ पर बनी एकलौती फिल्म गोदान (१९६३) मेँ होरी की भूमिका राजकुमार, धनिया की भूमिका कामिनी कौशल और गोबर की भूमिका महमूद ने निभायी थी। यह फिल्म बहुत प्रभावशाली नहीँ बनी है। परन्तु इस फिल्म मेँ राजकुमार और कामिनी कौशल का अभिनय प्रशंसनीय है। असहायता बोध, दायित्व, दाम्पत्य प्रेम जैसे कई कठिन विषयोँ को कामिनी कौशल ने अच्छी तरह निभाया है। कमसे कम हिन्दी साहित्य जगत् को इस फिल्म मेँ मूल कथा और उसके सिनेमा में निरूपण पर गहरा विचार करना चाहिये। सम्भवतः ऐसा १९६३ मेँ हुआ भी होगा, पर ऐसा कोई आलेख इंटरनेट पर उपलब्ध नहीँ है। इस तरह के विमर्शोँ को संरक्षित कर के प्रकाश मेँ लाना चाहिये। आज के समय मेँ गोदान की कथा कोई विशेष प्रभाव छोड़ पाती है, कहना कठिन है।
कामिनी कौशल ने चरित्र भूमिकाओँ मेँ लम्बी पारी खेली। मनोज कुमार, जिन्होँने फिल्म ‘शबनम’ (१९४९) मेँ दिलीप कुमार के चरित्र से प्रभावित हो कर अपना नाम मनोज कुमार अपना लिया था, ने कामिनी कौशल को अपनी सात फिल्मोँ मेँ रोल दिया। फिल्म ‘अनहोनी’ (१९७३) मेँ उन्होँने खल चरित्र भी निभाया। कामिनी कौशल की सक्रियता इक्कीसवीँ सदी तक रही, जिससे हम सभी परिचित हैँ।
कामिनी कौशल की तुलना हम भले मीना कुमारी के बर-अक्स करने मेँ हिचकेँ, लेकिन हमारे लिये कामिनी कौशल केवल व्यक्ति-मात्र नहीँ हैँ। कामिनी कौशल के साथ-साथ हम चाहे अनचाहे बॉम्बे टॉकीज, चेतन आनन्द, बिमल रॉय, अशोक कुमार, दिलीप कुमार, देव आनन्द, राज कपूर, लता मङ्गेशकर, गीता दत्त, किशोर कुमार, प्राण तक पहुँच ही जाते हैँ। साथ ही खेमचन्द प्रकाश, चितलकर रामचन्द्र, अनिल बिश्वास, सचिन देव बर्मन, राजा मेहदी अली खान, मजरूह सुल्तानपुरी, कमर जलालाबादी जैसी प्रतिभा याद आ जाती हैँ। स्वर्ण-युग मेँ जो सोने जैसी चमक और सहजता थी कि वह किसी भी रूप मेँ लुभाता है, वह अब चमक-दमक मेँ खो गया है।
कभी-कभी सोचता हूँ कि हमने वह नैसर्गिकता, मासूमियत और सहज विश्वास कैसे खो दिया? हो सकता है वह उस जमाने मेँ भी न रहा हो जैसा कि उस समय की फिल्मोँ मेँ प्रकट होता है, परन्तु यह तो तय है कि हमारे समकाल के सिनेमा मेँ गीतोँ मेँ, बोलोँ मेँ, संगीत मेँ, अभिनय मेँ, संवाद मेँ वह सहजता नहीँ रही कि आम भारतीय उससे जुड़ाव महसूस करे। यह दिशाहीनता है।
दिशाहीनोँ के लिये दिशासूचक यन्त्र आवश्यक उपकरण है। हिन्दी फिल्मोँ के स्वर्ण-युग की कलाकृतियाँ ऐसा ही यन्त्र का काम कर सकती हैँ, हालाँकि हमेँ उसे ठीक से देखने की दृष्टि विकसित करनी होगी।
अग्रहायण शुक्ल द्वितीया, संवत् २०८२