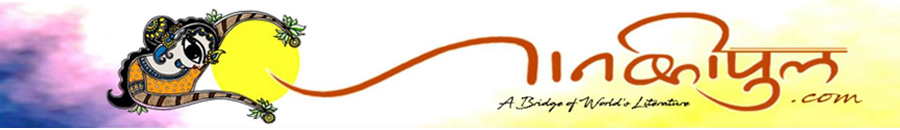वरिष्ठ कवि-आलोचक विष्णु खरे ने ‘जानकी पुल’ पर कमलेश का तआरूफ करवाया तो अनेक लोगों ने यह सवाल उठाया कि यह तो संस्मरण टाईप है. तो इस बार खरे साहब ने अपने ‘आलोचक फॉर्म’ में आते हुए उनकी कविताओं पर लिखा है. मेरे जानते कमलेश की कविताओं का यह सबसे अच्छा विश्लेषण है. आपके लिए- मॉडरेटर.
============================
( कमलेश को लेकर चल रहे विवाद के बारे में जानकर और ब्लॉग पर प्रकाशित उनकी कविताओं को पढ़कर जो पत्र मैंने ‘जानकी पुल’ के मॉडरेटर को लिखा था वह एक प्रारंभिक प्रतिक्रिया-जैसा था और स्वतंत्र रूप से लिखी गयी कोई टिप्पणी नहीं.वह निस्संदेह मुझे उपलब्ध उनकी कविताओं का कोई अर्ध-गंभीर विवेचन तक न था – हिंदी के ब्लॉग-(अधो)विश्व और Faecesbook की सम्मिलित ‘स्लमडॉग मिलियनेयर’ बम्पुलिस में आप ‘भाँग की पकौड़ी’ लेकर तो जा सकते हैं, ’भगवद्गीता’ नहीं पढ़ सकते.लेकिन हिंदी के ही कुछ नक़ली या असली अक़्ल के नाबीना – नक़ली कम असली ज़्यादा – पूछ रहे हैं कि ऐ बाSबाS,कमलेश की कविता का रास्ता कहाँ है? तो एक यकचश्म या अह्वल कोशिश यहाँ की जाती है.
राह में दो अड़ंगे फिर भी हैं. इशारे में किए गए इसरार के बावजूद ब्लॉग मॉडरेटर ने नहीं बताया है कि कमलेश की यह ‘नई’ लगाई गई कविताएँ कब और कहाँ की हैं.फिर यह कि इस टिप्पणीकार के पास उनका सिर्फ़ ‘पहचान’ सीरीज़ में 42 बरस पहले प्रकाशित अड़तालीस कविताओं वाला पहला मुकम्मल संकलन ‘जरत्कारु’ है,बाद में आए उनके संग्रह उसने देखे तक नहीं हैं.इसलिए कमलेश की कविताओं को पढ़ने-समझने की यह कोशिश कितनी भरोसेमंद,मुकम्मल और सार्थक होगी यह खुद इस टिप्पणीकार के लिए कह पाना कठिन है.
इस बीच सुना है कि अपने बौद्धिक-राजनीतिक रुझानों में कमलेश घोर दक्षिणपंथी हो चले हैं.संभव है उनके वक्तव्यों या गद्य में इसके प्रमाण मिलते हों – दुर्भाग्यवश ऐसे सुबूत भी मुझे फ़िलहाल मुहय्या नहीं हैं.लेकिन उनके दक्षिणपंथी विचार-विचलन से ज़्यादा उत्सुकता मुझे उनकी उत्तर-‘जरत्कारु’ कविताओं को देखने और उनमें हिन्दुत्ववादी-फाशिस्ट प्रच्छन्न-प्रकट तत्वों को पहचान पाने की है.कहा जा रहा है कि कमलेश इधर की अपनी कविताओं में भी ब्राह्मणवादी-स्वामी करपात्रीवादी हो गए हैं. हमारे छिन्दवाड़ा-गोंडवाना-महाकोसल में कहावत चलती है कि हाथी छोटा भी होगा तो सूअर से छोटा तो नहीं होगा.कमलेश दक्षिणपंथी कवि होंगे भी तो अटलबिहारी वाजपेयी से बदतर तो नहीं होंगे. अफ़वाह है कि नरेंद्र मोदी भी कवि हैं – मालूम नहीं हिंदी में या गुजराती में – लेकिन उनका कुछ भी मैंने मूल या अनुवाद में नहीं पढ़ा है,इश्तियाक़ भले ही बहुत है,इसलिए कह नहीं सकता कि यदि कमलेश उनकी ही किमाश के हैं तो क्या अटलबिहारी के इस आशंकित उत्तराधिकारी से उनकी बड़-छोट भी उपरोक्त गज-शूकर अनुपात की होगी ?
उत्तराखंड में हज़ारों स्त्री-पुरुष-बच्चे तीर्थयात्री कीचड़ में जिंदा दब गए.उधर सरकार ने जैमातादी जी की वैष्णोदेवी के सम्मान में उनकी मूर्ति वाला एक निहायत भोंडा और आपत्तिजनक पाँच रुपए का नया सिक्का ढलवाया है.और भी आगे ख़बर यह है कि देश में करोड़ों लोग 17 ( सत्रह ) रुपये रोज़ पर जिंदा हैं.क्या यह वक़्त महज़ कविता की चर्चा का,क्रांतिकारी कविता करने का है, या क्रांतिकारियों के निर्भीक समर्थन का ?
बहरहाल,कमलेश की कविता पर यह ‘एड हॉक’,‘कंडीशंस अप्लाइ’ टिप्पणी. वि.ख़. )
1971-72 में प्रकाशित कमलेश के पहले कविता-संग्रह ‘जरत्कारु’ की लगभग सारी रचनाएँ 1960 के दशक के उत्तरार्ध की ही हैं और उन प्रारंभिक कविताओं में से कुछ पर टी.एस.एलिअट (विशेषतः ‘जर्नी ऑफ़ द मैजाई’ तथा ‘लव-साँग़ ऑफ़ एल्फ़्रेड जे. प्रूफ्रॉक’), रघुवीर सहाय (विशेषतः ‘दे दिया जाता हूँ’), और सामान्यतः ‘नई कविता’ की भाषा-शैली, का कुछ तलछट असर देखा जा सकता है जो न अस्वाभाविक है और न आपत्तिजनक.ऐसी कविताओं में भी,और निस्संदेह अधिकांश दूसरी कविताओं में,कमलेश के स्वायत्त रुझान,निजी काव्य-संसार,अपनी भाषा-शैली स्पष्ट पहचाने जा सकते हैं.
इन कविताओं में कमलेश एक साथ एक जटिल और एक सहज सृजेता दिखाई देते हैं.मालूम पड़ जाता है कि कवि ने महान संस्कृत परम्परा को कितनी गहराई से आत्मसात् और बुद्धिसात् कर रखा है लेकिन उसकी अपनी जड़ें,क्योंकि वह वहीं जन्मा है, एक बहुविध अभावग्रस्त लोक-जीवन और विडम्बनापूर्ण,स्निग्ध किन्तु हृदयहीन, लोक-संस्कृति में ही हैं,पर जब वह उनसे बाहर की हाहाहूती दुनिया में दाख़िल-शामिल होता है तो उसका मुक़ाबिला समसामयिक, भयावह किन्तु संघर्षप्रेरक सम्पूर्ण भारतीय यथार्थ से होता है, फिर भी किसी सूरत वह अपने भीतर एक निजी,व्यक्तिगत माँद भी बचाए रखता है जहाँ एक चिथड़ा सुख और विषादों की एक कमली उसका इंतज़ार करते हैं.
‘जरत्कारु’,’देवप्रिया’ और ’विष्णुप्रिया’ वे कविताएँ हैं जिनमें कमलेश ने संस्कृत और यूनानी मिथकों का इस्तेमाल किया है.”एक कुएँ में लटक रहे थे सब पितर/बरगद की जड़ें पकड़े…सहारे-सूत्र चूहे काटते/ जा रहे हर पल…कौन से पुरखे लटक रहे थे जड़ों से ? / और इतिहास किस समय बदल जाता है चूहों में / हमारी पीड़ा के अंतिम सहारे-सूत्रों को / काटने लगता है ?” ‘देवप्रिया’ में कमलेश एक मिथक का उपयोग दूसरी,’इम्प्रोवाइज़्ड’,आंशिक रूप से अपना मिथक गढ़ने में करते हैं: “… – और मैं देखता हूँ यूनानियों के देवता / अपने-अपने कपड़े पहन कर कब्रिस्तान के दरवाज़े पर / खड़े हुए हैं – उनके मुख पर झलकता है संतोष / किसी नयी मानव-कन्या को फुसला कर / रतिकर्म में प्राप्त सफलता का.” संस्कृत शीर्षक देते हुए वह कविता को एक प्रूफ्रॉकीय फंतासी तक ले आते हैं : “ओ विष्णुप्रिया! हम शेर की हुंकार से आहत / छटपटाते रहते हैं उन नदियों में जिनकी दुग्ध-धवल तीक्ष्णता / हमें अंधा कर गयी होती है परियों के देश में…” हिंदी कविता में यह नई धृष्टता थी.
एक कविता में कमलेश ने कहा है : “कविता मांगती है तीखी संवेदना इस समय !” वह पूछते हैं : “…हमारे पुरखे,इतिहास के / करोड़ों कण जुगनू-से जगमगाते रहते,हमको डराते / अपनी करोड़ मृत्युओं,करोड़ प्रेमों,करोड़ पापों और करोड़ जन्मों से – / करोड़ों जन के ह्रदय का स्पंदन रात की शिराओं में कैसे पकडूँ,/कौन सा यातायात कर लूँ पूरी अशेष यात्राएं इन मार्गों की / और रात मेरी देह हो रह जाय.” ‘केवल तुम्हारी देह’ में ऐंद्रिकता और सामाजिकता का विरल यौगिक है : “मैं जो जानता हूँ भूख रोटियों की,नमक और मधु की,मैं जो /जानता हूँ आदमियों के बीच निर्वस्त्र / घूमने की,मैं जानता हूँ करोड़ों की भूख / और प्यास… अचानक देखता हूँ ज्योतित तुम्हारी देह,…”
गाँव का यदि एक ऐसा चित्र उनके यहाँ है : “…जाग पड़तीं हर तरफ फेत्कारें / सियारों-लोमड़ियों की …होशियार ! होशियार !! / – चौकीदार की हाँक,सिवान में / बाँटते चोरी का माल नकाबपोश,अलाव में / फूँक मारते हो जाते रोशन सारे षड्यंत्र / सारी हरकतें,सारी मनौतियाँ / गँवारों की,रात में गाँव / फफक-फफक कर रोती / औरत-सा हमारे ह्रदय से / फेंक दिया जाता है.” तो ‘मेरे बाप का बुखार’ जैसे एकदम अलग तेवर,भाषा और इकबाल की पंक्तियाँ : “ मुझे मेरे बाप ने पढ़ायी किताबें / और मैं भूलने लगा बैलगाड़ी की लीक पर / उड़ने वाली धूल / मुझे ख्याल आयीं गाँव भर की नीचताएँ / और मैं गढ़ने लगा सपने इकले जीवन के /…और मैं रोने लगा,रोने लगा एक रात / गाँव से दूर,बहुत दूर एक शहर में // मैं कमासुत बेटा कैसे हो सकता था ? / मैं गाँव की ढिबरी तले कैसे पढ़ सकता था? मैं उस धूल में ; कीचड़ में कैसे रह सकता था ? // और मैं रोने लगा,रोने लगा एक रात / मच्छड़ अब यहाँ मुझे काटते क्यों नहीं / मुझे भी क्यों नहीं होता मेरे बाप का बुखार”
कमलेश अपनी इस कविता में आखीर तक वजह नहीं बतलाते,सिर्फ यह कि “जो बच्चा उस साल मरा उम्र थी केवल तीन साल/जो बच्चा उस साल मरा वह पहने था कनटोप-कोट/जो बच्चा उस साल मरा उसके थे दोनों पाँव साबुत/जो बच्चा उस साल मरा वह सीख रहा था मानव-शब्द…” और ’फिर वही सिलसिला’ में यह स्वीकारोक्ति,यह पुकार : “आख़िरी बार आवाज़ दूँ तो किसको,अपने तो/वही यार,वही टूटती जमातों के सिलसिले/और वही निज़ाम जिसमें रहने से निस्तार नहीं/नियति हो जाति की या ज़माने की हालत हो /बेबसी तोड़ते कब आदमी लाचार नहीं”
क्या निराला-जैसी यह पंक्तियाँ आत्म-कथा का पूर्वाभास थीं ? : “वर्षों के प्रतिवाद हुए निष्फल,नगर से निष्कृत होकर/अनजान घरों को जाने वाली जंजाल लग रही सड़कों पर /हूँ खड़ा आज मैं भिखमंगे-सी आशा बाँधे/शायद कल वापस ले लें मुझको नागर-जन…//पाकर लोमड़ी की तरह मुझे जब कोई सांसारिक कुत्ता/लेता है खदेड़,तब कहीं चुन्नटें उठती हैं दिमाग़ में…”किन्तु कमलेश सिर्फ़ अपने लिए ही कातर नहीं हैं : “…फिर कैसे/जातियाँ सुन सकेंगी कोई भी सूक्ष्म ध्वनि,निकाल सकेंगी/कोई भी आवाज़,सूँघ सकेंगी कोई भी गंध,देख सकेंगी/कोई भी/कोई भी वस्तु फिर कैसे वापस आयेगी उनमें/महसूस करने की थोड़ी भी शक्ति,फिर कैसे…फिर/कैसे…फिर कैसे – फिर कौन सी जाती का प्रादुर्भाव होगा/इस धरती पर जब आदमी अपने को समेटता खुद लेगा/अपना कलेवा कर विलीन हो जाएगा – इस धरती पर अगले विकास-क्रम में फिर कौन आएगा”
कमलेश कभी यूँ भी सोचते थे : “जब भी संभव हो,किसी सोच-विचार के बिना/अलमारियों से निकाल कर किताबें फेंक दो/तस्वीरें उड़ा दो/बोरिया-बिस्तर जला दो/…चलते-फिरते रास्ता देखने वाले फ़क़ीर हो जाओ/जब भी संभव हो वे सारे शीशे तोड़ दो// जिनमें तुम्हारे/या किन्हीं के,/चेहरों के अक्स हैं !”वे देखते हैं कि एक दिन मानव चीतों की तरह इंजिनों की सीटियों,कारखानों की घड़-घड़ और बारूद के धमाकों से आतंकित करने वाले प्रभुता के फ़रमानों पर सिर्फ़ अपने पंजों की छाप छोड़ जाएँगे.
‘गिरे दिन’ कविता की बहुत कम पंक्तियाँ पुरानी या अप्रासंगिक हुई हैं : “घूमते रहते हैं अपने चेहरे लिए,लोग,अभी भी/उद्यानों में,सुनते हुए घरघराहट/विध्वंसक विमानों की,सुनाई नहीं देते/सही है,बमों के धमाके/लूटी नहीं जातीं,सही है/अनाजों की दूकानें,/सबको इजाज़त है भर ले/कोई भी स्वाँग,सब रहते हैं तैयार/धोखा खाने को जान या अनजान,शर्त सिर्फ़/गले में लटका लें तस्वीर/आप प्रधानमंत्री की./… फिर भी सफल हो जाते हैं सरकारी विज्ञापन हमें/गिरे दिनों की ऐयाशी उधार देने में,बसों की प्रतीक्षा में/राजनेताओं के नारे सुनते हम भी हो जाते हैं बहाल/उस हुजूम की नौकरी पर,पर कौन/रोक सकता है सड़े ठूँठ का भहरा पढ़ना,घोषित धोखों/की भाषा में बैंजनी,नीले,लाल फूलों के किस्मों की/पहचानें सारी उलट-पुलट जाती हैं,रोता है/देवता मुरदार आयुधों के नाम,ज़रूरी हो जाती है तब/कविता एक और किस्म की.”
इस सिलसिले में उनकी उपरोद्धृत “नई” कविता ‘क्रान्ति की प्रतीक्षा’ की अंतिम बहसतलब पंक्तियाँ देखी जाएँ : “तुम देखो साम्राज्यों का पतन और/सभ्यता में रोगों का जनमना,बढ़ना,/अब तुम जानते हो बरा नहीं पाओगे/किसी भी सामूहिक सामर्थ्य से/सारे घुन,तुम्हें मालूम है संकट/इतना सरल नहीं जितना शब्दों से/ लगता है,तुमने शब्दों की सरलता/वरण की है,पर संसार कहीं कोसों दूर/जटिल विकलता है.”
मुझे हैरत है कि इन पंक्तियों की समसामयिकता क्यों दिखाई नहीं देती : “…मुझे मालूम है कि इसी समय संभव था/कि सरकार नागरिक अधिकारों पर हमला करती,साबुन का/ दाम बढ़ाती और गेहूँ अमरीका से ज़्यादा ज़ा कम आयात करती और क्यों इसी समय/जगह-जगह हड़तालें हुईं,बसें जलीं,गोलियाँ चलीं/पुलिस की,और तस्वीर गिरी प्रधानमंत्री की/मैं बैठा नहीं रह सकता जब मुझे अपना वक़्त/धरती पर उतार लाना है,मुझे खुशी है/समय इस कोलाहल में धीरे-धीरे/पक्षधर होता जा रहा है.”
आज जो बहुत गाँव गाँव की काँव काँव मची हुई है उसके शायद बहुत पहले कमलेश ने कहा है,लेकिन आत्म-व्यंग के साथ ”…मेरे मन में केवल/ खेत आते हैं,सूखे हुए तालाब और परती की/जली हुई दूब जहाँ गाँव में/मेरा बचपन बीता है वहाँ के झोपड़े हैं/ और गलियाँ हैं और सारी गंदगी,मल और मूत्र.//लेकिन इतिहास कभी गाँवों का बाशिंदा/नहीं रहा,क्रान्ति हमेशा शहरों से हो कर/गुज़रती रही,मैं कैसे/दूर रहता उस मार्ग से.//मैं शहर में रहता हूँ,अपने बनाए कष्ट/झेलता हूँ,…किताबें पढता हूँ,सभाओं में जाता हूँ,प्रदर्शन करता हूँ,/बिना सर फोड़े हुए पुलिस का/जेल चला जाता हूँ.”
लेकिन यही कवि ऐसी पंक्तियाँ भी ले आता है: “खुला अभी बचा है वन के फैलाव से/धरती पर कच्छप पीठ-सा उठा हुआ/अजानी,अदेखी,संकरी पगडंडी है/पैत्रिक आवाजें वहाँ ले आती हैं”.हिंदी कवि इधर बहुत स्त्रीवत्सल होने के दावे करने लगे हैं,कमलेश के यहाँ औरतें अपनी उम्र की उस बेला को जानती हैं जब “आएँगे,मँडराते प्रेत सब/माँगेंगे/अस्थि,रक्त,मांस/सब दान में”.नैहर लौटा दी गयी ब्याहता की त्रासदी सिर्फ़ कमलेश की कविता में देखी है.लोर्का की कविता ( कमलेश ने लोर्का के हिज्जे ग़लत लिखे हैं – फ़ेदेरिको गार्सिया होना चाहिए,स्पैनिश भाषा में जब g के बाद a,o या u आते हैं तब g का उच्चारण ‘ग’ ही होता है,e और i से पहले ‘ख़’ किया जाता है ) से प्रेरित विदा-गीत अंतर-सांस्कृतिक असर लेने का उम्दा उदाहरण है लेकिन ब्याह का प्रस्ताव लेकर जानेवाले को ‘हज्जाम’ कहना ठीक नहीं,वह दूल्हे की दाढ़ी-कटिंग करने नहीं जाता,उसे सादर ‘नाऊ ठाकुर’ कहा जाता है,नेंग मिलता है,यूँ उसके साथ थोड़ी चुहलबाज़ी भी होती है.
‘अकाल के दृश्य’ जैसी दूसरी असली,ग्राफ़िक और मार्मिक कविता हिंदी में तो नहीं देखी,भले ही उसका उपशीर्षक यह कविता नहीं है हो.लेकिन यह सब कमलेश को उनके प्रतिक्रियावादी विचलनों से बरी नहीं करता.यदि वाक़ई उनके विचार फाशिस्ट होते जा रहे हैं तो उनका मुक़ाबिला किया ही जाएगा.लेकिन जितना मैंने उन्हें देखा है वह मुझे इसी परिणाम तक पहुँचाता है कि अब वे अधिक कन्फ़्यूज़्ड,अनर्गल,बेअसर बादमश्क ( विंडबैग ) हो चुके हैं.वैसे मैंने उन्हें एक ‘चिन्तक’ या राजनीतिक सक्रियतावादी के रूप में कभी गंभीरता से नहीं लिया – वे मुझे हमेशा एक ‘ओपेरा बूफ़ा’ के पात्र ही लगे जिसे मानों मोलिएर ने लिखा हो.वे रातोंरात पाला या पॉलिटिक्स बदल सकते हैं.
लेकिन यदि इस सब के बावजूद मुझे उनकी कुल कविता,जो मैं पढ़ नहीं पाया हूँ, अच्छी लगे तो यह मेरी और सृजन की समस्या है.मुझे इस का भी एहसास है कि मुझे कमलेश की कविता का कुछ अधिक विस्तृत और भीतरी विश्लेषण करना चाहिए था,लेकिन उसमें काफ़ी वक़्त लगता.