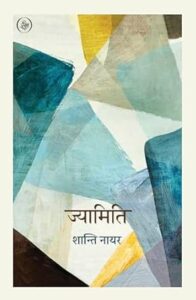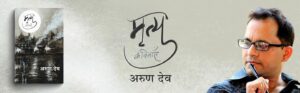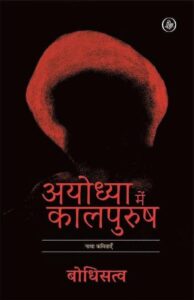पूनम अरोड़ा की पुस्तक ‘परख’ की समीक्षा
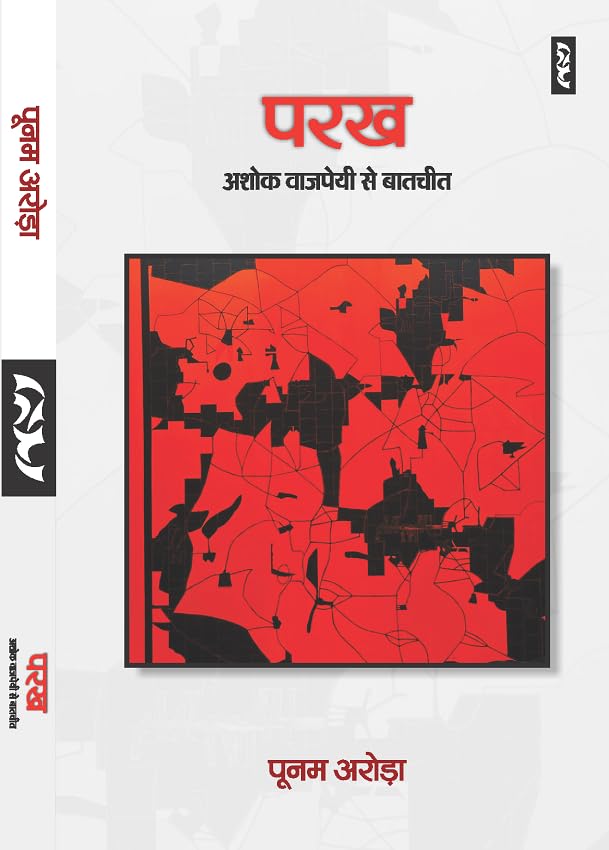
कवयित्री पूनम अरोड़ा की पुस्तक आई है ‘परख’, जो प्रसिद्ध कवि-लेखक-संस्कृतिकर्मी अशोक वाजपेयी से बातचीत पर आधारित पुस्तक है। इसी पुस्तक पर यह टिप्पणी लिखी है कवयित्री अमिता मिश्र ने। सेतु प्रकाशन से प्रकाशित इस पुस्तक की समीक्षा आप भी पढ़ सकते हैं- मॉडरेटर
=========================
यह साक्षात्कार पुस्तक एक अनकही दास्तान का सघन बिंदु है। जो ख्यातिलब्ध कवि,संस्कृतकर्मी अशोक वाजपेयी के साथ संवादों का सघन जखीरा लेकर आगे बढ़ती है ।यहां प्रश्न हैं और प्रश्नों के समुचित उत्तर भी। मनुष्यता यहां अपने सारे अंतरालों में विद्द्मान है ठिठकी हुई है वह स्वयं को बांट लेना चाहती है।
संवाद जो पोस्टट्रथ समय का एक महत्वपूर्ण कारक है। सम्वाद जिससे जमी हुई बर्फ को पिघलाया जा सकता है जिसकी उष्मा मनुष्यता में यकीन करने के लिए बाध्य करती है। जिस सम्वाद को मनोवैज्ञानिक बनाये रखने के लिए नसीहत दे रहे हैं उन्हें लगता होगा कि जब सब कुछ खत्म हो रहा होगा तभी भी सम्वाद के जरिये शायद कुछ बच जायेगा। यही संवादधर्मिता पुस्तक का हासिल है।
यूं तो अशोक वाजपेयी साहित्य और कला की दुनिया में अपना जरूरी हस्तक्षेप रखते हैं। वे इस देश के बड़े संस्कृतकर्मी हैं पर कवि, विचारक के रूप में उनके अंतस्तल को टटोल कर अभीष्ट उत्तर लाने में पूनम अरोड़ा ने जो तत्परता और संश्लिष्टता दिखाई है वहां कोई रिक्तता नहीं है।
पुस्तक के फ्लैप में लिखे अपने शब्दों में कवि मदन सोनी जी कहते हैं कि यूं तो अशोक वाजपेयी के अन्य भी साक्षात्कार आते रहे हैं पर यह पुस्तक उन साक्षात्कारों में छूट गये को पूरा करती है। “पूनम द्वारा लिए गए इस साक्षात्कार में हम अशोक वाजपेई को और उनके साथ-साथ स्वयं को, उनके लेखकीय अतरंग में, उनके कवि आलोचक- मानस की गहराइयों और तहों में झांकता हुआ पाते हैं आज जिसे हम अशोक वाजपेई नामक अत्यंत संश्लिष्ट संघटना के रूप में जानते हैं यह पुस्तक हमें उस संघटना की बुनियादों, उसकी निर्मिति की प्रक्रिया,अपने व्यापक परिवेश के साथ हुई उसकी टकराहटों और अन्त्तर्क्रियाओं से परिचित कराती है।“
पुस्तक की संरचना इस प्रकार है कि पढ़ते हुए धीरज भरा इत्मीनान मिलता है। इसे पढ़ते हुए अशोक जी की जीवन यात्रा में शरीक होना है । यद्दपि यह आत्मकथा नहीं है पर उनके जीवन के झंझावातों ,उनके नन्हें सुखों से गुजरना,उनकी शैली को आत्मसात करना ,उनके लिखे का बोध, उनकी वैचारिकी यहां यह सब प्राप्त होता है। साक्षात्कार लेने वाली पूनम अरोड़ा के पास प्रश्नों की तहदार बुनावट है। वे बहुत कुछ बोलती हैं कहती हैं तब तक कहती हैं जब तक प्रश्न अपने अंतिम छोर तक नहीं पहुंच जाते।प्रश्नों में गंभीरता,धीरता और गहराई है और अशोक जी के व्यक्तित्व को खोलने की अतरंगता भी। अशोक जी धीरे- धीरे सब कह जाते हैं और फिर एक उदासी भरे मौन में बातों को विराम दे दिया जाता है कहते हुए कहीं तो रुकना ही था।
कवि श्रीकांत वर्मा ने आक्टिवियो पॉज का साक्षात्कार लिया था।आक्टिवियो पॉज लैटिन अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान कवि चिंतक हैं। उनकी गिनती लैटिन अमेरिकी दुनिया के दो बड़े कवियों में की जाती है। पॉज के लिए कविता मनुष्य को सार्थक बनाने का रास्ता दिखाती है। पॉज सिर्फ कवि नहीं हैं वह एक महान विचारक भी हैं। इस साक्षात्कार में पॉज ने और भी बहुत से विषयों पर रोशनी डाली थी।
साक्षात्कार स्वयं को जानने, बताने का एक सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। अपने जीवन के सारे वितानों के साथ अपनी अंतरंगता में एक व्यक्ति खुलता है ।। वह अच्छा बुरा बेखौफ होकर कह डालता है अशोक जी ने भी बहुत कुछ कहा , कहना पड़ता है । उनके उत्तर मनुष्यता को सार्थक बनाने के लिए चिंतित दीख पड़ते हैं। पॉज अपने कथन में बार – बार शंका का पक्ष रखते हैं यह शंका ही प्रश्न करने के लिये प्रेरित करती है। अशोक जी कथनों में भी शंका का यह पक्ष उभर कर आया है।
साक्षात्कार की इस किताब को सहूलियत के लिए कुछ भागों में बांटा गया है। भागों के नाम हैं -प्रारम्भ नहीं,शब्दों के बीच की खाली जगह में,होना अनेक संभावनाओं पर,गुम्फित,कसौटी,अंत नहीं ये शीर्षक हैं। इन नामों का संगुफन ठहर कर और सुकून से किया गया है। प्रश्न दर प्रश्न सम्वादों में बहुत कुछ समेटने का प्रयास है।
अशोक जी एक प्रश्न के प्रत्युतर में लिखते हैं -” असाधारण होना दरअसल साधारण होने की सबसे कोमल और सत्य घटना है और ऐसी घटनाएं जीवन में कभी ना कभी जरूर घटती हैं।“
अशोक जी का अखबार में एक कॉलम आता है- ‘कभी -कभार’ जो काफी लम्बे अरसे से आ रहा है बहुत सारे पाठकों ने इस कॉलम के द्वारा उन्हें जाना। पूनम अरोड़ा लिखती हैं कि सर्वप्रथम मैंने अशोक जी को इसी कॉलम के माध्यम से जाना. मैंने स्वयं भी इसी के माध्यम से उन्हें जाना था। बहुत कम उम्र में उन्होंने लिखना शुरू किया था जिस धागे को वे आजीवन पकड़े रहे। उन्होंने अपने परिवेश, माता पिता और बेटी पर कविताएं लिखी। मां पर उनकी लिखी कविताएं विवादस्पद भी रही । इबारत से गिरी मात्राएं, उम्मीद का दूसरा नाम, कुछ रफू कुछ थिगड़े, शहर अब भी सम्भावना है, बहुरि अकेला, विविक्षा इत्यादि उनके काव्य संग्रह हैं। वे मानते हैं कि हर रचनाकार का अपना समय होता है जो आधुनिक होता है । इस अर्थ में गालिब और तुलसीदास का समय भी आधुनिक था। कविता के संदर्भ में अशोक जी विस्तार से बताते हुए कहते हैं -” कविता हमेशा कहने और न कहने के बीच में फंसी होती है। मेरा प्रिय रूपक गोधूलि है- अंधेरे और उजाले के बीच कविता गोधूलि में ही होती है।“ वे कहते हैं कि “कविता एक तरह से देहली दीपन्याय करती है, देहली पर स्थापित दीपक का न्याय। जब दीपक को देहली पर रख दिया जाता है तो इसका प्रकाश देहली के दोनों ओर होता है।”
दुनिया में हर क्षण बहुत कुछ दुःखित करने वाला घटता है सम्वेदनशील मन दुनिया में इस दुःखद को घटित होते नहीं देख सकता। इराक पर हमला और बाबरी मस्जिद का ढहना कवि को अंदर तक विचलित करता है।
“इतने लम्बे इतिहास, इतनी व्यापक और बहुल संस्कृति, इतने लम्बे और कठिन संघर्ष के बावजूद हमारी संस्थागत उपलब्धियां जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता- समता- न्याय, संवैधानिक और अन्य संस्थाएं इतनी आसानी से टूट फूट गयी हैं और लगातार बिखर और अवमूल्यित हो रही हैं। भारतीय समाज में भयानक टूटन है और उसे बचाने की चिंता और चेष्टा इतनी कम दिखाई देती है। “
अशोक जी अपने कथनों में बताते हैं कि उनमें बहुत कम उम्र में परिपक्वता आ गयी थी जिसे वे अकाल परिपक्वता के नाम से सम्बोधित करते हैं । हिंदी कवियों में अज्ञेय और शमशेर उन्हें प्रभावित करते हैं। अज्ञेय की तत्सम शब्दावली और शमशेर की एंद्रिकता उन्हें प्रभावित करती है। मुक्तिबोध के लिए वे लिखते हैं कि मुक्तिबोध जैसा होना सम्भव नहीं है। अंग्रेजी कविता में कीटस्, इलियट, वालेस स्टीवेंस उनके प्रिय कवि हैं। लातीनी अमेरिकी कवि आक्टियों पॉज एक कवि चिंतक के रूप में उनके आदर्श रहे हैं। कविता क्या है, को परिभाषित करते हुए अशोक वाजपेयी बताते हैं – “ कविता अदृश्य को, अकथ को दृश्य और कथन को अहाते में लाने की कोशिस करती है। अगर आपका रंगबोध घना हो तो आपको कुछ कविताओं में रंग भी महसूस हो सकते हैं। कुछ कविताएं नील वर्ण, कुछ रक्ताभ, कुछ पिपराई और कुछ हरीतिमा लिये हो सकती हैं।”
अशोक जी बहुत सी देश- विदेश की यात्राओं में रहे। उनका एक सुदृढ़ व्यक्तित्व है। वे विचार को दूर तक देख पाने में सक्षम हैं। वे कहते हैं -” मैं तो छोटे से दिये से थोड़ा सा उजाला करने की कोशिस का कवि हूं। “ वे संवाद की इस श्रृंखला में बहुत कुछ साझा करते हुए दीखते हैं जो उनके अनुभव विस्तार को बताते हैं। अशोक जी की संगीत, नृत्य और चित्रकारी में गहरी रुचि है। वे मानते हैं कि कविता सिर्फ सुंदरता को ही बचाना नहीं है बल्कि “ सुंदर को देखना- बचाना और हिंसा क्रूरता से जूझना कविता में एक साथ हो सकते हैं।“
अशोक जी ने काफी पुस्तकों के अनुवाद किये हैं जिनकी लम्बी श्रृंखला है। विश्व के बहुत से कवियों की कविताओं के अनुवाद उन्होंने हिंदी पाठकों को दिये। वे स्वतंत्रता, समता और न्याय की मूल्यत्रयी के कास्मिक फैलाव को मानते हैं। वे मानते हैं कि कविता जीवन में अतिरिक्त जगह की तरह आती है वह जबरन नहीं आ पाती।
‘लिखना जीने का ढंग है’ एक लेखक लिखते हुए इस तरह सोच पाता है।
जैसा कि बहुत से लोगों को पता है कि वे अपनी कविताएं टाइप राइटर पर लिखा करते हैं टाइप राइटर पर ही उन्होंने अपने लेखन का बहुत सा कार्य किया। वे कहते हैं कि कलावाद हिंदी में एक लोकप्रिय लांछन की तरह है । उन्हें पता हैं कि हिंदी की दुनिया कलावाद को सह नहीं पाती। वे साझा करते हैं कि हर सच्चे कवि को तिरस्कार के लिए तैयार रहना चाहिए क्योंकि ऐसा होता आया है। जबकि यह भी सच है कि बेहतर कवि होने का अभिप्राय यह नहीं है कि वह बेहतर मनुष्य भी हो।
वे मानते हैं कि आज की कविता में आत्मसंघर्ष अनिवार्य है उन्होंने सामाजिक दायित्व को भी एक कवि की तरह ही निर्वाह किया। वे कविता को लिखने के साथ ही उसके पाठ के भी उतने ही बड़े हिमायती हैं। “ मुझे लगता है कि फेसबुक पर कविता डालने के अलावा अगर साथ- साथ कवि या कवियित्री उसे पढ़े भी तो बेहतर सम्प्रेषण हो सकता है।”कदाचित यही कारण है कि वे कविता लिखने के साथ कविता पाठ पर भी उतना ही जोर देते हैं। वे शीर्षक को कविता की खिड़की मानते हैं।
इस साक्षात्कार पुस्तक में अशोक जी मनुष्य, कवि, कविता और जीवन के बहुत से धुर्वांतो पर बात करते हैं। वे मानते हैं कि लेखक को अपने समय को लेकर चौकन्ना होना होगा। उनका मानना है कि “ इस देश की बहुलता ही सच्ची एकता है वो सदियों से रही है । उसमें किसी एक भाषा, एक वर्ग, एक धर्म का वर्चश्व उसकी मौलिकता का ही खंडन होगा।” कवियों और लेखकों का काम सोते हुओं को जगाना भी होता है। अभिव्यक्ति लोकतंत्र में बहुत आवश्यक होती है।
वे पत्रकारिता पर भी सवाल उठाते हैं कि आज के अखबार सच को छुपा रहे हैं और झूठ को फैलाने का काम कर रहे हैं। वे प्रश्नवाचकता को छोड़ रहे हैं। बहुत कम पत्रकार हैं जो हाशिये का सच सामने लाने की कोशिस कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हम बैचैन लोग हैं पर हारे हुए लोग नहीं हैं। आज के समय में भारतीय नागरिक अधिक लोकतांत्रिक हैं सत्ता कम लोकतांत्रिक है।
“ कवि की वफादारी प्रथमतः और अंततः कविता भाषा- कल्पना – सचाई के प्रति होती है और अगर कोई शिविर इनके आड़े आए तो लेखक को उससे जल्दी मुक्ति पाकर अपनी स्वतंत्रता पर इसरार करना चाहिए। “
मिथकीय रचनाएं सदैव होती रही हैं। मनुष्य कितना भी आधुनिक हो जाये वह अपनी संस्कृति, परम्परा से बाहर नहीं है। इसीलिए वर्तमान में अतीत पर रोशनी डालती कुछ रचनाएं बार- बार लिखी गई हैं। “ वर्तमान की रचना और अतीत की पुनरर्चना साहित्य लगभग स्वाभविक रूप से करता आया है। हमारे यहां साकेत, राम की शक्तिपूजा, कामायनी, अंधा युग, संशय की एक रात, उर्वशी, एक कण्ठ विषपाई ऐसी ही आधुनिक काव्य कृतियां हैं।” इस तरह से अतीत पुनः पुनः हमारे सम्मुख होता है।
जो रची जाने वाली कृतियां हैं उनका मूल्यांकन किस तरह से होता रहा है । इस संदर्भ में वे कहते हैं कि सच्ची,खरी और निर्भीक तथा जिम्मेदार आलोचना हमेशा से कम रही है। अभिप्राय यह है कि इस देश में जिस तरह से अन्य कामों में अक्सर गफलत देखने को मिलती है वह आलोचना में भी अपने को रोंपे हुए है।
हिंदुत्व को परिभाषित करते हुए वे कहते हैं कि “ हिंदू परम्परा का एक अनिवार्य पक्ष रहा है प्रश्नवाचकता, विवाद और सम्वाद। उपनिषदों से लेकर ‘रामायण’ और ‘महाभारत’ छहों शास्त्रीय दर्शन सभी प्रश्न प्रधान ग्रंथ या वृतियां हैं। यह माना जाता है कि बिना पूंछे ज्ञान नहीं मिल सकता। नचिकेता यमराज से और अर्जुन कृष्ण से प्रश्न पूंछते हैं।” हिंदू मानस का अंतिम पुनराविष्कार महात्मा गांंधी से सम्भव हुआ था।
उन्होंने अपनी कविता में देवताओं का रूपात्मक इस्तेमाल किया है।
चूंकि अशोक जी साहित्य और कला को पढ़े लिखे जाने की जोर जुगत में पूरा जीवन भरसक लगे रहे हैं सम्भवतः इसे साहित्य के सभी प्रेमी स्वीकार कर सकेंगे। वे लिखते हैं कि “ मैंने दूसरों की कविता के आस्वादन, समझ और सराहना के लिए सैकड़ों अवसर मंच, पत्रिकाएं , आयोजन आदि जुटाए। “
स्त्रियों के लिखे जाने को वे इस प्रकार सम्बोधित करते हैं कि “साहित्य के लोकतंत्र का कुछ विलम्बित विस्तार है। वह साहित्य के भूगोल में अनेक नये और अप्रत्याशित अनुभव बिंब- छवियां – विडम्बनाओं को शामिल कर उसको विस्तृत कर रहा है। “ अशोक जी प्रगतिशील हैं यही प्रगतिशीलता उन्हें विभिन्न प्रकार की साहित्यिक गतिविधियों से जोड़ती रही है।
उनका मानना है कि लिखो तो इस तरह लिखो। जहां डर झेंप सब परे हो जाएं। लेखन में साहसी होना अनिवार्य है सच्चा होना भी जरूरी है।
अपने उत्तर के हवाले से वे कहते हैं कि “ साहित्य में कोई भी चित्रण फिर वह किसी सम्बन्ध, घटना, प्रसंग, प्रकृति, यौनिकता आदि का क्यों न हो ईमानदार, सच्चा, सम्वेदनशील होना चाहिए। ऐसा होकर ही वह साहित्य में अभिव्यक्ति का भूगोल विस्तृत या गहन करता है।”
स्त्री -पुरुष के प्रेम से जुड़ा साहित्य भारतीय समाज का अभिन्न हिस्सा रहा है। मंदिरों में उकेरी गयी कलाकृतियों में इसकी झलक देखने को मिलती है। फिर इसे कैसे मान लिया जाय कि यह अश्लील है। “ भारत की श्रेष्ठ प्रेम- रति कविता, दसवीं शती में लिखी गयी जयदेव की ‘गीत गोविंद’ है जो आज भी केरल के गुरुवायूर मन्दिर में हर दिन गायी जाती है। तमिलनाडु के भरत नाट्यम और उड़ीसा के ओडिसी शास्त्रीय नृत्यों में उसकी रोज ही अष्टपदियां गायी नाची जाती हैं। “
पुस्तक में बहुत से द्वीप हैं जहां कई पगडण्डियां खुलती नजर आती हैं जो जानने,सीखने और रचने के क्षितिज की ओर ले जाती हैं।जीवन अंतर्विरोधों का अंतहीन सिलसिला है, यह भी अशोक वाजपेयी अपने वक्तव्यों में कहने से नहीं चूकते ।
दरअसल पूरी पुस्तक रचनाशीलता को जानने समझने का सिलसिला है जिसमें धूप और छांव पाठक को दोनों मिलती है। पूनम अरोड़ा के प्रश्नों में गम्भीर दृष्टि की परख है वे उस शब्द भंगिमा को पकड़ने में कामयाब रही हैं जहां का प्रतिफल पठन पाठन की दुनिया के बेहतर विकल्प को प्रस्तुत करता है।
पुस्तक से सीखा जा सकता है। भाषा भी इसकी समृद्ध है। पढ़ते समय किंचित यह तो लगता है कि पढ़ने गुनने का जो माहौल अशोक जी के पास था क्या वह अन्यों का भी हासिल हो सकता है तो प्रत्युतर मिलता है वह सबके पास नहीं हो सकता। पर दृष्टि अवश्य अर्जित की जा सकती है।