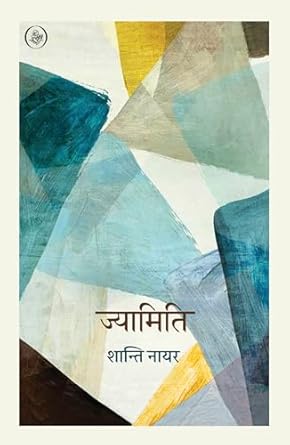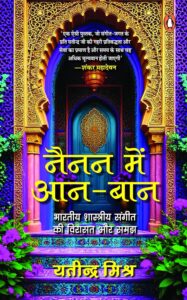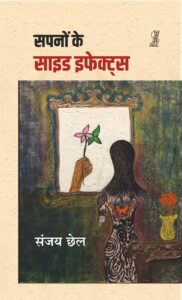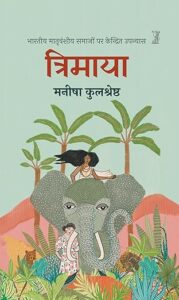शांति नायर के कविता संग्रह ‘ज्यामिति’ पर यह विस्तृत टिप्पणी लिखी है जानी-मानी कवयित्री सुमन केशरी ने। राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित इस संग्रह पर सुमन जी ने जो लिखा है यह उन कविताओं की व्याख्या भी करती है और यह अपने आप में एक स्वतंत्र पाठ भी है। आप भी पढ़ सकते हैं- मॉडरेटर
======================
अगर मैं कहूँ कि शांति नायर के संकलन- “ज्यामिति” की कविताएँ अच्छी हैं, तो अगला ही सवाल होगा क्यों? यानी कि इन कविताओं या किसी भी कविता को अच्छा कहने के मेरे मानदंड क्या हैं।
सबसे पहली बात विषय की विविधता, उसके चयन में कवि की संवेदनशीलता, उसका निर्वाह, यानी कि उसे कैसे प्रस्तुत किया गया है। निर्वाह में वैविध्य, अर्थात् एक ही विषय को लेकर लिखी गई कविताएँ दुहराव का शिकार तो नहीं हो गईं।
दूसरी बात कविता की अर्थवत्ता से संबद्ध है। कविता कितने अर्थ संभव करती है। कैसे व्यंजित होती है। व्यंजित होने वाले अर्थ क्या पाठक के मन-मस्तिष्क का परिष्कार करते हैं, उनमें प्रश्न उत्पन्न करते हैं?
तीसरी बात है, उन विषयों को भी उठाने का साहस, जिन पर आज कल एक खास ढंग से लिखने का चलन है। मसलन स्त्री या कोई अन्य पीड़ित अस्मिता का चरित्र हर हाल में पीड़ित, दुःखी अथवा अपने समूह के हित में कार्यरत ही होना चाहिए। उसके चरित्र में स्खलन दिखाना उस समूह के संघर्षों के प्रति असंवेदनशील व स्वार्थी होना मान लिया जाता है।
चौथी बात है, अपने आसपास के सामाजिक- राजनैतिक बर्ताव-व्यवहार के प्रति सचेतन ढंग से सोचना, उस पर अपनी बात रखना। उसकी अभिव्यक्ति के लिए नए प्रतीकों, बिंबों व मुहावरों को गढ़ना।
पाँचवी बात है कि कविता लिखी कैसे गई। क्या वह कोई नया, सार्थक अनुभव सृजित करती है। क्या इन कविताओं को पढ़कर लगा कि अरे, ऐसे भी तो बातों को रखा जा सकता है और व्यवस्था का पूरा चित्र सामने उभर आता है! अपने आसपास के अनुभवों, रोजमर्रा के कामकाज और समाज में पैठे मिथकों को देखने का कोई नया अंदाज। क्यों कि कोई भी भाषा-संस्कृति मिथकों के बिना संभव नहीं।
छठी बात है, अतीत के प्रति दृष्टिकोण। कवि अतीत को कुछ खो देने के नॉस्टेल्जिया भाव से देखती है और उसे सपने या कल्पना में पुनः जीने की चाह रखती है या उसे व्यतीत हो चुकने के भाव से देखती हुई, नए या वर्तमान को स्वीकारने का भाव रखती है। क्या यह स्वीकारना यथास्थिति को स्वीकारने जैसा है, अथवा इसमें कोई अन्य भाव भी समाए हुए हैं।
सातवीं बात, क्या कवि कविता को नए शब्द दे रही है। ऐसे शब्द जो आमतौर पर कविता लिखते हुए नहीं प्रयुक्त होते।
और भी कई बिंदु हो सकते हैं, पर ऊपर दिए बिंदुओं के आधार पर जब मैंने शांति नायर की कविताओं को पढ़ा तो लगा- बेशक, इन कविताओं को अच्छी कविताओं की, जरूरी कविताओं की श्रेणी में रखा जा सकता है।
“ज्यामिति” की कविताएँ पढ़ते हुए लगातार यह बात मन में आती रही कि इस कवि के पास कितने विषय हैं, जिनके माध्यम से यह मनुष्य मन की, समाज के बदलते जीवन की, राजनीति व देशकाल की, आर्थिक विसंगतियों आदि की ढेरों बातें कविता में पिरो देती है। संकलन की पहली कविता, संबंधों के महत्त्व को समझते हुए, उन्हें हर हाल में बचा लेने की कोशिश करती स्त्री की उस विवशता व विडंबना का चित्रण है, जो किसी भी कीमत पर जाले साफ़ कर देना चाहती है। “जाले” शीर्षक यह कविता लगभग हर परिवार की असलियत है, परिवार जिसको बनाए-बचाए रखने का भार अमूमन स्त्री के कंधों पर होता है, क्योंकि वह जानती है मानव जीवन में संबंधों के महत्त्व को। और संकलन की अंतिम कविता शीर्षक कविता है- “ज्यामिति”। यहाँ ज्योमेट्री के विभिन्न अंग- कोण, रेखा, त्रिकोण आदि के माध्यम से स्त्री-पुरुष संबंधों में निहित गैरबराबरी यूँ व्यक्त होती है, मानो जीवन का अंतिम सच वही है। बिंदु व रेखा लड़की/स्त्री सूचक हैं और कोण पुरुष सूचक। जरा देखें-
नुकीला त्रिकोण ज्यामिति का पहला पुरुष है
फिर चतुर्भुत आयत सभी पुरुष ही हैं
षट्कोण, अष्टकोण आदि की तो बात ही क्या
जिनके पास जितने नुकीले कोण हैं
वे उतने ही अधिक पुरुष हैं
तमाम बिंदु उनके अधीन हैं
बिंदुओं को बांधती रेखाएं भी हैं
वे युगों से नोकों को सहेज रही हैं…
ज्यामिति के आधार पर कितनी सहजता से शांति नायर स्त्री-पुरुष संबंधों की जमीनी हकीकत को सामने रख देती हैं। इस कविता के साथ मेरी दृष्टि में “मुनिवर और इडली” कविता को पढ़ा जाना बेहद जरूरी है। यह कविता ऋषि गौतम और अहिल्या प्रसंग पर है। गजब आधुनिक बोध की कविता है यह और साथ ही स्त्री की यौनिकता का रेखांकन करती कविता भी। घोल में खमीर उठने से पहले अगर इडली स्टीम होने के लिए रख दी जाए तो इडली सख्त ही बनेगी। और स्त्री? बिना उसकी शारीरिक जरूरत, प्रेफ़रेंस, सेक्स के लिए उसे व्यवस्थित रूप से उद्बुद्ध किए बिना अगर कोई पुरुष स्वयं को उस पर थोपता रहे, तो उसमें ठंडापन (फ़्रीजिडिटी) आना स्वाभाविक है और फिर उस पर पथराई होने का इल्जाम लगा देना कितना आसान। छोटी-सी कविता अनेक धरातलों पर खुलती, पाठक के मन में गौतम व अहिल्या के बारे में ढेरों प्रश्न जगा, उसके चित्त को पुनर्परिष्कृत करती है। आम, रोजमर्रा का व्यंजन इडली, और उसे पकाने की विधि का ऐसा मार्मिक प्रयोग! एक सचेत, जाग्रत स्त्री ही यह कविता रच सकती थी। इस कविता की ध्वन्यात्मकता पर ध्यान देने की भी जरूरत है। इस दृष्टि से कुछ अन्य कविताओं के साथ इस कविता को इस संकलन का हासिल कहा जा सकता है।
मुनिवर, सीख लेने चाहिए
घर के जरूरी काम (काम की द्विअर्थकता पर ध्यान दें)
घर बसाने से पहले
मालूम होना चाहिए आपको
घोल में खमीर उठने से पहले
चढ़ा दी जाए चूल्हे पर तो (सेज/सेक्स)
इडली सॉफ़्ट नहीं बनती
जमाना काफ़ी बदल चुका है
मुश्किल होगा लोगों को बहकाना
कि युगों की तपार्जित शक्ति से जनित
प्रचंड ताप से पथराई हुई है इडली (इडली में स्त्री को पढ़ें)
मिथक का अद्भुत आधुनिक प्रयोग है यह। मिथक जो हमारे मानस का अविभाज्य हिस्सा हैं, हमारी भाषा का जरूरी अंग। मिथकों का ऐसा ही अद्भुत प्रयोग “दावत की तैयारी” कविता में दिखलाई पड़ता है, जहाँ एक आदेशात्मक स्वर (सास जैसा) सभी बहुओं को काम करने को कहता है। कमाल इस बात में है कि ये बहुएँ कोई आम स्त्री नहीं बल्कि कैकयी, कौशल्या, सुमित्रा, उर्मिला, श्रुतकीर्ति, मांडवी व सीता के साथ साथ मंदोदरी, सूर्पनखा, ताड़का आदि भी हैं, यानि कि देवियों के साथ राक्षसियाँ भी। आखिर स्त्रियाँ तो सभी हैं, फिर उनमें भेद क्यों। रसोई तो सबको संभालनी है- देवी हो, मुनि-पत्नी अहिल्या हो या राक्षसियाँ। यह कविता देर तक मन में गूंजती रही, उसी तरह जैसे “पुट्टू बनाती लड़की”, जिसे पढ़ने के बाद लगा- पुट्टू बनाती या बनती? लड़की को पुट्टू की तरह देखना एक नए बिंब का सृजन है। यह व्यंजन भुने-गूंधे गए चावल को साँचे में ढाल कर बनाया जाता है। क्या औरत को भी सांचे में ही नहीं ढाला जाता? सोच-संस्कारों का ढांचा! ये सारी कविताएँ एक ओर तो स्मृति कोश में संचित कथाओं, शब्द-संपदाओं को जगाने वाली हैं, तो दूसरी ओर प्रदत्त मान्यताओं व विचारप्रणाली को प्रश्नबिद्ध करना सिखाने वाली रचनाएँ भी हैं। अपनी संरचना में इनमें से अधिकांश कविताएँ ध्वन्यार्थ प्रधान है। यहाँ पर “वृत्त” शीर्षक कविता का उल्लेख न करना भूल होगी। क्या यह सच नहीं कि छोटी बच्चियाँ स्कूल से लौटकर खेल खेल में टीचर की भूमिका अपना लेती हैं और बहुत गंभीरता से क्लास लेती हैं। इस कविता में भी वृत्त बनाना सीखती लड़की अपनी छोटी बहन को सिखाती है- केन्द्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं ‘त्रिज्या’… और छुटकी तुतलाती बोली में दुहराती है- केन्द्र से परिधि तक की दूरी को कहते हैं ‘तिरिया’। अब जरा इस कविता की ध्वन्यात्मकता पर ध्यान दें। केन्द्र यहाँ पुरुष का और उससे परिधि तक की दूरी- तिरिया अर्थात् स्त्री का प्रतीक है! एक पूरा दृश्य बनता है – बच्ची का मास्टरनी अवतार में पढ़ाने का। और कवि केवल एक शब्द- तिरिया- द्वारा पितृसत्ता में निहित गैरबराबरी का बखान कर देती है। यह कविता बहुत गहरे अर्थों में स्त्रीवादी कविता है। किंतु शांति नायर की दृष्टि यहीं तक सीमित नहीं है। वे स्त्रियों को केवल दबा दी गई अस्मिता के प्रतीक के तौर पर नहीं, बल्कि हाड़-मांस के ऐसे इंसान की तरह भी देखती हैं, जो अपनी एजेंसी का दूसरे को नष्ट करने के लिए भी निःसंकोच इस्तेमाल कर सकती है। “हत्या” ऐसी ही कविता है- कभी हुस्न के बाजार में…कभी मुस्कुराते मुस्कुराते..। मजे की बात यह है कि इस कविता के बारे में जब स्वयं कवि से बात हुई तो उनका कहना था कि “इस कविता में स्त्री दबी हुई है। वो हत्या करती है उत्तम पुरुष की और यह जो उत्तम पुरुष है, वह व्याकरण का उत्तम पुरुष हैयानि कि मैं, स्त्री अपने भीतर के “मैं” की हत्या कर रही है।” इस बातचीत के बाद मैंने उस कविता को एक बार फिर पढ़ा और मेरा पाठ वही था, जो मैंने ऊपर लिखा है, यानि कि जरूरी नहीं कि दबी अस्मिता के लोग क्रूर व अपराधी नहीं हो सकते। मनुष्य हैं, तो मनुष्यवत् वे कुछ भी सोच-कर सकते हैं, वैसे ही जैसे पुरुष! यहाँ पर इस कविता की वह ताकत दिखी पड़ती है, जिसे हम व्यंजना या बहुअर्थी होना कहते हैं। लिखने वाले व पढ़ने वाले, दोनों ने अपना अपना पाठ रचा। इसीलिए एक कवि और कविता की पाठक होने के नाते, मैं यह जोर देकर पुनः कहना चाहती हूँ कि कोई भी रचना और खासतौर से कविता बार बार सृजित होती है। की बार तो एक ही पाठक हर पाठ के साथ एक नया अर्थ पा लेता है। यह रचना की ताकत का सबूत तो है ही, पाठक के तैयारी को भी दर्शाता है।
शांति नायर की कविताओं में समाज कई रूपों में व्यक्त होता है। कहीं वह “गोंद” बन कर इतने रूपों में आता है कि वह कभी भय है, तो कभी बैर, कभी पूंजी है तो कभी चाशनी या मुस्कान ही। गोंद को ऐसे देखने का तरीका उस व्यंग्य शैली की उपज है, जो बड़े नामालूम ढंग से सही जगह पर चोट कर जाती है। इसी तरह “दूध फटना” कविता में खटाई शब्द का प्रयोग व्यापक संबंधों में आ रहे अविश्वासजनित खटास का सूचक है, जिसमें न आमिना के लिए पायसम बचाया जा सकता है और न कवि के लिए अब सिवइंया ही बचती हैं। इसी तरह से “गुब्बारे” कविता का एक वाक्य याद रह जाता है- हल्की चीजें आसानी से ऊपर उठ जाती हैं…। इन्हीं कविताओं के साथ “था और है के बीच”; “मूकम करोति वाचालम”; “दुनियादारी”; “कटना”; “लोकतंत्र में बौने”; “चर्चाएँ”; आदि कविताएँ राजनैतिक कविताएँ कही जा सकती हैं। इन कविताओं में शांति नायर की पक्षधरता बहुत साफ़ दिखाई पड़ती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे कि “एडजस्ट करो एंजॉय करो” में लड़की अम्मा को बताती है कि यह मॉल है, महल नहीं…इसी कविता में एक वाक्य विकास की पूरी अवधारणा पर मानो सवाल उठा देता है- “नहीं अम्मा, भटकी तुम नहीं/जाने कौन भटका और कब”। यह कविता अम्मा को सिखाती है कि “तेरहवीं मंजिल के फ्लैट पर/खुश रहो बेटे के ठाठ पर…हाँ रही बात थोड़े-से सुकून की/तो कुछ एडजस्ट करो अम्मा…” कैसा गहरा विडंबनाबोध इन दो पक्तियों से उत्पन्न होता है, यह बात पढ़कर एकदम समझ आ जाती है। महलों की तरह के मॉल और जमीन से जाने कितनी दूर घर, कि सही सही पाँव टिकाने का भी आसरा न रहे। बुढ़ापे में जो शरीर मिट्टी में मिलने को तैयार है, वह हवा में तैर रहा है! हम देखते हैं कि अपनी कविताओं में शांति नायर अर्थ के अनेक स्तर उद्घाटित करती चलती हैं। एक बात और ध्यान देनी चाहिए कि शांति नायर कुत्ते को विषय के रूप में बार बार प्रयोग करती है। वैसे भी समाज में कुत्ता कई मुहावरों से संबद्ध है। ये कविताएँ यह भी बतलाती हैं। “देसी कुत्ते”; “अहाते का कुत्ता”;”कुत्ता जी”; “कुत्ता और नाम”. इन सभी कविताओं में यह प्राणी-विशेष कब अपना रूप छोड़ मानव-अवतार ले लेता है, यह बात देखते ही बनती है। व्यंग्य काव्य के बेहतरीन उदाहरण है ये कविताएँ। इनमें दुहराव नहीं है, यह बात नोट करनी चाहिए।
एक और अन्य बात जिस ओर मेरा ध्यान गया, वह है अध्यापन के लिए नियत कोर्स में से ही विषय उठा अद्भुत कविता रचने का प्रयास।इस संग्रह में कई कविताएँ ऐसे ही लिखी गई हैं। मसलन “व्याकरण का पर्चा”। यहाँ जितनी भी स्त्रीवाचक संज्ञाएं हैं, उन्हें खाया जाना है (रोटी), जलना है (बाती) कटना है (तरकारी) आदि और पुल्लिंग हैं- चूल्हा, चाकू, दीया। सच में पढ़कर मन सिहर गया कि “बिस्तर पुल्लिंग होता है/उस पर बिछने वाली चादर स्त्रीलिंग/रति शब्द स्त्रीलिंग होता है/मगर सुख हमेशा होना चाहिए पुल्लिंग/…
जब मैंने किताब को पहली बार खोला, तो अपनी आदत के अनुसार जो पृष्ठ खुला, उस कविता को पढ़ने लगी। बरसों से किताब पढ़ने का मेरा तरीका यही रहा है।जो पेज खुले, वहीं से शुरुआत हो। पृष्ठ बीस पर छपी “अनुतान” ही इस संग्रह की पहली रचना थी, जिसे पढ़कर, अनुतान का अर्थ जानते बूझते भी मैंने गूगल किया और फिर तुरंत शांति जी को फ़ोन कर उनसे अर्थ पूछा।शब्द कैसे कहा गया, बलाघात कहाँ था, कितने उत्साह या उपेक्षा से कहा गया- आदमी की हैसियत इसी से पता चलती है। यह बात बहुत मार्मिक व प्रभावी ढंग से कविता बताती है। कविता शुरु होती है-
आदमी का बच्चा
जब सीखता है भाषा
वाक्य से पहले
शब्द से पहले
आत्मसात करता है अनुतान को…
इस कविता का वितान बहुत बड़ा है। यह कविता लिंग भेद से शुरु होकर आर्थिक सामाजिक स्तर पर मनुष्य की हैसियत को सामने ला रखती है। इस दृष्टि से यह बात निःसंकोच कही जा सकती है कि शांति नायर की चिंताएँ समाज के विभिन्न वर्गों से जुड़ी चिंताएँ हैं, वे निःसंकोच अपनी रचनाशीलता का दायरा बढ़ाए चलती हैं। मेरी दृष्टि में एक अच्छा कवि होने का यह पहला सोपान है, कि अपनी रचना का दायरा सिमटा मत रहने दो। हर मन में प्रवेश करो, साहित्य संभव ही होता है, परकाया प्रवेश द्वारा।
लिखते-पढ़ते हुए मैं अक्सर एक और काम करती हूँ। मैं कवि-कथाकार से (अगर संभव हो और संपर्क भी हो तो) उनकी प्रिय रचनाएँ जानना चाहती हूँ। इससे कई बातें एकसाथ सध जाती हैं। एक तो उन रचनाओं को पढ़ लिया जाता है, जो कोई भी लेखक चाहता है कि जरूर पढ़ा जाए और दूसरे उस लेखक की चिंताएँ, उसके सोच की स्थिति आदि का भी एक किस्म से आकलन हो जाता है। जब मैंने शांति नायर से उनकी प्रिय कविताओं के बारे में जानना चाहा, तो बहुत संकोच के साथ उन्होंने कुछ शीर्षक लिख भेजे। सौभाग्य से ये रचनाएँ मुझे भी उल्लेख योग्य लगी थीं। आप भी देखें- “व्याकरण का पर्चा”; “रामायण”; “गोंद”; “जाले साफ़ करती स्त्री”; “दस्ताने”; “कुत्ता और नाम”; “ज़ब्ती”; “अनुतान”; “अंततः”; “मत लिखा कीजिए” और “ज्यामिति”।
अंत में जिस कविता पर मैं कुछ विस्तार से बात करना चाहती हूँ, वह है- “रामायण”। इस कविता ने मुझे कई स्तरों पर छूआ। पुरुष जिस रामायण का पाठ कर रहा है, वह रामकथा वाली रामायण है, संभवतः तुलसीदासकृत रामचरितमानस। पुरुष चाहता है कि स्त्री भी इस रामायण को पढ़े, अगर पढ़ना संभव नहीं तो बैठकर कुछ सुन ही ले, ताकि कुछ तो अर्थ समझ में आ जाए। मगर स्त्री की स्थिति बिल्कुल उलट है। जब आर्यपुत्र नहा धोकर, ताजादम रामायण पढ़ रहे हैं और स्त्री को भी साफ़सुथरी होकर उसे पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तब वह स्त्री देख रही है कि चावल को पकने में लगेगा कुछ और समय/ आटा गुंथ चुका है/ बेलनी-सेंकनी है रोटियाँ/ दाल में छौंक लगा चुकी हूँ/ पक रहा है साग/ पीसनी है चटनी अभी…
यह तो स्थिति है, पर अगली पंक्तियाँ मार्मिक हैं और कविता वहीं है-
खुरदरी हथेलियों से
मैं लगातार
पलटती जा रही हूँ पन्ने
इस पुरातन रामायण के
अभी और
कुछ और
बस कुछ और
अनगिनत हैं इसमें चौपाइयाँ
कहना चाहती हूँ मैं भी-
कुछ चौपाइयों का ही सही
कर लीजिए वाचन आप भी
पर जानती हूँ
नहीं सिखाई गई होगी
यह लिपि आपको कहीं कभी
पढ़ रही हूँ
युगों से मैं इसे
न हो पाए वाचन अगर आपसे
नहाकर साफ़सुथरे हो आइएगा
देख लीजिएगा तनिक
सुन लीजिएगा जरा
रह ही लीजिएगा थोड़ी देर साथ
कुछ तो समझ आ पाएगा अर्थ!
यह कविता है नयी सदी की औरत का जागृति-गान। रोना-गाना नहीं, साफ़ साफ़ बताना कि आपके रामायण और मेरे रामायण में जो फ़र्क है, उसे जानने के लिए इस बार आर्यपुत्र को आना पड़ेगा। सीखने की तैयारी के साथ। इस कविता को पढ़ते हुए बार बार लगा कि हमारे आर्यपुत्र लोग स्त्री को पढ़ने-बढ़ने की सलाह तो देते हैं, पर वे स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करना चाहते, जिसमें स्त्री निश्चिंत हो कुछ पढ़ सके, कुछ रच सके…कुछ सोच सके!
यह कविता उसी सोचने की दिशा को पाठक के सम्मुख रखती है, इसीलिए सार्थक रचना बन जाती है!
अंत में एक बात का रेखांकन बहुत जरूरी है। शांति नायर दक्षिण की निवासी हैं। इन कविताओं को पढ़ते हुए भाषा में अंतर दिखता है और उपमाओं-बिंबों में भी। मैं के लिए उत्तम-पुरुष का प्रयोग चौंकाता है। अनुतान जैसी रचना नया शब्द दे जाती है। जाते जाते चलिए कविता की जरूरत के बारे में भी जान लें-
कविता का होना
कठिन दुष्कर समय में
तिनका-भर ही सही
डूबते को सहारा देता है
मंझधार में भी किनारा देता है!
आमीन
तो पाठकों! जब मैंने कहा कि शांति नायर एक बेहतरीन कवि हैं, तो क्या बिल्कुल ठीक नहीं कहा!