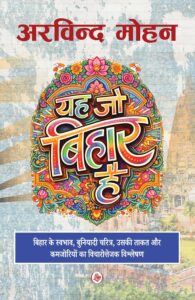मीडिया की भाषा-लीला– यह इस साल की सबसे सुसज्जित पुस्तक है. प्रकाशक वाणी प्रकाशन है. रविकांत की यह हिंदी में पहली प्रकाशित पुस्तक है. महज इससे रविकांत का महत्व नहीं समझा जा सकता है. पिछले करीब तीन दशकों में इतिहासकार रविकांत ने दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी पढने वाले विद्यार्थियों को जितना प्रभावित किया उतना शायद हिंदी के किसी प्रोफ़ेसर ने भी नहीं किया. इस दौरान हिंदी के जितने युवाओं ने हिंदी में अलग ढंग से काम किया वे सब किसी न किसी रूप में रविकांत से प्रभावित रहे. यह एक सच्चाई है. मैं खुद भी उन प्रभावित होने वाले लेखकों में रहा हूँ.
रविकांत मूलतः इतिहासकार हैं. इस पुस्तक में मूलतः सिनेमा की भाषा और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का ऐतिहासिक मूल्यांकन करने वाले कुछ लेख हैं. रविकांत ने हिंदी सिनेमा के इतिहास के ऊपर इतिहास विभाग से पीएचडी की है लेकिन यह किताब उनका शोध प्रबंध नहीं है. बल्कि पुस्तक में उस शोध के दौरान उन्होंने सिनेमा, उसकी भाषा को लेकर कुछ अलग-अलग लेख लिखे थे उसको एक साथ संकलित किया गया है. लेखक ने सिनेमा और रेडियो की भाषा और उसके ऊपर साहित्य के प्रभावों, भाषा के बदलते रूपों को लेकर भूमिका में विस्तार से उल्लेख किया है. हिंदी सिनेमा की ऐतहासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिहाज से ‘मीडिया की भाषा लीला’ की भूमिका पढने लायक है.
लेखक की चिंता के केंद्र में सिनेमा की, माध्यमों की भाषा है- हिंदी-उर्दू का द्वंद्व. आज हिंग्लिश भाषा का सिनेमा में जोर है लेकिन लेखक ने अपने एक लेख में यह याद दिलाया है कि असल में हिंदी की आड़ में उर्दू के ऐतिहासिक वर्चस्व को हम नजरअंदाज कर रहे होते हैं. इसलिए पुस्तक में लेखक ने उर्दू की उस ऐतिहासिक भूमिका को अपने लेखों के माध्यम से समझने की कोशिश की है. मेरे ख़याल से दो उदाहरन इस सन्दर्भ में दिए जा सकते हैं. हिंदी सिनेमा के सर्वकालिक महान अभिनेता दिलीप कुमार अपनी फिल्मों में खालिस उर्दू में संवाद बोलते रहे और तो वे भी सबसे लोकप्रिय अभिनेता रहे. इसी तरह हिंदी सिनेमा के सबसे लोकप्रिय गीतकार साहिर लुधियानवी रहे, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वे सिनेमा में उर्दू शायरी को लेकर गए और उन्होंने उसको स्थापित भी किया. बहरहाल, लेखक ने अपने लेखों में उर्दू के खालिस शब्दों का जमकर प्रयोग किया है. ऐसा लगता है रविकांत हिन्दुस्तानी भाषा के रूप के नहीं बल्कि देवनागरी में उर्दू लिखने के हामी हैं. भाषा को लेकर उनका दृष्टिकोण बहसतलब है.
किताब में दो लेख ऐसे हैं जिनसे बचा जा सकता था. एक लेख मनोहर श्याम जोशी के उपन्यास ‘कसप’ की भाषा को लेकर है. दूसरा लेख ‘हिंदी वेब जगत: भविष्य का इतिहास’ है. यह लेख वेब पर बरती जाने वाली शुरूआती हिंदी को लेकर है. अब इन्टरनेट पर हिंदी बहुत विकसित हो चुकी है. बहरहाल, इन्टरनेट पर हिंदी के शुरूआती प्रयासों को लेकर यह लेख ऐतिहासिक प्रकृति का है.
पुस्तक में कुल सात लेख हैं. एक लेख सिनेमा की पत्रिका ‘माधुरी’ को लेकर है. जो सिनेमा और साहित्य के अंतर्संबंधों को समझने के लिए बहुत उपयोगी लेख है. हालाँकि हिन्दुस्तानी सिनेमा और उर्दू को लेकर रविकांत ने इस लेख में भी सवाल उठाये हैं. मुझे हैरानी इस बात पर होती है कि रविकांत उर्दू को लेकर तो बहुत बात करते हैं लेकिन हिन्दुस्तानी को लेकर नहीं, जो हिंदी का सबसे प्रचलित रूप रहा है. हो सकता है हिंदी-उर्दू के सवालों को उठाने के पीछे रविकांत की अपनी राजनीति हो.
बहरहाल, रविकांत ने ही हमारे अन्दर प्रश्नाकुलता पैदा की. इसलिए उनकी इस किताब को पढ़ते हुए मन में कुछ सवाल उठे. एक हिंदी लेखक होने के नाते कुछ हिंदी वाले सवाल.
लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक संग्रहणीय किताब है. बहुत दिनों बाद शोधपूर्ण लेखों की ऐसी पठनीय किताब हिंदी में आई है. तमाम तरह के पूर्वाग्रहों के बावजूद यह किताब पढने के लिए मजबूर करती है. सिनेमा में दिलचस्पी रखने वालों को, सिनेमा के इतिहास को लेकर काम करने वालों को इस किताब को जरूर पढना चाहिए.
हालाँकि किताब क नाम ‘मीडिया की भाषा लीला’ क्यों रखा गया यह समझ में नहीं आया?
पुस्तक- मीडिया की भाषा लीला; लेखक- रविकांत; प्रकाशक- वाणी प्रकाशन, मूल्य-395(पेपरबैक)