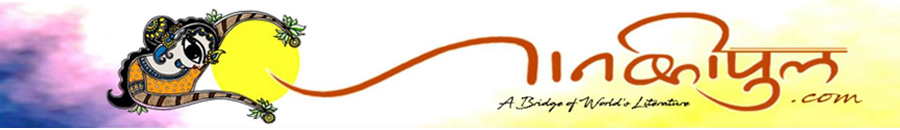ब्यावर, राजस्थान में रहने वाली युवा लेखिका राजनंदिनी राजपूत की यह कहानी इनबॉक्स में आई तो पढ़कर लगा कि साझा करना चाहिए। लिखने में संभावना दिखाई दे रहीं है। आप भी पढ़कर बताइएगा- मॉडरेटर
========================
उमा खरबूजे के फाँकों के बीच खड़ी थी। उसने चाकू उठाया, और फल की नरम, मीठी गंध हवा में फैल गई। फाँके काटते हुए उसकी उंगलियाँ चिपचिपी हो गईं, और उसका मन एक अजीब-सी बेचैनी से भर गया। उसने फाँके काटे, एक-एक करके उन्हें बाँट दिया—भाई के बच्चों को, माँ को, और जो बचा, उसे खुद खा लिया। आखिरी फाँका मुँह में डालते हुए उसने सोचा, “जब फल काटने वाला बीच में खाता है, तो भूखा क्यों लगता है?” यह सवाल उसके मन में चाकू की धार-सा चुभा।उसके विचार बेकाबू थे। “विचार नहीं आते लिखते वक्त,” उसने खुद से कहा, “विचार आते हैं बीड़ी का कश खींचते वक्त… नहीं, भूख से तड़पते वक्त… या फल को खत्म होते देखते वक्त।” उसका दिमाग किसी सूखे कुएँ की तरह था, जिसमें पानी की जगह यादें ठहरी हुई थीं—पीली, मुरझाई, समय की हवा से कटी-फटी।
वह दूसरे कमरे की खिड़की के पास जा खड़ी हुई। बाहर गली में लोग चल रहे थे। एक फेरीवाला चिल्ला रहा था, “खरबूजा! पचास का एक, सौ का दो!” उमा ने सोचा, “पचास, सौ रुपये के खरबूजे वही पचास, सौ रुपये के लगते हैं लेकिन जब भाई अपनी पत्नी के लिए वही खरबूजा लाता है, तो उसे कीमत की फिक्र नहीं होती। दोनों साथ बैठते हैं, हँसते हैं, फाँके काटते हैं, आराम से खाते हैं।” यह ख्याल उसके सीने में किसी काँटे की तरह गड़ गया।
उमा की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। या शायद हमेशा से ऐसी ही थी? वह सोच में डूब गई। गरीबी उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, फिर भी वह खुद को गरीब मानने से इनकार करती थी। लेकिन उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा था। स्मृतियाँ एक-एक करके जाग रही थीं—उनका रंग फीका पड़ गया था, पर उनकी चुभन अभी भी ताज़ा थी।उसकी माँ चारे का ठेला लगाती थी। पिता मजदूरी करते थे। पिता की यादें कम थीं, पर जो थीं, वे उसके दिमाग में किसी पत्थर पर खुदी इबारत की तरह अंकित थीं। वह तीन साल की थी जब पिता की मृत्यु हुई। शायद उसी वक्त उसने अनजाने में यह ठान लिया था कि पिता को याद रखना है—उनके चेहरे की झुर्रियाँ, उनकी खुरदुरी हथेलियाँ, उनकी थकी हुई आँखें।
स्कूल में मैडम ने एक बार कहा था, “तुम इतना चमकते हो, कहाँ से गरीब हो तुम?” यह कहते हुए उन्होंने छात्रवृत्ति का फॉर्म उसके हाथ में थमा दिया था। उमा को समझ नहीं आया था कि यह तारीफ थी या ताना।
कक्षा की एक लड़की ने उससे कहा था, “तुम्हें तो किताबें फ्री में मिल जाएँगी, एक बार मैडम से कहो न!” उमा ठिठक गई थी। “मुझे… मुझे क्यों दे देंगे किताबें?” उसका सवाल हवा में लटक गया था।
एक बार चचेरी बहन सपना के साथ छत पर खेलते वक्त उसकी चप्पल सामने वाले घर में जा गिरी थी। सपना का चेहरा डर से सफेद पड़ गया था। उमा ने हिम्मत जुटाकर आंटी से चप्पल माँगी। “वापस इधर चप्पल आया तो मार दूँगी,” आंटी ने घृणा भरी नज़र से उसे देखते हुए कहा था। उस नज़र ने उमा के भीतर कुछ तोड़ दिया था।
कॉलेज में वह एक ही कुर्ता पहनकर जाती थी। उसे वह कुर्ता पसंद था—हल्का नीला, सादा, उसमें वह सुंदर लगती थी। लेकिन एक दिन एक लड़की ने व्यंग्य में पूछा, “क्या टॉप वगैरह नहीं पहनती हो तुम?” उमा को झटका लगा। उसे समझ आया कि वह रोज़ एक ही कुर्ता पहनने पर हँसी का पात्र बन रही थी।
इंटर्नशिप के दौरान स्टाफ मैडम ने कहा, “मैं तुम्हें अपने कुर्ते दे दूँगी, वही पहनकर आ जाना।” उमा ने तुरंत मना कर दिया, “नहीं मैडम, मेरे पास कपड़े हैं, मैं सिलवा लूँगी।” पर मैडम की आँखों में दया थी, और वह दया उमा को अपनी गरीबी का आईना दिखा रही थी।
एक खरबूजे की कटी फाँकों ने उसके भीतर दबी स्मृतियों को हिला दिया था।
वह सोचने लगी—क्या वह कभी अमीर बनेगी? नहीं, अब वह ऐसा सोचती भी नहीं थी। क्या वह कभी फल आराम से खा पाएगी? क्या वह खरबूजे के फाँकों को काटकर, काँटे वाले चम्मच से, धीरे-धीरे, बिना जल्दबाजी के खा सकेगी? यह ख्याल भी अब उसे दूर की कौड़ी लगता था।
उमा पढ़ने में होशियार थी। कक्षा में हमेशा प्रथम। सबसे होनहार लड़की। लेकिन वह होनहार लड़की कहीं खो गई थी।
कक्षा नौ में उसे फोबिया नाम की बीमारी हुई थी। उस वक्त उसे इसका नाम भी नहीं पता था। अब मोबाइल पर गूगल सर्च करके उसे पता चला था कि इसे फोबिया कहते हैं। इस बीमारी ने उसकी जिंदगी को उलट-पुलट कर रख दिया था।
उसकी माँ जानकी देवी ने छह बच्चों को पाला था—अकेले। उमा को अपनी माँ पर गर्व था, पर इन दिनों गुस्सा भी आता था। क्यों नहीं माँ ने भाइयों को रोका? क्यों उन्हें बिगड़ने दिया? जब उनकी आवाज़ पहली बार ऊँची हुई थी, जब वे छोटों पर, बड़ों पर हावी हुए थे, तब माँ चुप क्यों रही थी?
“पाँचों उंगलियाँ बराबर नहीं होतीं,” माँ हमेशा यही कहती थी।
बीमारी की वजह से उमा की नौकरी छूट गई थी। अब वह भाई के घर में एक कमरे में सिमटी हुई थी। माँ का घर अब माँ का नहीं था। बच्चे माँ के पास नहीं, माँ बच्चों के घर में रह रही थी। उमा ने खुद को उस कमरे में कैद कर लिया था—जहाँ कोई उसे न देखे, न परखे।अब एकमात्र रास्ता शादी था। “शादी,” उसने सोचा, “लड़की का विशेषाधिकार। जहाँ उसे कमाने की ज़रूरत न पड़े। कोई और कमाए, और वह घर संभाले।” पूरी जिंदगी स्त्री होने के नुकसान उठाने के बाद, अब वह इसके फायदे क्यों न ले? पर गरीब की बेटी के लिए ऊँचे घर के रिश्ते नहीं आते।
गाँव के बेरोजगार लड़कों, दुकानदारों के प्रस्ताव आने लगे। उसके ख्वाबों में कोई आर्मी वाला, कोई सफेद शर्ट-पैंट में सजा, लंबा-चौड़ा नौजवान आता था। पर वह ख्वाब देखने से डरती थी। “नहीं,” उसने खुद को ताकीद की, “ऐसा सोचना भी मत। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो तू टूट जाएगी।
“क्या जिंदगी में कभी सुकून होगा? क्या उसका पति उसे समझेगा?
क्या वह कभी खरबूजे के फाँकों को काँटे वाले चम्मच से खा पाएगी? अभी उसके पास कोई जवाब नहीं था।
उसने अपने विचारों को थाम लिया। फिर एक गहरी साँस ली और नौकरी के विज्ञापन ढूँढने लगी।
उमा ने विज्ञापन की उस पतली, मुड़ी हुई कागज़ की पर्ची को हाथ में थाम लिया। स्याही धुँधली थी, जैसे समय ने उसे पहले ही मिटाने की कोशिश कर ली हो।
“डाटा एंट्री, बारह हज़ार महीना, महिलाओं के लिए विशेष अवसर।”
उसने कागज़ को उलट-पलट कर देखा, जैसे कोई पुरानी चिट्ठी हो जो किसी और के नाम लिखी गई हो। कमरे की दीवारें सिकुड़ती हुई मालूम हुईं—उनका प्लास्टर झड़ रहा था, और कोनों में मकड़ियों ने अपने जाले बुन रखे थे, जैसे वे भी उमा की तरह यहाँ फँस गए हों।
वह खिड़की के पास लौट आई। बाहर फेरीवाला अब भी चिल्ला रहा था, “खरबूजा! पचास का एक,
सौ का दो!
शून्य उसके पीछे ऐसे पड़ा था जैसे शून्य की खोज उसने ही की हो।
“शून्य से शुरूआत,” उसने खुद से कहा, “पर इस बार शून्य मेरा नहीं, मुझसे है।” और उस पल में, गली की धूल, फेरीवाले की आवाज़, और खरबूजे की गंध—सब कुछ एक अनंत चुप्पी में डूब गया।
=========================