
मानस चलन्तिका टीका के मटमैले पर्दे पर दास्तान-ए-वैशाली
Memory is the only one of our mental faculties that we accept as working normally when it malfunctions- Mary Warnock
कम लोगों को पता होगा कि जिस प्रतिभाबहुल हिंदी जगत ने एक ओर टेलीविज़न के लिए दूरदर्शन, स्वीमिंग पुल के लिए तरणताल जैसे शब्द गढ़े और दूसरी ओर इंस्पेक्टर के लिए निसपिटर (नासपिटा?), लार्ड के लिए लाट, अल्युमिनियम के लिए ललमुनियां इत्यादि का आविष्कार किया, उसी ने इन दोनों परंपराओं को मिलाते हुए मूवीज़-टाकीज़ यानी चलती बोलती तस्वीरों (के प्रदर्शन की जगह) के लिए एक शब्द दिया है–चलन्तिका टीका। बदकि़स्मती से यह शब्द ख़ुद अचलन्तिका साबित हुआ, पर बिहार के बेगूसराय क़स्बे से संबंध रखने वाले लोग वहां के ऐतिहासिक सिनेमाघर ‘श्रीकृष्ण चलन्तिका टीका’ के कारण इससे परिचित हैं, भले ही वे इसे जातिवाचक संज्ञा न मानते हों। वैसे भी यह मानने से ज़्यादा जानने या पहचानने का मामला है और मेरी महीन मेधा का साधुवाद कीजिए जिसने पहली ही भिड़न्त में इसकी जातिवाचकता के पहचान लिया। तब से जो भी सिनेमाघर मुझे अपना-सा लगा, उसे मैंने इस कुलनाम के साथ ही पुकारा है। यह सब सिर्फ़ इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मानस चलन्तिका टीका को रामचरितमानस का कोई चलताऊ किंवा प्रचलित भाष्य न समझ बैठें। यह तो कोटि-कोटि कविआए हुए जनों द्वारा कोटिशः प्रयुक्त रूपक अलंकार की एक और आज़माइश भर है। मानस चलन्तिका टीका, यानी मन रूपी टाकीज़।… फि़लहाल इसके मटमैले पर्दे पर स्मृति के मायावी प्रोजेक्टर से प्रक्षेपित एक और चलन्तिका टीका–वैशाली–की दास्तान देख-सुन रहा हूं, ज़ाहिर है, सुनाने के लोभ से। मूल में यह दास्तान काफ़ी कुछ धुंधली और विशृंखल है… और इस लिहाज़ से षायद वह दास्तान है ही नहीं। दिक़्क़त ये है कि उस धुंध और विशृंखलता को दूर किए बग़ैर सुनाने का काम हो नहीं सकता। इसलिए कुछ तो उस मायावी प्रोजेक्टर के चलते, जो माध्यम होने के साथ-साथ बहुधा हमारी ज़रूरत को भांप कर संपादक और सर्जक की भूमिका अखि़्तयार कर लेता है, और कुछ मेरी सचेत कोशिशों के चलते, अपने शब्दावतार में यह दास्तान काफ़ी हद तक सुसंबद्ध दिखाई पड़ेगी।
काश, स्मृति मूलतः इतनी व्यवस्था-प्रिय होती!
अब याद नहीं कि वह ख़बरनवीस कौन था जिसने हमारी सांध्य-सभा में यह स्कूप पेश किया कि ‘कौमनिटी सेंटर के पिछुअत्ती ए गो हॉल बनेगा।’ पटना में उन दिनों हॉल कहा जाए तो मतलब होता था, सिनेमा हॉल। दूसरे स्थानों और कालों में भी यह मतलब होता होगा, पर शायद तभी जब शब्द के प्रयोग का संदर्भ स्पष्ट हो। मसलन, ‘फलां फि़ल्म किस हॉल में चल रही है?’ मैं जिस भाषिक व्यवहार की बात कर रहा हूं, उसमें बिना किसी स्पष्ट संदर्भ के भी ‘हॉल’ का मतलब सिनेमा हॉल ही होता है, या कहिए, होता था। यह शायद उस ठिगने शहर का अपना तरीक़ा था, सिनेमा घरों की विराटता के प्रति सम्मान व्यक्त करने का। चारमंजि़ला इमारतें तक उन दिनों मुश्किल से मिलती थीं और हमने सुन रखा था कि बंबई में पच्चीसवीं मंजि़ल पर रहने वालों के घरों में आक्सीजन का सिलेंडर, एहतियातन, हमेशा मौजूद रहता है। इस सुनावत पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं थी। हम पढ़े-लिखे बालक थे और हमें पता था कि ऊंचाई के साथ-साथ वायुमंडल विरल होता जाता है।
बहरहाल, हॉल बनेगा की खुशी को अभी हम सहेज भी नहीं पाए थे कि ख़बरनवीस ने एक झटका दिया, गोया चुंबन के बाद चांटा, बक़ौल राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह। बताया, ‘बनेगा, बाकी अभी टाइम लगेगा। रिजर्व बैंक वाला लोग केस कर दिया है कि हमारा क्वार्टर के सामने हॉल नहीं बनना चाहिए। फैमिली वाला जगह है ना! हॉल बनने से त लफुआ सब का जुटान होने लगेगा।’ रिज़र्व बैंक वालों का इस तरह राजेंद्र नगर मोहल्ले की महान सांस्कृतिक उपलब्धि के आड़े आना हम सभी को बेहद नागवार गुज़रा। हमने सर्वसम्मति से इस लोकोक्ति को दुहराया कि ऊपर वाला सब कुछ देखता है; उसके यहां देर है, अंधेर नहीं। दो-एक ने तो लगे हाथ कभी इस बैंक में खाता न खुलवाने की क़सम खा ली और मेरी पक्की जानकारी है कि वे आज तक इस पर अडिग हैं।
अंधेर सचमुच नहीं था। रिज़र्व बैंक क्वार्टर्स वाले केस हार गये। ऐसा कुछ हक़ीक़त में हुआ था या कि अफ़सानों और अफ़वाहों में ही केस लड़ा भी गया और जीता-हारा भी गया, मैं नहीं जानता। पर यह सच है कि कुछ समय बाद हॉल बनने की शुरुआत हो गयी। यह सन् 75-77 के बीच का कोई समय रहा होगा जब संपूर्ण क्रांति की लहर के साथ शहर के तमाम लफंगों ने अपने को क्रांतिकारियों में शुमार करा लिया था और प्रतिक्रिया में भद्र समाज का एक बड़ा हिस्सा तमाम क्रांतिकारियों को लफंगों में शुमार करने लगा था। हॉल बनने की शुरुआत का जब समाचार मिला तो हममें से कइयों ने क्रांतिकारी लफंगों और लफंगे क्रांतिकारियों के मुंह से सुनी हुई बात ‘जे. पी. जिंदाबाद’ का उद्घोष किया। उत्साह के भाव को रसदशा तक पहुंचाने का यह माना हुआ तरीक़ा था। एक मित्र ने तो, जो उम्र में मुझसे तीन-चार साल बड़ा यानी चौदह-पंद्रह की लपेट में रहा होगा, उत्साह में क़दमकुआं थाने के गेट पर खड़े बंदूकधारी सिपाही को मामू कह कर हुलका दिया और फिर यज्जा-वज्जा शैली में भाग खड़ा हुआ। यह भी इमरजेंसी के दौर में उत्साह को व्यक्त करने की एक लोकप्रिय पद्धति थी। इसी में कभी तथाकथित मामू पीछे पड़ जाये तो पद्धति ज़रा मंहगी पड़ती थी। उस दिन भी हममें से एक को मुख़बिर बना कर मामू ने उत्साही बालक पुन्नू का घर खोज ही लिया। फिर उसे यह समझाने में पुन्नू के घर वालों को ख़ासी मेहनत करनी पड़ी कि लड़का हाॅल के ‘साइड’ यानी ‘साइट’ पर गया हुआ था और उसका काम चालू देख कर उत्साह में आ गया था। फिर जो कुछ हुआ, वह तो स्वाभाविक ही था। इसमें लड़के का क्या क़सूर!
बात वाजिब थी। हमारे इलाक़े को एक सिनेमा हॉल की जितनी सख़्त ज़रूरत थी और हॉल बनने की उम्मीद जगते ही इस ज़रूरत को जितनी शिद्दत से महसूस किया जाने लगा था, उसे देखते हुए पुन्नू का उत्साह और तज्जनित कर्म अनुचित नहीं था। उत्साह के कारणों की चर्चा आगे होगी; जहां तक तज्जनित कर्म का सवाल है, वह दौरे-जहां से मिली हुई एक रस्म की अदायगी भर थी, कोई मौलिक उद्भावना नहीं। इसके लिए भला एक बालक को क़सूरवार कैसे ठहराया जाता! दौरे-जहां का करिश्मा क्या था, यह इससे समझिए कि पप्पू के छोटे भाई (प.छो.भा.) ने, जो उन दिनों बोलना सीख ही रहा था, राइम-रटंत की शुरुआत ‘जाॅनी जाॅनी यस पापा’ या ‘मछली जल की रानी है’ जगह ‘देवकांत बरुआ, इंदू जी के … (तुक मिलाएं!)’ से की थी और वह भी बिना किसी के सिखाए। उम्र के थोड़े फर्क के बावजूद हमारी पीढ़ी की हालत कमोबेश प.छो.भा. जैसी ही थी। हमें भी न तो उस उथल-पुथल के टुच्चेपन की समझ थी, न ही उसके औदात्य की। तभी तो रात के आठ बजे जब हमारी गली से सौ क़दम के फ़ासले पर स्थित लोकनायक जयप्रकाष के आवास से थाली और कनस्तर बजने की आवाज़ें आनी शुरू होतीं और चंद मिनटों में पूरा पटना शहर थालियों-कनस्तरों की ढनढनाहट से गूंजने लगता, तब उसे प्रतिरोध का दिगंतव्यापी नाद मान कर नहीं, बड़ों के बचपने का इज़हार मान कर हमारी ख़ुशी सारे बांध तोड़ने लगती थी। हम उसमें काफ़ी बढ़-चढ़ कर योगदान करते थे जिसे आप चाहें तो प्रतिरोध के कोरस में हमारा ऐतिहासिक योगदान कह सकते हैं, पर जिसके पीछे हमारी प्रेरणा निहायत क्षणवादी होती थी। क्षणों में जीने की यह संकीर्णता एक बार ख़ासी मंहगी पड़ी थी जब रसोईघर से थाली-कनस्तर की मांग पर दुत्कारे जाने के बाद हमारे समवयस्क, तथापि आदरणीय मित्र मनोज जी ने हड़बड़ी में बिजली के खंभे को लोहे की छड़ से पीटना शुरू किया और ऊपर तारों के जमघट में ऐसी संपूर्ण क्रांति मची कि आस-पास के तीन-चार घरों में रात भर के लिए बत्ती गुल हो गयी।
तो कहना ये है कि हम नादान बालक थे और हमारे प्रतिनिधि पुन्नू की कारस्तानी प.छो.भा. की राइम-रटंत जितनी ही निश्पाप थी। हमें तो यह भी पता नहीं था कि सिपाही को मामू क्यों कहा जाता है। आज सोचता हूं तो इसका संबंध उस लोकविश्वास के साथ जान पड़ता है जिसके अनुसार भांजे को पीटने वाले के हाथ बुढ़ापे में कांपते हैं। उन दिनों पुलिस वालों से आंदोलनकारियों की मुठभेड़ें अक्सर हुआ करती थीं। ऐसी ही किसी घातक रूप से मज़ेदार मुठभेड़ में किसी लाठी खाते आंदोलनकारी ने किसी लाठी भांजते सिपाही को मामू कह कर उस लोकविश्वास का लाभ उठाने की कोशिश की होगी। तभी से यह मज़ाक चल पड़ा होगा और उत्साह के हर मौक़े को घातक रूप से मज़ेदार बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होने लगा होगा।
इस विषयान्तर के बाद अब चर्चा उस उत्साह के कारण, यानी हमारी ग़रज़मंदी की। उस समय तक पटना शहर के सभी सिनेमाघर गांधी मैदान और रेलवे स्टेशन के आस-पास थे। ये जगहें तब की यातायात सुविधाओं को देखते हुए हमारे इलाक़े से दूर पड़ती थीं। इससे हमें जो घाटे होते, वे इस प्रकार हैंः (1) अगर वाल्दैन से छुप कर फि़ल्म देखनी हो तो तीन के बजाय साढ़े चार घंटे घर से ग़ायब रहना पड़ता था, जिसमें रिस्क ड्योढ़ा था; (2) अगर अनुमति लेकर फि़ल्म देखना चाहें तो दूरी के नाम पर आवेदन को टाला जाता था। मसलन, ‘अगले महीने चाचा आयेंगे, तब जाना’; और (3) सिनेमाघरों के ‘शो-केस’ में लगे ‘स्टिल्स’ को देखने जैसे छोटे, किंतु अनिवार्य कार्य के लिए इतनी दूरी तय करनी पड़ती थी। ये सभी घाटे उस इलाक़े में रहने के चलते हमें उठाने पड़ते थे जो उस समय से एकाध दशक पहले तक पटना का एक छोर हुआ करता था। राजेंद्र नगर को छूती हुई रेलवे लाइन गुज़रती थी और उसके पार बाइपास था। यही पटना की दक्षिणी सीमा थी, हमारे होश संभालने से पहले तक, ऐसा हमने सुन रखा था। हमारे होशमंद होते-होते बाइपास के उस पार कंकड़बाग़ नामक एशिया की सबसे बड़ी कालोनी तेज़ी से बसने लगी थी। कंकड़बाग़ का अतीत, वर्तमान और भविष्य हमारे इलाक़े के मध्यवर्गीय घरों में अक्सर चर्चा का विषय हुआ करता था। वहां ज़मीन ले चुके लोग किराये के मकानों में रहने वाले अपने ऐसे परिचितों पर तरस खाते थे जो वहां एक कट्ठा ज़मीन तक नहीं ले सके, और वहां ज़मीन न ले पाने वाले यह कह कर अपनी तक़दीर को कोसते थे कि जब हज़ार रुपये कट्ठा ज़मीन मिल रही थी, तब यह सोच कर नहीं ली कि कौन जायेगा उस उजाड़ में रहने! ‘मति मारी गयी थी’–ऐसा यथार्थवादियों का निष्कर्ष होता, और ‘भगवान को मंज़ूर नहीं था’–इस नतीजे पर वे पहुंचते जो अपनी मति का सम्मान बचाने के लिए यथार्थवाद से दूर हट गये थे। ढेर सारी भविष्यवाणियों के हवाले से तरस खाने और ढेर सारी विगत परिस्थितियों के हवाले से अफ़सोस करने का यह चलन बड़ों की बैठकों में इतना हावी था कि हमारी किषोर पीढ़ी को जब परिपक्व बातचीत का शौक चर्राता तो हम इमरजेंसी की खूबियों-ख़ामियों पर चर्चा करने के साथ-साथ ‘कंकड़बाग़ में ज़मीन की ख़रीद-फ़रोख़्त, उर्फ़ क्या से क्या हो गया’ को भी अपनी चर्चा का विशय बनाते थे। वैसे सच पूछा जाए तो हम कभी इस बात से इत्तिफ़ाक़ नहीं रख पाए कि किसी भले आदमी को कंकड़बाग़ में जा बसना चाहिए। हमें तब किसी ने यह नहीं बताया था कि कंकड़बाग़ न बस रहा होता तो हमारे इलाक़े को सिनेमाघर का उपहार भी नहीं मिलता। उसके बसने के साथ-साथ षहर का केंद्र हमारी ओर खिसकता आ रहा था और सिनेमाघर की योजना राजेंद्र नगर के इसी नये स्टेटस का नतीजा थी। अगर बाइपास, जिसका नाम अब पुराना बाइपास हो चुका है, के पार खेत-ही-खेत होते तो उससे पचास क़दम इधर सिनेमाघर बनाने का ख़याल किसी के दिमाग़ में भला क्यों आता! इस तरह हमें कंकड़बाग़ का अहसानमंद होना चाहिए था जो कि, अज्ञानतावश, हम नहीं थे।
चर्चा सिनेमाघर की ज़रूरत पर चल रही थी। तो उसका ऐसा था कि वह सिर्फ़ हम किशोरों को नहीं, हमारे वाल्दैन को भी थी। सिनेमा मनोरंजन का मुख्य, बल्कि अपनी तरह का एकमात्र साधन था और आस-पास हॉल न होने की स्थिति में रिक्शा-भाड़ा इत्यादि मिला कर मामला ख़ासा खर्चीला पड़ जाता था। नौटंकी या फगुआ-चैती जैसे सामूहिक गान से अपना मनोरंजन करना या किसी की दालान पर घंटों बैठकी मारना संभव नहीं था, क्योंकि आखि़र शहरीपन भी कोई चीज़ होती है! यह सही है कि बग़ल के ही इलाक़े लोहानीपुर में यह शहरीपन नदारद था, पर हमारे थ्री-स्टार मुहल्ले में इस चीज़ की ख़ासी पूछ थी। मानसिकता के स्तर पर पूछ न भी होती तो वस्तुगत परिस्थितियों में वह शहरीपन विद्यमान था। सिंधियों, पंजाबियों, मारवाडि़यों और बंगालियों के कई परिवार हमारे मुहल्ले में रहते थे। आज हिसाब करने बैठता हूं तो थोड़ी हैरत होती है कि यह प्रेमपिपासु उस उम्र में जब-जब दिल के हाथों लाचार हुआ, उसकी वजह कोई-न-कोई पंजाबन या बंगालन थी। बिहारी परिवारों में भी कोई भोजपुरीभाषी इलाक़े से आता था, कोई मिथिलांचल से। इस सब तरह के बाशिंदों के बीच कोई कौटुम्बिक या पीढ़ीगत रिश्ता होने का सवाल ही नहीं था। इनके बीच पुश्तों के साझा अनुभव नहीं थे, एक-जैसा पेशा नहीं था, एक-जैसी नियति नहीं थी। ऐसे में शहरीपन उनका शौक नहीं, उनकी मजबूरी भी थी और मनबहलाव के गंवई साधन पूरी तरह उनकी पकड़ से छूट चुके थे। बस ले-देकर एक सिनेमा का आसरा रह गया था। इसके अलावा रेडियो नाम की भी एक चीज़ हुआ करती थी, जिसके शाॅर्ट-वेव पर कोई मनचाहा स्टेशन पकड़वाने में तनी हुई रस्सी पर चलने का-सा अनुभव होता था। इसे सिनेमा के विकल्प की तरह इस्तेमाल करना वैसा ही था जैसे विलायती शराब की कमी को देसी ठर्रे के बजाय चाय से पूरा करना। जहां तक टी.वी. सवाल है, ये उसके तुतलाने के दिन थे। उसका सर्वभक्षी विस्तार अभी बहुत दूर की चीज़ थी।
सिनेमा हाॅल बनने की शुरुआत के आस-पास ही टी.वी. का प्रवेश हमारे इलाक़े में हुआ था। राजेंद्र नगर रोड नं. 1 और 2 के जो मकान तिकोनिया पार्क की परिधि में और उसके आस-पास थे, उनमें से दो या तीन में ही टी.वी. सेट हुआ करता था। जिन-जिन घरों में यह बला थी, उनमें रविवार की शाम का तो आलम न पूछिए। बैठक में रखे सोफ़ों-कुर्सियों को दीवार से लगा दिया जाता और बीच की जगह में जाजिम-चादर इत्यादि बिछा कर बीसियों लोगों के बैठने की व्यवस्था की जाती। अक्सर यह व्यवस्था नाकाफ़ी साबित होती थी। इसलिए पांच बजे से शुरू होने वाली फि़ल्म के लिए लोग साढ़े चार बजे से ही जगह लूटने लगते थे। अंततः फि़ल्म शुरू होने के समय तक बैठक में मुख्यधारा के समाज के अलावा हाशिये का भी एक समाज दिखाई पड़ने लगता था, जिसमें सही समय पर आने वाले आगंतुकों के साथ-साथ मेज़बान परिवार के सदस्य भी शामिल होते थे। यह हाशिये का समाज खिड़कियों पर चढ़ा, दीवारों के सहारे खड़ा, या दरवाज़े की चैखट में अड़ा नज़र आता था।
मेज़बान परिवार के सदस्यों को हाशिये की जगह मुख्यधारा में बैठ कर फि़ल्म देखने का मौक़ा तभी मिलता जब कोई कला-फि़ल्म दिखाई जा रही हो। पर, ज़ाहिर है, इस मौक़े का भी वे पूरा-पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। आध-पौन घंटे में टी.वी. बंद कर दिया जाता और दूरदर्शन वालों को गरियाने का कार्यक्रम अगले ढाई घंटे तक जारी रहता। कई बार तो ऐसी फि़ल्म की घोषणा होते ही लोग रविवार की शाम का कोई और कार्यक्रम तय कर लेते थे। मिसाल के लिए, जिस रविवार को मणि कौल की ‘दुविधा’ आने वाली थी, उस शाम हमारे सभी महत्वपूर्ण ठिकानों पर ताला लगा पाया गया, या फिर यह सूचना मिली कि आज टी.वी. नहीं चलेगा। हार कर, कला की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हम बालकों को एक घर की बरसाती में रहने वाले घोष बाबू के यहां पहुंचना पड़ा, जो ‘मिली’ फि़ल्म के बरसातीवासी अमिताभ बच्चन की तरह ही पूरी दुनिया से कटे-कटे रहते थे। घोष बाबू ने बिना कोई खुशी या नाराज़गी ज़ाहिर किए हम लोगों को बरसाती में बैठाया और शुरुआती विज्ञापनों के बीच ही यह समझाया कि ‘फिलिम समझने वाला है, इसलिए आप लोक को इदर शांति से बैठना है…’। हम लोगों ने यथासंभव शांति से बैठने की कोशिश भी की, लेकिन हम उत्तरोत्तर इस कोशिश में असफल होते गये। अब धुंधली-सी याद है कि पहली बार हम लोगों के मुंह से फिक्क-सी हंसी तब निकली जब बैलों के गले की घंटियों और पहिये की चर्रक-चूं के साथ बहुत देर तक चलती रहने वाली बैलगाड़ी एक विशाल पेड़ के नीचे रुकी और नायक ने पर्दा हटाते हुए नायिका से पूछा–संभवतः उस फि़ल्म का पहला संवाद–‘केले खाओगी?’ इस हंसी से आगे बढ़ते-बढ़ते हम इस हद तक गये कि नायक को देवानंद का नौकर और नायिका को हेमा मालिनी की आया घोषित करते हुए कहकहे लगाने लगे। ठीक इसी समय घोष बाबू ने उठ कर टी.वी. बंद कर दिया और हम उनके कूचे से बेआबरू होकर निकले। बाहर हम लोगों के बीच यह मुद्दा बहसतलब बना कि घोष बाबू ने ऐसा हमारी हरकतों से ऊब कर किया था या फि़ल्म से ऊब कर?
उक्त प्रकरण से स्पष्ट है कि रविवार की फि़ल्म देखने के मामले में हम बालकों और किशोरों का हुजूम रिश्ते की नज़दीकी-दूरी और परिचय-अपरिचय की परवाह नहीं करता था। हम उंगली थाम कर पहुंचा पकड़ने वाले लोग थे। जहां थोड़ी-सी गुंजाइश दिखी, हम वहां पूरा क़ब्ज़ा जमा लेते। पर लड़कियों और माता-पिताओं की स्थिति ऐसी नहीं थी। माता-पिता तो हमारी तरह किसी भी घर में घुस जाने का गंवारपन दिखा नहीं सकते थे और जहां तक लड़कियों का सवाल है, उन्हें माता-पिता की निगाहों के सामने ही रहना था, इसलिए जहां वो नहीं, वहां ये नहीं। यों शहरीपन और गंवारपन की समझ हममें भी थी, लेकिन इस समझ की बिना पर मुफ़्त की फि़ल्म देखने का लोभ संवरण करना हमें ज़्यादती लगती थी। इस प्रकार लज्जा और लोभ में से बुजुर्ग लोभ का गला घोंटते थे, हम लज्जा का। और लड़कियां? मेरा अंदाज़ा है कि हर रविवार की शाम उनमें से ज़्यादातर, खुद अपना गला घोंटने की नाकाम कोशिश करती थीं।
तो यह था वह पूरा सांस्कृतिक परिदृश्य जिसके बीच रख कर आपको वैशाली सिनेमा हॉल के महत्व और उसके साथ जुड़ी हमारी उत्तेजना को समझना होगा। जी हां, यही नाम था उसका, जो हमने तब जाना जब पहली बार उसके प्रस्तावित निर्माण-स्थल पर गये। केस, हक़ीक़त या अफ़साने में, तब चल ही रहा था। इसलिए हॉल बनने की शुरुआत नहीं हुई थी। चारदीवारी से घिरे उसके परिसर में एक तरफ़ बड़े-से बोर्ड पर वास्तुकार की कल्पना में दिखने वाली वैशाली अंकित थी। इस तस्वीर में सब कुछ निहायत भव्य और सुंदर था, पर सबसे सुंदर थी उस नाम की लिखावट जो भवन के दाहिने हिस्से में उसके शिखर पर मुकुट की तरह सजा हुआ था। तस्वीर को देख हम सभी गौरवान्वित हुए, क्योंकि यह वह चीज़ थी जो ठीक हमारे मुहल्ले के मुहाने पर बनने जा रही थी। फिर तो जब-जब हम सामूहिक स्तर पर आत्मगौरव की थोड़ी भी कमी महसूस करते, उस साइट पर जाकर तस्वीर को देख आते थे। स्टे-आर्डर हटने के बाद जब काम की शुरुआत हुई, तब उस धूल-धक्कड़ में भी हमारा जाना-आना लगा रहा। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि हमारी अनवरत देख-रेख में वैशाली का निर्माण-कार्य संपन्न हुआ।
वैशाली के बनने के साथ-साथ उसके आस-पास कई चीज़ें बन रही थीं। बात ये थी कि रेलवे क्रासिंग की ओर जाती सड़क का वह हिस्सा थोड़ा वीरान-सा था, पर हॉल बनने की शुरुआत होते ही दूकानों और ढाबों की तादाद भी बढ़ने लगी। इस तरह काम पूरा होते-होते उस जगह की शक्ल काफ़ी बदल चुकी थी। बाद के दौर में सब्जि़यों की ख़रीदारी में बचाये गये पैसे से चाट, समोसा, मसाला डोसा इत्यादि खाना होता तो हम उत्तर में नाला रोड तक जाने के बजाय दक्षिण में वैशाली तक जाना पसंद करते थे। आखि़र नाला रोड हमारे होश संभालने से पहले का जमा-जमाया बाज़ार-क्षेत्र था, जबकि वैशाली और उसके आजू-बाजू का पूरा विकास हमारी देख-रेख में हुआ था!
खै़र! वैशाली बन कर खड़ी हो गई, तब उसके मुहूर्त का दिन तय हुआ और हम लोग उत्सुकतापूर्वक इंतज़ार करने लगे कि देखें, कौन-सी फि़ल्म लगती है! हमारी उत्सुकता की तान निराषा पर टूटी जब उसका उद्घाटन महान सामाजिक फि़ल्म ‘आनंद आश्रम’ से हुआ। फिर हमारे ही बीच के किसी परिपक्व दिमाग़ ने सुझाया कि जब शुरू के कुछ दिन वैसे ही हाउसफुल जाने हैं तो हॉल-मालिक क्या बेवकूफ़ है कि ‘आनंद आश्रम’ की जगह ‘डाॅन’ के चक्कर में पड़े (नया हॉल बनने पर लोग फि़ल्म नहीं, हाॅल देखने जाया करते थे)! इस सूझ से हमारी निराशा दूर हुई।… किंतु निराशा पर यह विजय बहुत टिकाऊ नहीं थी। हमने पाया कि एक के बाद एक महान सामाजिक या महा-फ़्लाॅप फि़ल्में हमारी इस महान उपलब्धि पर हावी हैं। भूले-भटके कभी कोई चर्चित फि़ल्म लग जाती थी। वह भी ज़्यादातर गांधी मैदान के पास के किसी हाॅल का शुरुआती हंगामा बांटने के लिए। ऐसी फि़ल्म आम तौर पर दो हफ़्ते के लिए लगाई जाती और हाउसफुल रहते हुए ही उतर भी जाती थी। बहुत कम हिट फि़ल्में ऐसी रह होंगी जो अकेले वैशाली के हिस्से आयी हों। इसमें हमें कोई संदेह नहीं था कि वैशाली पटना का सबसे उम्दा सिनेमा हाॅल है। पहली बार 70 एम.एम. स्क्रीन, पहली बार स्टीरियो साउंड सिस्टम, सबसे बड़ा और खुला हुआ परिसर। एलिफि़न्सटन की लाॅबी में जहां ब्लीचिंग पाउडर की गंध थी, वहीं वैषाली की लाॅबी में मशीन से भुने जाते पाॅपकाॅर्न और बढि़या इत्र की मिली-जुली खुशबू बसी थी। इन सबके बावजूद ‘जानी दुष्मन’, ‘कुर्बानी’, ‘हिम्मतवाला’, ‘मुकद्दर का सिकंदर’-जैसी फि़ल्में उसकी कि़स्मत में कम ही आती थीं और वह भी ज़्यादातर एलिफि़न्सटन, वीणा, अशोक या अप्सरा की थाली से फेंके गये टुकड़े की तरह। वजह शायद यह रही हो कि व्यावसायिक केंद्रों के आस-पास सिनेमाघरों के जो दो गुच्छे थे, उनसे छिटक कर वह एक रिहायशी इलाक़े में अलग-थलग पड़ी थी। किसी सुपरहिट फि़ल्म को उसके भरोसे छोड़ देने में वितरक पचास बार सोचते होंगे। मैं यह अंदाज़ा ही लगा सकता हूं, क्योंकि वितरण-व्यवसाय की प्राथमिकताओं और काम के तरीक़ों के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है।
मुझे यह भी पता नहीं कि कब वैशाली की स्तरहीनता को ही नियति मान कर हम आशा-निराशा से ऊपर उठ गये। साल-छह महीने में कोई ‘ए’ ग्रेड फि़ल्म लग जाती तो हम खुश होते थे। नहीं लगने की सूरत में दुखी नहीं होते थे। बाद को जब हमने हाफ़ टाइम से बिना टिकट फि़ल्म देखने का सिलसिला शुरू किया, तब यह बात अच्छी तरह दिमाग़ में बैठ गयी कि वैशाली जैसी भी है, हमारे बुरे दिनों की साथी है।
हाफ़ टाइम से फि़ल्म देखने का आइडिया हमारे बीच के ही किसी खुराफ़ाती दिमाग़ ने निकाला था। आइडिया यों था कि इंटरवल से ठीक पहले अगर हाॅल की चारदीवारी के भीतर चले आओ तो इंटरवल में बाहर निकली हुई भीड़ के साथ अंदर जाकर बैठा जा सकता है और बाद की आधी फि़ल्म देखी जा सकती है। ‘जानी दुष्मन’ का हाउसफुल दौर बीतने के बाद आइडिया पर अमल किया गया। क़ामयाबी मिली। उत्साहित होकर ‘जानी दुष्मन’ के उत्तरार्द्ध को हमने सात-आठ दफ़ा देखा। इसके बाद तो सिलसिला ही चल पड़ा। इस कार्रवाई में सिर्फ़ दो-तीन चीज़ों का ख़याल रखना पड़ता था। एक तो यह कि मैटिनी शो के दौरान चार से सवा चार बजे के बीच हाॅल की चारदीवारी के भीतर चले जाएं, क्योंकि इंटरवल से ठीक पहले मेन गेट बंद कर दिये जाते थे। दूसरा यह कि बालकनी में बैठें, क्योंकि उसके वर्गीय आधार के चलते वहां चेकिंग कम होती थी। तीसरे, एक बार में चार से ज़्यादा लोग न जाएं। ये सावधानियां बरतते हुए हम साल भर से ज़्यादा समय तक यह सिलसिला चला ले गये। उसके बाद, जैसा कि एक मूर्धन्य गीतकार कह गये हैं, छोटी-सी इक भूल ने सारा गुलशन जला दिया। हुआ यों कि एक दिन हम तीन लोग बालकनी के सुख से ऊब कर फर्स्ट क्लास में बैठ गये और वह भी ऐसी क़तार में जहां हमारे अलावा और कोई नहीं था। राजेंद्र कुमार की कोई फि़ल्म थी जिसका नाम सदमे के कारण भूल गया हूं। जनाब अभी यात्रा से लौट कर नायिका को तस्वीरों से भरी अलबम दिखा ही रहे थे कि हमारे चेहरों पर टाॅर्च की चुंधियाती रोशनी पड़ी। रोशनी ने टिकट की मांग की और हमने रोशनी से ही मुख़ातिब होकर कहा कि नहीं है। ‘तीनों को बुक करो,’ रोशनी ने गरज कर कहा। फिर दो लोग हमें अर्द्धचंद्र देकर बाहर की ओर चले। क़तारों के बीच धकियाये जाते हुए मैंने विधाता को धन्यवाद दिया जिसने हाॅल के भीतर अंधेरे का प्रावधान रखा है। साथ ही यह प्रार्थना भी की कि यह जो पारिभाषिक शब्दावली है, बुक करना, उसका कोई भयावह अर्थ न हो।
बाहर आये। पहलवान जी, अर्थात् मुख्य दरबान के सामने पेशी हुई। पहलवान ने क़द-काठी में सबसे बड़ा देख कर मुझी से पूछना शुरू किया।
‘अंदर कैसे आया?’
‘इंटरवल में।’
‘कहां रहता है?’
‘राजेंद्र नगर, 1 नंबर।’
‘कहां पढ़ता है?’
‘पाटलीपुत्रा।’
‘किस क्लास में?’
‘नौवां नवीन।’
‘सेक्शन?’
‘ए।’
‘रौल नंबर?’
‘एक।’
पहलवान हैरत से मुझे ऊपर-नीचे देखने लगा। आधे मिनट का विस्मित मौन। पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय में सेक्शन ‘ए’ का रोल नंबर 1 होने का मतलब था, पूरी क्लास में अव्वल आने वाला विद्यार्थी, और हमारे विद्यालय की साख ऐसी थी कि जो विद्यार्थी पूरी क्लास में अव्वल आता हो, उसे पहले से ही बिहार माध्यमिक बोर्ड के इम्तहान में अव्वल दस की सूची में आने का हक़दार मान लिया जाता था। लिहाज़ा, इस सूचना के बाद पहलवान का स्वर थोड़ा बदल गया। जैसे किसी देवता को पतित होता देख रहा हो, इस अंदाज़ में उसने पूछा, ‘पाटलीपुत्रा में फस्ट आता है, बोर्ड इम्तहान में मेरिट लिस्ट में रहेगा, और ई धंधा? क्लास-टीचर शमीम साहब हैं ना?’
‘जी।’
‘बतला दें उनको?’
‘…’
‘जाओ, भागो। आगे से आया है त बड़ी मार मारेंगे। बड़ा आदमी बनना है कि हाॅल का दरबानी करना है!’
हम बुक न किये जाने का–उसका जो भी मतलब हो–शुक्र मनाते बाहर आए। फिर बेटिकट क्या, बाटिकट भी हाॅल में घुसने का साहस कम-से-कम मुझे अगले एक-डेढ़ साल तक नहीं हुआ।
शायद इसी बीच हमारे बिहार माध्यमिक बोर्ड के इम्तहान भी हुए जिसमें सर गणेशदत्त पाटलिपुत्र हाई स्कूल की कक्षा दसवीं नवीन के सेक्शन ‘ए’ का रोल नंबर 1 अव्वल दस की सूची में अनुपस्थित पाया गया। इतना ही होता तब भी कोई बात न थी। उसी स्कूल के दो ‘गुमनाम’ विद्यार्थी उस सूची में मौजूद थे। तेज़ झटका लगा। नतीजा, मैं साहित्यकार बन बैठा। यह अपने लुप्त आत्मसम्मान को फिर से हासिल करने की बेचैन कोशिश की। ‘हमन दुनिया से यारी क्या’ वाली मुद्रा के चलते पुराने संगी-साथियों से मेल-जोल कम हुआ। परिचय के नये वृत्त बने। सिनेमाघरों के शो-केस में लगे ‘स्टिल्स’ देखने का शौक छूटा और उसकी जगह राजकमल प्रकाशन और पी.पी.एच. में खड़े होकर किताबें देखने का शौक तारी हुआ। वैशाली पास रह कर भी दूर होती गयी। अब उसके पास से गुज़रे कभी-कभी महीनों बीत जाते। कुल मिला कर, सन् 82 की माध्यमिक बोर्ड परीक्षाओं के बाद के इन वर्षों में वह मेरे सरोकार या उत्सुकता की चीज़ नहीं रह गयी थी। ऐसा नहीं कि मैंने उन दिनों फि़ल्में नहीं देखीं–‘हिम्मतवाला’ और ‘मुकद्दर का सिकंदर’ उन्हीं दिनों देखी गयी थी। ऐसा नहीं कि मैं कभी यों ही भटकता वैशाली के परिसर में नहीं गया–‘पुकार’ की होर्डिंग बनाते एक मज़दूर की कलाकारी किंवा कलाकार की मज़दूरी को नज़दीक से तभी देखा था। इन सबके बावजूद उन तीन-चार सालों की मेरी याददाश्त में वैशाली की मौजूदगी बहुत झीनी है।
हो सकता है, यह समझ बहुत सब्जेक्टिव हो, पर मुझे बहुत शिद्दत से महसूस होता है कि इस समय तक आते-आते मेरे लंगोटिया यार और मोहल्ले के लोग भी वैशाली से लगभग वीतराग हो गये थे। उनकी सांध्य-सभा में जब कभी मैं शामिल होता, वह कहीं भी एजेंडे पर नहीं होती। टेलीविज़न तिकोनिया पार्क को घेरने वाले सभी घरों में आ चुका था। हिंदी के बेमिसाल कि़स्सागो मनोहर श्याम जोशी के गढ़े हुए पात्र इन घरों के सदस्य बन चुके थे। प्रसारण की तकनीकी गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हो गया था और अब चलती-बोलती तस्वीरों की रबड़ के टुकड़े की मानिंद खींच-तान नहीं होती थी। तवे-जैसे रिकाॅर्ड की जगह कैसेट्स और उसमें भी टी-सिरीज़ के आने से मनचाहे गाने जब चाहे सुनने का अधिकार निम्नमध्यवर्गीय जनों को भी मिल गया था। रेडियो सीलोन से सिबाका गीतमाला सुनने के लिए तनी हुई रस्सी पर चलने की अब ज़रूरत नहीं रह गयी थी।
इन्हीं वर्शों में वैषाली के ठीक सामने वह फ़्लाईओवर बन कर तैयार हुआ था, जो रेलवे गुमटी के ऊपर से निकलता हुआ राजेंद्र नगर और कंकड़बाग़ को जोड़ता है। इसका निर्माण रुकवाने के लिए हाॅल वालों ने काफ़ी कोशिश की, क्योंकि इससे वैशाली के ठीक सामने की जगह तंग हो रही थी और भव्यता आहत। इसका निर्माण रुकवाने के लिए शायद रिज़र्व बैंक क्वार्टर्स वालों और आस-पास के दूसरे निवासियों ने भी कोशिश की, क्योंकि फ़्लाईओवर के साथ उन्होंने चोरी-झपटमारी का कोई नज़दीकी रक्त-संबंध ढूढ़ निकाला था।… पर विरोध के बावजूद जैसे वैशाली का बनना नहीं रुका था, वेसे ही फ़्लाईओवर का बनना नहीं रुका। ठीक-ठीक किस साल उसका काम पूरा हुआ, मुझे याद नहीं। पर इतना अवश्य याद है कि काम के दौरान वैशाली तक जाने वाले रास्ते की जो टूट-फूट हुई, उसकी लंबे समय तक क़ायदे से मरम्मत नहीं हो पायी और न ही मलबों को ठिकाने लगाया गया। शायद इसलिए कि मुख्य ट्रैफि़क के लिए अब यह रास्ता दरकार नहीं रह गया था।
कंकड़बाग़ तक जाने के लिए इस फ़्लाईओवर से गुज़रते हुए मैं वैशाली को ऊपर से देखता तो वह उतनी विराट और उत्तुंग नहीं लगती थी।
वह नवें दशक के मध्य से थोड़ा आगे या पीछे का कोई दिन रहा होगा जब फ़्लाई ओवर से गुज़रते हुए मैं उसे देख कर ठिठक गया। वहां एक अस्वाभाविक वीरानी थी। पार्किंग में कोई गाड़ी-स्कूटर नहीं, पीछे साइकिल-स्टैंड भी ख़ाली। टिकट-काउंटर के सामने क्यू के लिए लगाये गये लोहे के घेरे सूने पड़े थे। सामने की सीढि़यों पर इक्का-दुक्का लोग थे, जिन्हें देख कर लगा नहीं कि फि़ल्म देखने आए होंगे। सीढि़यों के ऊपर शीशे के दरवाज़े का एक पल्ला खोल कर पहलवान जी ने अपनी कुर्सी लगा रखी थी। दाहिनी ओर चारदीवारी के साथ किसी फि़ल्म की होर्डिंग लगी थी जिसकी फीकी रंगत बता रही थी कि फि़ल्म की कि़स्मत जैसी भी रही हो, होर्डिंग ने सिल्वर जुबली पूरी कर ली है। मुझे लगा कि हॉल बंद पड़ा है। लौट कर साथियों से पूछताछ की तो पता चला कि उसे बंद हुए दो महीने बीत चुके हैं। हाॅल के चार हिस्सेदार थे जिनमें कुछ अनबन चल रही थी। इस अनबन के बीच ‘कहानी फूलमती की’ और ‘नारद गाथा’-जैसी फि़ल्मों के सहारे वैशाली कई महीनों तक घिसटती रही। फिर जब अनबन अदालत तक पहुंच गयी, तब उसे बंद कर दिया गया।
लगता है कि ‘हमन दुनिया से यारी क्या’ वाले इस स्वयंभू साहित्यकार को ही नहीं, इसके स्थानीय भाई-बंदों को भी वैशाली के बंद होने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। पड़ा होता तो उसे लेकर चर्चाएं अवश्य होतीं और मैं दो महीने तक इस घटना से नावाकि़फ़ न रहता।
सन् 89 में मैं दिल्ली आ गया। हर गर्मी और जाड़े की छुट्टियों में पटना जाना होता। पता नहीं क्यों, अब वैशाली के ताज़ा हाल में मेरी दिलचस्पी बढ़ गयी थी। यह दिलचस्पी शायद वैसी ही थी, और है, जैसी किशोरावस्था में अपने बचपन की ज़ंग लगी तिपहिया साइकिल और विकलांग गुड्डे-गुडि़यों को लेकर होती है। हर बार मैं यह सुनने के लिए कान खड़े रखता कि वैशाली का क्या मामला चल रहा है। एक बार सुना, लालू प्रसाद यादव ने उसे ख़रीद लिया है (क्या इसलिए कि उसके बनने का समाचार सुनते ही हमने जे.पी. जिंदाबाद का नारा लगाया था!) और वह दुबारा चालू होने वाली है। दूसरी बार सुना, वह बात अफ़वाह थी। ख़रीदा किसी और ने है। चालू होने ही वाली थी कि नगरपालिका ने उसकी इमारत को ख़तरनाक पाया। बिना पर्याप्त मरम्मत के उसे जनता के लिए खोला नहीं जा सकता और हालत ये है कि नये मालिक ने अपनी पाई-पाई उसे ख़रीदने में ही झोंक दी है; अब वह मरम्मत नहीं करा सकता। तीसरी बार सुना कि उसे मालगोदाम में तब्दील करने की योजना है। यह मेरी अब तक की आखि़री जानकारी थी। जानकारी मिलते ही याद आया कि गांधी मैदान के सामने का एक सिनेमा हाॅल ‘रीजेंट’ बहुत पहले कभी मालगोदाम हुआ करता था। इसे क्या कहें! नियति का मज़ाक… जिसका फ़लसफ़ा बहुत पहले वैशाली में ही ग्रैंड रिवाइवल पर देखी गयी फि़ल्म ‘वक़्त’ ने समझाया था?
सन् 95 में अपनी ताज़ा-ताज़ा शादी के बाद मैं पटना गया था। पत्नी को लेकर फ़्लाईओवर की तरफ़ घूमने निकल गया। शाम का धुंधलका था जब ऊपर चढ़ते हुए उस पर मेरी नज़र पड़ी। उसके परिसर में धुंधलका थोड़ा और गहरा था, क्योंकि अंदर कहीं बिजली-बत्ती नहीं थी और बाहर की स्ट्रीट लाइट उतने विषाल परिसर की चारदीवारी से चार-पांच क़दम आगे ही दम तोड़ देती थी। चारदीवारी से लगा हुआ बाहर का हिस्सा भी, जहां कभी ठेलों, खोमचों, पान-सिगरेट की दूकानों और ढाबों का तांता हुआ करता था, बिल्कुल वीरान था। इस वीरानी और नीम अंधेरे में अपने सिर पर नाम का मुकुट सजाये वह ऐसी दिख रही थी, मानो दरबार का पूरा तामझाम समेट लिए जाने के बावजूद कोई बादषाह जड़ाऊ हीरों से ख़ाली कर दिये गये अपने तख़्त पर बैठा हो। मैंने पत्नी को वह दृश्य दिखाया। हम दोनों काफ़ी देर तक फ़्लाईओवर की रेलिंग पर टिके उसे देखते रहे और मुझे रेणु के वे पात्र याद आये जो गौने के बाद घर आती अपनी पत्नियों को निलहे साहबों की कोठी दिखाया करते थे।
ज़रा यहां गाड़ी धीरे-धीरे हांकना! कनिया साहेब की कोठी देखेंगी।… यही है मकै साहब की कोठी।… वहां है नील महने का हौज!
नयी दुलहिन ओहार के पर्दे को हटा कर घूंघट को ज़रा पीछे खिसका कर झांकती है–झरबेर के घने जंगलों के बीच ईंट-पत्थर का ढेर! कोठी कहां है?
दूल्हे का चेहरा गर्व से भर जाता है–अर्थात् हमारे गांव के पास साहेब की कोठी थी, यहां साहेब-मेम रहते थे।
उत्तरकांड
तारीख़ः 14 दिसंबर 2011। पटना गये हुए कथाकार मित्र विपिन कुमार शर्मा का एस.एम.एस. मिला है–‘वैशाली को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया है और वहां मॉल बनाया जा रहा है। वैशाली की एक ईंट भी अब उस जगह पर मौजूद नहीं है।’
‘वैशाली’ आॅल-कैप्स में है। शुक्रिया, विपिन भाई! वैशाली को बड़े हर्फों की इज़्ज़त बख्शने के लिए!
सन् 2000 में जब यह संस्मरणनुमा चीज़ लिखी थी, तब इसका इल्म न था कि वैशाली के दुबारा शुरू होने की अफ़वाहों में भी कुछ दम है। पर दम था। शायद जिन दिनों मैं लिख रहा था, उन्हीं दिनों वैशाली की नुची-चिंथी सीटों में नारियल के रेशे भरे जा रहे थे, उन पर रेक्सीन के नये कवर चढ़ाये जा रहे थे, कीलें ठोंकी जा रही थीं, पेंचें कसी जा रही थीं, सीलन से बदरंग हो आई दीवारों का रंग-रोगन चल रहा था, छिद्रों से भरे हुए मटमैले ‘रजतपट’ की गरिमा बहाल करने की कोशिश जारी थी, टूटे हुए शीशों को बदला जा रहा था, दीमक मारने वाली दवाई जगह-जगह इंजेक्ट की जा रही थी। 2002 या 03 में वह दुबारा चालू हुई होगी। यही समय था जब विपिन भाई ने ‘बहुवचन’ में यह संस्मरण पढ़ा और मुदित भए। दोस्तों को भी पढ़वाया। सबने तय किया कि जिसे एक लेखक ने इतनी आत्मीयता से याद किया है, उस वैशाली में सामूहिक रूप से फि़ल्म देखने चलें। वे गये। कोई बहुत सडि़यल-सी फि़ल्म लगी थी, लेकिन भाई लोगों की दिलचस्पी तो हाॅल में थी, फि़ल्म में नहीं।
दुखद, कि वह और भी सडि़यल निकला।
इस लेखक ने मानो उन्हें कमलिनियों से भरी किसी सुंदर झील का पता बताया था, और वहां काई और बदबूदार पानी वाली बास मारती गड़हिया मिली। मरम्मत के निशानों और कीटनाशकों की दुर्गंध से भरी वैशाली की सीट पर बैठे हुए किसी व्यतीत भव्यता की कल्पना करना भी उनके लिए दुष्कर साबित हुआ। मुझसे परिचय सात-आठ साल बाद होना था, वर्ना फ़ोन करके ज़रूर कहते कि आप कलम के धनी हैं, इसीलिए पाठ के भीतर एक ऐसी वैशाली रच पाए जिसका बाहर उस रूप में कभी कोई वजूद ही नहीं था। इस प्रशंसात्मक आरोप और आरोपात्मक प्रशंसा पर मैं क्या कहता? शायद यही कि वैषाली सचमुच में क्या थी, यह तो आपको दस्तावेज़ों में मिलेगा, पर वह मेरे लिए क्या थी, यह मेरे अलावा और कौन बता सकता है।
उन्हीं विपिन भाई का एस.एम.एस. मिला है कि वैशाली की इमारत को गिरा कर अब वहां माॅल बनाया जा रहा है।
नहीं, मुझे दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं। राजेंद्र नगर और लोहानीपुर में दस-बारह-चौदह साल की उम्र के ढेरों बच्चे आज भी होंगे जिनकी देख-रेख में माॅल का निर्माण-कार्य चल रहा होगा। वे सामूहिक स्तर पर जब भी आत्मगौरव की कमी महसूस करते होंगे, उस साइट का एक चक्कर लगा आते होंगे और वहां लगे बड़े-से बोर्ड पर भावी माॅल की तस्वीर देख कर आह्लादित-गौरवान्वित होते होंगे। फिर उत्साह के भाव को रसदशा तक पहुंचाने की लोकप्रिय विधियां अपनाते होंगे और आपस में ज़ोर-ज़ोर से बातें करते होंगे–इहां उप्पर में सिनेमा हाॅल बनतउ, बेट्टा! अउ बर्गर-पिज्जा, जिंस-जैकेट सब चीज के दुकान! समझले?
उन्हें लगता होगा कि उनके मुहल्ले की भी कुछ वक्अत है।
पर यह सोच कर थोड़ी मायूसी होती है कि उन बच्चों में से ज़्यादातर को, अगर वे उसी आय-वर्ग से आते हों जिससे मैं आता था, उस मल्टीप्लेक्स में फि़ल्म देखने का मौक़ा शायद ही कभी मिल पाएगा। डेढ़-दो सौ रुपये का टिकट लेकर उस हाॅल में जाना, जहां अपना पानी तक भीतर ले जाने की इजाज़त नहीं होती और अंदर मजबूरन हर चीज़ चारगुनी क़ीमत पर ख़रीदनी पड़ती है, उनमें से कितनों के नसीब में होगा? चलन्तिका टीकाओं का पूरा अर्थशास्त्र बदल चुका है। ज़्यादा लोगों से कम-कम पैसे लेने की जगह कम लोगों से ज़्यादा-ज़्यादा पैसे लेने का यह दौर है। फि़ल्में अपनी कमाई उन्हीं से पूरी किये ले रही हैं जो गांठ के पूरे हैं। जो गांठ के अधूरे हैं, उन्हें सीडी-डीवीडी और छोटा पर्दा मुबारक़! उन्हें सिनेमा हाॅल के जादुई अंधेरे में आत्मविस्मृत होने और विराट् पर्दे पर उभरती दुनिया में समा जाने की इजाज़त नहीं है। उन्हें छोटे पर्दे पर दिखती फि़ल्म की प्रतिकृति (रेप्लिका) से ही संतोश करना होगा, उसे ही फि़ल्म मानना होगा और ऐसा मानने के लिए उस सम्मोहक विराटता में गिरफ़्तार होने के तजुर्बों को पूरी तरह से भुलाना होगा। कुछ इस तरह, कि कभी याद भी न आये कि भूल गये हैं (अज्ञेय की काव्यपंक्ति हैः ‘इतना-सा दर्द कि याद आये कि भूल गया हूं, भूल गया हूं…’)।
गरज़ कि सिने-दर्शक तेज़ी से दो हिस्सों में बंटते जा रहे हैं–एक, जो हाॅल में जाकर फि़ल्में देख सकते हैं और दूसरे, जो नहीं देख सकते। दर्षक-दुनिया के ये नये ‘हैव्स’ और ‘हैवनाट्स’ हैं।
राजेंद्र नगर और लोहानीपुर के बच्चे ज़रूर खुश होंगे, पर क्या माॅल वहां के अधिसंख्य बच्चों के लिए कभी भी वह हो पाएगा जो हमारे लिए वैशाली थी?
========================
दुर्लभ किताबों के PDF के लिए जानकी पुल को telegram पर सब्सक्राइब करें

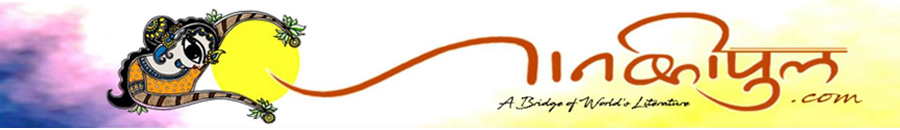
8 Comments
मै समझता हूँ कि दास्ताँ केवल वैशाली ''हाल 'की नहीं ,स्मृतिओं में ऐसा बहुत कुछ छुपा रहता है जो आपको भान कराये बिना उपस्थित हो जाता है ,
अपनी किशोरावस्था के दिन या आ गये। लगभग ऐसी ही परिस्थितियों में सिनेमा-टीवी देखना हुआ मेरा भी। पढ़ते हुए लगा कि अरे यह तो मेरा ही अनुभव है। संजीव भाई ने लाजवाब लिखा है, बहुत-बहुत बधाई।
मजा आ गया. लगा वैशाली किसी सिनेमा हॉल नहीं बल्कि किसी सत्तर के दशक की उस नायिका के यौवन की कथा सुना रहे हों जिसकी स्किप्ट डर्टी पिक्चर में जाकर चस्पा दी गई हो. मुझे अपने बिहार शरीफ का किसान सिनेमा याद हो आया. कभी हमने भी इसी तरह कचोट से याद किया था, अलबत्ता लिख नहीं पाए ऐसा..
लज़ीज़ और अज़ीज़ गद्य है. मैंने वैशाली सिनेमा के दूसरे सत्र में उसमें कुछ फ़िल्म देखे. चुंकि यह पटना में हमारी रिहाइश के समीप था और कदमताल करते हुए यहां तक की दूरी नापी जा सकती थी. हाल अच्छा था इसमें कोई शक नहीं लेकिन इसके बाहर का माहौल विपरित था. नव शहराती इसी वज़ह से नहीं जाते होंगे इसमें. वैसे मुझे यह बड़ी नाईंसाफ़ी लगती थी, जब भी मैं फ़्लाईओवर से गुजरते हुए बंद वैशाली को देखता. विद्यार्थियों के लिये यह हाल सबसे प्रासंगिक था. दुबारा शुरु हुआ तो लगा चलो अब तो कुछ सुविधा मिली सिनेमचियों को गांधी मैदान का वर्चस्व टूटा हालांकि तब तक मैं पटना छोड़ चुका था. अब की साल से मौल बनने की खबर सुन रहा हूं..गया तो देखुंगा जरूर कि कैसा बना है?
संजीव जी, आपका गद्य, विश्लेषण और कहन गजब का है। भरा-पूरा संसार और फिर उसी से दूरतलक निकलता एक नया संसार… बहुत खूब संजीव जी।
Pingback: buy psilocybin mushrooms united states
Pingback: vigrx plus
Pingback: https://www.kentreporter.com/reviews/phenq-reviews-urgent-side-effects-warning-honest-customer-truth/