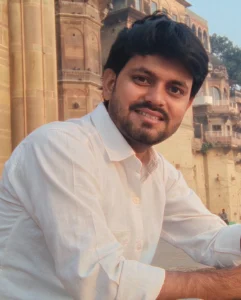आज पढ़िए मनीषा कुमारी की कविताएँ। मनीषा दौलत राम महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विशेष द्वितीय वर्ष की छात्रा हैं। यह देखना सुखद है कि इतनी कम उम्र में विचारों की इतनी गहनता, परिपक्वता उनके पास है – अनुरंजनी
===============================
1. मूर्ति
समाज में सरस्वती की मूर्तियाँ
गढ़ते हैं अनेकों कुम्हार,
स्त्रियाँ भी हाथ बँटाती हैं उनका
किंतु सोच एवं मेहनताने पर
जबरन अधिकार रहता है सिर्फ
पुरुषों का ही।
वे बनाते हैं
सुंदर एवं श्रृंगार में लिपटी हुई देह,
सजी-सँवरी दुर्गा की हाथों में तलवार
और तलवार के तले असुर,
जो उजागर करती है जातीय विभिन्नता से
उत्पन्न संकीर्णता को,
यह परिणाम है अधिकांश कुम्हारों के
अनपढ़ रखे जाने की,
अगर वे शिक्षित हो जायें
तब दुर्गा की तलवार के नीचे
गढ़ते नज़र आयेंगे प्रतिमायें
हिटलर, ज़ार और मुसोलिनी की।
ख़्याल में अक्सर आता हैं
कि इस पेशे पर स्त्रियाँ भी
रखें स्वयं का वर्चस्व,
और वे सरस्वती को साड़ी के फंदों से निकाल
पहना दें कोई आरामदायक लिबास,
जोड़ें बस दो ही हाथ
उसमें थमा दें कलम और किताब।
सजी हुई दुर्गा की जगह
वे स्थापित कर दें दुर्गावती को,
सरस्वती के बदले
गढ़ दें फुले को,
किसी मूरत की सूरत में
ढाल दें वे रोज़ा को,
मशाल पकड़कर हाथ ऊपर उठाये
क्लारा को,
क्रांति का झंडा फहराते हुए
कमला भसीन को
तब क्या दुनिया और सुंदर नहीं होगी?
2. बंद किया गया तुम्हें
बंधन! इसी शब्द की सीमितता के भीतर
बंद किया गया तुम्हें
हमेशा-हमेशा।
सभी ने पक्षी कहा
ताकि तुम इंसानों जैसी
हरकतें न करो,
इंसानों की धरती पर कब्जा न जमाओ
किंतु तुम पक्षी हो यह भी बस भ्रम है
क्योंकि, तुम्हारे ऊपर के आकाश को
बाँध दिया गया।
तुम्हें जिस पिंजरे का कैदी बनाया गया
उसमें पंख फड़फड़ाने तक की जमीं न थी
वहाँ निगरानी पर तैनात द्वारपालों ने
तुमसे तुम्हारी चहचहाहट की भी कुर्बानी ले लीं।
तुम कलाकार थी
किंतु तुम्हें अपनी कलाकारी को
रँगनी पड़ी काली रैना में,
मजदूरी को नाम देना पड़ा
किसी और का,
तुम्हें मिली केवल धार्मिक क़िताबें
दिन व्यतीत करने के लिए
किंतु जब तुम्हारे साथी ने
तुम्हें मिलाया गाँधी और मार्क्स से
तब लोगों ने तुम्हें और उन्हें घेरना चाहा था
व्यंग्यों और आलोचनाओं की दीवार से।
सामान्य-सी डिग्री पाने हेतु
तुम सभी की नजरों से बचती हुई
तमाम बहाने बनाकर
झूठ बोलते हुए
पहुँचती थी परीक्षा केंद्र तक।
अनेकों किताब पढ़ने के बावजूद भी
तुम किसी पर अपना नाम नहीं लिख सकी
शायद, इसीलिए कि तुम पढ़ना तो चाहती थी
किंतु इस सोच में कैद किया गया तुम्हें
कि किताब स्वयं पर उस हस्ताक्षर को ही
स्वीकृत करती है जो केवल पुरुष का हो,
पर देखना, तुम ख़ुद लिखोगी एक रोज़ किताब!
3. तुम्हारा वजूद ?
तुम जन्मी, बस जनम गयी!
बीना किसी वजूद के
अस्तित्व-विहीन समझी गई
जन्म से ही!
इंसानों की पंक्ति में
किसी ने शामिल नहीं किया तुम्हें,
तुम चिड़िया हो ऐसा सुना होगा तुमने
गीत-संगीत में और बात-चीत में,
किंतु ये अल्फाज़ उड़ गये होंगे
यूँ ही फिजाओं में,
मगर वहीं की वहीं रह गई तुम।
स्कूल में साथ थी मेरे
किंतु वहाँ पहुँचकर भी
विद्यार्थी नहीं बन सकी,
तुम बनी बस छात्रवृत्ति के पैसों को
घर तक पहुँचाने का साधन,
तुमने चाक पर गढ़े अनेकों खिलौने,
सड़क के उस मेले में बेचा भी उसे दिन-भर
किंतु शाम को तुमसे पूरी कमाई छीन ली गई,
दीपावली के दिन अच्छे पाकवान माँगते
तुम मिली थी गाँव के रईसों के चौखटें पर
किंतु गुलाबजामुन तुमने
एक पन्नी में बाँध लिया था
भाई को खिलाने के लिए ,
सोचो! तब तुम्हारा कोई वजूद भी था क्या?
आठवीं कक्षा में थी मैं तब तुम्हें देखा
दुर्गा जी की मूर्ति के पास,
अपने बच्चे को गोद में लिये
खड़ी थी पति के साथ,
तुम शायद फिर से माँ बनने वाली थी
ऐसा अनुमान किया था मैंने!
उसके एक बरस बाद ही
सुनने में आया कि तीसरे बच्चे को
पेट में लिये मर गई तुम,
तुम्हारी माँ बीमार रहती थी बहुत,
याद है मुझे वह भी उम्र से पहले ही
चल बसी थीं एकदम अचानक,
ईलाज भी नहीं कराया था उनका किसी ने,
अब मुझे एहसास होता है
उनकी अहमियत जानवर जितनी भी नहीं थी
उनको सिर्फ मशीन का ही रूप
दिया था हर किसी ने अपनी-अपनी चाक से
और बिल्कुल वही तुम्हें भी
और तुम्हारे बाद भी न जाने कितनों और को
गढ़ा जा रहा है उसी चाक पर
उनमें से कोई फूट गया तो फूट गया!
4.असमानता
अगर पृथ्वी पर इतनी असमानता न होती
तब यहाँ बोला, सुना, पढ़ा, लिखा और जिया जाता
केवल और केवल ‘प्रेम’ को!
असमानता से उपजे भयानक विध्वंसों की
प्रतियाँ उकेरने के क्रम में
स्याही की अनगिनत बूँदो को
आकार लेना पड़ता है उन शब्दों का
जिन्हें झाँकने मात्र से ही
आँखों के आगे नजर आने लगती है
धरती पर खत्म होती इंसानियत।
अथाह पृष्ठ की देह पर गिने जाते हैं
चीख, आँसू और अनेकों शरीर,
जो तब्दील हो गयी होती है
केवल और केवल लाश में ही
जिंदा या मुर्दा!
5. टुकड़े भर धूप
टुकड़े भर धूप की राह
देखती है देह जाड़े के दिनों में,
धूप के समानांतर ही ऊष्मा देती हैं लिहाफ भी
किंतु यह सभी की देह पर मौजूद नहीं,
बँधी मुठ्ठी में खालीपन की वज़ह से।
जाड़े के दिनों में धूप के टुकड़े के भीतर
हम कैद हो जाते हैं जैसे-तैसे, जब कभी
किंतु उन दिनों की रातें तो बीतती हैं
रूह को कँपकँपाती ही
लिहाफ़ के भीतर स्वयं को न पाकर,
जिसका सबसे बड़ा कारण पूँजी है ।
जब मैं महाविद्यालय में देखती हूँ
स्थाई कार्यों के लिए अस्थाई तौर पर
लोगों को मजबूर होकर मजदूरी करते हुए,
कक्षा में बड़ी मेहनत और ईमानदारी से
अतिथि शिक्षक को पढ़ाते हुए,
हम बच्चों के समक्ष ख़ूब सहजता एवं आत्मियता से
नयी जानकारियों को साझा करते हुए
तब विचारती हूँ कि कितना विकल्पहीन
बना दिया गया है हमें
कि सभी प्रकार से सक्षम होने पर भी
हम मजबूर हैं इस प्रकार से मजदूरी करने के लिए।
अतः हम कर रहे हैं ठेके की नौकरी
दिन-रात, चुपचाप
जिसकी वजह से दृश्य से कहीं दूर
चली जाती दिखाई पड़ रही हैं स्थाई नौकरियाँ
किंतु इस विकल्पहीन परिस्थिति में भी
हमारी साँसे तो जारी हैं,
इन्हीं साँसों को ढोने वाला
यह देह जिसकी जरूरतों को
पूर्ण करने हेतु काफी नहीं है
टुकड़े भर धूप का होना ,
इसके लिए आवश्यकता है पूँजी की
क्योंकि सदियों से ही वर्चस्व में है
धरती पर, केवल और केवल पूँजी ही।
6. फिट नहीं आओगी उस चौखटें में तुम
किसी शाम तुम जबरदस्ती निकली
घर से बाहर सब्जी खरीदने,
सब्जी खरीदना बहाने भर था
जो तुमने इसलिए बनाया
ताकि छुट्टियों के दिनों में
कुछ वक्त के लिए ही सही
खूब बोलना – हँसना संभव हो पाये
अपनी सहेलियों के संग।
बीतते समय के साथ तुमने सीखा
कॉलेज तक जाने हेतु
अकेले बस से सफर करना,
खुलकर आरंभ की तुम चलना
उस डगर के ऊपर जो पहुँचायेगा
समंदर के पार तक
तुम्हें ख़ूब विस्तृत करते हुए,
जिसका स्वप्न किसी दिन चुपके-से
देखा था तुमने अपने सजल नयनों में
और चौकन्नी होकर झुका ली थीं पलकें
ताकि कोई देख न ले उन्हें!
वक्त के अंतराल के उपरांत
अब, जब मैं झाँकती हूँ तुम्हारे अंत: में,
महसूस करती हूँ तुम्हें दौड़कर किसी
नये दौर के अंतर में प्रवेश करते
जिसके द्वार पर किसी निश्चित माप की
चौखट नहीं लगी है,
जिसके भीतर तुम मुक्त होकर जा सकोगी।
जहाँ से किसी शाम लौटनें का ख्याल करोगी
अगर घर कभी ,
तब तुम फिट नहीं आओगी उस चौखटें में ,
जिससे पार कराया गया था तुम्हें
तमाम सीमितताओं और बन्धनों में बाँधकर।
7. एक अंतराल तक नहीं आता
बरस बीतते हैं
किंतु एक अंतराल तक नहीं आता
दु:ख और तकलीफ के बीच ,
मजबूरी के बीच ,
मजबूर मजदूरों की स्थिति के बीच ।
पिछले बरस भी कोई मजदूर ,
जाड़े की देर शाम तक
अपने नन्हें बच्चे को ठेले पर बिठा
पैसे लेने-देने का काम सौंपे,
स्वयं सब्जी बेचने में व्यस्त दिखता था
इस बरस भी वह वैसे ही दिखा।
खुद नरम-मुलायम हाथ से
हैंडल खिंचते मिला वह मासूम
फिर उसी बाजार में,
जिसका छोटा भाई उसका हाथ बँटाता है
उसकी इस तकलीफ के बीच
एक अंतराल तक नहीं आया
इस बरस भी ।
वह इस बरस भी मजबूर ही है
शायद अगले बरस भी मजदूरी करने के लिए
वह मजबूर ही दिखेगा।
8. खिलखिलाओ तुम
खिलखिलाओ कि खिलखिलाना
तुम्हारी आदत में शामिल हो सके।
खिलखिलाओ कि दरवाज़े पर आसन जमाये
ससुर जी को तुम्हारे होने का एहसास हो सके।
खिलखिलाओ कि अब तुम घर की चौखट
पार कर सीमा को लाँघ रही हो।
खिलखिलाओ कि दिनभर बोझा ढोने के बाद
शाम को तुम अपने हिस्से के धान को
हासिल करने हेतु खुलकर लड़ना सीख रही हो।
खिलखिलाओ कि तुम नदी बनकर सागर में
विलीन होने की चाहत का नाश कर दी हो,
खिलखिलाओ कि तुम्हारे स्वप्न
अब समुंदर के उस पार जाने का है।
खिलखिलाओ कि सदियों के संघर्ष को
खूब मजबूती से जिंदा रखना है तुम्हें
शोषण के अंत तक।
खिलखिलाओ की अगला दौर तुम्हारा है
तो खिलखिलाकर दौड़ जाओ उस दौर तक।
खिलखिलाओ कि तुम्हारी खिलखिलाहट से
दरक रही है हर रोज़ रुढ़िवादी परंपरा की ईंट ।
खिलखिलाओं की तुमने तमाम वजहें
तराश ली हैं खिलखिलानें के लिए।
9. स्त्रियाँ लिख पाती हैं केवल संघर्ष की कहानियाँ
सहेजे या बिखरे हुए
अनगिनत पन्नों पर
उड़ती दिखाई पड़ती हैं
संघर्ष की अनंत कहानियाँ
जिसमें मौजूद हैं अधिकांश
मजदूर, किसान, दलित,
आदिवासी और स्त्रियाँ
किंतु पोर भर से भी कम दिखता है
लिखा हुआ कहीं किसी
पुरुष विशेष का संघर्ष!
संघर्ष के इतर सौंदर्य में भी
अक्सर मौजूदगी है स्त्रियों की ही,
पुरुष आये दिन खींच जाते हैं
अपनी कलम से चंद सुंदर शब्द
स्त्री सौंदर्य को केंद्र में रखकर,
किंतु, नगण्य लिखावट छापी जाती हैं
किसी स्त्री द्वारा पुरुष के सौंदर्य पर।
चूँकि स्त्रियों के पास स्वयं के ही दुख
इतने हैं कि वे सोच ही नहीं पाती
सौंदर्य के ऊपर लिखने हेतु ,
वे उकेरती हैं मजदूर, किसान , दलित
आदि की प्रताड़नाओं को
क्योंकि उनकी पीड़ा को
महसूस करती हैं वे हर रोज़
और जोड़ पाती हैं अपने आप से,
उन सभी की प्रताड़नाओं को
शब्दों में बाँधते वक्त
काँप जातीं होंगी उनकी कलम पकड़ी
वे उँगलियाँ भी
जो काँपती हैं पति या पिता द्वारा फेंकी गयी
खाने की थाल को धरती से उठाते वक्त
थरथराती हुई दोनों हथेलियों के साथ!
फिर वे कैसे छुपाकर रखें
इतनी हृदयविदारक वेदनाओं को
और कैसे गढ़ दें कोई काल्पनिक या
सुंदर तस्वीर जब उनकी स्वयं की
तस्वीर(अस्तित्व)को नष्ट
करने पर तुला हो यह समाज,
कमतर समझे उन्हें प्रत्येक क्षण
और कर दे उनकी
मजदूरी को कम
जो आजीवन उन्हें परतंत्र बनाये
रखने की सबसे अच्छी विधा है।
कई बार एक बात तैरते हुए
पहुँचती है कानों तक
कि अधिकांश स्त्रियाँ क्यों नहीं लिख पाती हैं
किसी पुरुष का संघर्ष?
मेरा मस्तिष्क इसका सहज उत्तर देता है
कि कोई भी स्री किसी पुरुष को,
कभी भी केवल उसके पुरुष होने हेतु
नहीं देखती प्रताड़ित होते एवं संघर्ष करते,
अपनी अस्मिता हेतु दुनिया से लड़ते
तब कोई स्त्री कहाँ से उपार्जित कर दे
उसके संघर्ष की कहानियाँ?
और कैसे खिंच दे कोरी कल्पना?
क्योंकि, लिखा वही जा सकता है
जो व्यतीत होता है आँखों के आगे
और हृदय में जो महसूस होता है।
तभी तो पुरुष भी नहीं लिख पाते अधिक
व्यक्तिगत या अपने वर्ग विशेष के लिए कुछ भी!
क्योंकि वह भी जानते हैं,
चाहे परिस्थिति कैसी भी हो
हमेशा से धरती पर स्त्रियाँ
हम से अधिक संघर्ष करती आयी हैं,
अपने अस्तित्व के लिए लड़ते आयी हैं ,
इसी का तो परिणाम है कि
पुरुष भी उकेर जाते हैं
सौंदर्य के साथ ही स्त्रियों के संघर्ष को भी
जैसे निराला ने कभी उकेरा था
तोड़ती पत्थर में
उस औरत के संघर्ष की एक प्रति को,
केदारनाथ अग्रवाल बयां करते पाये गये हैं
एक स्त्री के लोहे से गोली तक
बनने के खतरनाक सफ़र को,
फिर इन्हीं सहेजे और बिखरे हुए पन्नों के ऊपर
किसी प्रसंग का गवाह बनने के कारण ही
बड़ी स्पष्टता से खींच जाते हैं आलोक धन्वा भी
भागी हुई लड़कियों को।
10. किसी जाड़े का इंतजार नहीं करना पड़ता
किसी जाड़े का इंतजार नहीं करना पड़ता
स्त्रियों को कुछ भी ओढ़ने के लिए,
पनपते ही उन्हें ओढ़ाया जाता है
धरती पर दूसरी प्रजाति के होने का
एहसास कराने वाला शाल,
जब दे दिये जाते हैं हाथों में
कुछ खिलौने, वे खिलौने
जिसमें बंदूक या बैट-बॉल
शायद ही गिनती में आती है,
किंतु ,वहाँ अनगिनत गुड़िया
घर , किचेन-सेट जरुर मौजूद होता है।
वे जब चिड़िया की भाँति फुदकने लगती हैं
एक घर से दूसरे घर या गलियों में
और सोचती हैं कि ऐसे ही धीरे-धीरे पहुँच जाऊँगी
तमाम पगडंडियों को पार करते
कभी किसी दूसरे देश में,
तब उन पर घर की इज्जत होने का
लबादा लाद दिया जाता है
और इस लबादे के भीतर ठिठक कर
रह जाती हैं वे।
शादी होती है जब
तब आज भी गाँवों में
कौन ऐसी दुल्हन नहीं
जो आती है बड़े से घुंघट के
भीतर से झाँकते हुए
फिर चाहे वह पेशे से
किसी स्कूल की मास्टरनी ही क्यों न रहे?
उसे भी ढक दिया जाता है
परंपराओं के तले।
माँ बनने के उपरांत
वे मजबूर होती हैं
नटखटपन, लड़कपन या
अपने सख्त स्वभाव को पूर्णतः छोड़ने हेतु,
उन्हें जबरदस्ती ओढ़ना पड़ता है
अपनी हर पहचान के ऊपर
माँ नाम की लिखी गयी चादर को
क्योंकि उनके बच्चे को वे
कुर्सी पर बैठी अच्छी नहीं लगतीं
जैसे ‘बंटी’ को उसकी माँ(आपका बंटी)!
अंततः इन सभी आवरण के तले
ढक जाती हैं वे स्वयं ही,
लॉक कर लेती हैं अपने हृदय की
स्वतंत्र तरंगों को,
शायद वे धीरे-धीरे भूलने की
कोशिश करने लगती है अपने आप को,
फिर खोखली मुस्कुराहट के साथ
बड़े अच्छे से ओढ़कर निकलती हैं
इन सभी लबादों को वे हर रोज़
जिसके लिए उन्हें किसी जाड़े का
इंतजार नहीं करना पड़ता है ।