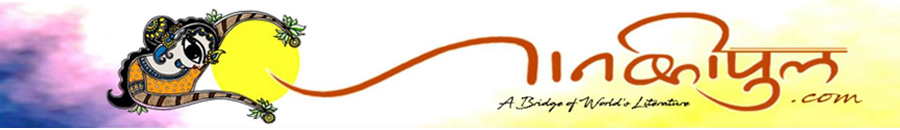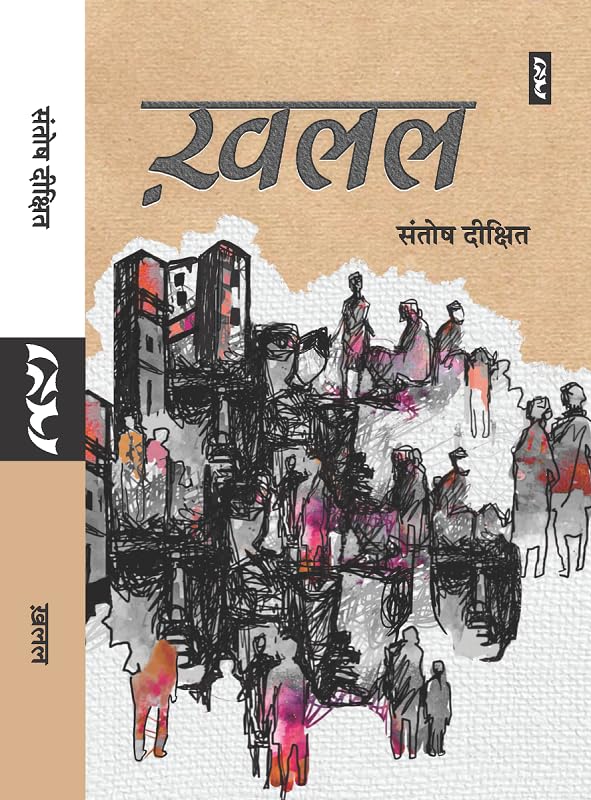वरिष्ठ लेखक संतोष दीक्षित का नया उपन्यास ‘ख़लल’ सेतु प्रकाशन से प्रकाशित हुआ है। समकालीन समय के सामाजिक-राजनीतिक बदलावों, सांप्रदायिकता को लेकर लिखे गये इस संवेदनशील उपन्यास पर बहुत अच्छी टिप्पणी लिखी है युवा कवि अंचित ने। आप भी पढ़ सकते हैं- मॉडरेटर
=======================================================
इधर के हालिया प्रकाशित उपन्यासों में संतोष दीक्षित की मुखरता और प्रतिबद्धता और खुली है और रेखांकित करने योग्य है। उनका ताज़ा प्रकाशित उपन्यास ‘ख़लल’ सबसे पहले तो इसलिए पढ़ा जाना चाहिए कि सरलताओं और सुविधाजनक चुप्पियों के समय में सीधी और खरी-खरी बात करना अब बहुत कम देखा जाने लगा है। अपने समय को तीक्ष्ण दृष्टि के साथ देखते हुए उसे बरतने के लिए और उस पर कथानक बुनने के लिए संतोष दीक्षित के पास एक उर्वर भूमि है और उसके साथ एक शानदार व्यंग्य से भरी कहन है जो उन विषयों से न सिर्फ़ पाठक का सीधा संबंध बनाती हैं, बल्कि कभी भी यथार्थ से दूर किसी कल्पना की तरफ़ जाने का समय नहीं देती। लिखत हमेशा पाठक को विचलित करती रहती है और कई बार तो गुस्से और निराशा से भरती भी है। क्या वर्तमान असमानताओं और हिंसाओं के समय में लेखक का उद्देश्य यही नहीं है?
भारतीय समाज की बुनावट इतनी गहन और उलझी हुई है कि उसका सीधा अन्वेषण और सरलीकरण संभव ही नहीं है। एक ही देश में इतनी सारी परतें हैं, इतनी गहमागहमी है और इतने सारे एक दूसरे को काटते-जोड़ते विमर्श हैं कि किसी प्रकार की केंद्रीयता या निष्कर्ष के लिए जगह नहीं बनती। भारतीय उपमहाद्वीप की खूबी भी यही सांस्कृतिक और भौगोलिक फैब्रिक है जहाँ एक साथ विभिन्न संसार रहते हैं, फलते-फूलते हैं और एक ऐसी काव्यात्मकता का निर्माण करते हैं जो हर किसी के पकड़े पकड़ नहीं आती। इक्कीसवीं सदी का भारत इस काव्यात्मकता में पूंजी की घुसपैठ से बना भारत है जिसने अस्मिताओं पर असर डाला है, जिसने जाति के शोषण को तोड़ा भी है और उसी तंत्र में नए कोण भी पैदा किए हैं, जिसने हिंदुस्तानी पब्लिक स्फीयर और हिंदुस्तानी विमर्श को कब्जाया भी है और क्षद्म ऐतिहासिकता से तोड़ने-बिगाड़ने की कोशिश भी की है। ऐसे में ‘ख़लल’ प्रतिरोध की हर परिभाषा पर खरा उतरता है और संतोष दीक्षित अपने चिर-परिचित अंदाज़ में उन बातों को दर्ज करते हैं जिनको मध्यवर्गीय सुविधा अनदेखा करना चाहती है। यह वह कैसे संभव करते हैं यह देखने वाली बात है।
दीक्षित जी के उपन्यासों ने खास तौर पर दो बिंदुओं पर सोचने को मजबूर किया है। एक तो यह कि उनकी रचना प्रक्रिया क्या है और एक यह कि समय का मनोविज्ञान इस तरह पकड़ने वाले उपन्यासकार का दिमाग़ किस तरह काम करता है। इन दोनों प्रश्नों के कम से कम आंशिक जवाब तो उनकी स्थानीयता में देखे जा सकते हैं। उनकी उपन्यासों की दुनिया से बहुत आसानी से जुड़ा जा सकता है। इसलिए नहीं कि लगभग हर उपन्यास एक ही ब्रह्मांड में घटित होता है, इसलिए भी कि कम से कम भारतीय उपमहाद्वीप में कहीं भी इस दुनिया को अपनी खिड़की खोलकर बाहर झांकते ही पाया जा सकता है – आर के नारायण की मालगुड़ी की तरह और मानवीय सुन्दरताओं से दूर नहीं पर कुरूपताओं को लेकर ज़्यादा सजग। यह वही दुनिया है जो हमारे कमरे के बाहर है और अपनी ईमानदारी और दोगले चरित्र के साथ, जहाँ प्रेम तो किवाड़ों के पीछे और अंधेरे में किया जाता है लेकिन गालियाँ, हत्याएँ, शोषण दिन के उजाले में बिना हिचके और इस नवउदारवादी समय की तार्किकता से पोषित, बिना ग्लानि और अफ़सोस के। फिर भी हिंसा के प्रकार होते हैं और जो हिंसा सामने से दिखती है, किसी किताब में उसका प्रक्षेपण आसान है और एक साधारण लेखक की पकड़ से भी बाहर नहीं है। लेकिन चूँकि यह “सो-कॉल्ड सोशलिज्म” पर लिखी गई कोई साधारण किताब नहीं है इसलिए यहाँ हिंसा का वह प्रकार दीक्षित जी के सामने खड़ा है जो न सिर्फ़ महीन है बल्कि मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी असर करता है और गहरी, पूर्णकालिक हानि और टूट की तरफ़ इशारा करता है। इसको समेटने में और कह सकने में क़ाबिलियत तो लगती ही है, उससे ज़्यादा बहादुरी। शिल्प के स्तर पर इसके लिए संतोष दीक्षित एक माइक्रोकॉस्म बनाते हैं जैसे अपने पुराने उपन्यासों में और उस कुशलता से कि यह व्हिटमैन की याद दिलाता है। सूचियों में संसार घटित होता है। अनगिन पात्र आते हैं, इस यथार्थ का एक चेहरा दिखाते हैं और देर तक ज़हन में बने रहते हैं। जाहिर है कि यह कर पाना आसान काम नहीं है। जो घट रहा है, अपनी ऐतिहासिकता के बिना नहीं घट रहा और कथानक में शायद सियाराम जी मुख्य पात्र लगते हों लेकिन सच्चे उत्तरआधुनिक अर्थों में इस समय का चिथड़ा जो अनगिनत कपड़ों को जोड़-जोड़ कर बना है, वह उपन्यास का मुख्य पात्र है।
संतोष दीक्षित ने भारतीय सरकारी दफ़्तरों, काम करने की जगहों, और इन पब्लिक स्पेसेज को काफ़ी नज़दीक से देखा है। इन जगहों का कामकाज ऐसा है कि भले ही यहाँ हम भारत के लोग ही काम करते हों, कोई इन जगहों में होना नहीं चाहता। इन जगहों में ऐसे बंटवारे हैं, ऐसे अलगाव हैं और ऐसे भ्रष्टाचार हैं जो गहरे जीवन को प्रभावित करते हैं और साथ ही हमारे समय का एक कटु और स्पष्ट दृश्य प्रस्तुत करते हैं। इसमें एक “अर्बननेस” भी निहित है जिस पर आगे। आज़ादी के बाद के भारत में और गांधी-नेहरू की विचारधारा में जिस बात का सबसे ज़्यादा उत्सव है वह यही है कि भारत विरुद्धों के सामंजस्य से बना है या अनेकता में एकता ही इस राष्ट्र को, इस ‘सभ्यता’ को मज़बूत बनाती है। यह समझना होगा कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद इस ‘राष्ट्र’ की फाल्ट लाइंस ऐसे उभर गईं हैं कि उसके समाधान के रूप में कोई ‘नैशनल एलिगरी’ हमारे सम्मुख नहीं है। यहाँ संतोष दीक्षित, सलमान रुश्दी की तरह, इस उत्तराधुनिक विमर्श में निहित एंटीथेसिस की पोलखोल में कहीं कहीं उस सिनिक की तरह भी दिखते हैं जो जानता है कि यह वह देश है जो आख्यानों के युद्ध में उलझा हुआ है और मध्यवर्गीय आकांक्षाओं से ऊपर कोई वृहत्तर चेतना नहीं जानता- यह समय की नब्ज है और कटुता से भरी है। यही मध्यवर्गीय आकांक्षा जिसके मूल में उम्मीद का वादा, सत्ता का वादा और संपत्ति के जमा होने का वादा है अब “अमेरिकन ड्रीम” की तर्ज पर “इंडियन ड्रीम” का निर्माण करती है और उसी के पीछे भागती रहती है। यह इस लिहाज से तो एक नया सोशल फैब्रिक तो है कि यह भारत के संदर्भ में इक्कीसवीं सदी में ही रचा-बसा है। उपन्यास ने इसे न सिर्फ़ खोला है, बल्कि एक ऐसे हास्य के साथ कि न सिर्फ़ वह ख़ुद पर हँसाये बल्कि वह असुविधा भी पैदा करे कि वह, हड्डी की तरह, देर तक गले में फँसा रहे।
उपन्यास में सारी मौजूँ बहसें हैं यह कहने की बात नहीं है। धर्मों, जातियों के बीच जिस तरह से स्टीरियोटाइपिंग होती है और प्रॉपेगैंडिस्ट विचारधारा का जो रेसिड्यू अब अधिक से अधिक उभरता जा रहा है और जिससे जीतने के कोई उपाय नहीं दिखते, उसका गहन अन्वेषण किताब प्रस्तुत करती है और शायद उसको किताब के ही एक वाक्यांश में सबसे अच्छे से कहा जा सकता है – एक श्रेष्ठताबोध के साथ हिटलरी जहालत के दौर”। किताब के इतने सारे किरदार इसी एक वाक्यांश की तरफ़ इशारा करते हैं और यह सब एक प्रतिबद्ध प्रगतिशील समग्रता के साथ उपन्यास में आता है और लेखक को प्रासंगिक बनाता है। अभी के समय में लिखने का प्रमुख प्रयोजन तो यही होना चाहिए और इसलिए बतौर उपन्यासकार संतोष दीक्षित को पढ़े जाने की ज़रूरत है, लगातार चिह्नित करने की ज़रूरत है। “अर्बननेस” पर लौटते हुए यह लगता है कि बिना किसी बाइनरी के यह कहा जा सकता है कि “ख़लल” एक भारतीय शहरी महाकाव्य है, कम से कम हमारा समय महाकाव्यों को रचने संबंधित जितनी छूटें देता हो। अपने सीमित पाठ में मुझे यह हमेशा लगता रहा है कि भारतीय गाँव को प्रेमचंद से लेकर शिवमूर्ति तक ने खूब लिखा है लेकिन भारतीय शहरों, विशेष कर उसके मध्यवर्गीय और निम्नमध्यवर्गीय जीवन के दृश्य हिन्दी में कम आए हैं और जब आए हैं तो एकपक्षीयता के साथ, समग्रता से दूर और भावकेंद्रित, अलग अलग स्थायी भावों से बने और उनसे बिना डिगे – संतोष जी ने इसे बदलने का खतरा उठाया है और पहले भी उठाते रहे हैं बिना किसी समझौते के। इसलिए भी ‘ख़लल’ ज़रूरी है और हमेशा रहेगा।