संजीव कुमार ऐसे आलोचक हैं जिनकी आलोचना-भाषा सर्जनात्मक गद्य का आनंद देती है. यही लेख देखिये- है तो आलोचना की भाषा पर बेहद गुरु-गंभीर टाइप लेख और मैं हूं कि इसकी भाषा पर मुग्ध हुआ जा रहा हूं. शायद इसी को लालित्यपूर्ण पांडित्य कहते होंगे. बहरहाल, यह लेख उन्होंने हाल में पटना में आयोजित एक सेमिनार में पढ़ा था जिसका आयोजन प्रसिद्ध आलोचक नन्द किशोर नवल की ७५ वीं जयंती पर किया गया था- प्रभात रंजन
=============================================
(इपंले को अहसास है कि यह आलेख अभी अल्पविकसित और कुपोषित है। इसलिए वह दोस्तों की सलाहों से लेकर लानतों तक को पुष्टई यानी टॉनिक के रूप में ग्रहण करने का वचन देता है। बजाएं,जितना बजाना हो!)
एक रचनाकार के रूप में–अगर कुछ अंडरग्राउंड कविताओं और ओवरग्राउंड कहानियों के आधार पर मैं रचनाकार होने का दावा कर सकता हूं तो–मैं उन कथाकारों और कवियों का आभार मानता हूं जिन्हें मैंने, बाली से लेकर बालिग तक, किसी भी उम्र में टूट कर प्यार किया। पर आलोचक के रूप में मेरी स्थिति ठीक उलट है। यहां मैं आभारी उन आलोचकों का हूं जिनसे मेरी पर्याप्त असहमति रही,क्योंकि अक्सर असहमतियों ने ही मुझे लिखने का माल मुहैया कराया। इस लिहाज से मुझे अपने शिक्षक और पहले वरिष्ठ कामरेड श्री नंदकिशोर नवल का उचित ही आभार व्यक्त करना चाहिए, जिनके मार्क्सवादी दौर की आलोचना से भी मेरी बहुतेरी असहमतियां रहीं और उत्तरमार्क्सवादी दौर की आलोचना से भी। नवल जी के पचहत्तर पूरे करने के अवसर पर आयोजित इस संगोष्ठी में यह आभार मैं पूरी गंभीरता से व्यक्त कर रहा हूं और बजि़द हूं कि इसे वदतोव्याघात न माना जाए, क्योंकि 1.असहमति का लक्ष्य बन पाने की योग्यता अपने-आप में किसी आलोचक की बड़ी उपलब्धि है,वर्ना हिंदी में, पदोन्नति के लिए किताबें छपवाने वालों को छोड़ भी दें तो,ऐसे आलोचकों की तादाद अच्छी-ख़ासी है जो मुझ सरीखे किसी जिज्ञासु के लिए सहमति-असहमति के दायरे से ही बाहर हैं। जिज्ञासुगण उन्हें गोदानते ही नहीं, असहमत तो क्या होंगे! और
2.आत्यन्तिक स्तर पर न सही, अभिभूत होना सिरजने की दिशा में जितना फलदायी होता है, उतना ही असंतुष्ट होना विचारने की दिशा में। तो क्या इसका आभार व्यक्त नहीं किया जाना चाहिए?
पर नवल जी का कृतज्ञ होने के और भी कारण हैं। पीछे जिस कारण का जि़क्र किया गया,वह तो सिर्फ़ चौंकाऊ होने की वजह से पहले स्थान पर है। दूसरे कारण उतने ही,या कई मामलों में उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उस छोटी उम्र में,जब आपको ‘क़दम-क़दम पर चौराहे’ मिलते हैं और ‘एक पैर रखते ही हज़ारों राहें फूटती’हैं,नवल जी के संपर्क ने मुझे आत्मानुशासन और योजनाबद्ध कार्य का मतलब समझने का अवसर दिया। अक्सर मैं जावेद अख़्तर और अपूर्वानंद जैसे अपने कर्मठ साथियों को नवल जी के इस प्रश्न पर बग़लें झांकते देखता, कि ‘इन दिनों किस चीज़ पर काम कर रहे हैं?’ तब मैं यह हिसाब लगाने लगता कि ये सीनियर-द्वय मुझसे कितने बड़े हैं और इन्हें पानी-पानी करने वाला यह वाटर-कैनन मेरी ओर कब मुड़ेगा। संगठन के काम के साथ-साथ अपनी पढ़ाई-लिखाई कितने समानुपातिक ढंग से चलाई जानी चाहिए,यह मैंने नवल जी से जाना, भले ही आज तक उसके अनुप्रयोग की असफल कोशिशें ही करता आया हूं।
पटना विश्वविद्यालय के उस माहौल में, जहां पदानुक्रम बहुत स्पष्ट रूप से परिभाषित थे और जहां आप अपने शिक्षक से कृपा या कोप की ही उम्मीद कर सकते थे, नवल जी के व्यक्तित्व ने उम्र के फ़ासलों को पाटती कॉमरेडरी के मायने समझाए। सन् 86 का वह दिन मैं नहीं भूल सकता जब पटना कॉलेज के सामने पीपीएच की दूकान पर किताबें देखते हुए मैंने पाया कि नवल जी पास खड़े हैं, यह कहते हुए कि ‘अपूर्व जी ने आपकी कविताएं पढ़वाईं। अच्छी हैं। प्रेम कविताओं को छिपाते क्यों हैं? लिखे जाने के बाद तो वह सबके लिए है।‘ निस्संदेह,वे सिर्फ़ एक कवि को नहीं, एक प्रेमी को भी प्रोत्साहित कर रहे थे और बी.ए. द्वितीय वर्ष के एक विद्यार्थी के लिए अपने से लगभग तीस साल बड़े, विश्वविद्यालयी विभाग में पहुंच चुके एक शिक्षक से जुड़ा यह तजुर्बा सन् 86 के पटना शहर में कितना विरल और रोमांचक था,इसे दिक्काल में बहुत दूर स्थित लोग नहीं समझ सकते।
अपने आलोचना-कर्म से भी और अभिधा में दिए गए मशवरों से भी,नवल जी ने यह समझाया कि समकालीन और निकट अतीत की रचनाएं पढ़ने के साथ-साथ अपनी परंपरा से परिचित होना—मसलन, तुलसीदास और मैथिलीशरण गुप्त को पढ़ना–कितना ज़रूरी है। मार्क्सवादी ‘सौंदर्यबोध’ की बात,और यह बात कि क्रांति की उथली ललकार नहीं,हर अच्छी और सुंदर चीज़ को बचाने का उद्यम प्रगतिशीलता की पहचान है,मैंने पहली बार उन्हीं के मुंह से सुनी, और सोचा कि इतने सुंदर आदमी से ही मैं ये बातें सुन सकता था।
ग़रज़ कि बहुत निकट न हो पाने और न रह पाने के बावजूद नवल जी को अक्सर मैंने अपने भीतर पाया, कभी अपनी आस्वाद-क्षमता के सकारात्मक, तो कभी नकारात्मक कारण के रूप में, कभी मुझे-कैसा-होना-चाहिए के नमूने के तौर पर और कभी मुझे-कैसा-नहीं-होना-चाहिए के उदाहरण के रूप में। अनुकरणीय और अननुकरणीय का विचित्र घालमेल… टिपिकल पितृ-छवि…।
शायद आपको लगे कि ‘आलोचना की भाषा’ से इन लगभग व्यक्तिगत बातों का क्या संबंध है। साफ़ कहूं,कोई संबंध नहीं।
पर लगे हाथ यह भी कहूं कि इस आलेख को लिखते हुए ‘क्या संबंध है’वाले वाक्य से ‘कोई संबंध नहीं’वाले वाक्य तक आने में मुझे कई घंटे लगे हैं। इन बीच के घंटों में मैं पूरी कोशिश करता रहा कि संबंध का कोई ऐसा तंतु निकाल लिया जाए जिसकी मदद से एक अखंड पट की तरह यह पूरा आलेख बुना जा सके, पर वह न हो पाया। यह सूचना स्वयं आलोचना के बारे में और किसी भी वैचारिक प्रवचन के बारे में एक वस्तुस्थिति का बयान करती है। वह यह कि एक स्तर पर आलोचक या विचारक भी समेकित ढांचा गढ़ने की कोशिश में कि़स्सागो जैसी भूमिका निभाता है। जिसे हम सृजन से बिल्कुल अलग धरातल पर उसके विश्लेषण, प्रशंसन और छिद्रान्वेषण की विधा मानते हैं, वह आलोचना भी कहीं एक रचना ही है। इसी ख़याल से इस लेख की शुरुआत में रचना और आलोचना के लिए अलग-अलग प्रेरणाएं बताते हुए भी इपंले (इन पंक्तियों के लेखक) ने यह कहने की सावधानी बरती थी कि इन्हें किसी आत्यन्तिक स्तर पर न लिया जाए,जिसका मतलब यह कि आप रचना और आलोचना को निरपेक्ष भाव से भिन्न न मान लें और इनकी कुछ बुनियादी समानताओं के प्रति सचेत रहें।
पर यहां एक दूसरी समस्या आती है। आप जानते हैं कि पिछले तक़रीबन चालीस सालों में पश्चिम में जिन विचारकों का सबसे अधिक दबदबा रहा,उन्होंने सभी ज्ञानानुशासनों की अभी तक की तमाम कारगुज़ारियों को कि़स्सागोई से अभिन्न बताने में कोई क़सर नहीं छोड़ी है। यह एक दूसरा सिरा है,जहां भाषा-मात्र को तत्वतः अप्रस्तुतविधानपरक या मेटाफ़ोरिकल मानते हुए और अर्थ को संकेतन की विभेदात्मक प्रकृति पर, न कि किसी तथाकथित संदर्भधर्मिता पर, निर्भर बताते हुए यह घोषणा की जाती है कि “सब साहित्य ही है, नृतत्वशास्त्र,भाषाविज्ञान,मनोविश्लेषण आदि नामों से जिन्हें हम जानते हैं, वह साहित्य के अलावा और कुछ भी नहीं” (पाल डी मान,ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट)। आलोचना, जो कि एक ज्ञानानुशासन भी है, उसकी रचना से आत्यन्तिक भिन्नता को नकारते हुए भी मैं इस कि़स्म की आत्यन्तिक अभिन्नता के पाले में खुद को नहीं पाता, यह अलग बात है कि फि़लहाल इससे बहस करने का मेरा कोई इरादा नहीं,क्योंकि मेरे पास न तो वह मूर्खतापूर्ण दुस्साहस है जो इसे आनन-फ़ानन में ख़ारिज करने के लिए दरकार है, न ही वह तैयारी और अवकाश जो इसके साथ गंभीर बहस चलाने के लिए होनी चाहिए। पर यह मुझे लगता है कि विचार के अत्यंत परिष्कृत औज़ारों से लैस यह चिंतन-प्रणाली जिस अतिवादी त्वरा के साथ मानव-विज्ञानों की श्रेणी में आनेवाले अनुशासनों के बीच किसी भी भेद से इंकार करती है,

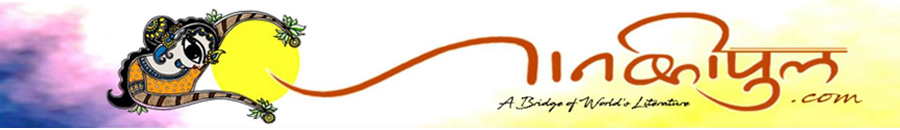

11 Comments
main sanjeev jee ki ek baat se khastaur pe sahmat hun ki kisi vishay ke sandarbh me hamari asahmati chahe wo kisi bhi roop me ho hamare bheetar ek naye nazariye ko janm deti hai….sahitya ka janm hi dwand se hua hai…abhivyakti aur madhyam ke dwand se….dwand hi srijan ka kendrabindoo hai.
sanjeevji ki bhasha mein ek layatmakta hai.itne sunder lekh ke liye badhai.kalawanti,ranchi.
sanjeevji ki bhasha mein ek layatmakta hai.itne sunder lekh ke liye badhai.kalawanti,ranchi.
संजीव का अंदाजे-बंया हमेशा मेरे में एक लुफ्त का संचार करता है …वह बात तो अपने विचार की रखते हैं पर रखते हैं अपनी रौ में … इतिहास व विचार के contradictions पर माएक्रोस्कोपी छान-बीन में जासूसी तरीके से अपनाना ..किस्सागोई में ठोक- पीट उस पर अपनी एक लताड़ –
एतिहासिक प्रक्रिया में मूल्यवान सन्दर्भों को जो सामने परत -परत दर खोलेगा हैं वह है रचना का अपना पाठ .
Sanjeev Bhai , excellent work … Alochna padhne men aanand aaye , is se perfect aalochna ho hi nahin sakti… aapke rachnatmak growth ki ek jhalak dekhne ko mili …. anand aa gaya ..
shailendra
संजीव की प्रखरता, अध्ययन, खुली दृष्टि और मौलिक अंवेषण, साथ ही रचनात्मकता और व्यंजना…उनकी आलोचना को ताज़गी देती है और जिस समकालीन रचनात्मकता के समानांतर हम क्रिएटिव आलोचना का ख्वाब देखते हैं उसे पूरा करती है, क्योंकि संजीव स्वयं एक कथाकार हैं…और आलोचक शुष्क आलोचक मात्र हो यह मिथक टूट्ने को है. – मनीषा कुलश्रेष्ठ
वाकई… भाषा पर ऐसी है कि मुग्ध हुए बिना नहीं रहा जा सकता… ऐसी भाषा में आलोचना… आलोचना में दिलचस्पी और व्यापकता बढ़ाने जैसा है…
vineet, kamaal! Main alochna ke liye isi bhasha ki sifarish kar raha hoon jo tumhari tippani mein hai. डिब्बाबंद वैचारिकी… हवा के संपर्क में आने से जल्दी खराब होने की संभवना… "सेवा" के बजाय "सर्विसिंग"… हालमार्क और ओके टेस्टेड,स्टीगर लगे इन डब्बों की एक्सपायरी और एमएफडी तारीख देने की बेचैनी… bhasha ko jab aap yah rachnatmak chhoot dete hain tabhi wah aapki ungli pakde anjaan ilaaqon tak le jaati hai. Ham hamesha is mugalte mein rahte hain ki karta to ham hain, isliye ham hi bhasha ko kahin le jaa sakte hain, bhasha hame kaise le jaayegi!
shukriya!
संजीव के लेखों से गुजरना कथा की किस्सागोई और पूर्वजों की डिब्बाबंद वैचारिकी(जिसकी सप्लाई साहित्यिक शिक्षकों द्वारा कक्षा-दर-कक्षा होती आयी है. इन डिब्बाबंद वैचारिकी को छात्रों के बीच सप्लाय करने के पहले इस बात की जरुरत महसूस नहीं की जाती कि इससे पहले खोलकर देख तो लें सही कि क्या और किस हालत में दे रहे हैं बल्कि न खुले इसके लिए अतरिक्त सावधानी बरती जाती है.कारण हवा के संपर्क में आने से जल्दी खराब होने की संभवना बढ़ जाती है. साहित्यिक दुनिया में वैचारिकी का प्रसार इसी डिब्बाबंद सप्लाय के पैटर्न पर होता आया है जहां संख्यात्मक स्तर पर बढ़ोतरी होने के बावजूद प्रक्रिया और उसमें लिथड़ने का विधान बहुत कम है,बहरहाल)के प्रति घोर कसमसाहट लिए एक साथ गुजरने जैसा है. इन्हें पढ़ते हुए अक्सर ज्ञान और समझ से कहीं पहले वो साहस अर्जित कर पाते हैं जिसमें बड़े से बड़े मूर्धन्य को हल्के से सटा देने(असहमति के संदर्भ में)में हिचक नहीं होती. कई बार ऐसे मूर्धन्य से तर्क करते हुए,असहमत होते हुए संजीव को जब पढ़ता हूं तो "प्लेजर ऑफ ट्रबल्स" की अनुभूति होती है जहां अपने ही आराध्य के पिटने और थोड़े वक्त के लिए आराध्यविहीन भक्त होने का सुख मिलता है.
आलोचना इतनी खुली हो सकती है कि सपाट तरीके से जिस थाली में खाते आए, उसी में छेद करने पर आमादा की जद तक मुहावरा हासिल कर ले, एक पाठक की हैसियत से इससे ज्यादा सुकून पढ़ते हुए और क्या हो सकता है ? हां इन छेदों के बीच से जो कुछ झांकता है, वो कम दिलचस्प नहीं है.संजीव में जब-तब अपने लेखन से एहसास करा जाते हैं कि प्रगतिशीलता,खुलापन,उदार जैसे शब्दों/अवधारणाओं/मान्यताओं के बीच भी धूल और जंग बराबर लगते-जमते रहे हैं और इसलिए अपने भीतर नियमित सर्विसिंग की जरुरत बनी रहती है. मेरे ख्याल से उनका लेखन हम पाठकों से पूर्ववर्ती के प्रति "सेवा" के बजाय "सर्विसिंग" की मांग ज्यादा करती है.अगर इस परिप्रेक्ष्य से इस लेख को देखें तो आलोचना के स्तर पर कुछ मूर्धन्य जाहे जो भी कीर्तिमान और प्रतिमान कायम किए हों लेकिन भाषाई स्तर पर कितना बड़ा छल किया है(संजीव इसके लिए न तो उन्हें छलिया करार देते हैं और न ही ये छल उनका है बल्कि स्वयं भाषा का है)ये समझते ही हमें कक्षा-दर-कक्षा चली आ रही डिब्बाबंद वैचारिकी के प्रति गहरी शंका पैदा होती है. हालमार्क और ओके टेस्टेड,स्टीगर लगे इन डब्बों की एक्सपायरी और एमएफडी तारीख देने की बेचैनी बढ़ जाती है.
संजीव का लेख अमूमन कथात्मक आलोचना है या फिर आलोचनात्मक कथा. मुझे नहीं पता कि इसकी साहित्यिक व्याख्या क्या होगी. आशय सिर्फ इतना भर है कि आप इनमें एक ही साथ कथा और आलोचना से गुजरने का गहरा एहसास पाते हैं. बौद्धिकता के आसपास अपनी इस समझ को बिठाने के चक्कर में अगर हमने गलत जार्गन का प्रयोग कर दिया है तो ये आगे के टिप्पणीकारों की जिम्मेदारी है कि दुरुस्त कर दें. लेकिन हां अगर मेरी इस एक पंक्ति को दोहराव या शाश्वत बनाने की प्रक्रिया का होड़ न माना जाए तो संजीव के लेख को पढ़ते हुए अक्सर साहित्यिक आलोचना की तरफ लौटने का मन करता है.
Pingback: Blue Meanie Mushrooms (Panaeolus Cyanescens) for sale
Pingback: วิเคราะห์บอล