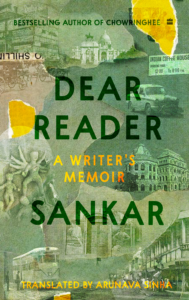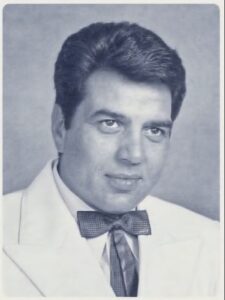वरिष्ठ लेखक जयशंकर का लिखा ‘वे निर्मल दिन’ का यह हिस्सा समास-26 में प्रकाशित हुआ था। चूँकि वरिष्ठ लेखक जयशंकर निर्मल वर्मा के संस्मरण उसके बाद भी लिखते रहे, हमें लगा कि बाद के हिस्सों को भी यहीं प्रकाशित करना चाहिए। हम समास पत्रिका के बहुत आभारी हैं। आज निर्मल वर्मा की पुण्यतिथि पर विशेष- मॉडरेटर
=========================
दिल्ली। अक्टूबर 1987। मैं आधुनिक कला संग्रहालय में निर्मलजी को ब्रिटिश कलाकार हेनरी मूर के एक मूर्तिशिल्प के सामने देख रहा हूँ। इन दिनों हेनरी मूर की कलाकृतियों का सिंहावलोकन चल रहा है। समूची गैलरी में, गैलरी के परिसरों में, उनकी कलाकृतियाँ नज़र आती रहती हैं। मेरे संग गैलरी में गगन गिल और उदयन वाजपेयी भी मौजूद हैं।
आज सुबह-सुबह ही, निर्मलजी की बरसाती में टाइम्स ऑफ़ इण्डिया से जाना कि इस बरस के साहित्य का नोबेल पुरस्कार, रूसी कवि जोसेफ़ ब्राडस्की को मिला है। वे अमेरिका में एक निर्वासित कवि का जीवन जी रहे हैं। उनके बूढ़े माता-पिता रूस में ही रहते रहे थे। बाद में निर्मलजी के यहाँ ही इनके गद्य की किताब ‘लेस देन वन’ देखी थी।
मैं और उदयन सुबह-सुबह ही दिल्ली पहुँचे। नाश्ते के बाद हम तीनों हंगारी फ़िल्म निर्देशक इस्तावन जाबो की फ़िल्म ‘मेफ़िस्टो’ देखने के लिए चाणक्य टॉकीज़ गये। रास्ते में हमें निर्मलजी टॉमस मान के इसी शीर्षक के उपन्यास के बारे में बताते रहे। उनके अनुसार दूसरे महायुद्ध के बाद मेफिस्टो का मिथक यूरोपीय कला और साहित्य में लौटता रहा है।
हम फ़िल्म के बाद कनॉट प्लेस आये थे। वहीं ‘बुकवर्म’ में हमें गगनजी मिली थी। हम लोगों ने अपना थोड़ा-सा वक़्त गलगोटियाँ और न्यू बुक डिपो में भी बिताया था। मैंने गलगोटिया से फ्रेंच लेखिका कॉलेट के दो उपन्यास खरीदे थे। बाकी लोगों ने भी अपने लिए कुछ किताबें खरीदीं थीं।
उन बरसों का कनॉट प्लेस कुछ और ही हुआ करता था। वहीं सड़के के एक हिस्से में हमारे साथ खड़े हुए निर्मलजी की एक तस्वीर अब भी मेरे एलबम में है। हमारे पीछे मिट्टी के कटोरे के क़रीब दाना चुगते हुए कबूतर हैं। हमारी यह तस्वीर गगनजी ने अपने कैमरे से खींची थी।
कनॉट प्लेस से हम चारों लोग मॉडर्न आर्ट गैलरी गये थे। हेनरी मूर की कलाकृतियों की प्रदर्शनी देखने के लिए। वहीं से हम लोग दरियागंज गये थे। गोलछा टाकीज़ के क़रीब के एक मकान में। वह निर्मलजी की बहन निर्मलाजी का घर था। हमने वहीं अपना दुपहर का खाना खाया था। उस दिन के पहले तक अनन्नास देखकर लुई बुन्वेल की फ़िल्म ‘नाज़रीन’ के पादरी के हाथ में रखे अनन्नास की कभी-कभार याद आ जाया करती थी लेकिन निर्मलाजी के घर में अनन्नास खाने के बाद, कभी-कभार बरबस ही अक्टूबर की उस दुपहर का आत्मीय-सा चित्र सामने खड़ा हो जाता है।
खाने के बाद हम लोगों ने इतालवी फ़िल्म निर्देशक अन्तोनियोनी की फ़िल्म ‘द पैसेंजर’ को टेलिविज़न पर देखा था। उस दिन को बीते हुए लगभग सैंतीस बरस होने को आ रहे हैं। याद नहीं आता कि उस दिन हम दरियागंज की पुरानी किताबों की दुकानों में गये थे भी या नहीं? निर्मलजी के साथ वहाँ जाने की कुछ यादें ज़रूर साथ है लेकिन वह दिन, यह दिन भी था, इसे निश्चित रूप से कह नहीं सकता हूँ।
शाम को किसी घड़ी में गगनजी अपने दफ़्तर या घर लौट गयी थीं। हम तीनों निर्मलजी के घर लौटे थे। निर्मलजी ने कुछ देर तक आराम किया था। वे नहाने के बाद बरसाती में आये थे। इधर-उधर की, हल्की-फुल्की बातों के बाद, हमने उनसे अन्तोनियोनी की शुरुआती दौर की फ़िल्म ‘द नाइट’ के बारे में सुनना शुरू किया। उन्होंने फ़िल्म की शुरुआत के ही एक दृश्य से कहना शुरू किया था। एक प्रसिद्ध लेखक और उसकी पत्नी अपने एक आलोचक मित्र से मिलने के लिए अस्पताल जाते है। उनका वह मित्र मरणासन्न है। लेखक की एक नयी किताब के आने की खुशी में एक बड़े उद्योगपति ने अपने विला में पार्टी का आयोजन किया है। वे दोनों अस्पताल से उस पार्टी में जाते हैं। लेखक वहाँ कुछ लोगों से मिलता रहता है और नायिका इधर-उधर अकेले ही भटकती रहती है। अपने आसपास के परिचित और अजनबी लोगों से क्षण भर के लिए मिलती-बतियाती है लेकिन ज़्यादातर कैमरा उसे अकेले घूमते हुए बताता रहता है। फिर फ़ोन से नायिका को अपने आलोचक मित्र के मरने की ख़बर मिलती है। फ़ोन का रिसिवर रखने के बाद नायिका वहाँ हो रहे नृत्य में शामिल हो जाती है।
इतने बरसों के बाद भी (मैंने यह फ़िल्म बाद में देखी थी) निर्मलजी का कहानी सुनाते-सुनाते दो शब्दों पर बार-बार लौटना अच्छी तरह याद आता है। वे थे- ‘डाँस एण्ड डेथ।’ मृत्यु और नृत्य- मृत्यु और जीवन का एक साथ होना। यहीं से वे हमारे और ग्रीक महाकाव्यों तक गये थे। होमर के ‘एलियाड’, हमारे ‘महाभारत’ पर। उस शाम महाकाव्यात्मक विस्तार और आयामों को समझाने के लिए एलियाड में हेक्टर की मृत्यु के पहले उसका अपने बचपन को याद किया जाना, मृत्यु का उसका पीछा करना भी याद आता है। उसी शाम उन्होंने हमारे पुराणों में आते हुए सेक्स और हिंसा के दृश्यों का ज़िक्र करते हुए, दोस्तोएवस्की की ईविल की धारणा पर भी कुछ कहा था।
उनके साथ बीती घड़ियों की स्मृतियों का लौटना, मेरे लिए उनकी बौद्धिक उत्तेजना, बौद्धिक जीवन्तता का लौटना है। उनके साथ बीते समय को याद करना, दूसरों के लिए उमड़ती उनकी भावनात्मक गरमाहट को महसूस करना है। मेरे लिए उनकी याद ग्रेस, परिश्रम, सच्चाई, स्वाधीनता और सौन्दर्य लिए हुए, एक कर्मठ और सच्चे लेखक की याद है। एक ऐसा लेखक जिसके लिए लिखना साधना, प्रार्थना और तपस्या बनी रही थी।
एक ऐसा लेखक जिसकी आत्मा इस जीवन, संसार और सृष्टि को प्रेम करते रहना चाहती रही थी और जिसने इन सबके साथ अथाह प्रेम किया भी था।
अपने आप को लेकर कह ही सकता हूँ कि उन्होंने मेरे यौवन के सुख और सौन्दर्य को गढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद की थी। अब निर्मलजी को जब कभी भी याद करता हूँ, अपने उन दिनों के सुख को ही नहीं, अपनी उन दिनों की चाहनाओं और भयों को भी याद करता हूँ। उनके साथ होता, उनका संग बना रहता और मैं अपने भीतर के बहुत सारे भयों से मुक्त रहा करता था। सिवाय इस एक भय के कि भूल से भी निर्मलजी की तरह की सच्ची, साफ़-सुथरी आत्मा के साथ ऐसा कुछ कर न दूँ कि उनको कष्ट पहुँचे, और मेरी तरफ से पहुँचे। मैं उनके किसी भी तरह के दुख का कारण बनने से बचे रहना चाहता था। बाद के बरसों में उनकी लम्बी बीमारी के उनके आखिरी बरसों में, मेरे साथ अपने इस भय के अलावा एक और भय भी जुड़ गया था। उनको हमेशा के लिए खो देने का भय, जो उनके जीवन के आखिरी कुछ बरसों में मेरे साथ निरन्तर बना रहा था। अन्ततः 25 अक्टूबर 2005 को मैंने उनको खो ही दिया था।
जून 1988 के आखिरी दिन। गर्मियों के जल्दी ही लौट जाने की याद से झरता आनन्द।
धीरे-धीरे निर्मलजी की कृतियों को पढ़ते हुए, उनसे बीच-बीच में मुलाकातों, पत्र-व्यवहार के आठ बरस होने को आये हैं। अब तक प्रकाशित उनकी हर किताब को कम से कम दो बार पढ़ ही चुका हूँ। इन सबसे थोड़ा-सा ही सही लेकिन इतना ज़रूर जाना है कि उनके व्यक्तित्व के भीतर एक अच्छा जीवन जीने के लिए, कुछ भी अच्छा रचने के लिए ज़रूरी, एक सभ्य नागरिक और लेखक के लिए अनिवार्य, संवेदना, सजगता, प्रखरता और समानुभूति बराबर बनी रही है, बढ़ती रही है।
उनके निबन्धों को पढ़ते-पढ़ते जानता रहा हूँ कि वे अपने कथेतर गद्य के माध्यम से, स्वयं को भूलते हुए मानवीय समाज में व्यक्ति और समुदाय के बीच एक जीवन्त किस्म के पारस्परिक प्रवाह को पैदा करने की तमाम लेखकीय चेष्टाएँ कर रहे हैं। उनके पास अपनी एक समर्पित अन्तर्दृष्टि है। मानवीय जीवन का अपना खुद का एक विज़न।
उनके इन निबन्धों में हम फूहड़ और परिष्कृत संस्कृति के बीच के टकरावों को महसूस कर सकते हैं। वे मास संस्कृति से अपनी आलोचनात्मक और कलात्मक अन्तर्दृष्टि के साथ, सवाल-जवाब करते हुए, निरन्तर कुछ न कुछ पूछते हुए अपना लेखकीय दायित्व निभाते हैं। अगर सवाल खड़े किये जाने की चिन्ताएँ उनके निबन्धों में हैं, उन सवालों से जुड़ा हुआ नैतिक आवेग और बौद्धिक जागरूकता भी वहाँ शामिल रहती है।
उनको सुनते हुए भी समझ में आता है कि आधुनिक मनुष्य का खोखला फूहड़ और संकीर्ण होते चले जाना उनको निराश करता है। उनको हमारे इधर के जीवन में रची-बसी सुख की विवेकहीन और असंगत धारणाएँ तकलीफ़ और तनाव देती हैं।
आधुनिक मनुष्य का संकीर्ण, अपरिष्कृत और आत्ममुग्ध बने रहना, उनके अपने भीतर के सांस्कृतिक विषाद को बढ़ाता रहता है लेकिन उनकी मनुष्य के भीतर आत्ममन्थन, आत्मचिन्तन की प्रवृत्तियों पर भी कम निष्ठा नहीं रही है। वे खुद अपनी निराशाओं के क्षणों में भी, कला और साहित्य के संसार के लिए, अपनी दिलचस्पी, निष्ठा और जोश को बराबर बनाये रखते हैं।
एक तरह से देखा जाए तब यह भी लगता रहता है कि साहित्य और कला की दुनिया ही वह दुनिया है, जहाँ से उनका अपना सुख बाहर आता है, अपने स्वप्न बाहर आते हैं।
दिल्ली की उनकी बरसाती की आरामकुर्सी पर बैठे हुए मैं उनके लेखक की दिनचर्या को देखता रहता हूँ। कितनी अनुशासित रहती है उनकी दिनचर्या। अपना लिख लेने के बाद, वे दिन भर कुछ न कुछ पढ़ते रहते हैं, अपने मित्रों और पाठकों को पत्र लिखते रहते हैं। उनसे मिलने आये लोगों से गहरी आत्मीयता के साथ मिलते रहते हैं। एक लेखक की भरी-पूरी दुनिया उनके साथ निरन्तर बनी रहती है।
अगस्त 1988। दिल्ली की हवाओं में उमस और घुटन-सी महसूस होती है। डीटीसी की बसों से कहीं भी आना-जाना होता है और समूची देह पसीने और गर्मी से लिथड़-सी जाती है। दुपहरों में निर्मलजी के घर पर ही रहता हूँ।
इन दिनों उनको सर्दी, बुखार और खाँसी ने घेर रखा है। बरसाती में फ़र्श के उनके बिस्तर के सिरहाने रखी धूसर रंग की मिट्टी की तश्तरी में उनकी इन दिनों की दवाईयाँ, पानी का जग और गिलास रखा रहता है। बीच-बीच में उनसे थोड़ी बहुत बातचीत होती रहती है। वे नीचे के अपने कमरे में आराम या अपना काम कर रहे होते हैं। मैं बरसाती की आरामकुर्सी पर बैठे-बैठे उनकी रैक से उठायी किसी किताब को पढ़ता रहता हूँ।
आज दुपहर में उनसे मिलने के लिए इलाजी (डालमिया) आयी थी। अज्ञेयजी के न रहने के बाद उनसे पहली बार मिलना हुआ है। उन्होंने भूटानी स्त्रियों की कत्थई रंग की पोशाक पहन रखी है। जाते समय वे मुझे हाल ही में आये हुए अपने ‘छत पर अपर्णा’ शीर्षक के उपन्यास की एक प्रति भेंट कर जाती है। उपन्यास का ब्लर्ब निर्मलजी ने लिखा है। इलाजी अपनी कुछ समस्याओं को निर्मलजी के सामने रख रही हैं। उनमें उनके घर की गाय को हुई कैंसर है। अपनी गाय की दैहिक पीड़ा की बात को वे गहरी करूणा के साथ व्यक्त कर रही हैं। निर्मलजी लेटे हुए ध्यान से उनकी हर बात को सुन रहे हैं। बीच-बीच में वे अपनी कोई टेबलेट ले लेते हैं।
इलाजी के जाने के बाद वे एकाध घण्टे तक सोये रहे। शाम को हमने बरसाती में ही चाय पी और बिस्कुट खाये। वे बताने लगे कि हाल ही में टाईम्स ऑफ़ इण्डिया की पत्रकार जहाँआरा वासी ने उनसे एक इंटरव्यू लिया है। उस इंटरव्यू में वे उनके उपन्यास ‘लाल टीन की छत’ के बारे में कुछ जानना चाह रही थी।
उस पत्रकार के सवाल की याद करते हुए उन्होंने बताया कि बरसों पहले उन्होंने अमेरिकी उपन्यासकार कॉर्सन मैकुलर्स की किताब ‘मेम्बर ऑफ़ द वेडिंग’ पढ़ी थी, जिसमें एक कस्बाती किशोरी के जीवन के आत्मीय पोर्ट्रेट ने उनको छू लिया था। शायद ‘लाल टीन की छत’ लिखते हुए बरसों पुरानी उस रिडिंग की छायाएँ भी उनके दिमाग में रही होंगी। अमेरिका के दक्षिणी इलाके के परिवेश और पात्रों को लेकर कार्सन मैकुलर्स की कुछ और भी कृतियों का ज़िक्र उन्होंने किया था। उसके बाद ही मैंने किताबों के उनके ही अनुपम कलेक्शन से मैकुलर्स के कुछ उपन्यास पढ़ने के लिए ले लिए थे, जिनमें उनका पहला ही उपन्यास ‘हार्ट इज़ ए लोनली हण्टर’ भी था। मुझे लगता है, उनके पहले ही उपन्यास का शीर्षक बाद में भी उनके उपन्यासों की केन्द्रीय थीम बनी रही थी।
मानवीय मन की भीतरी उथल-पुथल, दिल में उठते हुए वलवलों पर लिखे गये टेनेसी विलियम्स, ट्रूमेन कापोटे, हार्पर ली और कैथरीन पोर्टर के लिखे गये का भी उसी शाम वे ज़िक्र करते रहे थे। किसी लेखक का अपनी ज़मीन से गाढ़ा रिश्ता भी निर्मलजी को प्रभावित करने वाला एक बड़ा गुण रहा होगा। इसलिए भी विलियम फ़ॉकनर, चेख़व, प्रूस्त, वर्जिनिया वुल्फ़, मुक्तिबोध और फणीश्वरनाथ ‘रेणु’ का गद्य उन्हें भाता रहा था। अपने परिवेश और पात्रों के बीच खड़ा किया जाता अन्तर्सम्बन्ध, पात्रों के दिल और दिमाग का मार्मिक चित्रण, गहरायी और गम्भीरता से की गयी परिवेश और पात्र की जाँच-पड़ताल, उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्त्व रखती आयी थी।
मानवीय यथार्थ को आवेग और आवेश लिये जानने की उनकी गहरी लालसा भी एक बात रही है, जिनके कारण वे मुझे एक भारतीय और सिर्फ़ भारतीय लेखक लगते रहे हैं। यह भी रहा होगा कि अपनी ‘कव्वे और काला पानी’ जैसी मर्मस्पर्शी, असाधारण कहानी में उन्होंने हमें यह भी बताया था कि साधु-संन्यासी, फकीरां की ज़िन्दगी को पूरी तरह से फालतू मान लेना हमारी भूल ही हो सकती है। मानवीय यथार्थ वहाँ भी खड़ा रह सकता है। वहाँ भी कोई रौशनी खड़ी हो सकती है, कोई जीवन हमें पुकारता रहता है।
निर्मलजी को पढ़ते रहने के उनसे मुलाकातों के पहले दशक में उनके लेखक और व्यक्ति से सम्मोहित होता रहा था लेकिन उनकी मनीषा, उनके चिन्तन-मनन का बहुत थोड़ा-सा ही अंश समझ पाता था। पर तब भी इतना ज़रूर लगता रहता था कि जो कुछ वे लिख रहे हैं, जो कुछ वे कह रहे हैं, इन सबका मेरे लिए, मेरी अपनी भाषाओं के साहित्य, समाज और सभ्यता के लिए गहरा और गम्भीर अर्थ हमेशा बना रहेगा। निर्मलजी का लिखा गया, हमारी भाषाओं और साहित्य की एक दुर्लभ धरोहर हमेशा बनी रहेगी।
मार्सेल प्रूस्त ने स्मृति के जादू और रहस्य को कितनी अच्छी तरह जान-पहचान लिया था। इसकी याद एक और बार मेरे भीतर लौट आयी। मैंने बम्बई की फोर्ट इलाके की किताबों की दुकान स्ट्रैण्ड से फ्रेंच लेखक ले क्लेज़िगो का उपन्यास ‘वॉण्डरिंग स्टार’ खरीदा। किताब के कवर पर यहूदी चित्रकार बेन शाह का चित्र था।
बेन शाह के उस चित्र को देखकर निर्मलजी और गगनजी के साथ बीती दिल्ली की एक दुपहर याद आ गयी। साल याद नहीं। दिन अठारह नवम्बर था। गगनजी का जन्मदिन। हम तीनों कनॉट प्लेस में घूमते रहे थे। निर्मलजी ने म्यूज़िक टूडे की भक्तिमाला शृंखला में आये हुए कुछ कैसेट्स गगनजी के लिए खरीदे थे। वहीं के एम्पोरियम से गगनजी के लिए कुछ और चीजें भी। हम लोग एम्पोरियम के क़रीब के क़ॉफी होम में गये थे। हमने कनॉट प्लेस के गलियारे में फ्रूट चाट खायी थी। गलगोटिया से होते हुए, हम बेन शाह की प्रदर्शनी देखने आर्ट गैलरी में गये थे।
मेरे यह कहने पर कि निर्मलजी की कहानी ‘पहला प्रेम’ का नायक भी अपने प्रेम के दिनों में गलगोटिया की किताबों की दुकान में भी अपनी प्रेमिका का पीछा करता रहता है, उन्होंने एक बात कही थी, जो मुझे अब तक याद रही है। वे कह रहे थे कि जवानी की शुरुआत के दिनों में हमारी भावनाएँ उग्रता और तीव्रता लिये हुए भी रहती है लेकिन वे भावनाएँ स्थायी नहीं होती हैं।
उसी शाम को पटपड़गंज के अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए, उन्होंने बरसों पहले की दिल्ली को उसी दिल्ली में बिताये गये अपने कई-कई दिनों को कुछ ज़्यादा ही याद किया था।
मैंने खुद निर्मलजी के लिखे गये में आती दिल्ली की कितनी ही जगहों को, उनको पढ़ने के बाद ही एक-एक कर, ढूँढ-ढूँढकर देखा था। अपने शिमला प्रवास में मैंने हर उस जगह को देखने का प्रयत्न किया था, जिनका ज़िक्र उनके लिखे गये में आता रहा था, फिर चाहे वह संजौली का कब्रिस्तान रहा हो या सोलोन की कब्रें।
निर्मलजी के लिखे गये को पढ़ने की शुरुआत उन्नीस सौ सतहत्तर की गर्मियों की छुट्टियों में हुई थी। मेरे बारहवी पास होने पर डाक से आया गुनगुन दीदी का उपहार ‘लाल टीन की छत’। इस उपन्यास को पढ़कर मैं मन्त्रमुग्ध हुआ था। उनको और ज़्यादा पढ़ने की लालसा का मेरे भीतर जन्म हुआ और मैं उनकी कहानियों, संस्मरणों, निबन्धों और अन्य उपन्यासों को पढ़ता रहा, बार-बार पढ़ता रहा। उन्नीस सौ अस्सी के आसपास सम्भावना प्रकाशन से उनके लिखे गये का संचयन ‘दूसरी दुनिया’ शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। विदिशा में अपनी बैंक की नौकरी की शुरुआत में, उनके इस रीडर को दो बार पढ़ा था। इस संचयन में उनके लिखे गये का जादू ही रहा होगा कि मैं उनसे मुलाकात के लिए दिल्ली गया था।
तब तक उनकी कहानियों को पढ़ते-पढ़ते मैं थोड़ा-थोड़ा यह जानने लगा था कि दूसरों को जानना-पहचानना बहुत कठिन होता है। किसी को भी अच्छी तरह जानने के लिए ढेर सारे प्रयत्नों, खूब ज़्यादा परिश्रम की ज़रूरत रहती है।
उनकी कहानियों में मानवीय रिश्तों के बीच फैले हुए अँधेरे गलियारों, उनके पात्रों की प्रेम के बीच और बावजूद बनी हुई दूरियाँ, उन पात्रों की आन्तरिकता, उनका मौन, उनके संवाद और एकालाप, मेरे लिए मानवीय जीवन के एकदम नये और अजनबी आयामों को खोल रहे थे।
शायद उनको न पढ़ता तब इन बातों को गहराई और गम्भीरता से जान ही नहीं पाता कि एक आदमी सिर्फ़ आदमी नहीं होता है। हर आदमी वह इलाका भी होता है, जहाँ वह जन्मा है, जिस इलाके में वह पला-बढ़ा है। वह आदमी उन खेलों से भी परिभाषित होता है, जिनको वह खेलता आया था। उन देवताओं से भी जिनको वह पूजता रहा है। उस आदमी को उसकी पढ़ी गयी किताबों ने बनाया होता है और उसकी देखी गयी फ़िल्मों ने भी उसे गढ़ा होता है। इस तरह उनकी कहानियाँ पढ़ते-पढ़ते मेरी समझ में आने लगा था कि एक आदमी के बनने में समाज, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, विज्ञान, तकनीकी, धर्म और राजनीति की भी गहरी भूमिकाएँ बनी रहती हैं।
उनकी कहानियाँ ही थीं, जिनसे लेखन में परिवेश और पात्र के रिश्तों के बीच के संयोजन, संगम और सन्तुलन की आवश्यकता को मैंने जाना था। उनको पढ़ने के पहले, उनको पढ़ते हुए मैं और भी दूसरे देशी-विदेशी लेखकों को थोड़ा-बहुत पढ़ता ही आया था, लेकिन उनको पढ़ते हुए मैं कहीं पहुँच रहा था। उनका लिखा गया भी मुझे गढ़ रहा था। एक तरह से मुझे अपने जीने का कोई अर्थ, अच्छी तरह जीने की दिशाएँ मिल रही थीं।
मैं देशी-विदेशी किताबों के बारे में उनके लिखे गये को पढ़ता, अपनी मुलाकातों में नये-पुराने लेखकों के लेखन पर उनसे सुनता और फिर उन लेखकों को पढ़ना शुरू कर देता, पसन्द करना शुरू कर देता था।
उनके और उनके लेखन का सान्निध्य ही रहा कि मैं अपने लिए कितने ही लेखकों को खोज पाया था। उनको नहीं जानता तब मेरी पाठक की दुनिया बहुत ज़्यादा ग़रीब, बहुत ज़्यादा इकहरी, नीरस और संकीर्ण बनी रह गयी होती। यह भी याद आता है कि उन्होंने ही मुझे फ्राँसीसी लेखक फ्राकुआ मारिस के जीवन भर किताबों को पढ़ते रहने, अपनी पढ़ी गयी किताबों का जिक्र करते हुए अपने और अपने समय के बारे में उनके एक दिलचस्प आत्मकथा लिखे जाने की बात बतायी थी।
निर्मलजी का सुझाना, समझाना ही रहा था कि मैं न जाने कितने ही लेखकों, कलाकारों से अपना संवाद बना पाया था। इनमें डेनिश लेखक इसाक डेनिसन, दक्षिण अमेरिकी कॉर्सन मैकुलर्स, फ्लैनरी ओ कॉनर का लिखा गया भी था, जो आज भी मेरे पाठक के लिए अत्यन्त आत्मीय बना हुआ है।
कहा जाता है कि एक शान्त और ख़ामोश तालाब में किसी कंकड़ का गिर जाना भी, उस तालाब को पहले का तालाब नहीं रहने देता है। मेरे अपने जीवन में निर्मलजी का लेखन और स्वयं निर्मलजी, मेरे अपने सुख और सौभाग्य के स्त्रोत बने रहे हैं। उनके शब्दों की याद नहीं रही है लेकिन अपने शब्दों में उनकी कही गयी एक बात का ध्यान आ रहा है, जो न जाने किस परिप्रेक्ष्य में और कब उनसे सुनी थी पर जो सुनी थी उसे अपने शब्दों में उतार रहा हूँ-
‘वह एक आदमी ही था जिसने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा था और वह भी एक ही आदमी था, जिसने पहिये की खोज की थी।’
अपनी उम्र के बीस बरसों तक मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ और दिशाहीन रहा था। अपने खाली वक़्त को बर्बरता से बर्बाद करता हुआ एक निम्न वर्ग से आया हुआ वेस्टर। निर्मल वर्मा के लेखन, चिन्तन-मनन से संवाद शुरू हुआ और मैंने हमारे दो असाधारण लोगों को, उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। एक गाँधीजी, दूसरे रवीन्द्रनाथ ठाकुर। भोपाल के अपने निराला सृजनपीठ के आवास में उन्होंने इन दोनों को जानने के लिए प्रेरित किया था। उन दिनों वे गाँधीजी के अंग्रेज बच्चों के नाम लिखे गये पत्रों का संग्रह पढ़ रहे थे।
रवि बाबू के लिए अपने गहरे लगावों को बताते हुए निर्मलजी ने कहा था कि उनसे हमें यह भी सीखना चाहिए कि आदमी, फफूँद की तरह, अँधेरे में बढ़ नहीं सकता है, विकसित नहीं हो सकता है। आदमी को जीने के लिए प्रकाश की ज़रूरत रहती है और प्रकाश ज्ञान से मिलता है और ज्ञान परिश्रम, संघर्ष और समर्पण से। ये मेरी याद में आये शब्द हैं। उन्होंने बिल्कुल अलग तरह से, अलग शब्दों में यह सब बताया होगा। बयालीस बरसों के बाद उनके कहे गये का मर्म तो याद आ जाता है लेकिन उनके शब्द नहीं याद आते हैं। इसीलिए भी उनकी कही गयी कुछ बातों को इस भय से नहीं लिख पा रहा हूँ कि कहीं उनकी बातों के अर्थ का अनर्थ न कर दूँ।
दिल्ली में नवम्बर की दुपहर है। हम लोग करोलबाग के एक दक्षिण भारतीय रेस्तराँ से कुछ खाकर निर्मलजी की बरसाती में लौटे हैं। हाल ही में उनकी ‘टर्मिनल’ शीर्षक से कहानी आयी है। मेरे किसी सवाल से ज़िन्दगी में दुख या सुख के अनुभव, उन अनुभवों से गुज़रने और सहने को लेकर निर्मलजी कुछ कह रहे हैं। उनकी बातों का सन्दर्भ इधर प्रकाशित हुई उनकी कहानी ‘टर्मिनल’ है। अपनी बातों में वे खुद से सवाल कर रहे है कि क्या कोई ईश्वर का वैसे ही अनुभव कर सकता है, जैसा दुख या आनन्द का? उनकी बात का दायरा धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। उनकी बातों में रामकृष्ण परमहंस और रमण महर्षि का ज़िक्र आता है। प्रसिद्ध लेखक धनगोपाल मुखर्जी की पुस्तक ‘द फेस ऑफ़ साइलेंस’ का भी।
उस दुपहर का और उनका कहा गया बहुत कुछ भूल गया हूँ लेकिन जो कुछ धुँधला-सा याद रह गया है, वह निर्मलजी का यह कहना है कि-
‘यह पूछा जाना कठिन ही होता होगा कि आखिर में मानवीय ज़िन्दगी क्या है? फिर वह अर्थपूर्ण है भी या नहीं? कहीं ज़िन्दगी अन्धी किस्मत से जन्मी कोई ट्रैजिक भूल, कोई त्रासद बवण्डर तो नहीं है?’
अपनी बातों का विस्तार करते-करते वे ज़िन्दगी के रस, रहस्य और राग-विराग तक आये थे। इन बातों के बाद के दिनों में ही उनकी एक और असाधारण कहानी ‘एक अलग रौशनी में’ को आना था, जिसमें लम्बी बीमारी जीवन, मृत्यु और कला से जुड़े हुए सवालों को उतरना था। उनके इस संवाद के बाद ही उनके उपन्यास ‘अन्तिम अरण्य’ को आना था जिसमें फिर एक बार जीवन मृत्यु, प्रेम बुढ़ापा, अकेलापन और मानवीय मुक्ति जैसे शाश्वत सवालों को उतरना था।
अगर उनको सुनने से उनकी लिखी जा चुकी कृतियों को पढ़े जाने के पाठकीय रास्ते खुला करते थे तब कभी-कभार यह भी सम्भव हो पाता था कि उनके कहे गये में उनके आगे आने वाले किसी निबन्ध, किसी कहानी या उपन्यास की आहटों को सुना जा सकता था।
ऐसी किसी भावना, ऐसे किसी विचार के अंकुरण का कभी-कभी मैं गवाह बन जाता लेकिन जब उस भावना, उस विचार के विस्तार को अपनी समग्रता, अपना समूचापन लिए हुए देखता तब मुझे उनकी लेखकीय अन्तर्दृष्टि से गहरा आश्चर्य, गहरा आनन्द मिला करता था।
उन्नीस सौ पंचानवे के आते-आते मुझे साहित्य को थोड़ा-सा ठीकठाक ढंग से पढ़े जाने की तमीज़ आने लगी थी। पहले से कुछ बेहतर ढंग से क्लोज रीडिंग की आकांक्षा, ज़रूरत और प्रयास मेरे साथ रहना शुरू कर रहे थे। मेरे पाठक की ग़रीबी में कमी आयी थी।
अब मैं निर्मलजी के लेखन की सर्जनात्मक सच्चाई, उनके लिखे गये की अखण्डता और महत्त्व को कुछ और ज़्यादा गम्भीरता से देखने लगा था। उनके निबन्धों, उनसे लिए गये साक्षात्कारों में उनके चिन्तन-मनन के क़रीब जानता और वे मुझे हमारे समय, समाज और सभ्यता के एक कुशल दुभाषिये जान पड़ते। अपने वक्त के सांस्कृतिक दबावों को झेलता हुआ, उनसे संवाद और सवाल करता हुआ एक व्याकुल मन, जिसके अपने नैतिक आवेग रहे, अपनी लेखकीय जिम्मेवारियाँ भी।
एक बार मैं उनसे पूछ रहा था कि कुछ लोग आपके लिखे गये में सिर्फ़ उसके रूप, ढाँचे, भाषा और इस तरह आपके लेखन के सौन्दर्यात्मक आयामों की ही प्रशंसा करते रहते हैं। क्या यह आपको अपने सन्दर्भ में उचित अवलोकन जान पड़ता है?
कुछ देर तक मैं अपने खुद के लेखन पर हो रही बातों से बाहर आती उनकी घबराहट, उलझन और परेशानियों की छायाओं को उनके चेहरे पर देखता रहा था। कभी-कभार वह अपनी बात को अंग्रेज़ी में भी व्यक्त कर दिया करते थे और उस दिन मैंने उनसे शायद इन शब्दों को सुना था-
‘माई बुक्स आर नॉट पोएटिक एण्ड लिरिकल क्रियेशन्स ओनली…’
उसी दिन टॉमस मान की कहानी ‘टोनियो क्रोगर’ का ज़िक्र करते हुए, उन्होंने कला के सृजन में दोनों ही आयामों की उपस्थितियों की ज़रूरतों पर खुद को व्यक्त किया था। उनके अनुसार रचने में सौन्दर्यात्मक आयाम के साथ-साथ नैतिक आयाम को ध्यान में रखना ज़रूरी बात रही थी।
शायद उनके सोचने-समझने का यह इलाका भी रहा होगा कि उनकी अपनी पसन्द के लेखकों में टॉलस्टाय, टॉमस मान, हरमन हेस्से, सिमोन वेल और जार्ज ऑरवेल जैसे लेखक भी शामिल रहते आये थे। शायद यह भी रहा होगा कि वे सार्त्र की तुलना में, अल्बेयर कामू के लेखन के ज़्यादा क़रीब रहते आये थे। कर्म की नैतिकता का गहरा आग्रह भी रहा होगा, जो उन्हें गाँधीजी के इतना ज़्यादा निकट खड़ा करता रहा था। यहाँ उनकी किताब ‘धुँध से उठती धुन’ की इन पंक्तियों को उतारने का लोभ संवरण नहीं कर पाऊँगा-
‘जब मैं गाँधीजी के बारे में सोचता हूँ तो कौन-सी चीज़ सबसे पहले ध्यान में आती है? लौ- जैसी कोई चीज़- अँधेरे में सफ़ेद, न्यूनतम जगह घेरती हुई, पतली, निष्कम्प और पूरी तरह स्थिर प्रतिज्ञ, फिर भी जलती हुई, इतनी स्थिर कि वह जल रही है, इसका पता नहीं चलता। मोमबत्ती जलती है- लेकिन लौ? मैं जब कभी उनका चित्र देखता हूँ तो मुझे अपनी हर चीज़ भारी और बोझ लदी जान पड़ती है- अपने कपड़े, अपनी देह की माँस-मज्जा, अपनी आत्मा भी और सबसे ज़्यादा अपना अब तक का सब लिखा हुआ।
इन दिनों में निर्मलजी शिमला में रह रहे हैं। वे शिमला की यशपाल सृजनपीठ में अतिथि लेखक हैं। कुछ दिनों के बाद उन्हें जर्मनी में व्याख्यान देने है। वे अपना पेपर तैयार कर रहे हैं। अपने व्याख्यान के लिए भारत और यूरोप को लेकर काफ़ी कुछ पढ़ने में जुटे हुए हैं।
मैं शिमला में उनसे शाम के वक्त ही कुछ घण्टों के लिए मुलाकात कर पाता हूँ। हम दोनों मॉल रोड पर, रिज और गिरजाघर के क़रीब चहलकदमी करते रहते हैं। बीच-बीच में किसी बेंच पर बैठकर बातचीत करते हैं। वे कभी रेलिंग के क़रीब खड़े हुए, अपने बचपन की कुछ जगहों को दूर से बताते हैं। कभी जाखू की पहाड़ी, कभी अपना स्कूल, कभी वह बैंक जहाँ उनके चाचा काम किया करते थे।
मैं दिन में उनके सुझाये गये इलाकों में जाता हूँ। एक दुपहर में उस क्लब की इमारत भी देखने गया था, जहाँ कभी अमृता शेरगिल डांस सीखने के लिए जाया करती थी। कभी अपनी होटल के कमरे में टॉमस मान के उपन्यास ‘द मेजिक माऊण्टेन’ को पढ़ता रहता हूँ। मुझे यह उपन्यास मेरे तीसवें जन्मदिन पर निर्मलजी ने डाक से भिजवाया था।
शिमला के इन दिनों में हम लोग टॉमस मान और उनकी कृतियों को भी याद करते रहते हैं। हमारे बीच में यह जानकारी भी उतरती है कि 1927 में इस उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद के प्रकाशन के आसपास ही जवाहरलाल नेहरू ने इस उपन्यास को जेल में पढ़ा था, ऐसा जिक्र नेहरूजी की चिट्ठी में आता है।
निर्मलजी टॉमस मान के निर्वासन के बारे में, नाज़ियों के उनके साथ किये गये जुल्मों के बारे में भी बताते हैं। मुझे याद आता है कि किस तरह मशहूर कंडक्टर फुर्त वेंगलर ने उन्हें थियेटर के पीछे के रास्ते से नाज़ियों से बचाने के लिए बाहर निकाला था।
मान के लेखन को लेकर निर्मलजी से यह भी सुनता हूँ कि उन्होंने अपने समय के, अपने इतिहास के सवालों को गहराई और गम्भीरता से जिया था। उनको टॉमस मान का लेखन गहरी मानवीयता लिया हुआ, कालातीत लगता आया था। वे कहते भी आये थे कि टॉमस मान के लेखन की जड़े हमेशा से ही यथार्थ में धंसी रही और वे आजीवन खुद से, अपने समाज और देश से सवाल करते आये थे।
शिमला की शामों की उन घड़ियों में, उनका बीच-बीच में अपने बचपन को याद किया जाना याद आता है और इसके साथ-साथ न जाने किस लेखक का स्मृति के बारे में यह कहा जाना कि-
‘ह्यूमन मेमोरी इज़ ए पैराडाइज़ फ्राम विच वी केनॉट बी एक्सपैल्ड’
निर्मलजी के जाने के बाद, बीच-बीच में जब कभी टॉमस मान का कुछ भी पढ़ना शुरू हुआ है, तब-तब उनके साथ शिमला में बीते हुए अपने सर्दियों के चार-पाँच दिनों की बराबर याद आती गयी थी। वे टॉमस मान की कृतियों में आते हुए आवेग और करूणा को लेकर कहते, वे बताते कि मान के लिए लिखना किसी ईश्वरीय, पवित्र कर्म की तरह रहा होगा। उनसे यह भी सुनता कि मान के लेखन की सघनता, तल्लीनता और भावात्मकता ने उन्हें हमेशा ही छुआ है।
अब जब टॉमस मान की कहानियों को पढ़ता हूँ, निर्मलजी की उनके बारे में कही गयी इस बात को थोड़ा-सा ज़्यादा समझ पाता हूँ कि टॉमस मान ने मानवीय आत्मीयताओं को पकड़ने, मानवीय मन की आन्तरिकताओं को जानने-पहचानने और लेखकीय प्रवीणता लिए हुए व्यक्त करने की कितनी ज़्यादा, कितनी गहरी कोशिशें की थी।
टॉमस मान के उपन्यासों को लेकर निर्मलजी का कहा गया यह भी याद आता है कि ऐसा सब कुछ टॉमस मान ने लिखने के लिए ज़रूरी गीतिमयता को बनाते-बचाते हुए किया था। घिसे-पिटे मुहावरों, अलंकारों से दूरी बनाये हुए किया था। टॉमस मान की ही तरह निर्मलजी से ही ऐसे कुछ और देशी-विदेशी लेखकों, चिन्तकों और कलाकारों के बारे में जानता आया था। जिनके पास अपना एक विजन रहा था। अपनी गहरी समझ, अन्तर्दृष्टि और आत्मचेतना रहती आयी थी।
शिमला की निर्मलजी के साथ की उन चहलकदमियों की इंडियन कॉफ़ी हाउस की शामों की वहाँ के उनके आवास में बीते हुए क्षणों की कुछ धुँधली-सी, अस्पष्ट-सी यादें आती है। आहिस्ता-आहिस्ता और अजीब-सा अमूर्तन लिए हुए आती है और न जाने किस लेखक की कही गयी इन पंक्तियों का भी खयाल आता है-
‘द थ्रेड ऑफ़ मेमोरी इज़ नॉट फ्लो लाइक ए रिवर इट स्पूल्स लाइक ए रील एण्ड फीनिशेस सम डे।’
उनके करोलबाग के आवास के पिछले हिस्से में एक सार्वजनिक जगह को घेरे हुए फैंस के क़रीब, एक आदमी इस्त्री करने का काम किया करता था। कभी-कभार मैं अपने कपड़ों को इस्त्री करवाने उस जगह पर जाता। मेरे साथ निर्मलजी भी रहते। यह सब उनसे पहली मुलाकात के कुछ ही महिनों के बाद की बात है। मैं विदिशा से बैंक का अपना काम निपटाकर, शाम की ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल जाया करता था।
सुबह का वक़्त था। हम दोनों उसी जगह के क़रीब (शायद वह पब्लिक पार्क रहा होगा) एक बेंच पर बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। मैं उनकी कहानी ‘ज़िन्दगी यहाँ और वहाँ’ को किश्तों में आयी धर्मयुग के पुराने अंकों में पढ़ चुका था। वह मेरे थोड़ा सलीके से पढ़ने और कहानी लिखने की कोशिश किये जाने के शुरुआती दिन थे। तब तक हिन्दी कथाकारों में मुक्तिबोध, रेणु, मोहन राकेश, कृष्णा सोबती और निर्मली वर्मा की ही कहानियों में किसी की ज़्यादा, किसी की कम कहानियाँ पढ़ी थी।
‘ज़िन्दगी यहाँ और वहाँ’ अपनी विषयवस्तु, प्रसंगों और संरचना के कारण अत्यन्त असामान्य, अपना पर्सनल सिग्नेचर लिए हुए कहानी लगी थी। अपनी बाइस-तेइस की उम्र में प्रेम के ट्रेजिक महत्त्व को लेकर मैंने ऐसी एक भी कहानी हिन्दी में नहीं पढ़ी थी। उस लम्बी कहानी में प्रेम की कसक और पीड़ा के सन्दर्भ में मैं निर्मलजी को अपनी कच्ची, अधपकी प्रतिक्रियाएँ बता रहा था।
इतना भर याद आता है कि अपनी टूटती-बिखरती और काँपती आवाज़ में मैंने उस कहानी को पढ़कर महसूस हुए प्रेम के दुख को लेकर, अतृप्त प्रेम के शोक, व्यथा और अनकहे रह जाने के बारे में कहते-कहते प्रेम, रोमांस आदि पर कुछ सतही-सा, आधा-अधूरा और बनावटी कहा होगा।
वे अत्यन्त धीरता के साथ मुझे सुन रहे थे। उस समय में, उस उम्र में कहने और निर्मलजी के इतने गम्भीरता से सुनने की यादें, मुझे गहरी शर्म और संकोच में डुबा देती है। वे दूसरों को कितने ध्यान से सुना करते थे। खुद कितना कम लेकिन कितना ज़रूरी और महत्त्वपूर्ण कहने की पूरी कोशिशें किया करते थे। वे अपनी बात को आहिस्ता-आहिस्ता, तार्किकता, स्पष्टता और विवेकशीलता लिये हुए गढ़ने का प्रयत्न करते हुए जान पड़ते।
अब यह बात सालती है कि उनसे कम-से-कम दूसरों को अच्छी तरह, गम्भीरता से सुनना ही सीख लेता। उनका दूसरों को इतनी तल्लीनता, ज़िम्मेवारी और समझ लिये सुनना भी रहा होगा कि उनके फ़िक्शन में उतरती मानवीय आवाज़ें, प्रकृति की अपनी आवाज़ें, इतनी सच्ची और सटीक नज़र आती हैं। उनकी कितनी ही रचनाओं में हम पेड़ों और पहाड़ों को, नदियों और चट्टानों को पत्थर और पानी को कहते हुए सुन पाते हैं।
शायद ‘ज़िन्दगी यहाँ और वहाँ’ को लेकर हुई हमारी बातचीत की सुबह ही उनकी करोलबाग की बरसाती में आये हुए सर्वेश्वरदयाल सक्सेना को उनसे बातचीत करते हुए सुना था। उनका मुझ पर ऐसा गहरा अनुराग, ऐसी उज्ज्वल किस्म की कृपा ही रही कि मैं उनके साथ हिन्दी के कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथाकारों, कवियों और कलाकारों के अनौपचारिक संवादों का कभी-कभार गवाह भी बन सका था। अपनी उम्र के पच्चीस-छब्बीस बरसों के भीतर ही निर्मलजी के साथ इन रचनाकारों, कलाकारों के संवादों ने मुझे बहुत कुछ सीखाया और समझाया था।
आज अलग-अलग जगहों पर, निर्मलजी से संवादरत कुछ अब जीवित नहीं रहे। कुछ अब भी जीवित लेखकों-कलाकारों की यादें, हिन्दी समाज के एक समृद्ध बौद्धिक दौर की यादें दिला जाती हैं।
दयाकृष्ण, शामलाल, जगदीश स्वामीनाथन, रामकुमार, कमलेश, श्रीकान्त वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, कृष्ण बलदेव वैद, कृष्णा सोबती, अशोक वाजपेयी, रमेशचन्द्र शाह, रामचन्द्र गाँधी और अनन्त मूर्ति के साथ के उनके संवादों से मिले आनन्द आलोक और आश्चर्य को याद करता हूँ और सहज ही अपने उन बरसों के जीवन को लेकर अभिभूत हो जाता हूँ। आत्ममुग्धता से भर जाता हूँ। अपनी नगण्यता के गहरे अहसास से भले ही कुछ क्षणों के लिए लेकिन बाहर ज़रूर निकलता हूँ।
शायद वह बिहार प्रेस विधेयक के विरोध में बुद्धिजीवियों की बैठक रही होगी, जिसमें निर्मलजी ने भी अपनी असहमति दर्ज की थी। मध्यप्रदेश के एक दैनिक अखबार की ख़बर के शीर्षक में ही निर्मलजी का यह कथन छपा था- ‘अपनी शक्ल सुधारो, आइना मत तोड़ो’ ये उनको पढ़ने-जानने के एकदम शुरुआती बरस रहे थे। बाद में अपनी ज़िन्दगी के आखिरी-आखिरी बरसों तक उन्हें एक सार्वजनिक बुद्धिजीवी की तरह, अपने समय और सभ्यता के, अपने समाज और संस्कृति के, अपनी भाषा और साहित्य के ज्वलन्त सवालों और समस्याओं पर, साहस, स्पष्टता और स्वतन्त्रता लिए हुए पढ़ता और सुनता रहा था।
वे कहते भी आये थे कि भारतीय समाज में एक लेखक को कुछ ज़्यादा लेखक होना पड़ता है। उनके अनुसार भारतीय लेखक की ज़िम्मेवारियाँ भी कुछ ज़्यादा बनती थी, कुछ अलग तरह की रहती थीं।
कई बार अपने सच की खातिर, मानवीय स्वतन्त्रता पर अपने विश्वास और निष्ठा के लिए, वे तरह-तरह के आरोपों से घिरे रहे। दुखी भी हुए और अकेले भी लेकिन मैंने कभी भी उनको न अपने लिखने में और न अपने जीने में समझौता करते हुए, झूठ और चालाकी से अपना काम निकालते हुए देखा था। अपने जाने-पहचाने सच के लिए उनका निरन्तर बना रहा आग्रह, एक किस्म का उनका अपना सत्याग्रह, उनकी मृत्यु के लगभग उन्नीस बरसों के बाद भी, मेरे मन में उनके लिए गहरा आदर जगाता रहा है।
वह 1989 की गर्मियों की कोई शाम रही होगी। निर्मलजी एक महिने के लिए ‘आश्रम’ के अन्तर्गत भोपाल आये हुए थे। इन दिनों के आसपास ही उनके साठ बरस के हो जाने पर उन पर केन्द्रित ‘पूर्वग्रह’ के अंक को आना था। उनका उपन्यास ‘रात का रिपोर्टर’ लगभग पूरा हो चुका था। अप्रैल की आखिरी तारीख़ को अपने इस उपन्यास का एक बड़ा अंश उन्होंने भारत भवन के अन्तरंग में श्रोताओं के बीच पढ़ा था।
अच्छी तरह याद नहीं है कि क्या इसी शाम के आसपास की वह भी शाम रही थी, जब अशोकजी के भोपाल के 74 बंगलें के परिसर में मैं निर्मलजी, स्वामीजी, अशोकजी, वैद साहब, मदनजी और उदयन के साथ बैठा रहा था। उन लोगों की बातचीत में नागरिकता बोध, नागरिकता के विस्तार में बौद्धिक लोगों की भूमिका आदि विषय आते रहे थे। भारत में आपातकाल में लेखकों की भूमिका के सन्दर्भ में किसी ने अमेरिकी कवि एज़रा पाउण्ड की मुसालिनी से सहानुभूति का भी ज़िक्र किया था।
इतना ज़रूर याद है कि उस दिन सभी लोगों की बातों में लेखक-कलाकार की दृष्टियों से समाज, राजनीति और समाज व्यवस्था के अर्न्तविरोधों, विरोधाभासों को देखा-समझा जा सकता था। वहाँ भारतीय यथार्थ को यथार्थ की सतह के नीचे तक उतरकर देखने की चेष्टाएँ थीं। हमारे कुछ महत्त्वपूर्ण दिमागों के चिन्तन-मनन का गवाह बने रहना, उस शाम की मेरी एक उपलब्धि रही थी।
इस दिन से ही जुड़ी हुई, भोपाल के सर्किट हाउस की एक दुपहर याद आती है। अशोकजी के मकान में हुई बैठक के अपने तर्कों का विस्तार करते हुए निर्मलजी सभ्यता, विवेक और ज्ञान के खण्डहरों के बीच खड़े हुए बौद्धिक अन्तःकरण, इतिहास से मिली हुई सीखों, छलनाओं और दृष्टियों पर बता रहे थे। यह उनके सोचने-समझने का उनका जाना-पहचाना इलाका था। इन सब पर वे अपने विचारों और तनावों को अपने निबन्धों में व्यक्त करते आये थे।
सर्किट हाउस की खिड़की से ढलती दुपहर की धूप उतर रही थी। वहीं से बरसों पुराना, विशालकाय पेड़ नज़र आ रहा था। उन्होंने आपातकाल के दिनों की अपनी बेचैनियों के सन्दर्भ में यह भी कहा था कि अगर मैं बुराइयों के स्त्रोतों, स्वभावों को अपनी निगाहों से देखता नहीं हूँ, तब निश्चित रूप से अपनी ज़िन्दगी को, अपनी ज़िन्दगी के सच को देख ही नहीं सकूँगा। तब मुझे अपने ही सच को पाने के लिए और ज़्यादा भटकना पड़ेगा।
वे कह रहे थे कि लेखकों को अपने शब्दों को गहरी ज़िम्मेदारी के साथ चुनना और कहना चाहिए। उस दुपहर में उन्होंने गाँधीजी की सत्य पर अटूट आस्था का जिक्र करते हुए यह भी कहा था- ‘मेरी उन लोगों में दिलचस्पी बढ़ती ही गयी जो खुद को बदलने की अपनी कोशिशों को गहराइयाँ, निरन्तरता देते आये थे।’
आत्म-सुधार और आत्मावलोकन के इन मानवीय तत्वों का होना, उनके अनुसार हमारे सनकी उपभोक्तावादी दौर में और ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। एक-दूसरे की अच्छी तरह से, सच्चे ढंग से देखभाल किये जाने की हमारी मानवीय क्षमता का पतन उन्हें चिन्ताएँ देता रहा था। हमारे समाज में भाईचारे की स्थिति का जिक्र करते-करते उन्होंने बाइबिल में केन द्वारा अपने ही भाई एबेल की हत्या करने, पिता के पूछने पर उसके रखवाले न होने की बात कहानी कहने भी सुनायी थी। अपने इसी प्रवास में उन्हें अपने कुछ दिनों को पचमढ़ी में बिताना था। उनसे मुलाकात के लिए पचमढ़ी भी गया था। वहाँ वे हॉलीडे होम के एक घर में रुके हुए थे। पचमढ़ी की सेंट्रल स्कूल की लाइब्रेरी से इश्यु करवायी गयी अमृत-लाल नागर की कोई कृति पढ़ते रहे थे। पचमढ़ी में उनके साथ एक ही शाम बिता पाया था। उनको अचानक भोपाल लौटना पड़ा था। भूल से उनके लन्दन प्रवास के प्रीपोन होने का समाचार आ गया था। बाद में वे निर्धारित वक्त में लन्दन-प्रवास पर निकले थे।
मैं सम्भवतः अपनी इस बात को दुहरा रहा हूँ कि मैंने विचारों और भावनाओं के आत्मदर्शी आयामों को उनके लिखे गये में जितना पाया था, उतना ही कभी-कभार सम्भव हो पाते उनसे संवादों में भी। वे अपनी बातों को ज़िम्मेवारी, गम्भीरता और सहजता लिए हुए कहने की निरन्तर कोशिशों में जुटे हुए नज़र आते थे।
वे उन गर्मियों में पचमढ़ी के हॉलीडे होम में रुके हुए थे। आहिस्ता-आहिस्ता रात का अन्धेरा उनके कमरे में आने लगा था। उनको धीरे-धीरे अन्धेरा का उतरना, रात का शुरू होना भाता रहा था। मैं उनके लिखे गये में भी, मौसम के बदलावों के लिए, प्रकाश के परिवर्तन के प्रति उनकी संवेदना और समझ को देखता आया था। याद करता हूँ तब उनकी डायरियों, उनकी चिट्ठियों में भी ऋतुओं के बदलने, आने और जाने के कितने सारे ज़िक्रों को पढ़ा जा सकता है।
मौसमों के लिए उनकी चाहना और चेतना भी रही होगी कि वे सितम्बर में अपनी किसी नयी कहानी को शुरू करने की बात कहते, मार्च में उनको दिल्ली में बने रहना अच्छा लगता, मई और जून के महिने, उनके लिए विक्टोरियन युग के, उन्नीसवीं सदी के रूसी के उपन्यासों को पढ़ने के दिन बन जाया करते थे।
मुझे लगता है कि मौसम के शुरू होने की घड़ियाँ, उनके अपने किसी संकल्प की भी घड़ियाँ हो जाया करती थीं। वे अपने किसी उपन्यास या कहानी के पात्र की तरह ही अपने आप से यह सवाल करते हुए नज़र आते-
‘मौसम बदल रहा है, क्या मेरे अपने जीवन में भी कोई बदलाव आयेगा?’
सुबह की धूप का पेड़ों पर उतरना, आसमान को साफ़ होना, शाम का ढलते जाना, रात का चढ़ना, दुपहर का शुरू होना, जैसी हर प्राकृतिक प्रक्रिया को वे अपने लिखे गये में दर्ज करते रहे थे। सोचता हूँ कि वे भी टॉलस्टाय की इस बात से शत-प्रतिशत सहमति जताते रहे होंगे कि प्रकृति की अपनी नज़र में न कुछ सही होता है और न ही ग़लत। प्रकृति अच्छाई और बुराई के बीच में कोई भेद नहीं करती है। नैतिक-अनैतिक, अच्छा-बुरा, सच्चा-झूठा यह सब मानवीय धारणाएँ हैं, जिनसे प्रकृति अपनी दूरियाँ बनाये रखती हैं।
निर्मलजी ने अपने किसी निबन्ध में यह कहा भी है कि हम व्यक्ति को सर्वोपरि समझते रहते हैं लेकिन प्रकृति के लिए व्यक्ति का रत्तीभर भी महत्त्व नहीं रहता है। उनके लिए ऐसा होना, जीवन का एक बड़ा रहस्य रहा होगा।
उन्नीस सौ नब्बे के आसपास की करोलबाग की छत की एक और रात की शुरुआत को याद करता हूँ। सलमान रुश्दी की किताब के भारत में प्रतिबन्धित होने का प्रसंग है। निर्मलजी कह रहे है कि उनको यह बात चिन्ताएँ देती है कि इधर के लेखकों, बुद्धिजीवियों के मन में अपने समाज, संस्कृति और धर्म को लेकर सवालों की इतनी ज़्यादा और गहरी अनुपस्थिति, उदासिनता क्यों बनी हुई है?
वे यह भी बता रहे हैं कि आज़ादी के पहले और आसपास भी एक दौर रहा जब गीता पर टीकाएँ लिखी जाती रही थीं। तिलक, गाँधी और विनोबा की गीता पर टीकाएँ प्रकाशित होती रहीं लेकिन इधर इस तरह के संवादों-सवालों का सिलसिला रुक-सा गया है। दूसरे दशों में काफ़्का, वाल्टर बेन्यामिन, सॉल बेलो और ग्राह्म ग्रीन जैसे लेखकों ने अपने धर्म पर लगातार सवाल किया हैं और ऐसा किया भी जाना चाहिए। इस तरह वे हमारे देश में धर्म-निरपेक्षता पर होती रही बहसों और बातचीतों की सीमाओं को भी व्यक्त करते रहे थे।
किसी सवाल से बातों का प्रसंग बदला था। वे फ्रॉयड, वाल्टर बेन्यामिन द्वारा अपनी गम्भीर बीमारी के दिनों में भी अपना-अपना महत्त्वपूर्ण लेखन किये जाने का ज़िक्र करने लगे थे। उनका यह कहना था कि इस पृथ्वी पर मनुष्य का होना ही ईविल नज़र आता है। ‘मनुष्य के अलावा समूची सृष्टि सौन्दर्य और सन्तुलन के क़रीब दिखायी देती है।’ इस बात का सन्दर्भ डेविड एटेनबरो की पुस्तक ‘लाईफ़ ऑन अर्थ’ रही होगी, जिसे उन दिनों वे पढ़ रहे थे। उस किताब के अलावा, बरसाती में उनके बिस्तर के क़रीब चौकी पर मार्को पोलो के संस्मरणों की किताब भी रखी थी। वे एक ही दिन के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग किताब को पढ़ने के अभ्यस्त रहते आये थे। यह ज़रूर रहता कि अपनी बातों में, वे अपनी उन दिनों पढ़ी जा रही किसी किताब, देखी गयी किसी फ़िल्म का ज़िक्र कर दिया करते थे। इन्हीं दिनों में उन्होंने पीटर ब्रुक के निबन्धों की किताब और जोसेफ ब्राडस्की की से की गयी बातचीत को भी पढ़ा था।
उसी रात में उनसे ब्रॉडस्की के जिस कथन को अंग्रेज़ी में सुना था, उसका कामचलाऊ-सा अनुवाद यहाँ रख रहा हूँ। ‘हम किसी परिन्दे के गान का स्त्रोत जानने की ख़ातिर उसकी देह की चीर-फाड़ नहीं कर सकते है।’ अपनी मुलाकातों में, उनसे हुई बातों के बिन्दुओं को ज़रूर एक जगह नोट कर लिया करता था कि कभी उन सब बातों को अच्छी तरह से, सिलसिलेवार ढंग से अपनी डायरी में पक्का करूँगा, लेकिन ज़्यादातर ऐसे बिन्दु अपने कच्चे रूप में ही रह जाया करते थे।
उनके पास हमेशा ही अपना कोई आधा-अधूरा काम बाकी रहता और उस काम को पूरा करने का संकल्प, तनाव और चिन्ता भी। वे निरन्तर किसी को भी अपना समय दे ही नहीं पाते थे। अपने प्रवासों में, बीच-बीच में ही उनसे घण्टे-दो घण्टे मिलना होता और बीच-बीच में वे अपने आधे-अधूरे कामों को निपटाते रहते। इन कामों में देश-विदेश में दिये जाने वाले उनके व्याख्यान होते, किसी पत्रिका के लिए उनके निबन्ध या अपनी कोई अधूरी कहानी या उपन्यास। उनको पत्र-पत्रिकाओं के आग्रहों पर भी काफ़ी कुछ लिखना पड़ता था। उनसे अपनी अनौपचारिक बातों के सैकड़ों क्षणों को जब याद करता हूँ तब यह भी याद आता है कि उनकी किसी भी बात में आडम्बर, दिखावट नज़र नहीं आती थी। उन बातों में उनके ब्यूटिफु़ल माइण्ड का सोचने-समझने, चिन्तन-मनन का अपना-सा, असामान्य-सा ढंग हुआ करता था। उनका धीरे-धीरे, धीमी आवाज़ में, अपनी किसी बात को गढ़ना, अपने पूर्वग्रहों के आसपास भटकना, अपने संशयों और सवालों से लैस होते जाना।
अब लगता है कि यह मेरे लिए कितना अर्थपूर्ण, महत्त्वपूर्ण हो सकता था कि मैं उनसे सुनी गयी बातों को उसी समय के बाद अपनी नोटबुक में उतार लेता। उन बातों को बाद में अपनी समग्रता में समझने की कोशिशें करता। उन बातों का विस्तार और विकास, उनके लिखे हुए में खोजा करता। पर यह सब कभी भी नहीं हो सका। मेरे साथ समझ की कमी रही। मेरा गहरा आलस्य भी। कभी उनसे अपने सवालों के साथ औपचारिक रूप से बातचीत करने का आग्रह भी किया था लेकिन उन्होंने इन्कार भी किया और यह कहकर मुझ पर थोड़ा-सा नाराज़ भी हुए कि मुझे उनके लिखे गये में से ही मेरी जिज्ञासाओं का समाधान पाने की मेहनत करना चाहिए। शार्टकट से बचना चाहिए।
कभी-कभार यह भी होता आया था। मैं उनसे किसी किताब को अपने लिए मंगवाने, उनसे ली गयी किसी पुस्तक को लौटाने के लिए, बैंक के अपने परिचित किसी व्यक्ति को दिल्ली में उनके घर जाने के लिए कहा करता था। उस व्यक्ति का साहित्य और भाषा के संसार से दूर-दूर का रिश्ता नहीं रहता था।
वह लौटता और निर्मलजी के आतिथ्य, उनकी संवेदनशीलता सहृदयता और जिज्ञासा की प्रशंसा करने लगता। वह बताता कि निर्मलजी ने उनसे बैंक के बारे में, उनके परिवार और परिवेश के बारे में कितना कुछ जानना चाहा था। वे कितने ध्यान से आमला के मौसम, लोगों और जंगलों के बारे में उनसे सुनते रहे थे।
अल्बर्ट आइंस्टाइन ने शायद इसको ही पवित्र जिज्ञासा कहा होगा। निर्मलजी ने अपनी बच्चों जैसी पवित्र जिज्ञासा को कभी नहीं छोड़ा था। उनसे मेरी आखिरी मुलाकातें 2005 के अगस्त के तीसरे सप्ताह में हुई थी। फिर अक्टूबर के आखिरी दिनों में वे नहीं रहे। पर अगस्त की उन मुलाकातों में गम्भीर रूप से बीमार रहने के बीच और बावजूद, वे हमेशा की तरह मेरी देखी गयी फ़िल्मों, मेरी पढ़ी गयी किताबों को जानने की दिलचस्पी बनाये हुए थे।
उसी महिने नया ज्ञानोदय में छपी उनकी अन्तिम कहानी ‘अब कुछ नहीं’ छपी थी। उस कहानी को लेकर उनके अपने संशयों को बता रहे थे। मुझसे जानना चाह रहे थे कि क्या मैंने इस कहानी में अव्यक्त, छिपी हुई समलैंगिक कामुकता को महसूस किया है?
उस रात उन्होंने दूसरे महायुद्ध के परिवेश में युवा प्रेम पर केन्द्रित एक पोलिश फ़िल्म का यह कहकर ज़िक्र किया था कि समूचा संसार अतिसंवेदनशील, नाजुक और कमज़ोर लोगों के प्रति ही अपनी क्रूरता, अपने ओछेपन को जताता है।
एक बार उनका व्याख्यान समाप्त हो जाने के बाद वहाँ शामिल हुए एक श्रोता ने बेतुका सवाल किया था। उन्होंने धीरता-गम्भीरता से उसका भी उत्तर दिया था। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा था कि हमें अपने पाठकों, श्रोताओं के प्रति कृतज्ञ बने रहने की कोशिश करना चाहिए। आखिर इतनी सारी गतिविधियों को छोड़कर एक पाठक, एक श्रोता साहित्य और भाषा के पास आने का विकल्प चुनता है। उनके लिए यह कोई छोटी बात नहीं थी।
उनके पास पाठकों की ढेरों चिट्ठियाँ आया करती थीं। पर वे धीरे-धीरे, भले ही पोस्टकार्ड में उनके जवाब ज़रूर दिया करते थे। मनुष्य में कृतज्ञता पालन का होना, उनके लिए ज़रूरी बात बनी रही थी। वे छोटी-छोटी बातों के लिए भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना नहीं भूलते थे। उन्होंने देश-विदेश से मुझे कितने ही पिक्चर पोस्टकार्ड भेजे होंगे लेकिन कभी मैं एक भी तस्वीर, एकाध पिक्चर पोस्टकार्ड उनके लिए पोस्ट करता और वे न जाने कितनी बार शुक्रिया अदा किया करते थे। मैंने एक बार शान्ति निकेतन से उनके लिए रबीन्द्रनाथ ठाकुर का एक विरल-सा चित्र भिजवाया था। इसके लिए वे रामू गाँधी के सामने मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते रहे थे कि मैं गहरी शर्म में डूबता गया था।
यह उनका स्वभाव बना रहा। वे औपचारिकता, आदत के वशीभूत होकर नहीं, आवेग, विनम्रता लिए हुए कृतज्ञता व्यक्त किया करते थे। मैं उनकी इस मानवीयता, मार्मिकता को महसूस करता रहा था लेकिन यह भी सोचता रहा था कि इन सब बातों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, परिभाषित नहीं किया जा सकता है। मैंने न जाने कितनी बार उनके व्यक्तित्व के भीतर रचे-बसे उस बड़प्पन को महसूस किया था जो उतनी ही बार, बार-बार मुझे अपने छोटेपन की याद दिलाता रहा था।
लगभग पच्चीस बरसों तक मुझे उनका संग साथ मिलता रहा। मुझे न सिर्फ़ उनकी असाधारण कृतियों को पढ़ लेने का सौभाग्य मिला बल्कि उनसे मिलने-जुलने, बतियाने का सौभाग्य भी। वे अपनी अत्यन्त व्यस्त, मुश्किल घड़ियों में मुझे अपना समय देते रहे। मुझे निरन्तर चिट्ठियाँ लिखते रहे थे। उनकी कृतियों का होना, उनका मेरे जीवन में होना, मेरा अब तक का बड़ा सहारा रहता आया है। मुझे नहीं पता था कि उनके जाने के एकदम बाद मेरी अपनी साहित्यिक दुनिया इतनी ज़्यादा उजड़ी हुई, इतनी ज़्यादा टूटी-बिखरी होंगी। उनके जाने के बाद के कुछ बरसों तक, मैंने इस उजाड़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया था। फिर धीरे-धीरे उनकी कृतियों को पढ़ते-पढ़ते ही मैं अपने उजाड़ के अहसासों से बाहर आया था।
अब लगता है कि क्या यह कम बड़ी बात है कि वे अपने पीछे अपनी इतनी सारी ग्रेसफुल कृतियों को हम पाठकों के लिए छोड़ गये हैं। मुझे उनकी रचनाओं को पढ़ते रहना, भले ही कुछ कम, लेकिन उनके क़रीब होना, उनको सुनते रहना, उनकी उजली ममतामयी और उत्सुक निगाहों की तरफ देखते रहना ही जान पड़ता है।