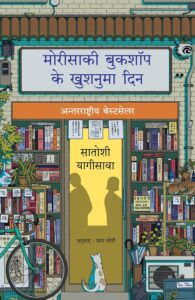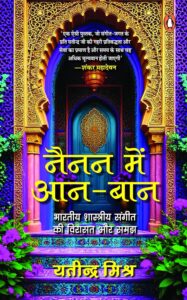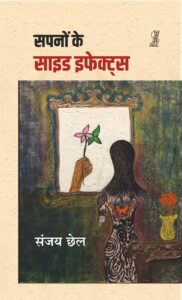ललित निबन्ध की विधा इन दिनों सोशल मीडिया की टिप्पणियों और समाचार-पत्रों के प्रकाशित आलेखों में क्षणिक रूप से उपस्थित होकर साहित्य-परिदृश्य से शीघ्र ही ओझल हो जाती है। हिन्दी के ललित निबन्धों की वैभवशाली परम्परा में भारतीय सौन्दर्यबोध से ओत-प्रोत ‘मन मति रंक’ एक प्रशंसनीय कड़ी है जो समकाल में भारतबोध को सहेज लेती है। इस संग्रह में भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर दृष्टिपात किया गया है, जिसे संगीतकर्मी, फ़िल्मकर्मी, अभिनेता, गायक और साहित्यकार जैसे कलाविदों के कर्मों के प्रतिफलन में समझा जा सकता है। यह एक सजग लेखक का साहित्य-मन्दिर में प्रथम पुष्प-अर्पण है। निश्चय ही पाठक इसके सौरभ से पूर्णता-बोध की ओर उन्मुख होंगे।
समीक्षा : एक सहज सवाल बहुधा मन मेँ आता है कि इन दिनोँ इन्फ्लुएँसरोँ, कथाकारोँ, कवियोँ, विद्वानोँ की भारी भीड़ और थोक मेँ मिलती साहित्य सम्बन्धित अनुशंसा मेँ असली-नकली, उपयोगी-अनुपयोगी, पठनीय-छद्म प्रचारित का भेद कैसे किया जाय? प्रमाण-चिन्तन की दृष्टि से इसका सबसे आसान तरीका ‘आगम प्रमाण’ है, अँगरेजी मेँ जिसे हम ‘टेस्टिमोनी’ कहते हैँ। आगम प्रमाण की शर्तेँ बड़ी आसान-सी होती हैँ, अव्यवहित प्रसिद्धि और उस पर संगत-सम्यक आस्था। ‘टेस्टिमोनी’ की यह व्यवस्था अपने स्वरूप मेँ जितनी सहज है, उसकी सुगमता उतनी ही कठिन है।
कई बार ऐसा होता है कि जो प्रारम्भ मेँ आशा की किरण दिखाता है, वही कालान्तर मेँ फीका पड़ जाता है। इसका एक उदाहरण ‘ए॰ आर॰ रहमान’ के हिन्दी फिल्म संगीत की दुनिया मेँ पदार्पण मेँ मिलता है। शुरुआत के दस सालोँ के बाद न भूतो न भविष्यति की भविष्यवाणी धूमिल पड़ गयी। आज आलम यह है कि रहमान को अपने पुराने गीतोँ को रिमिक्स करके काम चलाना पड़ रहा है। इसकी तुलना एस॰डी॰बर्मन या शङ्कर जयकिशन के बीस-पच्चीस साल की लम्बी कार्यावधि से करनी चाहिये। अतः संगीतकार प्यारेलाल का कहना कि ए॰ आर॰ रहमान सर्वश्रेष्ठ नहीँ है, ठीक ही सिद्ध हुआ।
उपरोक्त तुलना की आवश्यकता इसलिये आ पड़ी क्योँकि हिन्दी साहित्य की जो अधोगति है, उसकी मीमांसा रचनात्मक प्रतिभा के स्फोट और प्रकाश से ही समझी जा सकती है। हमारे समय मेँ आगम-प्रमाण का भौण्डा स्वरूप भविष्य को लेकर बढ़-चढ़ कर किये गये दावोँ मेँ प्रकट होता है, जैसे कि फलाना कालजयी रचना है। पता चलता है कि कालजयी रचना को दो साल के काल के बाद कोई पूछता तक नहीँ है। हमारे हिन्दी समाज मेँ इन दिनोँ लेखक और कवि अपनी कृतियोँ से नहीँ बल्कि बदतमीजियोँ और कुण्ठाओँ के कारण जाने जाते हैँ। ऐसा नहीँ है कि हिन्दी मेँ अच्छी कहानियाँ नहीँ लिखी जाती या मोहक कविताओँ का अभाव है। किन्तु यह कठोर सत्य है कि हिन्दी मेँ प्रतिष्ठित प्रतिभा का घोर अभाव है। कुछ साहित्यिक कृतियाँ अच्छी लिखने के बाद उसी स्तर का नवीन लेखन कम ही प्रकट होता है। जो भी नाम आज प्रतिमान के रूप मेँ गिने जाते हैँ, उनके कार्योँ पर विहंगम दृष्टि डाली जाय तो एकरूपता, दुहराव और एक-जैसी बनावट की जड़ता स्पष्ट हो जाती है। यह ‘व्यक्तिगत शैली’ के नाम पर छुप नहीँ सकती। बहुधा लोग इस जड़ता को राजनैतिक प्रतिबद्धता का नाम देते हैँ। कुछ अपनी कुण्ठा के कारण सर्वनिन्दा मेँ प्रस्तुत होते हैँ, जैसे कि फलाने साहित्यकार का समस्त लेखन कूड़ा है। इस तरह की टिप्पणियाँ कभी विस्तार मेँ ना जाकर बेहद छिछली किस्म की व्यक्तिगत राय अधिक होती हैँ। वस्तुतः बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन जैसी सर्वशून्यता भी ऐसे टिप्पणीकारोँ के हाथोँ से बहुत दूर ही है। किसी से पूछा दिया जाय कि शून्यवाद क्या है तो वह दुखती रग पर हाथ पड़ने के कारण कराह कर गालियाँ देने लगेगा कि आप साहब बहुत बड़े पण्डित बनते हैँ। लेकिन यह स्वीकारोक्ति कभी सामने नहीँ आती कि जिन शब्दोँ का प्रयोग किया जा रहा है, वास्तविकता मेँ उससे महानुभावोँ का सम्यक परिचय नहीँ है।
अगर हिन्दी साहित्य का पिछले पचास साल का इतिहास लिखना पड़े तो यह कहना कि अमुक पत्रिका के वसन्त विशेषांक मेँ अमुक कहानी अच्छी थी, निहायत ही बचकानी हरकत है। यह बचकानी इसलिये है कि इसमेँ आपकी भूमिका एक पेशेवर चटोर की तरह है जो यह बताता है कि अमुक शहर के अमुक चौराहे पर गोलगप्पे अच्छे बने हैँ या अमुक रेस्तराँ का खाना अच्छा है। जबकि अपेक्षित यह है कि उत्कृष्टता सहजता के साथ उपलब्ध हो कर पुनः मूल्याकंन हेतु प्रस्तुत हों।
हम जिस समय मेँ रह रहे हैँ, उसमेँ यदि निम्न अपेक्षाएँ साहित्य की दशा-दिशा तय कर सकेँगी, तब उनकी सार्थकता पर बहुत सन्देह किया जा सकता है: —
- निरन्तर पत्र-पत्रिकाओँ आदि मेँ छपना
- सोशल मीडिया पर कहानी या कविताओँ का प्रकाशन
- सोशल मीडिया पर प्रशंसा या आलोचना
यदि उपरोक्त बिन्दुओँ मेँ प्रथम बिन्दु सही होता तो हिन्दी साहित्य के सभी प्रतिमान प्रतिभाएँ पत्रिकाओँ मेँ प्रकाशित होने के कारण ही याद की जातीँ। यद्यपि यह सत्य है कि भारतेन्दु हरिश्चन्द्र, बाबू देवकीनन्दन खत्री, प्रेमचन्द आदि सभी पत्र-पत्रिकाओँ मेँ निरन्तर छपते रहे। किन्तु मूल्यांकन हेतु उनकी उपस्थिति उनके निश्चित आकार मेँ उपलब्ध पुस्तक या नाटक या कहानी संग्रह से ही की जाती है। शेष दो बिन्दुएँ पहले बिन्दु का माध्यम और विधा भेद से विस्तार मात्र हैँ।
पत्र-पत्रिकाओँ और उनका आधुनिक विकृत स्वरूप ‘सोशल मीडिया’ पर उपस्थिति निश्चित रूप से साहित्य समाज मेँ अपनी उपस्थिति दर्ज कराती है, पर वह मूल्याकंन और विमर्श हेतु आने वाले समय के लिये सहजता से उपलब्ध नहीँ होती। यहाँ पर छपी हुयी किताब काम आती है जहाँ एकबार प्रकाशित होने के बाद बदलाव सम्भव नहीँ है। यदि किसी को गम्भीरता से कुछ साहित्य सम्बन्धी कर्म करना हो, चाहे वह उत्कृष्ट पढ़ना हो या सुन्दर लिखना, उसका अन्तिम आश्रय एक पुस्तक के अतिरिक्त कुछ नहीँ हो सकता। यही वह अन्तिम रूप है जो बिना लेखक के किसी व्यक्तिगत प्रभाव के कालान्तर मेँ सत्य निरीक्षण के लिये प्रस्तुत होगा।
समकालीन हिन्दी परिदृश्य मेँ छायी घोर कुण्ठा और निराशा का एक महती कारण योग्य आलोचकोँ का नितान्त अभाव है। दूसरी बात यह है कि रचनाकारोँ मेँ आलोचना सहने की न्यूनतम शक्ति भी नदारद है। आमतौर पर आलोचना समीक्षा से शुरू होती है। वह या तो स्तुतिपरक होती है या फतवापरक। फतवा देने वाले भूतपूर्व नौकरशाह, स्वघोषित आलोचक और कवि आदि बहुतेरे हैँ। इनमेँ अधिकतर का कार्य बेहद घटिया किस्म का होता है।
इसका कारण मुख्यतः यह है कि बहुत से पाठकोँ, लेखकोँ और कवियोँ ने स्तरीय आलोचना पढ़ी ही नहीँ होती। इतना ही नहीँ, हमेँ पता ही नहीँ कि आलोचक की न्यूनतम अहर्ता क्या होनी चाहिये? शास्त्रीय दृष्टि से आलोचक का दर्जा कवि से कुछ कम होता है। अगर हम आज बाणभट्ट को पढ़ पा रहे हैँ तो इसके लिये शंकरकृत ‘संकेत’ नामक टीका के कारण ही। मल्लिनाथ के बिना कालिदास और माघ को पढ़ना कठिन है। हिन्दी मेँ निराला की ‘राम की शक्तिपूजा’ के लिये हमेँ श्री वागीश शुक्ल की ‘छन्द-छन्द पर कुमकुम’ आवश्यक प्रतीत होती है।
एक आलोचक बहुपठित, बहुश्रुत भावयित्री प्रतिभा का धनी होता है। अच्छे आलोचक को कई-कई विधाओँ और कलाओँ का ज्ञान होना आवश्यक होता है। वैसे यह शर्त अच्छे कवि और लेखक के लिये भी है, हालाँकि हिन्दी मेँ ऐसे प्रतिमान कम हैँ। हमारी समझ ऐसी बना दी गयी है कि बहुधा आलोचना को केवल समीक्षा तक सीमित कर दिया जाता है। जैसा कि ‘आलोचना’ शब्द का अर्थ है, लोचन (नयन) को अधिक बढ़ा कर देखना। इस क्रम मेँ हरेक कवि (=क्रान्तदर्शी, पद्यकार-पोएट नहीँ) साधारणतया आलोचक होता ही है। उसकी पसन्द या नापसन्द बड़ी तीखी होती है।
बहुत उम्दा किस्म के प्रतिभाशाली कवि और लेखक अपनी आलोचना को स्पष्ट और शुष्क आलोचना कर्म की अपेक्षा अपनी दृष्टि को रचनात्मक तरीके से अभिव्यक्त करते हैँ। ऐसी मौलिक अन्तर्दृष्टि प्रेमचन्द, जैनेन्द्र, यशपाल, अज्ञेय आदि के लेखन मेँ प्रस्तुत है ही। उनका अभीष्ट समाज की आलोचना या विचारोँ की आलोचना ही रही है।
वहीँ कुछ ऐसे लेखक होते हैँ जो कथा और कविता के बजाय सीधे-सीधे निबन्ध मेँ अपनी बात कहते हैँ, किन्तु कुछ लालित्य लिये हुए। हिन्दी मेँ हजारीप्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र तथा कुबेरनाथ राय ने अपनी आलोचनात्मक दृष्टि को ललित निबन्धोँ मेँ निबद्ध किया। उनकी आलोचना सभ्यतागत विमर्श, नैतिक विमर्श और भाषा विमर्श की गहराइयाँ को छूती हैँ।
आलोचना का तीसरा दर्जा बौद्धिकता का आवरण ओढ़े हुए समय की शिनाख्त या समकालीन साहित्य की अन्तर्दृष्टियाँ निकालने मेँ है। इसे तीसरा दर्जा कहने का कारण यह है कि यह प्रतिमानोँ की स्थापना की कोशिश है या किसी को बनाने-बिगाड़ने का खेल। इनमेँ अधिकतर अपने कन्धे पर लंगड़ोँ को बिठाते हुए या काले चश्मेँ पहने अन्धोँ का हाथ पकड़ कर सहारा देते नजर आते हैँ।
श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय एक समर्थ आलोचक हैँ जिन्होँने अपनी लेखकीय यात्रा सोशल मीडिया की टिप्पणियोँ से प्रारम्भ की। मीरजापुर मेँ कार्यरत हिन्दी के प्राध्यापक श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय का लिखा ‘मन मति रंक’ नाम का ललित निबन्ध संग्रह प्रकाशित हुआ है। अम्बुज जी हिन्दी प्राध्यापकोँ की महती परम्परा का वाहन करने वाले गिने-चुने व्यक्तियोँ मेँ हैँ जो कि भक्तिकाल, रीतिकाल, छायावाद, स्वतन्त्रता के उपरान्त सभी प्रतिमानोँ पर अपनी पकड़ रखते हैँ। उनकी एक साँस मेँ तुलसी, जायसी, सूरदास, बिहारी, कबीर से लेकर प्रेमचन्द, प्रसाद, निराला, अज्ञेय, शमशेर आदि विराजमान हैँ। आमतौर पर ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है।
मेरा छोटा-सा दावा है कि हिन्दी के नब्बे प्रतिशत से अधिक प्राध्यापकोँ को न रस-सिद्धान्त का ठीक से पता है और न ही ध्वनि सिद्धान्त का। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यह मास्टर्स मेँ अनिवार्य विषय के रूप मेँ पढ़ाया जाता है। ऐसा इसलिये कहा जा रहा है कि इस पर किसी तरह का विमर्श न कोई करता है और सम्बन्धित प्रश्न पूछने पर लोग बिदक जाते हैँ। सवाल यह है कि जब हिन्दी के अधिकांश प्राध्यापकोँ को न ठीक से वर्णमाला आती है, न ही पारम्परिक सौन्दर्यशास्त्र, न ही भाषा-दर्शन, न ही भक्तिकाल, न ही रीतिकाल, तो उनसे आलोचना की क्या उम्मीद की जाय? दरअसल मौलिक समस्या यह होती है कि हिन्दी पढ़ने वालोँ की पहली जिम्मेदारी ‘आलोचना’ भाव को सम्यक और पुष्ट करने की है, जबकि समझा यह गया है कि हिन्दी पढ़ने-पढ़ाने वाला ‘कवि’ और ‘कथाकार’ बनेगा। यह विचित्र है क्योँकि जो पढ़ाया जा रहा है वह तो आपको आता नहीँ है, और जो नहीँ पढ़ाया जा रहा है उसमेँ आप तीरंदाज बनने का ख्वाब रखते हैँ।
मेरी सीमित दृष्टि मेँ मैँ यही जानता हूँ कि हिन्दी मेँ अगर कोई अम्बुज पाण्डेय के समकक्ष अच्छे स्तर का ललित निबन्ध लिख सकते हैँ तो वे हैँ — ‘सुशोभित शक्तावत’। कुछ और युवा निबन्धकार भी हैँ, किन्तु जब वे कम से कम एक दशक की लम्बी पारी मेँ काम करेँगे तब ही वे मूल्याङ्कन के योग्य होँगे। बहुविध असहमतियोँ के बावजूद, यह कहा जा सकता है कि समकालीन हिन्दी साहित्य से राजनैतिक विमर्श निकाल कर लेखन देखा जाय, तो यह केवल मरुस्थल है। अम्बुज कुमार पाण्डेय नखलिस्तान की तरह आशा का दीपक जलाते हैँ कि सबकुछ अन्धकारमय नहीँ है।
‘मन मति रंक’ एक मानक पुस्तक है कि आलोचक की दृष्टि फिल्म, संगीत, साहित्य, लोक मेँ त्योहार, चित्रकार, गायक पर किस तरह पड़ती है। कला साधकोँ का कला कर्म क्योँ महत्त्वपूर्ण है? उनमेँ क्या महत्त्वपूर्ण है? मैँ समझता हूँ जो विद्यार्थी हिन्दी पढ़ रहे होँ, उन्हेँ यह पुस्तक अवश्य पढ़नी चाहिये। वह इसलिये क्योँकि आलोचना एकांगी नहीँ होती। उसे परम्परा को समझना होता है। जो प्रदत्त संसार है, वह बहुत जटिल और अनर्गल प्रतीत होता है। किन्तु बहुत समय गुजरने के बाद समझ आता है कि यह सब कुछ यादृच्छिक नहीँ है। भाषा कैसे अर्थ प्रदान करती है, संस्कृति कैसे मूल्योँ को लेकर चलती है और किस तरह संस्कृति सौन्दर्यबोध विकसित होने की मौलिक चेष्टा है, यह सभी कुछ आलोचना का प्रथम कर्त्तव्य है।
श्री अम्बुज कुमार पाण्डेय अपनी पुस्तक मन मति रंक मेँ जिन विषयोँ पर विचार करते हैँ, उनमेँ प्रमुख हैँ– कोणार्क, बनारस शहर, महाभारत, बाँस, ह्वी॰ शान्ताराम, बैजू बावरा, पण्डित जसराज, छन्नूलाल मिश्र, मणिकर्णिका घाट, कबीर, नामवर सिंह, किशोर कुमार, हेमन्त कुमार, उस्ताद बिस्मिल्ला खाँ, नामवर सिंह आदि, आदि।
हिन्दी साहित्य मेँ रुचि रखने वाले जो भी फेसबुक पर २०१५ से २०२० तक के बीच सक्रिय होँगे, वे अम्बुज कुमार पाण्डेय के कार्योँ से परिचित होँगे। उनमेँ से कई टिप्पणियाँ अब पुस्तक के आकार मेँ अब सुरक्षित हैँ। मुझे आशा है कि नवीन पीढ़ी इससे लाभान्वित होगी। जो सुधीजन हैँ, वे अम्बुज जी की पैनी दृष्टि से प्रसन्न होँगे। यह निश्चय ही हिन्दी के एक समर्थ आलोचक का पदार्पण है। मैँ कामना करता हूँ कि हिन्दी आलोचना का कदाचित नीरव आकाश उनके कार्योँ से भर उठे। वे न केवल ललित निबन्ध लिखते रहेँ बल्कि अन्य आलोचनात्मक कर्मोँ को सुसंगत रूप से प्रस्तुत करेँ।
– प्रचण्ड प्रवीर
मार्गशीर्ष अमावस्या, संवत् २०८२
=========================
पुस्तक : मन मति रंक
विधा : ललित निबन्ध
लेखक : अम्बुज कुमार पाण्डेय
प्रकाशक : वेरा प्रकाशन, जयपुर
क्रय हेतु गमक : मन मति रंक -अमेजॉन