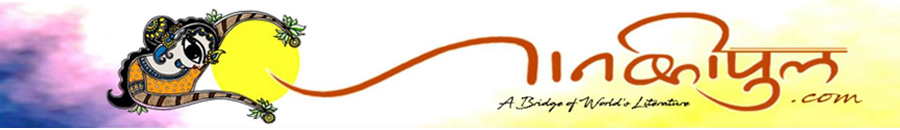आज पढ़िए उज़्मा कलाम की कहानी। उज़्मा ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया और दिल्ली विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की है और जोधपुर में एक संस्था के लिए काम करती हैं। लिखने के अलावा चित्रकारी का शौक़ रखती हैं। इनकी कहानी पढ़िए-
==================================
सुबह सवेरे ऐसी धमा-चौकड़ी मची कि मेरी आँख खुल गयी। मैंने कलाई घड़ी पर निगाह डाली तो साढ़े छः बज रहे थे। सुस्ती पूरे जिस्म में पानी की तरह बह रही थी। अभी पाँच -साढ़े पाँच बजे ही तो मैं सोई थी। उफ़! लोगो की तीखी आवाज़ मेरे कानो में चुभने लगी। इस तरह नींद खुलने से गुस्सा आया पर मैं कुछ कर नहीं सकती थी।
भारतीय रेल और स्लीपर क्लास सुबह-सुबह हुड़दंग कुछ इस तरह मच जाती है, मानो कोई बारात निकलने को बिल्कुल तैयार हो, लेकिन कुछ ना कुछ काम याद आते ही जा रहे हो। मैं आँखें खोले अपनी बर्थ पर लेटी रही। कुछ सुनते और कनखियों से देखते हुए, मैं आसानी से अंदाज़ा लगा रही थी कि सफ़र के साथी किन कामो में मशग़ूल है। रेल एक स्टेशन पर रुकी और कुछ नए लोगो ने डब्बे में घुसना शुरू किया। लोगो से ज़्यादा सामान था। सामानो ने सीटों के नीचे जगह बनाने और हंगरो पर टंगना शुरू कर दिया। मैंने आँखें बंद कर ली क्यूंकि कुछ भी आकर्षित करने वाला नहीं लगा।
अब खाने का दौर चल निकला। ‘यह तो पक्का मेथी के पराठे कि ख़ुशबू है’ नाक तो मेरी हमेशा से तेज़ थी। भले ही अम्मा के लाख समझाने और दो-चार थप्पड़ खाने के बावजूद भी बावर्चीखाने में मेरा दिल कभी नहीं लगा। खाने की ख़ुश्बू में कुछ ऐसी ताक़त होती है कि इंसान खुद-बखुद भूखा महसूस करने लगे और वही हुआ। भूख लग गयी। मेरे बैग में कोई पैक टिफ़िन नहीं था और फ़िल्हाल वह बैग भी मेरे पास नहीं था। मेरे एक साथी, जो साथ ही प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। उनका रेज़र्वेशन दूसरे डब्बे में था और वह बहुत ही शाइस्तगी से मेरा बैग भी अपने कंधो पर टाँगकर अपने डब्बे में ले गए थे। ताकि मुझे कोई तक़लीफ़ ना हो।
उनके दोनों ही कांधों पर भार था। एक पर उनका अपना बैग और एक पर मेरा। जिस कंधे पर मेरा बैग था वह कुछ ज़्यादा झुक रहा था। उनके कंधे मानो तराज़ू की कमानी की तरह लग रहे थे, जैसे कोई बनिया बड़ी तल्लीनता से दोनों तरफ़ के भार को बराबर करने की कोशिश कर रहा हो। वैसे मुझे अपने बैग उठाने की आदत है, पर यह पेशकश मुझे बुरी ना लगी। अम्मा अक्सर ही कहती, “भार तो मर्दो के कंधो पर अच्छा लगता है।” इस वजह से मैंने अपने सहकर्मी के कंधे पर भार देखकर, अपने अंदर उठने वाली हमदर्दी की लहरों को कंट्रोल किया।
“मैडम अब सीट खोल दीजिये, नीचे बैठ जाइये, खाने पीने में तक़लीफ़ हो रहीं है” मैं चौंककर अपने ख़्यालो से बाहर निकली। एक सफ़र के साथी मुझसे मुख़ातिब थे और मिडिल बर्थ खोल कर नीचे बैठने को कह रहे थे। अब आठ बज गए थे और खाने पीने का दौर पूरे जोश से चल निकला। पकवानों की ख़ुशबू नाक में समेटे मैं नीचे उतरी। चाय वाले से चाय ली और मेथी के पराठे, मसालेदार सब्जी, कचौड़ी, पुलाव की ख़ुशबू के साथ गटागट चाय पीने लगी।
एक मुस्लिम परिवार, शौहर बीवी और दो बच्चे मेरे बगल में और सामने एक अधेड़ उम्र की आंटी उनकी बहू और बेटा बैठे थे। इस तरह रिश्तों का अंदाज़ा आप भी देखकर लगाते ही होंगे। ख़ैर गाहे-बगाहे खाने-पीने में मशग़ूल सब मुझ पर नज़र डाल लेते। मैं कोई हसीन, दिलकश राजकुमारी जैसी नहीं दिखती हूँ, तो किसी भ्रम में ना आईएगा।
पड़ोस वाली माँ बच्चो के ना-नुकुर करने के बावजूद भी उन्हें खाना खिलाने में लगी थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सिर्फ़ यही उसकी ज़िन्दगी का मक़सद है । मैंने नज़र भर उस माँ को देखा और एक विचार सा आया ‘शायद अपने बच्चो को ज़्यादा प्यार करने वाली मायें ऐसी ही होती होंगी।’ ज़हन में कुछ ख़्याल हल्के-हल्के बादलो के टुकड़ो की तरह पल भर में लहरा गए। एक बार मेरी ख़ालाज़ात बहन अपने बच्चो को बहुत प्यार से मना मनाकर खाना खिलाने में मशग़ूल थी, और बच्चे नख़रों पे नख़रे कर रहे थे। तब अम्मा बोली, “हमें भी बड़ा शौक़ था, कि हम भी अपने बच्चो को ऐसे मना मनाकर खिलावें, लेकिन तुम कम्बख्तों ने तो कभी इसका मौका ही नहीं दिया।” ख़ैर जहाँ तक मुझे याद है, हम भाई-बहनो ने अम्मा को कभी ऐसी अच्छी अम्मा बनने का मौक़ा तो वाक़ई नहीं दिया था। जैसे ही खाना तैयार होता और नाक में ख़ुश्बू जाती। हम सब खुद ही बावर्चीखाने में पहुँचकर खा पीकर फ़ारिग हो जाते।
रेल वाक़ई बहुत अच्छी जगह है जहाँ बीते दिनों की बातें बहुत बढ़िया मिसालों के साथ दुबारा से यादों के दरवाज़ों पर दस्तक दे जाती है।
बगल वाली माँ को जबरन बच्चो को खिलाते देखकर मुझे फ़िक्र भी सतायी कि कहीं इन बच्चो का पेट ख़राब हो गया तो रेल के बैतुलख़ुला (शौचालय) की बची-कुची इज़्ज़त भी बेआबरू हो जाएगी। बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी इस क़दर खाने में जुटे थे जैसे पूरा बावर्चीखाना ही बाँध लाये हो। इस हालात में मेरा डर जायज़ था या नहीं, बोलिये आप क्या कहते है?
जब मैं बैतुलख़ुला से लौटी तब तक चाय का दूसरा दौर चल निकला था। अपने हैंडबैग से निकाले छोटे से रुमाल से हाथ मुँह पोछते हुए मेरी निग़ाह सामने वाली आंटी से जा मिली। उनसे नज़र हटी तो उनके हाथ में थमे हुए चाय के कुल्हड़ पर टिक गयी। जिसमे से भाप बड़ी ही आहिस्ता और प्यार से लहराती हुई बाहर निकल रही थी। जो आंटी के चेहरे से कहीं ज़्यादा ख़ूबसूरत लगी। कुछ सेकेण्ड भाप को देखने के बाद दुबारा नज़र मिली। आंटी की निगाह अब भी मुझ पर थी। अब की बार वह मुझे एक भूखी शेरनी जैसी लगी। मानो उसके सामने कोई ताज़ा, चिकना हिरन खड़ा हो और वह उसे दबोचना चाहती हो। मैंने जल्द ही निगाह हटाई और डब्बे की छत पर टिका दी। जिस पर पंखा बड़ी मेहनत मशक़्क़त करते और कई तरह की आवाज़ निकालते हुए भी धीमी रफ़्तार में चल पा रहा था। दिन चढ़ने के साथ-साथ गर्मी बढ़ती जा रही थी और पँखा अपनी ताक़त और हिम्मत जुटा कर लोगो को आराम देने की पूरी कोशिश कर रहा था।
पिछले आठ महीने से रेलगाड़ी मेरी ज़िन्दगी का एक ख़ास हिस्सा बनी हुई थी। हर आठवें-दसवें दिन किसी न किसी मंज़िल पर पहुँचने के लिए मैं रेल में सवार रहती। मेरे पैरो में कोई चक्कर सा पड़ गया था और मैं अलग-अलग राज्यों और जिलों के चक्कर लगा रही थी। रेल के सफ़र से लेकर कार्यकाल के अनेको अनुभवों से गुज़र रही थी। आज मेरा सीधा पाला औरतों से पड़ा। वैसे सफ़र में औरतें हमेशा होती लेकिन इससे पहले उन्होंने मुझमें इतनी दिलचस्पी नहीं ली, या यूँ कहे उनको मौका नहीं मिला।
चलिए, मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ। मेरे घर में मुखिया अम्मा ही है। बेचारी पर बड़ी ज़िम्मेदारी है। अब्बा की तो एक छोटी सी सजावटी सामान की दुकान है। जिसकी साज-सज्जा और आमदनी बढ़ाने की जद्दो-जहद में वह दिन रात गवांते लेकिन ‘ढाक के वही तीन पात।’ अम्मा की ज़िम्मेदारी का क्या कहना कम से कम पैसो में घर चलाना और नालायक़ बच्चो को मुआशरे के हिसाब का लायक बनाना। दोनों ही काम बड़े मुश्किल उसके हिस्से में आये। तीन नालायक़ बच्चो में एक मैं भी थी। दिन भर अम्मा की गालियां एक कान से सुन दूसरे से निकालती और इस तरह ऊँचे नीचे रास्तो पर भी ज़िन्दगी की गाड़ी आसानी से चलती हुई लगती।
मुझे पोस्ट-ग्रेजुएट में दिल्ली के एक विशविद्यालय में दाखिला मिल गया। जैसे-तैसे ट्यूशन वगैरह पढ़ाकर पढ़ाई पूरी की। पोस्ट-ग्रेजुएट तक तो अम्मा ने किसी तरह बर्दाश्त किया लेकिन इसके बाद तो कतई नहीं। बड़ी धूम-धड़ाक मची, गाली खायी, थप्पड़ खाये लेकिन अम्मा के साथ वापस नहीं गयी। अम्मा ने सारा गुस्सा अब्बा पर उतारा।
“तुम तो अपनी इसी दुकान में मरो और यहीं कब्र खुदवा के दफ़न हो जाओ। जाने कौन से रूपये झड़ रहे है। दुनिया जहान से कोई मतलब ही नहीं। लड़की ज़ात अकेली कहाँ रह रही है, क्या कर रही है, कुछ खबर नहीं।”
अब्बा पल भर अम्मा को देखते हुए आहिस्ता से बोले, “पढ़ रहीं है, और क्या?”
“पढ़ रहीं….” अब्बा की बात को दोहराते हुए, खा जाने वाली आँखों से घूरा “हो गयी पढ़ाई, अब कहो इससे कुछ करने की ज़रुरत नहीं। तुम लड़का देखो शादी करो इसकी।”
‘उफ़! यह शादी जिसने भी बनायी बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनायीं। कोई दाँव ना चले तो बस यहीं नुस्खा आज़माओ और चारो खाने चित’ दिमाग में सवाल कौंधा और जिस्म में कंपकपी। ।
“नौकरी करना चाहती है वह, कर लेने दो। लड़का देखना शुरू कर दो जब मिल जाए तब बुला लेना” अब्बा समझाने वाले लहज़े में अम्मा से बोले।
अम्मा चीखी, “या अल्लाह, तुम्हारा तो बुढ़ापे में दिमाग ख़राब हो गया।”
अब नौकरी तो कोई तश्तरी में सजाये खड़ा ना था, जो मनमाफ़िक़ हो। यह एक प्रोजेक्ट था। जिसमे देश के कुछ राज्यों के कुछ जिलों में जाकर किसानो से उनकी खेती के तरीको के बारे में डाटा इकठ्ठा करना था। यह विषय मेरी पढ़ाई का हिस्सा नहीं रहा, पर जल्दबाज़ी में इसका हिस्सा बनना पड़ा। अम्मा की लाख अड़ंगों के बावजूद, मैंने यह नौकरी दोनों हाथो से दबोच ली। क्यूंकि यही एक वजह थी फ़िलहाल शादी से बचने और दिल्ली में रुकने की।
ख़ैर अम्मा का फ़िक्रमंद होना भी वाजिब था। इक्कीसवीं सदी अपनी रफ़्तार से चल रही है। महिला उत्थान, समानता पर तरह-तरह से काम हो रहा है। ग़ैर-बराबरी को ख़त्म करने के लिए ज़ोर शोर से आंदोलन होते हमें दिखते है। अनेको योजनाएं लागू होने के बावजूद भी जब हम ज़मीन पर आएं, तो देखते है कतई बहुत बड़ा उत्थान ना हुआ कहीं। हाँ तरक़्क़ी से इन्कार नहीं किया जा सकता। लेकिन औरत और मर्द के बीच के अंतर को बरक़रार रखते हुए।
अब भी एक नौजवान औरत जो शादी शुदा ना हो। अकेले सफ़र कर रही हो, तो मामूली बात नहीं है। ऐसे में सोने पे सुहागा तो तब हो जाए। जब उसके साथ एक मर्द हो और वह ना तो उसका शौहर हो, ना महरम। ऐसी हालात से सबसे ज़्यादा दिक़्क़त हमजिंस को होती है और मर्द को दिक़्क़त तो नहीं कह सकते मगर कुछ और ही होता है।
अगर नौजवान औरत बिल्कुल अकेली सफ़र कर रही हो। तब आस-पास के मर्द ज़रा ज़्यादा चौकन्ने हो जाते है। मदद करने, बात करने के लिए एक टाँगपर खड़े रहते है। उसके पीछे मंशा कई तरह की हो सकती है। उसका बख़ान करने लगे तो यह कहानी पटरी से उतर जाएगी और हम मूल से भटक जायेंगे। वैसे मैं मर्दो के साथ वाली सूरतेहाल से गुज़र चुकी थी ।
एक सफर दिल्ली से शिमला की तरफ़ बहुत खूबसूरत रास्तो से गुज़र रहा था। अब से पहले मैंने ऐसी ख़ूबसूरती सिर्फ़ मूवीज़ में ही देखी थी। पटरी से कुछ कदमो की दूरी पर शीशम और देवदार के पेड़ बर्फ़ की उजली चादर ओढ़े खड़े थे। मैंने पहली बार अपनी नंगी आँखों से ऐसी ख़ूबसूरती निहारी जो सारे बन्धनो से आज़ाद खुले आसमान के नीचे दूर तक फैली थी। उसी के बीच मैं अपने आप को खड़ा महसूस कर रही थी।
“कहाँ जा रहीं है आप?” बगल में बैठे अच्छी कद काठी के साहब मुखातिब हुए।
अचानक सवाल से मैं चौंक गयी और फट से जवाब निकला, “जी.. शिमला”
“बहुत खूबसूरत जगह है। पहले गयी है आप? किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रहीं है?”
‘अब जा रही हूँ, तो कहीं और किसी वजह से तो जा ही रही होंगी। बेवजह तो सफ़र कर नहीं रही’ मेरे मन में खीज सी उठी। इतने सवालो का जवाब ना देने का दिल होते हुए भी मैं बोली, “जी घूमने जा रहीं हूँ।”
लो जान तो क्या छूटी, मार ली अपने पैरो पर कुल्हाड़ी। नौजवान लड़की अकेली हिल स्टेशन पर घूमे, यह तो हाज़मा बिगाड़ देने वाली बात हो गयी।
“मैं वहाँ नौकरी करता हूँ। मैं घुमा दूँगा आपको” चारो तरफ़ ख़ुशी ऐसी बिखरी जो समेटे ना सिमटे।
मैंने बिना किसी भाव के उन्हें ग़ौर से देखा। गुस्सा आया पर चुप रहना बेहतर लगा। चलो छोड़ो सफ़र ख़त्म, बात ख़त्म। कौन बहस करे।
एक स्टेशन आया साहब कॉफी सैंडविच साथ लिए।
‘अब क्या करें’ सोंचते हुए पहले तो मैंने मना किया। दो सैंडविच और दो कप कॉफ़ी और ऊपर से उनकी दरख़्वास्त करती उम्मीद भरी निगाहें। पिघल गयी। उनकी निगाहों से नहीं बल्कि गरम-गरम कॉफ़ी से निकलती हुई भाप से। हवा में बर्फीली ठंडक थी और कॉफ़ी पीने की तलब सिर्फ़ भाप को देखकर ही हो गयी। वैसे मुझे खाने में सब कुछ ही पसंद है, सिर्फ़ करेला और उड़द की दाल छोड़कर।
जब कभी यह दोनो चीज़ें बनती तो साथ में बहुत सारी अच्छी-अच्छी बातें भी अम्मा से सुनने को मिलती, “खाना-पानी से कभी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। खाना नसीब वालो को मिलता है। खाने को कभी इन्तज़ार नहीं कराना चाहिए। ये अल्लाह की नियामत है हर किसी को नसीब नहीं।”
‘खैर खाने से क्या बैर। यह भी नसीब से मिल रहा था’ कॉफ़ी सैंडविच ले लिया। ये अम्मा भी ना, कहीं पीछा नहीं छोड़ती। साथ खाना-पीना रिश्ते को और गहरा करते है तो ऐसा ही हुआ।
“जी कहीं रुकने का इंतज़ाम किया है आपने?” जवाब का इन्तज़ार किये बग़ैर, शायद ज़्यादा ही ख़ुश थे “मैं आपका बिल्कुल सही और सस्ती जगह ठहरने का इंतज़ाम करवा दूंगा।”
‘ओहो यह तो गले ही पड़ गए’ मैंने नज़र भर उन साहब को देखा।
“जी नहीं, मेरे शौहर है यहाँ। वह भी यहाँ नौकरी करते है।” फिर कोई सवाल दूसरी तरफ़ से नहीं उठा। बस यह कहानी यहीं ख़त्म हुई। यह आखिरी और ज़ोरदार हथियार था। जिसका इस्तेमाल ना चाहते हुए भी मुझे करना पड़ा। उनका चेहरा उतर गया। कॉफी, सैंडविच सब बेकार गया।
एक सफ़र में मुंबई से दिल्ली आते वक़्त, 40-45 साल के साहब से वास्ता पड़ा। उनकी खुशमिजाज़ी, नरमी और अदब से बात करने की वजह से मुझे उनकी हर बात का जवाब देना पड़ रहा था। सफ़र भी लम्बा था। जी बहलाने का और कोई तरीक़ा भी नहीं था। कब तक किताब पढ़ो और खिड़की से झांको। ऐसे में तो ज़ुबान ही तालू से चिपक जाए। तो मैंने कुछ-कुछ देर में ज़ुबान को उसका काम करने के लिए छोड़ दिया। हर स्टेशन पर वह उतरते।
“लीजिये चाय पीजिये।”
“लीजिये पानी की बोतल। आपकी बोतल में पानी ख़त्म हो गया है। अपने लिए ले रहा था तो आपके लिए भी ले लिया।”
मेरी बोतल में कितना पानी है या ख़त्म हो गया, इसका भी ख़्याल वह बखूबी रख रहे थे। पहले तो मैंने पैसे देने की कोशिश की। लेकिन उनका लख़नवी अंदाज़ में यूँ कहना, “ऐसे शर्मिंदा ना कीजिये।” मुझे अच्छा लगा। उसके बाद मैंने उन्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की। दिल्ली आने वाला था।
“आपका फ़ोन नंबर दे दीजिये। मैं एक सप्ताह यहीं हूँ। मुझे दिल्ली घुमा दीजियेगा।”
‘अब इतनी भी फ़ालतू ना हूँ’ मैं बुदबुदाकर रह गयी।
“जी कुछ कहा आपने?”
“जी नहीं।”
अब सफ़र के आखिरी पड़ाव पर क्या बहस, क्या लड़ाई। पूरा सफ़र आराम से कट गया और क्या चाहिए। दस डिजिट का एक मोबाइल नंबर तैयार किया और लिख कर दे दिया। साथ ही बताया “जब दिल्ली पहुँच जाऊँगी तब एक्टिव करुँगी।” रात गयी और बात गयी ।
ऐसे छोटे हसीन हादसे होते रहे। जो वक़्त गुज़ारने के लिए कुछ हद तक ठीक भी थे। ख़ैर सिक्के के दो पहलू होते है। मर्दज़ात बहुत अच्छी तो नहीं, पर पूरी तरह से बुरी भी नहीं है। एक सफ़र ऐसा भी रहा, जिसमे महीने भर पहले कराई टिकट में भी कन्फर्म सीट नहीं मिली।
‘कहीं ज़रा बैठने की जगह मिल जाती तो रात कट जाती’ सोचते हुए मैं एक मासूम सी दिखने वाली आंटी की कन्फ़र्म बर्थ के कोने में अपनी तशरीफ़ रखने ही वाली थी, कि उन्होंने अपने पैरो को हद से ज़्यादा फैला दिया। वह फैली हुई मोटी टाँगे और भैंस जैसी घूरती आँखें, मानो कह रही हो, ‘यह बर्थ मेरी है। मैंने ख़रीद ली है। गलती से भी मत बैठना, वरना अच्छा ना होगा।’ उनकी निगाहो से निकले लफ़्ज़ों को पढ़कर, मैं पीछे हट गयी।
“आप यहाँ बैठ जाइये”, सामने बैठे सज्जन वक़्त की नज़ाकत भाप कर बोले।
‘मरता क्या ना करता’ बैठ गयी।
वह सज्जन पूरी रात पैर समेटे एक तरफ़ बैठे रहें, और मैं दूसरी तरफ़।
सफ़र पूरा हुआ। चलते वक़्त उन्होंने फ़ोन नंबर भी नहीं माँगा । यह बात और थी, कि इस बार मेरा मन हुआ, फ़ोन नंबर लेन-देन करने का। फिर पल भर में ही ज़हन में एक ख़्याल डर के साथ कुलांचे भरते हुए आया, ‘अब तक तो अम्मा बर्दाश्त कर रही है, लेकिन इश्क़ तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। भले ही बदमाशों से पिटवाना पड़ जाए पर शादी करवा ही देगी और शादी के बाद?’ मैंने दिल में उठ रहे जज़्बातों को काबू किया। सर झुका कर शुक्रिया अदा किया। अपना बैग उठाकर फ़टाफ़ट कदमो से उतर गयी।
अब आज के सफ़र पर लौट ही आते है। पता नहीं आज अल्लाह ने क्या सिखाने की ठानी थी। सामने वाली आंटी चाय की सुड़की लेते हुए अपने उमड़ते घुमड़ते सवालो के साथ शुरू हो गयी।
“कहाँ जा रही हो”
“कोलकता”
“मायके”
“नहीं”
“ससुराल”
“नहीं”
जैसे मायके और ससुराल के अलावा कोई तीसरी जगह हो ही नहीं सकती जहाँ मैं जाऊँ।
मेरे सहकर्मी जो दूसरे डब्बे में बैठे सफ़र कर रहे थे। वह एक बार आये थे और कुछ नाश्ता दे गए थे। जो उन्होंने किसी स्टेशन पर ख़रीदा था। साथ ही बहुत अदब से कह गए थे, “कुछ और ज़रुरत हो तो बताना।”
इस छोटी सी गुफ़्तगू से, आस पास बैठे मर्दो को यह अंदाज़ा हो गया, कि मेरे साथ कोई मर्द है। तो इस बार किसी ने एक कप कॉफ़ी पिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। मैं समझ गयी इस बार सफ़र थोड़ा घाटे में जायेगा।
अब की बार पासा औरतों के हाथ पड़ा और उन्होंने बख़ूबी दिलचस्पी भी ली। अधेड़ उम्र की आंटी शुरू थी।
“तो क्या घूमने जा रही हो। जो अभी आये थे वह तुम्हारे आदमी है?”
“जी आदमी तो है, सिर्फ़ मेरे लिए क्यों? वह सारे जहां के लिए आदमी ही है।”
उन्होंने मेरे जवाब पर मुझे घूर कर देखा फिर बोली “अरे तुम्हारे पति है?”
वह सवालो की झड़ी लगा बैठी। मन उकताने लगा। मैं जानती थी कि पति बोल देने भर से आगे का झमेला ख़त्म हो जायेगा। लेकिन इस बार मेरा सच बोलने का दिल किया, “मेरे सहकर्मी है। हम काम से जा रहे है।”
“क्या! तुम्हारी शादी नहीं हुई? ऐसे किसी भी आदमी के साथ..” लफ़्ज़ मुँह में ठहर गए और चेहरे पर कई तरह की शिक़न आ गयी। चेहरे की हर एक सिलवट कई सवालो से बनी थी। जो मुझे दिख भी रही थी और महसूस भी हो रही थी। आस पास बैठी औरतों की निगाहें भी कई सवालो के साथ मुझे घूरती लगी। मानो मेरे हाथो कोई ग़ुनाह हो गया हो।
मेरे बगल में बैठा कुन्बा, बीवी तो सर से दुपट्टा बाँधे, गर्मी में स्लीपर क्लास में बच्चो में खपी-मरी जा रही थी। कभी पानी, कभी खाना, कभी पेशाब कराना। अब जब मेरी इतनी बड़ी हक़ीक़त उसके सामने खुल गयी तो उसकी चिड़चिड़ाहट और बढ़ गयी। उनके शौहर मियाँ बिल्कुल मेरे बगल में थे, और माहवार निकलने वाला रिसाला; पाक़ीज़ा आँचल लिए प्रेम कहानियाँ पढ़ रहे थे। जब उन्होंने कहानी ख़त्म करके किताब बंद की। तब मुझे लगा औरतों के सवाल-जवाब और शक़्क़ी निगाहों से बचने का यह सही रास्ता है, कि किताब हाथ में ले ली जाए।
“क्या मैं ले सकती हूँ।” किताब की तरफ़ हाथ बड़ाते हुए मैंने पूछा।
“यह उर्दू में है।”
“मुझे आती है।”
“अच्छा! क्या आप मुसलमान है?”
“जी।”
अब तो सामने वाली सास-बहू और दूसरी सीट पर बैठी हुई औरतों के विचारो के परखच्चे उड़ने लगे। सास बहू के कान के क़रीब पहुँचकर फ़ुसफ़ुसाने के अंदाज़ में बोली। लेकिन हक़ीक़त में सुनाने के लिए बोली,
“इनके यहाँ तो औरतें या तो सात परदे में होगी या फिर सीधे! राम राम”
“ही..ही..” बहू अपने चेहरे के सारे ऐबों को उभारते हुए तीखी निगाह के साथ खिलखिलाकर हँसी। बहू मेरी उम्र की होगी, लेकिन वह पति वाली थी और मैं बिन शौहर।
मैंने पाक़ीज़ा आँचल सिर्फ़ इसलिए पढ़ना चाहा, क्यूंकि मैं इन औरतों के अजीब ख़्यालों से अपना ध्यान हटाना चाहती थी। जबकि मुझे पाक़ीज़ा आँचल की कहानियाँ कतई पसंद नहीं आती। उसमे औरत का क़िरदार शर्म-लाज, नाज़ुकता और जिस्मानी ख़ूबसूरती से सराबोर होता जो हक़ीक़त से बिल्कुल परे है।
“आप इधर आ जाइये मैं उधर बैठूँगी” मुस्लिम बीवी ने अपने शौहर के साथ सीट बदली और शौहर को सुरक्षित कोने में बिठाया। बेचारी अभी तक तो बच्चो को संभालती-संभालती मरी जा रही थी। अब शौहर की भी इज़्ज़त आबरू की फ़िक्र में आँखों के नीचे के काले गड्ढे और गहरा गए। सामने वाली बहू अपने नए-नए सुहाग को बचाने के लिए, लगातार अपने पति की आँखों में आँखें डालकर बातें किये जा रही थी।
उफ़! पता नहीं, यह औरतें किस तरह के डर में जी रही थी। भले किसी भी मसले पर इनके विचार मिले ना मिले। हर जगह धर्म और जात-पात आड़े आ जाये, लेकिन शौहर और पति के मामले में विचार ज़रूर मिलते है। शौहर के गंदे कपडे धोएंगी, जूठे बर्तन साफ़ करेंगी, फरमाइशी खाना बनाएंगी फिर भी गाहे बगाहे कभी गुस्सा बर्दाश्त करेंगी तो कभी थप्पड़, लात-घूसें भी खा लेंगी । हद तो तब है, जब खुद की इज़्ज़त आबरू के साथ शौहरों की भी इज़्ज़त आबरू बचाने की कोशिश में मरी रहेंगी। फिर भी यह शादी और शौहर को ही अपनी और अपने जैसी तमाम औरतों की ज़िन्दगी की मंज़िल और मक़सद समझेंगी।
जिनकी शादी ना हो रही हो, उनके लिए दुआयें माँगेंगी। जिनकी शादी हो गयी हो उनको पति को फँसा के रखने के गुण सिखाएंगी। सात सोमवार, करवाचौथ के व्रत करेंगी। जिसकी शादी में देर हो रही हो तो उसके क़िरदार को लेकर शक करने लगेंगी। अगर कहीं मुझ जैसी मिल जाए जो ग़ैर मर्द के साथ सफ़र में हो तो फिर क्या कहना। औरत की इस हक़ीक़त से मुझे बस इतना समझ आता है कि इसमें मोहब्बत कम और मजबूरी ज़्यादा है। इन्हें ऐसा क्या मिल गया जो यह दूसरो के पास भी देखना चाहती है। इन सब ख़यालों से मैं थक गयी और ऊपर वाली बर्थ पर जाकर लेट गयी।
अब पति और शौहरों वाली औरतों को थोड़ा सुकून मिला। सामने वाली बहू ने भी लेटने की इच्छा ज़ाहिर की।
“तुम नीचे लेट जाओ मैं ऊपर चला जाता हूँ।”
सास और बहू दोनों एक साथ बोल पड़ी “नहीं..नहीं..तुम नीचे लेटो” और बहू बेचारी पाँच गज की साड़ी लपेटे इधर-उधर से सँभालती हुई ऊपर की बर्थ पर चढ़ी। बेटे को माँ की गोद में सिर रखकर लिटाया गया।
मेरी आँख लग गयी। घंटे भर बाद उठी तो घड़ी देखते ही मैं सीधे अपने सहकर्मी के डब्बे में चली गयी। यहाँ और बैठना मुनासिब ना लगा। हम दोनों बातों में मशग़ूल हो गए। स्टेशन आने वाला था। बड़ी देर से अगल-बगल बैठे परिवार हमें देख रहे थे। वह भी शायद रिश्ते का अंदाज़ा लगा रहे थे लेकिन कोई कड़ी पकड़ में नहीं आ रही थी। ऐसा मेरा अंदाज़ा है। मैं पहले ही दूध की जली थी, तो मेरा अंदाज़ा हल्की हल्की फूँक मारने लगा।
कुछ ही पल में सहयात्री ने पूछ लिया, “कोलकाता जा रहे है आप?”
“जी” सहकर्मी बोले।
“आप लोगों का घर है वहाँ?”
“नहीं काम के सिलसिले में।”
“ओह! अच्छा!” आगे पूछना तो बहुत कुछ चाहते थे, लेकिन पता नहीं किस लिहाज़ से पूछ नहीं पाए।
स्टेशन आ ही गया। हम दोनों अपने-अपने बैग उठाकर खड़े हो गए। इस बार मैं अपने सहकर्मी के कंधों को तराज़ू की कमानी नहीं बनाना चाहती थी।
आर.ऐ.सी. सीट की एक महिला, जो बहुत देर से हमें देखकर अंदर ही अंदर झुलसी जा रही थी और अपने अंदर सवालों का बवंडर रोके हुए थी। आखिरकार आखिरी लम्हा देखते हुए तपाक से पूछ बैठी, “आपके पति है?”
अब मेरे सब्र का बाँध जो पहले ही चरमरा चुका था। इस आखिरी लहर से फटाक से टूट गया और कुछ लफ्ज़ कीड़े-मकोड़ों की तरह बिलबिलाते हुए निकल पड़े, “नहीं जी, प्रेमी है, हनीमून मनाने आये है।”
मेरे सहकर्मी ने भौचक्के से मेरी ओर देखा। हमारी नज़रें मिली और हम दोनों के चेहरों पर गुस्से और मस्ती की मिली-जुली मुस्कराहट बिखर गयी।