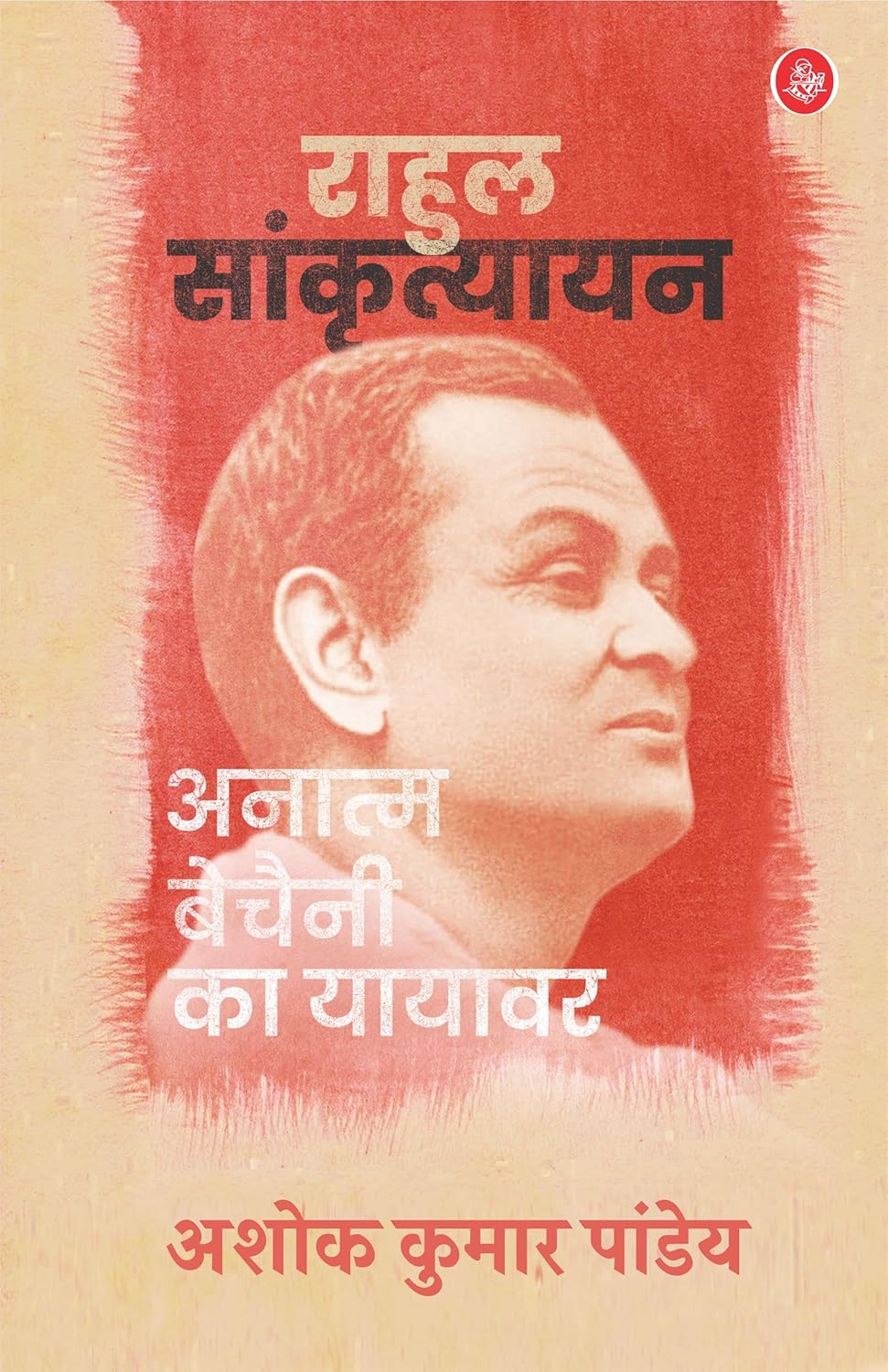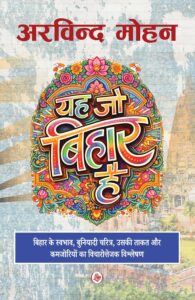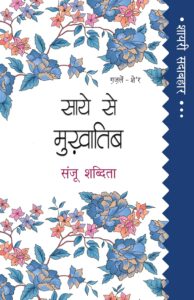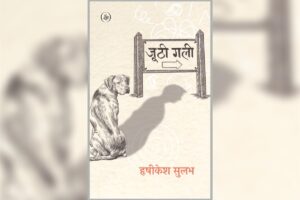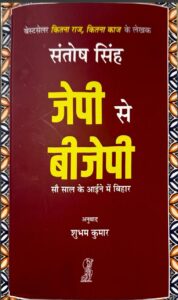‘संगत’ में काशीनाथ सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था। अंजुम शर्मा से हुई इस बातचीत में उन्होंने बताया है कि एक बार उन्होंने नामवर सिंह से पूछा कि कोई ऐसा है जो आपसे भी ज़्यादा पढ़ता हो। जवाब में नामवर सिंह ने दो नाम लिए- राहुल सांकृत्यायन और अज्ञेय। उन्होंने कहा कि ये दोनों मुझसे भी ज़्यादा पढ़ते हैं। आज राहुल सांकृत्यायनन की जयंती है। उनकी जयंती से याद आया कि इतिहासकार अशोक कुमार पांडेय ने उनकी जीवनी लिखी थी- ‘अनात्म बेचैनी का यायावर।’ राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित इस जीवनी का एक अंश पढ़िए और राहुल
=============================
वैसे तो राहुल की जीवन-यात्रा का यह अंश तत्कालीन सोवियत संघ और स्टालिन के बारे में अतिरेकी प्रशंसा से भरा हुआ है लेकिन यह विवरण भी कई तरह की धारणाओं को तोड़ता है; पहला तो यही कि समाजवादी रूस में भी शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम की खाई बरक़रार थी। प्रोफेसर को मंत्रियों के बराबर वेतन मिलता था तो शारीरिक श्रम करने वालों की आय उनसे बहुत कम थी। दूसरे धर्म वहाँ कम्युनिस्ट क्रांति के बाद भी प्रभावहीन नहीं हुआ था। राहुल की टिप्पणी है- ‘सरकारी छुट्टी न भी हो, सरकार चाहे बिल्कुल धर्मनिरपेक्ष हो, किन्तु वहाँ जनता व्यक्तिगत तौर पर धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आज भी रूसी गिरजे इतवार के दिन भक्तों से भरे रहते हैं। क्रिसमस के लिए हरी देवदार की शाखा ख़ूब बिकती है, और ऐसे बहुत कम ही घर होंगे, जिनमें क्रिसमस वृक्ष न लगा हो।‘[1] लोला से एक शिक़ायत तो उन्हें यह भी थी कि वह कम्युनिस्ट नहीं, ईसाई थीं और बेटे को ईसाई बना रही थीं। ईगोर ने तुलसीराम से मुलाक़ात के समय भी स्वीकार किया है कि वह ऑर्थडाक्स ईसाई हैं।
हालाँकि कहना मुश्किल है कि यही धार्मिक स्वतंत्रता बाक़ी धर्मों को मिली थी या नहीं। 3 दिसम्बर 1918 को जारी डिक्री में लेनिन के नेतृत्व में बनी सरकार ने मुसलमानों को अपने धर्म के पालन की स्वतंत्रता दी थी, और उनके अधिकारों को बाक़ी सोवियतों के समान ही महत्त्वपूर्ण बताया था[2] लेकिन स्टालिन के दौर में मुसलमानों का नस्ली सफ़ाया हुआ।[3] ऐसे ही 1928-38 के बीच बाक़ायदा बौद्ध धर्म के खिलाफ अभियान चला था। रूसी क्रांति के समय सोवियत संघ में बौद्ध ठीकठाक संख्या में थे। इस बिंदु पर सोवियत संघ में बौद्ध धर्म का विकास न केवल अपने चरम पर पहुँच गया था,बल्कि वास्तव में इसे पहले ही पार कर चुका था। सोवियत सत्ता के सुदृढ़ीकरण और नेता के रूप में स्टालिन के उदय ने धर्म के प्रति सोवियत नीति में एक क्रांतिकारी मोड़ को चिह्नित किया, और इस प्रकार बौद्ध धर्म की ओर भी। इस नीति के कारण व्यापक विनाश हुआ और 1930 के दशक के उत्तरार्ध तक,बौद्ध धर्म का अंतत: सर्वनाश हो गया।
असल में क्रांति के बाद बौद्धों ने बौद्ध धर्म की नास्तिकता और मार्क्सवादी धर्महीनता को सुसंगत बताते हुए सहजीविता की बात की और जब तक लेनिन थे सब ठीकठाक चला। लेकिन स्टालिन के आते ही सब बदल गया। पहले पार्टी के मुखपत्र में बौद्ध धर्म के ख़िलाफ़ अभियान चलाया गया और एक उग्र गॉडलेस असोसिएशन बनाया गया जिसका काम धर्मों के ख़िलाफ़ अभियान चलाना था। हालाँकि बौद्ध इस असोसिएशन में शामिल हो गए। फिर सीधी कार्यवाही शुरू हुई। 1928 में बौद्ध मठों पर भारी टैक्स लगा दिया गया। अगले साल कई मठों को बंद करके उनके लामाओं को साइबेरिया निर्वासित कर दिया गया। 1934 में वहाँ के सबसे प्रमुख बौद्ध लामा Agvan Dordzhiev को भी निर्वासित कर उलान-उदे की बदनाम जेल में डाल दिया गया और चार सालों के भीतर ही उत्पीड़न से उनकी मृत्यु हो गई।[4]
यह आश्चर्यजनक है कि राहुल के विवरणों में बौद्ध धर्म के प्रति स्टालिन के इस व्यवहार का भी कोई ज़िक्र नहीं मिलता, जबकि वह ख़ुद बौद्ध दर्शन को मार्क्सवाद के क़रीब मानते थे और दोनों की सुसंगतता और सहजीविता पर विश्वास करते थे। तुलसीराम लिखते हैं –
राहुल की रुचि तत्कालीन सोवियत संघ में साइबेरिया इलाके में बौद्ध मठों को देखने और उनका अध्ययन करने की थी। लेकिन वह जमाना स्टालिन का था और अनेक पाबंदियाँ लगी थीं। साइबेरिया में दुनिया की सबसे प्रसिद्ध बैकाल झील है, जिसके आर-पार बसने वाले क्षेत्र-बुर्यातिया, कल्माकिया और तुवा आदि पिछले चार सौ सालों से बौद्ध क्षेत्र है। हैरत होती है कि 60 डिग्री माइनस तापमान तक बर्फ से ढके इन क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं को परास्त बौद्ध धर्म वहाँ विकसित हुआ। जरा आप सोचिए जहाँ आदमी का पहुचना मुश्किल है, वहाँ बौद्ध विचारधारा कैसे पहुँची, वह भी चार सौ साल पहले? महापंडित राहुल इन क्षेत्रों को न सिर्फ देखना चाहते थे, बल्कि उनका गहन अध्ययन भी करना चाहते थे। वे तत्कालीन सोवियत सरकार द्वारा उत्पन्न की गयी परिस्थितियों की मजबूरी के कारण जिस बौद्ध संस्कृति को सामने नहीं ला सके मैं उसे बाहर लाना चाहता था।[5]
ईगोर ने भी अपने संस्मरण में इस ओर इशारा किया है लेकिन स्वयं राहुल इस पर एकदम खामोश हैं। रूस में रहते यह भय स्वाभाविक था लेकिन जीवन-यात्रा तो रूस से लौटने के बाद लिखी गई थी। फिर जवाहरलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी तक की तीखी आलोचना करने वाले राहुल सोवियत संघ में बौद्ध धर्म के संहारक स्टालिन पर इतने चुप क्यों हैं? कहना मुश्किल है कि ‘समाजवाद की बदनामी’ के भय से वह यह सब छिपा गए या फिर कोई निजी कारण था। अपनी जीवन यात्रा के आख़िरी खंड में जाकर वह स्टालिन की आलोचना पर सहमति जता सके हैं।
लेकिन, जाने-अनजाने में इशारे भी पर्याप्त हैं। क्रांति दिवस का वर्णन करते हुए राहुल लिखते हैं –
नगर के बड़े-बड़े घरों को भी सजाया गया था। जगह-जगह पर लेनिन और स्टालिन तथा दूसरे नेताओं के भी विशाल चित्र टंगे हुए थे। लेकिन पुस्तकालय के ऊपर लेनिन और स्टालिन का चित्र इतना ऊँचा था कि वह नीचे से चौतल्ले के ऊपर तक पहुँचता था। कोई जगह ऐसी नहीं थी, जिसमे स्टालिन का चित्र ना हो। जहाँ-तहाँ ‘ग्लावा बेलीकम स्टालिन’ (महान स्टालिन की जय) बड़े-बड़े अक्षरों में लगे हुए थे।[6]
यह दृश्य आज हमें जाना-पहचाना लगेगा और व्यक्तिपूजा का उदाहरण भी, लेकिन राहुल को उस दौर में यह सामान्य लगा था। इसके अलावा रूस में रहते उन्हें यह लगातार एहसास था कि सेंसर के चलते लिखना संभव नहीं। वह एकाधिक बार कहते हैं कि यहाँ अगर लिख भी लिया तो छपने के लिए भारत भेजने पर जाने वहाँ पहुँचेगा भी या फिर सेंसर कर दिया जाएगा। मध्य एशिया के इतिहास लेखन से पहले भी वह मध्य एशिया जाना चाहते थे लेकिन सोवियत सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। जीवन के आख़िरी दौर में जब वह चीन गए तो भी उनकी इच्छा एक आख़िरी बार तिब्बत जाने की थी लेकिन चीन की सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी। विडंबना है कि अपने सपनों की इन व्यवस्थाओं में उन्हें लिखने-पढ़ने-शोध की छूट नहीं मिली जबकि भारत के जिस लोकतंत्र से उन्हें सदा शिक़ायत रही, जिसके प्रधानमंत्री के लिए शायद ही उन्होंने कभी कोई सम्मानजनक वाक्य लिखा हो, वहाँ उन्हें मनचाहा लिखने-बोलने-छपने-घूमने की आज़ादी ही नहीं मिली, पद्मभूषण सहित अनेक सम्मान भी मिले और अवसर भी।
तीसरे यह कि उत्पादन के आँकड़े बढ़ाने के अलावा बाक़ी चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं था। इसकी खीज तो राहुल के यहाँ बार-बार दिखती है। स्टालिन के दौर का बचाव करते हमेशा उत्पादन बढ़ाने के तर्क दिए जाते हैं कि उसने कृषि के समूहिकीकरण और भारी औद्योगीकरण से कैसे रूस की तस्वीर बदल दी। हालाँकि उन आंकड़ों और इस प्रक्रिया के दीर्घकालीन असर को लेकर कई अध्ययन हुए हैं, लेकिन यहाँ उसके विस्तार में जाना विषयांतर होगा।
लेकिन एक बंधी-बंधाई नौकरी और पारिवारिक जीवन राहुल को रूस में लंबा बांधने में सफल नहीं हुआ और दूसरा साल ख़त्म होते ही उन्होंने लौटने की तैयारी करनी शुरू कर दी। अक्सर लिख-पढ़ न पाने की सुविधा को उनके लौटने का कारण बताया जाता है। राहुल ख़ुद भी यही कारण बताते हैं। लेकिन उन्हें पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि एक और बार वह भाग रहे थे, जैसे कनैला से भागे थे। स्वप्नदेश का स्वप्न शायद स्वप्न में ही सुंदर लगता है। सेंसर का बंधन और लोला जैसी आत्मनिर्भर महिला के साथ बराबरी वाला सम्बन्ध शायद उनके लिए सहज नहीं था। वह दोनों से भाग रहे थे जैसे। हालाँकि ईगोर ने लिखा है कि वह परिवार को भारत बुलाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जिस तरह वह भारत आने के बाद वह दो साल के भीतर कमला सांकृत्यायन से सम्बन्ध स्थापित कर लेते हैं और फिर 1950 में शादी कर लेते हैं, लगता नहीं कि वह इसे लेकर गंभीर थे। उसके बाद तो वह जैसे उस ओर से पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे।
लेकिन उनके इस निर्णय ने लोला के जीवन को मुश्किलों में डाल दिया । ईगोर बताते हैं-
1949 के बाद मेरी माँ का जीवन तेजी से बदल गया। पति यानी मेरे पिता से तलाक़ लेने से इंकार करने पर उन्हे अध्यापन के कार्य से हटा दिया गया और प्राच्य संस्थान के पुस्तकालय के पद से मुक्त कर दिया गया। जून 1949 में उन्हें लेनिनग्राद विश्वविद्यालय के प्राच्य वैज्ञानिक-अनुसंधान में सहायक वैज्ञानिक कर्मी के पद पर भेज दिया गया, जहाँ उन्होंने मंगोलियाई भाषा शास्त्र पर पाठ्य सामग्री तैयार करने का काम किया। लेकिन 1 अप्रैल 1950 को उन्हे इस पद से भी हटा दिया गया और प्राच्य संस्थान बंद किए जाने से वे बिल्कुल बेरोजगार हो गईं। विश्वविद्यालय से दी गई चरित्र-रिपोर्ट में कहा गया था : “ये. नि. सांकृत्यायन दुर्लभ विषय तिब्बती भाषाशास्त्र की विशेषज्ञ है; तिब्बती, मंगोल, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन भाषाएँ जानती है, पुस्तकालय विज्ञान की विशेषज्ञ और पुस्तकविद् है… ये. नि. के पति विदेशी नागरिक हैं और वे भारत में रह रहे हैं।“[7]
इस रिपोर्ट की अंतिम पंक्ति ने लोला के लिये कहीं नौकरी हासिल करना मुश्किल कर दिया था। असल में जब राहुल को भाषा सम्बन्धी सवाल पर जब कम्युनिस्ट पार्टी से निकाल दिया गया तो सोवियत संघ में लोला के लिए दिक़्क़तें और बढ़ गईं। सन् 1950 में सोवियत शासन ने लोला को आदेश दिया कि वे अपने विदेशी पति राहुल सांकृत्यायन को तलाक़ दे दें, अन्यथा उनकी नौकरी ख़तरे में पड़ जाएगी। लोला ने नौकरी से बर्खास्त होना स्वीकार किया और राहुल को तलाक़ नहीं दिया। फलतः मार्च 1950 में उन्हे नौकरी से निकाल दिया गया।[8] हालाँकि लोला और राहुल की कभी विधिवत शादी नहीं हुई थी लेकिन सोवियत समाज में बिना विवाह भी साथ रहने वालों को विवाहित ही माना जाता था। यही दौर था जब उन्होंने एक पत्र में राहुल से कुछ आर्थिक मदद मांगी थी, लेकिन उत्तर देने की जगह राहुल की अपनी जीवनयात्रा में जो टिप्पणी है उसका लब्बोलुबाब है कि ‘मैं कहाँ से मदद करूँ’.. वह लिखते हैं
लोला और ईगोर की चिट्ठी मिली, जिसमें पैसों की आवश्यकता भी बताई गई थी। लेकिन, यहाँ के पैसों का वहाँ मूल्य ही क्या था? बुलाने की तो बात भी नहीं कर सकता था।[9]
इस पंक्ति के बाद न बुलाने के कारण के रूप में उन्होंने लिखा है कि जैसी पढ़ाई रूस में मिल सकती थी या जो नौकरी रूस में मिल सकती थी उसका यहाँ सपना भी नहीं देखा जा सकता था। क्या सचमुच? क्या जया और जेता को उन्होंने कान्वेन्ट की शिक्षा नहीं दिलवाई? क्या उन्हें यहाँ सर्वसुविधायुक्त जीवन और नौकरियाँ नहीं मिलीं? कुछ पन्नों पहले ही उन्होंने बताया है कि इस साल वह आयकरदाता हो गए थे; आय प्रतिवर्ष 5000 रुपये से अधिक थी। जल्द ही उन्होंने मसूरी में एक बड़ा बँगला खरीद लिया था। क्या मुश्किल में पड़ी पत्नी और बच्चे की मदद करना उनकी जिम्मेदारी नहीं थी? क्या ईगोर का यह भरोसा सिर्फ़ एक भ्रम था कि उनके पिता ने उन्हें बुलाने की हर संभव कोशिश की? क्या राहुल पत्रों में झूठा दिलासा दे रहे थे?
हालाँकि प्रभाकर माचवे सहित कई लोगों ने यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि वह ईगोर के लिए तड़पते थे[10] लेकिन तुलसीराम द्वारा ईगोर के संस्मरण से उद्धरित यह प्रसंग बताता है कि आख़िरी क्षणों की बेहोशी में भले राहुल अग्रज पुत्र के नाम की रट लगा रहे लेकिन रूस से लौटने के बाद उन्होंने पलटकर नहीं देखा।
इन सबके बीच एक ऐसी घटना है जो पहले दुखी और फिर क्षुब्ध कर देती है।
ईगोर ने कहा कि सन् 1954 में राजकपूर की फिल्म ‘आवारा’ जो रूसी भाषा में डब की गई थी, को सेंटपीटर्सवर्ग के एक सिनेमा हाल में उन्होंने (ईगोर) देखा था। आवारा रूसी भाषा में ‘ब्राज्यागा’ कहते हैं। ईगोर ने कहा कि इस फिल्म के देखने के बाद उन्होंने राहुल सांकृत्यायन को भारत में एक चिठ्ठी भेजी और यह पुछा कि, “पिताजी, क्या मेरा जीवन ‘ब्राज्यागा’ की तरह है?’ किन्तु इस पत्र का ईगोर को जो जवाब आया, उसे याद कर वे आज भी दुखित जान पड़े, क्योंकि राहुल जी ने जवाब में लिखा था कि उनकी फिल्मों में कोई रुचि नहीं है, इसलिए ‘आवारा’ के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते।[11]
यह सच है कि राहुल को फिल्में पसंद नहीं आती थीं लेकिन मसूरी के अपने बंगले हर्न क्लिफ़ में रहते राहुल हर सप्ताहांत कमला के साथ सिनेमा देखने जाया करते थे, अख़बार आते ही थे उनके यहाँ और बंबई भी बहुत दूर नहीं थी। बेटे के कहने पर तो फिल्म का कथानक पता करना उनके लिए एकदम आसान था; फिर बेरुखी से दिया यह जवाब क्या कोई अपराधबोध था उस परित्यक्त किशोर पुत्र के प्रति जिसने रूस से उनके लौटते हुए जान लिया था कि वह अब कभी नहीं आएँगे।
लेकिन इन सबसे ज़्यादा दुखद तथ्य यह है कि महापंडित त्रिपिटिकाचार्य कॉमरेड राहुल सांकृत्यायन असल में अपने किशोर पुत्र से झूठ बोल रहे थे। उनकी जीवनयात्रा में दर्ज ब्यौरे के अनुसार 2 जून 1953 को वह यह फिल्म सपरिवार देख चुके थे। उनकी टिप्पणी है-
2 जून को पृथिवीराज और राजकपूर का नाम सुन करके हम ‘आवारा’ फिल्म देखने गए। अभी उसकी विदेशों में ख्याति नहीं हुई थी, तो भी मैंने लिखा था- “अब तक देखे गए भारतीय फ़िल्मों में अच्छा है, इसमें संदेह नहीं। सब दृष्टि से अच्छा कहना पड़ेगा।[12]
[1] पेज 90, मेरी जीवनयात्रा, जिल्द-3, राहुल सांकृत्यायन, पाँचवा संस्करण, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-2018
[2] https://www.marxists.org/history/ussr/government/foreign-relations/1917-1918/1917/December/3.htm
[3] Williams, B. G. (2002). The Hidden Ethnic Cleansing of Muslims in the Soviet Union: The Exile and Repatriation of the Crimean Tatars. Journal of Contemporary History, 37(3), 323–347. http://www.jstor.org/stable/3180785
[4] Buddhism in the Soviet Union: Annihilation or Survival? , HANS BRAKER, https://biblicalstudies.org.uk/pdf/rcl/11-1_036.pdf
[5] पेज 171, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और बौद्ध संस्कृति, तुलसीराम, महापंडित राहुल सांकृत्यायन स्मारक व्याख्यान: नई दुनिया की संभावना, (सं) मैनेजर पाण्डेय, अनिल कुमार पाण्डेय, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली-2017
[6] पेज 120, मेरी जीवनयात्रा, जिल्द-3, राहुल सांकृत्यायन, पाँचवा संस्करण, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-2018
[7] पेज 301, राहुल सांकृत्यायन: स्वप्न और संघर्ष में संकलित ईगोर सांकृत्यायन का संस्मरण ‘मेरी यशोधरा माँ येलेना सांकृत्यायन
[8] पेज 172, महापंडित राहुल सांकृत्यायन और बौद्ध संस्कृति, तुलसीराम, महापंडित राहुल सांकृत्यायन स्मारक व्याख्यान: नई दुनिया की संभावना, (सं) मैनेजर पाण्डेय, अनिल कुमार पाण्डेय, स्वराज प्रकाशन, दिल्ली-2017
[9] पेज 257, मेरी जीवनयात्रा, जिल्द-4, राहुल सांकृत्यायन, पाँचवा संस्करण, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-2018
[10] पेज 272, समय साम्यवादी, भाग-1,विष्णुचंद्र शर्मा, संवाद प्रकाशन, मेरठ-2006
[11] पेज 173, मेरी जीवनयात्रा, जिल्द-4, राहुल सांकृत्यायन, पाँचवा संस्करण, राधाकृष्ण प्रकाशन, दिल्ली-2018
[12] पेज 84, वही