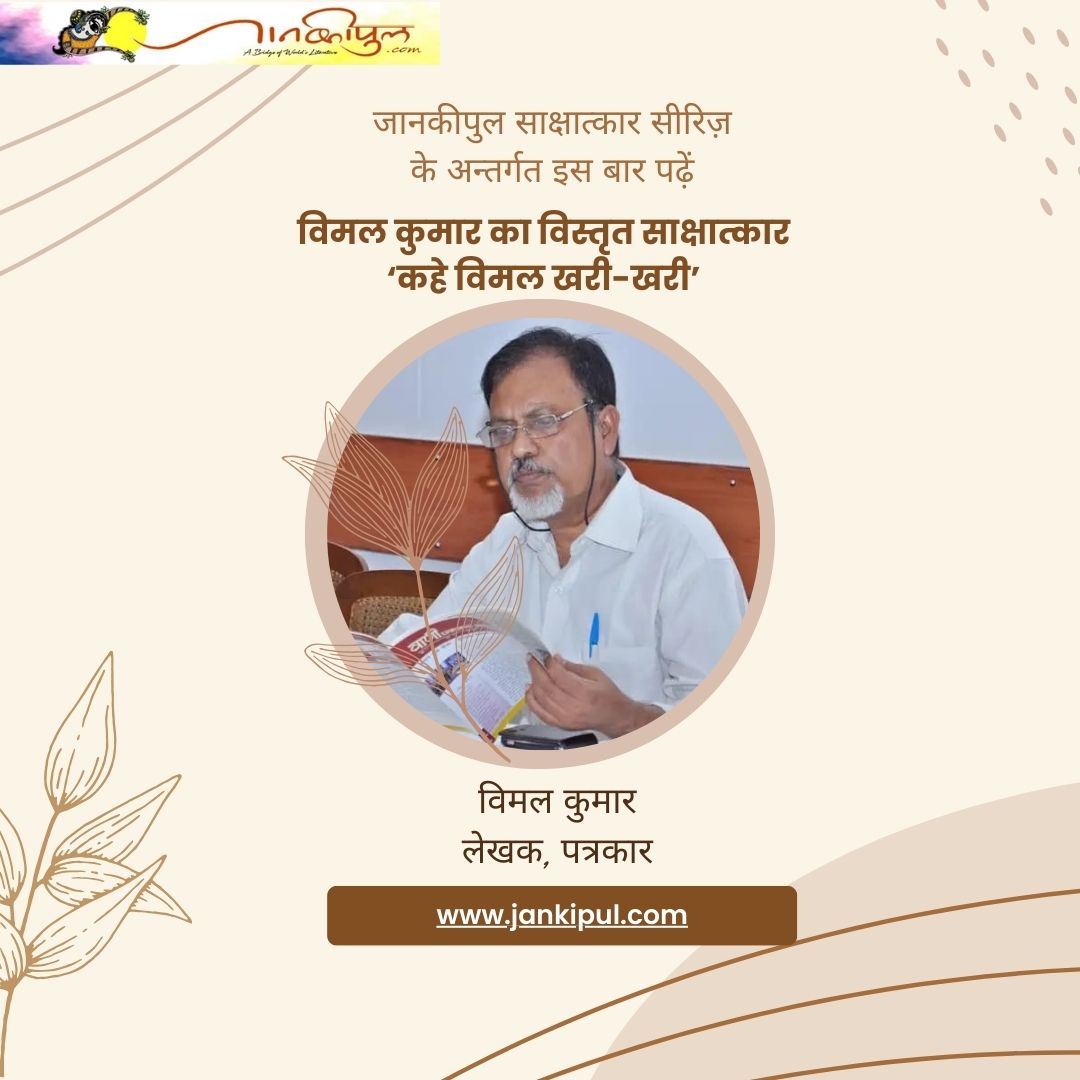हिन्दी में इंटरव्यू आमतौर पर सत्ताधीशों के लिए जाते हैं। यह मानकर कि वे बड़े लेखक होते हैं। लेकिन क्या सत्ता के आधार पर ही कोई बड़ा लेखक होता है? 1980 के दशक में ‘सपने में एक औरत से बातचीत’ कविता के लिए भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त कवि विमल कुमार सत्ताधीश नहीं हैं लेकिन हिन्दी की हर सत्ता को आईना दिखाने का काम करते रहे हैं। अपनी बेबाक़ टिप्पणियों के लिए जाते रहे हैं। वे हिन्दी साहित्य के चलते-फिरते इतिहास हैं। उनसे यह बातचीत कठिन ज़रूर थी लेकिन आख़िरकार हो गई। कठिन इसलिए क्योंकि उनको ट्रैक पर रखना आसान काम नहीं है। विमल कुमार जी के कई रूप हैं। इस बातचीत में वे अपने हर रूप में उपस्थित हैं। फ़ेसबुक पर उन्होंने मुझे विमल कुमार की प्रोफ़ाइल से ब्लॉक कर रखा है लेकिन अरविंद कुमार के नाम से मेरे वाल पर टिप्पणियाँ करते रहे हैं। बहरहाल, उनकी यह बातचीत पढ़िए। लंबी है है लेकिन रसदार है- प्रभात रंजन
=======
प्रश्न- विमल कुमार जी नमस्कार। आपसे पहला सवाल यह है कि दिल्ली के साहित्यिक परिदृश्य में आप किस तरह के बदलाव को महसूस करते हैं। आपको दिल्ली के साहित्यिक जगत में आये चालीस साल से अधिक का समय हो चुका है। वह कौन सी चीज है जिसे आप सबसे अधिक याद करते हैं?
उत्तर- मैं 1982 में दिल्ली आ गया था उच्च शिक्षा के लिए। मेरे माता पिता ने मुझे आईएएस बनाने के सपने के साथ मुझे दिल्ली पढ़ने को भेजा था। उन दिनों बिहार के निम्न मध्यवर्गीय परिवार के लोगों का यही सपना होता था, लेकिन मुझे तो दिल्ली आने से पहले ही पटना में साहित्य का “चस्का “लग चुका था। मेरी कविताएं शंकर दयाल सिंह की पत्रिका” मुक्तकंठ” “कृति संकल्प” “पहुंच” “ज्योत्स्ना” ,”समवेत” , जैसी पत्रिका में छप चुकी थी। पटना आकाशवाणी में युवा कार्यक्रम में मेरी कविताओं का पाठ हो चुका था। उन दिनों हृषिकेश सुलभ casual anouncer थे। विजयलक्ष्मी युववाणी की प्रभारी थी। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक एवम कमलेश्वर के मित्र मधुकर गंगाधर भी रेडियो में प्रोड्यूसर थे। उन्होंने भी मुझे एक बार कविता पाठ के लिए बुलाया था। वे रेणुजी के समकालीन थे। “नया” नाम से एक पत्रिका निकालते थे। बिंदु सिन्हा, उषा किरण खान, मिथिलेश्वर, मधुकर सिंह की कहानियां उन दिनों छप रहीं थी। दिनकर के समकालीन केदारनाथ मिश्र “प्रभात” जी को अपने मोहल्ले में सुन चुका था। “लाल धुआं”, रवींद्र राजहंस सत्यनारायण जी की कविताएं भी सुन चुका था। जे पी आंदोलन का जमाना था। बाद में नंद किशोर नवल जी से मिलता था। अरुण कमल तब एक युवा कवि के रूप में उभर रहे थे। आलोक धन्वा की चर्चा थी। मेरे ए एन कालेज में कुमारेन्द्र पारस नाथ सिंह टीचर थे। आचार्य शिवपूजन सहाय के ज्येष्ठ पुत्र डॉक्टर आनंदमूर्ति उस कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। बड़े विद्वान और सज्जन पुरुष, उनके सम्पर्क में आया।
इस बीच रांची से बीए इतिहास में किया। वहां बालेंदु शेखर तिवारी के सम्पर्क में आया तो नवल जी की पत्रिका “धरातल” में उदय प्रकाश, अरुण कमल, श्याम कश्यप और रामकृष्ण पांडेय की कविताएँ एक एक अंक में आई थी। नई कविता के दौर के प्रसिद्ध आलोचक नागेश्वर लाल (जो अपने लेख नयी कविता के प्रतिमान से चर्चित हुए थे। नामवर जी की किताब इसी नाम से आई और नामवर जी ने अपनी किताब की पहली पंक्ति में ही नागेश्वर लाल का जिक्र किया है।) और दिनेश्वर बाबू के सम्पर्क में आया। रांची में उर्दू के शायर प्रकाश फ़िक्री से भी मिलता था। आरा में जनवादी आलोचक चंद्रभूषण तिवारी से मिला था। उनको कविताएं दिखाई थी। पटना में रंजन सूरिदेव और निशांत केतु जी से मिला था। उन्हें अपनी कविताएं दिखाई थीं। चंद्रभूषण तिवारी जी ने मेरी कविता फुलझरिया को पढ़कर लाल पेन से रंग कर कहा कि इसमें एक सामंती युवक एक गरीब लड़की से प्रेम करता दिखाया जो प्रेम के नाम फरेब है। धर्मयुग में मंन्नू भंडारी की “त्रिशंकु” निर्मल जी की “दूसरी दुनिया” और प्रतिमा वर्मा की “राख” कहानी से आकृष्ट हुआ। लीलाधर जगूड़ी, बलदेव बंशी, कैलाश वाजपेयी, अजित कुमार, डॉक्टर विनय को धर्मयुग से ही जाना। मिथिलेश्वर की बाबू जी कहानी पढ़ी थी। इस तरह साहित्य में रुचि विकसित होने लगी थी। स्कूल में जे पी पर एक कविता लिखकर डाक
से भेज दी। उनका पत्र आया। इससे मैँ बहुत उत्साहित हुआ। लेकिन माता पिता का दवाब आईएएस की परीक्षा देने पर था। इसलिए दिल्ली आया। पिता जी 500 रुपए भेजते थे जबकि उनको 1200 रुपए ही नौकरी में मिलते थे।
बहरहाल जब दिल्ली आया तो मेरे भीतर साहित्यिक संस्कार के बीज पड़ चुके थे। मित्रों में दीपक से, जिनका अल्पायु में निधन हो गया, नीलाभ मिश्र (जो आउटलुक के संपादक बने), उनसे मेरी गहरी मित्रता हुई। यहां एक से एक बड़े साहित्यकार थे। उनकी तूती बोलती थी। अज्ञेय का बड़ा जलवा था। उनका एक प्रभा मण्डल था। वैसा प्रभामंडल मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। राजेन्द्र यादव, विद्यानिवास मिश्र जैसे लेखक सकुचाते सहमते मिलते थे। बाद में अज्ञेय जी से उनके घर पर दो बार मिला। एक बार राजेन्द्र उपाध्याय के सौजन्य से एक बार श्री राम वर्मा के सौजन्य से। उस समय रघुवीर सहाय “दिनमान” में थे और एक बड़े कवि पत्रकार के रूप में जाने जाते थे। इन लोगों से मिलने में डर भी लगता था।
आत्मविश्वास की कमी थी। पटना में रहते हुए हम लोग “दिनमान” जरूर पढ़ते थे। इसलिए दिनमान, धर्मयुग सारिका से जुड़े लेखकों को हम लोग जानते थे। दुष्यंत कुमार को सारिका और धर्मयुग में पढ़ चुके थे। जे पी पर धर्मवीर भारती की कविता “मुनादी” का असर था। रेणु जी हमलोगों के नायक थे। अलबत्ता उनको कभी देखा नहीं। बिहार के यशस्वी लेखक शिवपूजन सहाय, राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह और बेनीपुरी जी हम लोगों के प्रतीक पुरुष थे। मुझे याद है कि मैं सबसे पहले दिल्ली जाकर दिनमान के दफ्तर में ही गया था और बिना जान पहचान के सर्वेश्वर दयाल सक्सेना से मुलाकात की थी। क्योंकि मैंने उनकी “कुआओ नदी” किताब पटना में रहते हुए पढ़ रखी थी जिसका मुझ पर गहरा असर था और उस समय मैँ उनसे बहुत प्रभावित था। तब केदार नाथ सिंह की उतनी चर्चा नहीं थी, न विष्णु खरे की। अशोक वाजपेयी “अज्ञेय पर बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाये लेख” से चर्चा में थे। उनकी “पहचान” सीरीज और “शहर अब भी संभावना है” की चर्चा थी। अजीत कुमार से भी मिलता था। धर्मयुग में उनकी रचनाएं पढ़ चुका था। दिल्ली विश्वविद्यालय में विश्वनाथ त्रिपाठी नित्यानंद तिवारी के सम्पर्क में आया। मैं हिंदी का छात्र नहीं था पर अजय तिवारी और चारु मित्र से संवाद शुरू हुआ। आनंद प्रकाश के सम्पर्क में आया जो बड़े सज्जन पुरुष थे। बहुत ही ईमानदार। कुलदीप सलिल भी।नामवर जी, विद्यानिवास मिश्र को रांची में सुन चुका था। उनकी विद्वता की बहुत चर्चा थी। वे लोग अपने अद्भुत भाषणों से सबको प्रभावित करते थे। केदारनाथ सिंह का संग्रह “जमीन पक रही” आया था और उससे उनकी एक नई पहचान बनी थी। उन दिनों उदय प्रकाश कहानीकार के रूप में सामने आ रहे थे। उनका एक कविता संग्रह “सुनो कारीगर” आ चुका था जिसकी समीक्षा सर्वेश्वर जी ने दिनमान में की थी। मंगलेश डबराल का भी पहली कविता आ चुका था। विष्णु खरे, असद ज़ैदी का पहला कविता संग्रह जयश्री प्रकाशन से आया था लेकिन अभी वे बड़े कवि के रूप में स्थापित नहीं हुए थे जैसे कि बाद में कवि के रूप में उनकी पहचान बनी। उन दिनों खरे साहब की एक पुस्तक “आलोचना की पहली किताब” आई थी। इसकी बड़ी चर्चा हुई थी। पंकज बिष्ट का उपन्यास “लेकिन दरवाजा” उन दिनों आया था, उन्हें ओमप्रकाश साहित्य सम्मान मिला था। विष्णु नागर का संग्रह “तालाब में डूबी छह लड़कियां”और इब्बार रब्बी का दूसरा संग्रह “लोगबाग” भी आया था। मैंने
बलदेव बंसी की पत्रिका “विचार कविता” में एक लेख उदय प्रकाश, मंगलेश, रब्बी और दिविक रमेश की कविताओं पर लिखा था। उन्हीं दिनों तेजी ग्रोवर से डॉक्टर विनय के घर पर मुलाकात हुई थी। और तेजी ग्रोवर और उनके पहले पति अर्नेस्ट अल्बर्ट तथा अतुल वीर अरोड़ा के संयुक्त कविता संग्रह “जैसे परम्परा सजाते हुए” पर मैंने डॉक्टर विनय की पत्रिका “दीर्घा” में एक समीक्षा लिखी थी।यह वही दौर था जब विजय कुमार का पहला कविता संग्रह “अदृश्य हो जाएंगी सूखी हुई पत्तियां” आया था और मैंने उसकी और पंकज सिंह के पहले कविता संग्रह “आहटें आसपास“की समीक्षा ”दीर्घा” में लिखी थी। वे सविता सिंह से मिलने दिल्ली विश्वविद्यालय अक्सर आते थे। वहीं उनसे परिचय हुआ पर वे मुझसे कभी सहज नहीं लगे और न मैं कभी सहज हुआ।”दीर्घा” का एक कविता अंक भी आया था जिसमें मेरी कविताएं छपी थीं और सविता की भी।सविता मुझसे सीनियर बैच में थीं। वे मेरे जिले की थीं। वे मेरे साथ डॉक्टर विनय से मिलने उनके बेंगलुरु रोड घर पर गई थी। अनामिका अंग्रेजी की स्टूडेंट थी। सेंट स्टीफन कालेज में कविता प्रतियोगिता में पहली बार हम दोनों ने
कविता पढ़ी पर हम दोनों को कोई पुरस्कार नहीं मिला, वहीं उनसे परिचय हुआ। वैसे उनको पटना से जानता था। रविवार में उनके बारे में एक रिपोर्ट छपी थी। डॉक्टर विनय ने “दीर्घा” का आलोचना अंक निकाला जिसमे मैंने रामदरश मिश्र पर और स्नेहमयी चौधरी पर एक लेख लिखा था। उन्हीं दिनों मैंने नरेंद्र मोहन से लंबी कविताओं के रचना विधान पर 30-40 पेज का लंबा इंटरव्यू लिया था जो एक पत्रिका में धारावाहिक रूप से छपा था। अजीत कुमार को भी कविताएं दिखाईं थीं।
कुल मिलाकर परिदृश्य गहमागहमी से भरा था। तब सुधीर पचौरी और कर्ण सिंह चौहान एक आलोचक के रुप में छा रहे थे और अपने धुआंधार भाषणों से सबको प्रभावित कर रहे थे। उन दोनों की छवि एक क्रांतिकारी लेखक की छवि थी। लेकिन बाद में उन दोनों के विचारों में एक बड़ा परिवर्तन दिखाई दिया। जनवादी लेखक संघ की स्थापना हो चुकी थी और मुझे याद है कि उसके एक सम्मेलन में (जो मंदिर मार्ग पर हुआ था) मैं गया था और मनमोहन को पहली बार कविता सुनाते हुए देखा था – राजा का बजा बजा। वहां शुभा जी भी मौजूद थी लेकिन तब तक मेरा उनसे कोई परिचय नहीं हुआ था। उन्हीं दिनों डॉक्टर लक्ष्मीधर मालवीय भी आए थे।त्रिवेणी कला संगम में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लगी थी और वहां उनका भाषण हुआ था जिसकी एक रिपोर्ट विरोध में मैंने लिखी थी जो किसी पत्रिका में छपी। उदय प्रकाश जी से उन्हीं दिनों मुलाक़ात हुई थी। उन दिनों सारिका में सुरेश उनियाल बलराम, महेश दर्पण और अरुण वर्धन काम करते थे। रमाकांत जी के पुत्र विजय श्रीवास्तव “खेल भारती” पत्रिका में काम करते थे। गगन गिल “वामा “में आ चुकी थी। मैं उन दिनों दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान का छात्र था और पहली बार महेश दर्पण, विनोद भारद्वाज आदि से मेरा परिचय हुआ। दिनमान अब “दिनमान टाइम्स” बन गया था। देवी प्रसाद मिश्र भी उसमें काम करने लगे थे। मेरी एक कविता छपी थी और रघुवीर सहाय के साठवें जन्मदिन पर विनोद जी ने मुझसे एक लेख लिखवाया था। तब तक यूनीवार्ता में मैँ काम करने लगा था। विष्णु नागर जी से मेरा परिचय मेरे कवि मित्र अमिताभ बच्चन ने करवाया था और उसी के माध्यम से असद ज़ैदी से भी मेरा परिचय हुआ। तब हरियाणा के “पींग” अखबार में काम करने लगा था। यह 84 की बात होगी। नागर जी असद ज़ैदी, मंगलेश जी, इब्बार रब्बी ने मुझे बहुत स्नेह दिया ,जिसे भूल नहीं सकता। एक प्रकरण में असद जी से विवाद हुआ और रिश्ते खराब हो गए। तब से लेकर आज तक खटास बनी हुई है। उस विवाद के कारण मैं अपने पहले कविता संग्रह के विमोचन में नहीं गया। आधार प्रकाशन से 12 कवियों का सेट आया था। नागार्जुन ने विमोचन किया था। संग्रह आने से पहले जनसत्ता में मेरी कविताएं मंगलेश जी ने तीन चार बार छापी थी। उन्होंने ही मेरी कविता “पहल” को भेजी थी। तब छपी। नागर जी ने मेरी कविता सोमदत्त को भेजी थी तब साक्षात्कार में छपी। जिस पर 1986 का भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला। हरि भटनागर ने मेरी कविता का शीर्षक “आपको एक दिन खा जाएगा भेड़िया” दिया था। वे दिन बहुत सुंदर थे। कमला प्रसाद और भगवत रावत ने जो प्यार दिया उसे नहीं भूल सकता। वे लोग बढ़िया इंसान थे। जनसत्ता के दफ्तर में ही वीरेन डंगवाल से मेरी मुलाकात हुई थी और तब तक उनका पहला संग्रह नहीं आया था। वे मुझे प्यारे इंसान लगे। कुल मिलाकर रचनात्मक माहौल था और वरिष्ठों और कनिष्टों के बीच एक संवाद था जो धीरे-धीरे किन्ही कारणों से कम होता गया और बाद में टूटता भी गया। मुझे याद है कि उन दिनों अशोक वाजपेयी ने नामवर सिंह के खिलाफ भोपाल में कुछ बोला था तो उसके खिलाफ मंगलेश डबराल, पंकज बिष्ट, नागर जी आदि ने एक बयान जारी किया था जिस पर मुझसे भी उन्होंने हस्ताक्षर करवाए थे। उसका खामियाजा बहुत दिनों तक भुगतना पड़ा था। उन दिनों एक बहुत बड़ी घटना जनसत्ता के सती प्रकरण को लेकर हुई थी, जिसके विरोध में 42 लेखकों ने हस्ताक्षर किए थे और बहिष्कार किया था। उदय प्रकाश भी शामिल थे उसमें लेकिन दो साल के बाद उनकी कविता जनसत्ता में छपी, फिर सुरेश सलिल की भी रचना छपी। यह उस हस्ताक्षर का उल्लंघन था। आनंदस्वरूप वर्मा ने उसको लेकर अपनी पत्रिका में एक रिपोर्ट छापी कि कैसे इन लेखकों ने बहिष्कार का उल्लंघन किया। लेकिन बाद में खुद वर्मा जी जनसत्ता के लिए दक्षिण अफ्रीका में रिपोर्टिंग करने गए थे। मुझे वाम पंथी लेखकों का यह दोहरापन पसंद नहीं आया। धीरे-धीरे मुझे साहित्य की भीतरी राजनीति के बारे में पता चला और लगा कि यहाँ तो कई खेमे और गुट है, दरबार हैं। नामवर जी का एक जेएनयू गुट अलग था। राजेन्द्र यादव का दरबार अलग था। आईटीओ पुल के कवियों मंगलेश डबराल, प्रयाग शुक्ल, विष्णु नागर, असद ज़ैदी, इब्बार रब्बी का एक अलग ग्रुप था। इस तरह उन दिनों साहित्य के दो तीन सत्ता केंद्र बने हुए थे और इन्हीं केंद्रों से जुड़कर लेखक स्थापित हो रहे थे। लेकिन मेरा धीरे-धीरे इन तीनों ग्रुपों से मोहभंग होता गया और मुझे लगा कि उनके लेखन और कर्म में कई तरह के अंतर्विरोध हैं। क्योंकि हम लोग एक युवा कवि के रूप में इनसे शुरू में बहुत प्रभावित थे। लेकिन धीरे-धीरे हम लोगों को लगने लगा कि साहित्य में हर लेखक का स्वतंत्र व्यक्तित्व विकसित होना चाहिए। वह किसी का पिछलग्गू चेला भक्त न बने। लेकिन हमने देखा कि लोग भक्त हैं। यह भी देखा गया कि अगर आप किसी ग्रुप से साथ नहीं हो तो आपका तिरस्कार कर दिया जाता है, बहिष्कृत किया जाता है। लेकिन मैंने बाद में सबसे दूरी बना ली। मैंने एक सिद्धांत बना लिया। रचना की तारीफ करूंगा अगर मुझे अच्छी लगी तो चाहे उसने मुझसे सम्बंध क्यों न तोड़ लिए हों। रचना से दुश्मनी नहीं लेकिन, यहां तो मामला ही अलग है। साहित्य में लोग जानी दुश्मन हो जाते हैं। ऐसे माहौल और परिदृश्य से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मेरे साथी रचनाकार परिदृश्य पर आए। लेकिन आज मिस करता हूँ रामविलास जी, नामवर जी को, निर्मल जी को, रघुवीर जी, सर्वेश्वर जी को, कुंवर नारायण, मनोहर श्याम जोशी, मंन्नू भंडारी यादव जी को, मंगलेश जी, वीरेन डंगवाल, पंकज सिंह और नीलाभ को। अब साहित्य की दुनिया ही उजड़ गयी। यह लिखते हुए आँखें नम हो रही हैं। अब केवल अशोक जी बचे हैं। अब कोई नेतृत्वकर्ता नहीं।
प्रश्न – उन दिनों पत्र पत्रिकाओं का दौर था। हिंदुस्तान, दिनमान, सारिका जैसी पत्रिकाएँ निकलती थीं जिनमें साहित्य के लिए भी पर्याप्त स्पेस होता था। जरा उस दौर के बारे में बताइए जब साहित्य और पत्रकारिता में अंतर नहीं किया जाता था। जब लेखक संपादक होते थे और वे लेखक होने के साथ साथ बड़े पत्रकार भी होते थे।
उत्तर – आपका कहना सही है कि उन दिनों इन पत्रिकाओं में साहित्य के लिए पर्याप्त स्पेस था। क्योंकि इन पत्रिकाओं के संपादक साहित्यकार हुआ करते थे, चाहे धर्मयुग के संपादक धर्मवीर भारती हों या दिनमान के संपादक अज्ञेय और रघुवीर सहाय हों या साप्ताहिक हिंदुस्तान के मनोहर श्याम जोशी। नवभारत टाइम्स के संपादक भी अज्ञेय रहे। बाद में राजेंद्र माथुर थे। उनके जमाने मे अखबार अच्छा निकलता था। असल में जब से
रविवार की पत्रकारिता शुरू हुई तब से हिंदी पत्रकारिता में बदलाव हुआ। सुरेंद्र प्रताप सिंह धर्मयुग से आये थे पर वे कोई लेखक नहीं थे। उन्होंने एक नई तरह की पत्रकारिता शुरू की थी जहां पत्रकारों का संबंध सत्ता से विकसित हुआ था। आपको याद होगा कि उनकी शादी में 9 राज्यों के मुख्यमंत्री आए थे। यह पहली घटना थी हिंदी पत्रकारिता में जिसमें सत्ता का इतना भोंडा प्रदर्शन हुआ था लेकिन जब जनसत्ता निकला तो उसने अलग किस्म की पत्रकारिता शुरू की और वह बहुत लोकप्रिय हुई। राजेन्द्र माथुर और प्रभाष जोशी लेखकों के महत्व को समझते थे और उन्हें स्वतंत्रता देते थे। मंगलेश जी साहित्य का पन्ना निकालते थे और मेरे ख्याल से हिंदी में अब तक अखबारों में जितने साहित्य के पन्ने निकले उसमें सर्वश्रेष्ठ पन्ना उनका होता था। ले आउट और कंटेंट में भी। जनसत्ता में कविता का छपना एक घटना थी। पर मंगलेश जी थोड़ा पहाड़ वाद करते थे। उनके चैम्बर में युवतियां बैठी रहती थीं लेकिन हम लोगों को कभी बैठने के लिए नहीं कहते थे। शानी जी का भी यही हाल। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता था। ख़ैर।
शानी जी जब नवभारत टाइम्स में साहित्य के संपादक बने तो उन्होंने भी कुछ अच्छे पेज निकाले। देवी की मुसलमान कविता पर बहस शुरू हुई। फिर बाद में प्रयाग शुक्ल बने तो उन्होंने भी कुछ अच्छे पेज निकाले। लेकिन बाद में इस नवभारत टाइम्स का कबाड़ा हो गया और जनसत्ता का भी कबाड़ा हो गया। अब तो कोई जनसत्ता को पूछता नहीं है। यही हाल नवभारत टाइम्स का हुआ। भूमंडलीकरण और बाजार के दौर के बाद तो हिंदी पत्रकारिता का सत्यानाश हो गया। हिंदी क्या अब तो पूरी पत्रकारिता का सत्यानाश हुआ, खासकर जब चैनल आ गए तब तो पत्रकारिता का पतन ही हो गया। 40 साल हम लोग भी पत्रकार रहे पर इतनी एकपक्षीय पत्रकारिता कभी नहीं हुई चाहे गोदी मीडिया करे या मोदी विरोधी मीडिया। मैंने खुद को कभी पत्रकार नहीं कहा बल्कि शब्दों की क्लर्की ही माना। इस बदलाव से सबसे अधिक नुकसान साहित्य संस्कृति का हुआ। अब तो रंगमंच, संगीत, चित्रकला के लिए भी जगह नहीं। पुस्तक समीक्षा, फीचर सब बन्द हो गए। यह भी सच है कि आईटीओ पुल के लेखकों ने भी उस जमाने में एक गिरोह बंदी की। कुछ लोग हावी रहे। कुछ प्रकाशक उपकृत किये गए। प्रकाशकों ने भी उनकी किताबें छापीं। लेन देन हुआ। वाम- ग़ैर वाम खेमे बने। “हंस” का भी दरबार बना तो “आलोचना “का भी दरबार। इसकी तीखी प्रतिक्रिया हुई। साहित्य अकादमी में भी वही चेहरे। दूतावासों में भी वही लोग। लेकिन तब अच्छा साहित्य भी लिखा जा रहा था। गुणवत्ता थी लेकिन अब सब कुछ बाजार के हवाले मार्केटिंग के हवाले जन सम्पर्क के हवाले है। हिंदी में जाति और प्रान्त का हमेशा से बोलबाला रहा। उत्तर प्रदेश और ब्राह्मणों का दबदबा रहा। उन्हीं दिनों नामवर जी के 75 वें जन्म दिन पर “सहारा” में मैंने एक आलोचनात्मक लेख लिखा। उनके समारोह में सत्ता का प्रदर्शन हुआ था। राजनेता आये थे।उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा। नामवर जी ने सहारा में मुझे छापने से मंगलेश जी को मना कर दिया। वे मुख्य संपादक थे। दो साल बाद मंगलेश जी ने मुझे तब बताया जब उनका नामवर जी से खटास हो गया था। राजेन्द्र यादव ने भी मेरा एक भी शब्द “हंस” में नहीं छापा। उनके खिलाफ भी सहारा में लिखा था। वैसे बातचीत और मिलने में वे लोकतांत्रिक थे पर उन्होंने अपने चेले बनाये। कई लेखिकाओं और दलितों को जगह तो दी पर कई बार खराब और कमजोर रचनाएं भी छापीं। उन्होंने भी कई स्टंट किये। मैँ कभी हंस दरबार में नहीं गया।सच पूछिए तो नामवर के दरबार में भी नहीं गया। किसी के दरबार में नहीं गया। विष्णु खरे के दरबार में भी नहीं, जबकि युवा कवि, केदार जी और खरे साहब से मिलते थे फ्लैप लिखवाते थे, पांडुलिपियां दिखवाते थे। इन दोनों ने भी चेले बनाये। भक्त बनाये। उन दोनों की कविता और विद्वत्ता का मुरीद था पर उनके व्यक्तित्व का नहीं। सत्ता के साथ उन दोनो का रिश्ता था।नामवर जी का तो भाजपा नेताओं के साथ भी रिश्ता था। चंद्रशेखर के साथ, वी पी सिंह के साथ, अर्जुन सिंह, राजनाथ सिंह। एक तरह का ठाकुरवाद था उनमें और तो और शंकर दयाल सिंह की दस किताबों का उन्होंने विमोचन किया। मैँ उनके घर कभी नहीं गया। न किताब भेंट की। मुझे वे अपने बॉडी लैंग्वेज में ही एक सामंती व्यक्ति लगे। उन दिनों अशोक जी के खिलाफ भी लिखा था। मैं उनका भी प्रिय नहीं बन सका। आज वे सरकार के खिलाफ बोल रहे तो उनका समर्थन करता हूँ। उनमें भी बदलाव आया। अब वे भारत भवन वाले अशोक जी नहीं रहे।
हंस में तो आज तक ब्लैक लिस्टेड हूँ। आलोचना में भी ब्लैक लिस्टेड। ज्ञानपीठ, वागर्थ, समास बहुवचन में भी प्रतिबंधित। अरुण कमल जब संपादक बने तब बस एक बार अपवाद स्वरूप छपा, नहीं तो वहां भी ब्लैक लिस्टेड। अरुण प्रकाश जब समकालीन साहित्य के संपादक बने तो उनसे प्रेस कांफ्रेंस में एक सवाल पूछ दिया। उसके बाद उन्होंने ब्लैक लिस्टेड कर दिया। यही हाल जलेस, प्रलेस और जसम का है। उनके खिलाफ बोल कर देखिये। वे आपको ब्लैक लिस्टेड कर देंगे। न बुलॉएंगे, न छापेंगे। पिछले दिनों रेखा अवस्थी जी को एक पत्र में सब लिख दिया। दरअसल साहित्य में आंतरिक लोकतंत्र नहीं जिस तरह राजनीतिक दलों में नहीं। मंगलेश, विष्णु खरे कोई इससे अछूते नहीं रहे। इन सभी लेखकों के साथ मेरा अनुभव बाद में बहुत खराब रहा। बाद में हिंदी पत्रकारिता की असलियत जान गया। खुद जब बीसेक साल संसद गया, सैकड़ो प्रेस कांफ्रेंस गया, तो हकीकत मालूम हुई। साहित्य में भी नेक्सस काम करता है। पुरस्कार, किताबों के प्रकाशन समारोहों के आयोजन में वक्ता के रूप में निमंत्रण यूं ही नहीं मिलते। आप देख लें कौन लोग छाए रहे परिदृश्य पर, जो मठाधीधों के साथ थे, जिनके पीछे संगठन था, जो बड़े अधिकारी थे, साहित्य संपादक थे। ठाकुर या ब्राह्मण थे। कांग्रेस के समय सत्ता के साथ थे। कमेटियों में थे। अर्जुन सिंह के दरबार से जुड़े थे। बाद में खेल पलट गया। अब दूसरे लोग सत्ता के साथ हैं। संघ परिवार की तारीफ की जा रही है। मालिनी अवस्थी, सोनल मान सिंह के साथ लोगों के फोटो देख सकते है। लेखक का काम सत्ता का साथ देना नहीं, चाहे वह वाम की ही सत्ता क्यों न हो।
प्रश्न – आख़िर क्या कारण रहा कि पत्रकारिता को उच्चतर माना जाने लगा और साहित्य को कमतर? जबकि आप अच्छे से जानते हैं कि हिंदी में यह विभेद पहले बिल्कुल नहीं था? नब्बे के दशक में ऐसा क्या हुआ?
उत्तर – 1991-92 में जब भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई और नई आर्थिक नीति बनी तो भारत में पत्रकारिता में भी काफी बदलाव हुआ। कुछ पत्रकारों के पास पैसा अधिक आ गया और वह सत्ता के करीब होते चले गए। इसका असर यह हुआ कि समाज में उनका रौब और दब दबा बढ़ गया जबकि पहले के पत्रकार अलग थे। राजकिशोर जी, राजदीप सरदेसाई,बरखा दत्त, रवीश कुमार की तरह लोकप्रिय नहीं हुए जबकि उनके लेखन का सानी नहीं। प्रभाष जोशी किसी फार्म हाउस में नहीं रहते थे जबकि शेखर गुप्ता जैसे पत्रकार रहे। आज टी
वी एंकर 50 करोड़ के मकान खरीद रहे। एक करोड़ मासिक मिल रहा। लेखक के पास उस तरह ना तो पैसा आया और न उसका सत्ता के साथ वैसा गठबंधन हुआ जिस तरह एक पत्रकार का होता है। यह कारण है कि पत्रकार को अधिक मान्यता मिलने लगी और लेखक को कम। पत्रकारिता में ब्रांड एंबेसडर ही संपादक हो गए। संपादकों का कद घटा दिया गया। इन सब के कारण समाज में यह संदेश गया कि लेखक का कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है तो पत्रकार एंकर है। क्योंकि वह टीवी पर रोज दिखता है ,वह डिबेट में नजर आता है, जबकि डिबेट में कोई लेखक नहीं दिखता है।
प्रश्न – क्या साहित्य में मठाधीशी पहले से भी थी या 1980-1990 के दशक में बढ़ी?
उत्तर – साहित्य में मठाधीश पहले भी थे क्योंकि सत्ता के केंद्र भी थे। लेकिन वे आज की तरह नहीं थे। जब रामचंद्र शुक्ल हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे तो उनकी भी एक सत्ता थी। नंद दुलारे वाजपेयी बने तब उनकी भी सत्ता थी। यहां तक की हजार प्रसाद द्विवेदी और नामवर जी की भी सत्ता थी। वे लोग नौकरियां दिलवाने की स्थिति में थे। वे लोगों अपनी आलोचना से किसी को स्थापित करने की स्थिति में थे, पुरस्कार दिलवाने की कुव्वत रखते थे। उसे जमाने के बड़े प्रकाशकों के साथ उन लोगों के मधुर संबंध थे। वे उनके सलाहकार थे, लेकिन तब भी वह रचनाकार को महत्व देते थे। लेखकों को 60-70 तक महत्व दिया जाता रहा लेकिन धीरे-धीरे हिंदी की दुनिया में ताकत बढ़ती गई। पहले डॉक्टर नगेन्द्र और बाद में नामवर जी जैसे लोग बहुत ही ताकतवर हो गए थे। वह जिसको चाहते थे उसको स्थापित कर देते थे। नौकरी दिलवा सकते थे। अज्ञेय का भी बहुत ही जलवा था। धर्मवीर भारती के पास भी एक सत्ता थी।आपको पता ही होगा कि धर्मवीर भारती पर रबीन्द्र कालिया ने काला रजिस्टर लिखा था। अज्ञेय पर वे नाम से मधुसूदन आनंद ने कहानी लिखी। नामवर जी पर उदय प्रकाश ने कविता लिखी। मैनेजर पांडे पर उदय प्रकाश ने आचार्य की रजाई नामक कहानी लिखी थी। यहां तक की विभूति नारायण राय के पास सत्ता आई तो उनके भी खिलाफ कहानियां लिखी गईं। जब अशोक वाजपेयी भारत भवन में थे और संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। तो उनकी भी एक सत्ता थी तो हिंदी में सत्ता केंद्र शुरू से ही रहे हैं। यह हिंदी का ग़ैर- लोकतांत्रिक चरित्र रहा है। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी की दुनिया में आंतरिक लोकतंत्र कम है। नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच लगातार द्वंद्वात्मक रिश्ता भी कायम रहा है। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को जल्दी स्वीकार नहीं करती और नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को पढ़ती नहीं है। यह समस्या सोशल मीडिया के आने के बाद से ज्यादा हो गई है। मेरा मानना है कि जब नई पीढ़ी को साहित्य में कदम रखना पड़ता है तो उसे पूर्ववर्ती साहित्य में जो कुछ लिखा गया, इसकी मुख्य प्रवृत्तियां के बारे में उसे जानकारी रखनी चाहिए, हालांकि यह कोई नियम नहीं है। बहुत ऐसे रचनाकार हुए हैं जो पूर्ववर्ती लेखकों को
नहीं जानते हैं, लेकिन वह अच्छा लिखते हैं। अब अशोक जी ने युवा का आयोजन कर संवाद कायम किया है। यह काम लेखक संगठन नहीं कर पाए।हालांकि अब उनका ध्यान इस ओर गया है। नलिन रंजन सिंह ने अच्छा काम किया। समकालीन जनमत भी युवा को महत्व दे रहा है। पहले ये लोग भी आत्म मुग्ध थे।
प्रश्न – क्या सोशल मीडिया के दौर में मठाधीशी टूटी है? क्या सोशल मीडिया के दौर में संपादक अधिक लोकतांत्रिक हुए हैं?
उत्तर – सोशल मीडिया के आने से हिंदी में मठाधीशी टूटी है और पत्रिकाओं का भी वर्चस्व कम हुआ है। आप फेसबुक पर एक कविता लिखते हैं और हजारों लोग उसे देख लेते हैं और पढ़ लेते हैं। भले ही वे लाइक करें या कमेंट ना करें लेकिन आपकी रचना हजारों लोगों के सामने से गुजर जाती है। लेकिन किसी पत्रिका में रचना छपती है तो उसके छपने में बहुत समय लगता है और वह पत्रिका भी हजार-पाँच सौ या अधिकतम पाँच हज़ार की संख्या में ही निकलती है। ऐसे में सोशल मीडिया के आने से पत्रिकाओं का भी वर्चस्व टूटा है और संपादकों का भी अहंकार टूटा है। पहले पत्रिकाओं के संपादक भी नए लड़कों से सीधे मुंह बात नहीं करते थे। वह रचनाओं के चयन में भेदभाव करते थे और अपने चेले को प्राथमिकता देते थे। बहुत कम संपादक ऐसे हुए जिन्होंने ईमानदारी से अपने विरोधियों को भी छापा। हिंदी में हर पत्रिका चाहे ‘पहल’ हो या ‘हंस’ या ‘आलोचना’ या ‘तद्भव’, सबके अपने-अपने रचनाकारों का एक समूह है, वे रचनाकार उन पत्रिकाओं में ही अधिक छपते हैं। सोशल मीडिया के आने से बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म की पत्रिकाएं भी निकलने लगी और
कई तो उनमें से बहुत ही बेहतर काम कर रहे हैं। उनके हिट्स भी ज्यादा है। उनके सदस्य भी ज्यादा है। इसका नतीजा यह हुआ कि मठाधीशों की मठाधीशी कम हुई और साहित्य में लोकतंत्र विकसित हुआ। लेकिन यह भी सच है कि इस माध्यम को जो लोग इस्तेमाल करना नहीं जानते या कम जानते हैं या जो अपना प्रचार करने में कुशल नहीं है वह थोड़े कोने में पड़े हुए हैं। लेकिन बहुत सारे नए लेखक इस माध्यम का कुशलता से इस्तेमाल करते हैं और वह दिन रात अपनी ही रचना और किताबों के बारे में प्रचार में डूबे रहते हैं। सोशल मीडिया के आने से हिंदी के लेखक आत्म मुग्ध भी हुए है। वे दूसरों की रचनाओं के बारे में कम बात करते हैं, अपनी उपलब्धियां अपने पुरस्कार अपनी किताबों की चर्चा अधिक करते हैं। जबकि होना यह चाहिए कि हर व्यक्ति कम से कम सप्ताह में एक दूसरे रचनाकार की किताब या रचना के बारे में कोई पोस्ट लिखे या कोई जानकारी दें। इससे हम सब लाभान्वित होंगे। लेकिन सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोग अपना ही प्रचार करते हैं। फिर भी कुल मिलाकर पहले पत्रिकाओं का जो एकाधिकार था वह टूट गया है। अब कई लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पर छप कर लोकप्रिय हुए हैं जैसे सदानीरा, हिंदवी, समालोचन, शब्दांकन और आपके जानकी पुल आदि पर छपकर भी कई लेखक सामने आए हैं।
प्रश्न – आपको कविता के लिए भारतभूषण अग्रवाल पुरस्कार मिला और जिन दिनों हम दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे उन दिनों आपको कविता की बड़ी संभावना के रूप में देखते थे। आज हिंदी कविता की किसी सूची में आपका नाम नहीं दिखता। आप हिंदी कविता में स्वयं को कहाँ पाते हैं?
उत्तर – हिंदी साहित्य में सूचियां तो बनती बिगड़ती रहती हैं। मैँ सूचियों में शामिल होने के लिए नहीं लिखता, न उसकी परवाह करता हूँ। त्रिलोचन भी प्रगतिशीलों की लिस्ट पर कविता लिख चुके है। मैंने ऊपर ही लिखा है कि साहित्य में सत्ता विमर्श अधिक है। लिजलिजे लेखक अधिक हैं। चापलूस अधिक है। सच कहने से डरने वाले। मेरे लिए लेखन करियर नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो नामवर सिंह, राजेन्द्र यादव, अशोक वाजपेयी, विष्णु खरे के पास गया कि मेरी पांडुलिपि देख लें, भूमिका या फ्लैप लिख दें, मेरी किताब का विमोचन कर दें या मेरी किताब बड़े प्रकाशकों से छपवा दें। जिनके नाम सूचियों में हैं, उनके पीछे लेखक संगठन है, मठाधीशों के वरदहस्त भी हैं। हालांकि मुझे अपने बचाव में यह सब नहीं बोलना चाहिए। कवि को यह शोभा नहीं देता। यह भी सम्भव है कि लोगों को मेरा लिखा, मेरा व्यक्तित्व, मेरा आचरण न पसंद हो। उनकी नजर में मेरे लिखे में दम न हो। मैंने हमेशा अपनी कविता में अपनी बेचैनी को दर्ज किया है। बेबाकी के साथ। अपने समय समाज को रखने की कोशिश की है। कई बार लाउड भी हुआ। कई बार खराब भी लिखा। लेकिन मद्धम स्वर में गाकर बोर हो गया था। 2014 के बाद तीन संग्रह सत्ता के विरोध में आये। लगातार लिखता रहा, चाहे सरकार किसी की हो। कोई पार्टी हो। एक लेखक को अपने समय के अन्याय और दमन के खिलाफ जरूर लिखना चाहिए। मैंने अपनी कविता में खुद को कटघरे में रखा है। आत्मालोचना की है। श्रेष्ठ कविता, बढ़िया कविता के मॉडल के धोखे, भरम, मुगालते को भी जानता हूँ। मैं तो कवि-लेखक होने का दावा भी नहीं करता हूँ।मुझे बस सच लिखना है। खरी-खरी। लेकिन विष्णु खरे के दम्भ की तरह नहीं, सब पर हंटर चलाने वाले, कट्टर वामी लेखकों की तरह नहीं। लेकिन खरे साहब एक अच्छे कवि थे और उन्होंने जैनेंद्र पर, फिल्मों पर शानदार लिखा। कुछ सुंदर अनुवाद किये, इसलिए उनका सम्मान भी करता हूँ। मंगलेश जी और खरे साहब दोनों सुंदर गद्य भी लिखते थे। मंगलेश प्रिय कवि रहे। गद्य असद ज़ैदी का भी सुंदर है। इसलिए तमाम असहमतियों के बाद हम अपने लेखकों से प्यार करते हैं।
मेरी असहमतियां हैं लेखक समाज से, पर विनम्र असहमति। मेरा विश्वास साहित्य के लोकतंत्र में है। लेखक का मूल्यांकन उसके अवदान पर होना चाहिए पर साहित्य में न्यायपूर्ण मूल्यांकन नहीं है। बहुत सारे लेखक सूचियों से बाहर कर दिए गए। सबकी अपनी-अपनी सूचियां और अपने-अपने लेखक हैं।
मुझे लगता है कि लेखक को बेबाक, पारदर्शी और साहसी होना चाहिए। उसे अपने समय का सच लिखना चाहिए। नफा नुकसान देखकर नहीं लिखना चाहिए। तटस्थ रहने के नाम पर चुप्पी नहीं लगानी चाहिए।
प्रश्न – क्या आपको लगता है कि आपका पत्रकार आपके कवि पर हावी हो गया?
उत्तर – सम्भव है। करीब बीस साल संसद कवर किया। सत्ता को करीब से देखा। एक पत्रकार के रूप में, उसके गलियारे में घूमा। उसके छद्म पाखंड को देखा। ऐसे में मेरा पत्रकार हावी हो गया हो लेकिन हिंदी में कोई किसी को बारीकी से पढ़ता नहीं।
मेरे दो संग्रह के बाद शेष किताबें किसी ने पढ़ी नहीं। लोग फेसबुक से राय बनाते है। मैँ अपनी छवि नहीं बनाता बल्कि किसी छवि निर्माण का विरोधी हूँ। मैं रघुवीर सहाय के शब्दों में अपनी मूर्ति खुद ढहाता हूँ। लोग मेरे तंज को समझते नहीं। लोगों में सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं। मुझे आपने किसी लिट् फेस्ट, किसी संगठन, किसी अकेडमी, किसी फाउंडेशन में नहीं पाया होगा।मेरी रुचि नहीं इन सब में। हिंदी में बड़े-बड़े लेखकों के साथ ना इंसाफी हुई
है। वामपंथियों और कलावादी दोनों दोषी रहे हैं।
मैँ खुद को भीड़ से अलग दिखना चाहता हूं। गुटों और गिरोहों से बाहर।
प्रश्न – आप धीरे-धीरे हिंदी के साहित्यिक दुनिया के आलोचक क्यों होते गए?
उत्तर – पिछले दस साल से आलोचक हो गया हूँ पर किसी भी रचनाकार के खिलाफ नाम लेकर नहीं लिखा जैसा कुछ लोग लिखते हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत झगड़ा नहीं। बात व्यक्ति पर नहीं प्रवृतियों पर होनी चाहिए। मैँ क्रांति को लेकर मुगालता नहीं पालता। न दावा करता हूँ कि दुनिया को बदल दूंगा। फासीवाद से केवल मैँ लड़ रहा, यह मुगालता नहीं, यह प्रचार नहीं करता लेकिन कुछ लोग यह भ्रम पाले रखते हैं। वे एक दूसरे को ब्लॉक करते हैं। गंदी भाषा में हमले करते हैं। सम्बन्धों का कभी निर्वाह नहीं करते। स्क्रीन शॉट भेजते हैं। मॉर्फ़्ड वीडियो भेजते हैं। शराब पीकर गालियां देते हैं। मेरा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं, न निजी खुंदक। जिनका विरोध किया उसकी तारीफ भी की। उनका आज भी मुरीद हूँ। मेरा विरोध सैद्धांतिक है। वैसे मैं कोई संत नहीं। शुद्धतावादी नहीं। मैंने अवसरों को, पुरस्कारों को ठुकराया है। लेकिन यह कहकर मैँ खुद को नैतिक सिद्ध नहीं कर रहा, सबसे अलग नहीं पेश कर रहा। लोगों से असहमतियां हैं पर हिंदी के लेखक मेरे दुश्मन नहीं। हमें सत्ता से लड़ना है लेखकों से नहीं। इतनी समझ है मेरे भीतर।वाम का विरोधी नहीं हूँ बल्कि छद्म पाखंडी वामियों का विरोधी हूँ पर दक्षिण पंथियों के साथ हरगिज़ नहीं हूं। अवसरवादियों के साथ नहीं हूं। मेरी राजनीति साफ है।वैसे मैं खुद को दूध का धुला नहीं मानता। अपनी ईर्ष्या, लालच, वासना, कामना, लोभ का भी आलोचक हूँ। मुझे लगता है लेखक को पहले अपना आलोचक होना चाहिए। आत्मालोचना जरूरी है। लेकिन अधिकतर लेखकों ने मुल्लमा चढ़ा लिया है। उनमें सहजता, सरलता नहीं कुटिलता है, प्रदर्शन है। एक नकली बौद्धिकता है। एक बनावटी व्यक्तित्व है। विदेशी कविताओं का नकल है। आयातित भाषा और शिल्प।
प्रश्न – आपको लगता नहीं है जिस दौर में लेखक असहिष्णुता को लेकर मुखर हो रहे उस दौर में ख़ुद लेखकों की आपसी सहिष्णुता, आपसी सौहार्द भी कम हुआ है?
उत्तर – बिल्कुल सही कहा। असहिष्णुता के मुद्दे पर लेखकों की पुरस्कार वापसी का आज भी समर्थक हूँ। पर उनमें से कुछ लेखकों ने खुद असहिष्णुता का परिचय दिया है। हिन्दी के दो वरिष्ठ कवियों ने मेरे लिखे के कारण बातचीत करना बंद कर दिया। एक जमाना था जब आपसी विरोध के बावजूद लेखक बोलते थे। सातवें और आठवें दशक के दो कवियों के बीच मनमुटाव से वाकिफ हूँ पर सोशल मीडिया के दौर में फट से लोग ब्लॉक कर देते है। लेखिकाएँ भी ब्लॉक करती हैं पर यह भी सच है भाषा का स्खलन हुआ है। आलोचना भी हिंसक हुई है। महत्वकांक्षा, आत्म मुग्धता और सफलता बोध ने भी लेखक को असहिष्णु बनाया है। इसमें युवा पीढ़ी भी शामिल है। पूरे समाज मे प्रेम और सौहाद्र कम हुआ है। एक अजीब दौड़ में शामिल हैं हम सभी। सेलिब्रिटी बनने की चाह। वाम धारा के लोग भी कट्टर और संकीर्ण हैं तो कलावादी भी अपने दायरे से बाहर नहीं आना चाहते। स्वस्थ संवाद नहीं है। साहित्य में इस जड़ता को कोई तोड़ना नहीं चाहता। कटुताएँ काफी बढ़ गयी हैं। मैंने इस विषय पर बहुत सी कविताएं लिखीं।
प्रश्न – आपने स्त्रियों पर बहुत सारी कविताएं लिखीं और प्रेम कविताएं तो बहुत सारी ही लिखीं। आपके असफल प्रेम के किस्से भी चर्चित रहे पर प्रेम में यौनिकता को लेकर हिंदी में कम कविताएं क्यों लिखी गईं? इस पर आपकी क्या राय है?
उत्तर – हिंदी में प्रेम और यौनिकता को लेकर विचित्र किस्म की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलती हैं। मोरल पुलिसिंग अधिक है। एक तरह का आंतरिक सेंसरशिप काम करता है। नैतिकता का चाबुक लहराता रहता है। कब आपकी पीठ पर न पड़ जाए। अगर आप आज प्रेम कविता लिखते हैं तो तंज कसा जायेगा कि फासीवाद के दौर में प्रेम कविता लिखते है। दुनिया के सारे बड़े कवियों ने प्रेम कविताएं लिखीं। नाज़ीवाद के दौर में भी। फिल्में बनी। युद्ध मे भी प्रेम। क्रांतिकारी कार्यों में भी प्रेम लेकिन हिंदी में प्रेम कविता लिखना पिछड़ा माना जाता है। मेरा तो मानना है बिना प्रेम कविता लिखे कोई खाक कवि होगा। अगर आप प्रेम की बात करें और यौनिकता को बीच में ले आएं तो हाय तौबा मच जाएगी। मांसल प्रेम कविता लिखना गुनाह है जबकि जीवन मे हर कोई मांसल प्रेम करता है। हिन्दी समाज चाहता है कि आप ब्रह्मचारी बनकर प्रेम कविता लिखें। संत और ऋषि बनकर प्रेम कविता लिखें। प्रेम के आध्यात्मिक अनुभव पर लिखें।
प्रेम हमारे समाज मे एक जटिल घटना है। प्रेम होना आसान नहीं। उसका भी एक पावर डिस्कोर्स है, सोशल डिस्कोर्स है। इसलिए प्रेम के रास्ते मे अड़चने बहुत हैं। दुश्वारियां बहुत हैं। ख़ैर। प्रेम संसार की सबसे सुंदर और जरूरी चीज है। उसमें अगर यौनिकता हो तो और भी सुंदर। इससे अधिक मानवीय चीज़ और क्या हो सकती है। मेरी एक कविता है “मैँ संसार की सभी स्त्रियों से प्रेम करता हूँ” पर इसे अभिधा में न लें, व्यंजना में लें। स्त्री और पुरुष दोनों को प्रेम चाहिए, सेक्स भी चाहिए, लेकिन आप अपनी कविता में ये सब लिख दें तो लोग आपको काम लोलुप कवि कह देंगे। बहरहाल, मेरे लिए प्रेम एक तरह का यूटोपिया है। खुद को जानने पहचानने अपने अहं को जीतने की एक प्रक्रिया। लेकिन हम लोग अपने क्रोध ईर्ष्या लालच वासना को कहाँ जीत पाते है। प्रेम कविता इकहरी नहीं होनी चाहिए। उसमें द्वंद भी हो। उसमें आत्मसंघर्ष हो। देह को लेकर भी एक द्वंद हो। क्योंकि प्रेम एक रैखीय कार्रवाई नहीं। उसमें कई आयाम हैं। प्रेम एक भाव है। क्षण है। बस। असफल प्रेम में प्रेम की अधिक तीव्रता है।
प्रेम एक राजनीतिक सामाजिक कार्रवाई भी है। वह केवल निजी प्रसंग और व्यक्तिगत कार्रवाई नहीं। केवल भावनात्मक और दैहिक नहीं। मेरा मानना है कि असफल प्रेमी अच्छा कवि होता है। मंगलेश जी भी असफल प्रेमी थे। हम दोनों ने असफल प्रेम के किस्से संकेतों में शेयर किए हैं। प्रेम भी अपने समय के सत्ता विमर्श से संचालित होता है। प्रेम बहुत जटिल चीज़ है मेरे लिए। इतना दांव पेंच मुश्किल है मेरे लिए।
प्रश्न – आपने लेखकों का एक संयुक्त सांस्कृतिक मोर्चा बनाने का प्रयास किया पर वह विफल क्यों हो गया?
उत्तर – वाम लोग उस मोर्चे में अशोक जी को नहीं चाहते थे। अजय सिंह, वीरेंद्र यादव और कात्यायनी जैसे लोग अशोक जी को पसंद नहीं करते। मेरा मानना था मोर्चा व्यपाक हो। उसमें लिबरल्स भी हों। आज अशोक जी मोदी के खिलाफ लगातार बोल और लिख रहे हैं। लेकिन वाम लेखक संघ अपने बैनर तले हर कार्यक्रम करना चाहते हैं। हमने कहा कि हम एक संयुक्त बैनर के तले काम करें पर वे नहीं माने। हमने कहा वाम लेखक अपना नाम नीचे दें पर उन्होंने अपने बैनर तले अपना नाम जारी रखा। वे न्यूनतम शर्तों का भी पालन नहीं करना चाहते थे। वाम दल कभी एकजुट नहीं हो सकते। उनकी पार्टियां कवर करता रहा। वे बार- बार विलय की एक मोर्चा बनाने की बात करते रहे पर एक जुट नहीं हो पाए। कुछ संयुक्त कार्यक्रम किए पर उसका विस्तार नहीं हुआ। जलेस, प्रलेस, जसम के पदाधिकारियों की दुकान बंद हो जाएगी मोर्चा बनने से। उन्हें इस फासीवाद से लड़ना होता तो वे मोर्चा बनाते। कुछ कार्यक्रम किए पर व्यापक असर नहीं हुआ। खुद असगर वज़ाहत गम्भीर नहीं थे। उनका जो हाल हुआ वह आपके सामने है।
प्रश्न – हिंदी में रॉयल्टी के मुद्दे पर लेखक एकजुट क्यों नहीं?
उत्तर – विनोद कुमार शुक्ल की रॉयल्टी का मुद्दा उठा तो हमने अशोक जी से कहा इस पर एक कार्यशाला रखी जाए। लेखक, प्रकाशक, वकील सबको सामने रखकर बात हो। उन्होंने दिलचस्पी नहीं ली। लेखक संगठनों से कहा वे फिर आगे नहीं आये। राजकमल प्रकाशन की आलोचना करने से सभी बड़े लेखक चुप रहे। असल में कोई बड़े प्रकाशक से लड़ना नहीं चाहता। गगन गिल ने लड़ाई लड़ी तो लेखिकाओं ने भी उनका साथ नहीं दिया। वे अब राजकमल से मिल गयीं। ऐसे में कोई इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहता। प्रकाशक नाराज़ हो गया तो किताब कैसे छपेगी। यह मामला है। बड़े प्रकाशकों ने लेखकों को चंगुल में ले लिया है। लेखक संगठनों से जुड़े लोगों का नेक्सस है उनके साथ। अगर आप विरोध करें तो आपका पत्ता साफ हो जाएगा। विष्णु खरे ने थोड़ी हिम्मत जताई थी पर पहले तो वे खुद प्रकाशकों के साथ थे। प्रकाशक उन्हें लंदन ले गया था। जब उन्होंने अपनी किताब को दूसरे प्रकाशन के नाम से छाप कर बेचते हुए पाया तब वे उस प्रकाशक से नाराज़ हुए। आखिर बिल्ली के गली में घण्टी कौन बांधे। मैँ खुद 10 प्रकाशक बदल चुका हूं।
प्रश्न – आपने स्त्री दर्पण आखिर क्यों शुरू किया क्या इसके पीछे आपकी कोई निजी महत्वाकांक्षा थी या आपका कोई हिडन एजेंडा है?
उत्तर – प्रभात जी शायद आपको पता हो कि रेणु की जन्म शती जब शुरू हो रही थी तो मैंने गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक कार्यक्रम आयोजित किया था और वहां कुमार प्रशांत, अशोक वाजपेयी भी आए थे। तब हम लोगों ने फैसला किया था कि हम लोग रेणु की जन्म शती देश भर में मनाएंगे और इसके लिए एक राष्ट्रीय समिति भी गठित की गई थी। लेकिन कुछ दिन के बाद ही कोविड के कारण लॉकडाउन हो गया। अब समस्या थी कि हम उनकी जन्म शती कैसे मनाएँ। तब मेरे मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना हम लोग फेसबुक पर रेणु की जन्म शती मनाने का सिलसिला शुरू करें और इसके लिए मैंने मैला आँचल के नाम से एक ग्रुप बनाया। उस समय अनिल करमले भी साथ में थे और उसे ग्रुप के माध्यम से हम लोगों ने हर सप्ताह एक लेक्चर का आयोजन किया और पूरे साल भर यह सिलसिला चलता रहा। देश के करीब 60 लेखकों ने रेणु के बारे में अपने व्याख्यान दिए। इसका नतीजा यह हुआ कि कोविड में लोगों का आपस में संवाद हुआ, उन दिनों कोई अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था और हम लोग काफी बेचैनी की स्थिति में थे। यह एक नया प्रयोग था। पर रेणु की जन्म शती अभूतपूर्व ढंग से मनाई गई और उसके बाद नतीजा यह हुआ की कोविड में 14-15 पत्रिकाओं के विशेषांक रेणु पर निकले। माटी पत्रिका का संपादन मैंने किया। हिंदी साहित्य में यह पहली घटना होगी जब किसी लेखक की जन्म स्थिति वर्ष में इतनी पत्रिकाओं के अंक एक साथ निकले और करीब 500 से अधिक लोगों ने रेणु पर लिखा। जब लॉकडाउन थोड़ा रिलैक्स हुआ तो रेणु की जन्मशती के अंत में हमने फिर गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक आयोजन किया और 13-14 पत्रिकाओं का एक साथ लोकार्पण किया। जब यह सब संपन्न हो गया तो मेरे मन में ख्याल आया कि अब क्या किया जाए क्योंकि रेणु के कार्यक्रमों को साल भर में करीब सात आठ लाख लोगों ने देखा था। फिर मैंने सोचा कि हम स्त्रियों के लिए एक ग्रुप बनाते हैं और उनके साहित्य के बारे में विचार विमर्श शुरू करते हैं। तब मैंने स्त्री दर्पण नामक एक ग्रुप बनाया और धीरे-धीरे इसमें 13500 सदस्य हो गए पिछले 5 वर्षों में। रेणु वाले ग्रुप में तो करीब 3000 ही लोग सदस्य बने थे। स्त्री दर्पण, रेणु के ग्रुप से ज्यादा लोकप्रिय हो गया और यहां हमने अनेक कार्यक्रम किये। इस ग्रुप के साथ-साथ मैंने स्त्री दर्पण नाम से महिला लेखन की पहली बार एक अलग वेबसाइट बना दी, जिस पर आज की तारीख में 300 से अधिक लेखिकाओं के पेज बने हैं और काफी कुछ सामग्री हमने उसे पर डाली है। 100 की संख्या में वीडियो भी हैं। ग्रुप पर कई सारी गतिविधियां शुरू हो गईं। हमने करीब 40-50 लेखिकाओं के जन्मदिन पर आयोजन किया। उनके इंटरव्यू हुए। उनके बारे में लेख लिखे गए। उनकी रचनाओं का पाठ हुआ और वीडियो आदि भी बने। यह भी हिंदी साहित्य की पहली घटना थी। इतनी बड़ी संख्या में हिंदी की लेखिकाओं का जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया। क्योंकि आमतौर पर हिंदी में पुरुष लेखक का ही जन्मदिन मनाये जाने की परंपरा रही है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी का कभी जन्मदिन नहीं बनाया गया था, लेकिन स्त्री दर्पण ने यह काम किया। हमने रामेश्वरी नेहरू के जन्मदिन पर भी कार्यक्रम आयोजित किया। बाद में तो हमने इन दोनों पर सभागार में भी समारोह आयोजित किया जबकि उन पर आज तक हिंदी की दुनिया में कोई कार्यक्रम ही आयोजित नहीं किया गया था। स्त्री दर्पण की लोकप्रियता दिन-प्रति दिन बढ़ती गई और इस मंच से हमने अब तक करीब 15 16 सीरीज भी शुरू किये। सबसे पहले साहित्यकारों की पत्नियां जो काफी लोकप्रिय हुई और उसकी किताब भी निकली वह पूरी श्रृंखला अभी भी वेबसाइट पर लगी हुई है। उसके बाद सविता ने प्रतिरोध की कविता नामक एक श्रृंखला शुरू की उसकी भी किताब बनी है और वह भी वेबसाइट पर मौजूद है। श्री विलास सिंह ने दक्षिण अफ्रीकी कवित्रियों की कविताओं की एक सिरीज़ शुरू की। हिंदी में पहली बार अफ्रीकी कवित्रियों की श्रृंखला शुरू हुई और करीब 20 कवित्रियों की कविताएं हम लोगों ने पेश की। उसके बाद तो अनेक श्रृंखलाएं हम लोगों ने पेश की। पिछले दिनों रीता रामदास राम ने पुरुषों की स्त्री विषयक कविताओं की सिरीज़ पेश की और हमारी अम्मा नामक एक श्रृंखला पेश की थी। अब इन दोनों की पुस्तकें आ गई हैं। इस दौरान हमने एक स्त्री लेखा नाम से पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया और उसके अब तक 7 अंक निकल चुके हैं। पहली बार हमने हिंदी में स्त्री नवजागरण पर अंक निकाला। इसके अलावा स्त्री वार्षिकी भी निकाली। यह एक नया प्रयोग था। हिंदी में स्त्रियों की कोई वार्षिकी नहीं निकली थी। साथ ही साथ गीतांजलि श्री, मृदुला गर्ग पर भी हमने अंक निकाला और स्त्री की पुस्तकों पर भी एक अंक केंद्रित किया। गीतांजलि जी को बुकर मिला तो 20 दिन में अंक निकाल दिया। अभी स्त्री रंगमंच पर एक अंक निकाला है और अगला अंक हमारा कृष्णा सोबती पर केंद्रित है। इसके अलावा हमने स्त्री से जुड़े मुद्दों पर कई आयोजन भी किये सभागारों में और धीरे-धीरे स्त्री दर्पण का प्रचार-प्रसार हुआ और अभी यह एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म बन गया है।
इस मंच की खासियत यह है कि यह सभी स्त्रियां चलाती हैं और पत्रिका भी स्त्रियों के सहयोग से चलता है। रामेश्वरी नेहरू ने भी स्त्रियों के सहयोग से स्त्री दर्पण निकाला था। इसलिए हम लोगों ने भी इस प्लेटफार्म और पत्रिका में स्त्रियों को साथ लिया। जहां तक निजी महत्वकांक्षा की बात है इस मंच पर मैं अपना कोई फोटो नहीं डालता, किताब का प्रचार नहीं करता, अपना नाम नहीं डालता। सारे पोस्ट लिखता हूँ पर स्त्री दर्पण मंच के नाम से पोस्ट होता है। पोस्ट भी टीम के लोग करते हैं। यहां तक कि मैं जो कोई आयोजन करता हूं उसमें मंच पर नहीं होता हूं और ना ही कार्यक्रम का संचालन करता हूं। यहां तक कि किसी पोस्टर में मेरा नाम नहीं होता। इसलिए महत्वकांक्षा का सवाल नहीं। रही बात हिडेन एजेंडा की तो वह भी मैं बता दूं, हमारा कोई एजेंडा नहीं है। न हम कलावादियों और न वामपंथियों का प्रचार करते हैं। किसी एक लेखिका को महामंडित करने नहीं आये हैं। हम कोई स्त्री विमर्श का झंडा लहराने नहीं आए हैं और ना कोई श्रेय लेने आए हैं कि हम स्त्रियों के मुक्ति दाता है। हमें तो कुछ काम करना है जो अब तक साहित्य में नहीं हुआ था और इस काम को पूरा करने के लिए हमारी टीम जुटी हुई है। हमने मोबाइल के जरिए ही महादेवी वर्मा पर एक नाटक तैयार किया। रेणु की पत्नी पर एक नाटक तैयार किया, मुक्तिबोध पर भी एक नाटक तैयार किया। साथ ही साथ शिवरानी देवी पर भी हमने एक नाटक लिखा जो आकाशवाणी से प्रचारित प्रसारित किया गया। इस तरह हम लोगों ने अपने हर काम में स्त्री लेखन को जोड़ा है। आपको हर तरह की जानकारी हम इस प्लेटफार्म से दे रहे हैं। अगर किसी लेखिका को कोई महत्वपूर्ण पुरस्कार मिलता है, किसी का निधन हो जाता है, कोई महत्वपूर्ण समारोह आयोजित होता है तो उसकी सूचना हम यहां देते रहते हैं। लेकिन हमारे मंच की एक शर्त है। हम यूं ही किसी की कोई रचना इस पर नहीं लगाते हैं और किसी किताब का प्रचार तभी करते हैं अगर वह बहुत विशिष्ट हो। हमने किताबों पर भी चर्चा का कार्यक्रम आयोजित किया और पारुल बंसल ने करीब 25-26 किताबों पर चर्चा आयोजित की। अलका तिवारी, सुधा तिवारी, रीता दास राम, पारुल बंसल, अनुराधा, सोमा बनर्जी, कल्पना मनोरमा हमारी टीम की सदस्य है और इन सब के सहयोग से हम यह काम कर रहे हैं।
कल्पना मनोरमा हिंदी की वरिष्ठ लेखिकाओं की भेंटवार्ता की सिरीज़ चला रही है। अनुराधा कवित्रियों की सिरीज़ चला रही है। सुधा तिवारी ने अनुवाद की सिरीज़ चलाई। अलका तिवारी नवजागरण स्त्री प्रश्न पर काम करती हैं। अब साहित्य समाचार पारुल जी कर रही हैं। इस तरह 5 साल में हमने सैकड़ो कार्यक्रम आयोजित किये जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। स्त्री दर्पण अब एक प्लेटफार्म नहीं बल्कि आंदोलन बन चुका है, डिजिटल आंदोलन, क्योंकि हमारे प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में शायद ही साहित्य, संस्कृति के लिए कोई जगह नहीं बची है। मैं खुद 40 वर्ष पत्रकार रहा हूं और मैंने पाया है कि सबसे कम अगर स्पेस मीडिया में किसी का है तो संस्कृति का है। वह भी भूमंडलीकरण और बाजार के दौर में खत्म हो चुका है ।तो क्यों ना हम लोग इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का इस्तेमाल साहित्य के प्रचार-प्रसार के लिए करें और इसीलिए हमने यह प्लेटफार्म शुरू किया है। हम सबसे अनुरोध करते हैं कि आप कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आएं और इस प्लेटफार्म पर उसे चलाएँ। कई लोग सामने आए भी हैं और देखना है कि यह ग्रुप कैसे चलता है और कितना काम कर पाता है।
प्रश्न – आप अपने समकालीन लेखकों के बारे में क्या सोचते है? नवें दशक की कविता ने हिंदी को क्या दिया? उत्तर – देखिए प्रभात जी, मैं जब 1982 में दिल्ली आया था तो उन दिनों तेजी ग्रोवर, गगन गिल, हरिश्चंद्र पांडेय, अनूप सेठी, उदयन वाजपेयी, स्वप्निल श्रीवास्तव, कृष्ण कल्पित, कात्यायनी ,देवी प्रसाद मिश्र, संजय चतुर्वेदी, नवल शुक्ल, कुमार अंबुज, राजेन्द्र उपाध्याय, निर्मला गर्ग, अनामिका, सविता सिंह, बद्री नारायण, लालटू, सत्यपाल सहगल, निलय उपाध्याय, एकांत श्रीवास्तव आदि कविता में सक्रिय थे। इससे पहले मंगलेश जी, उदय प्रकाश, अरुण कमल, राजेश जोशी, विष्णु नागर, असद ज़ैदी के संग्रह आ गए थे। 1992 में 13 कवियों का संग्रह आया था। इसमें मेरा भी संग्रह आया था। इससे पहले चार कवि “होना शुरू होना” में आये थे। संजीव क्षितिज, उदयन वाजपेयी, शिरीष ढोबले, ध्रुव शुक्ल भी थे। रमन मिश्र ने एक किताब संपादित की थी जिसमें हरिश्चंद्र पांडेय, देवी, बोधिसत्व, बलि सिंह और खुद रमन मिश्र आदि भी थे। इस तरह साहित्य में एक नया परिदृश्य बन रहा था।
इनमें से कई कवि आज भी लिख रहे हैं और कुछ लोग तेजी से उभरे और आज स्थापित कवि हैं। इन कवियों की अलग अलग राजनीति है ,एजेंडा है। कुछ आज भी सत्ता के विरोध में हैं, कुछ सत्ता के साथ हैं। कुछ कट्टर और संकीर्ण भी हैं। कुछ लिबरल्स हैं। कुछ करियरवादी भी हैं। कुछ मानवतावादी होने की आड़ में सभी मंचों पर विद्यमान हैं। कुछ स्वतंत्र विचारों वाले हैं। कुछ संघ समर्थक भी हो गए। देवी प्रसाद मिश्र और कुमार अम्बुज इस पीढ़ी के प्रतिनिधि स्वर बनकर उभरे। स्त्रियों में तीन स्वर प्रतिनिधि बने। गगन गिल, अनामिका और कात्यायनी। ये तीन तरह की राजनीति के सौंदर्यबोध और यथार्थ बोध को चित्रित करती हैं। आठवें दशक के दौर में कोई कवयित्री नहीं थी। शुभा थीं जरूर पर आजतक उनका संग्रह नहीं आया। लेकिन नवें दशक में पांच कवयित्रियाँ थी। यह एक नयी परिघटना थी। एक नया पॉइंट था। सोवियत संघ का विघटन, नई आर्थिक नीति और भूण्डलीकरण की शुरुआत इसी दौर में हुई। इसलिए आठवें दशक से भिन्न चुनौतियां थीं। पहले की तरह पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स का नारा नहीं चला। जो लोग इस नारे को उठाते रहे उनकी कलई खुल चुकी थी। वे सत्ता प्रतिष्ठानों से पुरस्कार लेते रहे उनके समारोहों में जाते रहे। मठाधीशों के निकट रहे।
मैँ लांग नइंटीज़ की बहस में नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन मेरा भी मानना है कि बुनियादी रूप से नवें दशक की कविता का कोई नया प्रस्थान बिंदु नहीं था और वह पिछली कविता का विस्तार था। एक्सटेंशन था। आठवें दशक के कवि खुद को वामपंथी और प्रतिबद्ध होने का दावा करते थे। उनके अंतर्विरोध भी सामने आए। नवें दशक में कोई दावा नहीं था। इस दौर में दो तीन तरह की नई काव्य प्रवृत्तियाँ दिख रही थीं जो बाद में साफ साफ दिखने लगी। कुछ लोग वाम पर हमले करते हुए दक्षिण पंथ के खेमें में चले गए। संघ परिवार के निकट हो गए। आज की तारीख में कौन कहाँ खड़ा है, सबको पता चल गया है। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो नवें दशक के कवि सत्ता प्रतिष्ठानों से दूर रहे। वैसे अंतर्विरोध आठवें दशक के कवियों में भी थे। मैं आठवें बनाम नवें की बहस नहीं खड़ा करना चाहता। आज जिस मुकाम पर देश खड़ा हुआ है उसका मुकाबला हम सबको करना है। एक प्रगतिशील धर्मनिरपेक्ष मंच बनाकर राजनीतिक दलों की तरह नहीं जिसमें भ्रष्ट कांग्रेसी और समाजवादी भी हैं। सत्ता लोलुप भी हैं।
विजय कुमार ने आठवें दशक पर लिखा लेकिन नवें दशक की कविता पर सुविचारित लिखा नहीं गया। मेरा मानना है। 1980 से 2000 तक के बारे में लिखा जाए।
प्रश्न – 21 वीं सदी के लेखन के बारे में आपकी क्या राय है?
उत्तर – 21वीं सदी में हिंदी लेखन में विस्फोट हुआ है। मैंने दस पंद्रह साल पहले नई दुनिया में एक लेख लिखा था। बहुत बड़ी संख्या में नये लेखक और लेखिकाएँ सामने हाँ। हम लोगों ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इतनी बड़ी संख्या में लेखकों की नई पीढ़ी सामने आएगी। इस पीढ़ी में भी कई तरह की प्रवृत्तियां काम कर रही है। वैसे हर दौर में कई तरह की प्रवृत्तियां काम करती रही हैं, चाहे छायावाद हो या नई कविता या अकविता का दौर हो। अभी 21वीं सदी की कविता के बारे में विचार विमर्श शुरू नहीं हुआ है पर उसकी काव्य प्रवृत्तियां अलग-अलग दिखाई पड़ने लगी हैं। एक तरफ वैसे कवि हैं जो अपनी कविता में विदेशी कवियों के मुहावरे की तरह कविता लिखते हैं और उसे अमूर्त तथा रहस्यमय बनाने की कोशिश करते हैं।एक दूसरी प्रवृत्ति यह हैं कि वह यथार्थ से तीखा मुठभेड़ करते हैं और अपने समय को अपनी कविता में दर्ज करते हैं। एक तीसरी प्रवृत्ति यह भी है कि जो इन दोनों के बीच खड़ी है वह पूरी तरह किसी पलड़े की तरफ झुकी हुई नहीं है, वह अस्मिता विमर्श, अपनी पहचान और अपने निर्माण की प्रक्रिया में है और अपना स्वर पूरी तरह खोज नहीं पाई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि 10 साल में 21वीं सदी की कविता का परिदृश्य बहुत साफ हो जाएगा और कौन कहां खड़ा है यह सब को पता चल जाएगा। जैसे 90 दशक की कविता के कवियों के बारे में स्थिति अब साफ हो गई है। 21वीं सदी का दौर तो 90 दशक के दौर से भी ज्यादा चुनौती पूर्ण है और पिछले 10 सालों में जिस तरह देश की स्थिति बनी है, उसमें ये चुनौतियां अधिक महत्वपूर्ण हैं लेकिन यह भी सच है कि इन चुनौतियों का सामना करने वाली कविताएं कम लिखी जा रही हैं। जितना भयावह समय है उसमें रचनाकार को धारदार रचनाएं लिखनी चाहिए लेकिन बहुत कम कवि ऐसी तीखी और धारदार कविताएं तथा कहानी लिख रहे हैं। कुछ प्रतिभाशाली लोग अपनी ऊर्जा कौतुक विवाद खींचतान में बर्बाद कर रहे हैं। मुझे इस पीढ़ी से उम्मीद है और मैं उनकी कविताएं पढ़ता रहता हूं। मैंने हर कवि के एक दो संग्रह तो पढ़ें हैं, उनकी रचना में मेरी दिलचस्पी रही है। मैंने खुद “परिंदे” का एक स्त्री कविता अंक निकाला था। लेकिन यह सच है कि उनके साथ पिछली पीढ़ी का संवाद अभी कम है। इस पीढ़ी के कुछ कवि – कवयित्रियाँ आत्म मुग्धता के शिकार हैं। मैँ खुद को लेखक होने का दावा नहीं करता। ये सारी बातें एक पाठक के रूप में कह रहा हूँ। बाबुषा, लवली, लीना मल्होत्रा, अनुराधा सिंह के अलावा नेहा नरुका, प्रिया वर्मा, सपना भट्ट अनुपम, रूपम आदि की भी कविताएं पढ़ता हूँ। शिरीष मौर्य, अविनाश, सुधांशु फिरदौस, व्योमेश, महेश पुनेठा, गीत चतुर्वेदी, विहाग वैभव, पवन पराग आदि की कविताएं भी पढ़ता रहता हूँ।
प्रश्न – बिहार के पुराने लेखकों के योगदान का मूल्यांकन नहीं हुआ। उनकी उपेक्षा हुई?
उत्तर – बिहार के पुराने लेखकोँ और संस्थाओं के योगदान के बारे में हिंदी साहित्य में न तो कभी कोई चर्चा हुई और नहीं उनका मूल्यांकन हुआ। बिहार में बिहार बंधु अखबार, खडग विलास प्रेस, पुस्तक भंडार और आरा की नागरी प्रचारिणी सभा का बहुत बड़ा योगदान है। इनके बिना बिहार में हिंदी नवजागरण की कल्पना नहीं की जा सकती है लेकिन जब मैं दिल्ली आया तो यहां कभी भी न तो उनकी चर्चा हुई और न किसी ने नाम तक न लिया।
रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, विश्वनाथ त्रिपाठी, मैनेजर पांडेय आदि प्रेमचंद, रामचन्द्र शुक्ल, निराला हजारी प्रसाद द्विवेदी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा और गंगा पुस्तक माला, हिंदी साहित्य सम्मेलन, लहरी बुक डिपो, सरस्वती प्रेस, भारती भंडार आदि का जिक्र करते रहे लेकिन उन्होंने रामदीन मिश्र, रामलोचन शरण, आरा नागरी प्रचारिणी सभा, सदल मिश्र, अयोध्या प्रसाद खत्री, राजा राधिका रमण, शिवपूजन सहाय, बेनीपुरी जी का कभी
जिक्र नहीं किया। उन्होंने बिहार के आलोचकों नलिन बिलोचन शर्मा, डॉक्टर नागेश्वर लाल, सुरेंद्र चौधरी और
चंद्रभूषण तिवारी का भी कभी सार्वजनिक रूप से नाम नहीं लिया। अगर यह तीनों ना होते तो बिहार में आलोचना की नींव नहीं पड़ती। लेकिन दिल्ली के दरबार में उत्तर प्रदेश के लेखकों की ही चर्चा होती रही। गद्य के निर्माण में विश्वनाथ जी ने NCERT के लिए एक इतिहास लिखा तो अमरकांत का नाम लिया पर राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह, शिवपूजन सहाय, बेनीपुरी का नाम तक नहीं लिया। हमने उनका ध्यान दिलाया तो उन्होंने अपनी किताब में संशोधन किया। गुलेरी की कहानी “उसने कहा था” की बहुत चर्चा हुई हिंदी में लेकिन उससे 4 साल पहले राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह “कानों में कंगना” जैसी चर्चित कहानी लिख चुके थे। और मेरा तो मानना है कि “कानों में कंगना”, “उसने कहा था” से ज्यादा बढ़िया कहानी है।लेकिन हिंदी में उसकी चर्चा नहीं। इसी तरह 1926 में प्रकाशित शिवपूजन बाबू की “देहाती दुनिया” को लोग नहीं जानते जिसने हिंदी में आंचलिक लेखन की नींव रखी। मैला आँचल से 28 साल पहले यह आया था। अगले साल इस उपन्यास के 100 साल हो जाएंगे। शिवपूजन सहाय के जन्मशती वर्ष 1998 में परमाननंद श्रीवास्तव दूधनाथ सिंह, विजय मोहन सिंह आदि ने उसकी पहली बार चर्चा की तो लोग थोड़ा जानने लगे अन्यथा लोग जानते तक नहीं है और तो और बिहार के लोग भी बिहार के लेखकों के योगदान के बारे में नहीं जानते हैं। वे केवल नाम जानते हैं। शिवपूजन जी किसान आंदोलन में भी सक्रिय थे। अब कुछ ऐसे पत्र सामने आए हैं। बेनीपुरी जी के साथ भी यही हादसा हुआ। उनको लोग नाम से जानते तो थे पर उनके कार्यों से परिचित नहीं थे। सुरेश शर्मा ने उनकी रचनावली न निकाली होती तो लोग बेनीपुर के योगदान को नहीं जानते। वे राहुल जी से अधिक बार जेल गए, किसान आंदोलन में भाग लिया, समाजवादी आंदोलन में भाग लिया, समाजवादी पार्टी के संस्थापकों में से थे। लेकिन हमारे वामपंथी संगठनों ने उनकी कभी सुध नहीं ली। वे केवल राहुल जी का ही नाम लेते रहे। वे नागार्जुन की चर्चा करते रहे लेकिन नागार्जुन जिन बेनीपुरी के शिष्य थे उनका कोई नाम लेवा नहीं। उन्होंने कहानी, उपन्यास, यात्रा संस्मरण लिखे, शानदार गद्य लिखा और नाटक लिखा।13 पत्रिकाओं का संपादन किया उनका कोई नाम लेवा नहीं। नाटकों में भी नेमीचंद जैसे लोग आम्रपाली नाटक का नाम नहीं लेते थे। रामविलास जी ने मरने से पहले बेनीपुरी पर किताब संपादित की और उन्हें माखनलाल चतुर्वेदी और गणेश शंकर विद्यार्थी के समकक्ष रखा। लेकिन यह सब बहुत बाद में हुआ जब उनकी जन्म शती मनाई गई। मैंने सुरेंद्र मोहन और मस्तराम कपूर के साथ मिलकर बेनीपुरी की जन्म शती देश भर में मनाई थी। लेखकों की एक समिति भी बनाई थी जिसके तत्वावधान में कई कार्यक्रम हुए। बेनीपुरी का रचना संचयन भी साहित्य अकादमी से आया।
अब जाकर बेनीपुरी के बारे में लोगों की आंखें खुली हैं लेकिन अभी भी दूसरे अन्य लोगों के बारे में वे नहीं जानते। अब तो नलिन जी की रचनावली वाली आ चुकी है। उनके आलोचक महत्व को अब जाकर पहचान मिली है, जब एक छात्र अभय आनंद ने उन पर शोध कार्य किया और उनकी रचनावली तैयार की। लेकिन वह भी किसी और के नाम से छपी है। यह खुशी की बात है। उनकी रचनावली उनकी पत्नी कुमुद शर्मा ही निकालना चाहती थीं और उन्होंने राम विलास शर्मा से भूमिका लिखवाई थी। लेकिन उसकी सारी सामग्री बिहार के एक लेखक ने खो दी। बाद में जाकर कुछ साल पहले अभय आनंद के प्रयासों से रचनावली निकल पाई। गोपेश्वर सिंह ने भी नलिन जी पर किताबें लिखीं लेकिन इससे पहले बिहार के आलोचकों नंदकिशोर नवल या खगेन्द्र ठाकुर रविभूषण ने बिहार के लेखकों पर कोई किताब नहीं लिखी और अगर लिखी तो केवल दिनकर पर नवल जी ने। दिनकर का नाम ज्यादा हुआ लेकिन दिनकर ने खुद लिखा है कि ‘अगर बेनीपुरी न होता तो दिनकर न होता।’ दिनकर ने शिवपूजन जी के बारे में लिखा कि अगर शिवजी की सोने की मूर्ति बनवाई जाए और उस पर चांदी का वर्क चढ़ाया जाए तब भी उनके योगदान की भरपाई नहीं की जा सकती। बेनीपुरी ने शिवपूजन बाबू को अपना “साहित्यिक पिता” माना था। मैला आँचल के विमोचन समारोह की अध्यक्षता शिवपूजन बाबू ने की। उन्होने हिमांशु श्रीवास्तव और रेणु को युवा लेखक पुरस्कार भी दिया।आज हिमांशु जी को कोई नहीं जानता। बिहार के किसी भी लेखक का मूल्यांकन हुआ ही नहीं। रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना शिवपूजन सहाय को निराला के कहे पर समर्पित किया पर मतवाला का नायक निराला को बनाया। जबकि महादेव प्रसाद सेठ लिख चुके हैं कि मतवाला के मेरुदंड शिवपूजन जी थे। शिवपूजन सहाय ही बिहार में हिंदी नवजागरण के नायक थे। उन्होंने जितना निःस्वार्थ काम किया है, हिंदी की सेवा की, हिन्दी में बहुत कम लोग ऐसे हुए जो दूसरों के लिए जीते रहे। बच्चन ने भी उन्हें अपना साहित्यिक पिता माना था। निराला ने रामविलास जी के शब्दों में शिवपूजन जी ने राधा मोह गोकुल जी को बड़ा भाई माना। साहित्य, भाषा, पत्रकारिता के ये लोग निर्माता थे लेकिन वामपंथी कलावादी आलोचकों ने नाम ही नहीं लिया। बिहार के लेखकों के बारे में बिहार के लोगों को भी पता नहीं। भारतेंदु काल मे जैनेंद्र जैन जैसे नाटककार आरा में हुए उनका जिक्र शुक्ल जी ने नहीं किया। घराऊ घटना के लेखक को भी लोग नही जानते जो हिंदी का पहला यथार्थवादी उपन्यास है। शुक्ल जी ने जिनका नाम नहीं लिया वे लोग नहीं जाने गए।
प्रश्न – बिहार के वरिष्ठ लेखक बिहार की युवा प्रतिभा का नाम नहीं लेते।
उत्तर – आपका कहना सही है। ये रोग पहले से है। बिहार के लेखक दिल्ली के मठाधीशों की राह पर चलते हैं। मठाधीश जिनका नाम लेंगे उनका नाम वे लेंगे। अब युवा प्रतिभाएं मोहताज़ नहीं। आप देखिए हृषिकेश सुलभ, अवधेश प्रीत, निलय उपाध्याय, प्रियदर्शन, संजय कुंदन, कविता, नीला प्रसाद, वंदना राग, प्रत्यक्षा, उपासना झा, ज्योति रीता, पंखुरी सिन्हा, राकेश बिहारी, प्रेम रंजन, अनिमेष, हरे प्रकाश उपाध्याय, अचुत्यानंद मिश्र, रश्मि भारद्वाज, अणुशक्ति सब अपने बल बूते पर सामने आए। यह अलग बात है कि इनमें से अधिकतर दिल्ली में रहते हैं।
प्रश्न – पुरस्कारों के बारे में आपकी क्या राय है। हिन्दी में हर पुरस्कार विवाद से घिर जाता है। विनोद जी को ज्ञानपीठ मिला तो विवाद शुरू हो गया।
उत्तर – हिंदी में पुरस्कार आमतौर पर साहित्य के सत्ता विमर्श का ही एक हिस्सा है। कई बार यह पुरस्कार अच्छे लोगों को भी मिलता है लेकिन कई बार बुरे लोगों को भी मिलता है। लेकिन सवाल यह है कि किसी को पुरस्कार मिले या ना मिले इसको लेकर चिंतित क्यों रहा जाए। आखिर पुरस्कार लोलुपता हिंदी में क्यों हैं? मुझे तो कई बार लगता है हिंदी कविता की उड़ान भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से लेकर साहित्य अकादमी तक है, तो हिंदी कहानी की उड़ान रमाकांत स्मृति पुरस्कार से लेकर साहित्य अकादमी पुरस्कार तक है। अब इसमें लिट़्फेस्ट में मिलने वाले लख टकियान पुरस्कारों को भी आप जोड़ सकते हैं और साहित्य अकादमी के बाद बुकर पुरस्कार की दौड़ में हिंदी के लेखक शामिल हो जाते हैं। अगर वह खुदा न खास्ते शॉर्टलिस्टेड भी हो जाता है तो वह भी उसके लिए किसी बड़े पुरस्कार से कम नहीं। सवाल यह है कि आखिर किसी लेखक को पुरस्कार से क्यों मापा जाए? उसका आकलन उसकी रचना के आधार पर क्यों ना हो? अगर PEN पुरस्कार न मिले तो विनोद जी क्या महत्वपूर्ण लेखक नहीं, उदय प्रकाश महत्वपूर्ण नहीं। लेकिन यह भी सच है कि जब किसी को कोई बड़ा पुरस्कार मिलता है तो लोगों की निगाह उसके लेखन पर जाती है और समाज के आम लोग उस पुरस्कार से ही लेखक का आकलन करते हैं। आम आदमी को लगता है कि अगर किसी को ज्ञानपीठ पुरस्कार या साहित्य अकादमी पुरस्कार या बुकर पुरस्कार मिल गया तो वह लेखक ज़रूर बड़ा होगा, महत्वपूर्ण होगा लेकिन सच ऐसा नहीं है। कई लोग जिन्हें बड़े-बड़े पुरस्कार मिले हैं उनके लेखन में कोई दम नहीं है और कई ऐसे लोग जिन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला है उनका लेखन दमदार है। इसलिए मैं कहता हूं कि पुरस्कार किसी के लिखे का कोई मानक नहीं है। यह अलग बात है कि पुरस्कार मिलने से लेखक को थोड़ा प्रोत्साहन मिल जाता है। उसके अंदर थोड़ा आत्मविश्वास आ जाता है और उसे लगता है कि वह जो कुछ लिख रहा है वह ठीक-ठाक लिख रहा है, तभी तो उसे यह मान्यता मिल रही है। लेकिन यह भी सच है कि पुरस्कारों को देने लेने की भी एक राजनीति, एक गुटबाजी, एक पूर्वाग्रह, जाति, प्रान्त, परिचय, नेटवर्किंग भी काम करती है। और ज्यादा पुरस्कार उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो सत्ता विमर्श में शामिल हैं या सत्ता प्रतिष्ठान का विरोध नहीं करते, सबसे संतुलन बनाकर रखते। जो लोग निर्णायक बनाए जाते हैं वह भी किसी न किसी सत्ता विमर्श में शामिल हैं लेकिन हिंदी में इस समय पुरस्कार को लेकर बड़ा विचित्र हाल है। अब तो गली गली में पुरस्कार है। हिंदी में पुरस्कारों का एक लंबा इतिहास रहा है। मंगला प्रसाद पारितोषिक, देव पुरस्कार, सक्सेरिया पुरस्कार से लेकर आज के पुरस्कारों तक। कई बार बड़े-बड़े पुरस्कार किसी लेखक को पहले मिल गए और उनसे अधिक योगदान वाले लेखक को बाद में मिले। मैंने बीस साल पहले जनसत्ता में पुरस्कारों को लेकर कवर स्टोरी लिखी थी। तब 42 पुरस्कार थे। अब 60 से अधिक हो गए होंगे। हिंदी में दिनकर को, राहुल जी, शिवपूजन जी, बालकृष्ण शर्मा “नवीन” से पहले पदम भूषण मिला। निराला को तो कोई पदम पुरस्कार नहीं मिला और जिस दिनकर ने कहा था कि बेनीपुरी न होता तो दिनकर न होता, उस बेनीपुरी को तो पदमश्री तक नहीं मिला। लेकिन इससे बेनीपुरी का साहित्य में योगदान कम नहीं हो जाता है। निराला का अवदान कम नहीं होता। रेणु, अमरकांत, मार्कण्डेय, मंन्नू भंडारी, राजेन्द्र यादव को अकादमी पुरस्कार न मिलने से उनका महत्व कम नहीं। इस तरह के अनेक उदाहरण हैं कि लेखकों को पदम पुरस्कार नहीं मिले जबकि वे इसके हकदार थे। क्या नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, त्रिलोचन, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध को पदभूषण नहीं मिलना चाहिए था? क्या उसके हकदार नहीं थे? क्या देवी प्रसाद मिश्र और कुमार अंबुज, बद्री और अनामिका से अच्छे कवि नहीं लेकिन आज जो स्थिति है उसमें 100 साल के रामदरस मिश्र को केवल पद्म श्री देकर झुनझुना थमा दिया जाता है। लेकिन अब तो लेखक में वह आत्म सम्मान भी नहीं है कि उसे वह लौटा दे। मिश्र जी जीवन भर दक्षिण पंथी खेमे में रहे। पुरस्कार वापसी के समय अकादमी के साथ थे।विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो उसका चारों तरफ स्वागत किया गया है और कहा गया की रामभद्राचार्य को पुरस्कार देकर ज्ञानपीठ ने अपने चेहरे पर जो कालिख पोती थी उसे विनोद जी को देकर अपना चेहरा साफ कर लिया। लेकिन जो पुरस्कार रामभद्राचार्य जैसे दलित और मुस्लिम विरोधी हिंदुत्ववादी को दिया जाए उस पुरस्कार को आखिर क्यों लिया जाए? क्या हिंदी के लेखकों को उसका विरोध नहीं करना चाहिए। उस ज्ञानपीठ पुरस्कार को लेने का क्या औचित्य बचा है? आखिर जब हम अडानी द्वारा प्रायोजित पुरस्कारों का विरोध करते हैं तो ज्ञानपीठ भी तो एक पूंजीपति का पुरस्कार है। अब तो लिट् फेस्टिवल में भी पूंजीपतियों की राशि लगी हुई है। इसलिए अब पुरस्कार का कोई मतलब नहीं रह गया है। जिसको जो आस्था पुरस्कारों में है वह अपनी आस्था उसमें बनाए रख सकते हैं लेकिन यह सच है कि छोटा से छोटा पुरस्कार भी अब संदिग्ध हो गया है। क्योंकि ऐसे लोग निर्णायक बनाए जा रहे हैं जो खुद अभी कायदे से लेखक बने नहीं हैं लेकिन आप देख लीजिए कई नए लेखक भी एक ही नहीं दो-तीन निर्णायक समितियों के सदस्य हैं। कभी भारत भूषणअग्रवाल पुरस्कार के निर्णायकों में नामवर जी, केदारनाथ सिंह और विष्णु खरे जैसे लोग हुआ करते थे और अब देखिए उसके निर्णायक कौन-कौन लोग हैं। इसी तरह ज्ञानपीठ पुरस्कार में भी अब उस कद काठी के लोग निर्णायक नहीं बने हैं लेकिन यहां तो पुरस्कार पाने, निर्णायक बनने की होड़ लगी हुई है। अगर ऐसे में कोई सवाल खड़ा करता है तो लोग उसके खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं। विनोद कुमार शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला तो इसका किसी ने विरोध नहीं किया। उनका
विरोध अगर कुछ लोगों ने किया तो यह सवाल उठाकर किया कि आखिर पिछले 10 सालों में जो देश की स्थिति हो गई है, उसमें हमारा एक लेखक खुल कर क्यों नहीं बोलता? भारत की राजनीति जिस अधोगति से नीचे जा रही है और जिस तरह गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी बढ़ी है, स्त्रियों के खिलाफ हिंसा, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, क्या लेखक को उसके खिलाफ नहीं कुछ बोलना चाहिए? हिंदी के शीर्ष लेखकों से अभी भी लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि उसे सत्ता के खिलाफ अन्याय दमन के ख़िलाफ बोलना चाहिये। कई बार लिखने के साथ साथ बोलना भी पड़ता है। लेखक को अपने समय का सच कहना चाहिए उसे साहसी होना चाहिए और पारदर्शी भी। हिंदी समाज ने शुक्ल जी से भी यह उम्मीद पाली थी कि वह भी फासीवाद के दौर में अपनी बात खुलकर कहेंगे लेकिन शुक्ल जी ने कभी भी कोई ऐसी बात कही नहीं। इसलिए विवाद पुरस्कार को लेकर कम सच बोलने को लेकर है। शुक्ल जी के समर्थक कहते हैं कि लेखक को केवल अपने लिखे में ही अपनी बात कहनी चाहिए अपना स्टैंड लेना चाहिए। सार्वजनिक रूप से कुछ कहना और लिखना जरूरी नहीं है। चलिए थोड़ी देर के लिए यह भी मान लेते हैं। लेखन के लिए कोई अनिवार्य शर्त नहीं होती है, लेकिन आप सोचिए एक लेखक के रूप में न सही बल्कि एक नागरिक के रूप में क्या हमें इन घटनाओं का विरोध नहीं करना चाहिए? विनोद जी एक लेखक के तौर पर भले विरोध न करते लेकिन वे तो इस देश के एक नागरिक भी हैं। क्या देश के किसी नागरिक समाज से उम्मीद नहीं की जाती है कि वह कुछ कहे। पुरस्कार लौटाने से लेखक का कद ही बढ़ता है, लेने से नहीं बढ़ता। लेकिन आज तो 500 रुपए का भी कोई पुरस्कार लौटना नहीं चाहता। जब भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार को लेकर विवाद हुआ तो तीन युवा लेखकों ने मुझसे कहा कि हम लोगों को यह पुरस्कार लौटाना चाहिए लेकिन जब लौटाने की बारी आई तो लोग पलट गए, चुप लगा गए। केवल मैंने लौटाया। इसी तरह भुवनेश्वर में एक पुरस्कार इसलिए लौटाया कि आयोजकों ने पुरस्कार राशि में से खाने का पैसा काट लिया। तब किसी लेखक ने मेरा साथ नहीं दिया। देश भर से 13 युवा लेखकों को पुरस्कार मिला था। बाद में पता चला कि संस्कृति मंत्रालय से मिले अनुदान पर यह पुरस्कार दिया गया था। सीताकांत महापात्र सचिव थे। उन्होंने राजेन्द्र पांडा की संस्था को यह अनुदान दिया था। इब्बार रब्बी ने इसकी रिपोर्ट लिखी तो नवभारत टाइम्स में छपी नहीं। बाद में सव्यसाची की पत्रिका उत्तरार्ध में पूरी रिपोर्ट छपी। ये पुरस्कार राज्यपाल बी सत्यनारायण रेडी ने दिया था। मैं 13 लेखकों के हस्ताक्षर युक्त पत्र उनको देना चाहता था पर मुझे उनसे मिलने नहीं दिया गया। दिल्ली आया तो एक दिन सुरेंद्र मोहन जी ने मुझे रेड्डी साहब से मिलवाया। वे सुरेंद्र मोहन जी से मिलने सहविकास अपार्टमेंट आये थे। लेकिन सुरेंद्र जी के सामने रेड्डी साहब से मैंने शिष्टाचार वश कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तान टाइम्स की खबर से सुरेंद्र जी को पूरा प्रकरण पता था लेकिन जब रेड्डी साहब एक दिन संसद के गलियारे में मिल गए तो सारा किस्सा उनको सुनाया। वे चुप रहे। इसी तरह सीताकांत महापात्र को भी एक समारोह में बताया। इसलिए पुरस्कार सन्दिग्ध है। मुझे पता है किसको, कैसे पुरस्कार मिलता है। किसके साहित्य अकादमी अध्यक्ष से कितने मधुर संबंध हैं यह हमें पता है। पूरी दुनिया में ऐसे उदाहरण हैं जब लेखक ने सड़क पर उतर कर अपनी बात कही है, कई जेल भी गए हैं और सब ने तानाशाही और फासिज़्म विरोध किया है। ऐसे में अगर हम अपने किसी सिर्फ शीर्ष लेखक से ऐसी उम्मीद पालते हैं तो क्या गलत करते हैं? जो लोग भी उम्मीद रखते हैं उनमें से भी किसी ने यह नहीं कहा कि विनोद जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिलना चाहिए या उनके लेखन का कोई असर नहीं है, उनमें कोई गुणवत्ता नहीं है या उनका अवदान नहीं है। सवाल यह है कि हम लोग अगर लेखक के रूप में सत्ता का विरोध नहीं कर सके तो कब से कम एक नागरिक के रूप में तो अपना विरोध दर्ज कर सकते हैं। अब तो सोशल मीडिया भी एक प्लेटफार्म है जहां लोग अपनी बात कहते हैं। शायद यही कारण है कि पत्रकारों को और लड़कों को जेल भी जाना पड़ता है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि विरोध पर शुक्ल 90 साल की उम्र में जेल जाएँ और अपना विरोध दर्ज करें। लेकिन कम से कम उससे तो यह उम्मीद की जा सकती है और जनता को करना भी चाहिए कि उसका लेखक क्या बोल रहा है, कैसा आचरण कर रहा है, किस तरह की शिकायतें कर रहा है और किस तरह के सपने और उम्मीद पाले हुए है। लोग शमशेर, केदारनाथ अग्रवाल, श्रीकांत वर्मा, दिनकर, अज्ञेय के नाम पर दुकान खोलकर बैठे हैं। हर पुरस्कार की एक अन्तःकथा है। वैसे कई बार अच्छे लोगों को मिल जाता है पर यह अपवाद है। अब तो थोक के भाव से पुरस्कार दिए जाते हैं। कोई विदेश में रहनेवाला लेखक पुरस्कार देता है। अब तो बिना पैसे का पुरस्कार लेने वाले लेखकों की भी भीड़ है। अगर आपके पास पैसा है तो आप भी अपने पिता, माँ, पत्नी, बेटी, भाई सबकी स्मृति में पुरस्कार दे सकते हैं। अगर मेरे पास पैसा होता तो अपने नाम पर एक पुरस्कार शुरू करता। इसलिए पुरस्कार की अनंत कथाएं हैं पर पहल सम्मान, देवी शंकर अवस्थी सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल जैसे कुछ बेहतर पुरस्कार रहे। अब तो प्रकाशकों ने भी पुरस्कार शुरू कर दिए।
प्रश्न – आप स्त्री दर्पण मंच चलाते हैं और कुछ स्त्रियों को आप नाराज़ कर देते है वे आपकी शिकायत करती हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे।?
उत्तर – आपका सवाल वाजिब है। सब लोग मुझसे यह पूछते हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से कभी नहीं बोला। क्योंकि मैं कुछ बोलकर विवाद नहीं खड़ा करना चाहता। स्त्री दर्पण का उद्देश्य बड़ा है। वह किसी व्यक्ति का मंच नहीं है। वह मेरा मंच भी नहीं है। एक सामूहिक मंच है और टीम भावना से काम होता है। लेकिन कुछ लोग नाराज़ है, सहयोग नहीं करते। यह हिंदी की दुनिया का रिवाज है। यहां हर कोई नाराज़ रहता है। हर किसी की किसी न किसी से नहीं बनती है। इसमें मैँ भी शामिल हूँ लेकिन हमें कुछ काम कर के जाना है। हिन्दी में लोग काम कम करते हैं, निंदा आलोचना अधिक करते हैं, टांग अधिक खींचते हैं और प्रवृतियों की आलोचना नहीं कर के व्यक्तिगत हमले करते हैं, नाम लेकर और हिंसक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्त्री दर्पण शुरू किया तो एक कवयित्री ने मेरे खिलाफ लिखा कि मेरी कोई साहित्यिक समझ नहीं है और मुझे समारोह में मैत्रीय जी को नहीं बुलाना चाहिए। बाद में पता चला कि उस लेखिका का कोई विवाद मैत्रेयी जी से पहले हो चुका है लेकिन विवाद के बाद भी उस लेखिका से जुड़ी रचनाएं दो बार अपनी पत्रिका में छाप चुका हूं। मेरा विरोध प्रवृत्तियों से है। इसके बाद खुद मैत्रेयी जी स्त्री दर्पण के समारोह में युवा लेखकों की उदंडता से नाराज़ हो गयीं और विवाद खड़ा हुआ। बाद में उन्होंने स्त्री दर्पण से माफी मांग ली। उस समारोह में जिन लोगों ने मैत्रेयी जी का विरोध किया उन्होंने उनसे संबंध सुधार लिए और पुरस्कार भी लिए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में आटे में घुन की तरह मैँ पीसा, बेवकूफ बना।
दूसरा प्रकरण तब हुआ जब एक लेखिका ने मेरे ही कार्यक्रम में “स्त्री दर्पण” की आलोचना की और मुझे एक संपादक के रूप में अयोग्य करार दिया और कहा कि मैं खुद को चमकाने के लिए यह काम कर रहा हूं। इस मंच का संयोजक स्त्री को होना चाहिए लेकिन जब उसका जवाब देना चाहा तो मुझे अपनी बात नहीं कहने दी। मैं यहां स्पष्ट कर रहा कि हिंदी में कोई दूसरों के लिए काम करना नहीं चाहता लेकिन अगर कोई करता है तो उसमें मीन मेख लोग निकालते रहते हैं, उसकी टांग खींचते हैं, अशोक वाजपेयी भी यही कहते हैं। मैंने शुरू में कहा था कि स्त्री दर्पण एक खुला मंच है और हर व्यक्ति अगर कोई श्रृंखला चलाना चाहता है तो उसका स्वागत है। जो लोग नई योजना लेकर आए उनकी श्रृंखला चली। तीसरी घटना तब हुई जब एक वरिष्ठ कवयित्री ने अपने पुरस्कार के बारे में “कौन गली गए श्याम” का जिक्र किया और मैंने इस शीर्षक से एक कविता लिखी। लोगों ने उस कवयित्री को मेरे खिलाफ भड़काया और वह कवयित्री मुझसे काफी नाराज हो गयी। जबकि उस कविता में मैंने कवयित्री का नाम नहीं लिया। बाद में उस कवयित्री से मैंने लिखित माफी मांग ली। अगर मेरा कोई मित्र मेरे लिखे से आहत होता है तो माफी मांग लेता हूँ। फिर एक दूसरी कवयित्री मुझसे इस बात से नाराज़ हो गईं जब मैंने “कास्टिंग काउच” नामक कविता लिखी। उसमें भी किसी का नाम नहीं था। फिर लोगों ने प्रचारित किया। लोग कहने लगे – मैं टारगेटेड कविता लिख रहा हूँ। जबकि मैंने साहित्य की प्रवृत्तियों पर लिखा चाहा, वे पुरुष में हो या स्त्री में या मुझ में। कविता का कोई टारगेट यानी लक्ष्य तो होना ही चाहिए पर वह व्यक्तिगत नही। हिंदी में रचना के पीछे व्यक्ति को ढूंढने, उसे जोड़ने की परम्परा रही है। रचना को रचना की तरह पढ़ना चाहिए। शेखर अज्ञेय नहीं हैं। चंदर धर्मवीर भारती नहीं। लेकिन लोग प्रचारित करते हैं उदय प्रकाश ने गोरख पांडेय पर कहानी लिखी। दरअसल हिंदी की लेखिकाओं में बहनापा नहीं है। उनमें उसी तरह का ईर्ष्या द्वेष है जैसे पुरुष लेखकों में होता है। कुछ लोग उसे वैचारिक जामा पहनाते है। साहित्य में हमें रचना और लेखक की नहीं बल्कि प्रवृति पर बात करनी चाहिए। मेरा निजी रूप से किसी लेखक, लेखिका से विवाद नहीं। मैंने फिर दूसरी लेखिका से भी माफी मांग ली क्योंकि वो आहत हुईं थीं। मजेदार बात यह है कि ये लेखिकाएँ एक दूसरे का विरोध करती है पर एक ही मंच पर साथ साथ कविताएं पढ़ती है। तीसरी कविता इसलिए लिखी क्योंकि एक कवयित्री ने अशोक जी का नाम कविता में लिखकर युवा लेखिकाओं के चरित्र पर हमला किया। एक स्त्री को दूसरी स्त्री के चरित्र पर सार्वजनिक रूप से ओछी बात नहीं लिखनी चाहिए। उस कवयित्री ने मेरे ऊपर Below the belt हमला किया। मैंने जवाब नहीं दिया। इसके बाद भी इन तीनों को मैंने छापा। मेरा किसी से निजी खुंदक नहीं। विरोध विचारों से है बल्कि वह विरोध नहीं असहमति है। सम्भव है एक दिन उस कवयित्री से भी माफी मांग लूं अगर वे मुझसे आहत हों। एक युवा कवयित्री ने मुझे बुरा भला इसलिए कहा कि एक युवतर कवि की तारीफ कर दी। उन्होंने मुझसे झगड़ा किया बातचीत बन्द कर दी। ख़ैर। इन सबको मन ही मन माफ कर देता हूँ। पहले भी एक दो लेखिकाओं ने अजीबो गरीब आरोप लगाए, फेसबुक पर मेरे खिलाफ लिखा। मैंने तब “स्क्रीन शॉट” औऱ “इनबॉक्स” पर भी कविता लिखी। साहित्य में यह सब चलता रहता है। मैं स्त्रियों का उद्धार करने वाला कौन होता हूँ। किसी मुगालते में नहीं हूं। मैँ तो बस टाइम पास करता हूँ। फेसबुक पर हास्य परिहास से लोगों ने मुझे हल्का व्यक्ति समझ लिया। मैंने इन लेखिकाओं के जन्मदिन पर दिन दिन भर के कार्यक्रम किए। इनकी किताबों पर लिखा, इंटरव्यू लिए, लेकिन ये लोग मुझसे नाराज़ रहती हैं। मेरी शिकायतें करती हैं। लेकिन सब ऐसा नहीं करती। कुछ लोगों ने मेरी मदद भी की। सुधा अरोड़ा, शुभा, मधु कांकरिया, रोहिणी जी का रुख सकारात्मक रहा।
प्रश्न – आपने एक जमाने में अशोक जी के विरोध में भी लिखा पर आजकल उनका आप समर्थन क्यों करते हैं।
उत्तर – यह सच है कि एक जमाने में मैंने अशोक जी के खिलाफ एक लेख भी लिखा था और मेरा उनसे कोई विशेष संवाद नहीं था। तब अशोक जी कांग्रेस की सत्ता के साथ थे। वाम विरोधी थे। दरअसल जब पहली बार मेरी उनसे मुलाकात हुई तब वे संस्कृति मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। उन दिनों में एक पत्रकार के रूप में संस्कृति मंत्रालय भी कवर करता था। एक दिन अचानक संस्कृति मंत्रालय के दफ्तर में उनके कमरे में चला गया और नयी संस्कृत नीति के बारे में उनसे दरियाफ़्त की थी। वहीं पहली बार में उनसे मिला था। बातचीत के दौरान कुछ मुद्दों पर मेरी उनसे कुछ असहमतियाँ थी। बात आई गई। वह कभी-कभी संसद में तो कभी राष्ट्रपति भवन में तो कभी उपराष्ट्रपति भवन में मिलते थे क्योंकि उन दिनों मैँ वहां समारोह को कवर करने जाया करता था, लेकिन मेरा ज्यादा उनसे संवाद नहीं था और आज भी नहीं है। उनसे टेलीफोन पर जब कभी बात हुई एक पत्रकार के रूप में ही बात हुई। उनकी रचनाओं को हमेशा पढ़ता रहा और उनके पहले कविता संग्रह का मुरीद भी रहा। “फिलहाल”का भी मुरीद रहा लेकिन मैं उनका कोई भक्त नहीं रहा और न ही प्रिय पात्र। पुरस्कार वापसी के दौरान मैंने उनका समर्थन जरूर किया क्योंकि जब वे सत्ता के खिलाफ बोलने लगे तो मुझे एक दूसरे अशोक वाजपेयी नजर आए और मैं इस नए अशोक वाजपेयी का आज भी समर्थक हो गया। क्योंकि तब सत्ता के खिलाफ बोलने और लिखने वाले बहुत कम लेखक बचे थे।लेकिन 2014 के बाद पिछले 10 साल में अशोक जी ने लगातार सत्ता के खिलाफ धारदार बोला है और लिखा भी है। उनकी कविता में भी बदलाव आया है। इसलिए मैं इस “अशोक जी” का प्रशंसक हूं। मैं रजा फाउंडेशन की जीवनी योजना का मुरीद हूँ और आउटलुक में मैंने उस पर तीन-चार पेज की स्टोरी भी लिखी थी। जब उन्होंने युवा कार्यक्रम किया तब भी उसका समर्थन किया और आउटलुक में फिर एक स्टोरी लिखी। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मैं उनकी हर बात का समर्थन करता हूं। कई बार उनसे मेरी असहमतियाँ भी रहती हैं। और कई बार उनसे मेरे विवाद भी रहे हैं। लेकिन जब तक वह मोदी सरकार के खिलाफ बोलते और लिखते रहेंगे, मैं उनका समर्थन करता रहूंगा क्योंकि मेरा मानना है कि फ़ासीवाद के दौर पर जो कोई इस सत्ता का विरोध करता है, वह मेरा मित्र है। लेकिन उनसे कोई लाभ लेने के मकसद से नहीं किया। रज़ा फाउंडेशन के मंच पर कविता पढ़ने अब तक नहीं गया हूँ। कोई कसम भी नहीं खा रखी है। अभी तक कोई निजी लाभ नहीं लिया। स्त्री दर्पण ने रज़ा के साथ मिलकर दो दिन के प्रोग्राम जरूर किए हैं और यह साझा कार्यक्रम था और भविष्य में भी चाहूंगा कि हिंदी में कुछ अच्छे कार्यक्रम किये जाएँ। इसमें मेरा कोई व्यक्तिगत लाभ नही है और ना ही उनका कोई व्यक्तिगत लाभ है। हिंदी के हित के लिए अगर कुछ अच्छे काम हों तब हमेशा किसी का भी समर्थन करूंगा चाहे वह हिंदवी करे, संगत करे या कुछ वेबसाइट करें या ब्लॉग करें, पत्रिका करें। इसलिए मैंने हमेशा समालोचन का भी समर्थन किया है। पल्लव की पत्रिका का समर्थन किया है, अखिलेश की तद्भव पत्रिका, विनोद तिवारी की पत्रिका का समर्थन किया है। क्योंकि मेरा मानना है कि हिंदी में जब कुछ अच्छा कार्य हो तो हमें उसका स्वागत करना चाहिए चाहे उसे कोई व्यक्ति करे। इसलिए सुधा सिंह ,रूपा गुप्ता ,गरिमा जी, प्रज्ञा पाठक, सुजाता के कामों का स्वागत किया है।
प्रश्न – आप करीब 35 साल पत्रकार रहे। डेस्क और रिपोर्टिंग दोनों का अनुभव रहा। करीब 15 साल संसद कवर किया होगा। आपने एक लेखक और पत्रकार के रूप में क्या जाना, क्या देखा, क्या पाया?
उत्तर – मैं 84 से पत्रकार रहा। शुरू में 2 वर्ष मैंने हरियाणा के एक अखबार पींग से अपना करियर शुरू किया। फिर बाद में 86 में मैं विश्वविद्यालय की हिंदी सर्विस यूनीवार्ता में आ गया और तब से लेकर 2020 तक मैं वहां काम करता रहा। पहले तो मैं डेस्क पर था फिर बाद में कॉरस्पॉडेंट बन गया और उसके बाद करीब 15 साल से अधिक समय मैंने संसद की पत्रकारिता की। लोकसभा, राज्यसभा को कवर किया पर बाद में स्थायी रूप से राज्यसभा कवर करता रहा। मैं उस सदन का स्थाई कार्ड होल्डर पत्रकार था। एक पत्रकार के रूप में मुझे इस देश को जानने और समझने का सुंदर अवसर प्राप्त हुआ। अगर मैं पत्रकार नहीं होता तो शायद मैं इस देश को अच्छी तरह नहीं जान पाता, क्योंकि संसद की में जो बहसें होती हैं खासकर जो उसमें प्रश्न काल होता है उसमें आपको इतनी जानकारी मिलती है जो आपको किताबें पढ़ने से नहीं मिलती। आपको अपने मुल्क की हकीकत का पता चलता है। यूं तो आप संसद से बाहर रहकर भी इस देश को जानते और पहचानते हैं लेकिन संसद में जाकर आपको आंकड़ों से और रिपोर्ट से यह पता चलता है कि देश में कितना भ्रष्टाचार है, कितनी ग़रीबी है, कितनी बेरोज़गारी है, कितना कर्ज़ है, देश की आर्थिक स्थिति कैसी है, बजट का लोगों पर क्या असर पड़ता है और सरकार की कौन-कौन सी योजनाएं हैं और किन-किन योद्धाओं क्रियान्वयन यान्वन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? आप कैग की रिपोर्ट पढ़ते हैं, आप संसदीय समिति की रिपोर्ट पढ़ते हैं तो आप बहुत कुछ जानते हैं। वैसे तो आप अखबार के माध्यम से भी देश को कुछ जानते हैं लेकिन अखबारों में बहुत ज्यादा लंबी रिपोर्ट नहीं
छपती और हर रिपोर्ट भी नहीं छपती। उसमें कुछ ही हिस्सा छपता है। एक जमाने में संसद की बहुत सारी खबरें अखबार में छपती थीं लेकिन बाद में जिस तरह पत्रकारिता बदली, उसमें संसद की वही खबरें चलती है जिसमें हंगामा, शोरशराबा और एक दूसरे पर जान आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, उससे ही जुड़ी हुई खबरें छपती है। लेकिन देश में हर मंत्रालय की क्या स्थिति है, प्रश्नकाल में किस तरह के सवाल पूछे गए और किस तरह के जवाब दिए गए, उसके बारे में बहुत सारी जानकारी अब अखबारों में नहीं आती है और टीवी पत्रकारिता में तो वह भी नहीं होता जो प्रिंट पत्रकारिता में आपको पढ़ने को मिलता है। इसलिए आप इस देश के बारे में उतना नहीं जान पाते हैं जितना आपको जानना चाहिए था। इसलिए जब मैं सांसद जाने लगा तो मेरे लिए यह बहुत ही जानकारी पूर्ण और चुनौती पूर्ण भी काम था। इसलिए मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूं कि एक लेखक के रूप में मैंने अपने देश को करीबी से देखा, अगर मैं पत्रकार न होता तो शायद नहीं देख पाता। इसका असर मेरे लेखन पर भी पड़ा और मेरी दृष्टि भी थोड़ी बदली। मैं अब उस तरह से साहित्य नहीं देखता जैसे पहले देखता था। मेरे लिए साहित्य केवल भाषा शिल्प, रहस्य, अमूर्तन आदि का मामला नहीं। साहित्य वह नहीं जो अपने देश के समय और यथार्थ से कटा हुआ हो, जो काल्पनिक अधिक हो। आर्थिक नीति और भूमंडलीकरण के बाद जिस तरह देश बदला है, जिस तरह देश की संस्कृति बदली है, यहां तक की भाषा भी बदली है, पूरा का पूरा माहौल बदल चुका है। उसे पत्रकारिता ने अधिक दर्ज किया है साहित्य ने कम। हम आप आज एक दूसरे भारत में रहने लगे हैं और यह भारत तब भारत कम इसराइल अधिक है। यह भारत हिंदुस्तान कम अफगानिस्तान अधिक है। इस तरह से देश की संस्कृति और शिक्षा तथा अर्थव्यवस्था में जिस तरह के बदलाव हुए उसे एक नई किस्म का देश विकसित हुआ है जिसको हिंदी साहित्य पूरी तरह भी चित्रित नहीं कर पा रहा है। अगर मैं उपन्यासकार होता या एक कुशल कथाकार होता है तो मैं शायद उसे रचना में अधिक दिखाता क्योंकि कविता में बहुत सारी बातें लिखनी मुश्किल होती हैं। फिर भी मैंने इस बदले हुए भारत के बारे में बहुत सारी कविताएं लिखी है। इसलिए मेरा अनुभव एक पत्रकार के रूप में समृद्धकारी रहा और मैंने उसे बड़ा पॉजिटिव रूप में लिया। क्योंकि इससे पहले यह समझा जाता रहा है कि पत्रकार होने से आपके भीतर का साहित्यकार मर जाता है, लेकिन रघुवीर सहाय ने पत्रकारिता का साहित्य में सृजनात्मक इस्तेमाल किया है। वह भी संसद जाते थे। श्रीकांत वर्मा भी सांसद जाते थे लेकिन रघुवीर सहाय के संसद जाने और वर्मा के संसद जाने में फर्क था। रघुवीर सहाय का वह रास्ता नहीं था जो श्रीकांत वर्मा का था। श्रीकांत वर्मा संसद जाते-जाते कांग्रेस के महासचिव भी बनते हैं और राज्यसभा के सदस्य भी बनते हैं/ लेकिन रघुवीर सहाय का वह रास्ता नहीं था। वह एक पत्रकार थे और जीवन भर पत्रकार रहे। दलाल नहीं बने आज की तरह। इस संसद में हमारे विष्णु नगर भी जाते रहे लेकिन विष्णु नागर की पत्रकारिता अन्य पत्रकारों की तुलना में अलग है और वह धारदार है। वह पिछले कई सालों से इस सत्ता की पोल खोलते रहे हैं लेकिन कई पत्रकार इस संसद में जाते हुए बड़े दलाल बन जाते हैं। सत्ता के करीब हो जाते हैं। फार्म हाउस में रहने लगते हैं और मंत्रियों और नेताओं से उनका nexus विकसित हो जाता है और वह सत्ता के खेल में शामिल हो जाते हैं। लेकिन विष्णु नागर, उर्मिलेश जैसे पत्रकारों ने वह रास्ता नहीं चुना और भी बहुत सारे पत्रकार हैं जिन्होंने वह रास्ता नहीं चुना। लेकिन बहुत सारे ऐसे पत्रकारों को भी जानता हूं जिनके लिए पत्रकारिता सफल होने का एक माध्यम है और वह सांसद बने। उनमें से कई तो कई महत्वपूर्ण पदों पर गए लेकिन उनके लिखने में वह दम नहीं है, वह सच नहीं लिखते हैं। वह झूठ का समर्थन करते हैं या उस पर मौन रहते हैं। इसलिए मैं तो यह कहूंगा कि एक साहित्यकार को एक पत्रकार की तरह भी इस देश को देखना चाहिए। क्योंकि पत्रकार के पास जो निगाह होती और जो अनुभव होता है वह साहित्यकार को नहीं मिल पाता। साहित्यकार तो उन तमाम जगहों पर जा ही नहीं पाता है जहां पत्रकार जाता है। इसलिए एक साहित्यकार कल्पना और संवेदना की सूक्ष्मता पर आधारित होता है जबकि पत्रकार अपनी नंगी आंखों से चीजों को देखा है।
प्रश्न – हिंदी में एक कहानीकार से यह नहीं पूछा जाता कि उसकी नजर में हिंदी कविता कैसी है? एक कवि से भी नहीं पूछा जाता है कि उसकी नजर में हिंदी कहानी का कैसा परिदृश्य है और न ही कभी कहानीकारों से हिंदी आलोचना के बारे में कुछ पूछा जाता है। हर रचनाकार अपनी अपनी विधा में कैद रहता है और सिमटा रहता है। कहानी और उपन्यास पर आपकी क्या टिप्पणी है?
उत्तर – यह आपने सही सवाल किया है प्रभात जी। हिंदी की दुनिया में हम कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं करते कि आखिर हिंदी के बड़े कहानीकार कविता के बारे में कैसी राय रखते थे और हिंदी के बड़े कवि कहानियों के बारे में कैसी राय रखते हैं। हिंदी में कम ऐसे लेखक हुए हैं जो कहानीकार होते हुए कविता के अच्छे पाठक रहे हो और कवि होते हुए कहानीकार के पाठक रहे हों। राजेन्द्र यादव अच्छे कथाकार औऱ आलोचक थे लेकिन वह कविता के अच्छे पाठक नहीं थे। लेकिन शानी जी और ज्ञान रंजन एक कथाकार होते हुए कविता के अच्छे पाठक थे और उन्होंने अपनी पत्रिका में हंस से बेहतर कविताएं छापी हैं। लेकिन हम यह जान नहीं पाते कि निर्मल वर्मा की कविता के बारे में क्या राय थी? अशोक वाजपेयी समकालीन हिंदी कहानी में किस तरह की चीज पसंद करते हैं। क्योंकि वे अक्सर कविता का ही जिक्र करते हैं और कथा साहित्य में कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा, वैद साहब और विनोद कुमार शुक्ला के बाद आगे कभी किसी पर कोई टिप्पणी करते नहीं है। इसलिए हमें नहीं मालूम चलता है कि आखिर उनकी कहानियों के बारे में क्या राय है? हमें यह नहीं पता चला कि संजीव, शिव मूर्ति और प्रियम्बद समकालीन कविता के बारे में क्या राय रखते हैं? हमें यह भी नहीं पता चलता कि लीलाधर जगूड़ी या नरेश सक्सेना समकालीन कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं?यह सच है कि मैंने कविताएं अधिक पढ़ी हैं, कहानी कम पढ़ी है। इसलिए मैं कहानी और उपन्यास के बारे में अधिकारपूर्वक कुछ कह नहीं सकता हूं। लेकिन जितना कुछ पढ़ा है उससे मेरी एक राय बनी है जो भले समग्र न हो। मुझे लगता है कि हिंदी में प्रेमचंद का तो मूल्यांकन हुआ लेकिन उनके अन्य समकालीन कथाकारों का मूल्यांकन नहीं हुआ। पांडे बेचन शर्मा उग्र अपनी प्रतिभा में प्रेमचंद से कम नहीं थे। उनकी कहानी आप पढ़ लीजिए। उनका गद्य भी आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको जैनेन्द्र कुमार, यशपाल और भगवती चरण वर्मा तीन बड़े कथाकार नजर आते हैं। उसके बाद अज्ञेय आपके सामने नजर आते हैं लेकिन कहानीकार के रूप में उनका मूल्यांकन नहीं हुआ जैसे एक समय जयशंकर प्रसाद के कहानीकार के रूप में मूल्यांकन नहीं हुआ था। विजय मोहन सिंह ने जरूर एक बहुत ही अच्छा लेख उनकी कहानियों पर लिखा था। जैनेन्द्र को समझने के लिए विष्णु खरे ने एक शानदार लेख लिखा है। रेणु पर विश्वनाथ त्रिपाठी ने लेकिन मुक्तिबोध, रघुवीर सहाय और श्रीकांत वर्मा के कहानीकार रूप का मूल्यांकन नहीं हुआ। आज़ादी के बाद जो कथाकार आए उनकी कविता के बारे में क्या राय रही यह नजर नहीं आती। मोहन राकेश, कमलेश्वर आखिर हिंदी कविता के बारे में क्या सोचते थे, यह पता नहीं चलता। लेकिन यह सच है कि कुछ लोग ऐसे हुए जो कविता और कहानी साथ-साथ पढ़ते रहे, जैसे मैंने ऊपर जिक्र किया था शानी और ज्ञान रंजन। उसके बाद फिर कामतानाथ, मधुकर सिंह, मिथिलेश्वर आदि को छिटपुट पढ़ा और आज के समकालीन कथाकारों में संजीव, शिवमूर्ति, प्रियम्वद, उदय प्रकाश, स्वयं प्रकाश तथा पंकज बिष्ट को पढ़ा। मुझे शिव मूर्ति की कहानी पसंद है। अगर उनकी स्त्री दृष्टि थोड़ी प्रगतिशील होती तो और मुझे और अधिक पसंद आती है। संजीव मुझे कहानीकार से अधिक महत्वपूर्ण उपन्यासकार लगते हैं। प्रियम्वद की भाषा और शिल्प का मैं प्रशंसक हूँ लेकिन उनकी दृष्टि अगर उदय प्रकाश की तरह शार्प होती तो और वे और बड़े कथाकार हो सकते थे। स्वयं प्रकाश की कहानियों का मैं बहुत ही प्रशंसक रहा हूं और उन्हें किसी लेखक से कम नहीं मानता हूं। मधुसूदन आनंद की भी कहानियों का प्रशंसक रहा हूं। इस तरह शशांक की कहानी ‘घंटी’ बहुत शानदार कहानी लगती है। ऐसी शानदार कहानी कम लोगों ने लिखी है बाद की कहानीकारों में मुझे अखिलेश, राजेन्द्र दानी और हरि भटनागर की कहानी पसंद है। नए लोगों में मैंने पंकज सुबीर, पंकज मित्र, चंदन पांडे, कुणाल, शशि भूषण द्विवेदी, राकेश मिश्रा, विमल चन्द्र पांडेय, पराग मांदले, मनोज पांडेय आदि की भी कहानियां मैंने पढ़ी हैं। मनीषा कुलश्रेष्ठ की कहानियाँ मुझे पसंद है लेकिन राजनीतिक विचार नहीं। विभा रानी, कविता, प्रत्यक्षा तथा वंदन राग की कहानियां मैं जरूर पढ़ता रहता हूं। इसके अलावा विजयश्री तनवीर, अंजू शर्मा, सपना सिंह, ममता सिंह, आकांक्षा पारे और योगिता यादव की कुछ कहानियों को मैंने पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि ये लोग हिंदी कहानी को और आगे ले जाएंगे। लेकिन मैं सारी बातें एक पाठक के रूप में ही कह रहा हूं। मैँ कोई आलोचक नहीं हूँ। लेकिन किसी कहानीकार कि जब कोई कहानी आती है तो मैं उसे जरूर पढ़ता हूं चाहे वह दिव्या विजय, अनुकृति उपाध्याय, प्रियंका ओम हो या निधि अग्रवाल हो। इन लोगों पर मेरी निगाह रहती है कि आखिर यह लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। प्रियदर्शन, संजय कुंदन को बहुत अच्छा कहानीकार मानता हूं। एक जमाने में संजय ख्याति की भी कुछ कहानियां मुझे बहुत पसंद थीं लेकिन मैंने जैसा कि आपसे पहले कहा कि मैं कहानी कम पढ़ पाता हूँ कविताओं की तुलना में, इसलिए मैं कथाकारों के बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी करने से बचता हूँ। बाद के उपन्यास कम पढ़े हैं इसलिए उस पर कुछ बोलना उचित नहीं होगा।
प्रश्न – अच्छा ये बताएं अरविंद कुमार और विमल कुमार का क्या चक्कर है? कौन मौलिक है?
उत्तर – मेरा सर्टिफिकेट नाम अरविंद कुमार है। पुकार नाम विमल कुमार। पत्रकार के रूप में अरविंद हूँ लेखक के रूप में विमल लेकिन मौलिक विमल ही है। पत्रकार के रूप में किसी अधिकारी या नेता से मिला तो विमल कुमार के नाम से नहीं मिला। लेखकों से मिला तो अरविंद कुमार के रूप में नहीं। स्त्रीलेखा पत्रिका के लिए जब RNI के लिए आवेदन दिया तो सर्टिफिकेट नाम देना पड़ा। तब लोगों ने जाना कि अरविंद में ही हूँ। एक महिला इस बात को नहीं जानती थी उसने एक महिला से कहा विमल कुमार तो फर्जी आदमी हैं। दो-दो नाम से फेसबुक पर है।
प्रश्न – लोकप्रिय साहित्य और गम्भीर साहित्य में आप किस श्रेणी में खुद को शामिल करना चाहेंगे। क्या लोकप्रिय साहित्य खराब साहित्य नहीं होता?
उत्तर – मेरा मानना है कि साहित्य को लोकप्रिय होना चाहिए लेकिन इस तरह जैसे प्रेमचंद का साहित्य लोकप्रिय है, तुलसीदास का साहित्य लोकप्रिय है। हमें कुमार विश्वास की तरह लोकप्रिय नहीं होना है। हमें सुरेंद्र शर्मा की तरह लोकप्रिय नहीं होना है, अशोक चक्रधर की तरह लोकप्रिय नहीं होना है। हमें अगर लोकप्रिय होना है तो मीर की तरह, ग़ालिब की तरह, फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की तरह साहिर लुधियानवी की तरह, शैलेंद्र की तरह लोकप्रिय होना है। लेकिन यह सच है कि साहित्य में लोकप्रिय साहित्य और गंभीर साहित्य के बीच एक रेखा खींच दी गई है। यह इसलिए हुआ कि गंभीर साहित्य लिखने वाले लोग लोकप्रिय होना नहीं चाहते हैं। वे चाहते हैं कि वे अभिजन के ही लेखक बन रहें क्योंकि अभिजन के लेखक बने रहने में पुरस्कार, सम्मान, विदेश यात्रा, फैलोशिप है। लेकिन अगर आप जनता के लेखक बनेंगे तो आपको यह सब नसीब नहीं है। यह सारी समस्याएं आधुनिकता की समस्याएं हैं। जब हमारा समाज आधुनिक बनने लगा तब एक अभिजन समाज भी विकसित हुआ जो पहले के सामंती समाज से अलग था। इस समाज को कुछ नए सौंदर्य और नए भवबोध की चीज चाहिए थी और इसी वजह से हिंदी में भी एक गंभीर साहित्य उत्पन्न हुआ। अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव वैद, विनोद कुमार शुक्ल जैसे लेखक गंभीर लेखक कहलाए जबकि शैलेंद्र और नागार्जुन जैसे लेखक लोकप्रिय लेखक कहलाए। हालांकि लोकप्रियता भी एक तरह का मिथ है। क्योंकि हिंदी में अगर कोई लोकप्रिय है भी तो वह फिल्मी सितारों की तरह तो लोकप्रिय नहीं है या क्रिकेट के खिलाड़ी की तरह लोकप्रिय नहीं है। हां यह सच है कि लुगदी साहित्य लिखने वाले सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं। लेकिन यह भी सच है कि उनका लिखा साहित्य की कसौटियों पर साहित्य कम है। लेकिन फिर भी शेक्सपियर, टॉलस्टॉय, गोर्की, चेखव, ब्रेख्त, नेरुदा जैसे अनेक लेखक लोकप्रिय भी हैं और गंभीर भी हैं। हमें वैसा लिखना चाहिए जो गंभीर और लोकप्रिय दोनों हो लेकिन विनोद जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलने के समय अपने बयान में कहा था कि अगर मेरा कोई एक भी पाठक हिंदी में है तो मैँ संतुष्ट हूं यानी वह साहित्य को पाठकों की कसौटी पर नहीं रखना चाहते हैं। हिंदी में इस तरह का एक एलिटिज़्म विकसित हुआ है जो एक विशेष पाठक बनाना चाहता है वह सामान्य पाठकों की संवेदना के स्तर पर जुड़ना नहीं चाहता है। क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसकी रचना एक सामान्य पाठक समझ लेता है तो वह गंभीर साहित्य नहीं माना जाएगा। इस मिथ को तोड़ा जाना बहुत जरूरी है लेकिन आप लुगदी साहित्य के झंडाबरदार है। एक गलत बहस चला रहे है। सुना है कि आप मार्किट के आदमी हैं, प्रकाशकों के आदमी है। क्या यह सच है? आप साहित्य में एक सत्ता केंद्र बनना चाहते हैं ।
प्रश्न – लेकिन यही बात लोग आपके बारे में कहते हैं आपने स्त्रीलेखा निकाल कर समारोह कर, स्त्री दर्पण पेज बनाकर वेबसाइट बनाकर एक सत्ता केंद्र बनाया है।
उत्तर – इसका मतलब हम लोग आरोपों की एक ही नाव पर सवार हैं। बिना आरोप प्रत्यारोप के संवाद होता नहीं। यह सब साहित्य की जीवंतता की निशानी है।