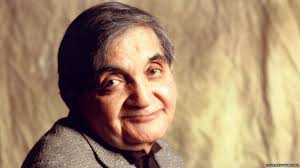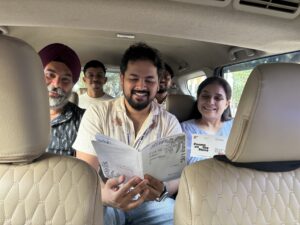आज महान लेखक निर्मल वर्मा की जयंती है। उनकी जयंती पर युवा शायर और दिल्ली विश्वविद्यालय के शोधार्थी अभिषेक कुमार अम्बर की इस लिखत की याद आई। उन्होंने बहुत दिलचस्प तरीक़े से लिखा है कि किस तरह से रानीखेत में उन्होंने निर्मल वर्मा की कहानी ‘परिंदे’ में वर्णित स्थलों की तलाश की। बहुत शोधपरक और आस्वादपरक लिखा है लेखक ने। आप भी पढ़ सकते हैं- मॉडरेटर
=======================================
जाते दिसम्बर की सुबह, अल्मोड़े में सर्दी अपने शबाब पर थी फिर भी माल रोड पर लोगों की चहलक़दमी सर्दी को ठेंगा दिखा रही थी। बच्चे पीठ पर बस्ता टाँगे झुंड बनाए स्कूल जा रहे थे तो वयस्क दफ़्तर की ओर तथा एक स्कूटी पर सवार हम तीन लोग चौराहे पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस को चकमा देकर रानीखेत। अल्मोड़े के बाज़ार को पार करने के बाद ट्रैफिक पुलिस का कोई ख़ास डर नहीं रहता और तीन लोग भी आराम से सफ़र कर सकते हैं और इसी चीज़ का फ़ायदा हम लोग आज उठा रहे थे।
आसमान पूरा कोहरे से भरा था, खेतों में सफेद पाले की चादर बिछी थी, चीड़ और देवदार के पेड़ ठिठुरते-से बलखाती पहाड़ी सड़कों पर नागिन सी लहराती गाड़ियों को देख रहे थे। जैसे-जैसे हम अल्मोड़ा से कोसी की ओर बढ़ते जा रहे थे कोहरा और घना होता जा रहा था अब पहाड़ भी धुँधले से हो गए थे 1-2 मीटर से ज़्यादा आगे की सड़क हमें साफ़ नहीं दिखाई दे रही थी लेकिन ऐसे में भी सुंदर भाई बड़ी कुशलता से गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि नौकरी की वजह से उनका रोज़ ही अल्मोड़ा से रानीखेत आना-जाना होता था। लेकिन मेरा और मोहित नेगी का पहला मौक़ा था और हम सुबह-सुबह की सर्दी से बेहाल हो रहे थे। हवा हमारे शरीर में शूल-सी चुभ रही थी। लेकिन रानीखेत भ्रमण का इतना उत्साह था कि हवा के थपेड़े सहे जा सकते थे।
रानीखेत भारत के सबसे ख़ूबसूरत हिल-स्टेशनों में से एक है जहाँ क़ुदरत का रूप देखने लायक है लेकिन रानीखेत घूमने की मेरी एक ख़ास वजह थी निर्मल वर्मा की कहानी ‘परिंदे’। मैंने परिंदे कहानी पहली बार बी.ए. के दिनों में पढ़ी थी और इस कहानी का जादू मेरे ऊपर ऐसा चढ़ा कि जब भी यह कहानी पढ़ता तो इस कहानी में खो-सा जाता, ऐसा लगता कि मैं इस कहानी को अपनी आँखों के सामने घटते देख रहा हूँ। जब लतिका, सुधा के कमरे में महफ़िल सजाए बैठी लड़कियों को झिड़क रही होती है तो लगता है मैं भी लतिका के बराबर में खड़ा यह घटना देख रहा हूँ, जब मिस. लतिका, डॉक्टर मुकर्जी, ह्यूबर्ट तीनों मुकर्जी के कमरे में छत पर बैठे ह्यूबर्ट से सेशोपाँ और चाइकोव्स्की के कंपोज़ीशन सुन रहे थे तो लगता जैसे मैं भी उनके साथ ही एक कुर्सी पर बैठा महफ़िल का लुत्फ़ ले रहा हूँ।
मैंने यह कहीं पढ़ा था कि निर्मल वर्मा ने ‘परिंदे’ कहानी रानीखेत के एक गर्ल्स हॉस्टल से लड़कियों की हँसी-खिलखिलाहट की आवाज़ को सुनकर लिखी थी। वैसे निर्मल ने कहानी में भी कई जगह ऐसे संकेत दे दिए हैं कि अगर कोई उनपर ध्यान दे तो आसानी से पहचान सकता है कि यह कहानी रानीखेत की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। पहला संकेत मिलता है जब डॉक्टर मुखर्जी के कमरे की छत पर बैठे लतिका को याद आता है “पहला साल जब वह डॉक्टर के संग पिकनिक के बाद क्लब गई थी। डॉक्टर बार में बैठे थे। बार-रूम कुमाऊँ रेजीमेंट के अफ़सरों से भरा हुआ था।” कुमाऊँ रेजीमेंट रानीखेत में ही अवस्थित है तो यह पक्का था कि यह कहानी रानीखेत की पृष्ठभूमि पर ही है लेकिन रास्ते भर मन में यह विचार भी आता रहा कि क्या जिस स्कूल, चर्च आदि को खोजने मैं निकला हूँ वो मुझे मिलेंगे भी या नहीं।
इसी ऊहापोह में हम मजखाली पहुँच गए थे जो रानीखेत और कोसी के बीच में कठपुड़िया के बाद पड़ता है। यहाँ से हम घने कुहरे से लदे बांज-बुराँश के जंगल को पीछे छोड़ आए थे और अब धीरे-धीरे आसमान पूरा साफ़ होने लगा था। इसके पीछे कारण यह था कि अब हम समुद्रतल से काफ़ी ऊँचाई पर आ गए थे और पहाड़ों में अधिकतर घाटियों में ही कोहरा अधिक होता है। एक निश्चित ऊँचाई के बाद कोहरा नहीं लगता और मजखाली शायद उसी ऊँचाई पर था। मजखाली में जब हमें सूर्य के दर्शन हुए तो एक अलग ही सुकून मिला। आधे घण्टे से भी अधिक समय तक कोहरे और पाले में सफ़र करने के कारण चलती गाड़ी में भी सूर्य की धूप ऐसे लग रही थी जैसे हम कहीं बैठ कर धूप सेंक रहे हों।
मजखाली से एक और साथी भी रानीखेत के सफ़र में हमारे साथ-साथ हो लिया और वह साथी था हिमालय पर्वत। वह एक ही स्थान पर खड़ा हमारे साथ-साथ चलने का भ्रम पैदा कर रहा था जैसे अक्सर चाँदनी रात में चाँद करता है। सुबह-सुबह के समय हिमालय (नंदा देवी, त्रिशूल पर्वत और पंचाचूली) एकदम दमक रहा था। हम गुनगुनी धूप का आनंद लेते रानीखेत पहुँचने वाले थे। रानीखेत के मुख्य बाज़ार से कुछ किलोमीटर पहले ही सड़क के दोनों तरफ़ दूर-दूर तक फैला ख़ाली मैदान नज़र आना लगा था, जो बुग्याल का भ्रम पैदा कर रहा था। यह मैदान एशिया का सबसे ऊँचाई पर प्राकृतिक रूप से बना गोल्फ़ ग्राउंड था। इसकी सुंदरता और गुनगुनी धूप का मज़ा लेने के मोह में हमने सुंदर भाई से कहा कि वह हमें यही छोड़ दें और स्वयं ऑफ़िस जाकर अपना काम निपटा दें ताकि दिन में हम साथ घूम सकें।
गॉल्फ़ ग्राउंड में घूमते हुए मुझे यह एहसास बार-बार हो रहा था कि शायद यही वो जगह होगी जहाँ स्कूल के बच्चों को चैपल में स्पेशल सर्विस के बाद पिकनिक पर लाया गया होगा और मिस्टर मुकर्जी, मिस वुड के पास घास पर लेट कर आराम फ़रमा रहे थे। गोल्फ़ ग्राउंड में चीड़ और देवदार के कुछ पेड़ बॉर्डर के जैसे ग्राउंड के चारों ओर खड़े थे, घास का रंग सर्दी की वजह से पीला पड़ गया था। पूरे ग्राउंड में आठ-दस लोग ही थे, जिनमें कुछ बच्चे भी शामिल थे जो ग्राउंड में पकड़म-पकड़ाई खेल रहे थे और बड़े लोग धूप में अधलेटे ऊँघ रहे थे।
कुछ वक्त धूप सेंकने के बाद गोल्फ़ ग्राउंड से पैदल ही हमने रानीखेत का रस्ता पकड़ा, पहाड़ों में यह एक समस्या है कि अगर आपके पास अपना वाहन नहीं है तो बस या टैक्सी के इंतज़ार में घंटों बीत सकते हैं तो ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प पैदल चलना ही होता है। वैसे भी अगर किसी शहर को अच्छे से जानना है तो उस शहर में पैदल घूमना चाहिए, आप शहर के सभी गली-कूचों से परिचित हो जाते हैं।
ऐसे ही पहाड़ी रास्तों पे चहलक़दमी करते हुए हम सोमनाथ ग्राउंड आ पहुँचे। यह ग्राउंड कुमाऊँ रेजीमेंट का ही हिस्सा है, जहाँ लतिका का प्रेमी गिरीश नेगी कार्यरत था। इस ग्राउंड का नाम मेजर सोमनाथ शर्मा के नाम पर रख गया था जिन्हें 1947 के भारत-पाक युद्ध के लिए परमवीर चक्र से नवाज़ा गया था। हो सकता है इसी ग्राउंड में बार-रूम में जाने से पहले गिरीश नेगी और मिस लतिका कभी-कभार शाम ढले टहलने आते हों, ग्राउंड में कुछ लड़के दौड़ लगा रहे थे जो शायद कुमाऊँ रेजीमेंट के ही जवान थे। एक बार को मन हुआ कि इन्हीं से पूछा जाए उस चर्च और हॉस्टल का रास्ता जिसके बराबर की सड़क पर कुमाऊँ रेजीमेंट के नौजवान सिपाही, चैपल के बग़ीचे से गुलाब तोड़ कर बालों में लगाए लड़कियों को देखकर अश्लील मज़ाक़ करते हैं तथा सिटी बजाते हैं। शायद यह भी उसी रास्ते से होकर गुज़रते हों।
सोमनाथ ग्राउंड घूमने के बाद हमने नज़दीक के एक ढाबे पर पेट-पूजा की और यह सोचने लगे कि उस चर्च का पता कैसे लगाएँ। मैंने पिछली रात ही परिंदे कहानी दोबारा पढ़ी थी ताकि उससे कुछ सुराग़ हाथ लग सकें और मैं इसमें कामयाब भी हुआ। सबसे पुख़्ता सुराग़ था कि यह स्कूल और चैपल रानीखेत से काठगोदाम जाने वाली सड़क पर पड़ता होगा। कहानी में जब लतिका, मुकर्जी और ह्यूबर्ट रात को महफ़िल जमाये बैठे होते हैं तो उसी समय निर्मल वर्मा ज़िक्र करते हैं कि “हवा के झौंके से मोमबत्तियों की लौ फड़कने लगीं। टैरेस के ऊपर काठगोदाम जानेवाली सड़क पर यू.पी. रोडवेज़ की आख़िरी बस डाक लेकर जा रही थी।” इस सुराग़ को पाकर हमने काठगोदाम वाली सड़क पकड़ ली, रास्ता बहुत ख़ूबसूरत था, एकदम साफ़ सड़कें और देवदार और बांज का जंगल, सड़क पर जगह-जगह रानीखेत छावनी की ओर से वहाँ पाए जाने वाले जानवरों से जुड़े तथ्य बोर्ड लगा कर बताए गए थे। इक्का-दुक्का गाड़ी ही कभी-कभार आती वरना रास्ता एकदम सुनसान था।
दिन का समय था इसलिए जंगली जानवरों का भी कोई डर नहीं था। लेकिन देवदार और चीड़ के ऊँचे दरख़्तों की शाख़ों पर कहीं-कहीं गरुड़ दिखाई दे रहे थे, जो थोड़ी-थोड़ी देर में अपने विशाल पंख फैलाए आसमान में घूम रहे थे। हम रानीखेत के मुख्य बाज़ार से काठगोदाम रोड पर कई किलोमीटर आगे आ चुके थे। मन में एक निराशा भी घर करने लगी थीं। इतना चलने के बाद भी हमें स्कूल या चैपल का कोई सुराग़ नहीं मिला था हमने अब फ़ैसला किया कि अब एक किलोमीटर में ही अगर वो जगह हमें मिल जाती है तो ठीक वरना हम सुंदर भाई को फोन करेंगे और सीधे झूला देवी मंदिर चले जाएँगे। सुबह से पैदल चलते-चलते दोपहर हो आई थी और थकान भी काफ़ी हो गई थी।
एक किलोमीटर चलने के बाद भी हमें कोई चैपल नहीं मिला तो हमने सुंदर भाई को फोन किया और फिर से हम तीनों एक स्कूटी पर सवार हो झूला देवी मंदिर की और जाने लगे। हम लोग कुछ दूर ही गए होंगे कि सड़क की बाईं ओर हमें एक बहुत प्राचीन और भव्य चर्च देखने को मिला, जिसके गेट पर बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा था St. Bonaventure Catholic Church, चर्च काफ़ी सुंदर था। चर्च जाने के लिए काठगोदाम वाली रोड से सीढ़ियाँ नीचे की ओर जाती थीं। मुझे समझने में एक पल नहीं लगा कि यह वही चर्च है जिसकी हमें सुबह से तलाश थी। निर्मल वर्मा ने अपनी कहानी में लिखा है कि “कंटोनमेंट जानेवाली पक्की सड़क पर चार-चार की पंक्ति में कुमाऊँ रेजीमेंट के सिपाहियों की एक टुकड़ी मार्च कर रही थी । फौजी बूटों की भारी खुरदुरी आवाज़ें स्कूल चैपल की दीवारों से टकराकर भीतर ‘प्रेयर-हाल’ में गूँज रही थी।” यह चर्च ठीक कंटोनमेंट जाने वाली सड़क के बगल में ही अवस्थित था।
चर्च में अंदर जाने के लिए जैसे ही हमने क़दम बढ़ाए हमारी नज़र चर्च के प्रांगण में घूमते विशालकाय कुत्ते पर पड़ी, कुत्ते ने भी हमें देख लिया था और वह गेट की ओर ही बढ़ा आ रहा था। ऐसे में अंदर जाना ख़तरे से ख़ाली नहीं था, कुत्ता खुला था और हम उसके लिए अजनबी थे। तभी हमारी नज़र अंदर घूमते कुछ लोगों पर पड़ी, वह शायद मजदूर थे जो चर्च की मरम्मत में लगे थे। हमने उन्हें आवाज़ दी, और कुत्ते को बाँधने के लिए कहा। उन्होंने हमें बताया कि यह कुत्ता काटता नहीं है बस आप घबराइयेगा मत। हम वैसे भी डॉग-लवर थे तो हम सीधे अंदर चले गए। अंदर जाते ही कुत्ता हमारे पास आया और उसने बारी-बारी से हम तीनों को सूँघा और जब उसे हम पर भरोसा हो गया तो वह एक तरफ़ जाकर बैठ गया।
चर्च 1899 ई. का बना था, यह सन क्रॉस के नीचे दर्ज था। चर्च रोमन शैली का एक शाहकार था और इस बात का सबूत कि कभी रानीखेत अंग्रेज़ों की पसंद रहा था तभी तो उन्होंने प्रार्थना के लिए सुदूर पहाड़ पर इतना भव्य चर्च बनाया। चर्च के चारों तरफ़ थोड़ी ख़ाली जगह थी, जहाँ कुछ फुलवारी लगी थी। जैसा ऊपर बताया कि चर्च में मरम्मत का कार्य चल रहा था जिसकी वजह से वह बंद था, किंतु हमारे अनुरोध पर उन्होंने अंदर जाने दिया। चर्च में ठीक सामने विशाल क्रॉस पर ईसा मसीह की प्रतिमा थी, प्रतिमा काफ़ी प्राचीन थी और अपने समय का एक एंटीक पीस। हॉल में दोनों तरफ़ पंक्तिबद्ध बेंच लगी थीं और दीवारों पर ईसा मसीह और मरियम की कई तस्वीरें और प्रतिमाएँ। चर्च के अंदर प्रवेश करते ही मैं उस सुबह में पहुँच गया जब “फ़ादर एल्मंड एक-एक शब्द चबाते हुए खँखारते स्वर में ‘सर्मन ऑफ़ द माउंट’ पढ़ रहे थे” और ईसा मसीह की मूर्ति के नीचे ‘कैंडलब्रियम’ पर जलती मोमबत्तियों की रोशनी आगे बैठी लड़कियों पर पड़ रही थी। पीछे अँधेरे में डूबे बेंचों पर लड़कियों खुसुर-पुसुर कर रही थी जो मैं उनके पीछे दरवाज़े के पास खड़ा सुन पा रहा था।
मैं भी अंदर जाकर एक बेंच पर बैठ गया और फ़ादर एलमंड का सर्मन सुनने लगा और देखा कि मेरे बराबर में ही डॉक्टर मुकर्जी ऊब और उकताहट से भरी जमहाइयाँ ले रहे हैं। एक बार को जी मैं आया उनसे हाथ मिला आऊँ लेकिन मिस वुड का तना चेहरा और भृकुटियाँ देखकर मैं शांत होकर प्रेयर सुनने लगा ‘जीसस सेड, आई एम द लाइट ऑफ़ द वर्ल्ड—ही दैट फ़ालोएथ मी शैल नॉट वाक इन डार्कनेस, बट शैल हैव द लाइट ऑफ़ द लाइट…।’ मोहित नेगी और सुंदर भाई के आवाज़ लगाने पर ये तिलिस्म टूटा और मैंने पाया कि मैं अकेला अभी तक चर्च में बैठा हूँ वो दोनों बाहर खड़े मेरा इंतज़ार कर रहे हैं।
चर्च तो मिल गया था लेकिन अब खोजना था वह स्कूल जिसमें मिस लतिका पढ़ाती थीं। इसमें फिर ‘परिंदे’ कहानी ने ही सहायता की, जिस रात लतिका, मुकर्जी और ह्यूबर्ट की महफ़िल जमी थी उसकी अगली सुबह जब लतिका खड़की से बाहर झाँक रही थी तो ‘स्कूल से ऊपर चैपल जाने वाली सड़क बादलों में छिप गई थी, केवल चैपल का ‘क्रास’ धुँध के पर्दे पर एक-दूसरे को काटती हुई पेंसिल की रेखाओं-सा दिखाई दे जाता था।’ यह बहुत महत्वपूर्ण सुराग़ था जो हमें स्कूल पहुँचा सकता था। इससे यह तो निश्चित था कि स्कूल चर्च से नीचे की ओर ही होगा क्योंकि चैपल के लिए सड़क स्कूल से ऊपर की ओर जाती थी और मिस लतिका की खिड़की से चर्च का क्रॉस भी दिखता था।
हम लोगों को चर्च के पास में ही एक छोटी सी पगडंडी-नुमा सड़क मिली जो नीचे जाती थी, हम लोग उस सड़क पर मुश्किल से 50-100 मीटर ही चले होंगे और हमें सामने ही स्कूल मिल गया। स्कूल का नाम था कैनोसा कान्वेंट स्कूल,स्कूल देखने में सुंदर था, विशाल प्रांगण के दाएँ हाथ पर स्कूल की इमारत थी, जो पुरानी थी लेकिन देखकर लग रहा था कि हाल ही में मरम्मत और रंग-रोगन हुआ है। गेट खुला था तो हम सीधे ही अंदर चले गए। क़दम रखते ही कुत्ते की ज़ोर-ज़ोर से भौंकने की आवाज़ आई, देखा तो दूर देवदार के पेड़ से एक कुत्ता बँधा है। मुझे लगा जैसे कुत्ते की भौं-भौं सुनकर अभी अंदर से करीमुद्दीन निकल कर आएगा और कुत्ते को शांत करते हुए हमसे पूछेगा कि आपको किस से मिलना है और मैं तपाक से बोल पड़ूँगा- मिस लतिका से।
कुत्ता ज़ोर-ज़ोर से भौंकता रहा लेकिन कोई भी अंदर से नहीं आया। ग़ज़ब का इत्तेफ़ाक़ था कि हम दिसम्बर के आख़िरी दिनों में यहाँ आए हैं, जिन दिनों का ज़िक्र निर्मल वर्मा ने कहानी में किया है। अभी दो रोज़ पहले ही तो क्रिसमस गया है, अगर हम कुछ दिन पहले यहाँ आते तो शायद उन सभी घटनाओं को आँखों से देख पाते, जिनको पक्का निर्मल वर्मा ने देखा होगा तभी तो एक-एक चीज़ का सटीक वर्णन किया है।
स्कूल की छुट्टी पड़ चुकी हैं और स्कूल में कोई नहीं है, मिस लतिका भी नहीं। स्कूल में घूमकर जब हम जाने लगे तो हमें एक महिला दिखीं जो कुछ घरेलू कार्य कर रही थीं। एक पल को लगा शायद यही मिस लतिका रही हों, लेकिन उनकी उम्र कहानी के हिसाब से काफ़ी कम थी (यह कहानी 1959 में प्रकाशित हुई थी), पर हो सकता था कि मिस लतिका इनकी माँ या दादी रही हों, हम तो बस क़यास ही लगा सकते थे। उन्होंने न हमसे कुछ कहा, न ही हमने उनसे कुछ पूछा। एक दूसरे को देखकर अपने-अपने रास्ते हो लिए।
स्कूल से बाहर निकलते ही हमें एक बुज़ुर्ग मिले जो शायद शाम की सैर को निकले थे। एक बार को उनसे पूछने का मन हुआ लेकिन फिर यह सोचकर कुछ न पूछ सका कि ज़रूरी तो नहीं इन्होंने ‘परिंदे’ कहानी पढ़ी ही हो, वो भाँप गए कि मैं उनसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ तो वह ख़ुद ही बोल पड़े।
आप लोग रानी झील घूमने आए हैं क्या?
हमने कहा – हाँ! रानी झील ही घूमने आए हैं!
तो वह कहने लगे कि आप यही पगडंडी पकड़ लीजिए जिससे मैं आ रहा हूँ यह रानी झील जाने का शॉर्टकट रास्ता है। हमने सोचा जब झील पास ही है तो वहाँ भी घूम आते हैं। वैसे भी परिंदे कहानी के इन स्थानों को देख कर हम बहुत ख़ुश थे। और उसी संबंध में बातें करते-करते स्कूल से नीचे को जाती पगडंडी पर बढ़ने लगे। पगडंडी पूरी तरह बांज के घने जंगल से घिरी थी। सूखे पत्तों से ढकी पगडंडी पर चलने से चरर-चरर की आवाज़ शाम के सन्नाटे को तोड़ रही थी। कुछ दूर चलने पर ही जंगल के दरमियान हमें एक चर्च के खंडहर दिखाई दिए। चर्च St. Bonaventure Catholic Church से भी प्राचीन लग रहा था लेकिन अब उसकी हालत बहुत ख़स्ता थी, कुछ दीवारें गिरी हुई थीं और छत और दीवारों पर पेड़-पौधे उगे थे। देखने में ही भूतिया इमारत लग रही थी। शाम का धुंदलका छाने लगा था तो हम उस जगह से जल्दी-जल्दी आगे बढ़ने लगे।
तकरीबन एक से डेढ़ किलोमीटर चलने पर हमें रानीझील दिखाई देने लगी। झील छोटी थी और चारों ओर बांज तथा देवदार के जंगल से घिरी थी। झील के किनारे कुछ पर्यटक पहले से ही मौजूद थे। छावनी परिषद ने यहाँ संगीत का इंतज़ाम भी किया था, मद्धम स्वर में नाइंटीज़ के गाने बज रहे थे, जिन पर कुछ जोड़े थिरक रहे थे। एक तरफ़ लगे ‘आई लव रानीखेत’ के साथ फोटो लेने के लिए कुछ लोग अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे और झील में 1-2 नौकाएँ चल रही थीं। मंज़र बहुत ख़ुबसूरत था। हम लोगों ने फ़ैसला किया कि बोटिंग की जाए। तीनों ने लगभग आधे घंटे तक बोटिंग की, हमने मछलियों को खिलाने के लिए पास ही बिक रहे मुरमुरे भी लिए थे, लेकिन झील में मुरमुरे डालने के बाद भी मछलियाँ नहीं दिख रही थीं, हो सकता था वह हमसे शरमा रही हों। ऐसे में हमने ही बोटिंग करते उन मुरमुरों का भोग लगाया।
शाम होने में अभी कुछ समय बाक़ी था और हमने झूला देवी के दर्शन नहीं किये थे, रानीखेत आकर अगर झूला देवी न जाएँ तो मन में एक कसक रहती, इसलिए हमने फ़ैसला किया कि 5 मिनट के लिए ही सही पर दर्शन कर आते हैं। झूला देवी मंदिर काठगोदाम वाली सड़क पर ही चर्च से कुछ किलोमीटर आगे था। हमको वहाँ स्कूटी से पहुँचने में दस मिनट ही लगे।मंदिर के बाहर हज़ारों घंटियाँ बँधी थीं, जो क्षेत्र में झूला देवी की मान्यता का प्रमाण थीं। कुमाऊँ में यह मान्यता है कि देवी-देवताओं द्वारा मनोकामनाएँ पूर्ण होने पर मंदिर में घंटियाँ चढ़ाई जाती हैं। मंदिर के गर्भगृह में माँ दुर्गा झूले पर विराजमान है जिसकी वजह से उन्हें झूला देवी के नाम से जाना जाता है। किवंदती है कि इस क्षेत्र में तेन्दुओं और गुलदारों का बहुत आतंक था वह अक्सर लोगों के जानवरों को मार देते थे। लोगों द्वारा जब देवी की अर्चना की गई तो एक रात देवी ने चरवाहे के सपने में आकर इस स्थान पर मंदिर स्थापित करने को कहा और तब से देवी तेदुओं- गुलदारों से लोगों तथा उनके जानवरों की रक्षा करने लगीं।
शाम धीरे-धीरे रात की ओर बढ़ने लगी थी और हम रानीखेत लगभग पूरा घूम चुके थे, हमने फ़ैसला किया कि पीडब्यूडी रानीखेत के अतिथि गृह में रुकने की बजाय अल्मोड़ा ही चलते है। रानीखेत में शाम का मंज़र बड़ा दिलफ़रेब था बांज और बुराँश के जंगल में दूर क्षितिज पर ढलते सूरज की लालिमा छन-छन कर आ रही थी। नंदा देवी और पंचाचूली की चोटियाँ श्वेत से स्वर्णिम हो गई थीं। हवा हौले-हौले ऊँघने लगी थी। सूर्यास्त होते ही जंगल स्याह हो गया था और हम तीन, मन में बाघ का डर लिए घने-वीरान जंगल से होते हुए रोशनी के शहर अल्मोड़ा की ओर बढ़े जा रहे थे। आज इस बात की ख़ुशी थी कि मैं उस एक-एक स्थान को देख पाया जहाँ शायद कहानी लिखने से पहले निर्मल आये होंगे। आज अगर निर्मल वर्मा हमारे बीच होते तो मैं उन्हें मिलकर ज़रूर यह बताता कि मैं आपकी ‘परिंदे’ कहानी को पढ़कर ही नहीं जीकर भी आया हूँ।